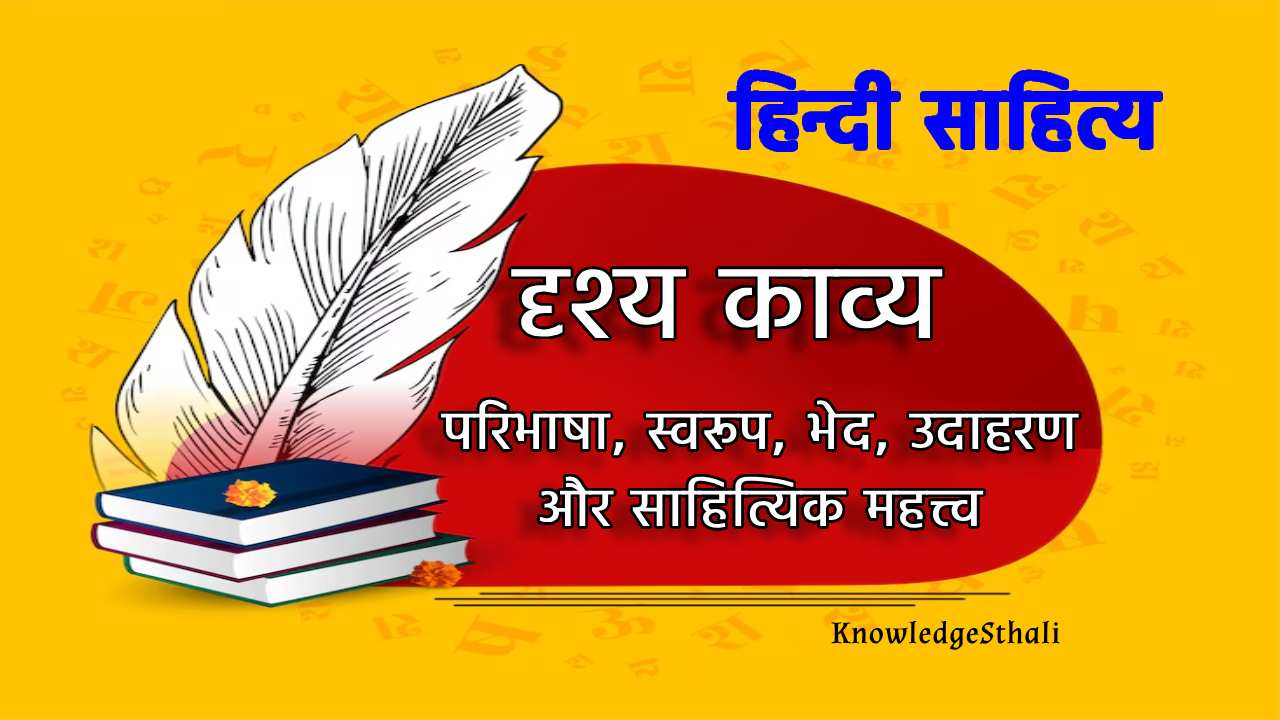भारतीय साहित्य की परंपरा अत्यंत समृद्ध और बहुआयामी है। यहां केवल वाचिक साहित्य (जो पढ़ा और सुना जाता है) ही नहीं, बल्कि ऐसा साहित्य भी विकसित हुआ है जिसे आँखों से देखा और अनुभव किया जा सकता है। इस दृश्य अनुभव से उत्पन्न काव्य को दृश्य काव्य (Drishya Kavya) कहा जाता है। यह केवल पठन-पाठन तक सीमित न होकर मंचन, अभिनय, नृत्य, संगीत और संवादों के माध्यम से सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
दृश्य काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें रस और भाव की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से होती है। पाठक नहीं, बल्कि दर्शक इसका केंद्र होता है। इस प्रकार दृश्य काव्य की अवस्थिति मंच और मंचीय कला से जुड़ी है।
भरतमुनि का नाट्यशास्त्र दृश्य काव्य की आधारशिला माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि नाट्य कला लोक-शिक्षा, मनोरंजन और धर्म-प्रचार का साधन है। दृश्य काव्य की परंपरा वैदिक संवादात्मक सूक्तों से लेकर आधुनिक रंगमंच और फ़िल्मों तक फैली हुई है।
दृश्य काव्य का विकास और इतिहास
भारतीय संस्कृति में दृश्य काव्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है।
- वैदिक काल में ही संवादात्मक सूक्तों के माध्यम से मंचन की नींव पड़ चुकी थी।
- रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में नाटकीयता और संवादों का जो स्वरूप मिलता है, उसने बाद के नाटककारों को प्रेरित किया।
- भरतमुनि का नाट्यशास्त्र दृश्य काव्य की आधारशिला है। इसमें नाटक के प्रकार, रस, भाव, अभिनय, नृत्य और संगीत सभी की विस्तृत चर्चा है।
- संस्कृत नाटकों में कालिदास, भास, भवभूति, शूद्रक आदि कवियों ने रूपक परंपरा को समृद्ध किया।
दृश्य काव्य की परिभाषा और स्वरूप
आचार्यों के अनुसार, जिस साहित्य को आँखों के सामने घटित होते हुए देखा जाए और जिसमें पात्रों, संवादों तथा घटनाओं के माध्यम से रस-भावों का आस्वाद हो, वही दृश्य काव्य कहलाता है।
- यहाँ शब्द मात्र नहीं, बल्कि अभिनय (Acting), अंगिकाभिनय (Gestures), सात्विक भाव (Emotions) और मंचीय गतिशीलता का भी महत्त्व होता है।
- दृश्य काव्य को समझने के लिए इसे केवल साहित्यिक दृष्टि से नहीं, बल्कि नाट्यशास्त्रीय दृष्टि से भी देखना आवश्यक है।
- आचार्यों के अनुसार “जिस साहित्य को आँखों से देखकर, प्रत्यक्ष दृश्यों के माध्यम से रस-भाव की अनुभूति की जाए, वही दृश्य काव्य है।”
- इसकी मूल विशेषता मंचीयता (Theatricality) है।
- इसमें अभिनय, हाव-भाव, वाणी, नृत्य और संगीत सभी का सम्मिलन होता है।
दृश्य काव्य के भेद
भारतीय काव्यशास्त्र में दृश्य काव्य का विशेष स्थान है। दृश्य काव्य वह है जिसे पढ़ने मात्र से नहीं, बल्कि मंच पर अभिनय और प्रस्तुति के माध्यम से भी अनुभव किया जाता है। आचार्यों ने दृश्य काव्य को मूलतः दो प्रमुख वर्गों में बाँटा है—
- रूपक
- उपरूपक
1. रूपक काव्य
(क) परिभाषा
संस्कृत आचार्यों ने रूपक को नाट्य का प्रमुख स्वरूप माना है।
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में रूपक की संक्षिप्त परिभाषा दी गई है—
“तदुपारोपात्तु रूपम्।”
👉 अर्थात् जब पात्र, कथानक और रस के तारतम्य से नाट्य का सजीव रूप उत्पन्न होता है, तब वह रूपक कहलाता है।
धनंजय ने दशरूपक में रूपक को इस प्रकार परिभाषित किया है—
“वस्तु-नायक-रसैः संहतं रूपकं भवति।”
👉 अर्थात् जब कथावस्तु, नायक और रस परस्पर संयुक्त होकर नाट्य की रचना करते हैं, वही रूपक है।
निष्कर्षात्मक परिभाषा:
रूपक वह नाट्यविधा है जिसमें विस्तृत कथा, विकसित पात्र और रसों का समुचित संयोग होकर दर्शकों के सामने जीवन का सजीव और सम्पूर्ण रूप प्रस्तुत होता है।
👉 इसमें ऐतिहासिक या पुराणकथाओं के साथ कवि की कल्पना का समन्वय पाया जाता है और नाट्य की गरिमा, गंभीरता एवं भावनात्मक सम्पूर्णता प्रकट होती है।
(ख) स्वरूप
- विस्तृत और व्यापक कथा-वस्तु।
- पात्रों की गहनता और चरित्र-निर्माण।
- रस एवं भावों का समन्वय।
- मंचन में पूर्णता और वैभव।
(ग) नाटक और रूपक का संबंध
- नाटक को रूपक का ही प्रमुख रूप माना गया है।
- भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में “रूपक” के स्थान पर “नाटक” शब्द का प्रयोग मिलता है।
- इसलिए रूपक का सबसे बड़ा भेद नाटक है।
रूपक के भेद
(i) परंपरागत दस भेद (दशरूपक)
भारतीय आचार्यों और धनंजयकृत दशरूपक में रूपक के दस भेद बताए गए हैं, जो वस्तु (कथानक), नायक और रस के आधार पर विभाजित हैं—
- नाटक – प्रसिद्ध कथा पर आधारित, पाँच से दस अंकों वाला, श्रृंगार, वीर और करुण रस प्रधान।
- प्रकरण – कवि-कल्पित कथा, धीर-प्रशांत नायक (क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य)।
- भाण – एकांकी, धूर्त या कपटी पात्र पर आधारित, हास्य-प्रधान।
- व्यायोग – एक अंक का, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के युद्ध का वर्णन, स्त्रियों की अल्प उपस्थिति।
- समवकार – तीन अंकों का, देव और दैत्य संबंधी कथा, वीर रस प्रधान।
- डिम – चार अंकों का, मानवेतर पात्र, रौद्र रस प्रधान।
- ईहामृग – चार अंकों का, प्रख्यात और कल्पित घटनाओं का मिश्रण, दिव्य स्त्री का अपहरण।
- अंक – एकांकी, करुण रस प्रधान, सामान्य नायक।
- वीथी – एकांकी, श्रृंगार रस प्रधान, आकाशभाषित संवाद।
- प्रहसन – हास्य रस प्रधान, ढोंगियों पर व्यंग्य।
(ii) अग्नि पुराण के अनुसार
अग्नि पुराण में दृश्य काव्य को विशेष रूप से विस्तृत किया गया है। इसमें रूपक और उपरूपक का पृथक उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि कुल 27 नाटकों का वर्णन किया गया है। इन 27 नाट्यरूपों में—
- 10 रूपक (दशरूपक के समान)
- 17 उपरूपक
माने गए हैं।
अग्नि पुराण के अनुसार रूपक के भेद हैं—
- नाटक (Nāṭaka)
- प्रकरण (Prakaraṇa)
- भाण (Bhāṇa)
- व्यायोग (Vyāyoga)
- समवकार (Samavakāra)
- डिम (Ḍima)
- ईहामृग (Īhāmṛga)
- अंक (Aṅka)
- वीथी (Vīthi)
- प्रहसन (Prahasana)
- त्रोटक (Troṭaka)
- नाटिका (Nāṭikā)
- सट्टक (Saṭṭaka)
- शिल्पक (Śilpaka)
- कर्ण (Karṇa) (विशिष्ट रूप से उल्लिखित)
- दुर्मल्लिका (Durmallikā)
- प्रस्थान (Prasthāna)
- भाणिका (Bhāṇikā)
- भाणी (Bhāṇī)
- गोष्ठी (Goṣṭhī)
- हल्लीशका (Hallīśaka)
- काव्य (Kāvya)
- श्रीगदित (Śrīgadita)
- नाट्यरासक (Nāṭyarāsaka)
- रासक (Rāsaka)
- उल्लाप्यक / उल्लाव्यक (Ullāpyaka / Ullāvyaka) (वर्णन में ‘Ullāpyaka’ संभवतः ‘Ullāvyaka’ का ही रूप है)
- प्रेक्षण (Preṅkhana)
यह विविधता भारतीय नाट्य परंपरा की समृद्धि और वैविध्य को दर्शाती है।
अतिरिक्त स्पष्टीकरण:
- “कर्ण (Karṇa)” का उल्लेख एक अनूठा नाम के रूप में मिला है, जो अन्य आचार्यों जैसे दशरूपक (भरतमुनि) में नहीं मिलता।
- कुछ रूपों जैसे उल्लाव्यक या उल्लाप्यक का लिप्यंतरण भिन्न हो सकता है (उल्लाप्यक — Ullāpyaka; उल्लाव्यक — Ullāvyaka)। स्रोत में अंग्रेज़ी में ‘Ullāpyaka’ लिखा गया है।
- कुल मिलाकर यह सूची 27 भेदों का समूह प्रदान करती है, जैसा कि अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
2. उपरूपक काव्य
(क) परिभाषा
रूपक की तुलना में जो नाट्यरूप आकार में छोटा, सरल और संगीत-प्रधान होता है, उसे उपरूपक कहा गया है।
विश्वनाथ कविराज ने साहित्यदर्पण में इसकी परिभाषा दी है—
“रूपकस्य लघुत्वेन यत् रूपं तदुपरूपकम्।”
👉 अर्थात् जो नाट्य रूप रूपक से लघु होता है, वही उपरूपक कहलाता है।
शारदतनय ने भावप्रकाशन में उपरूपकों को संगीतक कहा है और उनकी विशेषता यह बताई है कि—
“तेषां प्रायः सर्वेषां गीत-नृत्य-प्रधानता।”
👉 अर्थात् उपरूपक प्रायः सभी संगीत और नृत्य-प्रधान होते हैं।
निष्कर्षात्मक परिभाषा:
उपरूपक वह नाट्यरूप है जो आकार में रूपक से लघु, प्रस्तुति में संक्षिप्त तथा स्वर, गीत और नृत्य पर अधिक आश्रित होता है।
👉 इसमें कथानक सीमित होता है, पात्रों की संख्या कम होती है और अभिनय के स्थान पर संगीत तथा भावाभिनय को विशेष महत्व दिया जाता है।
रूपक की तुलना में उपरूपक छोटे और सरल होते हैं।
- इनका कथानक संक्षिप्त होता है।
- मंचन छोटा होता है।
- रस और भाव का संचार रूपक के समान होता है, परंतु वैभव और विस्तार की कमी रहती है।
(ख) स्वरूप
- लघु एवं सरल।
- गेय, नृत्य और संगीत प्रधान।
- कथानक सीमित, परंतु प्रभावशाली।
उपरूपक के भेद
उपरूपक के 18 भेद बताए गए हैं—
नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सदृक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लास्य, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीशा और भणिका।
प्रमुख आचार्यों के अनुसार
- विश्वनाथ कविराज ने उपरूपक के 18 भेद माने हैं, जिन्हें संगीतक भी कहा गया।
- राजा भोज ने 12 भेद बताए।
- शारदतनय ने 21 भेदों की स्वीकृति दी।
विशेष टिप्पणी :
- रूपक – विस्तृत और गंभीर नाट्यरूप (जैसे नाटक, प्रकरण, व्यायोग)।
- उपरूपक – लघु और संगीत-नृत्य प्रधान नाट्यरूप (जैसे नाटिका, रासक, गोष्ठी)।
- अग्नि पुराण में कुल 27 प्रकार के नाट्यरूप माने गए हैं, जिनमें ये 10 रूपक और 17 उपरूपक सम्मिलित हैं।
दृश्य काव्य (रूपक, उपरूपक) और अग्नि पुराण
अग्नि पुराण का जब हम ध्यान से अध्ययन करते हैं तो उसमें “रूपक” और “उपरूपक” का पृथक विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। उपरूपक” की संकल्पना की जड़ें अग्नि पुराण में हैं, परंतु उसका स्पष्ट रूप बाद की परंपरा में उभरा।
अग्नि पुराण की स्थिति
- अग्नि पुराण (अध्याय 338 और आसपास) में कुल 27 नाट्यरूपों का उल्लेख मिलता है।
- इसमें दस भेद वही बताए गए हैं जिन्हें परंपरा में “दशरूपक” कहा जाता है — (नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथी, प्रहसन)।
- इन दस के अलावा 17 और नाट्यरूप गिनाए गए हैं, जैसे – नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, परकरणिका, हल्लीशा आदि।
व्याख्या
- अग्नि पुराण में इन सबको सामूहिक रूप से नाट्यरूप (रूपक) ही कहा गया है।
- बाद के आचार्यों (जैसे विश्वनाथ कविराज, शारदतनय, राजा भोज आदि) ने इन अतिरिक्त 17 भेदों को उपरूपक नाम से व्यवस्थित किया।
- इसलिए यह स्पष्ट है कि “उपरूपक” शब्द का प्रयोग अग्नि पुराण में नहीं हुआ है, परंतु जो 17 भेद उसमें वर्णित हैं, उन्हें बाद की परंपरा में उपरूपक कहा गया।
👉 संक्षेप में:
- अग्नि पुराण = 27 नाट्यरूप (10 रूपक + 17 अन्य)
- उपरूपक का नाम = बाद की परंपरा में दिया गया, अग्नि पुराण में नहीं
इस प्रकार, भारतीय नाट्य और काव्य परंपरा में दृश्य काव्य को दो भागों—रूपक और उपरूपक—में विभाजित किया गया है।
- रूपक व्यापक और गंभीर नाट्य रूप है, जिसका प्रतिनिधि रूप नाटक है।
- उपरूपक छोटे, संगीत और नृत्य प्रधान नाट्य रूप हैं, जिनमें मनोरंजन और सौंदर्य का विशेष महत्व है।
इन विविध भेदों से भारतीय साहित्य में नाट्य परंपरा की गहराई, विस्तार और सांस्कृतिक समृद्धि का पता चलता है।
रूपक और उपरूपक : तुलनात्मक प्रस्तुति
| पहलू | रूपक | उपरूपक |
|---|---|---|
| परिभाषा (आचार्यों के अनुसार) | “तदुपारोपात्तु रूपम्।” (नाट्यशास्त्र, भरतमुनि) अर्थ: जब पात्र, कथा और रस के तारतम्य से सजीव रूप उत्पन्न होता है, तब वह रूपक कहलाता है। | “रूपकस्य लघुत्वेन यत् रूपं तदुपरूपकम्।” (विश्वनाथकृत साहित्यदर्पण) अर्थ: जो नाट्यरूप आकार में रूपक से छोटा होता है, वही उपरूपक कहलाता है। |
| स्वरूप | – विस्तृत और गंभीर नाट्यरूप। – कथा इतिहास-पुराण या कवि-कल्पित। – पात्रों का पूर्ण विकास। | – रूपक से लघु और संक्षिप्त। – कथा साधारण और सीमित। – पात्र कम, चरित्र-चित्रण अल्प। |
| रसाभिव्यक्ति | सभी रसों का सम्यक् संयोजन, रस-निष्पत्ति में परिपूर्णता। | रस और भाव का संचार तो होता है, किंतु उसकी तीव्रता और व्यापकता रूपक जैसी नहीं होती। |
| मंचन | पाँच से दस अंकों तक, व्यापक मंचन। | प्रायः एक अंक अथवा लघु रूप, संगीत और नृत्य प्रधान। |
| प्रमुख उदाहरण | नाटक, प्रकरण, व्यायोग, प्रहसन आदि। | नाटिका, त्रोटक, रासक, गोष्ठी, सट्टक आदि। |
संस्कृत आचार्यों के मत
1. भरतमुनि (नाट्यशास्त्र)
“तदुपारोपात्तु रूपम्।”
👉 अर्थ: जब कथा, पात्र और रस का सामंजस्य होकर नाट्य का सजीव रूप प्रकट हो, वही रूपक कहलाता है।
2. धनंजय (दशरूपक)
“वस्तु-नायक-रसैः संहतं रूपकं भवति।”
👉 अर्थ: जब कथावस्तु, नायक और रस परस्पर संयुक्त होकर नाट्य की रचना करते हैं, वही रूपक है।
3. विश्वनाथ कविराज (साहित्यदर्पण, 6.317)
“रूपकस्य लघुत्वेन यत् रूपं तदुपरूपकम्।”
👉 अर्थ: जो नाट्यरूप रूपक की अपेक्षा लघु होता है, वही उपरूपक है।
4. शारदतनय (भावप्रकाशन)
शारदतनय ने उपरूपकों की संख्या 21 बताई और उन्हें संगीतक नाम से संबोधित किया।
“उपरूपकाणि चतुर्विंशतिरुक्तानि, तेषां प्रायः सर्वेषां गीतनृत्यप्रधानता।”
👉 अर्थ: उपरूपक अनेक प्रकार के होते हैं, और अधिकांश में गीत तथा नृत्य का प्रधानत्व होता है।
निष्कर्ष
- रूपक : नाट्य का मुख्य और व्यापक रूप, जिसमें कथा, पात्र और रस का संपूर्ण सामंजस्य होता है।
- उपरूपक : रूपक का लघु रूप, जिसमें मंचन संक्षिप्त और संगीत-प्रधान होता है।
- अग्नि पुराण में दोनों का पृथक विभाजन नहीं है, किंतु परवर्ती आचार्यों ने अतिरिक्त 17 भेदों को उपरूपक की संज्ञा दी।
दृश्य काव्य की विशेषताएँ
- मंचीयता – दृश्य काव्य का अस्तित्व तभी है जब वह मंच पर प्रस्तुत हो।
- दर्शक-केंद्रितता – इसका उद्देश्य पाठक नहीं बल्कि दर्शक की संवेदना को छूना है।
- रस-भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति – दृश्य काव्य में रस केवल कल्पना से नहीं, बल्कि जीवंत अभिनय से अनुभव होता है।
- अभिनय और संगीत का संगम – दृश्य काव्य में भाषा के साथ-साथ आवाज़, हाव-भाव और लय भी उतने ही महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- कथानक और संवाद – कथा केवल बताई नहीं जाती, बल्कि पात्रों द्वारा जीकर दिखाई जाती है।
दृश्य काव्य और भारतीय समाज
भारतीय समाज में दृश्य काव्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा। यह—
- शिक्षा का माध्यम बना।
- धर्म और नीति के प्रसार का साधन रहा।
- लोक-जीवन की समस्याओं को उजागर करता रहा।
- सामाजिक एकता और संस्कृति संरक्षण में सहायक बना।
उदाहरण के लिए—
- नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि नाटक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी का समावेश होना चाहिए।
- कालिदास के नाटक केवल साहित्यिक नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के प्रतिबिंब भी हैं।
दृश्य काव्य का आधुनिक परिप्रेक्ष्य
आज के समय में दृश्य काव्य का स्वरूप बदल चुका है।
- पारंपरिक संस्कृत नाटक अब सीमित मंचन में दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आत्मा आधुनिक रंगमंच और थिएटर में जीवित है।
- हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के नाटककारों ने दृश्य काव्य की परंपरा को नया रूप दिया है।
- आज फ़िल्म और टेलीविजन को भी व्यापक अर्थों में दृश्य काव्य का आधुनिक स्वरूप माना जा सकता है, क्योंकि यह भी प्रत्यक्ष दृश्य और अभिनय के माध्यम से ही रसास्वादन कराता है।
दृश्य काव्य (रूपक और उपरूपक) के प्रमुख उदाहरण
1. संस्कृत नाटक (रूपक के उदाहरण)
- कालिदास
- अभिज्ञानशाकुंतलम् – नायक दुष्यंत और शकुंतला की प्रेमकथा। इसमें शृंगार और करुण रस का अद्भुत मिश्रण है।
- मालविकाग्निमित्रम् – प्राचीन प्रेमकथा का नाट्य रूप।
- विक्रमोर्वशीयम् – राजा पुरूरव और अप्सरा उर्वशी की कथा।
- भवभूति
- उत्तररामचरितम् – राम और सीता की करुण कथा, करुण रस का उत्कर्ष।
- मालती-माधव – प्रेम और नीति का संगम।
- भास
- स्वप्नवासवदत्तम् – राजनीतिक और प्रेम संबंधी द्वंद्व।
- प्रतिज्ञायौगंधरायणम् – राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला नाटक।
- शूद्रक
- मृच्छकटिकम् – चारुदत्त और वसंतसेना की कथा, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण।
2. प्रकरण, प्रहसन और व्यायोग के उदाहरण
- प्रकरण – भास का प्रतिज्ञायौगंधरायणम्।
- प्रहसन – हास्यप्रधान छोटे नाटक, जैसे भट्टनायक का भागवताजुकम्।
- व्यायोग – युद्धप्रधान नाटक, जैसे उरुभंगम् (भास द्वारा रचित)।
3. उपरूपक के उदाहरण
उपरूपक आकार में छोटे होते हैं, इनमें नृत्य, संगीत और संक्षिप्त कथानक का अधिक महत्व होता है।
- नाटिका – कालिदास की मालविकाग्निमित्रम्।
- रासक – गुजरात और राजस्थान में रासलीलाओं का मंचन।
- प्रेक्षणा – लोक-नाट्य शैलियों में छोटे नाटक जैसे भवाई (गुजरात), नौटंकी (उत्तर भारत)।
4. लोकनाट्य और भारतीय भाषाओं के उदाहरण
- हिंदी – भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी चौपट राजा (प्रहसन का उत्कृष्ट उदाहरण)।
- मराठी – तमाशा।
- बंगाली – जात्रा।
- तमिल – तेरुक्कूट्टू।
- असम – अंकिया नाट (शंकरदेव द्वारा)।
5. आधुनिक काल के उदाहरण
- मोहन राकेश – आधे-अधूरे (आधुनिक पारिवारिक यथार्थ का चित्रण)।
- धर्मवीर भारती – अंधा युग (महाभारत के युद्धोत्तर संदर्भ में गहन नाटकीय प्रस्तुति)।
- विजय तेंदुलकर – घाशीराम कोतवाल (मराठी में, राजनीतिक व्यंग्य का उदाहरण)।
दृश्य काव्य के उदाहरण : तालिका रूप में
| श्रेणी | उदाहरण | रचनाकार / क्षेत्र | विशेषता / टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| संस्कृत नाटक (रूपक) | अभिज्ञानशाकुंतलम् | कालिदास | शृंगार व करुण रस का अद्भुत संयोजन |
| मालविकाग्निमित्रम् | कालिदास | नाटिका रूप का उत्कृष्ट उदाहरण | |
| विक्रमोर्वशीयम् | कालिदास | प्रेम कथा व पौराणिक संदर्भ | |
| उत्तररामचरितम् | भवभूति | करुण रस की चरम अभिव्यक्ति | |
| मालती-माधव | भवभूति | प्रेम और नीति का संतुलन | |
| स्वप्नवासवदत्तम् | भास | राजनीतिक और प्रेम का मिश्रण | |
| प्रतिज्ञायौगंधरायणम् | भास | प्रकरण नाटक, राजनीति पर आधारित | |
| उरुभंगम् | भास | व्यायोग (वीर रस प्रधान) | |
| मृच्छकटिकम् | शूद्रक | सामाजिक जीवन और यथार्थ चित्रण | |
| अन्य संस्कृत रूपक | भागवताजुकम् | भट्टनायक | प्रहसन (हास्यप्रधान) |
| उपरूपक | मालविकाग्निमित्रम् (नाटिका रूप) | कालिदास | उपरूपक का उदाहरण |
| रासक | गुजरात/राजस्थान | रासलीला, नृत्यप्रधान | |
| प्रेक्षणा | लोक-नाट्य शैली | लघु नाट्य रूप, मनोरंजन | |
| लोकनाट्य | भवाई | गुजरात | सामाजिक व्यंग्य |
| नौटंकी | उत्तर भारत | लोकप्रिय लोक-नाट्य | |
| जात्रा | बंगाल | धार्मिक व सामाजिक विषय | |
| तमाशा | महाराष्ट्र | नृत्य-संगीत प्रधान | |
| अंकिया नाट | असम (शंकरदेव) | धार्मिक व भक्तिपरक | |
| तेरुक्कूट्टू | तमिलनाडु | लोकनाट्य शैली | |
| आधुनिक हिंदी नाटक | अंधेर नगरी चौपट राजा | भारतेंदु हरिश्चंद्र | प्रहसन, सामाजिक व्यंग्य |
| आधे-अधूरे | मोहन राकेश | आधुनिक पारिवारिक यथार्थ | |
| अंधा युग | धर्मवीर भारती | महाभारत-युद्ध के बाद का वैचारिक नाटक | |
| अन्य भारतीय भाषाएँ | घाशीराम कोतवाल | विजय तेंदुलकर (मराठी) | राजनीतिक व्यंग्य |
| तुगलक | गिरीश कर्नाड (कन्नड़) | ऐतिहासिक व राजनीतिक नाटक |
सारांश
- संस्कृत नाट्य परंपरा – कालिदास, भास, भवभूति और शूद्रक के नाटक।
- लोक-नाट्य परंपरा – रासलीला, नौटंकी, जात्रा, तमाशा आदि।
- आधुनिक हिंदी रंगमंच – भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती।
- भारतीय भाषाओं का रंगमंच – विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड आदि।
यानी, दृश्य काव्य केवल संस्कृत साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय नाट्यकला और आधुनिक रंगमंच दोनों में समान रूप से विद्यमान है।
निष्कर्ष
दृश्य काव्य भारतीय साहित्य की एक जीवंत धारा है जो केवल पढ़ने या सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे देखने और अनुभव करने से उसकी पूर्णता होती है। यह साहित्य और कला का ऐसा संगम है जिसमें रस, भाव, अभिनय और संगीत सभी मिलकर दर्शक को आत्मानुभूति की चरम सीमा तक ले जाते हैं।
- रूपक और उपरूपक इसके दो प्रमुख भेद हैं।
- रूपक में नाटक का विशेष स्थान है, जबकि उपरूपक छोटे और सरल रूप में साहित्य और नाट्य का संगम प्रस्तुत करते हैं।
- अग्नि पुराण में इनके अनेक भेदों का उल्लेख मिलता है, जो इस परंपरा की समृद्धि को दर्शाता है।
आज भले ही दृश्य काव्य के रूप बदल गए हों, पर उसकी मूल आत्मा—रस और भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति—आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यही कारण है कि दृश्य काव्य भारतीय संस्कृति की आत्मा और समाज की सामूहिक चेतना का दर्पण माना जाता है।
संदर्भ (References)
- भरतमुनि — नाट्यशास्त्र
- अग्नि पुराण — दृश्य काव्य और उपरूपक के भेद
- कालिदास — अभिज्ञानशाकुंतलम्, मालविकाग्निमित्रम्
- भवभूति — उत्तररामचरितम्
- शूद्रक — मृच्छकटिकम्
- हजारी प्रसाद द्विवेदी — हिंदी साहित्य का इतिहास
- विश्वनाथ त्रिपाठी — नाट्य और काव्य की परंपरा
इन्हें भी देखें –
- पाठ्य-मुक्तक और गेय-मुक्तक : परिभाषा, विशेषताएँ, उदाहरण, विश्लेषण, साहित्यिक महत्व
- श्रव्य काव्य : परिभाषा, प्रकार, विशेषताएँ और उदाहरण
- काव्य के सौन्दर्य तत्व: प्रयोजन, उल्लास और आधुनिक संदर्भों में उनकी प्रासंगिकता
- कविता : स्वरूप, विशेषताएँ, भेद, इतिहास, विधाएँ और महत्व
- काव्य और कविता : परिभाषा, उदाहरण, अंतर, समानता एवं साहित्यिक महत्व
- हिन्दी साहित्य की प्रमुख कहानियाँ और उनके रचनाकार | लेखक
- हिंदी उपन्यास और उपन्यासकार: लेखक और रचनाओं की सूची
- संस्मरण और संस्मरणकार : प्रमुख लेखक और रचनाएँ
- हिंदी साहित्य के प्रमुख रेखाचित्रकार और उनकी अमर रचनाएँ (रेखाचित्र)
- हिंदी डायरी साहित्य और लेखक
- क्या आरक्षण 50% सीमा से अधिक होना चाहिए? | संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक व्याख्या और समकालीन बहस
- सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण: रहस्य, विज्ञान, मान्यताएँ और आगामी ग्रहण
- ग्रैंड पैरेंट्स डे 2025: इतिहास, महत्व और मनाने के तरीके