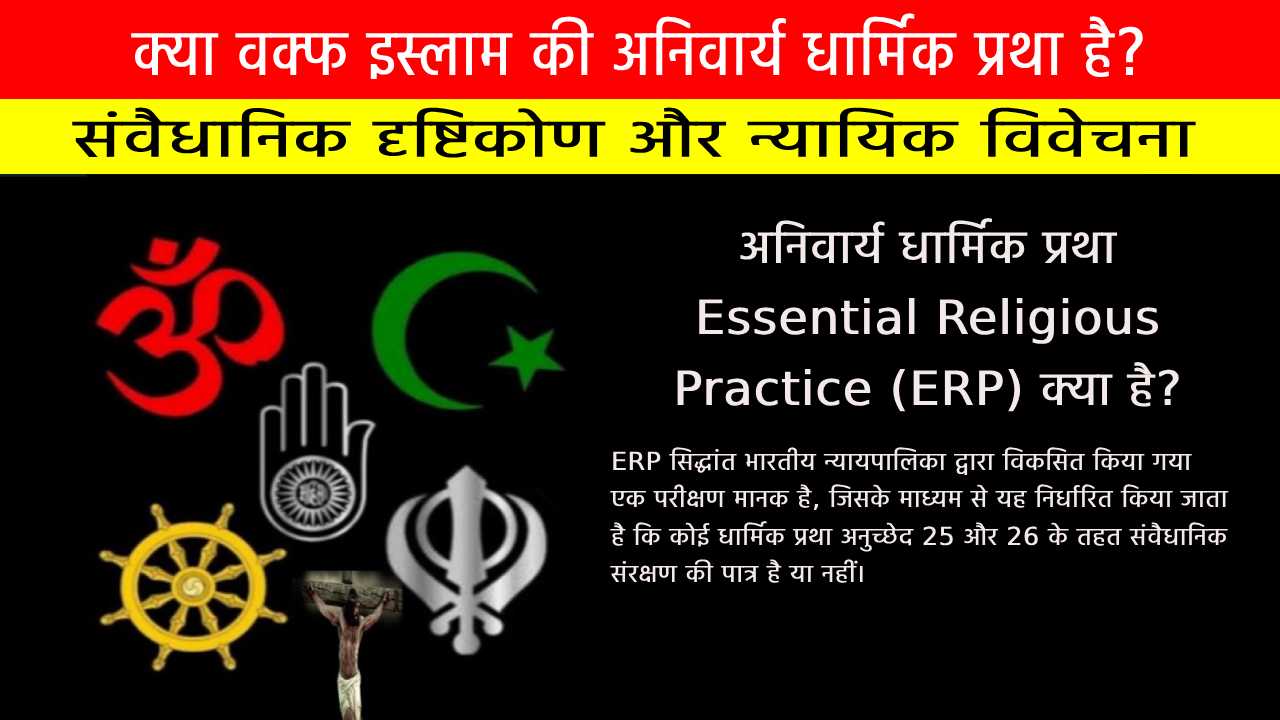भारत जैसे विविधतापूर्ण धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म और कानून का संबंध अत्यंत जटिल और संवेदनशील विषय है। धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान का मूलभूत हिस्सा है, परंतु इसकी सीमाएं भी स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण तर्क दिया कि इस्लाम में “वक्फ” की स्थापना कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practice – ERP) नहीं है। इस तर्क ने एक बार फिर “ERP सिद्धांत” की प्रासंगिकता और इसकी व्याख्या को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
वक्फ: एक परिचय
“वक्फ” एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है किसी संपत्ति को किसी धार्मिक, परोपकारी या समाजसेवी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर देना। इस्लाम में यह परंपरा काफी प्राचीन है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति का एक भाग मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, अस्पताल या गरीबों की सेवा जैसे धार्मिक या समाजसेवी कामों के लिए समर्पित किया जाता है। यह संपत्ति फिर वक्फ बोर्ड के अधीन आ जाती है और इसे धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक तरीकों से प्रबंधित किया जाता है।
वक्फ का मूल उद्देश्य परोपकार है, लेकिन क्या इसे इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा माना जा सकता है? इस प्रश्न ने संवैधानिक और धार्मिक दायरों में गहन बहस को जन्म दिया है।
केंद्र सरकार का तर्क: वक्फ ERP नहीं है
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया:
- वक्फ इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। यदि कोई मुसलमान वक्फ नहीं करता, तो उसका धार्मिक दर्जा या पहचान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे वह “कम मुसलमान” नहीं बनता और न ही इस्लाम से बाहर हो जाता है।
- वक्फ अपने स्वरूप में एक धार्मिक दान है, और दान तो हर धर्म में होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई प्रथा धार्मिक उद्देश्य से जुड़ी है, वह आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं बन जाती।
- वक्फ कानून धर्मनिरपेक्ष और प्रशासनिक है, और इसका उद्देश्य धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि संपत्ति प्रबंधन को नियमित करना है।
इन तर्कों से यह स्पष्ट होता है कि वक्फ को ERP के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसके बिना इस्लाम की मूल संरचना या पहचान नहीं बदलती।
Essential Religious Practice (ERP) क्या है?
ERP सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया एक परीक्षण मानक है, जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि कोई धार्मिक प्रथा अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संवैधानिक संरक्षण की पात्र है या नहीं।
ERP की न्यायिक परिभाषा:
सुप्रीम कोर्ट ने Commissioner of Police v. Acharya Jagadisharananda Avadhuta (2004) केस में कहा:
“किसी प्रथा को आवश्यक धार्मिक प्रथा तभी माना जा सकता है, यदि उसके न होने से धर्म की मूल पहचान ही बदल जाए।”
इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई धार्मिक कृत्य, नियम या प्रथा किसी धर्म के मूल विश्वास, उद्देश्य या पहचान का अभिन्न हिस्सा नहीं है, तो वह ERP के तहत संरक्षित नहीं हो सकती।
ERP का परीक्षण:
- क्या उस प्रथा के बिना धर्म का स्वरूप ही बदल जाएगा?
- क्या वह प्रथा धर्म के पवित्र ग्रंथों, परंपराओं या मान्यताओं से अनिवार्य रूप से जुड़ी है?
- क्या वह प्रथा धर्म के लिए इतनी केंद्रीय है कि उसे हटाया जाए तो धर्म की पहचान ही समाप्त हो जाए?
यदि उत्तर “हाँ” है, तभी वह ERP मानी जाएगी।
अनुच्छेद 25 और 26: धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा
अनुच्छेद 25 – धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता:
- हर व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है।
- यह अधिकार नागरिक और गैर-नागरिक दोनों को प्राप्त है।
- यह न केवल धार्मिक विश्वास, बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
- लेकिन यह अधिकार जन व्यवस्था, नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधीन है।
अनुच्छेद 26 – धार्मिक समुदायों के अधिकार:
- हर धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:
- धर्म या परोपकार के उद्देश्यों से संस्थान स्थापित करना और उनका संचालन करना।
- अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना।
- संपत्ति प्राप्त करना और उसका प्रशासन करना।
अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो ERP सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं:
1. Commissioner of Police v. Acharya Jagadisharananda Avadhuta (2004):
इस मामले में आनंदमार्ग संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर ‘तांडव नृत्य’ किए जाने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह इस संप्रदाय की ERP नहीं है, क्योंकि यह प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और 1955 तक यह प्रथा नहीं की जाती थी।
2. Shayara Bano v. Union of India (2017):
तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया और कहा कि यह इस्लाम की ERP नहीं है। इसे अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता।
3. हिजाब विवाद – कर्नाटक हाईकोर्ट (2022):
इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म का पालन आवश्यक है और हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, इसलिए इसे अनुच्छेद 25 का संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
ERP सिद्धांत की आलोचना और विवाद
ERP सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा धार्मिक प्रथाओं की “वैधता” और “आवश्यकता” पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। कई आलोचकों का मानना है कि यह धर्म और आस्था के मामलों में न्यायपालिका का अनुचित हस्तक्षेप है। धार्मिक समुदायों का यह तर्क है कि किसी धार्मिक प्रथा की आवश्यकता का निर्धारण केवल आस्था या धार्मिक संस्थाएं ही कर सकती हैं, न कि कोई राज्यसत्ता या अदालत।
हालांकि, न्यायपालिका का तर्क यह है कि जब कोई धार्मिक प्रथा सार्वजनिक व्यवस्था, महिला अधिकारों, बाल अधिकारों या संविधान के मूल मूल्यों का उल्लंघन करती है, तब यह निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है कि वह प्रथा ERP है या नहीं।
वक्फ का संवैधानिक और प्रशासनिक स्वरूप
भारत में वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। देशभर में वक्फ बोर्ड गठित किए गए हैं जो इन संपत्तियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं। इन बोर्डों की कार्यप्रणाली धर्मनिरपेक्ष होती है, और यह पूरी तरह से संविधान के तहत संचालित होती है।
केंद्र सरकार का यह रुख कि वक्फ ERP नहीं है, इस दृष्टिकोण पर आधारित है:
- वक्फ एक धार्मिक दान है, लेकिन दान किसी धर्म का ERP नहीं होता।
- वक्फ अधिनियम धर्मनिरपेक्ष कानून है जो धार्मिक प्रथा को बाधित नहीं करता।
- वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन धार्मिक आस्था के बजाय कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में किया जाता है।
निष्कर्ष: क्या वक्फ ERP है?
ERP सिद्धांत के आलोक में यदि वक्फ की समीक्षा की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि:
- वक्फ की अनुपस्थिति से इस्लाम की मूल संरचना या पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता।
- इसकी उपस्थिति इस्लाम में सराहनीय है, परंतु इसकी अनिवार्यता नहीं है।
- भारत में वक्फ प्रथा धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के अधीन है, और इसका उद्देश्य धार्मिक नहीं बल्कि परोपकारी एवं सामाजिक सेवा है।
इसलिए, वक्फ को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं कहा जा सकता, और इसे अनुच्छेद 25 या 26 के तहत ERP के रूप में संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल सकता।
यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने का नहीं, बल्कि धर्म और कानून के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है, जिससे संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना और सामाजिक न्याय दोनों का संरक्षण हो सके।
Polity – KnowledgeSthali
Current Affairs – KnowledgeSthali
इन्हें भी देखें –
- दल-बदल विरोधी कानून | Anti-Defection Law
- ChaSTE | चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट
- चिली गणराज्य और भारत | 76 वर्षों की मैत्री पर एक दृष्टि
- उत्तर सेंटिनल द्वीप | मानव सभ्यता से परे एक रहस्यमयी संसार
- नेशनल ई-विधान ऐप (NeVA) | नेवा
- भारतीय रेल बजट 2025 | निवेश, विकास और प्रभाव
- भारत का केंद्रीय बजट | एक व्यापक विश्लेषण
- तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर मिली नई जीवाणु प्रजाति – Niallia tiangongensis
- चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता पर ब्रिटेन-मॉरीशस समझौता
- नालंदा विश्वविद्यालय | प्राचीन गौरव और आधुनिक पुनरुत्थान की कहानी
- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता एवं नामांकन सूची | 2005–2025
- बानु मुश्ताक | अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका