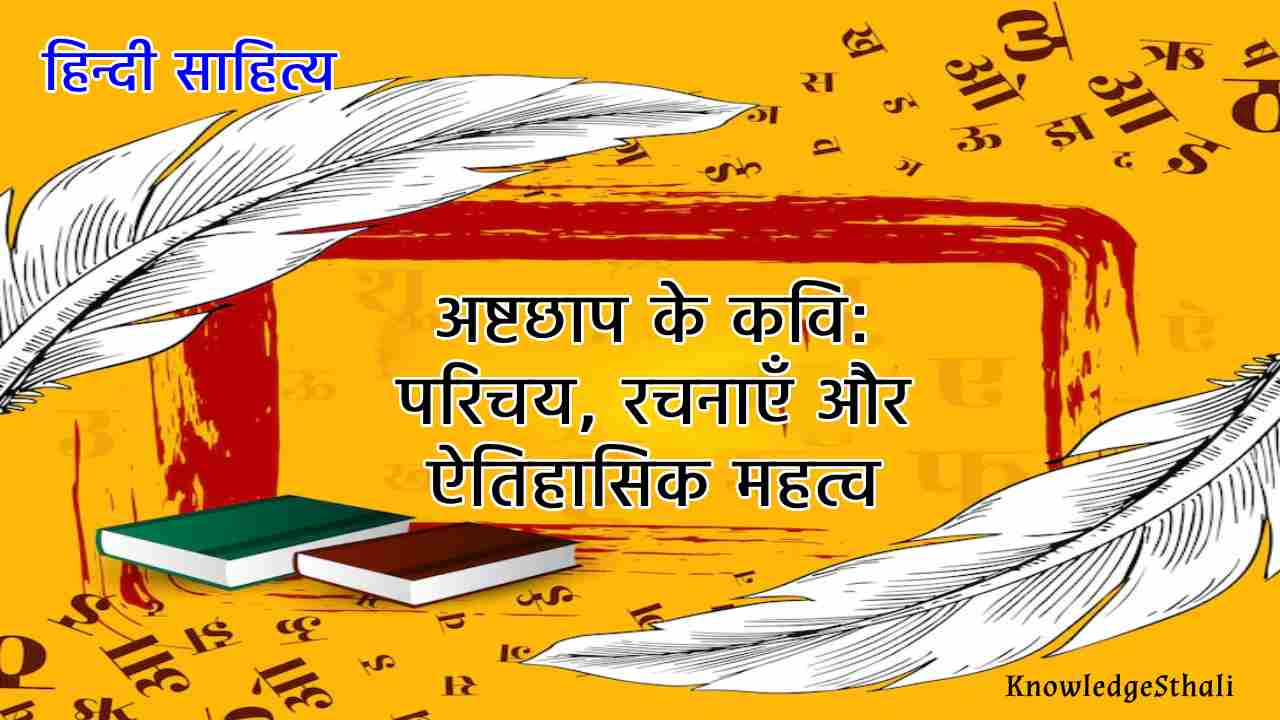यह लेख भक्ति काल की प्रमुख धारा पुष्टिमार्ग से जुड़े आठ विशिष्ट भक्त कवियों के समूह अष्टछाप पर केंद्रित है, जो न केवल श्रीकृष्ण भक्ति के महान साधक थे, बल्कि अत्यंत उत्कृष्ट रचनाकार, संगीतज्ञ और कीर्तनकार भी थे। इस लेख में प्रमुख कवि सूरदास और कुंभनदास के जीवन, काव्य और भक्ति दृष्टिकोण का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। सूरदास की वात्सल्य रस से भरपूर रचनाएँ, जैसे सूरसागर, श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती हैं, वहीं कुंभनदास की सादगीपूर्ण भक्ति, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों—”संतन को कहा सीकरी सों काम?”—में झलकती है।
लेख आगे बढ़कर अष्टछाप के अन्य कवियों – नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविंदस्वामी और चतुर्भुजदास – की सामाजिक पृष्ठभूमि, काव्य योगदान, तथा पुष्टिमार्ग में उनकी भूमिका का क्रमबद्ध विवेचन करता है। यह लेख यह भी स्पष्ट करता है कि अष्टछाप के कवि सामाजिक दृष्टि से विविध वर्णों से थे, किंतु सभी श्रीकृष्ण भक्ति में समान रूप से रमे हुए थे।
इसके अतिरिक्त, अष्टछाप की सांस्कृतिक महत्ता, उनके द्वारा स्थापित कीर्तन परंपरा, तथा संगठित कवि-मंडल के रूप में उनका ऐतिहासिक महत्व भी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। यह लेख हिंदी साहित्य और भारतीय भक्ति परंपरा में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक है।
परिचय: अष्टछाप क्या है?
अष्टछाप हिंदी साहित्य एवं भक्ति आंदोलन का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कवि समूह था, जिसकी स्थापना 1564 ईस्वी में की गई थी। यह समूह आठ प्रमुख कवियों का था, जिन्हें अष्टछाप कवि कहा गया। ‘अष्ट’ का अर्थ ‘आठ’ और ‘छाप’ का अर्थ ‘चिह्न’ होता है, अर्थात् ये आठ कवि वैष्णव संप्रदाय की रचनात्मक परंपरा में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले रचनाकार थे। इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रीकृष्ण की लीलाओं का अत्यंत भावनात्मक और सरस चित्रण किया।
अष्टछाप के कवियों को दो प्रमुख समूहों में बाँटा गया है —
- महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य
- श्री विट्ठलनाथ जी (वल्लभाचार्य जी के पुत्र) के शिष्य
| महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य | 1. सूरदास 2. कुंभन दास 3, परमानंद दास 4. कृष्ण दास |
| श्री विट्ठलनाथ जी (वल्लभाचार्य जी के पुत्र) के शिष्य | 5. छीत स्वामी 6. गोविंद स्वामी 7. चतुर्भुज दास 8. नंद दास |
ये सभी कवि पुष्टिमार्ग के अनुयायी थे और इनकी रचनाओं का मुख्य उद्देश्य श्रीकृष्ण की भक्ति, प्रेम और सेवा को समर्पित करना था। अष्टछाप की रचनाएँ संगीत, काव्य और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं।
भक्ति काल और अष्टछाप का स्थान
हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल (1350-1650 ई.) को साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इस युग को चार उपवर्गों में बाँटा गया है:
- संत काव्य
- सूफी काव्य
- कृष्ण भक्ति काव्य
- राम भक्ति काव्य
अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाओं में श्रीकृष्ण के बाल्य-रूप, रासलीला, गोचारण, क्रीड़ा, और गोपियों के साथ प्रेमपूर्ण संवादों का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है।
अष्टछाप कवियों की सूची
| क्रम | कवि का नाम | गुरु का नाम | संबंध |
|---|---|---|---|
| 1 | सूरदास | महाप्रभु वल्लभाचार्य | शिष्य |
| 2 | कुंभन दास | महाप्रभु वल्लभाचार्य | शिष्य |
| 3 | परमानंद दास | महाप्रभु वल्लभाचार्य | शिष्य |
| 4 | कृष्णदास | महाप्रभु वल्लभाचार्य | शिष्य |
| 5 | छीतस्वामी | श्री विट्ठलनाथ जी | शिष्य |
| 6 | गोविंदस्वामी | श्री विट्ठलनाथ जी | शिष्य |
| 7 | चतुर्भुजदास | श्री विट्ठलनाथ जी | शिष्य |
| 8 | नंददास | श्री विट्ठलनाथ जी | शिष्य |
प्रमुख अष्टछाप कवियों का परिचय एवं रचनाएँ
1. सूरदास (1478–1583 ई.)
जन्मस्थल: सीही गाँव (दिल्ली के समीप) / कुछ मतों के अनुसार रुनकता (मथुरा-आगरा मार्ग)
गुरु: महाप्रभु वल्लभाचार्य
विशेषता: अंधत्व के बावजूद अद्वितीय काव्यदृष्टि
सूरदास अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जीवन श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का काव्यात्मक चित्रण करते हुए बीता। वे श्री वल्लभाचार्य के संपर्क में गऊघाट पर आए और वहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई।
प्रमुख रचनाएँ:
- सूरसागर – श्रीकृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन
- साहित्य लहरी – काव्यशास्त्र संबंधी पद
- सूरसरावली – ब्रजभाषा में रचित श्रृंगार व वात्सल्य के पद
विशेष योगदान:
सूरदास ने वात्सल्य रस में अद्भुत गहराई पैदा की। यशोदा-श्रीकृष्ण के संवादों में उन्होंने माँ की ममता और बालक की चंचलता को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी शैली गेय, सहज और संवेदनात्मक है।
2. कुंभन दास (1468–?)
जन्म: जमुनावतो, मथुरा
गुरु: महाप्रभु वल्लभाचार्य
वर्ग: गौरवा क्षत्रिय
जीवन दृष्टिकोण: सादगी और भक्ति से परिपूर्ण
कुंभनदास की जीवनशैली बहुत सरल थी। उन्होंने कभी राज्य-सम्मान को महत्व नहीं दिया, बल्कि भक्ति को ही सर्वोपरि माना। जब अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया, तो लौटते हुए उन्होंने कहा:
“संतन को कहा सीकरी सों काम?
आवत जात पनहियाँ टूटी, बिसरि गयो हरि नाम।।”
रचनाएँ:
- विभिन्न त्योहारों (जन्माष्टमी, वसंत, रथयात्रा, गोवर्धन पूजा आदि) पर आधारित पद
- कृष्णलीला विषयक – गोचार, राजभोग, शयन, सुरति, दानलीला आदि
- गुरु भक्ति विषयक पद
कुंभनदास की भाषा सरल, ब्रजभाषा प्रधान और भावुक है। उन्होंने नित्यसेवा के अंतर्गत आने वाले कर्मों का भी रसपूर्ण वर्णन किया।
3. परमानंद दास (ज. संवत् 1606)
जन्मस्थल: कन्नौज (उत्तर प्रदेश)
गुरु: महाप्रभु वल्लभाचार्य
वर्ग: कान्यकुब्ज ब्राह्मण
विशेषता: माधुर्य रस के श्रेष्ठ गायक, रचनाओं में सहज भाव एवं ब्रज प्रेम
परमानंद दास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद दूसरा स्थान रखते हैं। उनका जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ, किन्तु भक्ति और काव्य दोनों में वे समृद्ध थे। उन्होंने श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला और ब्रज-जीवन का अत्यंत माधुर्यपूर्ण वर्णन किया। उनके पद मधुर, सरस और गेय हैं, जिनमें श्रृंगार और वात्सल्य का सुंदर समन्वय मिलता है।
प्रमुख रचनाएँ:
- परमानंद सागर – 835 पदों का संग्रह
- ध्रुव चरित्र – भक्त ध्रुव की कथा
- दानलीला – श्रीकृष्ण की दानलीला का चित्रण
- उद्धव लीला – उद्धव और गोपियों के संवाद पर आधारित
- वल्लभ संप्रदायी कीर्तन दर्प संग्रह
- संस्कृत रत्नमाला – संस्कृत पदों का संग्रह
विशेष योगदान:
परमानंद दास के पद ब्रज संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। उनमें भक्ति का सहज प्रवाह और काव्य की स्वाभाविकता स्पष्ट दिखाई देती है।
4. कृष्ण दास (ज. लगभग 1495 ई.)
जन्मस्थल: चिलोतरा, गुजरात
गुरु: महाप्रभु वल्लभाचार्य
वर्ग: कुनबी पाटिल
विशेषता: संगठन, व्यवहार-कुशलता, दृढ़ भक्ति
कृष्ण दास की जीवन कथा असाधारण है। बचपन में ही जब उन्होंने अपने पिता को अनुचित कृत्य करते देखा तो न्याय के पक्ष में खड़े हुए। भक्ति का मार्ग चुनने के बाद वल्लभाचार्य ने उन्हें ‘भेंटिया’ नियुक्त किया और बाद में श्रीनाथजी मंदिर के उत्तरदायित्व दिए। वे उत्कृष्ट व्यवस्थापक, भक्त और कवि थे।
प्रमुख रचनाएँ:
- जुगलमान चरित – राधा-कृष्ण की युगल लीला
- भ्रमरगीत – उद्धव और गोपियों का भावनात्मक संवाद
- प्रेमतत्त्व निरूपण – प्रेम के दर्शन पर आधारित रचना
विशेष योगदान:
कृष्ण दास की कविताओं में प्रेम और दर्शन का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। उनके रचनात्मक कौशल में संगठन और साधना दोनों झलकते हैं।
5. छीत स्वामी (1515–1585 ई.)
जन्मस्थल: मथुरा
गुरु: विट्ठलनाथ (गोस्वामी विठ्ठलाचार्य)
वर्ग: चौबे ब्राह्मण
विशेषता: सांसारिकता से वैराग्य की ओर यात्रा, बीरबल के पुरोहित
छीत स्वामी का जीवन पहले उद्दंडता से भरा था, लेकिन विट्ठलाचार्य के संपर्क में आकर उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। उनके पदों में श्रृंगार रस के साथ ब्रजभूमि के प्रति अद्भुत अनुराग दिखाई देता है। वे ब्रज की वायु, भूमि और संस्कृति से अत्यंत प्रेम करते थे।
प्रमुख रचनाएँ:
- आठ पहर की सेवा – नित्य सेवा के चरणों का भावपूर्ण वर्णन
- गोसाईं जी की बधाई – गुरुभक्ति पर आधारित पद
- कृष्ण लीला के विविध प्रसंग – रास, बाललीला, व्रज की सजीव झांकी
विशेष योगदान:
छीत स्वामी के पदों में भक्ति और ब्रजभूमि का अद्वितीय चित्रण मिलता है। उनकी रचनाओं में भावुकता और सौंदर्य बोध का सुंदर समन्वय है।
6. गोविंद स्वामी (1505–?)
जन्मस्थल: आतरी (भरतपुर, राजस्थान)
गुरु: विट्ठलाचार्य
वर्ग: सनाढ्य ब्राह्मण
विशेषता: कुशल गायक, रागों में पारंगत, गहन भक्ति
गोविंद स्वामी अष्टछाप के अंतिम कवि माने जाते हैं। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागकर श्रीनाथजी की सेवा को अपनाया और गोवर्धन के निकट कदमखाड़ी पर निवास किया। वे संगीत के गहरे ज्ञाता थे, और उनके पदों में संगीतात्मकता और भावपूर्ण काव्य का अद्भुत संगम है।
प्रमुख रचनाएँ:
- भूत सी भयावनी… – श्रृंगार और सौंदर्य व्यंजना का प्रसिद्ध पद
- मो मन बसौ श्यामा-श्याम
- देखो माई इत घन उत नंद लाल
विशेष योगदान:
उनकी भाषा बिंबात्मक, भावप्रवण और अत्यंत चित्ताकर्षक है। वे भक्ति और सौंदर्य के अद्वितीय कवि हैं।
7. चतुर्भुज दास (1520–1624 वि.सं.)
जन्मस्थल: जमुनावती गाँव
गुरु: विट्ठलनाथ जी
वर्ग: गौरवा क्षत्रिय
विशेषता: श्रीनाथजी के अंतरंग सखा, सरल स्वभाव
चतुर्भुज दास, कुंभनदास के पुत्र थे और वल्लभ संप्रदाय में उनका अत्यंत मान था। वे सरल, विनम्र और पूर्णत: समर्पित भाव से श्रीकृष्ण की सेवा में लीन रहते थे। उनके पदों में श्रीकृष्ण के सौंदर्य, श्रृंगार, नवीनता और लीलाओं का मोहक वर्णन है।
प्रमुख रचनाएँ:
- द्वादश यश – बारह ग्रंथों का संग्रह
- हितजू को मंगल
- मंगलसार यश
- शिक्षासार यश
विशेष योगदान:
चतुर्भुजदास के पदों में श्रीकृष्ण के प्रति सहज आकर्षण, गहराई और मधुरता है। भाषा सरस, चलती और भावपूर्ण है।
8. नंद दास (1420–1639 वि.सं.)
जन्मस्थल: रामपुर (अब श्यामपुर, कासगंज, उत्तर प्रदेश)
गुरु: गोस्वामी विट्ठलनाथ
वर्ग: सनाढ्य ब्राह्मण
विशेषता: संस्कृत व ब्रजभाषा के विद्वान, रसिक स्वभाव
नंददास अष्टछाप के एक प्रमुख कवि थे। वे अत्यंत रसिक प्रवृत्ति के थे और श्रीकृष्ण की रासलीला, व्रजविलास, श्रृंगार, बाल्य और ब्रज की भूमि पर विशेष प्रेम करते थे। भागवत की रासपंचाध्यायी का अनुवाद उनके विद्वत्व का प्रमाण है।
प्रमुख रचनाएँ:
- छोटो सो कन्हैया एक मुरली मधुर छोटी
- झूलत राधामोहन
- ऊधव के उपदेश सुनो ब्रज नागरी
- माई फूल को हिंडोरो बन्यो
- श्री लक्ष्मण घर बाजत आज बधाई
- भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जु देई
- अरी चल दूल्हे देखन जाय
विशेष योगदान:
नंददास ने श्रृंगार और वात्सल्य रस में रचनाएं कीं, जिनमें कृष्ण की लीलाओं का रसात्मक चित्रण मिलता है। उनकी भाषा ब्रज की मिठास लिए हुए है और कल्पनाशक्ति अत्यंत प्रभावशाली है।
अष्टछाप के कवियों की विशेषताएँ
अष्टछाप के कवि भक्ति काल के ऐसे विशिष्ट रचनाकार थे, जो वल्लभ संप्रदाय की पुष्टिमार्गीय परंपरा से जुड़े हुए थे। ये सभी कवि भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे और श्रीनाथजी की सेवा के लिए समर्पित थे। इनका काव्य मुख्यतः वात्सल्य, शृंगार, और माधुर्य रस से अनुप्राणित था।
इन आठों भक्त कवियों को भगवदीय कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी भक्ति केवल औपचारिक या साधनात्मक न होकर पूर्ण समर्पण और प्रेम से ओतप्रोत थी। ये सभी कवि श्रीनाथजी के मंदिर की नित्यलीला में भगवान के सखा रूप में सहभाग करते थे, इसीलिए इन्हें ‘अष्टसखा’ भी कहा जाता है। गोस्वामी विट्ठलनाथजी (वल्लभाचार्य के पुत्र) ने इन्हें कीर्तन एवं सेवा के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया था। उन्हीं के आशीर्वाद और निर्देशन से इस मंडल का नाम पड़ा — ‘अष्टछाप’।
सामाजिक विविधता
अष्टछाप के कवि विभिन्न सामाजिक और वर्णीय पृष्ठभूमियों से आते थे, जिससे वल्लभ संप्रदाय की सर्वसमावेशी दृष्टि पर प्रकाश पड़ता है:
- परमानंद दास – कान्यकुब्ज ब्राह्मण
- कृष्णदास – शूद्रवर्ण
- कुंभनदास – गौरव क्षत्रिय (राजपूत), परंतु जीवन में कृषिकर्म को अपनाया
- सूरदास – कुछ मतों के अनुसार सारस्वत ब्राह्मण, तो कुछ के अनुसार ब्रह्मभट्ट
- गोविंद स्वामी – सनाढ्य ब्राह्मण
- छीत स्वामी – माथुर चौबे (ब्राह्मण)
- नंददास – सोरों (सुक्रक्षेत्र) के सनाढ्य ब्राह्मण; महाकवि तुलसीदास के चचेरे भाई
- चतुर्भुजदास – गौरव क्षत्रिय; कुंभनदास के पुत्र
इस प्रकार अष्टछाप में जातिगत विविधता होने के बावजूद, सभी ने श्रीकृष्ण की भक्ति में समान निष्ठा और प्रेम प्रदर्शित किया।
रचनात्मक विशेषताएँ
अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में गेयता, भावप्रवणता, सरलता और रस-संपृक्ति विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। इनकी भाषा मुख्यतः ब्रजभाषा है, जो न केवल भाव सम्प्रेषण में सहायक रही, बल्कि लोक को भक्ति-संगीत से जोड़ने का माध्यम भी बनी।
इन कवियों में:
- कुंभनदास सबसे प्राचीन (ज्येष्ठ) थे
- नंददास सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं
- काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, सूरदास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जबकि नंददास को द्वितीय स्थान दिया जाता है
सूरदास को पुष्टिमार्ग का नायक कवि माना जाता है। उनकी ‘सूरसागर’ जैसी रचना वात्सल्य और श्रृंगार रस के अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करती है। नंददास की ‘रासपंचाध्यायी’, ‘भवरगीत’ और ‘सिद्धांतपंचाध्यायी’ काव्य सौष्ठव और भाषिक प्रांजलता के लिए प्रसिद्ध हैं।
अन्य कवियों की प्रमुख विशेषताएँ एवं रचनाएँ:
- परमानंद दास – परमानंद सागर में संकलित पदों में माधुर्य एवं लीलामय भाव
- कृष्णदास – भ्रमरगीत और प्रेमतत्त्व निरूपण जैसे दार्शनिक और भावात्मक काव्य
- कुंभनदास – कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, परंतु उनके फुटकर पद अत्यंत प्रसिद्ध हैं
- छीत स्वामी एवं गोविंद स्वामी – संकलित ग्रंथ नहीं, लेकिन भावसंपन्न पद कीर्तन में प्रचलित
- चतुर्भुजदास – द्वादश यश, भक्ति प्रताप आदि रचनाएँ; भाषा की सरलता एवं प्रभावशीलता
सांस्कृतिक योगदान
अष्टछाप का गठन उस समय हुआ जब भारत में संगठित रचनाकार या कलाकार मंडल की परंपरा प्रचलित नहीं थी। भक्ति काल में किसी आचार्य द्वारा कवियों, कीर्तनकारों और गायकों का ऐसा संघटन अद्वितीय था। अष्टछाप की यह परंपरा आधुनिक युग में भारतेंदु मंडल, रसिक मंडल, मतवाला मंडल, परिमल, प्रगतिशील लेखक संघ, और जनवादी लेखक संघ जैसी रचनात्मक संस्थाओं का पूर्वरूप मानी जा सकती है।
इन आठों भक्त-कवियों ने लगभग 84 वर्षों तक श्रीकृष्ण भक्ति, कीर्तन और काव्य के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। वे सभी अपने समय के श्रेष्ठ संगीतज्ञ, कविगायक और कीर्तनकार थे। इनकी भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवनदृष्टि थी, जो आज भी भारतीय संस्कृति की धरोहर बनी हुई है।
निष्कर्ष
अष्टछाप के कवियों ने हिंदी साहित्य को ही नहीं, भारतीय भक्ति परंपरा को भी अमूल्य योगदान दिया। उनकी कविताएँ केवल साहित्यिक रचनाएँ नहीं हैं, बल्कि भक्ति का साक्षात अनुभव हैं।
आज भी इन कवियों के पद श्रीनाथजी, द्वारकाधीश, और गोवर्धन के मंदिरों में गाए जाते हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया और ब्रजभाषा को साहित्य की एक समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित किया।
अष्टछाप केवल आठ कवियों का समूह नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है जो भक्ति, संगीत और साहित्य को एकत्रित करती है।
इन्हें भी देखें –
- यह मेरी मातृभूमि है | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- आकाशदीप कहानी- जयशंकर प्रसाद
- क़लम का सिपाही | प्रेमचन्द जी की जीवनी : अमृत राय
- कबीर दास जी के दोहे एवं उनका अर्थ | साखी, सबद, रमैनी
- कबीर दास जी | जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएँ एवं भाषा
- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ
- हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास
- हिंदी के विराम चिन्ह और उनका प्रयोग | 50 + उदाहरण
- भक्ति काल के कवि और उनके काव्य (रचनाएँ)
- सगुण भक्ति काव्य धारा: अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और साहित्यिक विशेषताएँ
- प्राकृतिक संसाधनों का तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक होने के आधार पर वर्गीकरण
- प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार या स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण
- प्राकृतिक संसाधनों का उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण