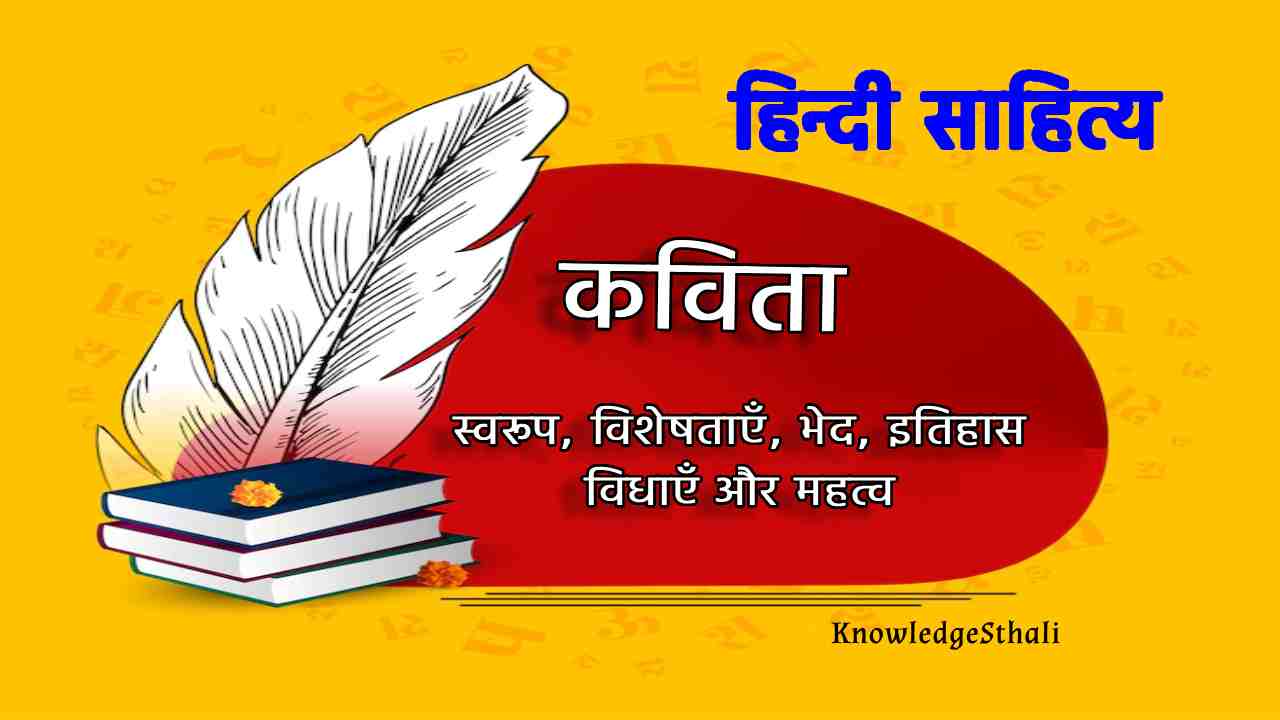मानव सभ्यता के आरंभ से ही भावनाओं, विचारों और अनुभवों को अभिव्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम कविता रही है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकली हुई भावनाओं की लहर है, जो पाठक या श्रोता के मन में कंपन उत्पन्न करती है। जब कोई भाव लय, छंद और अलंकारों के साथ अभिव्यक्त होता है, तो वह साधारण गद्य से आगे बढ़कर कविता का रूप धारण कर लेता है। कविता न केवल साहित्य की आत्मा मानी जाती है, बल्कि यह मानव के संवेदनात्मक जीवन को गहराई से छूने की क्षमता रखती है।
कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह यथार्थ को मात्र जस का तस चित्रित नहीं करती, बल्कि कवि की दृष्टि से संशोधित, सुसज्जित और भावनाओं से ओतप्रोत रूप में प्रस्तुत करती है। इसीलिए कहा जाता है कि कवि का सत्य, सामान्य सत्य से भिन्न होता है।
कविता का स्वरूप
कविता पद्यात्मक एवं छंद-बद्ध रचना होती है, जिसमें भावना की प्रधानता होती है। यह तर्क और युक्ति की बजाय रसानुभूति पर आधारित होती है। कविता का उद्देश्य मात्र जानकारी देना नहीं, बल्कि सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद प्रदान करना है।
कविता में—
- छंद उसे लय देता है
- अलंकार उसे सौंदर्य प्रदान करते हैं
- भावनाएँ उसे जीवंत बनाती हैं
कविता में यथार्थ का प्रस्तुतीकरण उस रूप में होता है, जैसा कवि ने अनुभव किया है और जिस रूप में वह उससे प्रभावित हुआ है। यही कारण है कि कविता में अतिशयोक्ति का प्रयोग भी दोष नहीं माना जाता, बल्कि वह अलंकार का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए—
“तेरा आंचल है चाँदनी की तरह, तेरे चेहरे की मुस्कान सूरज से भी तेज़ है”
यह तथ्यात्मक रूप से संभव न हो, फिर भी भावनात्मक स्तर पर यह अभिव्यक्ति सौंदर्य पैदा करती है।
कविता की परिभाषा
कविता साहित्य की सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली विधा है। यह केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि भावनाओं, विचारों और अनुभवों की आत्मीय अभिव्यक्ति है। कविता में कवि अपने हृदय की गहनतम संवेदनाओं को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, ताकि वे पाठक अथवा श्रोता के हृदय तक पहुँचकर उसे छू सकें।
कविता प्रायः छंद, अलंकार और लय से युक्त होती है, किन्तु आधुनिक युग में यह मुक्त रूप में भी लिखी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल सूचनाएँ देना नहीं, बल्कि भावों और संवेदनाओं को इस तरह प्रस्तुत करना है कि पाठक या श्रोता उसमें डूबकर आनंद, करुणा, प्रेरणा, प्रेम अथवा अन्य भावों का अनुभव कर सके।
कविता की विशेषता यह है कि वह प्रत्यक्ष सूचना न देकर अप्रत्यक्ष भावानुभूति कराती है। साधारण भाषा जहाँ तथ्य प्रस्तुत करती है, वहीं कविता भाव प्रस्तुत करती है। इसमें शब्द केवल माध्यम होते हैं, वास्तविक लक्ष्य है भावों का सौंदर्य, संवेदनाओं की तीव्रता और आत्मा की तरलता।
कविता की प्रमुख विशेषताएँ
- भावप्रधानता – कविता का मूल आधार हृदय की अनुभूति है।
- सौंदर्य-बोध – यह पाठक को कलात्मक आनंद, रस और सौंदर्य का अनुभव कराती है।
- लय और छंद – पारंपरिक कविता छंद, तुक और लय पर आधारित होती है, जबकि आधुनिक कविता मुक्तछंद में भी लिखी जाती है।
- प्रेरक और स्पर्शक प्रभाव – कविता पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति स्वयं को भावों की उसी अवस्था में अनुभव करता है, जिसमें कवि ने उसे लिखा।
- सामूहिक भावाभिव्यक्ति – कविता व्यक्तिगत अनुभूति को सामूहिक रूप देकर सबके लिए ग्राह्य बनाती है।
विद्वानों द्वारा दी गई कविता की परिभाषाएँ
- जयशंकर प्रसाद –
“कविता हृदय की उस कोमल अनुभूति का नाम है, जो शब्दों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करती है।” - रामचंद्र शुक्ल –
“कविता वह है, जो हृदयगत भावों का सामूहिक रूप में कलात्मक प्रदर्शन करती है।” - महादेवी वर्मा –
“कविता वह अनुभूति है, जो सीधे हृदय से फूटकर शब्दों में ढल जाती है।”
सरल शब्दों में कविता की परिभाषा
कविता हृदय की कोमल और गहन भावनाओं की वह कलात्मक अभिव्यक्ति है, जो भाषा के माध्यम से व्यक्त होकर पाठक या श्रोता को गहराई से स्पर्श करती है और उसे भावात्मक आनंद प्रदान करती है।
👉 अर्थात — कविता = भाव, अनुभव और सौंदर्य की भाषा।
कविता की विधाएँ
कविता एक व्यापक विधा है, जिसके अंतर्गत अनेक उपविधाएँ आती हैं। प्रत्येक विधा का अपना अलग स्वरूप, उद्देश्य और प्रस्तुतीकरण शैली होती है। प्रमुख विधाएँ निम्नलिखित हैं—
- गीत – मधुर लय, सरल भाषा और भावपूर्ण प्रस्तुति वाला पद्य।
उदाहरण: जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन के गीत। - दोहा – दो पंक्तियों का छंद, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 13 और 11 मात्राएँ होती हैं।
उदाहरण: कबीर, रहीम के दोहे। - भजन – ईश्वर की स्तुति में रचित रचना।
उदाहरण: सूरदास, मीरा के भजन। - ग़ज़ल – उर्दू-हिंदी में प्रचलित छंदबद्ध, तुकांत शेरों की श्रृंखला, जिसमें प्रेम, विरह या दार्शनिक भावनाएँ व्यक्त होती हैं।
उदाहरण: मिर्ज़ा ग़ालिब, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। - काव्यनाट्य, मुक्तक, सॉनेट, हाइकु – विशेष संरचना और भाव के आधार पर बनी अन्य विधाएँ।
इस प्रकार, कविता का संसार विविधता और रचनात्मक संभावनाओं से भरा हुआ है।
कविता के विषय
कविता का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मूलतः मानव जीवन ही इसका केंद्र बिंदु है, लेकिन कवि पशु-पक्षी, प्रकृति, ब्रह्मांड, समाज, इतिहास और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों तक पर भी कविता रच सकता है।
पुराने समय में कवियों के विषय अक्सर महापुरुष, ऐतिहासिक घटनाएँ और वीरगाथाएँ होते थे, जबकि आधुनिक कविता में जीवन के उपेक्षित और सामान्य पक्ष भी केंद्र में आने लगे हैं।
उदाहरण—
- भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सामाजिक समस्याओं को
- सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति और सौंदर्य को
- नागार्जुन ने किसानों और श्रमिकों की पीड़ा को
कविता का विषय बनाया।
आज के कवि छिपकली, केंचुआ, या टूटी हुई सड़क जैसे प्रतीत होने वाले सामान्य विषयों में भी गहरे जीवन सत्य और संवेदनाएँ खोज लेते हैं। यही कविता की वास्तविक शक्ति है—साधारण को असाधारण बना देना।
कविता और संगीत
कविता और संगीत का रिश्ता बहुत पुराना है। छंद कविता को लय प्रदान करता है, और यह लय पाठक या श्रोता के मन में संगीत का आभास कराती है। छंद की यति-गति, वर्गों की आवृत्ति और तुकांत मिलकर इसे और मधुर बनाते हैं।
हालाँकि, कविता और संगीत में मूल अंतर यह है कि—
- संगीत का आनंद नाद (स्वर) से मिलता है
- कविता का आनंद अर्थ से मिलता है
कविता में नाद-सौंदर्य, अर्थ-सौंदर्य का अनुगामी होता है। यानी, शब्दों की ध्वनि अर्थ को और प्रभावी बनाने में सहायक बनती है।
सादृश्य-विधान (अप्रस्तुत योजना)
कविता भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए सादृश्य-विधान का सहारा लेती है। इसमें कवि किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का वर्णन करने के लिए उसके सदृश किसी अन्य वस्तु का उदाहरण देता है।
उदाहरण—
- कमल के सदृश नेत्र
- चाँद-सा मुख
- सिंह के समान वीर
इस प्रकार की अभिव्यक्ति पाठक के मन में तुरंत चित्र उकेर देती है और भावनाओं को गहराई से पहुँचाती है।
शब्द-शक्ति
कविता का सबसे महत्वपूर्ण आधार शब्द हैं, और शब्द की अपनी एक शक्ति होती है, जिसे शब्द-शक्ति कहते हैं। यह वह क्षमता है जिससे शब्द अर्थ का बोध कराता है।
शब्द-शक्तियों के तीन मुख्य प्रकार हैं—
- अभिधा – मुख्य अर्थ का बोध कराना।
उदाहरण: “कमल” शब्द का अर्थ फूल। - लक्षणा – मुख्य अर्थ में बाधा होने पर अन्य संबंधित अर्थ का बोध कराना।
उदाहरण: “गाँव सो रहा है” – यहाँ गाँव से तात्पर्य गाँव के लोग। - व्यंजना – ध्वनि के माध्यम से अप्रत्यक्ष या भावात्मक अर्थ का बोध कराना।
उदाहरण: “फूल हँस रहे हैं” – यहाँ हँसना रूपक है, जो प्रसन्नता का भाव व्यक्त करता है।
कविता का रस लेने के लिए पाठक को शब्द के लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तक पहुँचना आवश्यक है। इसीलिए कवि शब्द-चयन में अत्यंत सावधानी बरतता है।
कविता और यथार्थ
कविता में यथार्थ का प्रस्तुतीकरण प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि कवि की दृष्टि से होता है। इसका अर्थ यह है कि कवि किसी दृश्य, घटना या भाव को अपने अनुभव और कल्पना से संवारकर प्रस्तुत करता है।
उदाहरण के लिए—
यदि कवि सूर्यास्त देख रहा है, तो वह इसे केवल वैज्ञानिक दृष्टि से “सूर्य का क्षितिज के नीचे जाना” नहीं कहेगा, बल्कि इसे “सुनहरे आभा में डूबता हुआ लाल सूरज” के रूप में चित्रित करेगा। यह भावनात्मक दृष्टि ही कविता को कला का दर्जा देती है।
कविता के सौन्दर्य-तत्व
कविता का वास्तविक आकर्षण केवल उसके विषय या विचार में ही नहीं, बल्कि उसकी प्रस्तुति, भाषा, लय और भावों में निहित होता है। यह आकर्षण उत्पन्न करने वाले प्रमुख घटकों को सौन्दर्य-तत्व कहा जाता है। काव्यशास्त्र में सौन्दर्य-तत्वों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि ये ही तत्व कविता को सामान्य लेखन से अलग और विशिष्ट बनाते हैं।
काव्य-भाषा
काव्य-भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है। इसमें रागात्मकता, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और नादात्मकता जैसे गुण विद्यमान रहते हैं। यह भाषा—
- कभी विचलित और अटपटी, तो कभी सुसंस्कृत और परिमार्जित
- कभी स्वच्छंद और लचीली, तो कभी जीवंत और प्रभावी होती है।
कवि अपनी अनुभूति को प्रेषणीय बनाने के लिए सामान्य भाषा में परिवर्तन कर देता है। वह शब्दों के अनेक विकल्पों में से वही चुनता है, जो भाव को सर्वाधिक सशक्त रूप से व्यक्त कर सके।
काव्य-भाषा में चित्रोपम और बिम्ब-विधायिनी शक्ति होती है। एक सफल कवि वह है, जो दृश्य का ऐसा वर्णन करे कि पाठक की कल्पना में उसका चित्र सजीव हो उठे। साथ ही इसमें सुकुमारता, कोमलता, नाद-सौन्दर्य और रसानुकूल वर्ण-योजना भी पाई जाती है।
कविता के प्रमुख सौन्दर्य-तत्व निम्नलिखित हैं—
- भाव-सौन्दर्य
- विचार-सौन्दर्य
- नाद-सौन्दर्य
- अप्रस्तुत-योजना का सौन्दर्य
1. भाव-सौन्दर्य
कविता का मूल तत्व भाव है। भाव-सौन्दर्य तब प्रकट होता है जब कवि के अंतर्मन में उपजे भाव पाठक या श्रोता के हृदय में भी उसी तीव्रता से संचारित हों। कविता में भाव केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है, जिसमें प्रेम, करुणा, शौर्य, सौन्दर्य, वियोग, आनंद—सभी का समावेश हो सकता है।
भाव-सौन्दर्य का अर्थ है—प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि भावों का परिस्थितियों के अनुसार मर्मस्पर्शी चित्रण। साहित्यशास्त्रियों ने भाव-सौन्दर्य को ही रस कहा है और रस को काव्य की आत्मा माना है।
काव्य में सामान्यतः नौ रस माने जाते हैं—शृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, शान्त, भयानक, अद्भुत और वीभत्स। परवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को भी अलग रस के रूप में स्वीकार किया है।
- सूरदास के बाल-वर्णन में वात्सल्य रस
- गोपियों के प्रेम में शृंगार रस
- भूषण की ‘शिवा बावनी’ में वीर रस का सुन्दर चित्रण मिलता है।
भाव, विभाव और अनुभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और यही कविता को हृदयग्राही बनाता है।
जब कवि अपनी अनुभूतियों को हृदयस्पर्शी भाषा में प्रस्तुत करता है, तो पाठक भी उन भावों में डूब जाता है। उदाहरण के लिए—
पात-पात पर बिखरी धूप सुनहरी,
मन मेरा हो आया वन-विहारी॥
इन पंक्तियों में कवि ने वसंत ऋतु के सौम्य वातावरण से अपने हृदय में उपजे आनंद का चित्र खींचा है।
वियोग की करुणा भी भाव-सौन्दर्य का सशक्त रूप है—
बिन तुम्हरे सूना सूना आँगन,
हर आहट लगती पग-चिन्हन॥
यहाँ ‘सूना सूना’ की पुनरावृत्ति हृदय की पीड़ा को और गहन बना देती है।
उपर्युक्त उदाहरण में करुण रस का अत्यन्त मार्मिक चित्रण हुआ है, जिससे पाठक उसमें डूब कर स्वयं ही उस रस की अनुभूति करने लगता है। यही इसका भाव सौन्दर्य है।
भाव-सौन्दर्य का प्रभाव तभी स्थायी होता है जब भाषा सहज, स्पष्ट और भावानुकूल हो, जिससे पाठक के मन में वही अनुभूति जागृत हो जो कवि ने अनुभव की थी।
भाव-सौन्दर्य के उदाहरण
(जहाँ मुख्य ज़ोर हृदय की गहन भावनाओं पर हो)
आँचल में छुपा लिया, जैसे तूफान से कोई दीप।
पलकें भीग रहीं थीं, पर मुस्कान रही अडिग अतीव।
आँखों में ममता का सागर, लहर-लहर उमड़ा आता।
हर स्पर्श में चुपचाप, एक संसार समा जाता।
ऐसे बेहाल बेवाइन सों, पग कंटक-जाल लगे पुनि जोए।
हाय, महादुख पायौ सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए।
देखि सुदामा की दीन दसा, करुना करिकै करुनानिधि रोए।
पानि परात को हाथ छुयौ नहिं, नैनन के जल सों पग धोए॥—नरोत्तमदास
बरगद की छाँव तले, थका पथिक सो जाता।
पत्तों की फुसफुसाहट में, बीते किस्से सुन जाता।
हवा सहलाती माथा, जैसे माँ थपकी देती हो।
मन भी अपनी थकान, पल में भूल जाता।
2. विचार-सौन्दर्य
कविता केवल भावनाओं का प्रवाह नहीं, बल्कि विचारों की गहराई भी है। विचार-सौन्दर्य तब उत्पन्न होता है जब कवि अपनी रचना में जीवन के सत्य, मानवीय मूल्यों और उच्च आदर्शों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। यह कविता को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन का माध्यम बना देता है।
जब कविता में विचारों की उच्चता और नैतिक मूल्यों का समावेश होता है, तो उसमें गरिमा उत्पन्न होती है। यह गरिमा कविता को प्रेरणादायक और स्थायी बना देती है।
- कबीर, रहीम, तुलसी और वृंद के नीतिपरक दोहे
- गिरधर की कुण्डलियाँ
इनमें जीवन की व्यावहारिक शिक्षा और प्रेरणा मिलती है।
आधुनिक कविताओं में भी विचार-सौन्दर्य के उदाहरण मिलते हैं—
- मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीयता और देश-प्रेम
- दिनकर की कविताओं में सत्य, अहिंसा और मानवीय मूल्य
- प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक गौरव
प्रगतिवादी कवि शोषितों की पीड़ा, अन्याय के विरोध और जनसाधारण के जीवन का यथार्थ चित्रण करके विचार-सौन्दर्य को सामाजिक दिशा देते हैं।
उदाहरण के लिए—
सत्कर्म ही जीवन का आभूषण,
धन-माना मिथ्या, सच्चा सज्जन॥
इन पंक्तियों में कवि ने सच्चे आभूषण को धन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सज्जनता बताया है।
कभी विचार-सौन्दर्य में सामाजिक सन्देश भी छिपा होता है—
बाँट खुशी तो दूनी हो जाती,
रख लो मन में दया की थाती॥
ऐसे विचार न केवल मन को छूते हैं, बल्कि व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं।
विचार-सौन्दर्य के लिए आवश्यक है कि संदेश स्पष्ट हो, परन्तु उपदेशात्मक बोझ न लगे; वह सहज भाव में ही पाठक के मन में उतर जाए।
विचार-सौन्दर्य के उदाहरण
(जहाँ गहरी सोच, दर्शन या जीवन की शिक्षा हो)
नदिया बहना सिखाती, ठोकर खाकर भी मुस्काना।
सूरज कहता हर सुबह, अँधियारे को है मिटाना।
फूल गिरकर भी महकते, सेवा करते चुपचाप।
जीवन का मर्म यही है, देना और निभाना आप।
बूँद-बूँद से भरता घड़ा, समय से ही फल आता।
जल्दी में तो सूरज भी, आधा ही ताप दिखाता।
धैर्य वो दीपक है, जो अँधियारा हर लेता।
जो रुककर चलता है, मंज़िल वो ही पाता।
काँटे राह में आते हैं, फूलों की कीमत बताने को।
अँधेरा घिरता है ताकि, चाँद आ सके जगमगाने को।
कठिनाई ही वो पाठशाला है, जो सिखाए चलना सच्चा।
संघर्ष ही है जीवन में, जीत का असली रास्ता।
3. नाद-सौन्दर्य
कविता में छन्द न केवल लय और गति का आधार है, बल्कि नाद-सौन्दर्य का भी प्रमुख स्रोत है। इसमें वर्ण, शब्द और तुक का ऐसा सुन्दर संयोजन होता है कि ध्वनि स्वयं कविता का अंग बनकर रसास्वादन कराती है। वर्णों के सार्थक और सुसंगठित विन्यास से कविता में संगीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, जिससे उसका सौन्दर्य बढ़ जाता है।
वर्णों की पुनरावृत्ति (अनुप्रास) और एक ही शब्द के विविध अर्थों का प्रयोग (यमक) नाद-सौन्दर्य को और प्रखर बनाते हैं। जैसे—
पिक-पिक पिक-पिक पुकारी बेली,
कुसुम कली मुसकानी खेली॥
यहाँ कोयल की पुकार और फूलों की मुस्कान, दोनों में नाद और दृश्य का अद्भुत सामंजस्य है।
मेघ-गर्जन और चपल बिजली की छवि को ध्वनि के माध्यम से व्यक्त किया गया है—
गगन गजर घन गहि-गहि घेरा,
चमक चपल चपला गगनेरा॥
इन पंक्तियों में ‘ग’, ‘घ’ और ‘च’ वर्णों की पुनरावृत्ति से ध्वनि-चित्र सजीव हो उठा है।
प्रकृति के मधुर प्रवाह का चित्रण भी इसी प्रकार संभव है—
छन छन छन छन झर झर झर झर,
बहे सलिल सरिता सुखभर॥
यहाँ जल-प्रवाह का निनाद शब्दों में प्रत्यक्ष हो रहा है।
तुकान्तता भी नाद-सौन्दर्य की एक महत्वपूर्ण विधि है, जैसे—
चमचम चमचम चंदा चाँदनी,
झमझम झमझम बरसे पानी॥
पदों की आवृत्ति भी ध्वनि को मधुर और प्रभावशाली बनाती है—
बोले रे पपीहा बोले, बोले रे पपीहा बोले,
सावन आए ना मोरे, सावन आए ना मोरे॥
इन सभी उदाहरणों में शब्द केवल अर्थ का संचार नहीं करते, बल्कि लय, ध्वनि और दृश्य तीनों को एक साथ गढ़कर कविता के सौन्दर्य को पूर्णता प्रदान करते हैं।
नाद-सौन्दर्य के उदाहरण
(जहाँ ध्वनि, लय, तुक और शब्द-संगीत मुख्य हो)
छन-छन छनके चूड़ियाँ, झन-झन बोले पायल।
टप-टप टपके फुहार, झर-झर झरता बादल।
घिर-घिर घन गरजें नभ में, चम-चम चमके बिजली।
झूम-झूम गाए मन, पावस लाए कजली।
दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झन झन
म्याँउ म्याँउ रे मोर, पीउ पिउ चातक के गन!
उड़ते सोनबलाक आर्द्र सुख से कर क्रंदन,
घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन।
(—पंत)
ठमक-ठमक पग धरे, नाचें मोर मयूर।
छनक-छनक घुँघरू बजे, छेड़े मन का सुरूर।
टप-टप रिमझिम बूँदें, झन-झन गूँजे छाजन।
धप-धप दिल भी बोले, आई सावन सावन।
4. अप्रस्तुत-योजना का सौन्दर्य
अप्रस्तुत-योजना (अर्थात अप्रत्यक्ष तुलना या रूपक) कविता में दृश्य, भाव या तथ्य को हृदयग्राही बनाने का सशक्त माध्यम है। इसमें कवि किसी उपमेय (जिसका वर्णन करना है) के लिए किसी उपमान (जिससे तुलना करनी है) का चुनाव करता है, जिसमें भाव या रूप का सादृश्य हो।
कविता में भावों को प्रभावी बनाने के लिए कवि अक्सर अप्रस्तुत-योजना या सादृश्य-विधान का प्रयोग करता है। इसमें कवि किसी वस्तु या भाव की तुलना किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से करता है, ताकि भाव की गहनता और प्रभाव स्पष्ट हो।
जैसे—
मुख तेरा जैसे पूर्णिमा का चाँद,
और नयन तेरे नभ के तारों समान॥
यहाँ नायक के मुख की तुलना पूर्णिमा के चाँद से और नेत्रों की तुलना तारों से की गई है।
प्रकृति से भी अप्रस्तुत-योजना के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं—
पत्ते जैसे ओस में भीगे,
वैसे ही मन तेरे प्रेम में भीगे॥
ऐसी उपमाएँ कविता में चित्रात्मकता, कोमलता और सौन्दर्य को बढ़ा देती हैं।
अप्रस्तुत-योजना में मुख्य ध्यान इस बात पर होता है कि तुलना स्वाभाविक लगे और वह पाठक के मन में तुरंत चित्र उकेर दे।
कवि अपने वर्णन को मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही बनाने के लिए अनेक कलात्मक साधनों का उपयोग करता है, जिनमें अप्रस्तुत-योजना (सादृश्य-विधान) विशेष महत्त्व रखती है। इसमें कवि किसी वस्तु, दृश्य, गुण या क्रिया की तुलना किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से करता है, जिससे वर्णन और अधिक जीवंत और प्रभावी बन जाता है।
अप्रस्तुत-योजना में यह आवश्यक है कि—
- सादृश्य स्पष्ट हो — उपमेय और उपमान के बीच रूप, धर्म या प्रभाव की समानता हो।
- भावानुकूलता बनी रहे — जिस वस्तु या क्रिया को लाया जा रहा है, वह मूल भाव के अनुकूल हो और उसे उभारने में सहायक हो।
कवि कभी रूप-साम्य, कभी धर्म-साम्य और कभी भाव-साम्य के आधार पर अप्रस्तुत-योजना का प्रयोग करता है। इसको सादृश्य के प्रकार कहते हैं, इनका विवरण नीचे दिया गया है:
सादृश्य के प्रकार—
(क) रूप-साम्य
जब दो वस्तुओं में आकार या रूप की समानता हो और उसी के आधार पर तुलना की जाए, तो यह रूप-साम्य कहलाता है।
जैसे —
नील कमल-से शीतल नयन,
अधरों पर जैसे चाँद का कण।
यहाँ नायक के नेत्रों की तुलना नीले कमल से और अधरों की तुलना चाँद के टुकड़े से की गई है, जिससे रूप की कोमलता और सौन्दर्य प्रकट होता है।
(ख) धर्म-साम्य
जब दो वस्तुओं के गुण, प्रवृत्ति या स्वभाव में समानता हो, तो यह धर्म-साम्य कहलाता है।
जैसे —
लहराती चूनर जैसे नभ में बिजुरी चमके,
दोनों ही मन में चंचलता और चकित कर जाएँ।
यहाँ चूनर की लहराहट और बिजुरी की चपल चमक — दोनों में गति और चकित करने का गुण समान है।
(ग) भाव-साम्य
जब दो वस्तुएँ या दृश्य एक जैसे भाव उत्पन्न करें, तो यह भाव-साम्य कहलाता है।
जैसे —
बिछड़ते मित्र को देखा तो लगा जैसे,
पतझड़ में वृक्ष अपना साया खो बैठा हो।
यहाँ वियोग का भाव मित्र के बिछड़ने और वृक्ष के छाया-रहित होने दोनों में समान रूप से व्यक्त हुआ है।
विशेष चित्रात्मक उदाहरण
कभी-कभी कवि अप्रस्तुत-योजना में ऐसा दृश्य खींचता है जो पाठक के मन में चित्र की तरह उभर आए।
जैसे —
पीले वस्त्रों में खड़ा प्रियतम, हरित कुंज के बीच,
जैसे अमलतास का फूल झूल रहा हो हरियाली में।
इसमें रंग-साम्य और सौन्दर्य-साम्य दोनों ही हैं, जो भाव को और प्रखर बना देते हैं। अप्रस्तुत-योजना का प्रयोग कविता के भाव को और अधिक जीवंत और प्रभावशाली बना देता है।
अप्रस्तुत-योजना के उदाहरण
यहाँ अप्रस्तुत-योजना के लिए एक कुछ उदाहरण प्रस्तुत है—
नभ में बिखरे मेघ जैसे, भीड़ उमड़ आई गाँव की।
बिजली-सी मुस्कान चमकी, छवि निखरी मनभावनी।
वर्षा की फुहार-सी बोली, हर मन को शीतल कर जाए।
मनो वसंत उतर आया हो, जीवन में खुशियाँ बरसाए।
यह चार पंक्तियाँ अप्रस्तुत-योजना (सादृश्य-विधान) का उदाहरण हैं, जहाँ कवि ने एक मानव-चित्रण को प्रकृति के दृश्यों के साथ जोड़ा है।
पंक्ति 1
“नभ में बिखरे मेघ जैसे, भीड़ उमड़ आई गाँव की।”
यहाँ भीड़ की तुलना आकाश में बिखरे मेघों से की गई है। रूप-साम्य है—जैसे मेघ आसमान में घिर आते हैं, वैसे ही गाँव में लोग चारों तरफ उमड़ आए हैं।
पंक्ति 2
“बिजली-सी मुस्कान चमकी, छवि निखरी मनभावनी।”
यहाँ मुस्कान की तुलना बिजली की चमक से की गई है। धर्म-साम्य है—दोनों अचानक प्रकट होते हैं और मन को आकर्षित करते हैं।
पंक्ति 3
“वर्षा की फुहार-सी बोली, हर मन को शीतल कर जाए।”
यहाँ बोली की मिठास और शीतलता को वर्षा की फुहार से जोड़ा गया है। प्रभाव-साम्य है—दोनों ही सुनने/महसूस करने वाले को ताजगी और सुकून देते हैं।
पंक्ति 4
“मनो वसंत उतर आया हो, जीवन में खुशियाँ बरसाए।”
यहाँ व्यक्ति की उपस्थिति को वसंत ऋतु से जोड़ा गया है। भाव-साम्य है—दोनों का आगमन वातावरण में उल्लास और ताजगी भर देता है।
उदाहरण — रूप-साम्य और धर्म-साम्य
खेत में फैला पीला सरसों, जैसे सोने का हो सागर।
हल्की-सी हवा में डोलें, मानो लहराए गजराज के कान।
सूरज की किरनें पड़ते ही, जगमग हो उठे हर एक दाना।
धरती मुस्काए मानो, पहन लिया हो स्वर्णिम गहना।
उदाहरण — भाव-साम्य और प्रभाव-साम्य
माँ का आंचल फैला जैसे, भोर का सुनहरा आकाश।
चिड़ियों की चहक-सी वाणी, देती मन को मधुर प्रकाश।
गोदी की ऊष्मा में खो जाए, जैसे सर्दी में धूप का आलिंगन।
उसकी ममता बरसती, जैसे सावन में झूम-झूम बरसात।
उदाहरण — मिश्रित साम्य
नदी की धार-सा निर्मल, उसका कोमल स्वभाव।
पर्वत-सा अडिग संकल्प, हर मुश्किल में रहे नवाभाव।
चाँदनी-सी शीतल वाणी, देती हर मन को आराम।
मानो प्रभात की पहली किरण, जग में बिखेर दे नया संदेश।
कविता के सौन्दर्य-तत्व ही उसे साधारण शब्दों के समूह से कला-कृति में परिवर्तित करते हैं। काव्य-भाषा की सजीवता, भावों की गहराई, विचारों की उच्चता, नाद का माधुर्य और अप्रस्तुत-योजना का कौशल—ये सभी मिलकर कविता को अमरत्व प्रदान करते हैं। एक श्रेष्ठ कवि इन तत्वों का संतुलित प्रयोग करके पाठक या श्रोता के हृदय में अमिट छाप छोड़ देता है।
काव्यास्वादन
कविता का वास्तविक आनन्द उसके अर्थ-ग्रहण में निहित होता है। कविता केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि भाव, रस और अलंकार का संगम है। अतः कविता का रसास्वादन करने के लिए पहले उसके मुख्य अर्थ को समझना आवश्यक है।
उदाहरण —
“मधुर मधुर मेरे दीपक जल” में केवल दीपक का जलना नहीं, बल्कि आशा, उजाला और जीवन के प्रतीकात्मक अर्थ भी निहित हैं।
मुख्यार्थ और अन्वय की आवश्यकता
कविता की वाक्य-संरचना प्रायः गद्य से भिन्न होती है। शब्दों का क्रम ऐसा हो सकता है कि अर्थ तुरंत स्पष्ट न हो।
ऐसी स्थिति में अन्वय (शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थ स्पष्ट करना) आवश्यक है।
अन्वय से—
- शब्दों का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट होता है।
- मुख्यार्थ के साथ-साथ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी उजागर होते हैं।
उदाहरण —
पंक्ति — “बरसत हरषि राम गृह आए”
अन्वय — “राम गृह आए, हरषि बरसत।”
अर्थ — “राम घर आए, तो आनंदवश आकाश भी जैसे बरसने लगा।”
विशेष शब्द-प्रयोग
कवि कई बार कविता में ऐसे शब्दों का साभिप्राय प्रयोग करता है—
- जिनके स्थान पर पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते।
- एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं और सभी प्रसंगानुकूल हो सकते हैं।
- एक ही शब्द अलग-अलग अर्थों में पुनः प्रयुक्त हो सकता है।
- विरोधी शब्दों का प्रयोग भाव-वृद्धि के लिए किया जाता है।
- एक ही प्रसंग में कई विशेष शब्द एक साथ प्रयुक्त हो सकते हैं।
ऐसे शब्दों की ओर विशेष ध्यान देकर ही अपेक्षित अर्थ समझा जा सकता है।
उदाहरण —
“साँझ सकाले दीप जले” — यहाँ “साँझ” और “सकाले” जैसे विरोधी समय-सूचक शब्द एक साथ आकर सौन्दर्य बढ़ाते हैं।
“साँझ” और “सकाले” समय-सूचक शब्द हैं।
- साँझ → शाम का समय, सूर्यास्त के बाद का समय।
- सकाले → सुबह का समय, सूर्योदय के आसपास का समय।
जब कवि दोनों को एक साथ प्रयोग करता है, तो यह सामान्य समय-क्रम के विपरीत होने के कारण विशेष सौन्दर्य पैदा करता है। यहाँ दीपक के जलने की बात केवल रात के अंधकार को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि प्रकाश, आशा और जीवन का उजाला सुबह-शाम हर समय बना रहना चाहिए।
काव्यास्वादन की प्रक्रिया
कविता के जिन तत्वों—रस, अलंकार, गुण और छन्द—का उल्लेख किया गया है, उनके संदर्भ में कविता का आस्वादन करना चाहिए।
इसके लिए—
- कविता के मूलभाव को समझकर उसे अपने शब्दों में लिखना।
- रस, अलंकार, गुण और छन्द आदि को पहचानकर उनकी उपयोगिता समझना।
- अच्छे भाव वाले पदों को कण्ठस्थ करना।
- कविता को बार-बार सस्वर (उच्चारण के साथ) पढ़ना, ताकि उसका भाव, लय और सौन्दर्य पूरी तरह हृदयंगम हो सके।
विशेष शब्द प्रयोग और उनका सौन्दर्य
कवि अपने भावों को सजीव करने के लिए ऐसे शब्दों का चयन करता है, जो अर्थ, ध्वनि और भाव तीनों स्तरों पर प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार वह विपरीतार्थक, बहुअर्थी या भाव-प्रधान शब्दों का संयोजन करता है, जिससे कविता में गहराई और संगीतात्मकता आती है।
1. विपरीत समयों का प्रयोग — “साँझ” और “सकाले”
“साँझ सकाले दीप जले”
यहाँ दीप का जलना केवल रोशनी देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह सतत जागरूकता, आशा और जीवन-प्रकाश का प्रतीक है, जो दिन-रात हर समय बना रहे।
2. बहुअर्थी शब्द — “चाँद”
“उसके मुख पर चाँद मुस्काया”
यहाँ “चाँद” का प्रयोग न केवल आकाश के चंद्रमा के रूप में है, बल्कि प्रिय के मुखमंडल के रूप की उपमा भी देता है, जिससे प्रेम और सौंदर्य का संयुक्त बोध होता है।
3. भाववृद्धि हेतु विरोधी शब्द — “अंधियारा” और “उजियारा”
“अंधियारा घटा, उजियारा बढ़ा”
इन विरोधी शब्दों का प्रयोग केवल रोशनी और अंधकार के भौतिक अर्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अज्ञान से ज्ञान, निराशा से आशा की ओर बढ़ने का संदेश देता है।
4. समान ध्वनि से नाद-सौन्दर्य — “कूल” और “कुंज”
“कूल-कुंज सब हुलस उठे”
यहाँ “कूल” (नदी का किनारा) और “कुंज” (वृक्षों का झुरमुट) की ध्वन्यात्मक समानता, कविता में मधुरता और नाद-सौन्दर्य का निर्माण करती है, साथ ही प्रकृति के हर्षोल्लास का दृश्य भी साकार करती है।
काव्य के भेद
काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं—श्रव्य-काव्य और दृश्य-काव्य।
1. श्रव्य-काव्य
वह काव्य जो कानों से सुना जाता है, श्रव्य-काव्य कहलाता है। इसके दो उप-भेद हैं—
- प्रबन्ध-काव्य
- मुक्तक-काव्य
1.1 प्रबन्ध-काव्य
प्रबन्ध-काव्य के अन्तर्गत महाकाव्य, खण्डकाव्य तथा आख्यानक गीतियाँ आती हैं।
(क) महाकाव्य
प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य के लक्षण—
- जीवन का व्यापक चित्रण।
- कथा इतिहास-प्रसिद्ध।
- नायक उदात्त एवं महान् चरित्र वाला।
- वीर, शृंगार या शान्तरस में से कोई एक रस प्रधान, शेष गौण।
- सर्गबद्ध संरचना (कम से कम 8 सर्ग)।
- धारावाहिकता एवं मार्मिक प्रसंगों का समावेश।
आधुनिक परिवर्तन — अब विषय के रूप में किसी भी युग की घटना या समस्या आ सकती है, नायक समाज का कोई भी विशेष क्षमताओं वाला व्यक्ति हो सकता है।
उदाहरण —
- संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं— रामायण, महाभारत।
- हिन्दी के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं— पृथ्वीराज रासो (हिंदी का प्रथम महाकाव्य), रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन आदि।
(ख) खण्डकाव्य
- नायक के जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण।
- महाकाव्य का संक्षिप्त रूप नहीं, बल्कि पूर्ण रचना।
- पूरे खण्डकाव्य में एक ही छन्द का प्रयोग।
उदाहरण — पंचवटी, जयद्रथ-वध, नहुष, सुदामा-चरित, पथिक, गंगावतरण, हल्दीघाटी, जय हनुमान।
(ग) आख्यानक गीतियाँ
- पद्यबद्ध कहानी का रूप।
- वीरता, पराक्रम, प्रेम, करुणा आदि का चित्रण।
- भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक।
- गीतात्मकता और नाटकीयता इसकी विशेषताएँ।
उदाहरण — झाँसी की रानी, रंग में भंग, विकट भद।
1.2 मुक्तक-काव्य
महाकाव्य या खण्डकाव्य से भिन्न, इसमें एक भाव, अनुभूति या कल्पना का स्वतंत्र चित्रण होता है।
- प्रत्येक छन्द स्वतन्त्र होता है।
- वर्ण्य-विषय अपने में पूर्ण होता है।
उदाहरण — कबीर, बिहारी, रहीम के दोहे, सूर और मीरा के पद।
इसके दो उपभेद होते हैं – पाठ्य-मुक्तक और गेय-मुक्तक।
(क) पाठ्य-मुक्तक
- विषय की प्रधानता।
- किसी प्रसंग, विचार या रीति का चित्रण।
उदाहरण — कबीर, तुलसी, रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे, बिहारी, मतिराम, देव की रचनाएँ।
पाठ्य-मुक्तक का एक उदाहरण—
धन से बड़ा है ज्ञान, इसे जितना बाँटो उतना बढ़ता है।
सत्य से ऊँचा मान, जो निभाए वही सदा चढ़ता है।
लोभ छोड़ कर प्रेम अपनाओ, यही है जीवन का सार।
जो मन को जीते वही सच्चा, वही है जग में सरदार।
कारण कि यह पाठ्य-मुक्तक है —
- इसमें विषय-प्रधानता है (ज्ञान, सत्य और प्रेम का महत्व)।
- भाव के साथ-साथ विचार और शिक्षा पर जोर है।
- प्रत्येक पंक्ति स्वतंत्र भाव देती है, पर मिलकर एक ही प्रसंग (जीवन-सत्य) को चित्रित करती है।
(ख) गेय-मुक्तक
- गीतिकाव्य या प्रगीति के रूप में जाना जाता है।
- भावप्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौन्दर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता और संगीतात्मकता की प्रधानता।
- अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी।
गेय-मुक्तक का एक उदाहरण प्रस्तुत है—
चाँद की चाँदनी बिखरे नभ में,
सपनों सा आलोक उतर आया।
मन के आँगन महके फूलों सा,
प्रेम का दीप फिर से जगमगाया।
यह उदाहरण गेय-मुक्तक है क्योंकि—
- इसमें भावप्रवणता (प्रेम और सौन्दर्य का चित्रण) है।
- संगीतात्मकता है (लय और ध्वनि में माधुर्य)।
- संक्षिप्तता है (चार पंक्तियों में पूर्ण भाव)।
- आत्माभिव्यक्ति और सौन्दर्यमयी कल्पना है।
2. दृश्य-काव्य
वह काव्य जो अभिनय के माध्यम से देखा और सुना जाता है, दृश्य-काव्य कहलाता है। इसका प्रमुख उदाहरण नाटक है।
दृश्य-काव्य के उदाहरण
- अभिज्ञानशाकुन्तलम् – महाकवि कालिदास (संस्कृत नाटक)
- मृच्छकटिकम् – शूद्रक (संस्कृत नाटक)
- मालती-माधव – भवभूति (संस्कृत नाटक)
- अंधेर नगरी – भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (हिन्दी नाटक)
- भारत दुर्दशा – भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (हिन्दी नाटक)
- संगीत रघुनाथ – जयशंकर प्रसाद (हिन्दी नाटिका)
- चन्द्रगुप्त – जयशंकर प्रसाद (हिन्दी ऐतिहासिक नाटक)
हिन्दी पद्य साहित्य का इतिहास
हिन्दी पद्य साहित्य का विकास कई शताब्दियों में क्रमशः हुआ है। विद्वानों ने इसे मुख्यतः चार कालखंडों में विभाजित किया है। यह विभाजन प्रत्येक युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों, काव्य-रूपों और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। प्रत्येक काल का अपना विशिष्ट साहित्यिक रूप, भाषा-शैली और प्रमुख कवि रहे हैं।
- आदिकाल (वीरगाथा काल) – 1000 ई. से 1350 ई. तक (विक्रम संवत् 1057 से 1407 तक)
- भक्ति काल (पूर्व मध्यकाल) – 1350 ई. से 1650 ई. तक (विक्रम संवत् 1407 से 1707 तक)
- रीति काल (उत्तर मध्यकाल) – 1650 ई. से 1850 ई. तक (विक्रम संवत् 1707 से 1907 तक)
- आधुनिक काल (गद्यकाल) – 1850 ई. से वर्तमान काल तक (विक्रम संवत् 1907 से अब तक)
1. आदिकाल (वीरगाथा काल)
अवधि: 1000 ई. से 1350 ई. तक (विक्रम संवत् 1057 से 1407 तक)
मुख्य प्रवृत्ति: वीर रस की प्रधानता, युद्ध-गाथाओं और शौर्य-कथाओं का वर्णन।
इस काल में साहित्य का उद्देश्य शौर्य, पराक्रम, देशभक्ति और जातीय गौरव का प्रचार करना था। अधिकांश रचनाएँ राजाओं, योद्धाओं और वीरांगनाओं के यशगान पर आधारित थीं।
भाषा: प्रारंभिक अपभ्रंश, ब्रजभाषा और राजस्थानी का मिश्रण।
मुख्य कवि एवं रचनाएँ: चंदबरदाई (पृथ्वीराज रासो), जैन कवि, तथा अन्य चारण-कवि।
2. भक्ति काल (पूर्व मध्यकाल)
अवधि: 1350 ई. से 1650 ई. तक (विक्रम संवत् 1407 से 1707 तक)
मुख्य प्रवृत्ति: भक्ति-भावना और ईश्वर-प्रेम की अभिव्यक्ति।
इस काल में साहित्य धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं से परिपूर्ण रहा। यह काल आगे दो प्रमुख धाराओं में विभाजित है—
- निर्गुण भक्ति धारा – जिसमें ईश्वर को निराकार, निर्गुण और निरंजन माना गया। प्रमुख कवि: कबीर, दादू, रैदास, गुरुनानक आदि।
- सगुण भक्ति धारा – जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूज्य माना गया। यह धारा आगे दो रूपों में बंटी—
- रामभक्ति शाखा – तुलसीदास (रामचरितमानस) आदि।
- कृष्णभक्ति शाखा – सूरदास, मीरा, नंददास आदि।
3. रीति काल (उत्तर मध्यकाल)
अवधि: 1650 ई. से 1850 ई. तक (विक्रम संवत् 1707 से 1907 तक)
मुख्य प्रवृत्ति: शृंगार रस की प्रधानता, काव्यशास्त्रीय नियमों का पालन।
इस काल में साहित्य दरबारी वातावरण में पनपा और सौन्दर्य, प्रेम, श्रृंगार, नायक-नायिका के वर्णन, तथा अलंकारों के प्रयोग पर बल दिया गया।
भाषा: ब्रजभाषा का अत्यधिक प्रचलन।
मुख्य कवि एवं रचनाएँ: बिहारी (बिहारी सतसई), केशवदास, भूषण, पद्माकर, घनानंद आदि।
4. आधुनिक काल (गद्यकाल)
अवधि: 1850 ई. से वर्तमान काल तक (विक्रम संवत् 1907 से अब तक)
मुख्य प्रवृत्ति: राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार, यथार्थवाद और व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति।
इस काल में हिन्दी साहित्य में गद्य का विकास हुआ और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से नई विचारधाराओं का प्रसार हुआ। यह काल आगे तीन प्रमुख प्रवृत्तियों में विभाजित है—
- भारतेन्दु युग – भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और नवजागरण।
- द्विवेदी युग – महावीरप्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में भाषा-शुद्धि, छन्दबद्धता और आदर्शवाद।
- छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता – जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, नागार्जुन, अज्ञेय आदि।
हिन्दी पद्य साहित्य के चारों कालों की संक्षिप्त सारणी —
| काल | अवधि (ईस्वी) | अवधि (वि. संवत्) | मुख्य प्रवृत्ति | प्रमुख कवि/रचनाएँ | प्रतिनिधि पंक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| आदिकाल (वीरगाथा काल) | 1000 – 1350 | 1057 – 1407 | वीर रस, युद्ध-गाथा, शौर्य-गान | चंदबरदाई (पृथ्वीराज रासो), जैन कवि, चारण-कवि | ढाल, तलवार, भाले बरसे, रण में बाजी बाज। वीर पुकारत धाय चले, छिन्न भुजंग समान॥ |
| भक्ति काल (पूर्व मध्यकाल) | 1350 – 1650 | 1407 – 1707 | भक्ति भावना, ईश्वर प्रेम, निर्गुण व सगुण काव्य | कबीर, तुलसीदास (रामचरितमानस), सूरदास, मीरा | मन तजहुँ तजाइ देहि, हरि बिनु और न कोई। तुलसी ऐसे हरि भजै, जैसे जल में कोई॥ |
| रीति काल (उत्तर मध्यकाल) | 1650 – 1850 | 1707 – 1907 | शृंगार रस, अलंकार प्रधान काव्य | बिहारी (बिहारी सतसई), केशवदास, भूषण | नैन सनेह पगे, कचनो करत अघाय। हिय हिय मोरि रघुनन्दन, तिहिं परत न पाय॥ |
| आधुनिक काल (गद्यकाल) | 1850 – अब तक | 1907 – अब तक | राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार, यथार्थवाद, व्यक्तिगत भाव | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, निराला | वंदे मातरम्! जय भारत, जय जय जननी, तेरी सन्तानें जागीं, कर लें जग में ध्वनि॥ |
कविता की विशेषताएँ
परिभाषा
कविता वह रचना है जिसमें भाव, कल्पना, और लय का सुंदर समन्वय होता है। इसे एक रेखा, वाक्यांश, या वाक्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो काव्य के गुण या लय के साथ जुड़ा हो।
पद्य को कविता का स्वर-समूह माना जा सकता है, जो एक संपूर्ण छंद भी हो सकता है। ‘कविता’ शब्द का प्रयोग किसी रचना के अंश या पूर्ण रूप, दोनों के लिए होता है।
- भाव और लय का समन्वय – कविता में भाव, कल्पना और लय का सुंदर मेल होता है।
- अनुभूति की अभिव्यक्ति – कवि अपने अनुभवों और भावनाओं को कलात्मक रूप से व्यक्त करता है।
- रसदशा – हृदय की मुक्त अवस्था, जिसमें कविता रस उत्पन्न करती है।
- भावयोग – कविता भावनाओं की साधना है, जो कर्मयोग और ज्ञानयोग के समान महत्त्वपूर्ण है।
- रचनात्मक स्वतंत्रता – कविता संवादात्मक न होकर विशुद्ध कलात्मक होती है।
- विविध विधाएँ – गीत, ग़ज़ल, दोहा, भजन आदि प्रमुख रूप हैं।
काव्य का स्वरूप
कविता का मूल स्वरूप ऐसा होता है जो केवल संवादात्मक या अभियोगात्मक व्याख्या न होकर, भावों की स्वतंत्र और कलात्मक अभिव्यक्ति हो। जब कवि अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से मुक्त होकर, विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त-हृदय अवस्था को प्राप्त करता है।
रस और भावयोग
हृदय की यह मुक्तावस्था ही रसदशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा होती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्ति रस के रूप में प्रकट होती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे ही कविता कहा जाता है। यह साधना भावयोग है, जिसे कर्मयोग और ज्ञानयोग के समकक्ष माना गया है।
प्रमुख विधाएँ
कविता की अनेक विधाएँ हैं—
- गीत – जीवन के अनुभवों को लयात्मक रूप में व्यक्त करना।
- ग़ज़ल – विशेषतः उर्दू साहित्य में लोकप्रिय, जिसमें शेरों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है।
- दोहा – दो पंक्तियों का छंद, जिसमें प्रत्येक पंक्ति (चरण) निश्चित मात्रा का होता है।
- भजन – ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाला काव्य।
कविता कैसे लिखें?
कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों का मार्मिक स्वरूप दिखाई देता है और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस अवस्था में मनुष्य कुछ समय के लिए स्वयं को भूलकर अपनी सत्ता को लोक-सत्ता में लीन कर देता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति बन जाती है।
कविता-लेखन के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार होता है और सम्पूर्ण सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक संबंध सुरक्षित और सुदृढ़ रहता है।
भावों का सामंजस्य
जगत अनेक रूपों से युक्त है और हमारा हृदय अनेक भावों से। कविता का उद्देश्य इन भावों का सामंजस्य जगत के विभिन्न रूपों, व्यापारों और तथ्यों के साथ स्थापित करना है। इन्हीं भावों के माध्यम से मानव-जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव प्राचीन काल से करती आई है।
मूल रूप और व्यापार
जिन प्राकृतिक रूपों और मानवीय क्रियाओं से मनुष्य आदि काल से परिचित है, वे कविता के मूल स्रोत हैं। इन्हें हम मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। कविता में गहराई और रस उत्पन्न करने के लिए इन्हीं मूल रूपों और व्यापारों का सहारा लिया जाता है।
मूल रूपों के उदाहरण – वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, चट्टान, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र आदि।
मूल व्यापारों के उदाहरण – पानी का बहना, पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, मेघ का बरसना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, किसी को बचाना, आग में झोंकना आदि।
इन प्राकृतिक रूपों और प्राचीन मानवीय क्रियाओं में भावों को जागृत करने की गहरी शक्ति होती है, क्योंकि इनमें वंशानुगत वासनाओं और अनुभवों की दीर्घ परंपरा निहित है। इसके विपरीत, कारखानों, इंजनों, विमानों, चेक, दस्तावेज़ों जैसी आधुनिक वस्तुओं और क्रियाओं में वह सहज रसोत्पादकता नहीं होती जो मूल रूपों और व्यापारों में पाई जाती है।
कविता लेखन के चरणबद्ध सुझाव
- भावनाओं का चयन करें
- पहले यह तय करें कि आपकी कविता का मुख्य भाव क्या होगा — प्रेम, करुणा, वीरता, प्रकृति, दर्शन या कोई सामाजिक संदेश।
- भाव स्पष्ट होने से कविता में एकता बनी रहती है।
- विषय से जुड़ाव बनाएं
- कविता का विषय केवल देखा-सुना न हो, बल्कि अनुभव किया गया हो।
- अपने जीवन, परिवेश और स्मृतियों से सामग्री लें।
- मूल रूप और व्यापार अपनाएँ
- प्राकृतिक और मानवीय मूल प्रतीकों का प्रयोग करें, जैसे — नदी, चाँद, बारिश, पक्षी, दीपक, खिलना-मुरझाना आदि।
- ये तत्व पाठक में सहज भाव-जागरण करते हैं।
- भाषा और लय
- भाषा सरल, भावपूर्ण और चित्रात्मक होनी चाहिए।
- छंद (मीटर) का पालन करें या मुक्तछंद अपनाएँ, लेकिन लय अवश्य रखें।
- चित्रात्मकता और प्रतीक
- शब्दों के माध्यम से ऐसा चित्र बनाएं कि पाठक दृश्य को महसूस कर सके।
- प्रतीकों और रूपकों से भावों की गहराई बढ़ाएँ।
- संक्षिप्तता और प्रभाव
- कविता में अनावश्यक शब्द न जोड़ें।
- हर पंक्ति भाव और अर्थ को आगे बढ़ाए।
- पुनर्लेखन और परिष्कार
- पहली बार लिखने के बाद कविता को दोबारा पढ़ें, अनावश्यक शब्द हटा दें, भाव स्पष्ट करें।
- लय और ध्वनि-सौंदर्य की जाँच करें।
उदाहरण 1 – प्रकृति-आधारित कविता (भाव: शांति और सौंदर्य)
नीले नभ में तैर रही,
सफेद-सी रुई की नाव,
पवन की कोमल बाहों में,
सोता है मेरा गाँव।
उदाहरण 2 – सामाजिक संदेश वाली कविता (भाव: जागरूकता)
अंधियारे को कोसने से,
कुछ भी नहीं बदलता,
एक दीया जला कर देखो,
कैसे जगमग पल भर चलता।
उदाहरण 3 – भावुक/व्यक्तिगत कविता (भाव: विरह)
तेरे बिना सूना है आँगन,
सूने हैं सब फूल,
तेरी यादें जैसे सावन,
बरसें धूप के मूल।
कविता का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व
कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज का दर्पण भी है। यह एक ओर जहाँ व्यक्ति के आंतरिक भावों को व्यक्त करती है, वहीं दूसरी ओर समाज की समस्याओं, संघर्षों और आकांक्षाओं को भी सामने लाती है।
इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय कविता ने जनता में जोश भरने का कार्य किया। मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्राकुमारी चौहान जैसे कवियों की रचनाएँ आज भी प्रेरणा देती हैं।
सांस्कृतिक दृष्टि से कविता भाषा को समृद्ध करती है और साहित्य में नए प्रयोगों को जन्म देती है।
आधुनिक कविता
आधुनिक युग में कविता के विषय, शैली और भाषा में काफी परिवर्तन आया है। अब यह केवल छंद और तुकांत तक सीमित नहीं, बल्कि मुक्तछंद और प्रयोगवाद जैसी शैलियों में भी लिखी जा रही है। आधुनिक कवि अपने समय की विडंबनाओं, राजनीतिक संघर्षों और व्यक्तिगत अनुभवों को भी बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं।
निष्कर्ष
कविता भावनाओं का सजीव चित्रण है, जो मनुष्य को उसकी संवेदनाओं, कल्पनाओं और विचारों से जोड़ती है। यह एक ऐसी कला है जिसमें भाषा, संगीत, चित्रात्मकता और भावनाएँ मिलकर सौंदर्य का अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं।
कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से समृद्ध करना, समाज को दिशा देना और जीवन के हर पक्ष को संवेदनाओं के रंग में रंगना है।
इन्हें भी देखें –
- आत्मकथा – अर्थ, विशेषताएँ, भेद, अंतर और उदाहरण
- जीवनी – परिभाषा, स्वरूप, भेद, साहित्यिक महत्व और उदाहरण
- संस्मरण – अर्थ, परिभाषा, विकास, विशेषताएँ एवं हिंदी साहित्य में योगदान
- हिंदी साहित्य में रेखाचित्र : साहित्य में शब्दों से बनी तस्वीरें
- पद्म सिंह शर्मा कृत ‘पद्म-पराग’ : रेखाचित्र अथवा संस्मरण?
- हिन्दी के यात्रा-वृत्त और यात्रा-वृत्तान्तकार – लेखक और रचनाएँ
- यात्रा-वृत्त : परिभाषा, इतिहास, विशेषताएँ और विकास
- हिंदी डायरी साहित्य और लेखक
- रिपोर्ताज – अर्थ, स्वरूप, शैली, इतिहास और उदाहरण
- आलोचना : स्वरूप, अर्थ, व्युत्पत्ति, परिभाषा, प्रकार, विकास और उदाहरण
- आलोचना और आलोचक | हिन्दी में आलोचना का स्वरूप एवं विशेषताएँ