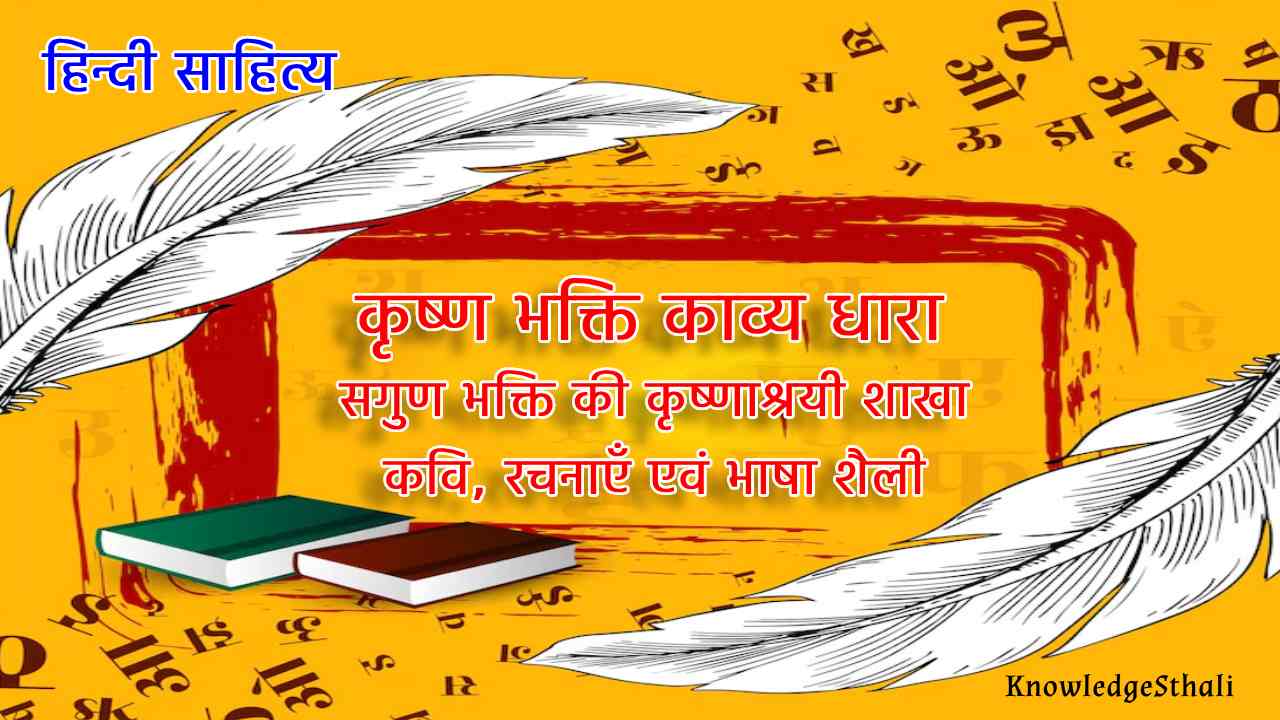यह विस्तृत हिंदी लेख कृष्ण भक्ति काव्यधारा या कृष्णाश्रयी शाखा की समृद्ध परंपरा, दर्शन, प्रमुख कवियों, रचनाओं और उनकी काव्यगत विशेषताओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की इस प्रमुख शाखा में श्रीकृष्ण को ईश्वर, प्रेमी, मित्र, बालक और नायक के विविध रूपों में चित्रित किया गया है। लेख में वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग, अष्टछाप के आठ प्रमुख कवियों (सूरदास, कुंभनदास, नंददास आदि), संप्रदाय-निरपेक्ष भक्त कवियों (मीरा बाई, रसखान), एवं अन्य संप्रदायों जैसे निम्बार्क, राधावल्लभ, हरिदासी और गौड़ीय संप्रदाय के योगदान का सुंदर संयोजन किया गया है।
इस लेख में कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विधाओं – बाल लीला, वात्सल्य रस, श्रृंगारिक प्रेम, नारी मुक्ति, लोकभाषा ब्रज का सौंदर्य, तथा भ्रमरगीत परंपरा जैसे विषयों को क्रमबद्ध और सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। सूरदास, रसखान, मीरा, नरोत्तमदास आदि कवियों की जीवनी, उनकी प्रमुख रचनाएँ, भाव-विशेषताएँ और साहित्यिक योगदान का सूक्ष्म विवेचन इसमें सम्मिलित है।
यह लेख हिंदी साहित्य, विशेष रूप से भक्तिकाल के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकगण, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और भक्ति रस के प्रेमियों के लिए एक संदर्भग्रंथ के समान है। यह केवल एक साहित्यिक लेख नहीं, बल्कि कृष्ण भक्ति परंपरा की जीवंत सांस्कृतिक यात्रा का दर्शन है।
प्रस्तावना
भारतीय भक्ति आंदोलन में दो प्रमुख धाराओं की पहचान होती है – रामभक्ति और कृष्णभक्ति। इनमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श के रूप में तथा कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम और प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा गया। इस लेख में हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा (या कृष्णाश्रयी शाखा) का विस्तृत विवेचन करेंगे – इसमें सम्मिलित प्रमुख संप्रदाय, उनके कवि, रचनाएँ, दार्शनिक दृष्टिकोण, साहित्यिक विशेषताएँ और इस काव्यधारा का सामाजिक योगदान।
कृष्ण भक्ति काव्यधारा (कृष्णाश्रयी शाखा) की परिभाषा और उद्भव
कृष्ण भक्ति काव्यधारा उन भक्त कवियों की साहित्यिक परंपरा है जिन्होंने विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण को आराध्य मानकर अपनी कविताओं में उनके विविध रूपों – बालरूप, रासलीला, गोपियों के प्रति माधुर्य प्रेम, वात्सल्य भाव, और लीलामयी छवियों का चित्रण किया। यह धारा विशेष रूप से उत्तर भारत में, विशेषतः ब्रजभूमि में, मध्यकालीन भारत (15वीं से 17वीं शताब्दी) के दौरान पल्लवित हुई।
भक्ति आंदोलन और कृष्ण की लोकप्रियता
मध्यकाल में जब भारतीय समाज जातिवाद, बाह्याचार और धार्मिक आडंबरों से घिरा हुआ था, तब भक्ति आंदोलन एक जनांदोलन के रूप में उभरा। इस आंदोलन में भक्त कवियों ने ईश्वर की व्यक्तिगत अनुभूति, प्रेम, सेवा और समर्पण को भक्ति का मार्ग बताया।
कृष्ण, एक ऐसे आराध्य बने जो:
- बालक के रूप में वात्सल्य का प्रतीक बने,
- रासलीला में प्रेम का माधुर्य दिखाते हैं,
- भगवद्गीता में ज्ञान और कर्मयोग का मार्ग बताते हैं।
इसलिए कृष्ण का व्यक्तित्व भक्तों के विविध भावों के लिए उपयुक्त माध्यम बन गया – सखा, बालक, प्रेमी, मार्गदर्शक और परमात्मा।
ब्रज क्षेत्र और कृष्ण काव्यधारा (कृष्णाश्रयी शाखा)
ब्रजमंडल, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना आदि क्षेत्र है, कृष्ण की लीलाओं की पृष्ठभूमि माना जाता है। यहाँ कृष्ण भक्ति का संचार लोकधर्म और संस्कृति के गहरे भावों के साथ हुआ। इसी क्षेत्र से कृष्ण भक्ति काव्यधारा का सूत्रपात हुआ और ब्रजभाषा इस काव्य की प्रमुख अभिव्यक्ति भाषा बनी।
प्रमुख कृष्ण भक्ति संप्रदाय (कृष्णाश्रयी शाखा) और उनके कवि
कृष्ण काव्यधारा में अनेक संप्रदाय सक्रिय रहे। प्रत्येक संप्रदाय का अपना दार्शनिक दृष्टिकोण, भक्ति मार्ग और काव्य-संस्कार रहा। इन संप्रदायों के अंतर्गत ऐसे अनेक भक्त कवि हुए जिन्होंने साहित्य को समृद्ध किया।
1. वल्लभ संप्रदाय (पुष्टि मार्ग)
- संस्थापक: महाप्रभु वल्लभाचार्य (1479–1531)
- दर्शन: शुद्धाद्वैत
- भक्ति मार्ग: पुष्टि मार्ग (समर्पण और अनुग्रह पर आधारित)
- आधार ग्रंथ: श्रीमद्भागवत
वल्लभाचार्य ने कृष्ण को संपूर्ण ब्रह्म का स्वरूप माना और ‘लीला’ को भक्ति का सर्वोच्च रूप बताया। वे भक्ति को ईश्वर की ‘पुष्टि’ (अनुग्रह) का परिणाम मानते थे।
अष्टछाप के कवि:
वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ (विट्ठलनाथजी) ने मिलकर आठ कवियों को दीक्षित किया जिन्हें “अष्टछाप” कहा गया:
वल्लभाचार्य द्वारा दीक्षित:
- सूरदास – वात्सल्य और श्रृंगार के कवि; “अष्टछाप का जहाज”
- कुंभनदास – माधुर्य भाव के संयमी कवि
- परमानंददास – मधुर श्रृंगार के पोषक
- कृष्णदास – भक्ति रस के प्रमुख गायक
विट्ठलनाथ द्वारा दीक्षित:
5. छीत स्वामी
6. गोविंद स्वामी
7. चतुर्भुजदास
8. नंददास – सूरदास के बाद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कवि
इन कवियों ने गायन-परंपरा के माध्यम से कृष्ण-लीला को लोकवाणी में रच दिया। सूरदास के काव्य से ब्रजभाषा को अद्वितीय साहित्यिक ऊँचाई मिली।
2. निंबार्क संप्रदाय
- संस्थापक: निम्बार्काचार्य
- दर्शन: द्वैताद्वैत
- कृष्ण-राधा को एकमेक प्रेम रूप माना गया
प्रमुख कवि:
- श्री भट्ट
- हरिव्यास देव – राधा-कृष्ण के सखा भाव का चित्रण
3. राधावल्लभ संप्रदाय
- संस्थापक: हित हरिवंश
- विशेषता: राधा को कृष्ण से श्रेष्ठ मानना
- भक्ति मार्ग: निष्कलुष राधा-भक्ति
प्रमुख कवि:
- हित हरिवंश – राधा के प्रति पूर्ण समर्पण और माधुर्य भाव की प्रधानता
4. हरिदासी संप्रदाय (सखी संप्रदाय)
- संस्थापक: स्वामी हरिदास
- विशेषता: कृष्ण की उपासना को राधा के दृष्टिकोण से देखना
प्रमुख कवि:
- स्वामी हरिदास – स्वयं को गोपी के रूप में मानकर भक्ति करना
5. चैतन्य संप्रदाय (गौड़ीय संप्रदाय)
- संस्थापक: चैतन्य महाप्रभु (बंगाल)
- दर्शन: अचिन्त्य भेदाभेद
- भक्ति मार्ग: संकीर्तन
प्रमुख कवि:
- गदाधर भट्ट – राधा-कृष्ण की संकीर्तन भक्ति के उपासक
6. संप्रदाय निरपेक्ष कवि
कुछ कृष्ण भक्त कवि किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े, परंतु उनका काव्य अत्यंत प्रभावशाली रहा।
मीरा बाई – राजपूत कुल की संत कवियित्री
- विषम सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद राणा साँगा जैसे सामंती व्यवस्था के विरोध में अपनी स्वायत्तता बनाए रखी।
- “मैं तो सांवरे के रंग रांची” जैसे पदों में प्रेम और विद्रोह दोनों को अभिव्यक्त किया।
- मीरा का काव्य स्त्री विमर्श और नारी मुक्ति का पहला स्वर था।
रसखान – मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के अनन्य भक्त
- ब्रजभूमि, यमुना तट, गोपियों और बालकृष्ण की बाल लीलाओं का मोहक चित्रण
- “मानुष हौं तो वही रसखान…” जैसे पदों में आत्मा की करुणा और समर्पण दृष्टिगत होती है
कृष्ण भक्ति काव्य की साहित्यिक विशेषताएँ
कृष्ण भक्ति काव्यधारा केवल धार्मिक या भक्ति रस में सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें गहन साहित्यिकता, मनोवैज्ञानिक गहराई, सांस्कृतिक चित्रण और सामाजिक व्याख्या भी मिलती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण
कृष्ण को अवतारी पुरुष नहीं, पूर्ण ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया। वे अचिंत्य, अलौकिक और सर्वव्यापक हैं।
2. बाल लीला और वात्सल्य भाव
- कृष्ण की बाल लीलाएँ – माखन चोरी, यशोदा के साथ वात्सल्य, ग्वालबालों के संग क्रीड़ा
- सूरदास ने वात्सल्य रस की जो अनुभूति दी, वह वैश्विक काव्यधारा में अद्वितीय मानी जाती है।
3. श्रृंगारिक माधुर्य
- राधा-कृष्ण के प्रेम में श्रृंगार रस की कोमलता, विरह और संयोग की अनुभूतियाँ प्रकट होती हैं
- गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेमाभक्ति माधुर्य भाव का श्रेष्ठ उदाहरण है
4. नारी मुक्ति का स्वर
- कृष्ण भक्ति काव्यधारा वह एकमात्र शाखा रही जिसमें नारी विमर्श की स्पष्ट चेतना मिलती है
- मीरा बाई इसका सशक्त उदाहरण हैं जिन्होंने परंपराओं की अवहेलना कर कृष्ण को पति माना
5. सामान्यता और लोक-संस्कृति का समावेश
- गोवर्धन पूजा, रासलीला, होली आदि पर्वों का चित्रण
- आम जनता की भाषा, शैली, बोली और भावनाओं को स्थान मिला
6. काव्य रूप और भाषा
- मुक्तक काव्य की प्रधानता – स्वतंत्र पदों के रूप में रचना
- ब्रजभाषा प्रमुख माध्यम – माधुर्य और लालित्यपूर्ण भाषा
- गेय पद परंपरा – संगीत के माध्यम से भक्ति का प्रचार
7. काव्य में दर्शन और काव्य सौंदर्य का अद्भुत समन्वय
- एक ओर भक्ति, दूसरी ओर गहन काव्य-कला का प्रदर्शन
- भाव, भाषा, लय और अभिव्यक्ति का संतुलन
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के विषय में कहा:
“यद्यपि तुलसीदास के समान सूरदास का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है, किंतु जिस सीमित भूमि में उन्होंने प्रवेश किया, उसका कोई कोना उन्होंने छोड़ा नहीं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर ने जो किया, वहाँ तक और किसी कवि की दृष्टि नहीं पहुँची।”
कृष्ण भक्ति काव्यधारा – अन्य विशेषताएँ और दार्शनिक पृष्ठभूमि
1. कृष्ण भक्ति काव्य का साहित्यिक और दार्शनिक स्रोत
कृष्ण भक्ति काव्यधारा का दार्शनिक और साहित्यिक आधार अत्यंत समृद्ध है। इसके दो प्रमुख स्रोत माने जाते हैं:
1.1 श्रीमद्भागवत पुराण
कृष्ण लीला का सबसे प्रामाणिक वर्णन श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध में प्राप्त होता है। विशेषतः 46वें और 47वें अध्याय में राधा और गोपियों के माध्यम से कृष्ण के विरह और माधुर्य प्रेम का जो चित्रण किया गया है, वही आगे चलकर “भ्रमरगीत” की परंपरा का आधार बना।
1.2 महाभारत और गीतगोविन्द
महाभारत में कृष्ण का एक रणनीतिकार और तत्वज्ञान का प्रचारक रूप मिलता है। वहीं, संस्कृत काव्य में जयदेव का “गीतगोविन्द” कृष्ण-राधा के माधुर्य रस का अद्वितीय ग्रंथ है। इसी काव्य की परंपरा को हिंदी के आदिकवियों ने आगे बढ़ाया।
2. विद्यापति का योगदान
विद्यापति (14वीं–15वीं शताब्दी) मैथिली भाषा के महान भक्त कवि थे। वे आधुनिक भारतीय भाषाओं में राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाले सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। विद्यापति ने जयदेव के गीतगोविन्द से प्रेरणा लेकर “विद्यापति पदावली” की रचना की, जिसमें राधा-कृष्ण के मधुर प्रेम, विरह-वेदना और माधुर्य का सरस वर्णन है।
उनके पदों की भावनात्मक गहराई का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं इन पदों को गाते-गाते भावविभोर हो जाते थे और कई बार मुर्छित तक हो जाते थे।
👉 इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हिंदी में कृष्ण काव्य परंपरा का बीज विद्यापति ने बोया, जिसे सूरदास, रसखान, मीरा आदि ने आगे विकसित किया।
3. भ्रमरगीत परंपरा
भ्रमरगीत कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गोपियों द्वारा उद्धव के समक्ष व्यक्त विरह-भाव की अभिव्यक्ति है। श्रीमद्भागवत पुराण के दशम स्कंध के 46वें और 47वें अध्यायों में इस प्रसंग का वर्णन है। गोपियाँ कृष्ण से अपने मिलन की आकांक्षा में उद्धव को उलाहना देती हैं। यह संवाद अत्यंत मार्मिक, व्यंग्यात्मक और भावप्रवण होता है।
- हिंदी में भ्रमरगीत परंपरा की नींव सूरदास ने रखी।
- बाद में नंददास ने भी अपने “सुदामा चरित” में इसका उल्लेख किया।
- इस परंपरा में प्रेम का विरह पक्ष अत्यंत कोमलता से सामने आता है।
4. श्रीनाथ मंदिर, गोवर्धन और अष्टछाप
- वल्लभ संप्रदाय की उपासना परंपरा का प्रमुख केंद्र श्रीनाथ मंदिर है, जिसकी स्थापना पूर्णमल खत्री ने की थी।
- इस मंदिर में अष्टछाप के कवियों द्वारा “अष्ट भाग सेवा विधि” के अंतर्गत सेवा-गान किया जाता था।
- अष्टछाप की स्थापना विठ्ठलनाथ (वल्लभाचार्य के पुत्र) द्वारा 1565 ई. में की गई थी। किंतु कुछ ग्रंथों में इसका आरंभ 1519 ई. भी उल्लेखित है।
5. 84 वैष्णव की वार्ता और वैष्णव साहित्य
- “84 वैष्णव की वार्ता” वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख साहित्यिक कृति है जिसमें वल्लभाचार्य के 84 प्रमुख शिष्यों के जीवन व भक्ति प्रसंगों का वर्णन है।
- इसी प्रकार “252 वैष्णव की वार्ता” में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन मिलता है।
- ये वाङ्मय रचनाएँ भक्तों के चरित्र, साधना, सेवा भावना और समाज सुधार के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।
6. पुष्टि मार्ग और रागानुगा भक्ति
- वल्लभाचार्य के दर्शन शुद्धाद्वैतवाद पर आधारित थे। उन्होंने भक्ति को “पुष्टि” यानी ईश्वर की अनुग्रहजन्य कृपा का परिणाम माना।
- इस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। यह मार्ग “निस्वार्थ रागानुगा भक्ति” (राग आधारित भक्ति) पर केंद्रित है – जिसमें भक्त अपने को कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है।
- वल्लभाचार्य की रचनाएँ जैसे सुबोधिनी, भागवत टीका और अनुभाष्य में इसी भक्ति की दार्शनिक व्याख्या मिलती है।
प्रमुख कृष्ण भक्ति संप्रदायों की विचारधाराएँ – सारांश
| संप्रदाय | प्रवर्तक | दार्शनिक आधार | भक्ति स्वरूप | प्रमुख कवि |
|---|---|---|---|---|
| वल्लभ संप्रदाय | वल्लभाचार्य | शुद्धाद्वैत | पुष्टि मार्ग, रागानुगा भक्ति | सूरदास, नंददास, कुंभनदास आदि (अष्टछाप) |
| निम्बार्क संप्रदाय | निम्बार्काचार्य | द्वैताद्वैत | राधा-कृष्ण की युगल उपासना | हरिव्यास, श्रीभट्ट |
| राधावल्लभ संप्रदाय | हित हरिवंश | राधा प्रधान उपासना | राधा को ईश्वर के रूप में | हित हरिवंश |
| हरिदासी संप्रदाय | स्वामी हरिदास | सखी भाव | राधा-कृष्ण के प्रेम की अनुभूति | स्वयं स्वामी हरिदास |
| गौड़ीय/चैतन्य संप्रदाय | चैतन्य महाप्रभु | अचिन्त्य भेदाभेद | संकीर्तन भक्ति, ब्रज रूप की उपासना | गदाधर भट्ट, नरोत्तमदास |
| संप्रदाय निरपेक्ष | — | — | समर्पण और प्रेम भाव | मीरा बाई, रसखान |
कृष्ण भक्ति काव्यधारा का वैचारिक और साहित्यिक आधार अत्यंत व्यापक है। विद्यापति से लेकर सूर, रसखान, मीरा और स्वामी हरिदास तक एक परंपरा विकसित होती है जो न केवल भक्ति का चित्रण करती है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना, स्त्री विमर्श, लोकभाषा और संगीत के साथ आत्मसात होकर जनमानस को प्रभावित करती है।
कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ
कृष्ण भक्ति काव्यधारा की समृद्ध परंपरा में असंख्य कवियों ने भाग लिया, किंतु उनमें से कुछ कवि अपने काव्य के भाव, भाषा, संगीतात्मकता, भक्ति के स्वरूप और साहित्यिक योगदान के कारण विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये कवि अलग-अलग संप्रदायों से संबंधित हो सकते हैं, किंतु इनकी भक्ति भावना और काव्य कला ने उन्हें कालजयी बना दिया।
नीचे प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों की संक्षिप्त परिचयात्मक सूची उनके जीवनकाल, प्रमुख रचनाओं और विशेषताओं सहित दी जा रही है।
1. सूरदास (1478–1573)
- जन्म: 1478 ई.
- मृत्यु: 1573 ई.
- संप्रदाय: वल्लभ संप्रदाय (अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि)
- स्थान: सीही (हथीन, हरियाणा), ब्रज क्षेत्र
- विशेषता: कृष्ण की बाल लीलाओं और वात्सल्य भाव का अद्भुत चित्रण
- भाषा: ब्रजभाषा
- रचनाएँ:
- सूरसागर: श्रीमद्भागवत पर आधारित 12 स्कंधों में सवा लाख पदों का संग्रह, जिसमें अब लगभग 45,000 पद उपलब्ध हैं।
- सूरसारावली: 1103 पद; विष्णु के एक वर्ष के व्रत वर्णन
- साहित्य लहरी: 118 पदों की एकाधिक भाव-छटाओं वाली रचना
- भ्रमरगीत सार: श्रीमद्भागवत के भ्रमरगीत प्रसंग पर आधारित
सूरदास को “वात्सल्य रस का सम्राट” माना जाता है और उनकी रचनाएँ गेय शैली में अत्यंत लोकप्रिय हैं।
2. कुंभनदास (1468–1582)
- जन्म: 1468 ई.
- मृत्यु: 1582 ई.
- संप्रदाय: वल्लभ संप्रदाय (अष्टछाप के कवि)
- जन्मस्थान: गोवर्धन, मथुरा
- विशेषता: अत्यंत निष्कलुष भक्ति; राजदरबार में गाने से इनकार
- भाषा: ब्रजभाषा
- रचनाएँ:
- केवल फुटकर पद उपलब्ध हैं
इनके पदों में गहरी अध्यात्मिक तन्मयता और सांसारिक उपेक्षा झलकती है।
3. नंददास (1513–1583)
- जन्म: 1513 ई.
- मृत्यु: 1583 ई.
- संप्रदाय: वल्लभ संप्रदाय (अष्टछाप के कवि)
- जन्मस्थान: रामपुर (उत्तर प्रदेश)
- भाषा: ब्रजभाषा
- विशेषता: अत्यंत विद्वान कवि; प्रबंध काव्य शैली में दक्ष
प्रमुख रचनाएँ (13 रचनाएँ):
- रास पंचाध्यायी
- सिद्धांत पंचाध्यायी
- अनेकार्थ मंजरी
- मानमंजरी
- रूपमंजरी
- विरहमंजरी
- भँवरगीत
- गोवर्धनलीला
- श्याम सगाई
- रुक्मिणी मंगल
- सुदामा चरित
- भाषादशम स्कंध
- पदावली
4. परमानंद दास
- संप्रदाय: वल्लभ संप्रदाय (अष्टछाप के कवि)
- रचना: परमानंद सागर
- पदों में श्रृंगार और माधुर्य भाव की प्रमुखता
5. कृष्णदास
- संप्रदाय: वल्लभ संप्रदाय (अष्टछाप के कवि)
- रचना: जुगलमान चरित्र – राधा-कृष्ण के युगल स्वरूप का वर्णन
6. छीत स्वामी, गोविंद स्वामी
- संप्रदाय: वल्लभ संप्रदाय (अष्टछाप के कवि)
- रचनाएँ: केवल फुटकल पद ही उपलब्ध हैं
7. चतुर्भुजदास
- संप्रदाय: वल्लभ संप्रदाय (अष्टछाप के कवि)
- प्रमुख रचनाएँ:
- द्वादशयश
- भक्ति प्रताप
- हितजू को मंगल
8. श्री भट्ट
- संप्रदाय: निम्बार्क संप्रदाय
- रचना: युगल शतक – राधा-कृष्ण की युगल उपासना को केंद्र में रखते हुए
9. हित हरिवंश
- संप्रदाय: राधावल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक
- रचना: हित चौरासी – 84 भावमय पदों का संग्रह, जिनमें राधा को प्रधानता दी गई है
10. स्वामी हरिदास
- संप्रदाय: हरिदासी संप्रदाय (सखी भाव के प्रवर्तक)
- रचना: हरिदास जी के पद – अत्यंत भावप्रवण पदों में राधा के दृष्टिकोण से कृष्ण का चित्रण
11. ध्रुवदास
- रचनाएँ:
- भक्त नामावली – वैष्णव संतों की जीवनी
- रसलावनी – भक्तिपूर्ण काव्य संग्रह
12. मीरा बाई (1498–1547)
- जन्म: 1498 ई.
- मृत्यु: 1547 ई.
- संप्रदाय: संप्रदाय निरपेक्ष
- जन्मस्थान: मेड़ता (राजस्थान)
- विशेषता: स्त्री मुक्ति और आत्म समर्पण का आदर्श; लोकनायिका
प्रमुख रचनाएँ:
- मीराबाई पदावली
- नरसी जी का मायरा
- गीत गोविंद टीका
- राग गोविंद
- राग सोरठ के पद
मीरा ने सामंती बंधनों से मुक्त होकर स्त्री चेतना और भक्ति का उदात्त उदाहरण प्रस्तुत किया।
13. रसखान (1533–1610 लगभग)
- जन्म: 1533 ई.
- मृत्यु: 1610 ई.
- वास्तविक नाम: सैय्यद इब्राहीम
- संप्रदाय: संप्रदाय निरपेक्ष (मुस्लिम होकर भी कृष्णभक्त)
- भाषा: ब्रजभाषा
- विशेषता: कृष्ण के प्रति प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित
प्रमुख रचनाएँ:
- प्रेमवाटिका – 52 दोहों की अद्भुत श्रृंखला
- सुजान रसखान
- दानलीला
रसखान का काव्य कृष्ण प्रेम की अनन्य ऊँचाइयों को दर्शाता है।
🔹 14. नरोत्तमदास (1493–1548 लगभग)
- जन्म: संवत 1550 (1493 ई.)
- मृत्यु: संवत 1605 (1548 ई.) के लगभग
- संप्रदाय: कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबद्ध, यद्यपि अष्टछाप से पृथक
- जन्मस्थान: जिला सीतापुर (उत्तर प्रदेश)
- भाषा: सरस, प्रवाहमयी ब्रजभाषा
- शैली: काव्यात्मक नाट्य शैली; संवाद प्रधान; मंचन योग्य काव्य
- छंद-विधान: दोहा, कवित्त, सवैया, कुंडली
- विषय-वस्तु: कृष्ण और सुदामा की भावुक मित्रता, दारिद्र्य का आत्मीय चित्रण, भक्ति और करूणा की गहराई
- प्रमुख रचनाएँ:
- सुदामा चरित –
नरोत्तमदास की यह सर्वप्रसिद्ध रचना है। इसमें कृष्ण और उनके बालसखा सुदामा की मित्रता, सुदामा की निर्धनता, और कृष्ण द्वारा उसे दिए गए आत्मीय स्नेह और सम्मान का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण है।
सुदामा चरित में राजसी वैभव और गरीब भक्त की तुलना न कर भावनात्मक गहराई से ईश्वर के भक्तवत्सल रूप को उजागर किया गया है। यह काव्य इतने प्रभावी ढंग से लिखा गया है कि इसका पाठन या गायन श्रोता को भावविभोर कर देता है। - ध्रुव चरित –
विष्णुभक्त बालक ध्रुव की अडिग निष्ठा, बाल-विरक्ति और ईश्वरीय कृपा प्राप्ति की कथा। यह भी नरोत्तम की भक्ति भावना और साधना-शक्ति का परिचायक है। - विचार माला –
भक्ति मार्ग और जीवन के गूढ़ नैतिक-अध्यात्मिक विचारों पर आधारित एक चिंतनपरक रचना। इसमें धर्म, भक्ति, वैराग्य और आत्मज्ञान के विषयों को सहज शैली में प्रस्तुत किया गया है। - 👉 विशेष उल्लेखनीय यह है कि नरोत्तमदास की रचनाएँ लोकधर्मी हैं, उनमें भक्ति का साथ-साथ मानवता, सामाजिक समता और करुणा का भी समावेश है। वे केवल कृष्ण भक्त नहीं, मानवीय संवेदनाओं के काव्यनाटककार भी हैं।
- उनकी भाषा अत्यंत प्रवाहमयी, सरस और गेय है। यही कारण है कि आज भी सुदामा चरित भजन, नाटक, कीर्तन और लोकगायन की प्रिय विधा बना हुआ है।
सारणीबद्ध रूप में कृष्ण भक्त कवि और रचनाएँ
नीचे दिए गए सारणी में कृष्ण भक्त कवि (कृष्णाश्रयी शाखा के कवि) और उनकी रचनाओं को व्यवस्थित रूप में दिया गया है –
| क्रम | कवि/रचनाकार | प्रमुख रचनाएँ |
|---|---|---|
| 1 | सूरदास | सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमरगीत |
| 2 | परमानंद दास | परमानंद सागर |
| 3 | कृष्ण दास | जुगलमान चरित्र |
| 4 | कुंभन दास | फुटकल पद |
| 5 | छीत स्वामी | फुटकल पद |
| 6 | गोविंद स्वामी | फुटकल पद |
| 7 | चतुर्भुजदास | द्वादशयश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल |
| 8 | नंददास | रास पंचाध्यायी, भँवर गीत, सुदामा चरित, रूपमंजरी आदि |
| 9 | श्री भट्ट | युगल शतक |
| 10 | हित हरिवंश | हित चौरासी |
| 11 | स्वामी हरिदास | हरिदास जी के पद |
| 12 | ध्रुव दास | भक्त नामावली, रसलावनी |
| 13 | मीरा बाई | मीराबाई पदावली, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद |
| 14 | रसखान | प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दानलीला |
| 15 | नरोत्तमदास | सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला |
निष्कर्ष
कृष्ण भक्ति काव्यधारा भारतीय भक्ति काव्य की सबसे व्यापक और विविध रूप वाली धारा है। इसमें:
- आध्यात्मिक प्रेम,
- सामाजिक चेतना,
- काव्य-कला,
- लोक-संस्कृति
एक साथ घुलमिल जाती है।
सूरदास, मीरा, रसखान जैसे कवियों ने इसे लोकमानस से जोड़कर समग्र भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। यह धारा केवल भक्ति नहीं, बल्कि कविता, संगीत, लोक परंपरा और सामाजिक सुधार का संगम है।
कृष्ण भक्ति काव्य धारा को एक सांस्कृतिक आंदोलन भी कहा जा सकता है — जिसमें दर्शन, काव्य, संगीत, समाज और आत्मिक मुक्ति के स्वर एकसाथ सुनाई देते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्र.1: कृष्ण भक्ति काव्यधारा किसे कहते हैं?
उत्तर: कृष्ण को भगवान के रूप में आराध्य मानकर उनकी लीलाओं, प्रेम, और बाल रूप का चित्रण करने वाली साहित्यिक धारा को कृष्ण भक्ति काव्यधारा कहा जाता है।
प्र.2: अष्टछाप के कवि कौन थे?
उत्तर: अष्टछाप में सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंदस्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास शामिल थे।
प्र.3: कृष्ण भक्ति में कौन-से रस प्रमुख हैं?
उत्तर: श्रृंगार रस और वात्सल्य रस।
प्र.4: कृष्ण भक्ति में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ?
उत्तर: प्रमुखतः ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ।
प्र.5: मीरा बाई का क्या योगदान है?
उत्तर: मीरा बाई ने नारी मुक्ति, आत्म-समर्पण और प्रेम भक्ति का स्वर दिया। वे सामाजिक विद्रोह और आध्यात्मिक प्रेम की प्रतीक हैं।
प्र.6: सूरदास की प्रमुख विशेषता क्या है?
उत्तर: सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के अप्रतिम कवि हैं, जिनके काव्य में बालकृष्ण की मोहक छवि मिलती है।
प्र.7: रसखान किस संप्रदाय से थे?
उत्तर: वे संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि थे।
प्र.8: वल्लभाचार्य ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया?
उत्तर: ‘पुष्टि मार्ग’ का – जो ईश्वर की कृपा पर आधारित भक्ति मार्ग है।
प्र.9: हरिदासी संप्रदाय का मुख्य भाव क्या था?
उत्तर: कृष्ण को राधा के दृष्टिकोण से देखना अर्थात सखी भाव।
प्र.10: कृष्ण भक्ति काव्यधारा में सामाजिक प्रभाव क्या रहा?
उत्तर: इस धारा ने स्त्री स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता, लोक-संस्कृति के संवर्धन और सामाजिक समानता को बल दिया।
प्रश्न 11: कृष्ण भक्ति काव्यधारा क्या है?
उत्तर: यह मध्यकालीन हिंदी काव्य की एक प्रमुख भक्ति शाखा है, जिसमें कवियों ने भगवान श्रीकृष्ण को केंद्र बनाकर काव्य रचना की। इसमें उनका बाल स्वरूप, रासलीला, वात्सल्य और प्रेम भाव प्रमुख हैं।
प्रश्न 12: कृष्ण भक्ति काव्यधारा को अन्य नामों से क्या जाना जाता है?
उत्तर: इसे कृष्णाश्रयी शाखा या कृष्ण काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न 13: कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं?
उत्तर: सूरदास, मीरा बाई, रसखान, नंददास, कुंभनदास, नरोत्तमदास, परमानंद दास, कृष्णदास, स्वामी हरिदास आदि।
प्रश्न 14: अष्टछाप क्या है?
उत्तर: अष्टछाप वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा दीक्षित आठ प्रमुख कवियों का समूह है, जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर पद रचना की।
प्रश्न 15: अष्टछाप के कवियों के नाम क्या हैं?
उत्तर: सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी।
प्रश्न 16: कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर: वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा का प्रयोग, लोकजीवन की सजीवता, गेय पद परंपरा, नारी मुक्ति का स्वर, तथा राधा-कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति।
प्रश्न 17: कृष्ण भक्ति काव्य के आधार ग्रंथ कौन-कौन से हैं?
उत्तर: श्रीमद्भागवत पुराण (विशेषकर दशम स्कंध), महाभारत, गीत गोविंद (जयदेव) और विद्यापति पदावली।
प्रश्न 18: सूरदास की प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमरगीत।
प्रश्न 19: मीरा बाई किस संप्रदाय से संबंधित थीं?
उत्तर: मीरा संप्रदाय निरपेक्ष थीं, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति को वैष्णव परंपरा में कृष्ण को समर्पित किया।
प्रश्न 20: रसखान कौन थे और उनकी प्रमुख रचनाएँ क्या हैं?
उत्तर: रसखान मुस्लिम भक्त कवि थे, जिन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम में संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनकी रचनाएँ हैं – प्रेमवाटिका, सुजान रसखान, दानलीला।
प्रश्न 21: नरोत्तमदास की प्रसिद्ध रचना कौन-सी है?
उत्तर: सुदामा चरित, जिसमें कृष्ण-सुदामा की मित्रता का भावुक चित्रण है।
प्रश्न 22: पुष्टि मार्ग क्या है?
उत्तर: वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित भक्ति मार्ग, जिसमें श्रीकृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानकर ‘शुद्धाद्वैत’ दर्शन के आधार पर सेवा-भाव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।
प्रश्न 23: ब्रजभाषा का महत्त्व कृष्ण काव्यधारा में क्यों है?
उत्तर: चूंकि कृष्ण की लीलास्थली ब्रजभूमि है, इसलिए ब्रजभाषा उनके जीवन और लीलाओं को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई, जिससे यह भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा बन गई।
प्रश्न 24: श्रृंगार और वात्सल्य रस के क्षेत्र में सूरदास का क्या योगदान है?
उत्तर: सूरदास ने इन दोनों रसों में अद्वितीय चित्रण किया। वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने में उनका योगदान सर्वोपरि है।
Hindi – KnowledgeSthali
इन्हें भी देखें –
- राम भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- पदबन्ध (Phrase) | परिभाषा, भेद एवं उदाहरण
- प्रत्यय किसे कहते हैं? भेद एवं 100+ उदाहरण
- उपसर्ग किसे कहते हैं? भेद और 100+ उदाहरण
- पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द 500+ उदाहरण
- महाराजा विक्रमादित्य – एक महान सम्राट का गौरवमयी इतिहास (101ई.पू.-19ई.)
- सातवाहन वंश | SATVAHAN DYNASTY | 60 ई.पू. – 240 ईस्वी
- छत्रपति शिवाजी महाराज (1674 – 1680 ई.)
- History of Goa गोवा का इतिहास
- भारत की जनजातियाँ | Tribes of India
- राष्ट्रीय खेल नीति 2025: भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना में मिला ‘ऑर्डर ऑफ द स्टार’ सम्मान
- RailOne ऐप: भारतीय रेलवे की डिजिटल क्रांति की नई दिशा
- महाबोधि मंदिर: बौद्ध धर्म की पवित्र धरोहर और प्रशासनिक विवाद
- ग्लूटाथायोन | एंटीऑक्सिडेंट की जननी या सौंदर्य के नाम पर खतरा?