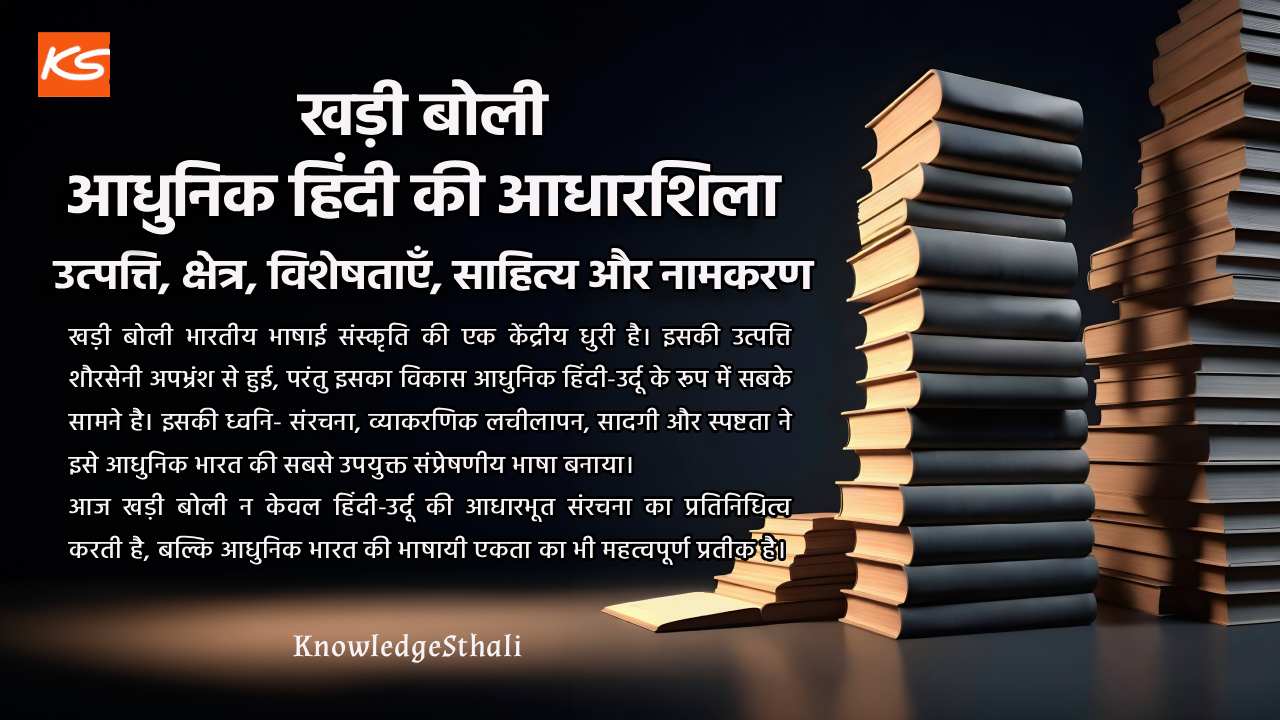भारतीय उपमहाद्वीप की भाषायी परंपरा जितनी प्राचीन है, उतनी ही विविध और व्यापक भी। यहाँ की हर भाषा, हर बोली और हर उपबोली अपने भीतर हजारों वर्षों का विकास, प्रयोग और सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए चलती है। इन भाषायी धाराओं में खड़ी बोली का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यही बोली आगे चलकर आधुनिक मानक हिंदी और उर्दू, दोनों की रीढ़ बनी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली यह भाषा न केवल लोक-प्रयोग में व्यापक है, बल्कि आधुनिक साहित्य, मीडिया, प्रशासन, न्यायालय और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी आज की प्रमुख भाषा-पद्धति का आधार बन चुकी है।
यह लेख खड़ी बोली को उसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति से लेकर उसके आधुनिक साहित्यिक रूप, भाषाई विशेषताओं, भौगोलिक विस्तार और नामकरण तक विस्तारपूर्वक समझाता है।
खड़ी बोली का परिचय: मानक हिंदी का आधारभूत स्वरूप
खड़ी बोली (कभी-कभी ‘खरी बोली’, ‘कौरवी’, ‘नागरी’ आदि नामों से भी संदर्भित) वह बोली है जिसने उत्तर भारत की भाषायी संरचना को एक आधुनिक ढांचा दिया। जहाँ ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली आदि लोकबोलियों में भक्ति साहित्य और काव्य की समृद्ध परंपराएँ विकसित हुईं, वहीं खड़ी बोली 19वीं–20वीं शताब्दी में आधुनिक गद्य, व्याकरणिक मानकीकरण और राष्ट्रभाषा-निर्माण का माध्यम बनी।
‘खड़ी बोली’ शब्द का अर्थ प्रायः मानक, सीधी, सरल और स्पष्ट भाषा माना जाता है। यद्यपि हर भाषा की अपनी एक मानकीकृत बोली होती है, किंतु ‘हिंदी’ की मानक भाषा का आधार मेरठ–सहारनपुर–मुज़फ्फरनगर के मध्यवर्ती भूभाग की कौरवी/खड़ी बोली को माना गया है।
इन क्षेत्रों में ‘खड़ी’ का उच्चारण स्थानीय ध्वन्यात्मकता के कारण ‘खरी’ भी हो जाता है, जिसका अर्थ ‘शुद्ध’ या ‘ठेठ स्थानीय भाषा’ होता है।
भाषिक वंशावली: संस्कृत से आधुनिक हिंदी तक की यात्रा
खड़ी बोली का भाषिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से आधुनिक हिंदी-उर्दू की संरचना उजागर होती है। इसकी वंशावली इस प्रकार है—
संस्कृत → प्राकृत → शौरसेनी अपभ्रंश → खड़ी बोली → आधुनिक हिंदी/उर्दू
- संस्कृत: भारत की प्राचीन धर्म, दर्शन, साहित्य की मूल भाषा।
- प्राकृत: संस्कृत से विकसित जनभाषाएँ, जैसे शौरसेनी, अर्धमागधी आदि।
- शौरसेनी अपभ्रंश: उत्तर भारत के पश्चिमी भाग में विकसित एक अपभ्रंश भाषा।
- खड़ी बोली: शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोली।
यही बोली आगे चलकर दो प्रमुख साहित्यिक रूपों की जननी बनी—
(1) आधुनिक मानक हिंदी (देवनागरी लिपि)
(2) आधुनिक उर्दू (नस्तालीक लिपि)
इस प्रकार, खड़ी बोली केवल एक बोली नहीं, बल्कि उत्तर भारतीय भाषिक संस्कृति का केन्द्रीय आधार है।
खड़ी बोली का ऐतिहासिक विकास
(पुनर्संयोजित, विस्तृत और स्वाभाविक रूप से परिवर्तित संस्करण)
खड़ी बोली का इतिहास जितना सरल दिखाई देता है, उतना है नहीं। आधुनिक हिन्दी के जिस रूप को आज हम पढ़ते-लिखते हैं, उसकी जड़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इसी बोली में पैवस्त हैं। यह बोली न तो ब्रजभाषा की कोमलता लिए होती है और न अवधी की गीतात्मकता—बल्कि इसकी पहचान इसकी सीधी, स्पष्ट और व्यवस्थित भाषा-प्रकृति से होती है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली पर आधारित रूप विकसित होते-होते ‘हिन्दी’ बना, जबकि इसी बोली के फारसी-अरबी मिश्रित रूप ने ‘उर्दू’ का स्वरूप ग्रहण किया। इस प्रकार खड़ी बोली आधुनिक हिन्दी-उर्दू की साझा धुरी बनकर उभरती है।
प्रारम्भिक चरण: एक नई संपर्क-भाषा की तलाश
दिल्ली-सहारनपुर-मेवात के आसपास का इलाका सदियों से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। जब मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, तो शासकों और सैनिकों–व्यापारियों को ऐसी भाषा चाहिए थी, जिसमें वे स्थानीय लोगों से सरलता से संवाद कर सकें।
ब्रजभाषा और अवधी उस समय साहित्यिक रूप से प्रतिष्ठित थीं, परंतु इन दोनों में ध्वनि-संरचना अपेक्षाकृत कठिन थी। इसी वजह से नवागंतुक समुदायों ने मेरठ, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के बीच बोली जाने वाली सहज बोली को अपनाना शुरू किया—और यही बोली आगे चलकर “खड़ी बोली” के नाम से प्रसिद्ध हुई।
इस बोली में समय के साथ फारसी, तुर्की और अरबी के शब्द शामिल होते गए, जिससे भाषाई प्रवाह और अधिक मिश्रित रूप लेता गया। यही सम्मिश्रण आगे चलकर ‘उर्दू’ के विकास का आधार बना।
अमीर खुसरो का योगदान: खड़ी बोली का साहित्य में प्रवेश
14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस उभरती बोली को साहित्य में जगह दी। वह न केवल इस बोली में काव्य-रचना करते थे, बल्कि लोकभाषाओं को दरबारी परिवेश तक ले गए। उनके लेखन ने यह प्रमाणित कर दिया कि यह भाषा केवल बोलचाल की सीमा में ही बंधी नहीं है—यह रचनात्मकता को भी सहजता से सहन कर सकती है।
इसी दौर में खड़ी बोली का स्वरूप लोकप्रिय होता गया, और दिल्ली की सांस्कृतिक हलचल में यह प्रमुख अभिव्यक्ति-भाषा बनती चली गई।
मध्यकालीन साहित्यिक परिदृश्य और खड़ी बोली की सीमित उपस्थिति
15वीं और 16वीं शताब्दी में, यद्यपि कुछ कवियों ने खड़ी बोली में प्रयोग शुरू किया था, फिर भी अवधी और ब्रजभाषा की साहित्यिक परंपरा इतनी सशक्त थी कि खड़ी बोली को प्रमुख स्थान नहीं मिल सका। तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति, रहीम—ये सभी एक सशक्त साहित्यिक परंपरा स्थापित कर चुके थे और खड़ी बोली उस समय मुख्यतः बोलचाल और सीमित गद्य लेखन तक सीमित रही।
18वीं–19वीं शताब्दी: आधुनिक हिन्दी गद्य का जन्म
असली परिवर्तन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू होता है। इस समय से हिन्दी गद्य की एक नई धारा विकसित होने लगी, और दिल्ली-आगरा क्षेत्र के पंडितों व शिक्षित वर्ग ने खड़ी बोली को गद्य लेखन के लिए उपयुक्त पाया।
इस युग में कई विद्वानों ने आधुनिक हिन्दी गद्य को आकार दिया—
- लल्लूलाल,
- मुंशी सदासुखलाल,
- सदल मिश्र,
इन लेखकों ने पहली बार व्यवस्थित व्याकरण और गद्य-विन्यास के साथ खड़ी बोली को साहित्य की मुख्यधारा में लाना शुरू किया। लल्लूलाल के “प्रेमसागर” को तो आधुनिक हिन्दी गद्य का प्रथम महत्त्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है।
हिन्दी और उर्दू: एक ही मूल बोली के दो स्वरूप
दिलचस्प बात यह है कि हिन्दी और उर्दू दोनों का जन्म इसी खड़ी बोली की शाखाओं से हुआ—
- मुसलमान साहित्यकारों ने फारसी और अरबी शब्दों को मिलाकर एक नई साहित्यिक परंपरा विकसित की, जो आगे चलकर “उर्दू” कहलायी।
- हिन्दू लेखकों ने संस्कृत शब्दों को आधार बनाकर परिष्कृत “हिन्दी” की रचना की।
इसलिए हिन्दी-उर्दू विवाद के ऐतिहासिक संदर्भ में भी खड़ी बोली एक पुल की तरह दिखाई देती है, जिसने दोनों को समान रूप से जन्म दिया और पोषित किया।
आधुनिक साहित्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा
19वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 20वीं शताब्दी के आरंभ आते-आते खड़ी बोली हिन्दी का मानक रूप बन चुकी थी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और छायावाद—इन सभी movements ने खड़ी बोली को साहित्य की धुरी बना दिया।
निराला, प्रसाद, प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त जैसे रचनाकारों ने आधुनिक हिन्दी साहित्य को जो चमक दी, उसकी बुनियाद भी इसी बोली पर टिकी हुई थी।
इसी काल में हरिऔध ने ‘प्रिय प्रवास’ जैसा महाकाव्य लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में न केवल गद्य बल्कि उच्च कोटि का पद्य साहित्य भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार यह बोली ‘मानक हिन्दी’ का पर्याय बन गई।
समग्र रूप में ऐतिहासिक निष्कर्ष
खड़ी बोली का इतिहास तीन-चार सदी में धीरे-धीरे विकसित हुआ, अचानक नहीं। मध्यकाल की बोलचाल और संपर्क भाषा से शुरू हुई यह यात्रा आधुनिक राष्ट्रभाषा हिन्दी के गठन तक पहुँचती है।
- मुस्लिम शासकों ने इसे बोलचाल के माध्यम के रूप में अपनाया,
- संत-सूफी परंपरा ने इसमें रस भरा,
- 18वीं शताब्दी के विद्वानों ने इसे गद्य का रूप दिया,
- और 19वीं–20वीं शताब्दी के साहित्यकारों ने इसे मानक भाषा का दर्जा दिला दिया।
आज खड़ी बोली केवल एक बोली नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय भाषाई संरचना की आधारशिला है।
खड़ी बोली के नामकरण पर विचार
विभिन्न विद्वानों ने खड़ी बोली को अलग-अलग नामों से संबोधित किया है—
डॉ. जॉर्ज ग्रियर्सन
- Vernacular Hindustani (वर्नाक्युलर हिन्दुस्तानी)
- ‘High Hindi’ (हाई हिन्दी)
डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी
- ‘जनपदीय हिन्दुस्तानी’
- साहित्यिक रूप—‘साधु हिन्दी’ या ‘नागरी हिन्दी’
अन्य ऐतिहासिक नाम
- हिन्दुई
- हिन्दवी
- दक्खिनी/दखनी
- रेखता
- हिंदोस्तानी/हिन्दुस्तानी
इन नामों से खड़ी बोली के निरंतर विकास और विभिन्न भाषायी रूपों से उसके जीवंत संबंधों की जानकारी मिलती है।
भौगोलिक विस्तार: खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है?
खड़ी बोली का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तक एक अखंड बोलचाल की धारा के रूप में फैली हुई है।
मुख्य बोली क्षेत्र
- मेरठ
- सहारनपुर
- मुज़फ्फरनगर
- देहरादून
- रामपुर
- बुलंदशहर
- गाजियाबाद
- हापुड़
- बागपत
- बिजनौर
- मुरादाबाद
- शामली
- अमरोहा
- संभल
- हरिद्वार
- उधम सिंह नगर
- अंबाला
- कलसिया (हरियाणा क्षेत्र)
इन विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाने वाली कौरवी/नागरी/खड़ी बोली में स्थानीय विविधताएँ भी मौजूद हैं, परंतु मूल भाषिक ढांचा समान रहता है।
खड़ी बोली से जुड़े विविध मत और इसकी भाषिक धारा
खड़ी बोली के बारे में जितने मत प्रचलित हैं, उतने शायद ही किसी अन्य भारतीय बोली को लेकर देखने को मिलते हों। इसे कहीं खरी बोली, कहीं कौरवी, और कहीं नागरी कहा जाता है। समय के साथ इसके स्वरूप, नाम और उद्गम को लेकर विद्वानों ने अलग-अलग दृष्टियाँ सामने रखी हैं। इन विविध मान्यताओं ने न केवल खड़ी बोली के भाषिक इतिहास को बहुआयामी बनाया, बल्कि इसके विकास-क्रम को समझने के नए-नए रास्ते भी खोले।
नामकरण का प्रश्न: ‘खड़ी’ या ‘खरी’?
अधिकांश लोग मानते हैं कि खड़ी बोली के लिए ‘खरी’ शब्द का पहला उल्लेख लल्लूलाल के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेमसागर पर मिलता है। माना जाता है कि कठोर और स्पष्ट उच्चारण वाली यह बोली ब्रज जैसी कोमल बोलियों से अलग दिखती थी, इसलिए इसे “खड़ी”—यानी सीधी, स्पष्ट और दृढ़—नाम दिया गया।
कई भाषाशास्त्रियों का यह भी मत है कि ‘खड़ी’ शब्द का तात्पर्य एक ऐसी भाषा से है जो व्यवस्थित, स्थिर और विकसित रूप धारण कर चुकी हो—इसलिए इसका उपयोग मानक हिन्दी के आधार-रूप के लिए भी सहज माना गया।
बोली और उर्दू—एक समानता और एक दूरी
कुछ विद्वान खड़ी बोली को ग्रामीण और शुद्ध भाषा की श्रेणी में रखते हैं और उर्दू से इसे भिन्न मानते हैं। वहीं दूसरी ओर, कुछ का विचार है कि उर्दू और खड़ी बोली एक ही भाषिक मिट्टी से उपजे पौधों की तरह हैं—फर्क केवल शब्द-सामग्री और लिपि का है। उर्दू में फारसी-तुर्की-अरबी प्रभाव बढ़ा, जबकि खड़ी बोली का मानकीकरण संस्कृत-आधारित शब्दावली के साथ हुआ।
खड़ी बोली की उत्पत्ति के बारे में विविध मत
खड़ी बोली की उत्पत्ति को लेकर भी कई सिद्धांत मिले हैं। अधिकांश शोधों के अनुसार यह बोली किसी एक क्षण में जन्म नहीं लेती, बल्कि सदियों की भाषा-यात्रा के बाद विकसित होकर आज के रूप में सामने आई है।
प्राकृत–अपभ्रंश–खड़ी बोली की विकास-श्रृंखला
हिमालय और विन्ध्य के मध्य का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में “आर्यावर्त” कहा जाता था। समय के साथ यहाँ भाषाओं की एक लंबी शृंखला विकसित हुई—
संस्कृत → पालि → शौरसेनी प्राकृत → शौरसेनी अपभ्रंश → खड़ी बोली
शौरसेनी अपभ्रंश का स्वतंत्र साहित्य तो बहुत अधिक नहीं मिलता, परन्तु मध्यकालीन अपभ्रंश रचनाओं—विशेषकर भोज और हम्मीरदेव के काल—में खड़ी बोली के शुरुआती रूप स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं।
भक्तिकाल में निर्गुण संतों द्वारा प्रयुक्त सधुक्कड़ी भाषा में भी खड़ी बोली के तत्व देखने को मिलते हैं, जिसने इसके आगे के विकास-मार्ग को और सुदृढ़ बना दिया।
खड़ी बोली पर मुस्लिम प्रभाव: एक महत्वपूर्ण चरण
कई भाषा-चिंतक यह मानते हैं कि जिस रूप को आज हम “खड़ी बोली” कहते हैं, उसे आकार देने में मुस्लिम शासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दिल्ली और उसके आसपास बसे तुर्क-अफ़ग़ान शासकों तथा सैनिकों को एक ऐसी स्थानीय भाषा की आवश्यकता थी, जो संवाद का सरल माध्यम बन सके। इसी आवश्यकता ने खड़ी बोली को तेज़ी से फैलने में सहायता की।
इसी खड़ी बोली में जब अरबी-फारसी शब्दों का अधिक इस्तेमाल होने लगा, तो उर्दू का स्वरूप विकसित हुआ। इसलिए कई विशेषज्ञों का मत है कि उर्दू एक अलग भाषा नहीं, बल्कि खड़ी बोली ही की एक शैलीगत शाखा है।
विद्वानों के दृष्टिकोण: मतों का विस्तृत परिदृश्य
खड़ी बोली पर भाषाविदों ने समय-समय पर अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ दृष्टियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं।
डॉ. ग्रियर्सन का मत
जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक साहसिक मत रखते हुए कहा कि खड़ी बोली का आधुनिक रूप अंग्रेजों के प्रयासों से निर्मित हुआ। उनके अनुसार—
- मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली उजड़ी।
- उर्दू शायर—जैसे मीर, इंशा—पूर्वी भारत के शहरों में बसने लगे।
- दिल्ली के व्यापारी भी इनके साथ स्थानांतरित हुए।
- इन लोगों की बोलचाल की भाषा नए नगरों में फैलकर “बाजार की भाषा” बन गई।
ग्रियर्सन का मानना था कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज अधिकारियों, विशेष रूप से गिलक्राइस्ट, ने हिन्दी को व्यवस्थित रूप में स्थापित कराया और लल्लूलाल को प्रेमसागर जैसे ग्रंथ लिखवाए, जिसने खड़ी बोली गद्य की नींव को मजबूत किया।
लल्लूलाल और सदल मिश्र का योगदान
लल्लूलाल और सदल मिश्र को खड़ी बोली गद्य-विकास का अग्रदूत माना जाता है, परन्तु उन्हें इसका जन्मदाता कहना अत्युक्ति होगा। खड़ी बोली की जड़ें उनके समय से बहुत पहले तैयार हो चुकी थीं। लेकिन यह सत्य है कि इन दोनों ने पहली बार इसे साहित्यिक गद्य के रूप में उपयोग कर लोकप्रियता प्रदान की और एक मानकीकृत रूप देने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई।
उर्दू और खड़ी बोली का ऐतिहासिक संबंध
उर्दू साहित्य के प्रारंभिक रचनाकारों—खुसरो से लेकर ज़फ़र और वाजिद अली शाह तक—ने खड़ी बोली आधारित ‘रेख्ता’ शैली में ही काव्य-रचना की। यह सिद्ध करता है कि उर्दू की बुनियाद खड़ी बोली पर ही आधारित रही है, चाहे आगे चलकर उसकी शब्द-संपदा और लिपि में कितना ही परिवर्तन क्यों न आया हो।
खड़ी बोली गद्य के आधुनिक प्रतिष्ठापक
यद्यपि शुरुआती संरचना लल्लूलाल–सदल मिश्र–इंशाअल्ला खाँ की देन थी, परन्तु खड़ी बोली को राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठा भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा शिवप्रसाद ‘सितारे हिन्द’ ने दिलाई।
- भारतेंदु ने सरल, सहज और आधुनिक गद्य के माध्यम से इसे सामाजिक-साहित्यिक मंच पर स्थापित किया।
- राजा शिवप्रसाद ने शैक्षिक एवं प्रशासनिक स्तर पर इसे बढ़ावा दिया।
भारतेन्दु युग के बाद खड़ी बोली की विजय लगभग सुनिश्चित हो गई और आधुनिक हिन्दी साहित्य इसी के आधार पर खड़ा हुआ।
इस प्रकार:
खड़ी बोली का स्वरूप किसी एक व्यक्ति या एक युग की देन नहीं है—यह एक लंबी भाषिक प्रक्रिया का परिणाम है।
- शौरसेनी अपभ्रंश की विरासत,
- संत साहित्य का प्रभाव,
- मुस्लिम शासन की संपर्क-भाषा की आवश्यकता,
- अंग्रेजी शासन की नीतियाँ,
- और आधुनिक हिन्दी लेखकों का योगदान—
इन सभी ने मिलकर खड़ी बोली को वह स्थान दिलाया, जहाँ आज यह मानक हिन्दी के रूप में खड़ी है।
खड़ी बोली की भाषिक विशेषताएँ: ध्वन्यात्मकता, व्याकरण और शब्द-रचना
खड़ी बोली की कुछ प्रमुख भाषिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—
(1) अकारांत प्रधानता
खड़ी बोली में अधिकांश शब्द ‘अ’ ध्वनि पर समाप्त होते हैं।
उदाहरण:
- करता
- घोड़ा
- खोटा
- क्रिया
यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण व्याकरणिक विशेषता है।
(2) मूर्धन्य ‘ल’ का प्रयोग
खड़ी बोली में ‘ळ/ल़’ ध्वनि का प्रयोग मिलता है, जो मानक हिंदी में प्रायः अनुपस्थित है।
उदाहरण—
- बाळक → बालक
- जंगळ → जंगल
यह प्राचीन प्राकृत और अपभ्रंश ध्वनियों का अवशेष है।
(3) द्वित्व व्यंजन
यहाँ दोहरे व्यंजनों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है।
उदाहरण—
- बेट्टी
- रोट्टी
- जात्ता
- गड्डी
मानक हिंदी में ये शब्द प्रायः—बेटी, रोटी, जाता, गाड़ी—हो जाते हैं।
(4) न/भ के स्थान पर ण/ब का प्रयोग
स्थानीय उच्चारण में
- न → ण
- भ → ब
जैसे परिवर्तन दिखते हैं।
उदाहरण— - खाना → खाणा
- जाना → जाणा
- कभी → कबी
- सभी → सबी
यह परिवर्तन खड़ी बोली की क्षेत्रीय ध्वनि–संरचना को चिह्नित करते हैं।
(5) क्रिया-रचना में मानक हिंदी से साम्य
खड़ी बोली की क्रिया-प्रणाली आधुनिक हिंदी से काफी मेल खाती है।
जैसे—
- वह चलता है → वह चले हैं (स्थानीय रूप)
यहाँ ‘है’ का ‘हैं’ रूप स्थानीय शैली में अधिक सुना जाता है।
(6) निश्चयार्थक भूतकाल में ‘या’ प्रत्यय
खड़ी बोली के भूतकाल में ‘या’ रूप सामान्यतः प्रयोग किया जाता है—
उदाहरण—
- बैठा → बैठ्या
- उठा → उठ्या
- गया → गय्या
यहाँ ‘या’ प्रत्यय निश्चयार्थ और पूर्णता का बोध कराता है।
साहित्य में खड़ी बोली का विकास: आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव
भारतीय साहित्यिक इतिहास में खड़ी बोली का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
ब्रजभाषा और अवधी से भिन्न खड़ी बोली साहित्य
जहाँ भक्ति-युग में ब्रजभाषा और अवधी का वर्चस्व था, वहीं आधुनिक युग में पत्रकारिता, कहानी, उपन्यास, नाटक और भाषा-आंदोलन के कारण खड़ी बोली प्रमुख बनी।
इस बोली ने—
- आधुनिक गद्य का विकास
- राष्ट्रवादी लेखन
- आधुनिक कविता
- शिक्षा और प्रशासनिक भाषा
को संगठित रूप दिया।
खड़ी बोली के प्रथम कवि: अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’
आधुनिक खड़ी बोली साहित्य के प्रथम कवि अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ माने जाते हैं।
उनकी साहित्यिक उपलब्धियाँ—
- हिंदी साहित्य सम्मेलन के दो बार सभापति
- ‘विद्यावाचस्पति’ उपाधि
- खड़ी बोली काव्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख कवि
हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ (निज़ामाबाद) में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य: ‘प्रिय प्रवास’
हरिऔध जी द्वारा रचित ‘प्रिय प्रवास’ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
महत्व—
- आधुनिक हिंदी काव्य में नया मोड़
- उच्च कोटि की भाषा
- राष्ट्रीय चेतना का संचार
- मंगलाप्रसाद पारितोषिक से सम्मानित
‘प्रिय प्रवास’ के कारण खड़ी बोली पहली बार ‘काव्य’ के रूप में स्थापित हुई।
खड़ी बोली का सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव
आज खड़ी बोली—
- सरकारी कार्यालयों
- न्यायालय
- मीडिया
- शिक्षा
- साहित्य
- सार्वजनिक संवाद
में सबसे व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है।
आधुनिक हिंदी और उर्दू पर प्रभाव
- उर्दू में नस्तालीक लिपि के साथ खड़ी बोली का संरचनात्मक ढांचा
- हिंदी में देवनागरी लिपि के साथ मानकीकरण
- दोनों भाषाओं के साहित्य, पत्रकारिता और संवाद में समान व्याकरणिक आधार
इस प्रकार खड़ी बोली केवल एक बोली नहीं, बल्कि दो बड़ी आधुनिक भाषाओं की जड़ है।
खड़ी बोली और संबंधित भाषाएँ
खड़ी बोली के आसपास कई निकट-सम्बद्ध भाषाएँ व बोलियाँ विकसित हुईं—
- ब्रजभाषा
- अवधी
- भोजपुरी
- उर्दू
- मानक हिंदी
इनसे खड़ी बोली का सतत भाषिक-विनिमय चलता रहा, जिसने इसकी संरचना को समृद्ध किया।
खड़ी बोली में प्रचलित विशिष्ट शब्दावली
खड़ी बोली की स्थानीयता और बोलचाल के रंग को समझने के लिए इसके कुछ विशिष्ट शब्द अत्यंत परिचित हैं। ये शब्द न केवल क्षेत्रीय अभिव्यक्ति को उजागर करते हैं, बल्कि भाषा की जड़ों और सांस्कृतिक धरातल को भी सामने लाते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए जा रहे हैं, जो परंपरागत रूप से खड़ी बोली के क्षेत्र में प्रचलित रहे हैं:
1. दैनिक जीवन से जुड़े सामान्य शब्द
- खाट – पारंपरिक लकड़ी की चारपाई।
- खात – खेत-खलिहान में प्रयुक्त खाद का सामान्य नाम।
- खेस – सफेद सूती कपड़ा, जिसे प्रायः शरीर ढकने या ओढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है।
- साब्बण – स्नान करने या कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त साबुन।
- सनिच्चर – स्थानीय उच्चारण में ‘शनिवार’ का रूप।
- सकूटर – स्कूटर के लिए बोली जाने वाली आम ध्वनि-परिवर्तित संज्ञा।
- खड़ा-खाणा – टेबल पर सजे भोजन की व्यवस्था, आधुनिक अर्थ में ‘बुफे’ प्रणाली।
2. शारीरिक क्रियाओं और ध्वनियों से जुड़े शब्द
- खड़का – किसी भी प्रकार की आवाज़, हल्की-सी टकराहट या शोर का बोध कराता शब्द।
- खाँस्सी / खुर्रा – खाँसी के लिए प्रयुक्त ग्रामीण-सहज रूप।
3. पारिवारिक व सांस्कृतिक सन्दर्भ
- साळिगिराम – बोलचाल में पत्नी के भाई के लिए प्रयोग होने वाला संबोधन।
- साईं – काजल के लिए प्रयुक्त स्थानीय शब्द, विशेषकर पुराने ग्रामीण क्षेत्रों में।
4. विशिष्ट और कम प्रचलित रूप
- खीस – गाय या भैंस के बछड़ा जनने के तुरंत बाद निकलने वाला पीला गाढ़ा द्रव्य, जिसे कई स्थानों पर औषधीय माना जाता है।
- सांक्कळ – दरवाज़ा बंद करने के लिए चिटकनी या लोहे की ज़ंजीर।
- सपा – स्वच्छ या साफ़ होने की स्थिति को दर्शाने वाला शब्द।
- सरभंग होणा – नैतिकता या आचरण से पूरी तरह च्युत होने के भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा।
भारतेंदु हरिश्चंद्र और खड़ी बोली की भाषा-जागृति
खड़ी बोली के साहित्यिक विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने न केवल आधुनिक हिन्दी गद्य को नई दिशा दी, बल्कि काव्य के माध्यम से भी मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसकी स्वभाषा के संवर्धन पर ही आधारित होती है। इसी भावना को व्यक्त करने वाली उनकी सुप्रसिद्ध कविता आधुनिक हिन्दी के भाषा-चेतना आंदोलन की आधारशिला मानी जाती है।
भारतेंदु मनुष्य और समाज दोनों की उन्नति को भाषा से जुड़ा हुआ मानते हैं। वे कहते हैं कि विदेशी भाषाएँ सीखना उपयोगी अवश्य है, परंतु यदि व्यक्ति अपनी भाषा के ज्ञान से ही वंचित हो जाए तो यह एक प्रकार का सांस्कृतिक खोखलापन बन जाता है। शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान और विद्या की वास्तविक चमक तभी आती है जब वह अपनी भाषा में समझी और आत्मसात् की जा सके।
इसी भावना को उन्होंने कविता में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है—
“निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।
अंग्रेज़ी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन
पै निज भाषाज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।।
उन्नति पूरी है तबहिं जब घर उन्नति होय
निज शरीर उन्नति किये, रहत मूढ़ सब कोय।।
वे आगे यह स्पष्ट करते हैं कि भाषा केवल बोलने का साधन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली कड़ी है। यदि घर-परिवार के लोग एक ही भाषा और एक ही विचारधारा से जुड़े हों, तभी समाज में बौद्धिक और सांस्कृतिक मजबूती आती है। यही कारण है कि वे भाषा एकता को राष्ट्रीय उन्नति का मूल मानते हैं—
“निज भाषा उन्नति बिना, कबहुँ न ह्यैहैं सोय
लाख उपाय अनेक यों भले करो किन कोय।।
इक भाषा इक जीव इक मति सब घर के लोग
तबै बनत है सबन सों, मिटत मूढ़ता सोग।।”
भारतेंदु यह भी कहते हैं कि अपनी भाषा में विद्या की चर्चा करने से ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचता है। अन्य भाषाओं में उपलब्ध शिक्षा का मूल्य तभी है जब उसे अपनी भाषा के माध्यम से समाज तक ले जाया जाए—
“और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात
निज भाषा में कीजिए, जो विद्या की बात।।
तेहि सुनि पावै लाभ सब, बात सुनै जो कोय
यह गुन भाषा और महं, कबहूं नाहीं होय।।
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार
सब देसन से लै करहू, भाषा माहि प्रचार।।”
देश की भाषाई विविधता और उससे उत्पन्न जटिलताओं पर भी भारतेंदु ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके अनुसार, भारत में मत, परंपरा और भाषा की बहुलता के कारण कई तरह के सामाजिक-भाषाई संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि एक साझा भाषा—विशेषकर देशज, सरल और समझने में सुगम भाषा—को विकसित किया जाए। उनकी दृष्टि में खड़ी बोली ने यही भूमिका निभाई—
“भारत में सब भिन्न अति, ताहीं सों उत्पात
विविध देस मतहू विविध, भाषा विविध लखात।।
सब मिल तासों छाँड़ि कै, दूजे और उपाय
उन्नति भाषा की करहु, अहो भ्रातगन आय।।’’
भारतेंदु की यह कविता न केवल भाषा-प्रेम की घोषणा है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि खड़ी बोली क्यों आधुनिक हिन्दी की आधारशिला बनी। उन्होंने इसे मात्र साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंतन और सांस्कृतिक जागरण का माध्यम बनाया। इसी कारण उनका यह काव्य आधुनिक हिन्दी के इतिहास में विशेष स्थान रखता है।
निष्कर्ष
खड़ी बोली भारतीय भाषाई संस्कृति की एक केंद्रीय धुरी है। इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई, परंतु इसका विकास आधुनिक हिंदी-उर्दू के रूप में सबके सामने है। इसकी ध्वनि- संरचना, व्याकरणिक लचीलापन, सादगी और स्पष्टता ने इसे आधुनिक भारत की सबसे उपयुक्त संप्रेषणीय भाषा बनाया।
साहित्य में ‘प्रिय प्रवास’ के माध्यम से इसका काव्यात्मक स्वरूप स्थापित हुआ। प्रशासन और शिक्षा में यह मानकीकृत रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा बन गई। दिल्ली से लेकर मेरठ, सहारनपुर, हरिद्वार तथा अंबाला तक इसका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र इसे उत्तर भारत की एक सशक्त भाषायी पहचान देता है।
आज खड़ी बोली न केवल हिंदी-उर्दू की आधारभूत संरचना का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि आधुनिक भारत की भाषायी एकता का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है।
खड़ी बोली का इतिहास भारतीय भाषिक विकास की एक दीर्घ, बहुप्रवाह और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध यात्रा का परिचायक है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी प्राचीन भाषाओं की निरंतर परंपरा से विकसित होकर यह बोली दिल्ली-Meerut क्षेत्र की जनभाषा बनी और कालांतर में आधुनिक हिन्दी तथा उर्दू—दोनों की आधारशिला सिद्ध हुई। इसके स्वरूप, नामकरण और उद्भव को लेकर विद्वानों में अनेक मत अवश्य मिलते हैं, परंतु एक बात स्पष्ट है कि खड़ी बोली किसी एक व्यक्ति, एक शासन या एक युग की देन नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का संयुक्त परिणाम है।
मुस्लिम शासनकाल में यह बोली फारसी और अरबी शब्दों से मिश्रित होकर उर्दू के रूप में विकसित हुई, जबकि भारतीय परंपरा में संस्कृतनिष्ठ रूप ने आधुनिक हिन्दी को जन्म दिया। बाद के काल में लल्लूलाल, सदल मिश्र, मुंशी सदासुखलाल, इंशा, राजा शिवप्रसाद और विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे साहित्यकारों ने इसे गद्य और पद्य की प्रतिष्ठित भाषा बनाने में निर्णायक योगदान दिया। भारतेंदु की भाषा-जागरण संबंधी कविता से स्पष्ट होता है कि खड़ी बोली केवल भाषाई साधन नहीं, बल्कि सामाजिक उन्नति और राष्ट्रीय चेतना का आधार भी रही।
खड़ी बोली की अपनी विशिष्ट शब्द-संपदा, सहज संरचना, स्पष्ट उच्चारण और व्यावहारिकता ने इसे उत्तरी भारत के सांस्कृतिक जीवन का स्वाभाविक भाषिक माध्यम बनाया। आज आधुनिक हिन्दी साहित्य, संवाद, मीडिया और शिक्षा—सबकी नींव इसी बोली पर टिकी है। यह कहना उचित है कि खड़ी बोली का विकास भारतीय समाज की एकता, सांस्कृतिक संगति और भाषिक परिपक्वता का महत्वपूर्ण दर्पण है।
समग्र रूप से देखा जाए, तो खड़ी बोली केवल एक बोली नहीं, बल्कि भारत की बहुभाषी आत्मा को जोड़ने वाला वह सशक्त सेतु है, जिसने हिन्दी को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया और उर्दू को विशिष्ट साहित्यिक पहचान दी। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही इसे भारतीय भाषाओं में अद्वितीय बनाती है।
इन्हें भी देखें –
- कौरवी बोली और नगरी (नागरी) बोली : उद्भव, क्षेत्र, विशेषताएँ और आधुनिक हिन्दी पर प्रभाव
- हरियाणी (हरियाणवी) बोली : इतिहास, क्षेत्र, भाषिक विशेषताएँ, शब्दकोश, साहित्य और संस्कृति
- सप्तक के कवि : तार सप्तक से चौथा सप्तक | हिंदी साहित्य की नयी धारा का ऐतिहासिक विकास
- भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक | Darshan & Pravartak
- गुरु-शिष्य परम्परा: भारतीय संस्कृति की आत्मा और ज्ञान की धरोहर
- नाट्यशास्त्र : उद्भव, विकास, अध्याय, टीकाएँ एवं भारतीय नाट्य परम्परा
- सरस्वती पत्रिका : इतिहास, संपादक और संपादन काल
- हिंदी ध्वनियों (वर्णों) के उच्चारण स्थान, वर्गीकरण एवं विशेषतायें
- हिंदी भाषा के स्वर : परिभाषा, प्रकार और भेद
- हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह : अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलन्त | परिभाषा, प्रयोग एवं महत्व
- हिंदी वर्णमाला में व्यंजन : परिभाषा, प्रकार और भेद