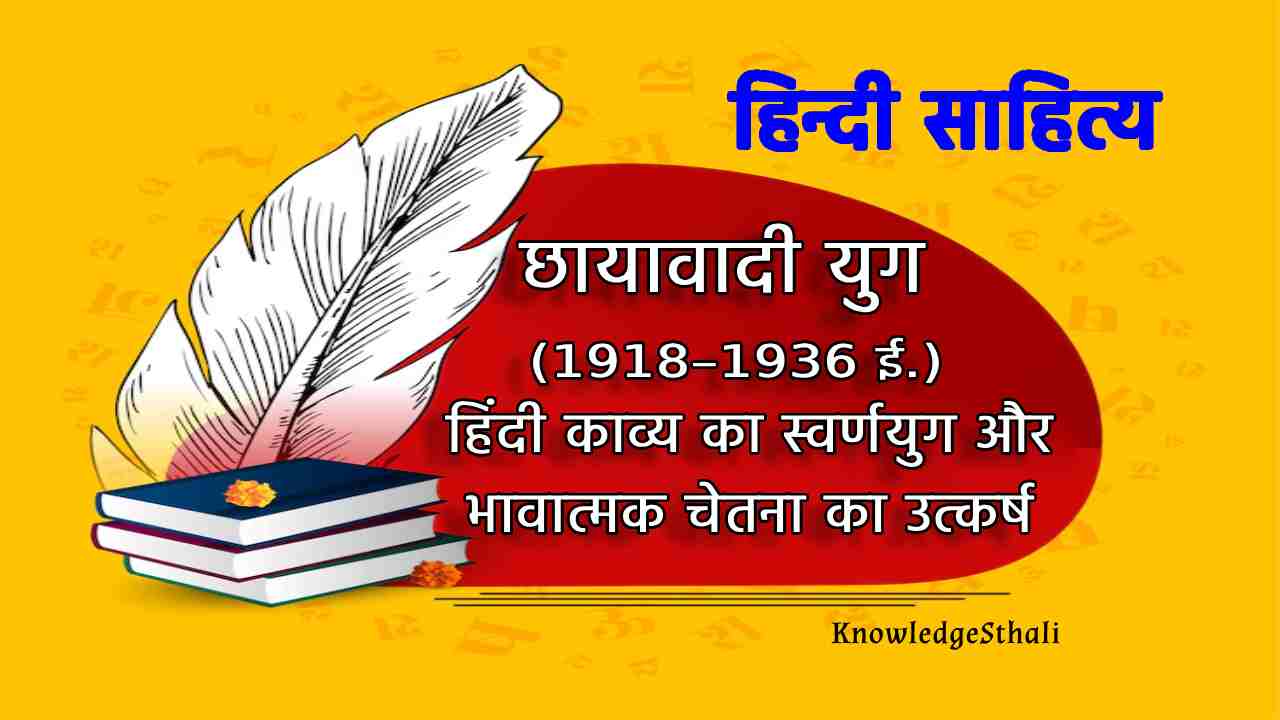हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक युगों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक युग अपनी विशिष्ट विशेषताओं, प्रवृत्तियों और साहित्यिक दृष्टिकोणों के लिए जाना जाता है। इस क्रम में 1918 ई० से 1936 ई० तक का समय छायावादी युग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। छायावाद ने हिंदी काव्य को केवल रूपगत या भाषा संबंधी नहीं, बल्कि भावनात्मक, दार्शनिक और कलात्मक दृष्टि से भी एक नई ऊँचाई दी। यह युग “द्विवेदी युग” की औपचारिकता और नैतिक आग्रहों से आगे बढ़कर आत्मानुभूति, सौंदर्यबोध, रहस्यवाद और प्रकृति की भावनात्मक अनुभूति की ओर प्रवृत्त हुआ।
इस लेख में हम छायावाद के अर्थ, इसकी विशेषताओं, प्रमुख कवियों, इस युग के अन्य साहित्यकारों और हिंदी साहित्य पर इसके प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे।
छायावादी युग (1918 ई.–1936 ई.)
हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ कविता ने पारंपरिक बंधनों से मुक्त होकर आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यबोध और भावनात्मक गहराई की नई दिशाएँ प्राप्त कीं। यह युग न केवल भावप्रवणता का प्रतीक बना, बल्कि उसमें मानव आत्मा की गूढ़ गहराइयों, प्रकृति की आत्मीयता, नारी की स्वतंत्र चेतना तथा रहस्यबोध की अभिव्यक्ति ने कविता को एक गहन आंतरिक स्वर प्रदान किया।
छायावादी कवि ‘मैं’ के माध्यम से अपने निजी अनुभवों को सार्वभौमिक बना देने में समर्थ रहे। इस काल में कविता आत्मपरकता से अनुप्राणित हुई और सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति का स्वर मुखर हुआ। प्रकृति के साथ एक गहरा आत्मिक संबंध स्थापित करते हुए कवियों ने उसमें मानवीय अनुभूतियों को प्रतिबिंबित किया।
इस युग में नारी का चित्रण भी विशुद्ध सौंदर्य या श्रृंगार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह संवेदनशीलता, आत्मबल और स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतीक बनकर सामने आई। साथ ही, रहस्यवाद ने कविता को गूढ़ गहराइयों से जोड़ा, जहाँ अज्ञात और असीम के प्रति जिज्ञासा स्पष्ट रूप से झलकती है।
छायावादी युग केवल आत्मलीनता तक सीमित न रहकर सांस्कृतिक चेतना और मानवीय संवेदना को भी उजागर करता है। भाषा की दृष्टि से यह काल अत्यंत परिमार्जित, कोमल-कांत पदावली से युक्त तथा अलंकारिक अभिव्यक्ति का काल रहा। कवियों ने पारंपरिक छंदों के साथ-साथ मुक्तछंद और विविध काव्यरूपों का भी नवाचारपूर्ण प्रयोग किया।
छायावाद का उद्भव और समयसीमा
हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी युग (1918–1936) एक ऐसा समय था, जिसने कविता को एक नया स्वरूप, नई संवेदना और नई भाषा दी। इस युग को हिंदी का “स्वर्ण युग” भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में हिंदी कविता में वह भावप्रवणता, सौंदर्यबोध और व्यक्तिवाद आया जिसने इसे विश्व साहित्य के समकक्ष खड़ा कर दिया। छायावाद ने हिंदी कविता को न केवल विषयवस्तु में नया आयाम दिया, बल्कि उसकी भाषा, शिल्प और प्रस्तुति में भी मौलिकता का संचार किया।
छायावाद का अर्थ और परिभाषा
छायावाद शब्द को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने छायावाद के अलग-अलग अर्थ प्रस्तुत किए हैं। यह भिन्नता ही इस शब्द के गूढ़ और बहुआयामी स्वरूप को दर्शाती है।
- मुकुटधर पांडे: “रहस्यवाद” के रूप में
- सुशील कुमार: “अस्पष्टता” के रूप में
- महावीर प्रसाद द्विवेदी: “अन्योक्ति पद्धति” के रूप में
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल: “शैली बैचित्र्य”
- नंददुलारे वाजपेयी: “आध्यात्मिक छाया का भान”
- डॉ. नगेंद्र: “स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह”
इन सभी मतों से यह स्पष्ट होता है कि छायावाद केवल एक काव्य शैली नहीं, बल्कि एक आंतरिक भावजगत की प्रस्तुति है जहाँ कवि अपने मन के कोमलतम भावों को रूपायित करता है।
नामवर सिंह के शब्दों में –
“छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा की उन कविताओं का द्योतक है, जो 1918 ई. से 1936 ई. (‘उच्छवास’ से ‘युगांत’) तक लिखी गईं।”
छायावाद का मूल भाव व्यक्ति की आंतरिकता, रहस्यात्मकता और प्रकृति के प्रति आत्मीय दृष्टिकोण में निहित है। यह द्विवेदी युग की तर्कशील और नैतिकतावादी प्रवृत्तियों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी।
छायावाद की पृष्ठभूमि
द्विवेदी युग (1900–1918) हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना, सुधारवाद और यथार्थवाद का युग था। यह समय नैतिक और राष्ट्रीय विचारों का था, लेकिन इसमें काव्यात्मकता और भावनात्मकता का अभाव था। यही कारण है कि 1918 के आसपास कविता ने यथार्थवाद से हटकर सौंदर्यबोध, व्यक्तिवाद और प्रकृति की ओर लौटना शुरू किया।
छायावाद इसी पृष्ठभूमि में एक काव्यात्मक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ।
छायावाद: द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया और नवीन काव्य चेतना का उदय
हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद एक ऐसा युग रहा है जिसने कविता को बाह्य यथार्थ से हटाकर आंतरिक अनुभूतियों, प्रकृति, रहस्य और सौंदर्य की ओर उन्मुख किया। यह युग “द्विवेदी युग” के पश्चात आरंभ हुआ और हिंदी कविता को एक नया आयाम प्रदान किया।
बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध को छायावाद का उत्कर्षकाल माना जाता है। इस कालखंड को जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों का युग कहा जाता है। इन कवियों को छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ माना जाता है, जिन्होंने हिंदी कविता को आत्मा की गहराइयों तक पहुँचाया।
छायावाद की उत्पत्ति दरअसल द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के रूप में हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में जहाँ कविता में नैतिकता, उपदेशात्मकता और सामाजिक सरोकारों की प्रधानता थी, वहीं छायावादी युग में कवियों ने स्वयं की अनुभूतियों, व्यक्तिगत भावनाओं और प्रकृति के सजीव चित्रण को प्रमुखता दी।
प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह के अनुसार, “छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह उन समस्त कविताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो 1918 ई० से 1936 ई० (प्रसाद की उच्छवास से पंत की युगान्त) के बीच लिखी गईं।”
छायावादी कविता को सामान्यतः ऐसी कविता कहा जा सकता है जिसमें भावों की छाया किसी और दिशा में पड़ती है – यानि कहा कुछ और जाता है लेकिन अर्थ की गहराई में कुछ और अनुभूति समाहित होती है। जैसे कि सुमित्रानंदन पंत की निम्न पंक्तियाँ:
“कहो कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोयी, अहा
तुम्हें भी त्याग गया क्या अलि नल-सा निष्ठुर कोई।”
यहाँ प्रतीकात्मक भाषा में नारी स्वातंत्र्य और त्याग की पीड़ा व्यक्त होती है, जो छायावादी शैली की विशेषता है।
इस युग में कविता के अंतरंग और बहिरंग दोनों में परिवर्तन आया। अब वस्तु निरूपण के स्थान पर अनुभूति निरूपण महत्वपूर्ण हो गया। गद्य गीत, भाव तरलता, रहस्यात्मकता, मर्मस्पर्शी कल्पना, प्रकृति की जीवंतता, स्वतंत्र चिंतन और राष्ट्रभक्ति – यह सब छायावादी युग की विशिष्ट पहचान बन गए।
छायावाद ने कविता को न केवल भावनात्मक ऊँचाई दी, बल्कि उसे कलात्मक गहराई भी प्रदान की। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा, पंत की पल्लव और महादेवी वर्मा की यामा जैसी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को एक नया सौंदर्यबोध दिया।
इस प्रकार, छायावाद ने द्विवेदी युग के बौद्धिक अनुशासन के स्थान पर मानसिक स्वतंत्रता, कलात्मक प्रयोग और आत्मिक संवेदना की स्थापना की, जो आगे चलकर हिंदी कविता की विविध धाराओं का आधार बनी।
सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियाँ:
“कहो कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोयी, अहा
तुम्हें भी त्याग गया क्या अलि नल-सा निष्ठुर कोई।”
— सुमित्रानंदन पंत
इन पंक्तियों का अर्थ:
कवि एक स्त्री से (या स्त्री की छवि से) पूछते हैं —
“कहो, तुम कौन हो जो इस पेड़ के नीचे दमयंती जैसी प्रतीत हो रही हो, क्या तुम्हें भी किसी नल जैसे प्रियजन ने त्याग दिया है?”
यहाँ “दमयंती” और “नल” महाभारत से लिए गए प्रसिद्ध पौराणिक पात्र हैं। दमयंती एक अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थीं, जिन्हें उनके पति नल ने एक समय विपत्ति में त्याग दिया था।
संपूर्ण भावार्थ:
कवि ने जिस स्त्री को देखा है, वह दुख, पीड़ा और त्याग की मूर्ति लग रही है। उसकी स्थिति देखकर कवि को दमयंती की याद आ जाती है। वह पूछते हैं —
क्या तुम्हें भी किसी निष्ठुर (निर्दयी) प्रिय ने त्याग दिया है, जैसे कभी नल ने दमयंती को?
यह पंक्ति नारी की पीड़ा, त्याग, और अंतर्मन की वेदना का प्रतीक है। साथ ही, यह छायावादी काव्य की विशेषता — प्रतीकात्मकता, कल्पनाशीलता और भावात्मकता — को भी उजागर करती है।
निहितार्थ (गहराई में):
- यह पंक्तियाँ नारी स्वातंत्र्य, विरह वेदना, और सहानुभूति के भावों को व्यक्त करती हैं।
- यहाँ “छाँह में विश्राम करती नारी” वस्तुतः त्याग और संवेदना की मूर्ति है, जो सामाजिक यथार्थ और भावनात्मक गहराई दोनों को छूती है।
यह छायावादी काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है जहाँ प्रकृति, इतिहास, और आत्म-भावना एक साथ एक सशक्त चित्र में सन्निविष्ट हो जाते हैं।
छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ: कवि और उनकी रचनाएँ
1. जयशंकर प्रसाद (1889 – 1937)
विशेषताएँ: रहस्यवाद, इतिहासबोध, सांस्कृतिक चेतना, गहन भावनात्मकता, सौंदर्योपासना, गहन दार्शनिकता।
प्रमुख रचनाएँ:
- कामायनी (महाकाव्य)
- आँसू, झरना, आलोक, लहर (काव्य संग्रह)
- कंकाल, तितली (उपन्यास)
- चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी (नाटक)
प्रसिद्ध पंक्ति:
“अरुण यह मधुमय देश हमारा।”
योगदान: छायावाद को गूढ़ता, दार्शनिक गहराई और ऐतिहासिक संदर्भ देने वाले जयशंकर प्रसाद ने काव्य के साथ-साथ नाटक, उपन्यास और निबंध में भी छायावाद की भावभूमि को प्रतिष्ठित किया।
2. सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ (1896 – 1961)
विशेषताएँ: विद्रोहात्मकता, विद्रोही भाव, शोषण के प्रति आक्रोश, प्रकृति का सजीव चित्रण, आत्मचेतना, शिल्प प्रयोग।
प्रमुख रचनाएँ:
- परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, गीतिका (काव्य संग्रह)
- तुलसीदास, बिल्लेसुर बकरिहा (उपन्यास)
- प्रभा, चोटी की पकड़ (कहानी)
- राम की शक्ति पूजा (नाटकात्मक काव्य)
प्रसिद्ध पंक्ति:
“वह तोड़ती पत्थर।”
योगदान: निराला ने छायावाद को परंपरा से जोड़ने के साथ-साथ उसे सामाजिक चेतना और विद्रोह की दिशा भी प्रदान की। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं।
3. सुमित्रानंदन पंत (1900 – 1977)
विशेषताएँ: प्रकृति के प्रति अनुराग, सौंदर्यबोध, आध्यात्मिक चिंतन।
प्रमुख रचनाएँ:
- पल्लव, गुंजन, युगांत, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चाँद
प्रसिद्ध पंक्ति:
“चमक उठी सुन्दरता जग में।”
योगदान: पंत जी की कविता में सौंदर्य और प्रकृति की लय है। वे छायावादी काव्य के सच्चे सौंदर्योपासक माने जाते हैं। उनके काव्य में गूढ़ दार्शनिकता भी मिलती है।
4. महादेवी वर्मा (1907 – 1987)
विशेषताएँ: करुणा, वेदना, त्याग, आत्मसंवेदना की तीव्रता, नारी-संवेदना।
प्रमुख रचनाएँ:
- नीहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा (काव्य)
- स्मृति की रेखाएँ, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ (निबंधात्मक गद्य)
प्रसिद्ध पंक्ति:
“यह जीवन पथ का मेरा पथिक अकेला।”
योगदान: महादेवी वर्मा छायावादी युग की एकमात्र प्रमुख महिला कवयित्री थीं। उन्होंने नारी संवेदना, वेदना की कोमल अभिव्यक्ति और आत्मपीड़ा को काव्य का विषय बनाया। वे “छायावाद का मूल स्वर” मानी जाती हैं।
छायावाद के प्रमुख कवि और उनसे प्रभावित रचनाकार
छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं —
जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा।
इन चारों कवियों ने छायावाद की कोमलता, रहस्यात्मकता, सौंदर्यबोध, और आत्म-अनुभूति को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त कर इस युग को साहित्यिक ऊँचाइयाँ प्रदान कीं।
इनमें महादेवी वर्मा को छायावाद का “मूल स्वर” कहा जाता है क्योंकि उन्होंने छायावाद की मूल अवधारणाओं — आत्मिक पीड़ा, करुणा, और भावात्मक सूक्ष्मता — को सबसे गहराई से जिया और प्रस्तुत किया।
छायावाद का प्रभाव केवल इन चार कवियों तक सीमित नहीं रहा। कई अन्य कवियों ने भी इससे प्रेरणा पाई और छायावादी प्रवृत्तियों को अपनाया:
- रामकुमार वर्मा — प्रारंभिक छायावादी रचनाओं के बाद नाटक विधा की ओर उन्मुख होकर प्रसिद्ध नाटककार बने।
- माखनलाल चतुर्वेदी — उनके काव्य में छायावाद की सौंदर्य चेतना के साथ-साथ राष्ट्रवाद का भी गहरा प्रभाव रहा।
- हरिवंशराय बच्चन — उन्होंने छायावादी भावभूमि पर प्रेम और वेदना को गहराई से प्रस्तुत किया, विशेषतः मधुशाला में।
- रामधारी सिंह ‘दिनकर’ — प्रारंभिक रचनाओं में छायावाद का प्रभाव रहा, परंतु बाद में वे राष्ट्रवाद और वीर रस के प्रवक्ता बन गए।
इनके अतिरिक्त भी कई अन्य कवि इस युग से प्रभावित हुए, जैसे:
- हरिकृष्ण ‘प्रेमी’
- जानकी वल्लभ शास्त्री
- भगवतीचरण वर्मा
- उदयशंकर भट्ट
- नरेंद्र शर्मा
- रामेश्वर शुक्ल ‘अंचल’
इन सभी ने छायावादी भावबोध — जैसे प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, भावनात्मक सूक्ष्मता — को अपने काव्य में स्थान दिया। कुछ ने इसे आत्माभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण किया, तो कुछ ने इसे सामाजिक संदर्भों से जोड़ते हुए आगे बढ़ाया।
इस प्रकार छायावाद केवल एक काव्य प्रवृत्ति नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक साहित्यिक चेतना बना जिसने हिंदी साहित्य के विविध रचनाकारों को प्रभावित किया और उन्हें स्वानुभूति के धरातल पर रचना करने की प्रेरणा दी।
रचना की दृष्टि से छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार
छायावादी युग केवल काव्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस कालखंड में साहित्य की लगभग सभी विधाओं — आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध — में रचनात्मक उन्नयन हुआ। इस युग के रचनाकारों ने छायावादी भावभूमि को विभिन्न साहित्यिक रूपों में व्यक्त कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत है रचना की दृष्टि से छायावादी युग के प्रमुख रचनाकारों का वर्गीकरण:
1. समालोचक / आलोचक
छायावाद की समीक्षा और मूल्यांकन करने वाले विद्वान आलोचकों ने इस युग की गहराई और विशेषताओं को उजागर किया:
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल
- पद्म सिंह शर्मा
- विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
- श्यामसुंदर दास
- डॉ. रामकुमार वर्मा
- डॉ. रामरतन भटनागर
इन आलोचकों ने छायावादी काव्य की आलोचना, विवेचन और विवेचना के माध्यम से इसके स्वरूप और महत्व को स्थापित किया।
2. कहानी लेखक
छायावादी युग के दौरान हिंदी कहानी साहित्य में भी भावनात्मक गहराई और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का विकास हुआ। प्रमुख कहानीकार इस प्रकार हैं:
- मुंशी प्रेमचंद
- जयशंकर प्रसाद
- सुमित्रानंदन पंत
- सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’
- गुलेरी
- सुदर्शन
- विनोद शंकर व्यास
- जैनेंद्र कुमार
- हृदयेश
- कौशिक
इन लेखकों की कहानियाँ छायावादी भावबोध से अनुप्राणित थीं — जिनमें भावुकता, आत्मवेदना और मानव मन की सूक्ष्म परतों का चित्रण हुआ।
3. उपन्यासकार
छायावादी युग के उपन्यासकारों ने उपन्यास को यथार्थ से जोड़ने के साथ-साथ आत्मचेतना और मनोवैज्ञानिक गहराई की दिशा में भी अग्रसर किया:
- प्रेमचंद
- जयशंकर प्रसाद
- उग्र
- जैनेंद्र कुमार
- हृदयेश
- प्रतापनारायण श्रीवास्तव
- भगवतीचरण वर्मा
- वृंदावनलाल वर्मा
- गुरुदत्त
इन उपन्यासों में समाज, इतिहास, व्यक्ति, मन और अंतर्द्वंद्व को बड़ी ही सूक्ष्मता और कलात्मकता से प्रस्तुत किया गया है।
4. नाटककार
छायावादी युग का नाट्य साहित्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद द्वारा हिंदी नाटकों को एक नया संस्कृतिक और काव्यात्मक आयाम मिला। अन्य प्रमुख नाटककार हैं:
- जयशंकर प्रसाद
- सेठ गोविंद दास
- गोविंद वल्लभ पंत
- लक्ष्मीनारायण मिश्र
- उदयशंकर भट्ट
- रामकुमार वर्मा
इन नाटकों में इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना, और मानवीय भावनाओं का सशक्त समावेश देखने को मिलता है।
5. निबंध लेखक
छायावादी युग में निबंध साहित्य भी भावात्मक और विचारप्रधान बनकर उभरा। इस समय के निबंधकारों ने भाषा की कोमलता और शैली की कलात्मकता को अपनाया:
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
- रामचंद्र शुक्ल
- माधव प्रसाद शुक्ल
- बाबू श्यामसुंदर दास
- पद्म सिंह
- अध्यापक पूर्णसिंह
इन लेखकों ने साहित्य, समाज, संस्कृति और मानव मन की जटिलताओं पर गहन विचार प्रस्तुत किए।
छायावादी युग ने हिंदी साहित्य को केवल कविता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि साहित्य की विविध विधाओं में भावात्मकता, सौंदर्यबोध, रहस्यवाद, और आत्माभिव्यक्ति की गहरी छाप छोड़ी। यह युग एक बहुआयामी रचनात्मक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने हिंदी साहित्य को भावात्मक गहराई और कलात्मक ऊँचाई प्रदान की।
छायावादी युग के कवि और उनकी प्रमुख काव्य रचनाएँ
छायावादी युग (1918–1936 ई.) में हिंदी कविता ने आत्मानुभूति, सौंदर्यबोध, रहस्यवाद और प्रकृति की ओर उन्मुख होकर एक नवीन संवेदना का सृजन किया। इस युग के प्रमुख कवियों ने अपनी विशिष्ट रचनाओं के माध्यम से इस युग को एक सशक्त साहित्यिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। साथ ही, कुछ रचनाकारों ने ब्रजभाषा में भी रचनाएँ कर छायावादी चेतना को परंपरा से जोड़ने का कार्य किया।
1. छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ
जयशंकर प्रसाद (1889–1936 ई.)
- चित्राधार (ब्रज भाषा में रचित कविताएँ)
- कानन-कुसुम
- महाराणा का महत्त्व
- करुणालय
- झरना
- आंसू
- लहर
- कामायनी (महाकाव्य)
सुमित्रानंदन पंत (1900–1977 ई.)
- वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी
- ग्राम्या, स्वर्ण-किरण, स्वर्ण-धूलि, युगान्तर
- उत्तरा, रजत-शिखर, शिल्पी, प्रतिमा, सौवर्ण
- वाणी, चिदंबरा, रश्मिबंध, कला और बूढ़ा चाँद
- अभिषेकित, हरीश सुरी सुनहरी टेर, लोकायतन, किरण वीणा
सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ (1898–1961 ई.)
- अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना
- कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना
महादेवी वर्मा (1907–1988 ई.)
- रश्मि, निहार, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा
2. अन्य छायावादी कवि और रचनाएँ
डॉ. रामकुमार वर्मा
- अंजलि, रूपराशि, चितौड़ की चिता, चंद्रकिरण
- अभिशाप, निशीथ, चित्ररेखा, वीर हमीर, एकलव्य
हरिकृष्ण ‘प्रेमी’
- आँखों में, अनंत के पथ पर, रूपदर्शन
- जादूगरनी, अग्निगान, स्वर्णविहान
3. ब्रजभाषा में छायावादी रचनाएँ
छायावादी युग में मुख्य रूप से खड़ी बोली में काव्य रचना हुई, लेकिन कुछ रचनाकार ऐसे भी थे जिन्होंने ब्रजभाषा की समृद्ध परंपरा को जीवित रखते हुए छायावादी चेतना को उसके माध्यम से व्यक्त किया।
भारतेंदु युग में ब्रजभाषा का व्यापक प्रयोग हुआ था, परंतु छायावादी युग में यह गौण रूप में उपस्थित रही। इन कवियों का मत था कि ब्रजभाषा की लंबी काव्य परंपरा ने उसे काव्य के लिए स्वाभाविक भाषा बना दिया है।
प्रमुख ब्रजभाषा रचनाकार और रचनाएँ:
- रामनाथ जोतिषी – रामचंद्रोदय
- रामकथा पर आधारित यह रचना युगबोध के अनुसार है और इसमें रामचंद्रिका (केशवदास) का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें विभिन्न छंदों का सफल प्रयोग हुआ है।
- रामचंद्र शुक्ल – बुद्धचरित
- यह “लाइट ऑफ़ एशिया” का भावानुवाद है, जो सरल और व्यावहारिक भाषा में लिखा गया है। शुक्ल जी मूलतः आलोचक थे।
- राय कृष्णदास – ब्रजरस
- यह ब्रजभाषा में रचित एक उल्लेखनीय काव्य है।
- जगदंबा प्रसाद मिश्र ‘हितैषी’ – कवित्त-सवैये
- ब्रज छंदों में सशक्त रचना।
- दुलारे लाल भार्गव – दुलारे-दोहावली
- दोहा छंद में रचित ब्रजभाषा काव्य।
- वियोगी हरि – वीर सतसई
- इसमें राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है।
- बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ – ऊर्म्मिला
- यह महाकाव्य उर्मिला के उज्ज्वल चरित्र को केंद्र में रखकर रचा गया है। इसमें ब्रजभाषा का वैशिष्ट्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।
- अनूप शर्मा – फेरि-मिलिबो (1938)
- यह चंपू काव्य कुरुक्षेत्र में राधा-कृष्ण के पुनर्मिलन पर आधारित है, जो अत्यंत मार्मिक है।
- रामेश्वर ‘करुण’ – करुण-सतसई (1930)
- इसमें करुणा, अनुभूति की तीव्रता और व्यंग्य की सशक्त उपस्थिति है।
- किशोरीदास वाजपेयी – तरंगिणी
- इसमें प्राचीनता और नवीनता का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है।
- उमाशंकर वाजपेयी ‘उमेश’
- उनकी रचनाओं में भाषा और संवेदना की दृष्टि से नवीनता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।
इन कवियों की रचनाओं में छायावाद की सूक्ष्म भावभूमि, अनुभूति की तीव्रता और भाषा की कलात्मकता विद्यमान है। यदि ब्रजभाषा में काव्य रचना का परिमाण अधिक होता, तो यह काल ब्रजभाषा का छायावाद कहा जा सकता था। फिर भी, इन रचनाओं ने छायावादी चेतना को परंपरा से जोड़कर साहित्यिक समृद्धि में योगदान दिया।
छायावादी युग में ब्रजभाषा काव्य की परंपरा और योगदान
छायावादी युग (1918–1936 ई.) मुख्यतः खड़ी बोली हिंदी की काव्य-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, किंतु इस युग में एक वर्ग ऐसा भी था जो ब्रजभाषा की पुरानी काव्य-धारा को जीवित रखने का प्रयास कर रहा था। सूरदास, तुलसीदास, सेनापति, बिहारी और घनानंद जैसी प्रतिभाओं से समृद्ध ब्रजभाषा को छायावादी युग के कुछ रचनाकारों ने नई चेतना के साथ अपनाया।
ब्रजभाषा की स्थिति:
भारतेंदु युग में जहाँ ब्रजभाषा में विपुल मात्रा में काव्य रचना हुई, वहीं छायावादी युग तक आते-आते वह गौण हो गई। फिर भी कुछ कवियों का यह मत था कि ब्रजभाषा की दीर्घकालीन काव्य परंपरा ने इसे साहित्य के लिए उपयुक्त बना दिया है। अतः उन्होंने इसी भाषा में छायावादी सूक्ष्मताओं को प्रकट करने का प्रयास किया।
छायावादी काव्यधारा का द्वैध रूप: प्रमुख प्रवृत्तियाँ और कवि
छायावादी युग (1918–1936 ई.) में हिंदी कविता में आत्मानुभूति, सौंदर्यबोध, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वर प्रमुखता से उभरा। इस युग के कवियों को दो प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है:
- मुख्य छायावादी काव्य धारा के कवि
- राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि
मुख्य छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं, जिन्होंने आत्माभिव्यक्ति, प्रकृति-सौंदर्य, रहस्यवाद और प्रेम जैसे तत्वों को केंद्र में रखकर छायावादी कविता की सशक्त अभिव्यक्ति की।
इस वर्ग में प्रमुख नाम हैं:
- जयशंकर प्रसाद
- सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’
- सुमित्रानंदन पंत
- महादेवी वर्मा
- राम कुमार वर्मा
- उदय शंकर भट्ट
- वियोगी
- लक्ष्मी नारायण मिश्र
- जनार्दन प्रसाद झा ‘द्विज’
दूसरी ओर, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने राष्ट्रप्रेम, स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक चेतना को प्रमुख विषय बनाया।
इस प्रवृत्ति के प्रमुख कवि हैं:
- माखन लाल चतुर्वेदी
- सिया राम शरण गुप्त
- सुभद्रा कुमारी चौहान
इन दोनों धाराओं ने मिलकर छायावादी युग को हिंदी काव्य के एक समृद्ध और बहुआयामी कालखंड के रूप में प्रतिष्ठित किया।ता आहे इन दोनों धाराओं के कवियों की रचनाओं की सूची दी गयी है –
1. मुख्य छायावादी काव्य धारा के कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएँ
| क्रम | कवि (रचनाकार) | प्रमुख रचनाएँ |
|---|---|---|
| 1. | जयशंकर प्रसाद | उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छवास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आँसू, लहर, कामायनी (झरना से कामायनी तक छायावादी कविता मानी जाती है) |
| 2. | सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ | अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा |
| 3. | सुमित्रानंदन पंत | उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन (छायावादी युगीन रचनाएँ); अन्य रचनाएँ: युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझड़, स्वर्ण काव्य, लोकायतन |
| 4. | महादेवी वर्मा | नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत – इन सभी का संकलन यामा नामक काव्य संग्रह में |
| 5. | राम कुमार वर्मा | रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा |
| 6. | उदय शंकर भट्ट | राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष |
| 7. | वियोगी | निर्माल्य, एकतारा, कल्पना |
| 8. | लक्ष्मी नारायण मिश्र | अन्तर्जगत |
| 9. | जनार्दन प्रसाद झा ‘द्विज’ | अनुभूति, अन्तर्ध्वनि |
2. राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएँ
| क्रम | कवि (रचनाकार) | प्रमुख रचनाएँ |
|---|---|---|
| 1. | माखनलाल चतुर्वेदी | कैदी और कोकिला, हिमकिरीटिनी, हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा |
| 2. | सियारामशरण गुप्त | मौर्य विजय, अनाथ, दूर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, बापू, दैनिकी |
| 3. | सुभद्राकुमारी चौहान | त्रिधारा, मुकुल, ख़ूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी, वीरों का कैसा हो वसंत |
छायावादी युग ने हिंदी काव्य को नई भावभूमि और संवेदना प्रदान की। जहाँ मुख्य छायावादी कवियों ने आत्माभिव्यक्ति और सौंदर्य चेतना को स्वर दिया, वहीं राष्ट्रवादी कवियों ने सामाजिक–राजनीतिक जागरूकता के साथ भारतीय संस्कृति और स्वाधीनता आंदोलन की भावना को स्वर प्रदान किया। इन दोनों धाराओं ने मिलकर हिंदी कविता को समृद्ध और विविध रूप में प्रस्तुत किया।
छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएँ
छायावाद हिंदी काव्य का एक ऐसा युग रहा जिसमें व्यक्ति के आत्मिक स्वर को अभिव्यक्ति मिली। इस युग की सबसे विशिष्ट पहचान ‘मैं’ शैली या उत्तम पुरुष में आत्माभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से कवियों ने अपने आंतरिक भाव-जगत को मुखर किया। यह आत्माभिव्यक्ति केवल वैयक्तिक न होकर, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति और आत्म-विस्तार की चेतना से भी ओतप्रोत थी।
छायावादी कविता में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम दिखाई देता है, किंतु यह प्रेम केवल वर्णन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कवि स्वयं को प्रकृति में विलीन करते हुए उसके साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। साथ ही, इस युग की कविता में नारी प्रेम को भी एक उच्च भावभूमि प्रदान की गई है, जहाँ नारी केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं बल्कि स्वतंत्र चेतना की प्रतिनिधि बनकर उभरती है।
छायावादी काव्य में रहस्यवाद एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है, जो अज्ञात और असीम के प्रति जिज्ञासा से जुड़ा हुआ है। कवियों ने आत्मा, ईश्वर और सृष्टि के रहस्यों को अनुभूति के धरातल पर समझने का प्रयास किया।
इसके साथ ही, इस युग में सांस्कृतिक चेतना, मानवतावाद तथा सामाजिक सरोकारों की भी स्पष्ट झलक मिलती है। यद्यपि यह युग आत्म-केंद्रित रहा, फिर भी उसमें राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक गौरव के स्वर कहीं न कहीं प्रकट होते हैं।
छायावादी युग की कविता में स्वच्छंद कल्पना, विविध काव्य-रूपों का प्रयोग, तथा मुक्त छंद की प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है। प्रकृति संबंधी बिंबों की बहुलता ने इस काव्य को सौंदर्य की नवीन ऊँचाइयाँ प्रदान कीं।
भाषा की दृष्टि से छायावादी कविता में ललित-लवंगी, कोमल-कांत पदावली का प्रयोग हुआ है, जिसमें भावों की गहराई और लयात्मकता दोनों का समुचित संतुलन मिलता है। काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस युग में भारतीय अलंकारों के साथ-साथ अंग्रेजी साहित्य से प्रेरित मानवीकरण (personification) एवं विशेषण विपर्यय (Transferred Epithet) जैसे अलंकारों का भी प्रभावशाली उपयोग देखने को मिलता है।
इन समस्त विशेषताओं के कारण छायावाद को हिंदी कविता का ‘स्वर्ण युग’ कहा जाता है, जहाँ संवेदना, सौंदर्य और चेतना का त्रिवेणी संगम स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।
छायावाद युग में प्रयुक्त विविध काव्य रूप
छायावादी युग में कवियों ने काव्य-रूपों के संदर्भ में भी नवाचार किया। इस युग में न केवल भाव और विषय की विविधता दृष्टिगोचर होती है, बल्कि काव्य की शैलियों और संरचनात्मक प्रयोगों में भी नवीनता स्पष्ट होती है। कवियों ने पारंपरिक छंदबद्धता को बनाए रखते हुए भी मुक्तछंद, गीतिकाव्य, लंबी कविता तथा प्रबंध काव्य जैसे विविध रूपों में अपनी रचनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्त किया।
1. मुक्तक काव्य
छायावादी युग में मुक्तक काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य रूप रहा।
मुक्तक वह कविता होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है और जिसका अन्य छंदों से कोई पूर्वापर संबंध आवश्यक नहीं होता।
प्रत्येक छंद स्वतंत्र रूप से सम्पूर्ण अर्थ देने वाला होता है। हिंदी में कबीर, रहीम, मीराबाई आदि की रचनाओं को मुक्तक की श्रेणी में रखा जा सकता है।
रीतिकाल में भी अधिकांश कविताएँ मुक्तक रूप में रची गईं। छायावादी कवियों ने इसी परंपरा को आधुनिक संवेदना के साथ आगे बढ़ाया।
आगे “मुक्तक काव्य” की परिभाषा, स्वरूप और छायावादी युग में उसकी लोकप्रियता पर चर्चा की है। । ⬇
2. गीतिकाव्य
छायावाद में गीतिकाव्य की भी सशक्त उपस्थिति रही। इसमें भावपूर्ण, संक्षिप्त और गेय रचनाएँ होती हैं, जिनमें कोमल भावनाओं की प्रधानता होती है।
प्रमुख गीतिकाव्य रचनाएँ हैं:
- जयशंकर प्रसाद – करुणालय
- सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ – पंचवटी प्रसंग
- सुमित्रानंदन पंत – शिल्पी, सौवर्ण रजत शिखर
3. प्रबंध काव्य
प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिसमें कथा का क्रमिक विस्तार होता है तथा चरित्रों का विकास होता है।
इस शैली में प्रमुख रचनाएँ हैं:
- जयशंकर प्रसाद – कामायनी, प्रेम पथिक
- सुमित्रानंदन पंत – ग्रंथि, लोकायतन, सत्यकाम
- निराला – तुलसीदास
4. लंबी कविता
छायावादी युग में लंबी कविताओं के माध्यम से भी भावनाओं की गहराई और वैचारिकता को अभिव्यक्त किया गया।
प्रमुख लंबी कविताएँ हैं:
- प्रसाद – प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण
- निराला – सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा
- पंत – परिवर्तन
इस प्रकार छायावादी युग में काव्य रूपों की दृष्टि से भी एक उल्लेखनीय बहुविधता देखी जाती है, जो इस युग को हिंदी साहित्य में प्रयोगशीलता और सौंदर्यबोध का विशिष्ट कालखंड सिद्ध करती है।
मुक्तक काव्य की परंपरा: छायावाद से पूर्व की दृष्टि
मुक्तक काव्य का अर्थ
‘मुक्तक’ शब्द संस्कृत मूल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है — स्वतंत्र, अपने आप में पूर्ण, अथवा अन्य से असंबद्ध। काव्य के सन्दर्भ में, मुक्तक उस कविता को कहते हैं जो किसी कथा, पात्र, या अन्य छंदों से जुड़ी न होकर स्वयं में संपूर्ण हो। यह काव्य-रूप सीमित शब्दों में गहरे भावों की अभिव्यक्ति करता है।
मुक्तक काव्य की परिभाषा
मुक्तक काव्य वह काव्य-रचना है जिसमें प्रत्येक छंद अथवा पद स्वतंत्र होता है और उसका अर्थ, अभिप्राय अथवा भाव-प्रस्तुति किसी अन्य छंद या रचना पर निर्भर नहीं होता। मुक्तक काव्य में न तो कथा-क्रम की आवश्यकता होती है, न पात्रों की निरंतरता, और न ही किसी विशिष्ट संरचना की। यह शैली भाव प्रधान होती है तथा लघुता में गाम्भीर्य की विशेषता को अपने में समेटे होती है।
मुक्तक काव्य की प्रमुख विशेषताएँ
हिंदी साहित्य में मुक्तक काव्य एक ऐसी सशक्त और प्रभावशाली काव्य-शैली रही है जो अपने संक्षिप्त रूप में गहन भावाभिव्यक्ति करती है। मुक्तक काव्य वह काव्य है जिसमें प्रत्येक छंद या पद अपने आप में पूर्ण, स्वतंत्र एवं स्पष्ट अर्थ रखने वाला होता है। इसका किसी कथा, प्रसंग या अन्य छंदों से कोई तारतम्य नहीं होता। इस शैली की रचनाएँ सामान्यतः किसी एक भाव, विचार या अनुभूति की संक्षिप्त लेकिन प्रभावी प्रस्तुति करती हैं।
मुक्तक काव्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- स्वतंत्रता: प्रत्येक छंद अन्य छंदों से निरपेक्ष होता है।
- पूर्णता: हर छंद अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करता है।
- कथावाचकता का अभाव: इसमें किसी कथा, पात्र या प्रसंग का क्रमबद्ध वर्णन नहीं होता।
- भावप्रधानता: मुक्तक में विचारों, भावनाओं या अनुभूतियों की तीव्र और संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है।
हिंदी साहित्य की परंपरा में कबीर और रहीम के दोहे, मीराबाई के भजन, बिहारी सतसई, तथा संस्कृत साहित्य में कालिदास का ‘ऋतुसंहार’ और भर्तृहरि का ‘शतकत्रय’ मुक्तक काव्य के प्रसिद्ध उदाहरण माने जाते हैं। इन रचनाओं ने न केवल मुक्तक काव्य को समृद्ध किया, बल्कि छायावाद युग के कवियों को भी इस शैली की ओर प्रेरित किया।
मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य से भिन्न होता है। जहाँ प्रबंध काव्य में कथानक, चरित्र, क्रमबद्धता और विषयगत एकता प्रमुख होती है, वहीं मुक्तक काव्य अपने संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली भावपक्ष के कारण अलग पहचान रखता है। छायावाद युग में इस शैली को नया रूप मिला, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय काव्य परंपरा में गहराई तक फैली हुई थीं।
मुक्तक काव्य की परंपरा: प्रमुख रचनाएँ और रचनाकार
छायावाद से पूर्व की काव्य-परंपरा में मुक्तक शैली का व्यापक और समृद्ध विकास हुआ। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा ब्रजभाषा आदि भाषाओं में रचित अनेक काव्य-ग्रंथों में मुक्तक विधा का प्रयोग हुआ, जो स्वतंत्र छंदों के माध्यम से भाव, विचार, नीति, भक्ति एवं सौंदर्य की गहन अनुभूति कराते हैं। इन काव्यों में जीवन की विविध अनुभूतियों, रहस्यात्मक तत्वों, मानवीय भावनाओं तथा दार्शनिक दृष्टिकोण की सहज प्रस्तुति मिलती है।
नीचे प्रमुख मुक्तक काव्य रचनाएँ एवं उनके रचनाकारों की सूची दी गई है, जो मुक्तक काव्य के ऐतिहासिक विकास एवं व्यापकता को दर्शाती है और यह स्पष्ट करती है कि छायावादी युग में इस शैली की पुनर्प्राप्ति हुई।
| क्रम | रचना | रचनाकार |
|---|---|---|
| 1. | अमरुकशतक | अमरुक |
| 2. | आनन्दलहरी | शंकराचार्य |
| 3. | आर्यासप्तशती | गोवर्धनाचार्य |
| 4. | ऋतुसंहार | कालिदास |
| 5. | कलाविलास | क्षेमेन्द्र |
| 6. | गण्डीस्तोत्रगाथा | अश्वघोष |
| 7. | गांगास्तव | जयदेव |
| 8. | गाथासप्तशती | हाल |
| 9. | गीतगोविन्द | जयदेव |
| 10. | घटकर्परकाव्य | घटकर्पर या धावक |
| 11. | चण्डीशतक | बाण |
| 12. | चतुःस्तव | नागार्जुन |
| 13. | चन्द्रदूत | जम्बूकवि |
| 14. | चन्द्रदूत | विमलकीर्ति |
| 15. | चारुचर्या | क्षेमेन्द्र |
| 16. | चौरपंचाशिका | बिल्हण |
| 17. | जैनदूत | मेरुतुंग |
| 18. | देवीशतक | आनन्दवर्द्धन |
| 19. | देशोपदेश | क्षेमेन्द्र |
| 20. | नर्ममाला | क्षेमेन्द्र |
| 21. | नीतिमंजरी | द्याद्विवेद |
| 22. | नेमिदूत | विक्रमकवि |
| 23. | पञ्चस्तव | श्री वत्सांक |
| 24. | पवनदूत | धोयी |
| 25. | पार्श्वाभ्युदय काव्य | जिनसेन |
| 26. | बल्लालशतक | बल्लाल |
| 27. | भल्लटशतक | भल्लट |
| 28. | भाव विलास | रुद्र कवि |
| 29. | भिक्षाटन काव्य | शिवदास |
| 30. | मुकुन्दमाल | कुलशेखर |
| 31. | मुग्धोपदेश | जल्हण |
| 32. | मेघदूत | कालिदास |
| 33. | रामबाणस्तव | रामभद्र दीक्षित |
| 34. | रामशतक | सोमेश्वर |
| 35. | वक्रोक्तिपंचाशिका | रत्नाकर |
| 36. | वरदराजस्तव | अप्पयदीक्षित |
| 37. | वैकुण्ठगद्य | रामानुज आचार्य |
| 38. | शतकत्रय | भर्तृहरि |
| 39. | शरणागतिपद्य | रामानुज आचार्य |
| 40. | शान्तिशतक | शिल्हण |
| 41. | शिवताण्डवस्तोत्र | रावण |
| 42. | शिवमहिम्नःस्तव | पुष्पदत्त |
| 43. | शीलदूत | चरित्रसुंदरगणि |
| 44. | शुकदूत | गोस्वामी |
| 45. | श्रीरंगगद्य | रामानुज आचार्य |
| 46. | समयमातृका | क्षेमेन्द्र |
| 47. | सुभाषितरत्नभण्डागार | शिवदत्त |
| 48. | सूर्यशतक | मयूर |
| 49. | सौन्दर्यलहरी | शंकराचार्य |
| 50. | स्तोत्रावलि | उत्पलदेव |
| 51. | हंसदूत | वामनभट्टबाण |
| 52. | लाल शतक (दोहे) | अशर्फी लाल मिश्र |
इन रचनाओं ने मुक्तक शैली की विशिष्ट पहचान बनाई। संस्कृत व मध्यकालीन साहित्य में जहाँ भक्ति एवं नीति परक मुक्तकों की भरमार रही, वहीं आधुनिक युग में कबीर, रहीम, तुलसीदास, मीरा, बिहारी आदि ने हिंदी को इसकी समृद्ध परंपरा दी। यह परंपरा छायावाद युग में पहुँचकर भावुकता, आत्म-अनुभूति और कल्पना के नए विस्तार के साथ पुष्ट हुई।
“छायावादी युग में मुक्तक काव्य की लोकप्रियता अचानक नहीं आई, बल्कि यह शैली प्राचीन भारतीय काव्य-परंपरा में गहराई से निहित रही है। संस्कृत, अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी साहित्य में मुक्तक शैली का विपुल प्रयोग मिलता है। प्रस्तुत सूची इस बात का प्रमाण है कि मुक्तक काव्य की परंपरा एक समृद्ध एवं सुदीर्घ परंपरा रही है, जिसे छायावादी कवियों ने आधुनिक काव्य चेतना के साथ पुनर्जीवित किया।”
निष्कर्ष
छायावादी युग में जहाँ खड़ी बोली के माध्यम से कवियों ने आत्मा की सूक्ष्म अनुभूतियों को काव्य में अभिव्यक्त किया, वहीं कुछ साहित्यकारों ने ब्रजभाषा की काव्य परंपरा को समकालीन भावभूमि से जोड़ते हुए काव्य रचना की। इन रचनाओं में नवीनता, भाव-गंभीरता और छायावादी सूक्ष्मता विद्यमान है। यदि इस काल में ब्रजभाषा में रचना का परिमाण अधिक होता, तो यह कहा जा सकता था कि यह युग ब्रजभाषा का भी छायावाद युग होता।
छायावाद युग: महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
🔹 1. छायावाद किस युग को कहते हैं?
उत्तर: हिंदी साहित्य के इतिहास में सन् 1918 से 1936 तक के काल को छायावाद युग कहा जाता है। यह युग आत्माभिव्यक्ति, प्रकृति-प्रेम, नारी सौंदर्य और रहस्यवाद का युग है।
🔹 2. छायावाद शब्द का क्या अर्थ है?
उत्तर: ‘छाया’ का अर्थ है ‘प्रतिबिंब’ या ‘आभा’, और ‘वाद’ का अर्थ है ‘धारा’ या ‘मत’। छायावाद आत्मचेतना, भावुकता और सौंदर्य की एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है।
🔹 3. छायावाद युग के चार प्रमुख स्तंभ कौन-कौन हैं?
उत्तर: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा।
🔹 4. छायावादी कविता की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:
- आत्माभिव्यक्ति
- रहस्यवाद
- प्रकृति-प्रेम
- नारी सौंदर्य का चित्रण
- सांस्कृतिक चेतना
- स्वच्छंद कल्पना
- कोमल-कांत पदावली
- मुक्त छंद का प्रयोग
🔹 5. छायावादी युग में प्रयुक्त प्रमुख काव्य-रूप कौन-से हैं?
उत्तर: मुक्तक काव्य, गीति काव्य, प्रबंध काव्य और लंबी कविता।
🔹 6. ‘कामायनी’ किसकी रचना है और यह किस प्रकार का काव्य है?
उत्तर: यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है। यह छायावाद युग की प्रतिनिधि रचना है।
🔹 7. ‘नीरजा’, ‘नीहार’ और ‘रश्मि’ रचनाएँ किसकी हैं?
उत्तर: महादेवी वर्मा की।
🔹 8. ‘राम की शक्ति पूजा’ किसकी प्रसिद्ध कविता है?
उत्तर: सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ की।
🔹 9. ‘उच्छ्वास’, ‘पल्लव’, ‘गुंजन’ रचनाएँ किस छायावादी कवि की हैं?
उत्तर: सुमित्रानंदन पंत की।
🔹 10. छायावादी युग की कविताओं में नारी की छवि किस रूप में चित्रित की गई है?
उत्तर: नारी को सौंदर्य, करूणा, त्याग, शक्ति और स्वतंत्र चेतना के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है।
🔹 11. छायावादी युग की भाषा की विशेषता क्या है?
उत्तर: ललित, कोमल-कांत, संस्कृतनिष्ठ और भावप्रवण भाषा; काव्य में अधिकतर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है।
🔹 12. रहस्यवाद का छायावाद से क्या संबंध है?
उत्तर: छायावाद में रहस्यवाद का प्रभाव स्पष्ट है, जहाँ कवि आत्मा और परमात्मा के अज्ञात संबंध को अनुभव करता है।
🔹 13. छायावादी युग में मुक्त छंद का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: यह कवि की भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को संभव बनाता है और बंधनमुक्त काव्य रचना को बढ़ावा देता है।
🔹 14. ‘सरोज स्मृति’ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? इसका विषय क्या है?
उत्तर: निराला द्वारा लिखी गई यह कविता उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु पर आधारित है।
🔹 15. कौन-से दो छायावादी कवि आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं?
उत्तर: रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी।
🔹 16. छायावाद युग में ब्रजभाषा में किस-किसने काव्य रचना की?
उत्तर: रामनाथ जोतिसी, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’, दुलारे लाल भार्गव, आदि।
🔹 17. ‘ऊर्म्मिला’ महाकाव्य किसकी रचना है और इसका विषय क्या है?
उत्तर: बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ की रचना है; इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग व धैर्य का चित्रण है।
🔹 18. मुक्तक काव्य की परिभाषा क्या है?
उत्तर: वह काव्य जिसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, कथा-संलग्नता नहीं होती। उदाहरण: दोहे, शतक आदि।
🔹 19. ‘मेघदूत’, ‘गीतगोविंद’, ‘शतकत्रय’ किस प्रकार के काव्य हैं?
उत्तर: ये सभी मुक्तक काव्य की परंपरा में आते हैं।
🔹 20. छायावाद में प्रकृति चित्रण की भूमिका क्या है?
उत्तर: प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं, बल्कि भावों की संवाहिका, प्रेरणा और आत्मा के स्वरूप के रूप में चित्रित किया गया है।
🔹 21. छायावादी युग में राष्ट्रवाद का स्वर किस कवि की रचनाओं में मुखरित हुआ?
उत्तर: माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, सियारामशरण गुप्त आदि की रचनाओं में।
🔹 22. छायावादी युग की समाप्ति कब मानी जाती है?
उत्तर: लगभग 1936 ई. में छायावादी युग का अंत माना जाता है, इसके बाद प्रगतिवाद का प्रभाव बढ़ा।
MCQ (बहुविकल्पीय प्रश्न) – उत्तर सहित
प्र.1: छायावाद युग के चार प्रमुख स्तंभ कौन-कौन से हैं?
A. भारतेंदु, द्विवेदी, प्रसाद, पंत
B. निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी
C. निराला, तुलसीदास, जायसी, सूर
D. मैथिलीशरण गुप्त, चतुर्वेदी, महादेवी, पंत
उत्तर: B. निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी
प्र.2: ‘कामायनी’ किस कवि की रचना है?
A. निराला
B. पंत
C. प्रसाद
D. महादेवी
उत्तर: C. प्रसाद
प्र.3: छायावादी कविता में किस तत्व की प्रमुखता होती है?
A. समाज सुधार
B. राष्ट्रवाद
C. आत्माभिव्यक्ति
D. भक्ति
उत्तर: C. आत्माभिव्यक्ति
प्र.4: ‘राम की शक्ति पूजा’ किस रचनाकार की प्रसिद्ध कविता है?
A. सुमित्रानंदन पंत
B. महादेवी वर्मा
C. सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’
D. जयशंकर प्रसाद
उत्तर: C. सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’
प्र.5: छायावाद युग में प्रयुक्त भाषा की विशेषता क्या थी?
A. उर्दू मिश्रित भाषा
B. बोलचाल की भाषा
C. कोमल-कांत पदावली, संस्कृतनिष्ठ
D. फारसी मिश्रित शैली
उत्तर: C. कोमल-कांत पदावली, संस्कृतनिष्ठ
लघु उत्तरीय प्रश्न – उत्तर सहित
प्र.6: छायावाद का शाब्दिक अर्थ क्या है?
उत्तर:
छायावाद का शाब्दिक अर्थ है – “छाया का वाद” या “प्रतीकों व बिंबों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति”। हिंदी साहित्य में यह एक काव्यधारा है जिसमें आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यबोध, रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम को विशेष महत्व दिया गया।
प्र.7: छायावादी युग के प्रमुख सामाजिक दृष्टिकोणों में कौन-कौन से विषय सम्मिलित हैं?
उत्तर:
- नारी स्वतंत्रता और गरिमा
- सामाजिक रूढ़ियों का विरोध
- सांस्कृतिक चेतना
- मानवतावाद
- व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता
प्र.8: ‘यामा’ किसकी काव्यकृति है? इसका क्या महत्व है?
उत्तर:
‘यामा’ महादेवी वर्मा की संकलनात्मक काव्यकृति है, जिसमें उनकी प्रमुख रचनाएँ ‘नीहार’, ‘रश्मि’, ‘नीरजा’ और ‘सांध्य गीत’ सम्मिलित हैं। इसे छायावादी युग की श्रेष्ठतम काव्यकृति माना जाता है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न – उत्तर सहित
✦ प्रश्न 1: छायावाद युग की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालिए।
उत्तर:
- परिचय:
- छायावाद हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण युग है (1918–1936 ई.)
- यह युग आत्माभिव्यक्ति, कल्पना और सौंदर्य की प्रधानता के लिए जाना जाता है।
- मुख्य विशेषताएँ:
- आत्माभिव्यक्ति (मैं शैली): कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और जीवन-दृष्टि को केंद्र में रखता है।
- प्रकृति प्रेम: प्रकृति का मानवीकरण एवं उसके माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति।
- रहस्यवाद: अज्ञात, असीम और ईश्वर के प्रति जिज्ञासा।
- नारी प्रेम और उसकी मुक्ति: नारी को सौंदर्य, करुणा और स्वतंत्र सत्ता के रूप में चित्रित किया गया।
- सांस्कृतिक चेतना: भारतीय परंपराओं, गौरव और संस्कृति का पुनर्मूल्यांकन।
- मुक्त छंद और भाषिक सौंदर्य: ललित, कोमल, संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग।
- स्वच्छंद कल्पना: कवियों ने कल्पना को बंधनों से मुक्त कर दिया।
- निष्कर्ष:
छायावाद युग भावात्मकता और आत्म-केन्द्रित रचनाशीलता का युग था जिसने हिंदी कविता को नया सौंदर्य-बोध और दिशा दी।
✦ प्रश्न 2: छायावादी युग में प्रयुक्त विविध काव्य-रूपों का विवेचन कीजिए।
उत्तर:
- परिचय:
- छायावादी कवियों ने पारंपरिक काव्य रूपों के साथ-साथ नए प्रयोग किए।
- उन्होंने मुक्तक, प्रबंध, गीति, लंबी कविता आदि काव्य-रूपों में सफल रचनाएँ कीं।
- विविध काव्य-रूप:
- मुक्तक काव्य: आत्म-अनुभूति की अभिव्यक्ति (प्रसाद की ‘आँसू’, महादेवी की ‘नीहार’)
- गीति काव्य: संगीतात्मकता एवं भावप्रधानता (निराला की ‘पंचवटी प्रसंग’, पंत की ‘शिल्पी’)
- प्रबंध काव्य: कथात्मक शैली और दार्शनिकता (प्रसाद की ‘कामायनी’, पंत की ‘लोकायतन’)
- लंबी कविता: प्रेरणात्मक और स्मृतिपरक (निराला की ‘राम की शक्ति पूजा’, ‘सरोज स्मृति’)
- निष्कर्ष:
- छायावाद युग में काव्य-रूपों की विविधता ने हिंदी कविता को विषय, शिल्प और संरचना की नई ऊँचाई दी।
✦ प्रश्न 3: छायावादी काव्यधारा में रहस्यवाद की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
- परिचय:
- रहस्यवाद छायावादी युग की केंद्रीय विशेषता है।
- यह व्यक्ति और ब्रह्म के संबंध को सूक्ष्म रूप में उजागर करता है।
- रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ:
- ईश्वर और आत्मा का मिलन: परम सत्ता से आत्मा की एकात्मकता का चित्रण।
- प्रतीकात्मकता: रहस्य को प्रकृति और बिंबों के माध्यम से व्यक्त करना।
- कालिदासीय परंपरा का पुनर्सृजन: रहस्य को सौंदर्यबोध से जोड़ना।
- सार्वभौमिक जिज्ञासा: ब्रह्मांड के अज्ञात और अमूर्त पहलुओं की खोज।
- प्रमुख उदाहरण:
- जयशंकर प्रसाद की ‘कामायनी’ में मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रहस्य।
- सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में आत्मा की उड़ान और ब्रह्मानंद की झलक।
- निष्कर्ष:
- रहस्यवाद ने छायावाद को गहराई और दार्शनिकता प्रदान की। यह युग केवल भाव का नहीं, आत्मिक खोज का भी युग बना।
✦ प्रश्न 4: छायावादी कवियों द्वारा नारी की अवधारणा पर विवेचन कीजिए।
उत्तर:
- परिचय:
- छायावाद युग में नारी को परंपरागत दृष्टिकोण से अलग, एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में देखा गया।
- नारी की प्रमुख छवियाँ:
- सौंदर्यबोध की प्रतिमूर्ति: नारी को प्रकृति, कला और सौंदर्य का प्रतीक माना गया।
- संवेदनशील और आत्मबल से युक्त: महादेवी वर्मा की कविताओं में विरहिणी नायिका के माध्यम से स्त्री की पीड़ा व गरिमा।
- स्वतंत्र सत्ता: स्त्री को पुरुष की परछाईं नहीं, आत्मनिर्भर इकाई के रूप में चित्रित किया गया।
- प्रमुख उदाहरण:
- प्रसाद की ‘कामायनी’ में श्रद्धा, इड़ा और मनु की त्रयी।
- महादेवी वर्मा का सम्पूर्ण काव्य – स्त्री चेतना का उद्घोष।
- निष्कर्ष:
- छायावादी युग में नारी साहित्यिक दृष्टि से सशक्त रूप में प्रस्तुत हुई, जिसने आगे के नारीवादी विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया।
✦ प्रश्न 5: छायावादी भाषा और शैली की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
उत्तर:
- परिचय:
- भाषा किसी युग के सौंदर्यबोध और विचारधारा की संवाहक होती है।
- छायावादी भाषा की विशेषताएँ:
- ललित-लवंगी कोमल भाषा: कोमल पदावली, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली।
- मानवीकरण और प्रतीक-चित्रण: प्रकृति और भावनाओं को मानवीय रूप देना।
- मुक्त छंद: बंधनरहित अभिव्यक्ति, लय की स्वतंत्रता।
- तुलना:
| युग | भाषा शैली |
|---|---|
| भारतेंदु युग | सहज, व्यावहारिक, प्रबोधनात्मक |
| द्विवेदी युग | तर्कपूर्ण, सुधारवादी, निबंधात्मक |
| छायावाद युग | भावात्मक, कल्पनाशील, सौंदर्यपूर्ण |
निष्कर्ष:
- छायावादी भाषा काव्यात्मक सौंदर्य और आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनी।
✦ प्रश्न 6: छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:
छायावादी युग हिंदी कविता का वह कालखंड है जिसमें कवियों ने आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यबोध, रहस्यवाद और मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रमुखता दी। इस युग की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं:
- आत्म-विस्तार और सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति:
कवियों ने आत्मा की स्वतंत्रता और सामाजिक बंधनों से मुक्ति की भावना को व्यक्त किया। - आत्माभिव्यक्ति (‘मैं’ शैली/उत्तम पुरुष शैली):
इस युग की कविताएँ कवि के अंतर्जगत की अभिव्यक्ति हैं। ‘मैं’ की शैली में कवि स्वयं को कविता का विषय बनाता है। - प्रकृति-प्रेम:
प्रकृति को केवल सजावटी पृष्ठभूमि न मानकर, संवेदना और चेतना का स्रोत समझा गया। - नारी प्रेम एवं उसकी मुक्ति का स्वर:
नारी को केवल सौंदर्य का प्रतीक न मानकर उसकी भावनात्मक, मानसिक स्वतंत्रता और गरिमा पर बल दिया गया। - सांस्कृतिक चेतना और मानवतावाद:
कविताओं में भारतीय संस्कृति की पुनर्स्मृति, गौरव और मानवमूल्यों का चित्रण किया गया। - अज्ञात व असीम के प्रति जिज्ञासा (रहस्यवाद):
छायावाद रहस्यवादी प्रवृत्तियों से युक्त है, जिसमें कवि परमात्मा, आत्मा और अज्ञेय शक्तियों के प्रति आकर्षित हैं। - स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष:
यथार्थ के स्थान पर कल्पना और भावनाओं को प्राथमिकता मिली, जो कवियों की रचनात्मक स्वतंत्रता को दर्शाती है। - विविध काव्य-रूपों का प्रयोग:
गीति, प्रबंध, मुक्तक, लंबी कविता आदि सभी रूपों में रचनाएँ लिखी गईं। - काव्य-भाषा:
भाषा संस्कृतनिष्ठ, कोमल-कांत पदावली से युक्त तथा भावाभिव्यक्ति के अनुकूल रही। - प्रकृति-संबंधी बिम्बों की बहुलता:
कविता में फूल, पत्ते, चंद्रमा, वर्षा, झील, पवन आदि बिम्बों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। - मुक्त छंद का प्रयोग:
कवियों ने छंदों के बंधन से मुक्त होकर अपनी बात कही, जिससे शैली अधिक अभिव्यंजक बनी। - अलंकारों का प्रयोग:
भारतीय परंपरागत अलंकारों के साथ-साथ अंग्रेजी साहित्य से लिए गए मानवीकरण (personification) तथा विशेषण-विपर्यय (Transferred epithet) अलंकारों का प्रभाव भी स्पष्ट है।
👉 ये विशेषताएँ छायावाद को विशिष्ट बनाती हैं और हिंदी साहित्य में इसे एक नया मोड़ प्रदान करती हैं।
✦ प्रश्न 7: छायावाद और प्रबंध काव्य की तुलना कीजिए।
उत्तर:
| विषय | छायावाद | प्रबंध काव्य |
|---|---|---|
| केंद्र | आत्माभिव्यक्ति, भाव | कथा-आधारित निरूपण |
| छंद | मुक्त छंद | बंद छंद |
| भाव | रहस्य, कल्पना, सौंदर्य | घटनात्मक, उद्देश्यपूर्ण |
| उदाहरण | ‘नीरजा’, ‘सरोज स्मृति’ | ‘कामायनी’, ‘प्रेम पथिक’ |
इन्हें भी देखें –
- हिंदी भाषा का इतिहास
- भाषा एवं उसके विभिन्न रूप
- हिंदी वर्णमाला- स्वर और व्यंजन | Hindi Alphabet
- वर्तनी | परिभाषा, भेद एवं 50+ उदाहरण
- संधि – परिभाषा एवं उसके भेद | Joining
- समास – परिभाषा, भेद और 100 + उदाहरण
- अलंकार- परिभाषा, भेद और 100 + उदाहरण
- रस | परिभाषा, भेद और उदाहरण
- मुहावरा और लोकोक्तियाँ 250+
- द्विवेदी युग (1900–1920 ई.): हिंदी साहित्य का जागरण एवं सुधारकाल
- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ
- पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका
- सोकोट्रा द्वीप (Socotra Island): एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर
- संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई मतदान नीति: रणनीतिक स्वायत्तता की ओर एक परिपक्व यात्रा
- ट्रेकोमा (Trachoma) : वैश्विक स्वास्थ्य संकट से मुक्ति की ओर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि