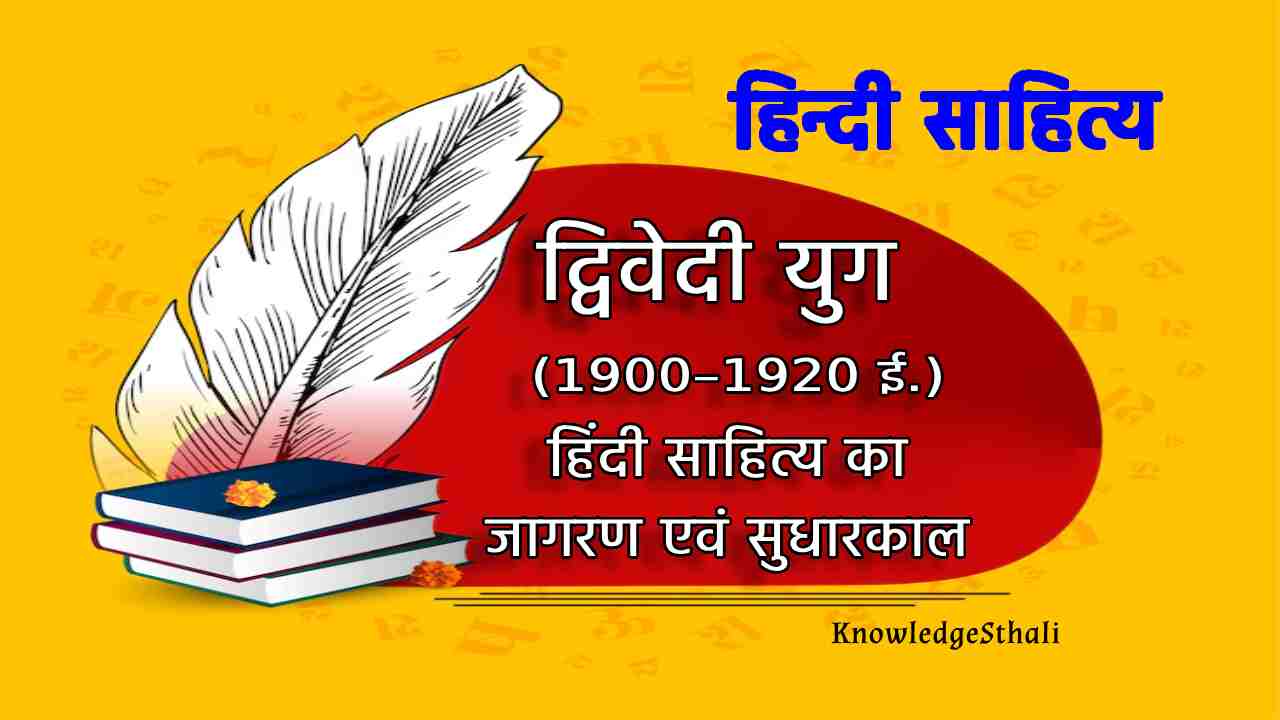हिंदी साहित्य का इतिहास अपने भीतर विविध युगों और आंदोलनों को समेटे हुए है। बीसवीं शताब्दी के आरंभिक दो दशकों (1900–1920) को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग का नामकरण उस समय के महान साहित्यकार, संपादक, आलोचक और विचारक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, जिनकी प्रेरणा और दिशा-निर्देश में हिंदी साहित्य ने एक नए युग में प्रवेश किया। इस युग को “जागरण-सुधार काल” के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में साहित्य ने समाज को दिशा देने, सामाजिक कुरीतियों पर चोट करने और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
द्विवेदी युग (1900 ई.–1920 ई.)
हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग (1900 से 1920 ई.) एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी कालखंड रहा है। यह वह युग था जब हिंदी साहित्य ने परंपरागत श्रृंगारिक विषयों से बाहर निकलकर राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों को आत्मसात किया। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा दी और इसे आधुनिकता की ओर उन्मुख किया।
इस काल को ‘जागरण और सुधारकाल’ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता और वैचारिक प्रबोधन के बीज अंकुरित हुए। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली को स्थापित करने, गद्य लेखन की विधाओं को परिपक्व बनाने और साहित्य को जीवन के यथार्थ से जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास इसी युग में हुआ।
द्विवेदी युग की समय-सीमा
द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के इतिहास में 1900 ई. से 1920 ई. तक की अवधि को कहा जाता है। यह काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदी साहित्य में सुधार, जागरण और नवनिर्माण का युग था। इस युग को “जागरण-सुधार काल” भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में साहित्य के माध्यम से समाज को नैतिकता, आदर्शवाद, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार की दिशा में प्रेरित किया गया।
द्विवेदी युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
द्विवेदी युग उस समय की उपज है जब भारत अंग्रेज़ी शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और भारतीय समाज में अशिक्षा, अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव और महिलाओं की दयनीय स्थिति जैसी समस्याएं व्याप्त थीं। राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हो रही थी और स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत हो रही थी। ऐसे समय में हिंदी साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से न केवल साहित्यिक मानदंडों को स्थापित किया, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी कारगर भूमिका निभाई।
द्विवेदी युग का नामकरण
द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का वह कालखंड है जो 20वीं शताब्दी के पहले दो दशकों — 1900 से 1920 ई. तक विस्तृत माना जाता है। इस युग में हिंदी कविता ने श्रृंगारिकता से आगे बढ़कर राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ियों से स्वच्छंदता की ओर स्पष्ट परिवर्तन किया। यह काल न केवल साहित्यिक दिशा परिवर्तन का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक चेतना और सुधार की भी नींव पड़ी।
इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है, जो इस समय के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्यिक नेता माने जाते हैं। उन्होंने न केवल हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, बल्कि हिंदी के कोश निर्माण, व्याकरण की स्थिरता, और विशेष रूप से खड़ी बोली के परिष्कार में उल्लेखनीय योगदान दिया। यही कारण है कि उन्होंने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने का सफल प्रयास किया।
द्विवेदी युग को सही अर्थों में “जागरण-सुधार काल” कहा जाता है, क्योंकि इस समय साहित्य केवल सौंदर्य और कल्पना का माध्यम न रहकर, सामाजिक उत्थान, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीय जागृति का उपकरण बन गया।
द्विवेदी युग के निर्माता: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
इस युग का नाम “द्विवेदी युग” आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को केंद्र में रखकर रखा गया। वे केवल एक संपादक या लेखक नहीं थे, बल्कि विचारों के शिल्पी, भाषा-शास्त्र के जानकार, संस्कृत-साहित्य के अध्येता और नवीन हिंदी गद्य एवं पद्य के निर्माता थे।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी (1864–1938) द्विवेदी युग के सर्वमान्य साहित्यिक पथ-प्रदर्शक थे। उन्होंने न केवल हिंदी साहित्य को एक सुनियोजित दिशा दी, बल्कि अपने संपादकीय कौशल, वैचारिक स्पष्टता और साहित्यिक नेतृत्व से इस युग को एक संगठित रूप प्रदान किया।
सन् 1903 में उन्होंने प्रतिष्ठित ‘सरस्वती’ पत्रिका का संपादन संभाला, जो हिंदी के नवजागरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाली पत्रिका थी। इसके माध्यम से द्विवेदी ने लेखकों को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया, जिससे हिंदी गद्य लेखन को स्थायित्व प्राप्त हुआ।
उनकी दृष्टि संस्कृत साहित्य की समृद्ध परंपरा से पोषित थी, किंतु वे रूढ़ियों के विरोधी थे। उन्होंने वेदों से लेकर संस्कृत काव्य-परंपरा और पंडितराज जगन्नाथ तक के साहित्य को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा और उपयोगितावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान
- 1903 में उन्होंने ‘सरस्वती’ पत्रिका का संपादन संभाला।
- उन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।
- हिंदी गद्य को सुस्पष्ट, परिष्कृत और शुद्ध रूप प्रदान किया।
- कवियों को खड़ी बोली में लेखन के लिए प्रेरित किया।
- उन्होंने आदर्शवाद, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को साहित्य की आत्मा बनाया।
द्विवेदी युग की विशेषताएँ
द्विवेदी युग में साहित्य को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और जागरण का साधन माना गया। इस युग की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना
- रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत, स्वतंत्रता की आकांक्षा और मातृभूमि के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है।
- सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति
- बाल विवाह, विधवा जीवन, जात-पात, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों पर साहित्यकारों ने चोट की।
- नैतिकता और आदर्शवाद
- साहित्य में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास हुआ। ‘सत्यम, शिवम, सुंदरम’ के आदर्शों को अपनाया गया।
- नारी सहानुभूति और समानता
- नारी के प्रति करुणा, सहानुभूति और अधिकारों की चर्चा प्रमुख रही।
- प्रकृति चित्रण
- कई कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रित किया, किंतु वह यथार्थ और उद्देश्यपरक था।
- भाषा शैली
- सरल, सरस, शुद्ध खड़ी बोली में लेखन को प्राथमिकता दी गई।
- शृंगार का मर्यादित रूप
- कविता में शृंगार रस तो था, पर वह मर्यादित और नीति-आधारित था।
द्विवेदी युग की विधाओं का विकास
इस युग में कविता के साथ-साथ अन्य साहित्यिक विधाओं का भी विकास हुआ।
निबंध साहित्य का विकास:
द्विवेदी युग में निबंध विधा का भी अद्भुत विकास हुआ। निबंध लेखन में विचार प्रधानता और भाषा की स्पष्टता पर बल दिया गया। इस युग के निबंधकारों ने भाषा को परिष्कृत, विचारों को गम्भीर, और शैली को तर्कनिष्ठ बनाया।
🔹 प्रमुख निबंधकार:
- महावीर प्रसाद द्विवेदी: सामाजिक, साहित्यिक और वैचारिक विषयों पर अत्यंत गंभीर निबंध लिखे।
- श्यामसुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्णसिंह आदि ने विचारोत्तेजक और ललित निबंधों की रचना की।
- प्रमुख निबंधकार:
- महावीर प्रसाद द्विवेदी
- श्यामसुंदर दास
- माधव प्रसाद मिश्र
- बालमुकुंद गुप्त
- चंद्रधर शर्मा गुलेरी
- अध्यापक पूर्णसिंह
उपन्यास विधा का विस्तार:
हालाँकि उपन्यास विधा भारतेन्दु युग में प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन द्विवेदी युग में यह और विकसित हुई। इस युग के उपन्यास मनोरंजन के साथ-साथ समाज का दर्पण भी बने। इस समय के उपन्यासों में नैतिक शिक्षा, संस्कार, पारिवारिक आदर्श और समाजिक मूल्यबोध प्रमुख रहे।
🔹 प्रमुख उपन्यासकार:
- किशोरीलाल गोस्वामी: इनके उपन्यासों में कल्पनाशीलता और घटनाओं की रोचकता होती थी।
- बाबू गोपालराम गहमरी: इन्होंने उपन्यासों में मनोरंजन के साथ नैतिकता को समाहित किया।
- प्रमुख रचनाकार:
- किशोरीलाल गोस्वामी
- बाबू गोपालराम गहमरी
हिंदी कहानी का प्रारंभ:
हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही माना जाता है। प्रथम हिंदी कहानी मानी जाने वाली “इंदुमती” इसी काल में लिखी गई। इस युग की कहानियाँ विषय-वस्तु, शिल्प और उद्देश्य की दृष्टि से परिपक्व होने लगीं।
🔹 प्रमुख कहानियाँ एवं लेखक:
- किशोरीलाल गोस्वामी की ‘इंदुमती’ को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है।
- चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ‘उसने कहा था’—यह कहानी हिंदी साहित्य में भावनात्मक गहराई और कथाशिल्प की दृष्टि से ऐतिहासिक मानी जाती है।
- प्रमुख कहानियाँ:
- “इंदुमती” – किशोरी लाल गोस्वामी
- “उसने कहा था” – चंद्रधर शर्मा गुलेरी
- “ग्राम” – जयशंकर प्रसाद
- “ग्यारह वर्ष का समय” – रामचंद्र शुक्ल
- “दुलाई वाली” – बंग महिला
नाटक विधा का प्रारंभिक विकास
इस युग में हिंदी नाटक लेखन भी प्रारंभिक विकास में था। यद्यपि नाटकों की संख्या सीमित थी, फिर भी समाज सुधार के लिए इनका प्रयोग किया गया।
🔹 प्रमुख नाटककार:
- अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’
- शिवनंदन सहाय
- राय देवीप्रसाद पूर्ण।
इनके नाटकों में आदर्शों का चित्रण और नैतिक उद्देश्य विद्यमान रहता था।
समालोचना
हिंदी समालोचना का शास्त्रीय और वैज्ञानिक स्वरूप इसी युग में उभर कर सामने आया। आलोचना अब केवल भावुकता नहीं, तार्किक विवेचन पर आधारित होने लगी।
पद्मसिंह शर्मा इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैं। साथ ही रामचंद्र शुक्ल भी आलोचना के एक नए युग का सूत्रपात करने वाले सिद्ध हुए। साहित्यिक समालोचना का आरंभ भी द्विवेदी युग की देन है।
🔹 प्रमुख आलोचक:
- पद्मसिंह शर्मा
- महावीर प्रसाद द्विवेदी
- रामचंद्र शुक्ल (बाद में विकास करते हैं)
द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ
द्विवेदी युग (1900–1920 ई.) हिंदी साहित्य का एक ऐसा चरण है जिसमें काव्य को सामाजिक जागरण, राष्ट्रभक्ति, नैतिकता और आदर्शवाद का माध्यम बनाया गया। इस युग के कवियों ने साहित्य को मात्र मनोरंजन का साधन न मानकर उसे समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का वाहक बना दिया। खड़ी बोली में लिखी गई इनकी रचनाओं ने हिंदी कविता की भाषा और दिशा दोनों को नया रूप दिया।
इस काल के प्रमुख कवियों ने सरल, सुस्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में काव्य रचनाएँ प्रस्तुत कीं, जो आज भी साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नीचे दिए गए हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएँ—
1. नाथूराम शर्मा ‘शंकर’
प्रमुख रचनाएँ:
- अनुराग रत्न
- शंकर सरोज
- गर्भरण्डा रहस्य
- शंकर सर्वस्व
2. श्रीधर पाठक
प्रमुख रचनाएँ:
- वनाष्टक
- काश्मीर सुषमा
- देहरादून
- भारत गीत
- जार्ज वंदना
- बाल विधवा
3. महावीर प्रसाद द्विवेदी
प्रमुख रचनाएँ:
- काव्य मंजूषा
- सुमन
- कान्यकुब्ज अबला-विलाप
4. अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’
प्रमुख रचनाएँ:
- प्रियप्रवास
- पद्यप्रसून
- चुभते चौपदे
- चोखे चौपदे
- बोलचाल
- रसकलस
- वैदेही वनवास
5. राय देवीप्रसाद ‘पूर्ण’
प्रमुख रचनाएँ:
- स्वदेशी कुण्डल
- मृत्युंजय
- राम-रावण विरोध
- वसंत-वियोग
6. रामचरित उपाध्याय
प्रमुख रचनाएँ:
- राष्ट्र भारती
- देवदूत
- देवसभा
- विचित्र विवाह
- रामचरित-चिन्तामणि
7. गयाप्रसाद शुक्ल ‘सनेही’
प्रमुख रचनाएँ:
- कृषक क्रंदन
- प्रेम प्रचीसी
- राष्ट्रीय वीणा
- त्रिशूल तरंग
- करुणा कादंबिनी
8. मैथिलीशरण गुप्त
प्रमुख रचनाएँ:
- रंग में भंग
- जयद्रथ वध
- भारत भारती
- पंचवटी
- झंकार
- साकेत
- यशोधरा
- द्वापर
- जय भारत
- विष्णुप्रिया
9. रामनरेश त्रिपाठी
प्रमुख रचनाएँ:
- मिलन
- पथिक
- स्वप्न
- मानसी
10. बाल मुकुन्द गुप्त
प्रमुख रचनाएँ:
- स्फुट कविता
11. लाला भगवानदीन ‘दीन’
प्रमुख रचनाएँ:
- वीर क्षत्राणी
- वीर बालक
- वीर पंचरत्न
- नवीन बीन
12. लोचन प्रसाद पाण्डेय
प्रमुख रचनाएँ:
- प्रवासी
- मेवाड़ गाथा
- महानदी
- पद्य पुष्पांजलि
13. मुकुटधर पाण्डेय
प्रमुख रचनाएँ:
- पूजा फूल
- कानन कुसुम
द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की सारणी
द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने वाले कई महान कवि सक्रिय रहे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना, देशभक्ति, नारी संवेदना, नैतिकता और आदर्श जीवन मूल्यों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया। इन कवियों की रचनाएँ खड़ी बोली हिंदी में लिखी गईं और इन्होंने हिंदी कविता को रूप, भाषा और विषय की दृष्टि से परिष्कृत किया।
निम्नलिखित सारणी में द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नामों के साथ उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख किया गया है, जो इस युग की साहित्यिक समृद्धि का सजीव प्रमाण हैं।
| क्रम | कवि (रचनाकार) | प्रमुख रचनाएँ |
|---|---|---|
| 1 | नाथूराम शर्मा ‘शंकर’ | अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरण्डा रहस्य, शंकर सर्वस्व |
| 2 | श्रीधर पाठक | वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, जार्ज वंदना, बाल विधवा |
| 3 | महावीर प्रसाद द्विवेदी | काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज अबला-विलाप |
| 4 | अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ | प्रियप्रवास, पद्यप्रसून, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, बोलचाल |
| 5 | राय देवीप्रसाद ‘पूर्ण’ | स्वदेशी कुण्डल, मृत्युंजय, राम-रावण विरोध |
| 6 | रामचरित उपाध्याय | राष्ट्र भारती, देवदूत, रामचरित-चिन्तामणि |
| 7 | गयाप्रसाद शुक्ल ‘सनेही’ | कृषक क्रन्दन, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग |
| 8 | मैथिलीशरण गुप्त | भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत, द्वापर, रंग में भंग |
| 9 | रामनरेश त्रिपाठी | मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी |
| 10 | बाल मुकुन्द गुप्त | स्फुट कविताएँ |
| 11 | लाला भगवानदीन ‘दीन’ | वीर क्षत्राणी, नवीन बीन, वीर पंचरत्न |
| 12 | लोचन प्रसाद पाण्डेय | प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी |
| 13 | मुकुटधर पाण्डेय | पूजा फूल, कानन कुसुम |
मैथिलीशरण गुप्त – युग प्रवर्तक कवि
द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कवि मैथिलीशरण गुप्त थे।
- उनकी रचनाएँ भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा आदि आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती हैं।
- उन्होंने राष्ट्रीय चेतना, पौराणिक पात्रों के माध्यम से सामाजिक सन्देश और नारी जीवन की पीड़ा को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया।
द्विवेदी युग का कविता के क्षेत्र में योगदान
कविता का स्वरूप और विषयवस्तु
द्विवेदी युग की कविताओं में एक ओर राष्ट्रीयता की भावना है, तो दूसरी ओर सामाजिक सुधार और नीतिपरक शिक्षा का समावेश। इस समय कविताओं का उद्देश्य समाज को सुधारना, नैतिक मूल्यों को स्थापित करना और देशप्रेम की भावना को जाग्रत करना था। कविता की भाषा में आदर्शवाद का समावेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। द्विवेदी युग की कविताएँ इतिवृत्तात्मक (narrative) शैली में थीं। द्विवेदी युग को “इतिवृत्तात्मक कविता युग” भी कहा गया।
🔹 प्रमुख विषय:
- देशप्रेम, स्त्रीविमर्श, आदर्श जीवन, त्याग, धर्म, वीरता, सामाजिक न्याय।
- श्रृंगारिकता सीमित और संयमित थी।
- भारत का अतीत और गौरवगान
- राष्ट्रीय भावना और जन-जागरण
- समाज-सुधार और नैतिक शिक्षा
🔹 प्रमुख कवि:
- मैथिलीशरण गुप्त: इन्होंने खड़ी बोली में महाकाव्यात्मक रचनाएँ कीं। ‘भारत-भारती’ जैसी रचना ने जन-जागरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।
- अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’: इनकी रचनाओं में नीति, देशभक्ति और सामाजिक जागृति के भाव मुखर हैं। काव्य की भाषा सरस, परिष्कृत और प्रवाहपूर्ण रही।
- श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ आदि ने भी इस युग में उल्लेखनीय काव्य रचनाएँ कीं।
इस युग में ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने लेना शुरू कर दिया, फिर भी कुछ रचनाकारों जैसे जगन्नाथदास रत्नाकर ने ब्रज में सरस रचनाएँ दीं।
द्विवेदी युग की साहित्यिक उपलब्धियाँ
- खड़ी बोली को साहित्यिक स्वरूप मिला।
- गद्य और पद्य दोनों का संतुलित विकास हुआ।
- साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया गया।
- कविता में आदर्शवाद और उद्देश्यपरकता का समावेश हुआ।
- आधुनिक आलोचना पद्धति की नींव पड़ी।
द्विवेदी युग की साहित्यिक विशेषताएँ:
इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ अनेक स्तरों पर प्रकट होती हैं, जैसे—
1. आदर्शवाद और नैतिकता का प्रभाव:
द्विवेदी युग में साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पाठकों में नीति, आदर्श, आत्म-निर्माण और राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करना था। नीतिवादी दृष्टिकोण के कारण श्रृंगार जैसे विषयों का चित्रण मर्यादित ढंग से हुआ।
2. राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना:
भारत का गौरवशाली अतीत, देशभक्ति, स्वदेश-प्रेम, सामाजिक सुधार, नारी-मुक्ति, शिक्षा, छुआछूत, बाल-विवाह और विधवा-विवाह जैसे मुद्दे साहित्य के केंद्र में आए।
3. भाषा का परिष्कार:
इस युग में हिंदी भाषा, विशेष रूप से खड़ी बोली, को साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया। द्विवेदी जी के नेतृत्व में भाषा में संस्कृतनिष्ठता, स्पष्टता, तार्किकता और गंभीरता आई।
4. गद्य विधाओं का विकास:
यही वह काल था जब हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं—निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक और समालोचना—का सृजनात्मक विस्तार प्रारंभ हुआ।
द्विवेदी युग की सीमाएँ
यद्यपि द्विवेदी युग में साहित्य का नवनिर्माण हुआ, परंतु इसके साथ कुछ सीमाएँ भी रहीं—
- रचनाओं में कहीं-कहीं उपदेशात्मकता अधिक हो गई।
- भाव पक्ष की अपेक्षा बौद्धिकता पर ज़्यादा ज़ोर रहा।
- कविता में भावनात्मक विविधता और कल्पना का अभाव रहा।
- शृंगार, करुण, हास्य जैसे रसों की उपेक्षा हुई।
- श्रृंगार, प्रकृति चित्रण आदि पर नैतिकता का इतना प्रभाव पड़ा कि वे सीमित हो गए।
- महिला रचनाकारों की संख्या नगण्य रही।
- महिला लेखन, दलित चेतना या विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की झलक अल्प रही।
निष्कर्ष
द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के इतिहास में जागरण, सुधार और संगठन का युग है। इस युग ने साहित्य को एक उद्देश्य, दिशा और लक्ष्य प्रदान किया। इस युग की सबसे बड़ी देन यह रही कि उसने साहित्य को समाज से जोड़ा और साहित्यकारों को समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगुआई में हिंदी साहित्य ने श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ि से स्वच्छंदता की ओर संक्रमण किया, जिसकी परिणति छायावाद के रूप में हुई। इस प्रकार, द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ कहा जा सकता है, जिसने न केवल भाषा और साहित्य को गढ़ा बल्कि जनजागरण की एक स्थायी ज्योति भी प्रज्वलित की।
द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का संक्रमण काल था, जहाँ से आधुनिकता की यात्रा आरंभ हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदी साहित्य ने रूढ़ियों से विद्रोह कर सामाजिक यथार्थ और राष्ट्रीय चेतना की ओर प्रस्थान किया।
इस युग में न केवल भाषा का परिष्कार हुआ, बल्कि साहित्य का उद्देश्य, सरोकार और दिशा भी परिवर्तित हुई। यह युग साहित्य को मनोरंजन से मुक्त कर जन-जागरण, नैतिक उत्थान और सामाजिक सुधार का माध्यम बनाने में सफल रहा। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य की मजबूत नींव है, जिस पर आगे चलकर छायावाद, प्रगतिवाद, और नई कविता जैसे आंदोलन विकसित हुए।
द्विवेदी युग : महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
यहाँ द्विवेदी युग से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जो छात्रों, शोधकर्ताओं एवं साहित्य प्रेमियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे:
1. द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है?
उत्तर: द्विवेदी युग का समय 1900 ई. से 1920 ई. तक माना जाता है।
2. द्विवेदी युग का नाम ‘द्विवेदी युग’ क्यों पड़ा?
उत्तर: इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभावशाली नेतृत्व और साहित्यिक योगदान के कारण पड़ा।
3. द्विवेदी युग को और किस नाम से जाना जाता है?
उत्तर: इसे जागरण-सुधार काल भी कहा जाता है।
4. द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर: इस युग की प्रमुख विशेषताएँ हैं: देशभक्ति, सामाजिक सुधार, नारी सहानुभूति, नैतिकता, आदर्शवाद, और सरल खड़ी बोली में लेखन।
5. इस युग में किस भाषा शैली को प्राथमिकता दी गई?
उत्तर: खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया।
6. द्विवेदी युग का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
उत्तर: समाज में जागरूकता लाना, नैतिकता स्थापित करना और राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करना।
7. द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन-कौन थे?
उत्तर: मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’, श्रीधर पाठक, गयाप्रसाद शुक्ल ‘सनेही’, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदि।
8. मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर: भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध आदि।
9. महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर: काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज अबला-विलाप।
10. ‘भारत भारती’ रचना किस कवि की है और इसका क्या महत्व है?
उत्तर: ‘भारत भारती’ मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध राष्ट्रवादी काव्य है, जो भारतीय संस्कृति और चेतना को जाग्रत करता है।
11. ‘सरस्वती’ पत्रिका का क्या योगदान रहा?
उत्तर: ‘सरस्वती’ पत्रिका के संपादन के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई रचनाकारों को गढ़ा और साहित्य को दिशा दी।
12. द्विवेदी युग की कविता शैली कैसी थी?
उत्तर: यह युग इतिवृत्तात्मक (narrative) शैली का था, जिसमें उद्देश्यपरकता और नीति का समावेश होता था।
13. इस युग में हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ?
उत्तर: हिंदी कहानी का आरंभ इसी युग से हुआ; ‘इंदुमती’ (किशोरीलाल गोस्वामी) को पहली हिंदी कहानी माना जाता है।
14. ‘उसने कहा था’ कहानी किसकी रचना है और इसका महत्व क्या है?
उत्तर: यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और यह हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में गिनी जाती है, जिसमें प्रेम और बलिदान की भावना है।
15. द्विवेदी युग में शृंगार रस को किस रूप में प्रस्तुत किया गया?
उत्तर: इस युग में शृंगार रस को मर्यादित और नैतिक रूप में प्रस्तुत किया गया।
16. द्विवेदी युग की सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है?
उत्तर: खड़ी बोली का साहित्यिक रूप में स्थापन और साहित्य को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाना इसकी सबसे बड़ी देन है।
17. द्विवेदी युग के कवियों का सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था?
उत्तर: इन कवियों का दृष्टिकोण आदर्शवादी, नैतिकतापरक और समाजोन्मुखी था।
18. द्विवेदी युग के किस कवि को “राष्ट्रीय कवि” कहा जाता है?
उत्तर: मैथिलीशरण गुप्त को “राष्ट्रीय कवि” कहा जाता है।
19. ‘प्रियप्रवास’ किसकी रचना है और यह किस शैली में है?
उत्तर: ‘प्रियप्रवास’ अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ की रचना है और यह खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है।
20. ‘कृषक क्रंदन’ किस कवि की रचना है और इसका क्या संदेश है?
उत्तर: यह गयाप्रसाद शुक्ल ‘सनेही’ की रचना है, जिसमें किसानों की पीड़ा और सामाजिक शोषण पर प्रकाश डाला गया है।
📝 Objective Questions (MCQs) – द्विवेदी युग से संबंधित
प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर बोल्ड में दर्शाया गया है।
1. द्विवेदी युग का समय क्या है?
A. 1850–1880
B. 1880–1900
C. 1900–1920
D. 1920–1940
2. द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा?
A. भारतेंदु हरिश्चंद्र
B. जयशंकर प्रसाद
C. महावीर प्रसाद द्विवेदी
D. रामचंद्र शुक्ल
3. ‘भारत भारती’ किस कवि की रचना है?
A. हरिऔध
B. मैथिलीशरण गुप्त
C. श्रीधर पाठक
D. सनेही
4. ‘प्रियप्रवास’ की रचना किसने की?
A. हरिऔध
B. सनेही
C. त्रिपाठी
D. द्विवेदी
5. द्विवेदी युग को और किस नाम से जाना जाता है?
A. भक्ति काल
B. छायावाद काल
C. जागरण-सुधार काल
D. आधुनिक काल
6. ‘उसने कहा था’ कहानी के लेखक कौन हैं?
A. जयशंकर प्रसाद
B. बालमुकुंद गुप्त
C. गोपालराम गहमरी
D. चंद्रधर शर्मा गुलेरी
7. ‘इंदुमती’ किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है?
A. बंग महिला
B. किशोरीलाल गोस्वामी
C. रामचंद्र शुक्ल
D. श्यामसुंदर दास
8. ‘सरस्वती’ पत्रिका का संपादन किसने किया?
A. महावीर प्रसाद द्विवेदी
B. अयोध्यासिंह उपाध्याय
C. हरगोविंद
D. रामनरेश त्रिपाठी
9. ‘कृषक क्रंदन’ का विषय क्या है?
A. युद्ध
B. किसान की पीड़ा
C. प्रेम
D. शृंगार
10. मैथिलीशरण गुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है?
A. आदर्श कवि
B. भक्ति कवि
C. राष्ट्रीय कवि
D. प्रगतिशील कवि
11. ‘काव्य मंजूषा’ किसकी रचना है?
A. सनेही
B. महावीर प्रसाद द्विवेदी
C. त्रिपाठी
D. पाठक
12. ‘वीर क्षत्राणी’ किस कवि की रचना है?
A. मुकुटधर पांडेय
B. लाला भगवानदीन ‘दीन’
C. गहमरी
D. रामचरित उपाध्याय
13. ‘देवदूत’ किसकी रचना है?
A. हरिऔध
B. पाठक
C. रामचरित उपाध्याय
D. गुप्त
14. ‘यशोधरा’ का लेखक कौन है?
A. श्रीधर पाठक
B. बालमुकुंद गुप्त
C. मैथिलीशरण गुप्त
D. मुकुटधर पांडेय
15. द्विवेदी युग में कौन-सी भाषा शैली प्रमुख थी?
A. अवधी
B. ब्रजभाषा
C. खड़ी बोली हिंदी
D. भोजपुरी
16. ‘पथिक’ किस कवि की रचना है?
A. सनेही
B. रामनरेश त्रिपाठी
C. पाठक
D. मुकुटधर
17. ‘स्फुट कविता’ किसकी रचनाएँ हैं?
A. द्विवेदी
B. बाल मुकुन्द गुप्त
C. त्रिपाठी
D. दीन
18. ‘नवीन बीन’ किस कवि की रचना है?
A. पाठक
B. मुकुटधर पांडेय
C. लाला भगवानदीन ‘दीन’
D. रामचरित उपाध्याय
19. ‘पूजा फूल’ किसकी रचना है?
A. द्विवेदी
B. मुकुटधर पांडेय
C. सनेही
D. त्रिपाठी
20. ‘प्रवासी’ रचना किस कवि की है?
A. हरिऔध
B. त्रिपाठी
C. पाठक
D. लोचन प्रसाद पाण्डेय
इन्हें भी देखें –
- रानी सारन्धा | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- बेटी का धन | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- बड़े घर की बेटी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- शराब की दुकान | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- सुहाग की साड़ी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास
- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ
- भाषा एवं उसके विभिन्न रूप
- भारतेन्दु युग (1850–1900 ई.): हिंदी नवजागरण का स्वर्णिम प्रभात
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY): भारत के कृषि क्षेत्र में समग्र सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम
- भारत में टेस्ला की ऐतिहासिक एंट्री: मुंबई के बीकेसी में पहला शोरूम और भारत के ईवी क्षेत्र का नया युग
- नई लाइकेन प्रजातियाँ और पश्चिमी घाट में सहजीवन का रहस्य: Allographa effusosoredica की खोज
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA): भारत में दत्तक ग्रहण की निगरानी और नियमन की आधारशिला