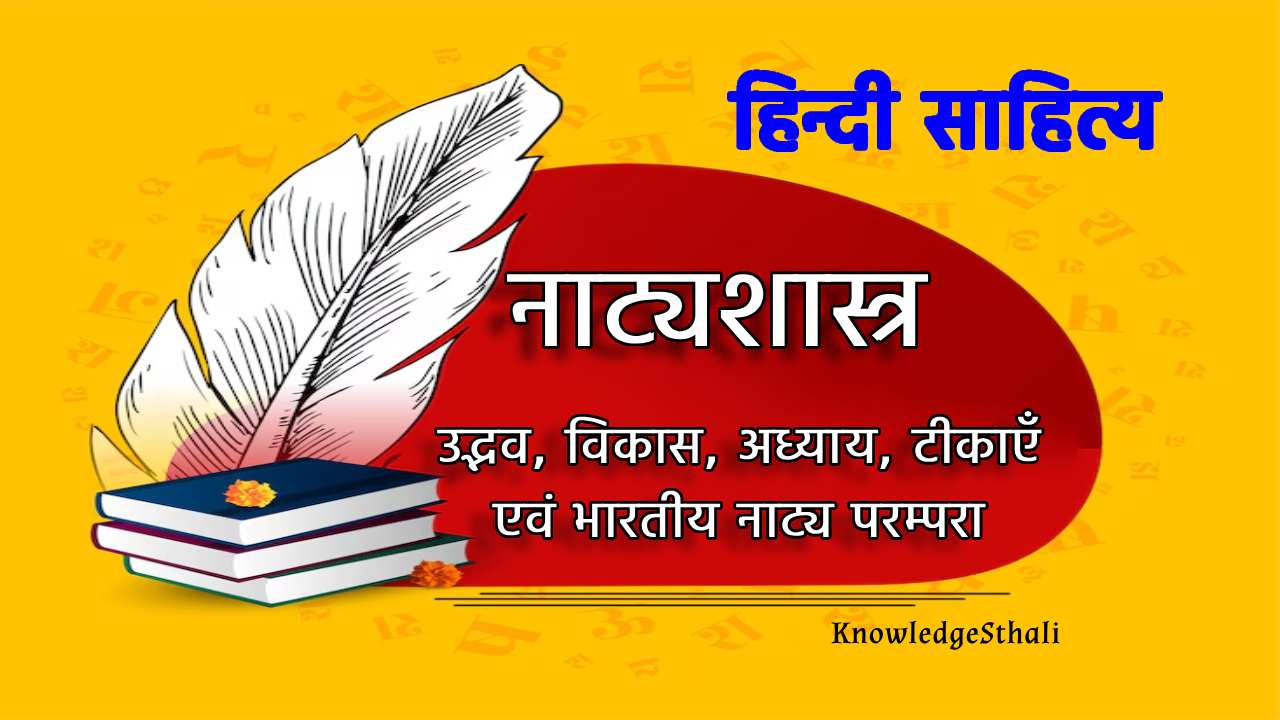भारतीय संस्कृति में कला का स्थान सदैव सर्वोपरि रहा है। नृत्य, संगीत, अभिनय और काव्य जैसी ललित कलाएँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति भी मानी जाती हैं। इन्हीं कलाओं का संगम हमें भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है। यह नाट्यकला का सर्वप्राचीन और सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, वाद्य, कविता और सौंदर्यशास्त्र से जुड़े लगभग सभी पहलुओं का विस्तारपूर्वक विवेचन है।
भारतीय परंपरा में इसे “नाट्यवेद” भी कहा गया है। भरतमुनि ने इसे केवल एक कला-विषयक ग्रंथ न मानकर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन माना है। इसीलिए नाट्यशास्त्र का अध्ययन हमें केवल नाटक-लेखन और अभिनय की विधियों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन की गहनता और सामूहिक चेतना का बोध भी कराता है।
नाट्यशास्त्र का उद्गम और रचनाकार
नाट्यशास्त्र की रचना भरतमुनि ने लगभग 300 ईसा पूर्व की। विद्वानों के अनुसार भरतमुनि का जीवनकाल 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है।
“नट्” धातु से बना “नाट्य” शब्द गिरने-नाचने और अभिनय करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भरतमुनि का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि कला के माध्यम से समाज को शिक्षित करना और जीवन के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करना था।
भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी। चार वेद जहाँ केवल ब्राह्मणों तक सीमित माने जाते थे, वहीं नाट्यवेद को सभी वर्णों और वर्गों के लिए उपलब्ध कराया गया। यह “सार्वभौमिक कला-दर्शन” है, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी भागीदारी कर सकता है।
नाट्यशास्त्र के लेखक
भरतमुनि नाट्यशास्त्र के प्रमुख रचयिता माने जाते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार, उन्हें नाट्यविद्या का लोक प्रचारक और व्यवस्थित शास्त्र रूप देने वाला आचार्य कहा जाता है। प्राचीन टीकाकार उन्हें ‘द्वादशसाहस्रीकार’ तथा ‘षट्साहस्रीकार’ की उपाधि से उद्धृत करते हैं।
भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में अभिनय, रस, भाव, संगीत, नृत्य, वेशभूषा, छंद, अलंकार आदि सभी विषयों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित विवेचन किया। उनके ग्रंथ को ‘नाट्यवेद’ कहा गया है।
नाट्यशास्त्र की टीकाओं और व्याख्याओं में अभिनवगुप्त (अभिनवभारती) सर्वाधिक प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त उद्भट, शंकुक, कीर्तिधर, भट्टनायक आदि प्राचीन टीकाकारों ने भी नाट्यशास्त्र पर टीकाएँ की हैं।
भरतमुनि की रचना और उनके शिष्यों की टीकाएँ नाट्यशास्त्र को न केवल नाट्यकला का मूल आधार बनाती हैं, बल्कि भारतीय साहित्य और रससिद्धांत की भी नींव प्रदान करती हैं।
नाट्यशास्त्र का स्वरूप
नाट्यशास्त्र को भारतीय कलाओं का विश्वकोश कहा जा सकता है। इसमें नाटक, काव्य, अभिनय, संगीत, नृत्य, शिल्प और ललित कलाओं के विविध रूपों का वर्णन मिलता है।
- इसमें कुल 36 अध्याय (कुछ संस्करणों में 37) हैं।
- इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं।
- इन अध्यायों में नाट्यरचना, अभिनय, पात्रों की प्रकृति, रस और भाव की उत्पत्ति, वाद्य और नृत्य की विधि, रंगमंच की संरचना, दर्शकों की भूमिका आदि का सूक्ष्म विवेचन है।
नाट्यशास्त्र की व्यापकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह केवल नाटक-रचना का नियमावली ग्रंथ न होकर सम्पूर्ण भारतीय सौंदर्यशास्त्र और रंगमंचीय परंपरा का आधार-ग्रंथ है।
नाट्य शब्द का अर्थ एवं नाट्य की परिभाषा
नाट्य शब्द का अर्थ
नाट्य शब्द का तात्पर्य उस काव्य से है जिसे अभिनय और रंगमंच पर प्रस्तुत करके प्रत्यक्ष अनुभव कराया जा सके।
साहित्यशास्त्र में काव्य के दो भेद माने गए हैं – दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य।
- दृश्य काव्य वह है, जिसमें भावक (दर्शक) किसी घटना या वस्तु का प्रत्यक्ष चाक्षुष ज्ञान ग्रहण करता है। यह रंगमंच पर अभिनीत होकर साकार रूप में आनंद प्रदान करता है।
- श्रव्य काव्य वह है, जिसमें आनंद केवल श्रवण और कल्पना मार्ग से प्राप्त होता है।
जिसका अभिनय किया जा सके, उसे दृश्य काव्य कहते हैं – “दृश्यं तत्राभिनेयं”। यही दृश्य काव्य रूप या रूपक के नाम से भी जाना जाता है।
रूपक शब्द की व्युत्पत्ति
‘रूपक’ शब्द की निष्पत्ति रूप धातु में ण्वुल प्रत्यय के योग से होती है।
- ‘रूप’ और ‘रूपक’ दोनों ही शब्द साहित्य में ‘नाट्य’ के द्योतक हैं।
- नाट्यशास्त्र में ‘दशरूप’ शब्द का प्रयोग नाट्य की विविध विधाओं के अर्थ में किया गया है।
नाट्य की परिभाषा
नाट्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए दशरूपककार आचार्य धनंजय ने इसकी परिभाषा दी है –
“अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्”
अर्थात्, किसी अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य कहलाता है।
दूसरे शब्दों में, जीवन के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, वीरता, करुणा आदि भावों की विविध स्थितियों का अनुकरण जब अभिनय, संवाद और संगीत के माध्यम से रंगमंच पर किया जाता है, तो वही नाट्य कहलाता है।
भरतनाट्यम् : नृत्य रूप में नाट्य का स्वरूप
भरतनाट्यम् (Bharatanatyam) को भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है।
- इसका विकास और प्रसार तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा हुआ।
- प्रारंभिक काल में देवदासियों से जुड़ा होने के कारण इसे उचित सम्मान नहीं मिला।
- किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ई. कृष्ण अय्यर और रुकीमणि देवी के प्रयासों से यह नृत्य पुनः प्रतिष्ठित हुआ।
भरतनाट्यम् मुख्यतः दो अंशों में सम्पन्न होता है –
- नृत्य – जो शरीर के अंगों की गतियों से उत्पन्न होता है।
- अभिनय – जिसमें रस, भाव और कल्पना की अभिव्यक्ति प्रमुख होती है।
इस प्रकार भरतनाट्यम् नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि नाट्य के रसात्मक और भावात्मक तत्वों की साकार अभिव्यक्ति भी है।
नाट्यशास्त्र के उद्देश्य और महत्व
भरतमुनि का नाट्यशास्त्र केवल रंगकला की तकनीक का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति है।
- पुरुषार्थ की प्राप्ति – नाटक के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाना।
- सामाजिक शिक्षा – समाज में व्याप्त अन्याय, दुख और कुरीतियों को उजागर कर लोगों को जागरूक करना।
- मनोरंजन – कला के माध्यम से जनमानस को आनंद और सौंदर्य-बोध प्रदान करना।
- समन्वय – नृत्य, संगीत, अभिनय, शिल्प और साहित्य जैसी विविध कलाओं को एक मंच पर लाना।
नाट्यशास्त्र में वर्णित प्रमुख विषय
1. अभिनय का चतुर्विध स्वरूप
भरतमुनि ने अभिनय को चार भागों में विभाजित किया –
- आंगिक अभिनय – शारीरिक हावभाव और मुद्राएँ।
- वाचिक अभिनय – संवाद, उच्चारण और ध्वनि।
- आहार्य अभिनय – वेशभूषा, अलंकरण और दृश्य सज्जा।
- सात्त्विक अभिनय – भावनात्मक अभिव्यक्ति, आँसू, रोमांच, भय आदि।
2. रस और भाव का सिद्धांत
नाट्यशास्त्र में रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया का गहन विवेचन है। आठ प्रमुख रस बताए गए – श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत। बाद में शान्त रस को भी जोड़ा गया।
3. नाट्यरूप और दशरूपक
भरतमुनि ने नाटकों के विभिन्न रूपों की चर्चा की है। इनमें नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोग, भाण आदि शामिल हैं।
4. संगीत और नृत्य
नाट्यशास्त्र में गीत और वाद्य की विधि, स्वर, लय, ताल तथा नृत्य की मुद्राओं का अत्यंत सूक्ष्म विवरण है। “ताण्डव” और “लास्य” नृत्य की चर्चा भी विस्तार से की गई है।
5. रंगमंच और दर्शक
नाट्यशास्त्र में रंगमंच की रचना, सजावट, पर्दा, मंच की दिशा आदि का विस्तृत विवरण है। साथ ही दर्शकों की भूमिका पर भी बल दिया गया है, क्योंकि नाटक तभी सफल है जब दर्शक उससे रसास्वादन कर सके।
नाट्यशास्त्र के पाठ और संस्करण
नाट्यशास्त्र की पाठ-परंपरा बहुत जटिल रही है।
- षट्साहस्त्री संहिता – लगभग 6000 श्लोकों वाला संक्षिप्त पाठ।
- द्वादशसाहस्त्री संहिता – 12000 श्लोकों वाला विस्तृत पाठ।
विद्वानों में इस पर मतभेद रहा कि कौन सा पाठ प्राचीन है।
- धनञ्जय ने षट्साहस्त्री को प्रामाणिक माना।
- भोजराज ने द्वादशसाहस्त्री को प्रमुख माना।
- अभिनवगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध व्याख्या अभिनवभारती षट्साहस्त्री पाठ पर लिखी।
शारदातनय ने अपने भावप्रकाशन में दोनों पाठों की चर्चा की है। कई विद्वान मानते हैं कि पहले एक विस्तृत पाठ था, जिसे बाद में संक्षेपित किया गया।
नाट्यशास्त्र की व्याख्या परंपरा
नाट्यशास्त्र पर अनेक आचार्यों ने व्याख्या लिखी, परन्तु सबसे महत्वपूर्ण है –
- अभिनवगुप्त की अभिनवभारती – जिसमें उन्होंने नाट्यशास्त्र के सौंदर्यशास्त्रीय पहलुओं को गहराई से समझाया।
- अन्य विद्वानों जैसे धनिक, भोज, रामकृष्ण कवि आदि ने भी अपने मत प्रस्तुत किए।
इन व्याख्याओं से यह सिद्ध होता है कि नाट्यशास्त्र केवल प्राचीन काल में ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत में भी नाट्यकला का मूल ग्रंथ बना रहा।
नाट्यशास्त्र का प्रभाव और योगदान
- भारतीय नाट्यकला पर प्रभाव – संस्कृत नाटकों से लेकर लोकनाट्य और आधुनिक रंगमंच तक, सभी पर इसका गहरा असर है।
- साहित्य और काव्यशास्त्र पर प्रभाव – रस सिद्धांत ने बाद के आचार्यों जैसे आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि को प्रभावित किया।
- नृत्य और संगीत पर प्रभाव – भरतमुनि के नृत्य और लय संबंधी सिद्धांत आज भी भारतीय शास्त्रीय नृत्यकलाओं (भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी) में प्रयुक्त होते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय महत्व – नाट्यशास्त्र विश्व का पहला ऐसा ग्रंथ है, जिसमें नाटक, अभिनय और सौंदर्यशास्त्र का इतना व्यापक विवेचन मिलता है। पश्चिमी नाट्यशास्त्र (जैसे एरिस्टोटल की Poetics) से भी इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।
नाट्यशास्त्र की मौलिकता और सार्वभौमिकता
नाट्यशास्त्र का सबसे बड़ा महत्व इसकी मौलिकता और व्यापकता में है।
- इसने कला को केवल राजदरबार या विशेष वर्ग तक सीमित न रखकर, सम्पूर्ण समाज के लिए सुलभ बनाया।
- इसमें मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षण और जीवन-दर्शन का भी समन्वय है।
- इसकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि कला मानव जीवन की गहनतम भावनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है।
नाट्यशास्त्र के अध्याय
भरतमुनि का नाट्यशास्त्र केवल अभिनय या नाटक की विधियों का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक सम्पूर्ण कलावैज्ञानिक शास्त्र है। इसमें कुल 36 अध्याय (कुछ पाठान्तरों में 37) उपलब्ध हैं, जिनमें नाटक, रस, अभिनय, संगीत, नृत्य और रंगमंच से संबंधित सभी पहलुओं का विस्तृत विवेचन है।
अभिनवगुप्त के अनुसार नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय और लगभग 4426 श्लोक (कुछ गद्यांश सहित) हैं। इन अध्यायों की संख्या भी प्रतीकात्मक मानी जाती है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा दर्शन में 36 मूल तत्त्व स्वीकार किए गए हैं और नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय इन्हीं तत्त्वों के प्रतीक माने गए हैं।
1. नाट्य की उत्पत्ति और प्रारंभिक विधान
- पहला अध्याय – नाट्य की उत्पत्ति का विवरण।
- दूसरा अध्याय – मण्डप (रंगमंच) की रचना और विधान।
- तीसरा से पाँचवाँ अध्याय – नाट्य आरंभ से पूर्व की विधियाँ और प्रक्रियाएँ।
2. रस और भाव
- छठा और सातवाँ अध्याय – रस और भाव का विस्तृत विवेचन।
- यहीं से भारतीय काव्यशास्त्र का रस सिद्धांत जन्म लेता है।
3. अभिनय का स्वरूप
- आठवाँ और नवाँ अध्याय – अंग और उपांग के माध्यम से अभिनय का स्वरूप।
- अगले चार अध्याय (10 से 13) – गतियों और करणों का विवरण।
4. छंद, अलंकार और स्वरविधान
- अध्याय 14 से 17 – छंद, अलंकार और स्वरों की व्यवस्था।
- इसमें काव्य की लयात्मकता और ध्वनि की सौंदर्यात्मकता का विवेचन है।
5. नाटक के भेद और वृत्ति
- अध्याय 18 और 19 – नाटकों के भेद और कलेवर का विवरण।
- 20वाँ अध्याय – वृत्ति का विवेचन।
6. अभिनय की विविधताएँ
- 21वाँ अध्याय – विभिन्न प्रकार के अभिनयों की विशेषताएँ।
- 22 से 34 अध्याय – गीत और वाद्य से संबंधित विस्तृत विवरण।
7. भूमिविकल्प और उपसंहार
- 35वाँ अध्याय – भूमिविकल्प का विवेचन।
- 36वाँ अध्याय – उपसंहारात्मक, जिसमें संपूर्ण ग्रंथ का समापन है।
नाट्यशास्त्र के अध्याय : सारणीबद्ध रूप
| क्रमांक | अध्याय का नाम (संस्कृत/संक्षिप्त) | विषय-वस्तु / विवरण |
|---|---|---|
| 1 | नाट्योत्पत्ति (Natyotpatti) | नाट्य की उत्पत्ति और उद्देश्य |
| 2 | मण्डपविधान (Mandapavidhan) | नाट्यशाला/मण्डप की संरचना का विधान |
| 3–5 | पूर्वरंग (Purvaranga) | नाट्य आरम्भ से पूर्व की अनुष्ठानिक प्रक्रियाएँ |
| 6 | रस (Rasa) | रस सिद्धान्त की व्याख्या |
| 7 | भाव (Bhava) | भावों का स्वरूप और वर्गीकरण |
| 8–9 | उपाङ्ग एवं अङ्ग (Upanga & Anga) | अभिनय में अंग-उपांगों की भूमिका |
| 10–13 | चारी एवं करण (Chari & Karana) | गतियों और करणों का विवेचन |
| 14–17 | छन्द एवं अलंकार (Chhanda & Alankara) | छन्द, अलंकार और स्वरविधान |
| 18–19 | दशरूप एवं कलेवर (Dasharupa & Kalevara) | नाट्य के भेद और नाट्यकलेवर का विवरण |
| 20 | वृत्ति विवेचन (Vritti-vivechana) | वृत्तियों का विवेचन |
| 21 | अभिनय (Abhinaya) | विभिन्न प्रकार के अभिनयों की विशेषताएँ |
| 22–34 | गीत–वाद्य विधान (Geet–Vadya Vidhan) | वाद्य, स्वर और संगीत का विस्तृत विवरण |
| 35 | भूमिविकल्प (Bhumivikalpa) | भूमिविकल्प और मंच व्यवस्था |
| 36 | उपसंहार (Upasamhara) | नाट्यशास्त्र का निष्कर्ष एवं उपसंहार |
- कुछ पाण्डुलिपियों में 37वाँ अध्याय भी मिलता है, जिसका उल्लेख निर्णयसागरी संस्करण में है।
- चौखंबा संस्कृत सीरीज, वाराणसी से भी एक भिन्न पाठ प्रकाशित हुआ है।
नाट्यशास्त्र के पाठान्तर
नाट्यशास्त्र मुख्यतः दो पाठान्तरों में उपलब्ध है –
- औत्तरीय पाठ
- दाक्षिणात्य पाठ
इसके अतिरिक्त एक 37वाँ अध्याय भी कुछ पांडुलिपियों में कठिनाई से मिलता है, जिसे निर्णयसागरी संस्करण के संपादक ने सम्मिलित किया है।
- चौखंबा संस्कृत सीरीज, वाराणसी से प्रकाशित संस्करण ‘निर्णयसागरी पाठ’ से भिन्न है।
- इस प्रकार नाट्यशास्त्र की पाठ-परंपरा में कई भिन्नताएँ पाई जाती हैं।
नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों की सूची
- नाट्योत्पत्ति
- नाट्यमण्डप
- पूर्वरंग
- पूजाविधान
- ताण्डवविधान
- रस
- भाव
- उपाङ्ग अभिनय
- अङ्ग अभिनय
- चारीविधान
- मण्डलविधान
- गति
- प्रचार
- करणा
- युक्ति
- धर्मी
- व्यञ्जक
- छन्दोविधान
- छन्दोविचिति
- काव्यलक्षण
- काकुस्वर
- व्यञ्जन
- दशरूप
- सन्धिनिरूपण
- वृत्तिविकल्पन
- आहार्याभिनय
- सामान्याभिनय
- नेपथ्य
- पुंस्त्र्युपचार
- चित्राभिनय
- विकृतिविकल्प
- सिद्धि
- व्यञ्जकजाति
- विकल्प
- तातोद्यविधान (वाद्य का विवेचन)
- भूमिविकल्प एवं उपसंहार
नाट्यशास्त्र के विषयों का संक्षिप्त परिचय
भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र भारतीय काव्यशास्त्र और रंगमंच परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 36 अध्यायों के अंतर्गत नाट्य के विभिन्न पक्षों—नाट्य की उत्पत्ति, रंगमंच, अभिनय, रस-भाव, छन्द-अलंकार, भाषा, वेशभूषा और वाद्य संगीत आदि—का विस्तृत विवेचन किया गया है। यहाँ काशी संस्करण के आधार पर प्रारंभिक अध्यायों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है।
प्रथम अध्याय : नाट्यवेद की उत्पत्ति
भरतमुनि ने आत्रेय आदि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में बताया कि नाट्यवेद का निर्माण चारों वेदों के अंशों से हुआ है—
- ऋग्वेद से पाठ्यांश,
- सामवेद से संगीत,
- यजुर्वेद से अभिनय,
- अथर्ववेद से रस।
भरतमुनि ने इस वेद को अपने सौ पुत्रों को पढ़ाया।
द्वितीय अध्याय : रंगमंच (पेक्षागृह)
इस अध्याय में नाट्यप्रदर्शन हेतु आवश्यक पेक्षागृह का वर्णन है। इसमें उसके तीन प्रकार, उनके शिल्प, आकार तथा साधनों का विस्तृत विवेचन किया गया है।
तृतीय अध्याय : धार्मिक क्रियाएँ और पूजा
इसमें नाट्यमण्डप में सम्पन्न की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं का निरूपण है। विभिन्न देवताओं की पूजा तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों का उल्लेख किया गया है।
चतुर्थ अध्याय : ताण्डव और अंगहार
भरतमुनि ने देवताओं के सम्मुख अमृत मन्थन का नाट्यप्रयोग तथा महेश्वर के आदेश से ताण्डव की उत्पत्ति का वर्णन किया है। ताण्डव नृत्य, अंगहार और शिल्प की सांगोपांग विवेचना भी की गई है।
पंचम अध्याय : पूर्वरंग विधान
इसमें नाट्यप्रयोग के आरम्भ में किये जाने वाले नान्दी, प्रस्तावना और ध्रुवाओं का विस्तृत विवेचन है।
षष्ठ अध्याय : रस का विवेचन
भरतमुनि ने रसों का सम्यक स्वरूप, उनके प्रकार और महत्व का निरूपण किया है। यह अध्याय भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत की नींव है।
सप्तम अध्याय : भावों का विवेचन
इसमें स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव (संचारी भाव) और सात्विक भाव का विस्तारपूर्वक वर्णन है।
अष्टम अध्याय : अभिनय का वर्गीकरण
नाट्य में चार प्रकार के अभिनय बताए गए हैं—
- आंगिक,
- वाचिक,
- आहार्य,
- सात्विक।
इनकी विशेषताओं का विस्तृत विवेचन किया गया है।
नवम अध्याय : आंगिक अभिनय
इस अध्याय में शरीर के अंगों—हस्त, कुक्षि, कटि, जानु और पाद—के अभिनय का विवेचन किया गया है। साथ ही, नृत्य में हस्तमुद्राओं की परमोपयोगिता बताई गई है।
दशम अध्याय : अंगों का परिचालन
वक्ष, कटि और शरीर के अन्य भागों के पाँच प्रकार के परिचालन और उनके उपयुक्त अवसरों पर अभिनय में प्रयोग का वर्णन है।
एकादश अध्याय : चारियाँ और करण
इसमें चारियों के 16 भौमि और 16 आकाशिकी प्रकार, उनके लक्षण और प्रयोग बताए गए हैं। साथ ही, खण्ड करण और मण्डल की नाटयोपयोगिता का विवेचन किया गया है।
द्वादश अध्याय : मण्डल विधान
इस अध्याय में मण्डलों की संख्या, लक्षण और नाट्यप्रयोग में उनके उपयोग का वर्णन है।
त्रयोदश अध्याय : गति प्रचार
पात्रों की गति उनके अवसर और अवस्था के अनुकूल किस प्रकार होनी चाहिए, इसका विवेचन है। देव, राजा, मध्यवर्ग, स्त्री-पुरुष और निम्न वर्ग की गतियों का भी विवरण दिया गया है।
चतुर्दश अध्याय : प्रवृत्तियाँ
रंगमंच पर घर, उपवन, जल, स्थल आदि प्रदेशों को दिखाने की पद्धति तथा चार प्रकार की प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है।
पञ्चदश अध्याय : वाचिक अभिनय – अक्षर और छन्द
यहाँ वाचिक अभिनय का आरम्भ होता है। इसमें अक्षरों, स्वर-व्यंजन, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, गुरु-लघु, यति और मात्रा का विवेचन है।
षोडश अध्याय : वृत्तियाँ और छन्द
वाचिक अभिनय में प्रयुक्त वृत्तियों और छन्दों का निरूपण किया गया है। इसमें आर्या और उसके विभिन्न प्रभेदों का भी वर्णन है।
सत्रहवाँ अध्याय : काव्यलक्षण और अलंकार
इस अध्याय में काव्य के 36 लक्षणों और अलंकारों (उपमा, रूपक, दीपक, यमक आदि) का विवेचन है। इनके गुण-दोष भी बताए गए हैं।
अठारहवाँ अध्याय : भाषाएँ और विभाषाएँ
नाट्य में संस्कृत, प्राकृत और देशी भाषाओं (अपभ्रंश) के प्रयोग का वर्णन है। उच्चारण भेद और भाषा परिवर्तन की विशेषताओं का भी विवेचन किया गया है।
उन्नीसवाँ अध्याय : पात्र-सम्बोधन और भाषा-शैली
विभिन्न वर्गों—उच्च, मध्यम और नीच—के पात्रों को संबोधित करने की प्रणालियाँ और उनके नामकरण की विधियाँ दी गई हैं। साथ ही, स्वर-व्यंजन, द्रुत और विलम्बित गेय अलंकारों का भी उल्लेख है।
बीसवाँ अध्याय : दशरूपक
इस अध्याय में नाटक के दशरूपक—भान, प्रकरण, व्यायोग, डिम, समवकार, अंक, वीथि, ईहामृग, प्रहसन और अंकशक—का लक्षण और वैशिष्ट्य प्रस्तुत है।
इक्कीसवाँ अध्याय : सन्धि और अवस्थाएँ
नाटक की कथा-वस्तु के आधिकृत और प्रासंगिक भेदों का निरूपण है। इसमें पाँच सन्धियाँ, पाँच अवस्थाएँ, पाँच अर्थप्रकृतियाँ तथा उनके अवयवों का विस्तृत विवेचन किया गया है।
बाईसवाँ अध्याय : वृत्तियाँ
नाटकोपयोगी वृत्तियों का वर्णन है। भगवान विष्णु और मधुकैटभ युद्ध की कथा के माध्यम से इन वृत्तियों की उत्पत्ति और उनके रसों से संबंध को स्पष्ट किया गया है।
तेइसवाँ अध्याय : आहार्य अभिनय
इसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार और पात्रों की वेशभूषा से संबंधित नियम बताए गए हैं।
चौबीसवाँ अध्याय : सामान्य अभिनय
इस अध्याय में सभी प्रकार के अभिनयों का सामान्य विवेचन किया गया है।
पच्चीसवाँ अध्याय : वैशिक पुरुष
इसमें वैशिक पुरुष का लक्षण और उसके सामान्य गुणों का वर्णन है।
छब्बीसवाँ अध्याय – चित्राभिनय
इस अध्याय में चित्राभिनय का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ उन आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनयों के विशेष अंगों का उल्लेख है, जिनका सामान्य अभिनय के अंतर्गत विस्तार से वर्णन नहीं हो पाया था।
चित्राभिनय का आशय है – सूक्ष्म और विशिष्ट परिस्थितियों में किए जाने वाले अभिनय का निरूपण, जिसमें भावों और क्रियाओं की सूक्ष्मता को विशेष महत्त्व दिया गया है।
सत्ताइसवाँ अध्याय – सिद्धिव्यंजनाध्याय
इस अध्याय को सिद्धिव्यंजनाध्याय कहा जाता है। इसमें नाट्य-प्रदर्शन में प्राप्त होने वाली देवी सिद्धि और मानुषी सिद्धि दोनों का सांगोपांग विवेचन है। साथ ही, नाट्य प्रस्तुति के समय उत्पन्न होने वाले विघ्नों और व्यवधानों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यह अध्याय दर्शाता है कि नाट्य केवल कला नहीं बल्कि दैवीय अनुग्रह और साधना से संपन्न एक गंभीर प्रक्रिया भी है।
अट्ठाइसवाँ अध्याय – संगीत शास्त्र
नाट्यशास्त्र के इस अध्याय में संगीत शास्त्र का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। इसमें स्वरों, रागों, गान विधियों और वाद्य-वादन की संगति का उल्लेख मिलता है। भरतमुनि ने संगीत को नाट्यकला का अनिवार्य अंग बताया है, क्योंकि बिना संगीत के नाट्यकला की प्रभावोत्पादकता अधूरी रहती है।
उन्तीसवाँ अध्याय – जाति और रस प्रयोग
इस अध्याय में विभिन्न जातियों के रसाश्रित प्रयोग का विस्तार से वर्णन है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार वर्ण और अलंकार नाट्यकला में प्रयोग होते हैं और उनकी उपयुक्तता क्या है। जाति के आधार पर भाव और रस की अभिव्यक्ति का यह विवेचन नाट्यशास्त्र को अत्यंत सूक्ष्म और शास्त्रीय गहराई प्रदान करता है।
तीसवाँ अध्याय – वंशी वादन
नाट्यशास्त्र का यह अध्याय वंशी (बांसुरी) के स्वरूप और उसकी वादन विधि पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि बांसुरी के स्वर किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और नाट्य-प्रदर्शन में उनका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। इस अध्याय में वंशी की संगीतात्मक भूमिका और उसकी भावानुकूलता का भी विवेचन है।
इकतीसवाँ अध्याय – ताल विधान
इस अध्याय में ताल, लय और समय-नियमन के लिए ताल विधान का विस्तृत निरूपण है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार विभिन्न तालों का प्रयोग करके नाट्य और संगीत को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ताल को नाट्य और संगीत का आधारभूत तत्व मानकर इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है।
बत्तीसवाँ अध्याय – ध्रुवाध्याय
इस अध्याय को ध्रुवाध्याय कहा जाता है। इसमें नाट्य प्रस्तुति के दौरान पात्रों की विभिन्न अवस्थाओं और प्रसंगों में गाई जाने वाली ध्रुवाओं (नियत गान) का उल्लेख है। ध्रुवा गान पात्र की मनःस्थिति और प्रसंग विशेष को स्पष्ट करने में सहायक होता है।
तैतीसवाँ अध्याय – वाद्याध्याय
नाट्यशास्त्र का यह अध्याय वाद्याध्याय कहलाता है। इसमें मृदंग आदि अवन वाद्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। वाद्यों के प्रकार, उनकी रचना, वादन विधि और नाट्य में उनकी भूमिका का सूक्ष्म विवेचन इस अध्याय में प्राप्त होता है।
चौँतीसवाँ अध्याय – नायक-नायिका का स्वरूप
इस अध्याय में पुरुष और स्त्रियों की विभिन्न प्रकृतियों और स्वभावों का विवेचन किया गया है। विशेष रूप से चार प्रकार के नायकों के लक्षणों का निरूपण मिलता है। यह अध्याय नाट्य में पात्र-चित्रण और चरित्र-निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
पैंतीसवाँ अध्याय – भूमिका पात्र विकल्पाध्याय
इस अध्याय को भूमिका पात्र विकल्पाध्याय कहा जाता है। इसमें नाट्यमंडली के सदस्यों का विभाजन करते समय उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं और योग्यताओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। नाट्य दल के प्रबंधन और संगठन की दृष्टि से यह अध्याय अत्यंत उपयोगी है।
छत्तीसवाँ अध्याय – नाट्य का अवतरण
यह नाट्यशास्त्र का अंतिम अध्याय है। इसमें मुनियों ने भरतमुनि से पृथ्वी पर नाट्य के अवतरित होने के विषय में पुनः प्रश्न किया। इसके उत्तर में भरतमुनि ने दो आख्यान प्रस्तुत किए –
- भरतपुत्रों द्वारा मुनियों के उपहासकारी नाट्य के कारण ऋषियों के शाप की कथा।
- राजा नहुष की प्रार्थना पर स्वर्गस्थ नाट्य का पृथ्वी पर अवतरण।
कुछ संस्करणों में नाट्यशास्त्र 36 अध्यायों का है, तो कुछ में 37 अध्याय बताए गए हैं, जिसमें नहुष की कथा का भी वर्णन मिलता है।
नाट्यशास्त्र की विशेषताएँ
- नाट्यशास्त्र में कुल 12,000 पद्य (4426 श्लोक और कुछ गद्य) थे।
- इसे द्वादशसाहस्री संहिता भी कहा जाता है।
- बाद में इसका संक्षिप्त संस्करण (6000 पद्य) प्रचलित हुआ, जिसे षट्साहस्री संहिता कहा गया।
- भरतमुनि को ‘उभय संहिताकार’, ‘द्वादशसाहस्रीकार’ और ‘षट्साहस्रीकार’ कहा जाता है।
- नाट्यशास्त्र के वाक्यों को भरतसूत्र कहते हैं।
- यह ग्रंथ नाट्य संविधान और रस सिद्धांत की मौलिक संहिता है।
- इसे आर्ष सम्मान प्राप्त है और पिछले 2000 वर्षों में नाट्य और रस का ऐसा विस्तृत निरूपण किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता।
नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय (एक-पंक्ति सारांश)
| क्रमांक | अध्याय का नाम (संस्कृत) | विस्तृत एक-पंक्ति सारांश |
|---|---|---|
| 1 | नाट्य उत्पत्ति (नाट्यनाट्य) | नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति, देवताओं द्वारा नाट्य का निर्माण और उसकी सामाजिक उपयोगिता का वर्णन। |
| 2 | मण्डपविधान | नाट्य प्रस्तुतियों हेतु रंगमंच (मण्डप) की रचना, माप, दिशा और निर्माण नियम। |
| 3 | पूर्वरंग-पूजा | नाटक आरम्भ से पहले देवताओं की पूजा, अनुष्ठान और मंगलाचरण की प्रक्रिया। |
| 4 | ताण्डव पूर्वरंग | नृत्य और ताण्डव की विधियाँ, पूर्वरंग के दौरान होने वाले नृत्य रूप। |
| 5 | अर्हण-पूर्वरंग विधान | नाट्य प्रदर्शन से पहले की उपासना, पूजा और अनुष्ठानिक क्रियाओं का विस्तार। |
| 6 | रस विधान | रसों का स्वरूप, उनके प्रकार और उत्पत्ति के साधन – रससिद्धान्त का मूल विवेचन। |
| 7 | भाव विधान | स्थायी, व्यभिचारी और सात्विक भावों का विश्लेषण; भाव-रस संबंध का प्रतिपादन। |
| 8 | उपाङ्ग अभिनय | नेत्र, भ्रू, नासिका आदि उपांगों के माध्यम से अभिनय की अभिव्यक्ति। |
| 9 | अङ्ग अभिनय | हस्त, पाद, वक्ष, कटि आदि प्रमुख अंगों द्वारा अभिनय और उनकी विशेषताएँ। |
| 10 | चारी विधान | चारियों (चालों) का वर्णन, जो गतियों और नृत्याभिनय का आधार हैं। |
| 11 | मण्डल विधान | नृत्य में मण्डल (वृत्ताकार गतियाँ) और उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति। |
| 12 | गति प्रचार | गतियों के प्रकार, उनकी उपयुक्तता और भावानुसार प्रयोग। |
| 13 | करण विधान | करों (हस्त-मुद्राओं) का विवेचन, उनके अर्थ और प्रयोजन। |
| 14 | युक्ति | अभिनय व नाट्य प्रस्तुति में प्रयुक्त युक्तियाँ और तकनीकी पक्ष। |
| 15 | धर्मी | नाट्यधर्मी – लोकधर्मी और नाट्यधर्मी, उनके बीच का अंतर और प्रयोग। |
| 16 | व्यञ्जक | अभिनय के व्यंजक तत्त्व – भाषा, भाव और संकेतों की भूमिका। |
| 17 | छन्दोविधान | छन्दों की संरचना, प्रकार और नाट्य में उनका प्रयोग। |
| 18 | छन्दोविचिति | छन्दों की विविधता और अनुप्रास, अनुपात, गति आदि का विवेचन। |
| 19 | काव्यलक्षण | नाट्य में प्रयुक्त काव्य के लक्षण और उनकी काव्यात्मक विशेषताएँ। |
| 20 | काकुस्वर | काकु (स्वरभेद) और स्वर-प्रयोग के नियम, संवाद की भावपूर्ण प्रस्तुति। |
| 21 | व्यञ्जन | उच्चारण, स्वर-व्यंजनों के गुण और अभिनय में उनका प्रयोग। |
| 22 | दशरूप निरूपण | नाटक के दशरूप (भान, प्रकरण, डिम, समवकार, व्यायोग आदि) का वर्णन। |
| 23 | सन्धि निरूपण | सन्धि (मुक्क, प्रकीर्णक, गर्भ, अवमार्ग, निर्वहण आदि) का विश्लेषण। |
| 24 | वृत्ति विकल्पन | चार वृत्तियों (भारती, आरण्य, कैशिकी, सात्वती) का विवेचन। |
| 25 | आहार्य अभिनय | वेशभूषा, आभूषण, वस्त्र और आहार्य सामग्री का वर्णन। |
| 26 | सामान्य अभिनय | सामान्य अभिनय की विशेषताएँ, जो सभी रूपों में प्रयुक्त होती हैं। |
| 27 | नेपथ्य विधान | नेपथ्य (पर्दे के पीछे का कार्य), साज-सज्जा और रंगमंच व्यवस्था। |
| 28 | पुंस्त्र्य उपचार | पात्रों में स्त्री और पुरुष रूपों की प्रस्तुति की कला। |
| 29 | चित्र अभिनय | चित्र, आकृतियों और कलात्मक माध्यमों द्वारा अभिनय की विशेषताएँ। |
| 30 | विकृति विकल्प | विकृत अभिनय, हास्य और व्यंग्यात्मक रूपों का वर्णन। |
| 31 | सिद्धि व्यञ्जक | नाटक की सफलता के साधन और दर्शकों पर उसके प्रभाव। |
| 32 | जाति विकल्प | जातियों (साहित्यिक व नाट्यिक परम्पराएँ) का विवेचन। |
| 33 | तातोद्य विधान | तात वाद्यों (स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स) का विवेचन। |
| 34 | सुषिरातोद्य लक्षण | सुषिर वाद्यों (वायु वाद्य जैसे बाँसुरी) का विवेचन। |
| 35 | ताल गुण दोष विचार | तालों के प्रकार, गुण-दोष और उनका उपयोग। |
| 36 | प्रकृति-नाट्यशाप-भूमिकाविकल्प-गुह्यतत्त्वकथन | नाट्य की प्रकृति, श्राप, भूमिकाएँ और गूढ़ तत्त्वों का उपसंहार। |
👉 इस प्रकार नाट्यशास्त्र के अध्याय केवल नाटक और अभिनय की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच और सौंदर्यशास्त्र के एक सम्पूर्ण विश्वकोश के रूप में सामने आते हैं।
नाट्य साहित्य का उद्भव
संस्कृत रूपकों के उद्भव और विकास का प्रश्न नाम-रूपात्मक जगत की सृष्टि की भांति विवादास्पद रहा है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इसके उद्भव के विषय में भिन्न-भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन भारतीय परंपरा नाट्यवेद का रचयिता ब्रह्मा को मानती है तथा लोक-प्रचारक के रूप में भरतमुनि को निर्दिष्ट करती है, जबकि आधुनिक विद्वान इससे भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं।
उद्भव सम्बन्धी भारतीय मत
1. दैवीय उत्पत्ति सिद्धान्त
इस सिद्धान्त के अनुसार नाट्यविद्या का उद्भव देवों की प्रार्थना पर हुआ।
- शुभंकर ने अपने संगीत दामोदर में लिखा है कि इन्द्र के आग्रह पर ब्रह्मा ने एक ऐसे वेद की रचना की जिससे सामान्य जन का मनोरंजन हो सके।
- इस प्रकार ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस ग्रहण कर पंचमवेद नाट्यवेद की रचना की गई।
- सर्वप्रथम भगवान शिव ने ब्रह्मा को नाट्यवेद की शिक्षा दी, फिर ब्रह्मा ने भरतमुनि को और भरतमुनि ने इसे मानव समाज में प्रचारित किया।
- दशरूपककार आचार्य धनंजय ने भी इसी मत को स्वीकार किया है।
2. संवादसूक्त सिद्धान्त
इस मत के अनुसार नाटक का बीज वेदों में निहित संवादों से अंकुरित हुआ।
- ऋग्वेद के यम-यमी संवाद, पुरूरवा-उर्वशी संवाद, इन्द्र-इन्द्राणी संवाद आदि इसके प्रमाण हैं।
- यजुर्वेद में अभिनय, सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में रसों की संस्थिति विद्यमान है।
- इन्हीं आधारों पर रूपकों का विकास हुआ।
उद्भव सम्बन्धी पाश्चात्य मत
1. वीरपूजा सिद्धान्त
- डॉ. रिजवे के अनुसार नाटकों का उद्भव वीरों की पूजा से हुआ।
- प्राचीन काल में दिवंगत वीरों की आत्मा को प्रसन्न करने हेतु नाट्य-अभिनय किया जाता था।
- किंतु अधिकांश विद्वानों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया।
2. प्रकृति परिवर्तन सिद्धान्त
- डॉ. कीथ का मत है कि प्राकृतिक परिवर्तनों को मूर्त रूप में देखने की अभिलाषा से नाटक का उद्भव हुआ।
- उदाहरण के लिए कंसवध नाटक में इसका संकेत मिलता है।
- किंतु यह मत भी सर्वमान्य नहीं हुआ।
3. पुत्तलिका नृत्य सिद्धान्त
- जर्मन विद्वान डॉ. पिशेल ने नाटक की उत्पत्ति पुत्तलिकाओं के नृत्य और अभिनय से मानी।
- नाटकों में प्रयुक्त सूत्रधार और स्थापक शब्द पुत्तलिका नृत्य से संबंधित माने जाते हैं।
- महाभारत, बालरामायण और कथासरित्सागर में दारूमयी पुत्तलिकाओं का उल्लेख इस मत को पुष्ट करता है।
- परन्तु इसे भी सार्वभौम स्वीकृति नहीं मिली।
4. छाया नाटक सिद्धान्त
- डॉ. लथर्स और क्रोनो के अनुसार नाटकों का उद्भव छाया-नाटकों से हुआ।
- महाभाष्य में छाया-नाटकों और छाया-मूर्तियों का उल्लेख मिलता है।
- किंतु दूतांगद नामक छाया-नाटक अपेक्षाकृत नया होने के कारण इसे मूल स्रोत मानना उचित नहीं माना गया।
5. मेपोल उत्सव सिद्धान्त
- कुछ विद्वानों का मत है कि नाटकों का उद्भव इन्द्रध्वज महोत्सव जैसी परंपराओं से हुआ।
- पाश्चात्य देशों में मई-पोल उत्सव के दौरान लोग बाँस गाड़कर उसके चारों ओर नृत्य-गान करते थे, जो इन्द्रध्वज की तरह था।
- किंतु दोनों उत्सवों के समय और स्वरूप में अंतर होने के कारण यह मत भी मान्य नहीं हुआ।
अन्य मत
कुछ विद्वान नाटकों के उद्भव का आधार लोकप्रिय स्वांग या वैदिक अनुष्ठान मानते हैं, किंतु इन मतों को भी व्यापक स्वीकृति नहीं मिल सकी।
उपर्युक्त भारतीय और पाश्चात्य मतों से स्पष्ट है कि नाट्य साहित्य का उद्भव अत्यन्त विवादास्पद विषय है।
- भारतीय परंपरा नाट्यवेद का रचयिता ब्रह्मा और प्रचारक भरतमुनि को मानती है।
- आधुनिक विद्वानों ने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से इसके उद्भव को जोड़ा।
किन्तु यह कहना कठिन है कि इनमें से कोई एक ही मत नाट्य के उद्भव का मूल कारण है। संभवतः सभी मतों के सम्मिलित प्रभाव से संस्कृत नाट्य का उद्भव और विकास हुआ।
नाट्य का विकास
1. वैदिक युग में नाट्य तत्त्व
ऋग्वेद से ही हमें नाट्य के अस्तित्व का संकेत मिलने लगता है। सोम यज्ञ के अवसर पर दर्शकों के मनोरंजन हेतु अभिनय प्रस्तुत किया जाता था। ऋग्वेद के संवाद सूक्त नाटकीयता की ओर संकेत करते हैं।
- यजुर्वेद में ‘शैलूष’ शब्द आया है, जिसका अर्थ ‘नट’ (अभिनेता) है।
- सामवेद में संगीत का महत्व है, जो नाट्य का मुख्य अंग है।
इस प्रकार गीत, नृत्य और वाद्य – तीनों ही तत्त्व वैदिक काल में प्रचलित थे और नाट्य परम्परा का आधार बने।
2. रामायण और महाभारत में नाट्य तत्त्व
- रामायण में नाट्य के तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।
- महाभारत में नट, नर्तक, गायक और सूत्रधार जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे उस समय तक नाट्यकला की प्रसिद्धि प्रमाणित होती है।
3. पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख
- हरिवंशपुराण में ‘कोबेररम्भाभिसार’ नामक नाटक के अभिनय का वर्णन है। इसमें शूर ने रावण का और मनोवती ने रम्भा का रूप धारण किया था।
- मार्कण्डेय पुराण में भी काव्य, संलाप और गीत के साथ नाटक का उल्लेख मिलता है।
4. व्याकरण और भाषाशास्त्रियों का योगदान
- महर्षि पाणिनी ने अपनी अष्टाध्यायी में नट सूत्रों का उल्लेख किया है।
- महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ‘कंसवध’ और ‘बलिबन्ध’ नामक नाटकों का उल्लेख करते हुए ‘शोभनिक’ शब्द का प्रयोग किया है।
5. कौटिल्य का अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने नट, नर्तक, गायक एवं कुशीलव शब्दों का प्रयोग किया है। यह दर्शाता है कि नाट्यकला उस समय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी।
6. भरतमुनि और नाट्यशास्त्र
संस्कृत नाट्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य भरतमुनि माने जाते हैं। उन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें नाट्य से संबंधित सभी विषयों का विस्तार से विवेचन किया गया है। भरतमुनि ने अन्य आचार्यों – कोटल, शाण्डिल्य, वात्सम, धूर्तिल आदि का भी उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके समय तक नाटकों की रचना और प्रस्तुति विधिवत् विकसित हो चुकी थी।
7. परिष्कृत संस्कृत नाटकों का युग
वेदों से लेकर भरतमुनि तक नाट्य का क्रमिक विकास होता रहा। परिष्कृत संस्कृत नाटकों की रचना का काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का पूर्वार्द्ध माना जाता है।
- प्रारम्भिक संस्कृत नाटकों में भास के नाटक अत्यधिक प्राचीन और प्रतिष्ठित माने जाते हैं।
- भास के पश्चात संस्कृत नाट्य परम्परा को समृद्ध करने वाले आचार्य और कवि थे –
शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति, विशाखादत्त, मुरारि, शक्तिभद्र, दामोदर मिश्र, राजशेखर, दिङ्नाग, कृष्णमिश्र, जयदेव, वत्सराज आदि।
इन उच्चकोटि के नाटककारों ने संस्कृत साहित्य की गौरवशाली परम्परा को और अधिक समृद्ध किया।
नाट्यशास्त्र पर टीका
अभिनवभारती – सर्वाधिक प्रामाणिक टीका
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र पर की गई सबसे महत्वपूर्ण और विद्वत्तापूर्ण टीका अभिनवगुप्त कृत अभिनवभारती है। यह टीका गायकवाड सीरीज़ के अंतर्गत बड़ौदा से प्रकाशित हुई थी। अभिनवगुप्त ने इसे लगभग 1013 ई. में पूरा किया।
यह भाष्य न केवल नाट्यशास्त्र का सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्यान माना जाता है, बल्कि इसे नाट्यशास्त्र का जीवंत दार्शनिक व्याख्यान भी कहा जाता है। अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र को ‘नाट्यवेद’ की संज्ञा दी।
प्रारम्भिक टीकाकार
अभिनवगुप्त से पूर्व भी अनेक विद्वानों ने नाट्यशास्त्र पर टीकाएँ प्रस्तुत कीं। इनमें प्रमुख हैं –
- उद्भट
- लोल्लट
- शंकुक
- कीर्तिधर
- भट्टनायक
इन सभी ने अपने-अपने दृष्टिकोण से भरतसूत्रों की व्याख्या की और काव्यशास्त्र संबंधी विविध वादों की प्रतिष्ठा की।
व्याख्याता आचार्य और उनके वाद
नाट्यशास्त्र के व्याख्याताओं ने अपने-अपने मत प्रस्तुत किए, जिनसे काव्यशास्त्र में विभिन्न वादों का जन्म हुआ। प्रमुख आचार्य और उनके वाद इस प्रकार हैं –
- रीतिवादी – भट्ट उद्भट
- पुष्टिवादी – भट्ट लोल्लट
- अनुमितिवादी – शंकुक
- मुक्तिवादी – भट्टनायक
- अभिव्यक्तिवादी – अभिनवगुप्त
अन्य टीकाकार
इनके अतिरिक्त नखकुट्ट, मातृगुप्त, राहुलक, कीर्तिधर, थकलीगर्भ, हर्षदेव तथा श्रीपादशिष्य ने भी नाट्यशास्त्र पर अपनी-अपनी व्याख्याएँ कीं।
इनमें सबसे प्राचीन टीका श्रीपादशिष्य कृत भरततिलक है।
संगीत और नृत्य पर टीकाएँ
नाट्यशास्त्र के संगीताध्याय पर भी अनेक विद्वानों ने टीकाएँ कीं। इनमें प्रमुख हैं –
- भट्ट सुमनस्
- भट्टवृद्धि
- भट्टयंत्र
- भट्ट गोपाल
भरतमुनि के शिष्य मातंग, दत्तिल और कोहल ने नाट्यशास्त्र के आधार पर स्वतंत्र संगीतपरक ग्रंथों की रचना की।
इसी प्रकार सदाशिव और रंदिकेश्वर ने नृत्य पर तथा भट्ट तौत ने रसमीमांसा पर ग्रंथ लिखे।
नाट्यशास्त्र की मान्यता
- संस्कृत नाट्यकार – कालिदास, बाण, श्रीहर्ष, भवभूति आदि ने नाट्यशास्त्र को अपनी रचनाओं का आधार और प्रमाणिक ग्रंथ माना।
- प्राचीन टीकाकारों ने भरतमुनि को ‘द्वादश साहस्रीकार’ और ‘षट्साहस्रीकार’ की उपाधि दी है।
- नाट्यशास्त्र का रसाध्याय भारतीय मनोविज्ञान का आधार ग्रंथ माना जाता है।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय काव्यशास्त्र का “नाट्य संविधान” और “रस सिद्धान्त” की मौलिक संहिता है। इसके वाक्य भरतसूत्र कहे जाते हैं और यह भारतीय काव्य और नाट्य परम्परा की सबसे बड़ी धरोहर है।
निष्कर्ष
नाट्यशास्त्र भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। भरतमुनि द्वारा रचित यह ग्रंथ केवल नाट्यकला का ही शास्त्र नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन का संवाहक है। इसमें अभिनय, रस-भाव, नृत्य, संगीत, छंद, अलंकार, वाद्य और वेशभूषा तक का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है, जिसके कारण इसे “नाट्यवेद” और भारतीय संस्कृति का “नाट्य-संविधान” कहा गया।
भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इसके उद्भव के विभिन्न मत दिए, किन्तु इसकी व्यावहारिकता और गहनता ने इसे न केवल भारतीय नाट्य परंपरा, बल्कि काव्यशास्त्र और रससिद्धांत का भी आधार-ग्रंथ बना दिया। अभिनवगुप्त की अभिनवभारती जैसी टीकाओं ने इसकी गूढ़ता को और भी स्पष्ट किया।
वेदों से लेकर कालिदास, भास, भवभूति तथा आधुनिक साहित्यकारों तक इसकी परंपरा सतत प्रवाहित रही है। अभिनय का चतुर्विध स्वरूप, रस-भाव का सिद्धांत, संगीत और नृत्य का विवेचन तथा रंगमंच की संरचना – ये सब इसे “कला का वेद” बनाते हैं।
आज भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और सौन्दर्यशास्त्र की जड़ें नाट्यशास्त्र में ही दिखाई देती हैं। यही कारण है कि यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन का सार और संस्कृति की जीवनदृष्टि का दर्पण है। इस प्रकार नाट्यशास्त्र भारतीय संस्कृति का अमर और शाश्वत ग्रंथ है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुपम धरोहर के रूप में सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा।
इन्हें भी देखें –
- सरस्वती पत्रिका : इतिहास, संपादक और संपादन काल
- लेखक: परिभाषा, प्रकार और प्रमुख साहित्यकार
- भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक | Darshan & Pravartak
- संप्रदाय और वाद : उत्पत्ति, परिभाषा, विकास और साहित्यिक-दर्शनिक परंपरा
- गुरु-शिष्य परम्परा: भारतीय संस्कृति की आत्मा और ज्ञान की धरोहर
- हिंदी साहित्य की विधाएँ : विकास, आधुनिक स्वरूप और अनुवाद की भूमिका
- ब्राह्मी लिपि से आधुनिक भारतीय लिपियों तक: उद्भव, विकास, शास्त्रीय प्रमाण, अशोक शिलालेख
- पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द 500+ उदाहरण
- विलोम शब्द | विपरीतार्थक शब्द | Antonyms |500+ उदाहरण
- हिंदी के विराम चिन्ह और उनका प्रयोग | 50 + उदाहरण
- कारक: परिभाषा, भेद तथा 100+ उदाहरण
- शब्द शक्ति: परिभाषा और प्रकार | अमिधा | लक्षणा | व्यंजना