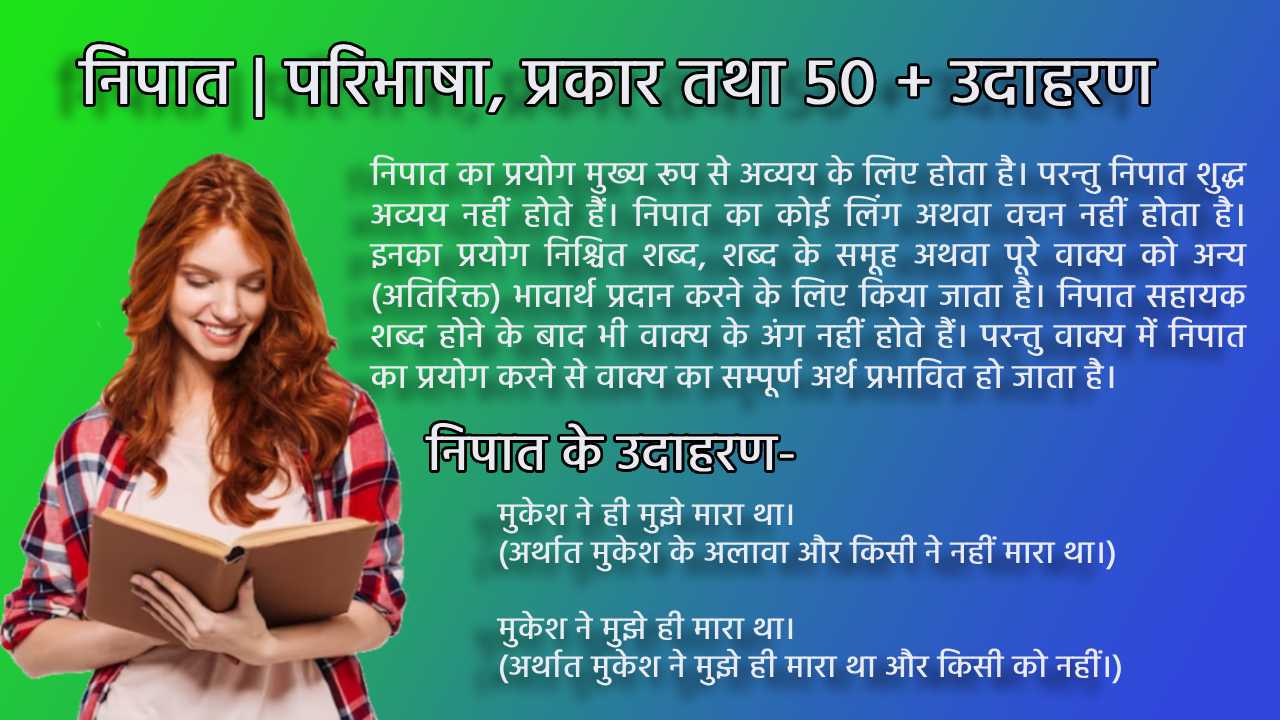निपात का प्रयोग मुख्य रूप से अव्यय के लिए होता है। परन्तु निपात शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। निपात का कोई लिंग अथवा वचन नहीं होता है। इनका प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द के समूह अथवा पूरे वाक्य को अन्य (अतिरिक्त) भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। निपात सहायक शब्द होने के बाद भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। परन्तु वाक्य में निपात का प्रयोग करने से वाक्य का सम्पूर्ण अर्थ प्रभावित हो जाता है।
जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ अथवा भाव में विशेष बल देते हैं, वे अव्यय शब्द, निपात अव्यय कहलाते हैं। हिंदी में अधिकांशतः निपात उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं, जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। अर्थात निपात जिस शब्द के बाद लगते हैं उस शब्द को बल (विशिष्टता) प्रदान करते है। निपात को अवधारक भी कहा जाता है क्योंकि ये शब्द अवधारणा देते है।
निपात (Particle) की परिभाषा
किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी निश्चित शब्द पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को निपात कहते है।
जैसे- ही, भी, तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश आदि।
निपात के उदाहरण
- मुकेश ने ही मुझे मारा था। (अर्थात मुकेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा था।)
- मुकेश ने मुझे ही मारा था। (अर्थात मुकेश ने मुझे ही मारा था और किसी को नहीं।)
- मुकेश ने मुझे मारा ही था। (अर्थात मुकेश ने मुझे सिर्फ मारा था, और कुछ नहीं किया था, जैसे गाली आदि नहीं दिया था।)
- आप ही जाओगे। (अर्थात सिर्फ आप ही जाओगे और कोई नहीं जायेगा।)
- कल ही बारिश होगी। (अर्थात कल ही बारिश होगी दूसरे दिन नहीं।)
- आपको आज रात रुकना ही पड़ेगा।
- आपने तो हद कर दी।
- कल मै भी आपके साथ चलूँगा।
- महात्मा गांधीजी को बच्चे तक जानते है।
- धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता।
- नीरव खाने के साथ पानी भी पिता था।
शब्दों का वर्गीकरण : यास्क मुनि और श्री किशोरीदास वाजपेयी का दृष्टिकोण
मानव भाषाएँ विविधता से पूर्ण हैं और हर भाषा का अपना विशिष्ट शब्द-संग्रह होता है। इन शब्दों का वर्गीकरण समय–समय पर अनेक आचार्यों और भाषाविदों ने विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर किया है। भारतीय भाषाविज्ञान परंपरा में शब्द-वर्गों का सर्वाधिक प्राचीन और वैज्ञानिक वर्गीकरण यास्क मुनि द्वारा माना जाता है। उन्होंने न केवल शब्दों की प्रकृति का विश्लेषण किया, बल्कि उनके व्याकरणिक स्वरूप को भी व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया।
यास्क मुनि का शब्द-वर्गीकरण
यास्क मुनि के अनुसार भाषा के शब्द चार प्रमुख वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। इसका आधार उनके प्रसिद्ध सूत्र में मिलता है—
‘चत्वारि पदजातानि – नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात।’
इस सूत्र का भावार्थ यह है कि पद (शब्द) मूलतः निम्नलिखित चार वर्गों में व्यवस्थित होते हैं—
- नाम (संज्ञाएँ)
- आख्यात (क्रियाएँ)
- उपसर्ग
- निपात
इस वर्गीकरण की विशेषता यह है कि यह शब्दों के अर्थ, प्रयोग और भाषिक संरचना—तीनों को ध्यान में रखकर किया गया है। भारतीय व्याकरण में आज तक जितने भी वर्गीकरण विकसित हुए, उनमें यास्क मुनि की परिकल्पना का आधारभूत स्थान बना रहा।
श्री किशोरीदास वाजपेयी का मत
आधुनिक हिंदी व्याकरण के विख्यात व्याकरणाचार्य श्री किशोरीदास वाजपेयी ने शब्द-वर्गीकरण को सरल और व्यवहारिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भाषा के शब्दों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—
1. नाम और आख्यात (संज्ञाएँ और क्रियाएँ)
ये शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं और वाक्य में अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं।
2. उपसर्ग और निपात (या अव्यय)
ये शब्द स्वयं में स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते। वाक्य में उपस्थित संज्ञा या क्रिया के साथ संयोजित होकर विशेष भाव उत्पन्न करते हैं और अभिव्यक्ति को सुगठित बनाते हैं।
किशोरीदास जी के मत में नाम और आख्यात वाक्य के मूल आधार हैं, जबकि उपसर्ग और निपात इन आधारों को विशिष्ट अर्थ-छटा देने वाले सहायक तत्व हैं।
निपात का स्वरूप और विशेषता
निपात वे शब्द हैं जो वाक्य में प्रमुख अर्थ न देकर भाव, बल, निषेध, प्रश्न, स्वीकृति जैसे सूक्ष्म संकेतों को व्यक्त करते हैं। इनके पास स्वतंत्र वस्तुगत अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें अव्यय वर्ग का सहायक शब्द कहा जाता है।
निम्न शब्द निपात के उदाहरण हैं—
तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश आदि।
इन शब्दों की विशिष्टता यह है कि—
- ये अपने आप में कोई पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करते।
- वाक्य में जुड़कर किसी शब्द, शब्द-समूह या पूरे वाक्य के भाव को बदल देते हैं।
- ये न तो संज्ञा हैं, न विशेषण, न सर्वनाम और न क्रिया-विशेषण; अतः इनका स्थान अन्य शब्द-भेदों से भिन्न है।
उदाहरण के लिए—
- “वह आएगा” और “वह तो आएगा”—दोनों वाक्यों के भाव में स्पष्ट अंतर है।
- “यह कार्य सरल है” और “यह कार्य ही सरल है”—दूसरे वाक्य में निपात ‘ही’ विशेष बल प्रदान करता है।
अर्थात् निपात वाक्य में मौजूद तो अवश्य हैं, किंतु वे वाक्य के “अर्थ-स्वरूप” को प्रभावित करते हैं, न कि “वस्तुगत अर्थ” को।
निपात की उपयोगिता और भाषिक महत्त्व
यद्यपि निपात स्वयं पूर्ण अर्थ नहीं रखते, फिर भी इनका प्रयोग वाक्य को सही भावाभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना भाषा अपनी प्राकृतिक सहजता, स्पष्टता और भाव-गांभीर्य खो देती है।
- ये भाषा को भावपूर्ण बनाते हैं।
- वाक्य को अर्थपूर्ण दिशा देते हैं।
- वक्ता की मंशा, स्वर, भावना, ज़ोर, निषेध आदि को स्पष्ट करते हैं।
- हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति-शक्ति इन सहायक अव्ययों पर काफी हद तक निर्भर करती है।
निपात ऐसा सहायक शब्द भेद है जिसमें वे शब्द आते हैं जिनके प्रायः अपने शब्दावलोसंबंधी तथा वस्तुपरक अर्थ नहीं होते हैं।” यथा- तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश।
अन्य शब्द भेदों तथा निपात में जो भिन्नता है वह यह है कि अन्य शब्द भेदों का अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि का अपना अर्थ होता है परन्तु निपात का अपना अर्थ नहीं होता है। वाक्य को अतिरिक्त अर्थ अथवा भावार्थ प्रदान करने के लिए निपात का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द-समुदाय या पूरे वाक्य में किया जाता है।
निपात भाषा के ऐसे सहायक अव्यय हैं जो स्वयं किसी स्वतंत्र अर्थ को व्यक्त नहीं करते, परंतु वाक्य में इनके प्रयोग से कथन की भाव-धारा बदल जाती है। ये वाक्य को विशिष्ट अर्थ, भाव या जोर प्रदान करते हैं और इस प्रकार संपूर्ण अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण बनाते हैं।
निपात के प्रमुख कार्य
निपात वाक्य में अलग-अलग प्रकार की भावनाएँ और अर्थ-सूक्ष्मताएँ उत्पन्न करते हैं। इनके मुख्य कार्य निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं—
1. प्रश्न प्रकट करना
जब किसी कथन को सवाल के रूप में रखना हो, तब निपात का प्रयोग किया जाता है।
उदाहरण: क्या वह विद्यालय गया था?
2. अस्वीकृति या निषेध सूचित करना
निपात का प्रयोग यह बताने के लिए भी किया जाता है कि कोई घटना या तथ्य सत्य नहीं है।
उदाहरण: वह घर पर नहीं है।
3. विस्मय या भावविभोरता व्यक्त करना
किसी कथन में आश्चर्य, प्रशंसा या भावपूर्ण उद्गार व्यक्त करने हेतु भी निपात का प्रयोग होता है।
उदाहरण: कैसी सुहावनी रात है!
4. किसी शब्द या विचार पर बल देना
वक्तव्य में किसी विशेष तथ्य पर जोर देने के लिए भी निपात अत्यंत उपयोगी होते हैं।
उदाहरण: मुझे भी इसका पता है।
निपात के प्रकार
निपात निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं-
| क्रम संख्या | निपात के प्रकार | प्रयुक्त होने वाले निपात शब्द |
|---|---|---|
| 1. | सकारात्मक / स्वीकृतिबोध / स्वीकारात्मक निपात | हाँ, जी, जी हाँ |
| 2. | नकारात्मक निपात / नकारबोधक निपात | नहीं, जी नहीं |
| 3. | निषेधात्मक निपात | मत |
| 4. | प्रश्नबोधक निपात | क्या |
| 5. | विस्मयादिबोधक निपात | क्या, काश |
| 6. | तुलनात्मक निपात / तुलनाबोधक निपात | सा |
| 7. | अवधारणबोधक निपात | ठीक, करीब, तक़रीबन, लगभग |
| 8. | आदरबोधक निपात | जी |
| 9. | बलदायक निपात / बलप्रदायक निपात | तो, ही, भी, भर, सिर्फ, तक, केवल |
यास्क मुनि ने निपात के तीन भेद माने है-
- उपमार्थक निपात : यथा- इव, न, चित्, नुः
- कर्मोपसंग्रहार्थक निपात : यथा- न, आ, वा, ह;
- पदपूरणार्थक निपात : यथा- नूनम्, खलु, हि, अथ।
1. स्वीकारात्मक निपात
स्वीकारात्मक निपात- हाँ, जी, जी हाँ।
ये सब निपात स्वीकृति को व्यक्त करते हैं तथा सदैव स्वीकारार्थक उत्तर के आरम्भ में आते हैं।
प्रश्न- आप विद्यालय जाते हो ?
उत्तर- जी।
प्रश्न- वे सब घर जा रहे हैं ?
उत्तर- जी हाँ।
जी तथा जी हाँ निपात विशेष आदरसूचक स्वीकारार्थक उत्तर के समय प्रयुक्त होते हैं। ये स्वीकारात्मक निपात है।
2. नकारात्मक निपात
नकारात्मक निपात – नहीं, जी नहीं।
प्रश्न: तुम्हारे पास यह पुस्तक है ?
उत्तर- नहीं।
3. निषेधात्मक निपात
निषेधात्मक निपात – मत।
- आज आप मत जाइए।
- मुझे अपना मुँह मत दिखाना।
4. आदरार्थक निपात
आदरार्थक निपात – क्या, न।
- क्या- तुम्हें वहाँ क्या मिलता है ?
- न- तुम अँगरेजी पढ़ना नहीं जानते हो न ?
5. तुलनात्मक निपात
तुलनात्मक निपात – सा।
- सा- इस लड़के सा पढ़ना कठिन है।
6. विस्मयार्थक निपात
विस्मयार्थक निपात – क्या, काश।
- क्या- क्या सुन्दर लड़की है !
- काश- काश ! वह न गया होता !
7. बलार्थक या परिसीमक निपात
बलार्थक या परिसीमक निपात – तक, भर, केवल, मात्र, सिर्फ, तो, भी, ही।
तक- मैंने उसे देखा तक नहीं। हमने उसका, नाम तक नहीं सुना।
भर- मेरे पास पुस्तक भर है। उसको अपनी कॉपी भर दे दो।
केवल- वह केवल सजाकर रखने की वस्तु है।
मात्र- वह मात्र सुन्दर थी, शिक्षित तो नहीं थी।
ही- उसका मरना ही था कि घर-का-घर बर्बाद हो गया।
भी- मैं भी यहीं रहता हूँ।
8. अवधारणबोधक निपात
अवधारणबोधक निपात – ठीक, लगभग, करीब।
ठीक- ठीक समय पर पहुँचा। ठीक पाँच हजार रुपये उसने दिये।
लगभग- लगभग पाँच लाख विद्यार्थी इस वर्ष प्रवेशिका की परीक्षा दे चुके हैं।
करीब- इस समय करीब पाँच बजे हैं।
9. आदरसूचक निपात
आदरसूचक निपात – जी।
जी- यह निपात व्यक्तिवाचक या जातिवाचक नाम, उपाधि तथा पद आदि सूचित करने वाले संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होता है।
जैसे- इन्दिरा जी, गुरुजी, डॉक्टर जी, वर्माजी।
निपात अव्यय शब्द ऐसे शब्द हैं जो स्वतंत्र रूप से कोई विशेष अर्थ प्रदान नहीं करते और न ही वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। ये शब्द मुख्य रूप से वाक्य में अन्य शब्दों या पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं और वाक्य के संपूर्ण अर्थ को एक नया भाव या गहराई प्रदान करते हैं।
निपात के 50 उदाहरण
निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में विशेष बल देने, भाव प्रकट करने या अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ निपात के 50 उदाहरण दिए गए हैं –
- मैंने तो पहले ही कहा था।
- रमेश ही इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है।
- अब तो हद ही हो गई।
- तुम्हें यह काम आज ही पूरा करना होगा।
- मुझे भी इस बारे में जानकारी है।
- वह तो हमेशा से ऐसा ही करता आ रहा है।
- तुम तक नहीं जानते कि यह कितना महत्वपूर्ण है।
- उसे मात्र पढ़ाई से मतलब है।
- हमने तो पहले ही मना कर दिया था।
- यह तो बहुत अच्छा हुआ।
- तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो।
- वह भी मेरे साथ बाजार चला गया।
- यह बात सच ही निकली।
- तुम्हें केवल अपने बारे में सोचने की आदत है।
- आज ही उसने मुझसे बात की थी।
- तुम्हारे कारण ही यह सब हुआ।
- मुझे भी उसके घर जाना था।
- उसने तक इस बात को स्वीकार कर लिया।
- बच्चे तो खेलना ही पसंद करते हैं।
- अब तो बस इंतजार ही करना होगा।
- तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी।
- यह कार्य स्वयं ही हो जाएगा।
- तुम भी यह कर सकते हो।
- यह मात्र एक अफवाह थी।
- तुम तक परेशान हो गए।
- अब भी समय है, संभल जाओ।
- मुझे ही क्यों सजा दी गई?
- पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है।
- वह तो हमेशा से ऐसा करता आ रहा है।
- मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया।
- तुम ही सबसे अच्छे दोस्त हो।
- यह बात सत्य ही निकली।
- तुमने भी यह सुना होगा।
- खेल मात्र मनोरंजन के लिए होते हैं।
- उसने तो कुछ कहा ही नहीं।
- आज तक यह समस्या बनी हुई है।
- यह कार्य केवल तुम्हारे लिए है।
- तुम तो बेकार की चिंता कर रहे हो।
- वह भी परीक्षा में सफल हो गया।
- मुझे ही क्यों दोष दिया जा रहा है?
- अब तो बस धैर्य रखना होगा।
- यह तो बहुत आसान है।
- तुम ही इसके उत्तरदायी हो।
- हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
- यह केवल एक सुझाव था।
- तुम्हें अवश्य ही यह समझना चाहिए।
- तुम तक नहीं जानते कि यह कितना महत्वपूर्ण है।
- हमें भी इस यात्रा में शामिल होना चाहिए।
- तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।
- धन मात्र से जीवन सफल नहीं होता।
ये सभी वाक्य निपात शब्दों के प्रयोग के उदाहरण हैं, जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है और उसमें विशेष भाव प्रकट होता है।
निपात शब्दों का मुख्य उद्देश्य वाक्य के प्रभाव को बढ़ाना और उसमें अतिरिक्त अर्थ जोड़ना होता है। ये शब्द अक्सर वाक्य में जोर, विरोध, सहमति, असहमति, या अन्य भावनाओं को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। उदाहरणस्वरूप, “भी”, “तो”, “ही”, “केवल”, “अवश्य” आदि निपात शब्द हैं जो वाक्य में विशेष प्रभाव डालते हैं। इन शब्दों का स्वतंत्र उपयोग संभव नहीं होता, लेकिन इनके बिना वाक्य में भाव की कमी महसूस हो सकती है। इस प्रकार, निपात अव्यय वाक्य को अर्थपूर्ण और प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं।
इन्हें भी देखें-
- निपात (अवधारक) : परिभाषा, भेद, उदाहरण और व्याकरणिक भूमिका
- अव्यय | परिभाषा, प्रकार तथा 100 + उदाहरण
- हिंदी के विराम चिन्ह और उनका प्रयोग | 50 + उदाहरण
- अनेकार्थी शब्द |500 +उदाहरण
- विलोम शब्द | विपरीतार्थक शब्द | Antonyms |500+ उदाहरण
- पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द 500+ उदाहरण
- विशेषण (Adjective)- भेद तथा 50+ उदाहरण
- छंद : उत्कृष्टता का अद्भुत संगम- परिभाषा, भेद और 100+ उदाहरण
- कारक: परिभाषा, भेद तथा 100+ उदाहरण