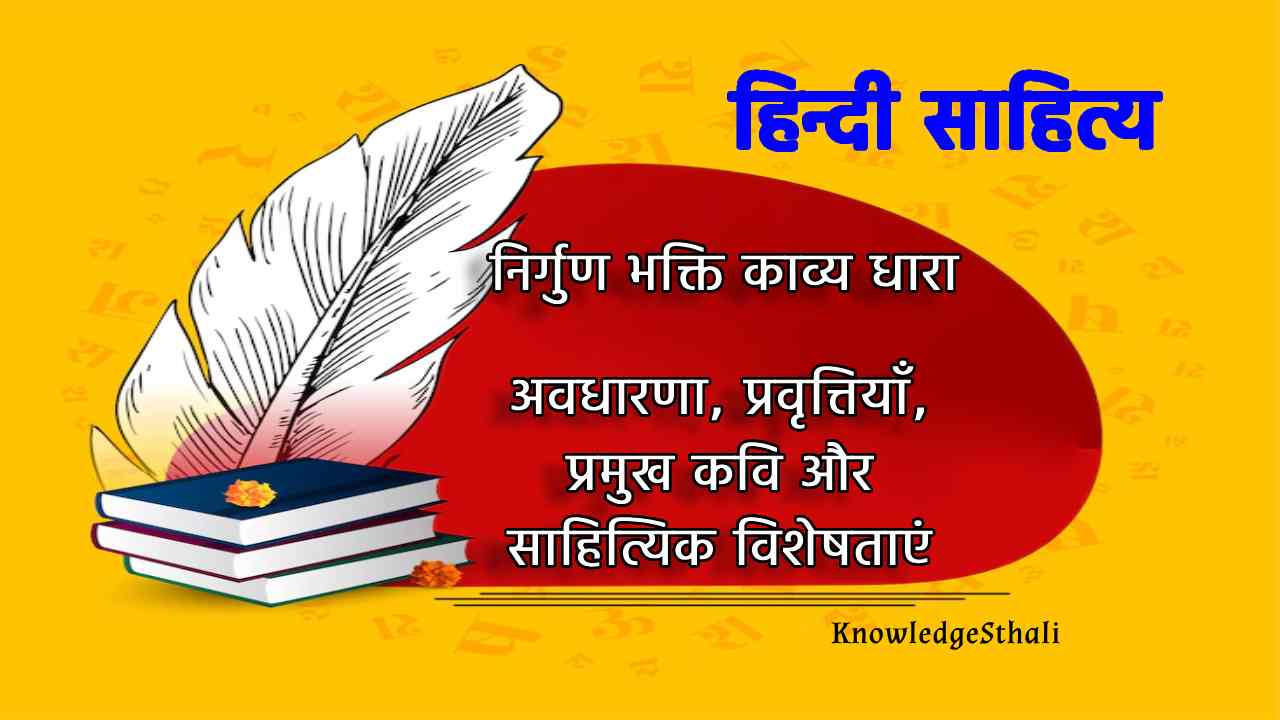हिंदी साहित्य का इतिहास अपने भीतर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलनों की अनेक परतें समेटे हुए है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य, जिसे ‘भक्ति काल’ के नाम से जाना जाता है, को हिंदी साहित्य का “स्वर्ण युग” कहा गया है। यह काल 1350 ई. से 1650 ई. के मध्य का है, जब हिंदी साहित्य में धार्मिकता और भक्ति के रंग गहरे हुए। इस काल के अंतर्गत दो प्रमुख काव्य धाराएँ विकसित हुईं – निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा।
निर्गुण भक्ति काव्य धारा का तात्पर्य उस साहित्य से है जिसमें ईश्वर को निराकार, निरगुण, अलौकिक और सर्वव्यापक रूप में स्वीकार किया गया है। इस धारा के कवियों ने मूर्तिपूजा, धार्मिक आडंबर, जाति-पांति और बाह्याचारों का विरोध किया तथा एक ऐसे ईश्वर की बात की जो हृदय में बसता है और जिसे ज्ञान, प्रेम व साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
निर्गुण भक्ति काव्य धारा का उद्भव और पृष्ठभूमि
निर्गुण भक्ति का उदय एक सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में हुआ। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। हिन्दू समाज में धार्मिक रूढ़ियों, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंड और अंधविश्वास ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। आम जनजीवन में व्याप्त असुरक्षा, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक अन्याय के बीच भक्ति एक नया आश्रय बनी।
डॉ. रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जब मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया और हिंदुओं को अपने गौरव, मंदिर, पूजा और परंपराओं से वंचित कर दिया गया, तब उनमें वीर रस या आत्मगौरव के गीतों का स्थान भगवान की भक्ति और शरणागत भाव ने ले लिया।
इस समय संत परंपरा ने जन्म लिया जिसमें व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति करने लगा। भक्त कवियों ने घोषित किया कि ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, बल्कि हृदय में स्थित चेतना है, जिसे किसी भी रूप में देखा या पाया जा सकता है। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर और मानव के बीच की दूरी को समाप्त किया और कहा कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति या धर्म का हो, ईश्वर का प्यारा हो सकता है।
निर्गुण भक्ति काव्य धारा की शाखाएँ
निर्गुण भक्ति काव्यधारा को दो प्रमुख शाखाओं में बाँटा गया है:
इन दोनों शाखाओं में एकता भी है और भिन्नता भी। ज्ञानाश्रयी शाखा ने ईश्वर को आत्मा के रूप में, निराकार, निर्गुण और ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी प्रेम और इश्क़ को साधना का माध्यम मानते थे।
1. संत काव्य धारा (ज्ञानाश्रयी शाखा)
विशेषताएँ:
- ईश्वर का निराकार रूप: संत कवियों ने ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना। उनके अनुसार ईश्वर न कोई रूप धारण करता है, न कोई अवतार लेता है, वह सर्वत्र है।
- गुरु की महिमा: संत परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु को ब्रह्म के समान माना गया। कबीर कहते हैं –
“गुरु गोविंद दोउ खड़े, काके लागूं पाय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।” - जातिवाद का विरोध: संत कवियों ने जाति-पांति के भेदभाव को नकारा और इसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बताया।
- सीधी-सादी भाषा: इन कवियों की भाषा सधुक्कड़ी या खिचड़ी कही जाती है, जिसमें सहजता और जनभाषा की मिठास है।
- धार्मिक अंधविश्वास का खंडन: संत काव्यधारा के कवियों ने मूर्तिपूजा, तीर्थ, व्रत, पूजा-पाठ, यज्ञ आदि बाह्याचारों की कटु आलोचना की।
- मानवता का संदेश: इन कवियों के अनुसार सबसे बड़ी भक्ति मानव सेवा है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, मनुष्य में भी निवास करता है।
प्रमुख संत कवि:
- कबीरदास: संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। इन्होंने हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों की रूढ़ियों की आलोचना की। उनकी रचनाएँ ‘बीजक’ में संग्रहीत हैं।
“पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय।
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।” - रामानंद: भक्ति आंदोलन के एक अग्रदूत। इन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच-नीच को समाप्त कर सभी को ईश्वर भक्ति की राह दिखाई।
- रैदास: समाज में समानता और मानवता के पक्षधर।
“मन चंगा तो कठौती में गंगा।” - सदना, दादूदयाल, नाभादास, पीपा, सेना नाई, आदि अन्य संत कवियों ने भी निर्गुण भक्ति की परंपरा को विस्तार दिया।
2. सूफी काव्य धारा (प्रेमाश्रयी शाखा)
सूफी कवि इस्लामी आध्यात्मिक परंपरा से प्रभावित थे, जिसमें ‘इश्क-हकीकी’ यानी ‘ईश्वर से प्रेम’ को सर्वोपरि माना गया। सूफियों ने प्रेम को साधना का माध्यम माना।
प्रमुख सूफी कवि:
- मलिक मुहम्मद जायसी: प्रेमाख्यान परंपरा के प्रतिनिधि कवि। उनकी प्रसिद्ध रचना “पद्मावत” एक अद्भुत allegorical (रूपक) कथा है जिसमें रानी पद्मावती और रत्नसेन के माध्यम से प्रेम और त्याग का संदेश है।
- मुल्ला दाउद: ‘चंदायन’ के रचयिता। यह रचना सूफी प्रेम मार्ग की विशेषताओं से युक्त है।
- कुतुबन: इन्होंने ‘मृगावती’ की रचना की जिसमें प्रेम और आत्मा की यथार्थ खोज को रूपायित किया गया है।
विशेषताएँ:
- प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग माना गया।
- ईश्वर को ‘माशूक’ और आत्मा को ‘आशिक’ के रूप में चित्रित किया गया।
- रूपक शैली में काव्य रचना – जैसे पद्मावती एक आदर्श सौंदर्य का प्रतीक है जो आत्मा की मुक्ति की ओर संकेत करती है।
- भाषा में फारसी और हिंदी का मेल।
निर्गुण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
1. सामाजिक कुरीतियों का विरोध
निर्गुण संत कवियों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, पाखंड, जातिवाद, बाह्याचार, और धर्म के नाम पर हो रहे शोषण का तीव्र विरोध किया। इन्होंने समाज को आडंबर से मुक्त करने और सत्य की ओर ले जाने का प्रयास किया।
2. शिक्षा का अभाव और अनुभवजन्य ज्ञान
अधिकांश संत कवि उच्च शिक्षित नहीं थे, फिर भी उनका जीवन-ज्ञान अत्यंत प्रखर था। उन्होंने अपने अनुभवों को आधार बनाकर सत्य की खोज की।
कबीर ने लिखा –
“मसि कागद छूयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ।
चारिक जुग को महातम, मुखहिं जनाई बात।”
3. मानवतावाद
निर्गुण काव्यधारा की सबसे बड़ी देन मानवतावाद है। ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष जाति, वर्ण या धर्म का होना आवश्यक नहीं। मनुष्य मात्र से प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है।
4. लोकभाषा का प्रयोग
निर्गुण संतों ने संस्कृत या फारसी जैसी शास्त्रीय भाषाओं के बजाय अवधी, ब्रज, खड़ी बोली जैसी जनभाषाओं में रचना की, जिससे उनकी बात सीधे जनमानस तक पहुँच सके।
निर्गुण काव्य का साहित्यिक रूप
- निर्गुण भक्ति साहित्य मुख्यतः मुक्तक काव्य के रूप में लिखा गया।
- इसमें दोहा, साखी, पद, सबद जैसे काव्यरूपों का प्रचलन रहा।
- कथात्मकता का अभाव है, रचनाएँ अनुभवजन्य हैं।
- रचनाओं में अक्सर गूढ़ दर्शन और जीवन के गहरे सत्य छिपे होते हैं।
- यह काव्य आत्मा और परमात्मा के संबंध की पड़ताल करता है।
निर्गुण काव्य की भाषा और शैली
निर्गुण संतों की भाषा को सधुक्कड़ी या खिचड़ी कहा जाता है। यह विभिन्न बोलियों और भाषाओं का मिश्रण थी – अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, फारसी और अरबी शब्दों का भी समावेश हुआ।
भाषा की विशेषताएँ:
- सहज, सरल, प्रभावशाली
- कहावतों और मुहावरों का प्रयोग
- लाक्षणिकता और प्रतीकों की उपस्थिति
- गूढ़ तत्वज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करना
निर्गुण भक्ति काव्य की ऐतिहासिक महत्ता
- यह काव्यधारा सामाजिक क्रांति का माध्यम बनी। इसने दलितों, वंचितों और शोषित वर्गों को आवाज़ दी।
- धार्मिक सहिष्णुता और एकता का संदेश दिया।
- मध्यकालीन भारत में धर्मनिरपेक्ष और उदार चेतना का विकास किया।
- जनभाषा में साहित्य सृजन की सशक्त परंपरा स्थापित की।
निष्कर्ष
निर्गुण भक्ति काव्यधारा भारतीय समाज और साहित्य की उस चेतना का प्रतीक है जिसमें मनुष्य के अंतःकरण को सर्वोच्च माना गया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने धर्म, जाति, भाषा और परंपरा की संकीर्णताओं को तोड़कर आध्यात्मिकता और सामाजिक समता का संदेश दिया।
आज जब समाज फिर से जातिगत विषमताओं, धार्मिक कट्टरताओं और बाह्याचारों की ओर लौट रहा है, तब निर्गुण संतों की वाणी और दर्शन हमें फिर से मानवीय मूल्यों की ओर लौटने की प्रेरणा देते हैं।
कबीर, रैदास, दादू, जायसी आदि संतों की वाणी केवल साहित्य नहीं, बल्कि मानवता का शाश्वत संदेश है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा।
निर्गुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित प्रश्नोत्तर (FAQs with Answers)
- निर्गुण भक्ति काव्य धारा क्या है?
निर्गुण भक्ति काव्य धारा वह काव्य परंपरा है जिसमें ईश्वर को निराकार, निर्गुण (गुणरहित) एवं अलौकिक रूप में माना गया है। इसमें मूर्ति पूजा, मंदिर आदि का विरोध किया गया है और आत्मा-परमात्मा के मिलन को महत्व दिया गया है। - निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धारा में क्या अंतर है?
सगुण भक्ति काव्य धारा ईश्वर को साकार रूप में पूजती है (जैसे राम, कृष्ण), जबकि निर्गुण भक्ति काव्य ईश्वर को निराकार और निरगुण मानती है। - निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख शाखाएँ कौन-कौन सी हैं?
इसके दो प्रमुख शाखाएँ हैं – ज्ञानाश्रयी शाखा (संत काव्य धारा) और प्रेमाश्रयी शाखा (सूफी काव्य धारा)। - संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में क्या अंतर है?
संत काव्य धारा भारतीय दर्शन और साधु-संन्यासी परंपरा से जुड़ी है जबकि सूफी काव्य धारा इस्लामी सूफी परंपरा पर आधारित है और प्रेम मार्ग पर बल देती है। - कबीरदास किस काव्य धारा से संबंधित हैं?
कबीरदास निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी (संत) शाखा से संबंधित हैं। - निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए।
कबीर, रैदास, दादूदयाल, नानक, सेन नाई, नामदेव, मुल्ला दाउद, कुतुबन, मलिक मुहम्मद जायसी आदि। - निर्गुण काव्य धारा की भाषा की क्या विशेषताएँ हैं?
इनकी भाषा ‘सधुक्कड़ी’ या ‘खिचड़ी’ कहलाती है, जिसमें लोकभाषा, बोलचाल, तत्सम-तद्भव शब्दों का मिश्रण होता है। - ‘सधुक्कड़ी’ या ‘खिचड़ी’ भाषा किससे संबंधित है?
यह संत कवियों की मिश्रित, सहज, जनभाषा आधारित शैली है। - निर्गुण काव्य में किस प्रकार के काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है?
अधिकतर रचनाएँ पद और दोहे के रूप में हैं। यह मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। - संत काव्य धारा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
धर्म और समाज के आडंबरों, जाति-पाँति और रूढ़ियों का विरोध कर जनमानस में आध्यात्मिक चेतना का विकास। - निर्गुण काव्य धारा में गुरु का क्या महत्व है?
गुरु को परमात्मा से भी बड़ा माना गया है। गुरु ही ज्ञान का प्रकाशक है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। - कबीर के काव्य में किस प्रकार की सामाजिक चेतना दिखाई देती है?
उन्होंने जात-पात, धार्मिक पाखंड, ऊँच-नीच और आडंबर का तीव्र विरोध किया। - निर्गुण भक्ति काव्य में वर्ण व्यवस्था का किस प्रकार विरोध किया गया है?
जाति के आधार पर भेदभाव को गलत ठहराया गया। कबीर, रैदास जैसे कवियों ने इसे सामाजिक शोषण माना। - सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम क्या हैं?
मुल्ला दाउद, कुतुबन, मंझन, मलिक मुहम्मद जायसी आदि। - मलिक मुहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं?
पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, आखिरी कलाम आदि। - ‘बीजक’ किसकी रचना है और उसका महत्व क्या है?
यह कबीर की वाणियों का संकलन है, जिसमें उनके दोहे, रमैनी और साखियाँ संग्रहीत हैं। - निर्गुण काव्य धारा के कवि किस जाति वर्ग से आते थे?
अधिकांश संत कवि निम्न जातियों से थे – जैसे कबीर (जुलाहा), रैदास (चमार), दादू (धुनिया)। - निर्गुण कवियों की शिक्षा के स्तर के बारे में क्या कहा जा सकता है?
ये अधिकतर औपचारिक शिक्षा से वंचित थे लेकिन अनुभव, श्रवण और भ्रमण से ज्ञान प्राप्त किया। - ‘मसि कागद छूयो नहीं’ दोहे का क्या भावार्थ है?
कबीर कहते हैं कि उन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ीं, न ही कलम पकड़ी, फिर भी उनका ज्ञान जीवनानुभव से उत्पन्न हुआ है। - निर्गुण कवियों की साधना और भक्ति पद्धति कैसी थी?
इनकी भक्ति सहज, सरल, आडंबरविहीन, आत्मानुभूति पर आधारित थी। - निर्गुण काव्य धारा का समाज सुधार में क्या योगदान रहा है?
इन्होंने जातिवाद, पाखंड, धार्मिक भ्रष्टाचार का विरोध कर सामाजिक समरसता और भातृत्व भावना को बढ़ावा दिया। - रामानंद किस काव्य धारा से संबंधित थे?
ये सगुण भक्त कवि माने जाते हैं लेकिन इनके शिष्य निर्गुण भक्ति के प्रमुख प्रचारक बने। - नामदेव का भक्ति साहित्य में क्या योगदान है?
नामदेव ने मराठी और हिंदी में भजन लिखे। इन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। - ‘चंदायन’ और ‘मृगावती’ किन कवियों की रचनाएँ हैं?
‘चंदायन’ – मुल्ला दाउद, ‘मृगावती’ – कुतुबन। - निर्गुण काव्य में प्रबन्ध शैली की अनुपस्थिति का क्या कारण है?
निर्गुण काव्य अधिकतर भाव और अनुभूति पर आधारित है, इसलिए प्रबंध (कथात्मक) शैली के बजाय मुक्तक शैली अपनाई गई। - संत कवियों की भाषा क्लिष्ट क्यों मानी जाती है?
यह दार्शनिकता और प्रतीकों से भरपूर होती है, साथ ही विभिन्न भाषाओं के मिश्रण के कारण भी कठिन हो जाती है। - ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखाओं में क्या अंतर है?
ज्ञानाश्रयी शाखा आत्मज्ञान, वैराग्य, ध्यान पर बल देती है; प्रेमाश्रयी शाखा प्रेम, भाव, सौंदर्य और आत्म-विलयन पर बल देती है। - निर्गुण भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक रहा?
उत्तर भारत, विशेषकर काशी, बनारस, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में। - निर्गुण भक्ति काव्य में आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या कैसे की गई है?
आत्मा-परमात्मा की एकता, माया का मोह, ब्रह्मज्ञान, गुरु की कृपा आदि तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। - डॉ. श्यामसुंदर दास ने संत काव्य के विषय में क्या कहा है?
उन्होंने कहा कि संतों ने जनता को विपत्ति के समय जीने की प्रेरणा दी, आडंबरों का खंडन किया और सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर किया
Hindi – KnowledgeSthali
इन्हें भी देखें –
- सूफी काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- संत काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- कृष्ण भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- राम भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- यह मेरी मातृभूमि है | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- आकाशदीप कहानी- जयशंकर प्रसाद
- क़लम का सिपाही | प्रेमचन्द जी की जीवनी : अमृत राय
- कबीर दास जी के दोहे एवं उनका अर्थ | साखी, सबद, रमैनी
- कबीर दास जी | जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएँ एवं भाषा
- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ
- हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास
- हिंदी के विराम चिन्ह और उनका प्रयोग | 50 + उदाहरण
- भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य | Folk dances and Classical dances of India