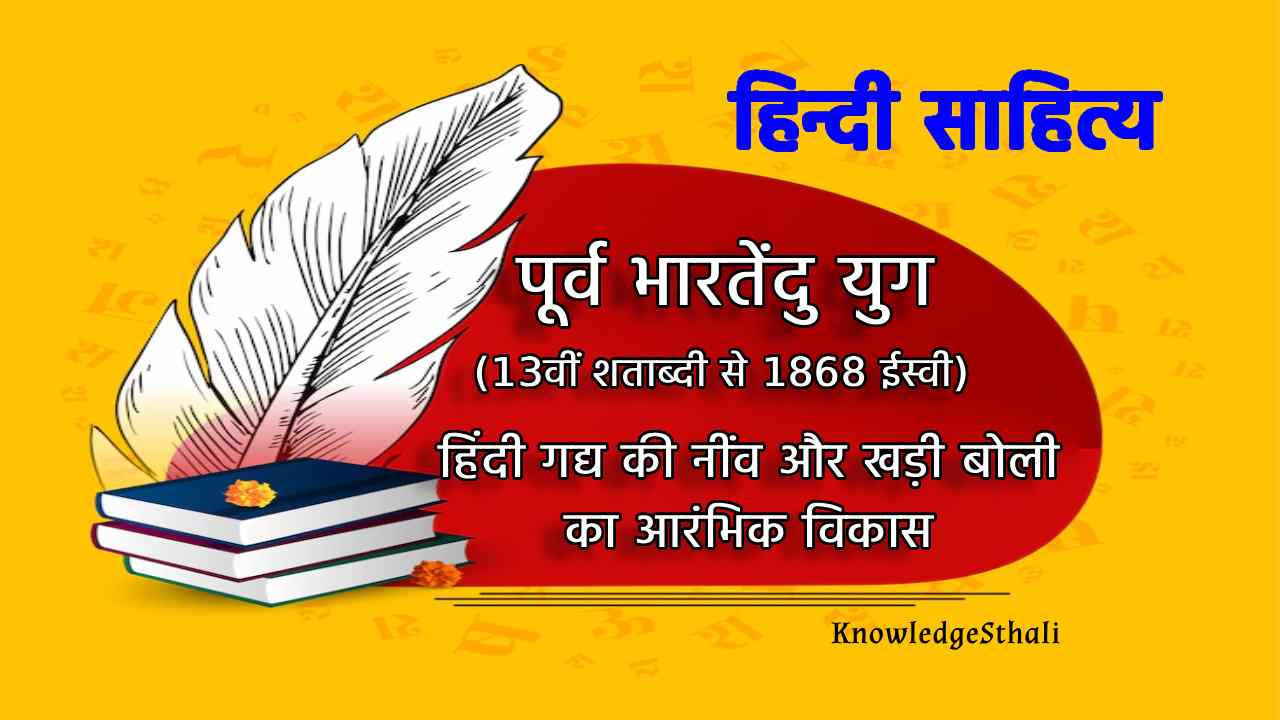“पूर्व भारतेंदु युग” हिन्दी साहित्य के उस परिवर्तनशील समय को उजागर करता है, जब गद्य ने कविताओं की छाया से निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी शुरू की और खड़ी बोली ने लेखनी का स्वर पकड़ा। यह युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक फैला था और इसमें हिन्दी गद्य अपने शैशव अवस्था में था। इस लेख में लल्लू लाल, इंशा अल्ला खाँ, सदल मिश्र और राजा शिवप्रसाद ‘सितारे हिन्द’ जैसे महत्वपूर्ण लेखकों की भूमिका को विस्तार से समझाया गया है, जिन्होंने ब्रज और फारसी की प्रधानता वाले साहित्यिक परिदृश्य में खड़ी बोली को साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।
लेख में प्रेमसागर और रानी केतकी की कहानी जैसी ऐतिहासिक गद्य रचनाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिनमें खड़ी बोली का पहला सुविचारित और स्वाभाविक प्रयोग दिखाई देता है। इसमें इंशा अल्ला खाँ द्वारा प्रयुक्त “हिंदी छुट” की अवधारणा विशेष महत्व रखती है, जो उस समय की भाषिक शुद्धता की चेतना को दर्शाती है। इसके साथ ही ब्रिटिश शासन, आधुनिक शिक्षा और प्रेस की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है, जिसने हिन्दी गद्य को सामाजिक और संवादात्मक स्वरूप प्रदान किया।
यह लेख न केवल भाषा-शिल्प का मूल्यांकन करता है, बल्कि साहित्यिक विकास की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषिक प्रक्रिया को भी समग्र रूप में प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों, शोधार्थियों और भाषा प्रेमियों के लिए यह लेख अत्यंत उपयोगी और संदर्भात्मक सामग्री प्रदान करता है।
पूर्व भारतेंदु युग (13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी)
‘पूर्व भारतेंदु युग’ हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग से पूर्व का वह काल है जिसमें गद्य का प्रारंभिक विकास हुआ। यह काल 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक माना जाता है। इस अवधि में खड़ी बोली हिन्दी धीरे‑धीरे स्थापित हो रही थी, उस परंपरा का विकास हुआ जिसने बाद में भारतेंदु युग में गद्य को उत्कर्ष पर पहुंचाया। यह वह युग है जिसमें गद्य‑लेखन की नींव पड़ी, लेखन का स्वरूप बदला और आधुनिक हिन्दी साहित्य की धारा ने आकार लिया।
पूर्व भारतेंदु युग समय-सीमा की व्याख्या
- शुरुआती चरण (13वीं शताब्दी – 16वीं शताब्दी): उस समय हिन्दी का स्वरूप अभी पूर्ण विकसित नहीं था, बिरबली, प्रेमघन आदि के कभी‑कभी रचनाएँ हुईं लेकिन गद्य सीमित रूप में।
- मध्यकाल (17वीं – 18वीं शताब्दी): खड़ी बोली की गद्यधारा की पहली महत्वपूर्ण रचना “चन्द छन्द बरनन की महिमा” अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखी गई, जिसमें संस्कृत तत्सम और ब्रजभाषा दोनों का इस्तेमाल हुआ।
- नवीन प्रारंभ (19वीं शताब्दी): इस समय में लेखन और प्रकाशन की प्रक्रियाएँ तेज हुईं। नई पत्रिकाएँ, अख़बार, व्यावहारिक गद्य—ये सब बढ़ने लगे। इसी युग में 1868 के बाद भारतेन्दु हरिश्चंद्र का उदय हुआ।
इस प्रकार, 13वीं शताब्दी से 1868 तक की अवधि, आज ‘पूर्व भारतेंदु युग’ के रूप में परिभाषित की जाती है।
हिन्दी गद्य की प्रारंभिक अवस्था
- इस युग में गद्य का स्वरूप मिश्रित भाषा (संस्कृत, ब्रज और स्थानीय बोलियों) में था।
- चन्द छन्द बरनन की महिमा जैसी गद्यरचनाएँ मध्यकालीन स्वरूप की रचना थीं, जिसमें खड़ी बोली का प्रारंभिक प्रयोग होता दिखता है।
हिन्दी गद्य का प्रारंभिक विकास
• “चन्द छन्द बरनन की महिमा”
यह गद्य की प्रथम उल्लेखनीय रचना मानी जाती है। इसमें संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ ब्रज बोलियाँ भी शामिल थीं, जो उस समय की मिश्रित भाषा स्थिति को दर्शाती है।
• खड़ी बोली का विकास
खड़ी बोली हिन्दी धीरे‑धीरे लोकजीवन में लोकप्रिय हुई। राजा शिवप्रसाद ‘सितारे हिन्द’ जैसे साहित्यकारों ने इसे और पुष्ट किया। उन्होंने किताबों व अख़बारों में खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ किया, जिससे यह भाषा स्थापित होती चली गई।
• प्रारंभिक लेखक और गद्य प्रबंधन
इस युग में चार प्रमुख गद्यप्रवर्तक माने जाते हैं:
- इंशा अल्ला खाँ — रानी केतकी की कहानी
- सदासुखलाल — सुखसागर
- लल्लू लाल — प्रेमसागर
- सदल मिश्र — (रचनाएँ, संभवतः सदसँग जैसी)।
इन लेखकों से पहले गद्य की व्यापकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस विधा को प्रारंभ किया।
प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएँ
1. इंशा अल्ला खाँ
- रचना: रानी केतकी की कहानी — यह गद्य‑कथा प्रारंभिक हिन्दी गद्य की एक पहली पहचान थी। इसमें एक कथा के रूप में जीवन‑घटनाओं का वर्णन था, जो गद्य विधा की ओर पहला कदम था।
2. लल्लू लाल
- रचना: प्रेमसागर — हिन्दी गद्य में उत्तम प्रयास रहा। लल्लू लाल को ‘गद्य का प्रवर्तक’ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली में गद्य प्रयोग को प्रभावशाली बनाया।
3. सदल मिश्र
- सदल मिश्र प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य के लेखकों में शामिल थे। उनकी रचनाएँ जैसे सुखसागर आदि ने कथा विधा में स्पष्टता और नैतिकता को जोड़ा।
- इनकी रचनाएँ हिन्दी गद्य में स्पष्टता और सहजता लाईं। इस युग के लेखन में साधारण जनजीवन और नैतिक कथानक प्रमुख थे।
4. राजा शिवप्रसाद ‘सितारे हिन्द’
- राजा शिवप्रसाद ‘सितारे हिन्द’ काशी (वाराणसी) से सम्बद्ध थे। उन्होंने गद्य लेखन में खड़ी बोली स्थापित करने में भूमिका निभाई। उनके लेखन और संपादन के माध्यम से समाचार‑पत्रों और अन्य पत्रिकाओं में खड़ी बोली का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ।
- इन्होने गद्य लेखन को सामाजिक विमर्श का माध्यम बनाया।
लल्लू लाल और प्रेमसागर
- लल्लू लाल ने 1804–10 के बीच अपनी रचना प्रेमसागर लिखी, जो 1810 में प्रकाशित हुई। यह ब्रज भाषा की कथा को खड़ी बोली में रूपांतरित पहली चर्चित कृति है (Del‑Agra खड़ी बोली)।
- Jules Bloch जैसे भाषाविद ने इसे आधुनिक संस्कृत-तटस्थ हिंदी की दिशा में पहला कदम माना।
- यह कृति हिन्दी गद्य को एक मानकीकृत रूप देने में अतिशय महत्वपूर्ण दिखती है।
इंशा अल्ला खाँ और रानी केतकी की कहानी
रचनाकाल एवं महत्व
- रानी केतकी की कहानी संभवतः 1803 ईस्वी के आसपास रची गई खड़ी बोली की पहली कहानी के रूप में जानी जाती है।
- लेखक सैय्यद इंशा अल्ला खाँ ‘इंशा’ थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से “हिंदवी छुट” की इच्छा व्यक्त की—अर्थात, कोई विदेशी बोली या पुट न हो, केवल सहज खड़ी बोली।
भाषा शैली एवं उद्धरण
कहानी की शुरुआत खुद लेखक की यह अभिव्यक्ति स्पष्ट करती है:
“यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट।”
एक जगह वे कहते हैं:
“हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो … जैसे भले लोग अच्छे आपस में बोलते चालते हैं।”
ये वाक्य खड़ी बोली की स्वाभाविकता पर जोर देते हैं—जहाँ न ब्रज का गहिरापन हो, न उर्दू-फ़ारसी का पुट, बल्कि आम जनजीवन जैसा सहज व्यवहार।
कथा की सामग्री
- कहानी में रानी केतकी और कुँवर उदैभान की प्रेम कथा और भावनात्मक संघर्ष है।
- ऊपर उद्धृत अंशों में कथा में प्रकृति‑वर्णन, संस्कृति‑परंपरा तथा नारी‑भावना का चित्रण मिलता है:
“रानी केतकी अपनी माँ की इस बात पर अपना मुँह थुथा कर उठ गई और दिन भर खाना न खाया।”
रानी की आत्मीय प्रतिक्रिया, मदनबान की बीच‑बचाव की सुविधा, और पारिवारिक संवाद कथा को प्रभावी बनाते हैं।
शैली विश्लेषण
संवाद शैली अत्यंत लोक‑सहज और प्रवाहपूर्ण है, जिसमें दोहों, भाववाचक पंक्तियों, और जीवनाभास वाले वर्णन शामिल हैं।
उदाहरण के लिए दोहरे:
दोहरा
“छा गई ठंडी साँस झाड़ों में
पड़ गई कूक सी पहाड़ों में।”
दोहरा
“हम नहीं हँसने से रुकते, जिसका जो चाहे हँसे।
है वही अपनी कहावत या फँसे जी आ फँसे॥
अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झाँटा लग गया।
पाँव का क्या ढूँढ़ती हो जी में काँटा लग गया॥”
ये पंक्तियाँ केवल साहित्यिक सजावट नहीं, बल्कि भाव की माधुर्यता और प्राकृतिक लोकख्याति को दर्शाती हैं।
समाजिक‑सांस्कृतिक संदर्भ
• ब्रिटिश संपर्क और समाज परिवर्तन
18वीं‑19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के प्रभाव से शिक्षा, प्रेस, प्रशासन और सामाजिक चेतना में बदलाब आया। विश्वविद्यालय, प्रेस, अफ़सरशाही, आधुनिक शिक्षा ने हिन्दी गद्य को नया आधार दिया। आधुनिक विद्यालय, पत्र-पत्रिका, विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से खड़ी बोली जनता तक पहुँची। जिससे हिन्दी गद्य को एक व्यवस्थित रूप मिला।
• पत्रिकाओं और अख़बारों का उदय
इस युग में समाचार पत्र और पत्रिकाएँ चलने लगीं। कुछ स्थानीय स्तर पर शुरुआत हुईं, जहाँ लेखन और सामाजिक विमर्श गद्य में हो रहा था। राजा शिवप्रसाद जैसे लोगों ने इन्हें संपादित एवं संचालित किया, जिससे जनता तक हिन्दी गद्य पहुँचा। राजा शिवप्रसाद जैसे संपादकों की अग्रणी भूमिका से हिन्दी गद्य आम आदमी की भाषा में विकसित हुआ। इससे हिन्दी साहित्य में गद्य निबंध, समाचार, अनुवाद आदि की विधाएँ विकसित हुईं।
• गद्य में प्राकृतिकता और व्यावहारिकता
प्रेमघन जैसे पूर्व कवियों ने गद्य में भावुक प्रशस्ति लिखी, पर यह मुख्यतः कविता‑शैली से अधिक गद्य न था। परन्तु लल्लू लाल, सदल मिश्र आदि ने कथा‑कहानी, चरित्र‑वर्णन, सामाजिक वर्णन आदि की दिशा में काम किया।
साहित्यिक विशेषताएँ
• भाषा और शैली
भाषा एक संक्रमणकालीन अवस्था में थी—संस्कृत (तत्सम), ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण। इसमें धीरे‑धीरे खड़ी बोली का प्रभाव बढ़ा, और गद्य‑शैली सरल‑सहज हुई।
• विषय‑वस्तु
प्रारंभ में कथा, नैतिक दंतकथा, सरलीकृत जीवन‑दृष्टांत, आदर्श पात्रों पर लेखन हुआ। रानी केतकी आदि में नैतिक घटना‑कथाएँ प्रमुख रहीं।
• उद्देश्य
शिक्षा‑उदासीव, नैतिकता और समाज सेवा—
इसमें स्पष्ट सामाजिक संदेश था—प्रेरणा देना, जीवन‑मूल्यों पर प्रकाश डालना और भाषा को सामान्य जनता तक पहुंचाना।
विश्लेषण
- लल्लू लाल की प्रेमसागर ने ब्रज भाषा की कथा को खड़ी बोली में बदलकर आधुनिक गद्य का प्रथम रूप प्रदान किया।
- इंशा अल्ला खाँ की रानी केतकी की कहानी ने खड़ी बोली में पहली कथा के रूप में यह संदेश दिया कि गद्य केवल संस्कृत-तटस्थ न होकर, जन‑भाषा में भी खूबसूरती से सुसज्जित हो सकता है।
- इन दोनों रचनाओं ने खड़ी बोली की मान्यता जीवित की और हिंदी गद्य के विकास की नींव रखी।
महत्व और भूमिका
पूर्व भारतेंदु युग का प्रमुख योगदान हिन्दी गद्य को जन‑भाषा (खड़ी बोली) में प्रस्थापित करना था। लल्लू लाल और इंशा अल्ला खाँ जैसे लेखकों ने प्रारंभिक गद्यगत संरचना को आकार दिया। इस युग की रचनाएँ बाद के भारतेंदु युग और आधुनिक हिन्दी साहित्य की नींव बनीं।
• आधुनिक गद्य की नींव
यदि उत्तर गद्य के विकास की परंपरा को ट्रेस करें, तो पूर्व भारतेंदु युग वह पहला चरण है जिसने गद्य को जीवंत किया। यह आधार बना जिससे भारतेंदु युग (1868‑1900) में गद्य, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि की विविधता आई।
• साहित्य‑संस्कृति में पुल की तरह
यह युग प्राचीन काव्य‑परंपरा और आधुनिक गद्य‑आधारित साहित्य के बीच एक पुल का कार्य करता है। कविता केन्द्रित साहित्य से गद्य‑केन्द्रित साहित्य तक का परिवर्तन इसी युग में संचालित हुआ।
• भाषा‑व्यवस्था
यह युग खड़ी बोली को मानक भाषा रूप में स्थापित करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण सन्दर्भ है। बाद में राजा शिवप्रसाद जैसे लोग आगे आए, लेकिन इन साहित्यकारों के प्रयासों ने खड़ी बोली को मान्यता दी।
निष्कर्ष एवं सारांश
पूर्व भारतेंदु युग (13वीं शताब्दी – 1868) हिन्दी साहित्य में एक परिवर्तनकारी दौर है जिसमें गद्य की नींव रखी गई। इस युग का साहित्य सम्राट अकबर के दरबारी कवि गंग के ‘चन्द छन्द बरनन की महिमा’ से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के अंत तक फैला।
मुख्य लेखक—इंशा अल्ला खाँ, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिवप्रसाद—जिनकी रचनाएँ नैतिक‑कथा, प्रेम‑कथा, जीवन‑वृत्तांत, सामाजिक विमर्श पर आधारित थीं, उनके माध्यम से हिन्दी गद्य का प्रारंभ हुआ। इन लेखकों ने खड़ी बोली को अपनाया और सामान्य जनजीवन को विषय बनाया।
इस युग ने साहित्य में शिल्प और भाषा दोनों में नया आयाम जोड़ा। इससे मिली पंरपरा ने 1868 में भारतेन्दु युग के गद्य‑पुनर्जागरण को संभव बनाया। इसलिए इसे आधुनिक हिन्दी गद्य की नींव माना जाता है।
इन्हें भी देखें –
- भारतेन्दु युग (1868–1900 ई.): हिंदी नवजागरण का स्वर्णिम प्रभात
- द्विवेदी युग (1900–1920 ई.): हिंदी साहित्य का जागरण एवं सुधारकाल
- प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता: छायावादोत्तर युग के अंग या स्वतंत्र साहित्यिक प्रवृत्तियाँ?
- हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और उसका ऐतिहासिक विकास | 1850 ई. से वर्तमान तक
- रीतिकाल (1650 – 1850 ई.): हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकालीन युग
- हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि और काव्य (रचनाएँ)
- भारतेंदु युग (नवजागरण काल) की समय-सीमा, स्वरूप और युग-निर्धारण की समीक्षा
- हिन्दी साहित्य के सर्वप्रथम कवि: एक विमर्श
- हिंदी के प्रमुख एकांकीकार एवं एकांकी | लेखक और रचनाएँ
- हिन्दी एकांकी: इतिहास, कालक्रम, विकास, स्वरुप और प्रमुख एकांकीकार
- शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला