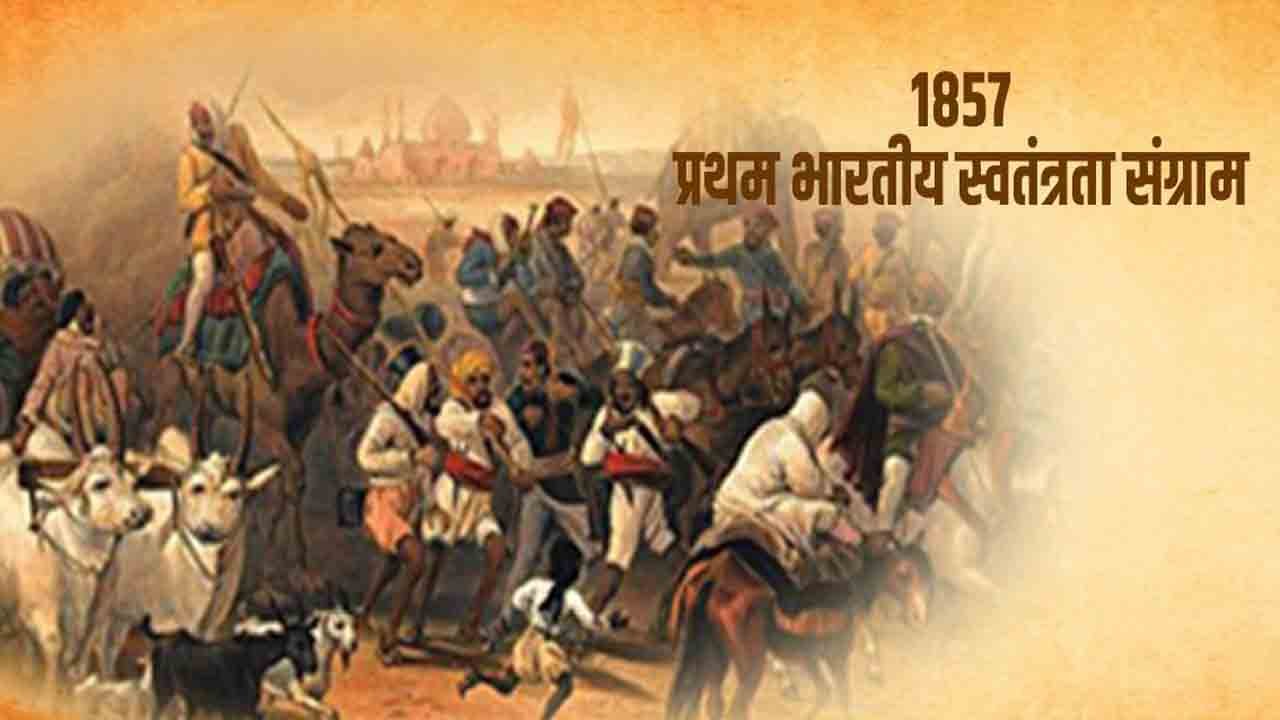भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दुनिया द्वारा आदर्श स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। भारतीयों द्वारा औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1857 ई. में वृहद् स्तर पर क्रांति की गयी थी, इस क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों के अत्याचारी शासन के विरुद्ध वर्ष 1857 ई. की क्रान्ति को भारत की स्वतंत्रता में मील का पत्थर माना जाता है जिसके कारण अंतत देश के अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों को दिशा प्राप्त हुयी। 1857 की क्रान्ति का वृहद् प्रभाव यह रहा की इसके माध्यम से अंग्रेजी शासन की राजसत्ता हिल गयी, एवं देश के नागरिको में स्वतंत्रता की चेतना की लहर दौड़ गई।
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1600 ई. में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त किया गया। वर्ष 1608 ई. में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वप्रथम गुजरात के सूरत में आगमन हुआ। इसके पश्चात अपनी कुटिल नीतियों के कारण इसके द्वारा लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया। कभी छल-कपट तो कभी सहायक-संधि द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के विभिन भागों पर अपना अधिकार किया जाने लगा।
साथ ही अपनी कुटिलता का विस्तार करते हुए ब्रिटिशर्स द्वारा समय-समय पर व्यापारिक सिद्धांत एवं अन्य कारणों से भी देश पर कब्ज़ा किया जाता रहा। और अंततः इन सभी नीतियों का परिणाम यह हुआ की व्यापार करने के उद्देश्य से देश में आये फिरंगी इस देश के मालिक बन बैठे। अपने शासन के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा विभिन नीतियों का अनुसरण किया जाता रहा जिसके परिणामस्वरूप भारतीय नागरिको में असंतोष पैदा होने लगा था। इसी असंतोष का परिणाम रहा की वर्ष 1857 ई. में भारतीयों का अंग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह फूट पड़ा, जिसे की 1857 की क्रान्ति के नाम से जाना जाता है।
| आरम्भ तिथि | 10 मई 1857 |
| प्रमुख स्थान | मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध |
| प्रमुख व्यक्ति | मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, बहादुर शाह जफ़र, महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड विलियम बैंटिक |
| परिणाम | विद्रोह का दमन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, नियंत्रण ब्रिटिश ताज (महारानी विक्टोरिया) के हाथ में |
1857 की क्रान्ति
ब्रिटिशर्स द्वारा भारतियों पर किये जा रहे अत्याचार, भारतीयों के प्रति भेद-भाव तथा दुराचार का परिणाम यह रहा कि भारतीयों में असंतोष फैलने लगा। और इस असंतोष का परिणाम यह रहा कि भारतीय लोगों का गुस्सा अंग्रेगी शासन के खिलाफ फुट पड़ा। भारतीय लोगों का यह गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक क्रांति का रूप ले लिया। इसी क्रान्ति को 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया। हालाँकि इस क्रांति को अंग्रेजी शासन द्वारा दबा दिया गया, परन्तु इस क्रांति ने भारतियों के मन में आज़ादी के प्रति जोश और अंग्रेजी शासन के मन में दहशत भर दिया। इन क्रांति में जिन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका विवरण इस प्रकार है –
मंगल पाण्डे
29 मार्च, 1857 ई. को मंगल पाण्डे नामक एक सैनिक ने ‘बैरकपुर छावनी’ में अपने अफ़सरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियम ’34 एन.आई.’ को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3 एल.सी. परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नये कारतूस लेने से इंकार कर दिया।

आज्ञा की अवहेलना करने के कारण इन 85 घुडसवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। ‘खुला विद्रोह’ 10 मई, दिन रविवार को सांयकाल 5 व 6 बजे के मध्य प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी ’20 एन.आई.’ में विद्रोह की शुरुआत हुई, तत्पश्चात् ‘3 एल.सी.’ में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियाँ चलाई। मंगल पाण्डे ने ‘हियरसे’ को गोली मारी थी, जबकि ‘अफ़सर बाग’ की हत्या कर दी गई थी।
विद्रोह का प्रसार
11 मई को मेरठ के क्रान्तिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुँचकर, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने मुग़ल सम्राट बहादुरशाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। यह विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस आदि में बड़ी तेजी से फैलने लगा तथा शीघ्र ही बिहार तथा झांसी में भी फैल गया। अंग्रेज़ों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 21 सितम्बर, 1857 ई. को दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकार कर लिया, परन्तु संघर्ष में ‘जॉन निकोलसन’ मारा गया और लेफ्टिनेंट ‘हडसन’ ने धोखे से बहादुरशाह द्वितीय के दो पुत्रों ‘मिर्ज़ा मुग़ल’ और ‘मिर्ज़ा ख्वाज़ा सुल्तान’ एवं एक पोते ‘मिर्ज़ा अबूबक्र’ को गोली मरवा दी।
लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून, 1857 ई. को हुई। यहाँ के क्रान्तिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजीडेन्सी के घेराव के उपरान्त ब्रिटिश रेजिडेंट ‘हेनरी लॉरेन्स’ की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउट्रम ने लखनऊ को दबाने का भरसक प्रयत्न किया, परन्तु वे असफल रहे। अन्ततः कॉलिन कैम्पवेल’ ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च, 1858 ई. में शहर पर अधिकार कर लिया। वैसे यहाँ क्रान्ति का प्रभाव सितम्बर तक रहा।
रानी लक्ष्मीबाई
5 जून, 1857 ई. को क्रान्तिकारियों ने कानपुर को अंग्रेज़ों से छीन कर अपने अधिकार में ले लिया। नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया, जिनका वास्तविक नाम ‘धोंदू पन्त’ था। तात्या टोपे ने इनका सहयोग किया। यहाँ पर विद्रोह का प्रभाव 6 सितम्बर तक ही रहा। कॉलिन कैम्पवेल के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना ने 6 सितम्बर, 1857 ई. को कानपुर को पुनः अपने क़ब्ज़े में कर लिया। परन्तु तात्या टोपे कानपुर से फरार होकर झांसी पहुँच गये।
रानी लक्ष्मीबाई, जो गंगाधर राव की विधवा थीं, वे भी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने के कारण अंग्रेज़ों से नाराज़ थीं। तात्या टोपे के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवाये। इन दोनों ने ग्वालियर पर भी क्रान्ति का झण्डा फहराया और वहाँ के तत्कालीन शासक सिंधिया द्वारा विद्रोह में भाग लेने पर रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब को पेशवा घोषित किया, परन्तु शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने जून, 1858 ई. में ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया।

झांसी पर अंग्रेज़ी सेना ने ह्यूरोज के नेतृत्व में 3 अप्रैल, 1858 ई. को अधिकार कर लिया। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। बरेली में ‘ख़ान बहादुर ख़ाँ’ ने स्वयं को नवाब घोषित किया। बिहार में जगदीशपुर के ज़मींदार ‘कुंअर सिंह’ ने बिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ विद्रोह का झण्डा फहराया। बनारस में हुए विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया। जगदीशपुर के विद्रोह को अंग्रेज़ अधिकारी विलियम टेलर एवं मेजर विंसेट आयर ने दबाया।
बहादुरशाह ज़फ़र की गिरफ्तारी

जुलाई, 1858 ई. तक क्रान्ति के सभी स्थानों पर विद्रोह को दबा दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे ने विद्रोह में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इलाहाबाद की कमान ‘मौलवी लियाकत अली’ ने सम्भाली थी। कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया। 20 सितम्बर, 1857 ई. को हुमायुँ के मक़बरे में शरण लिए हुए बहादुरशाह द्वितीय को पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चला तथा उन्हें बर्मा (रंगून) निर्वासित कर दिया गया।
1857 की क्रान्ति के कारण
1857 की क्रान्ति अंग्रेजो द्वारा लम्बे समय से भारतीय जनता पर किए जाने वाले विविध प्रकार के अत्याचारों का परिणाम थी। इसके परिणामस्वरूप उपजे असंतोष की परिणिति ही 1857 के विद्रोह के रूप में हुयी थी। यहाँ आपको इसके सभी प्रमुख कारणों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है :-
राजनैतिक कारण (Political Cause)
अपनी विस्तारवाद की नीति के कारण अंग्रेजो के द्वारा लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था जिसके लिए कभी व्यपगत सिद्धांत तो कभी शासको के कुप्रबंधन का हवाला देकर विभिन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। इससे अन्य रजवाड़े एवं रियासतें भी अपनी सत्ता को लेकर चिंतित हो गयी। इसमें मुख्य घटनाएँ इस प्रकार थी :-
- अंग्रेजो द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को मान्यता ना देना
- व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा, झाँसी एवं नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय
- नाना साहब की पेंशन को बंद करना
- अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप में पदच्युत करना
आर्थिक कारण (Economic Cause)
1857 की क्रान्ति के प्रमुख कारणों में अंग्रेजो द्वारा देश की जनता का आर्थिक रूप से शोषण भी क्रांति के लिए जिम्मेदार था। अंग्रेजों द्वारा मनमाने कर, लगान की अत्यधिक राशि एवं कर उगाही के लिए अमानवीय तरीकों से देश की जनता में आक्रोश था। क्रांति के आर्थिक कारण के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है :-
- अंग्रेजो द्वारा मनमाने कर से जनता को मुश्किलें
- ब्रिटिश नीतियों के फलस्वरूप पारम्परिक जमींदारों एवं महाजनों की जमीन का सरकार के अधीन होना
- ब्रिटिशर्स द्वारा भारत से कच्चा माल आयात एवं निर्मित उत्पाद का निर्यात होने से स्थानीय व्यापारियों को हानि
- विभिन नीतियों के माध्यम से नागरिको का अत्यंत आर्थिक शोषण
सामाजिक और धार्मिक कारण (Religious Cause)
हमारे देश में सदैव से ही धर्म को प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है। यही कारण है की जब अंग्रेजो द्वारा ईसाई मिशनरी के माध्यम से धर्मान्तरण एवं लम्बे समय से चली आ रही सामाजिक प्रथाओं को समाप्त किया गया तो भारत के नागरिको को यह अंग्रेजो की साजिश प्रतीत हुयी। सामाजिक और धार्मिक कारण के तहत मुख्य कारण निम्न प्रकार से थे :-
- पश्चिमी सभ्यता के प्रसार से देश के नागरिकों को खतरा महसूस होना
- ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतऱण
- विभिन सामाजिक प्रथाओं का उन्मूलन जो को अंग्रेजों को क्रूर लगती थी (सती एवं भ्रूण हत्या आदि)
- ईसाइयों की अन्य धर्मो की तुलना में विशेषाधिकार
- शिक्षा, रेलवे एवं टेलीग्राफ विस्तार भी नागरिको द्वारा संदेह के रूप में देखा गया
इस प्रकार से इन कारणों के फलस्वरूप देश में 1857 की क्रान्ति की शुरुआत हुयी।
1857 की क्रान्ति, तात्कालिक कारण
1857 की क्रान्ति की आग देश में लम्बे समय से सुलग रही थी। यहाँ आपको 1857 की क्रान्ति के प्रमुख कारणों के बारे में जानकारी प्रदान की गयी है। वास्तव में देखा जाए तो देश में विभिन कारणों से क्रांति की स्थितियाँ पैदा हो चुकी थी जिसे की बस एक चिंगारी की जरूरत थी। 1857 की क्रान्ति की पटकथा पहले से ही तैयार की जा चुकी थी जिसे शुरू करने के लिए बस एक छोटी सी शुरुआत की जरूरत थी। वर्ष 1857 में ब्रिटिसर्श द्वारा भारतीय सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर नई ‘एनफिल्ड’ राइफल प्रदान की गयी। इस राइफल में कारतूस भरने के लिए इसे मुँह से खोलना पड़ता था।
जल्द ही सिपाहियों के मध्य यह खबर फ़ैल गयी की इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुयी है। ऐसे में इन कारतूसों के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा हिन्दुओं और मुस्लिमो का धर्म भ्रष्ट करने की अफवाहें भी जोर पकड़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप मंगल पांडेय नामक भारतीय सिपाही द्वारा विद्रोह कर दिया गया जिन्हें अंग्रेजो द्वारा 8 अप्रैल 1857 को फांसी चढ़ा दिया गया। इन सभी तात्कालिक कारणों से 1857 की क्रान्ति की शुरुआत हुयी।
1857 की क्रान्ति की प्रमुख घटनाएँ
1857 की क्रान्ति के दौरान पूरे देश में स्वतंत्रता की इच्छा अपने जोरों पर थी। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर-प्रदेश के मेरठ जिले से हुयी। यहाँ विद्रोही सैनिको ने सभी अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला एवं दिल्ली की ओर बढ़ चले। जनता ने इस विद्रोह में सैनिको का भरपूर साथ दिया और अन्य महत्वपूर्ण नेताओ ने भी इस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया।
11 मई 1857 को प्रातः 11 बजे विद्रोही लालकिले में पहुंचे और मुग़ल बादशाह बहादुरशाह जफ़र को क्रांति का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। अनिच्छुक होने के बावजूद क्रांतिकारियों के आग्रह पर बहादुरशाह जफ़र ने क्रांति का नेता बनना स्वीकार कर दिया। इसके पश्चात देश के विभिन भागो में क्रांति शुरू हो गयी। हालांकि इस क्रांति का मुख्य केंद्र उत्तर भारत ही था। इस दौरान की प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार है :-
- दिल्ली- दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व मुग़ल बादशाह बहादुरशाह जफ़र ने संभाला जबकि यहाँ सैन्य नेतृत्व बख्त खाँ के हाथों में था। दिल्ली इस दौरान क्रान्ति का सञ्चालन केंद्र था।
- अवध (लखनऊ)- अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजो ने कुशासन के आरोप में गद्दी से हटा दिया था। इसके कारण अवध की जनता में व्यापक गुस्सा भरा हुआ था। 1857 की क्रान्ति के दौरान लखनऊ में क्रांति की बागडोर बेगम हजरत महल ने संभाली।
- कानपुर- पेशवा बाजीराव द्वितीया के दत्तक पुत्र पुत्र नाना साहब को अंग्रेज गवर्नर लार्ड डलहौज़ी द्वारा पेंशन देने से इंकार कर दिया गया था। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब एवं सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे द्वारा संभाला गया।
- झाँसी- झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजो द्वारा मान्यता देने के इंकार कर दिया गया। 1857 की क्रान्ति में बुंदेलखंड का नेतृत्व करते हुए झाँसी की रानी द्वारा असाधारण वीरता का परिचय दिया गया।
- बिहार- बिहार में क्रांति का नेतृत्व जमींदार कुंवरसिंह के द्वारा किया गया जो इस क्रांति के दौरान वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए।
इस क्रांति के दौरान विभिन भागो में क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को मारा गया एवं बंदी बनाया गया साथ ही ब्रिटिश शासन के प्रतीक स्थलों पर भी हमले किए गए।
1857 की क्रान्ति के प्रमुख नेता
1857 की क्रान्ति में जिन नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई उनका विवरण इस प्रकार है-
- बहादुरशाह
- झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई
- नाना साहब
- बेगम हजरतमहल
- कुँवर सिंह
- मौलवी अहमदुल्ला
बहादुरशाह
क्रांतिकारियों ने मुग़ल बादशाह बहादुरशाह के नेतृत्व में क्रांति का संचालन किया। वैसे, मुग़ल बादशाह असक्षम और बूढ़ा हो चुका और इन सब झमेले में पड़ना नहीं चाहता था फिर भी क्रांतिकारियों के निवेदन से उसे इस क्रांति का हिस्सा बनना पड़ा। सारे क्रांतिकारियों ने बहादुरशाह जफ़र को निर्विवाद रूप से विद्रोह का नेता स्वीकार कर लिया। लेकिन वही हुआ जो होना था। बहादुरशाह नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहा। वह बंदी बना लिया गया। उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी।
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई
1853 ई. में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झाँसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। रानी को पेंशन दे दी गई। लक्ष्मीबाई इससे अत्यंत क्रुद्ध थीं। शुरुआत में उन्होंने विद्रोह में दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर परिस्तिथि से बाध्य होकर उन्होंने विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर दिया। मार्च, 1858 ई. में जब ह्यूरोज ने झाँसी पर आक्रमण किया तब रानी ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया। झाँसी को असुरक्षित जान अप्रैल में रानी अपने दत्तक पुत्र के साथ झाँसी छोड़कर कालपी चली गई।
कालपी में भी रानी को हार का सामना करना पड़ा। वहां से वह ताँत्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुँची। ग्वालियर पर विद्रोहियों ने सिंधिया, जो अंग्रेजों का मित्र था, को हराकर कब्ज़ा कर लिया। सिंधिया को आगरा भागना पड़ा। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया परन्तु इसी बीच अंग्रेजी सेना ग्वालियर में भी टपक पड़ी। 17 जून, 1858 ई. को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी वीरगति प्राप्त की। ताँत्या टोपे को गिरफ्तार करके फाँसी दे दी गई। एक महिला हो कर भी बहादुरी के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना किया, यह बात भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है।
नाना साहब
कानपुर में विद्रोह का संचालन नाना साहब की नेतृत्व में हुआ। वह अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने बाजीराव के मृत्यु के बाद उसका पेंशन बंद कर दिया था। इससे नाना साहब गुस्सा हुए और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने का सोचा। जब मेरठ में विद्रोह आरम्भ हुआ उसके बाद नाना साहब ने कानपुर पर अधिकार कर स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने मुग़ल बादशाह बहादुरशाह को भारत का सम्राट और खुद को उसका गवर्नर घोषित कर दिया।
ताँत्या टोपे और अजीमुल्ला के सहयोग से नाना साहब ने अंग्रेजों से कई युद्ध किये। अंग्रेजी सेना मजबूत थी। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने कानपुर, बिठूर और नाना साहब के अन्य ठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया। हार कर नाना साहब नेपाल के जंगलों में छुप गये। आज तक कोई नहीं जानता कि उसके बाद वह कहाँ गए और उनका क्या हुआ।
बेगम हजरतमहल
अवध क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था। अवध की क्रांति का सञ्चालन बेगम हजरतमहल ने किया। नवाब वाजिदअली शाह को अपदस्थ किए जाने के उपरान्त बेगम ने बिरजिस कदर नामक अवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर दिया और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। बेगम को अवध के जमींदारों, किसानों, सिपाहियों आदि सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। उनकी सहायता से बेगम हजरतमहल ने अंग्रेजों को अनेक स्थानों पर हराया और अंततः अंग्रेजों को लखनऊ की रेजीडेंसी में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। अनेक कठिनाइयों के बाद ही अंग्रेज़ पुनः लखनऊ पर अधिकार करने और अवध में विद्रोह को शांत करने में सफल हो पाए।
कुँवर सिंह
बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुँवर थे। वैसे कहने को तो वह एक बहुत बड़े जमींदार थे पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अपने जमींदारी का प्रबंध Board of Revenue को सौंपना चाहते थे पर इस कार्य में वह असफल रहे। कुछ दिनों बाद कुँवर सिंह आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति में पहुँच गए। दानापुर में विद्रोह कर रहे कुछ क्रांतिकारियों ने आरा पहुँच कर कुँवर सिंह को विद्रोह का दायित्व सँभालने को कहा।
कुँवर सिंह बूढ़े हो चुके थे पर फिर भी उन्होंने इस विद्रोह का सञ्चालन करने का निर्णय लिया। नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने अवध और मध्य भारत में भी युद्ध किया। उन्होंने जगदीशपुर, आरा आदि जगहों पर अंग्रेजों को हराया। बलिया के निकट गंगा पार करते समय वह अत्यंत घायल हो चुके थे। उनके बाँह में गोली लगी थी। उन्होंने स्वयं अपने बाँह को काट डाला। 23 अप्रैल, 1858 ई. को जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गयी। उनके बाद उनके भाई अमर सिंह ने भी अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा पर वे उनके सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाए और उन्हें जगदीशपुर छोड़कर भागना पड़ा।
मौलवी अहमदुल्ला
फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने भी 1857 के विद्रोह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। वह मूल रूप से मद्रास के रहने वाले थे। मद्रास में भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना बनायी थी। वे जनवरी, 1857 को फैजाबाद आये। अंग्रेज़ सरकार पहले से उनके आगमन से सतर्क थी। कंपनी ने उनको पकड़ने के लिए सेना भेजी। मौलवी ने डटकर मुकाबला किया। अवध क्रांति में भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रमुख नेता बन कर उभरे। जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्ज़ा किया तो मौलवी अहमदुल्ला रोहिलखंड का नेतृत्व करने लगे। यहीं पुवैन के राजा ने मौलवी की हत्या कर दी। इस कार्य के बदले में उस धोखेबाज राजा को अंग्रेजों के द्वारा 50,000 रु. पुरस्कार स्वरूप मिले।
1857 की क्रान्ति की असफलता का कारण
1857 की क्रान्ति के तहत क्रांतिकारियों के द्वारा भारत को औपनिवेशिक आजादी से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया था और अंग्रेजो को भारत से बाहर खदेड़ने का संकल्प लिया गया था। हालाँकि इस क्रांति के असफल होने के प्रमुख कारण निम्न है :-
- समय से पूर्व क्रांति- 1857 की क्रान्ति अपने निर्धारित समय से पूर्व ही शुरू हो गयी थी जिसके कारण सभी योजनाएँ पूर्ण रूप से अमल में नहीं लायी जा सकी। इसी के परिणामस्वरूप क्रांति को अंग्रेजो के द्वारा आसानी से कुचला गया।
- नेतृत्व का अभाव– इस क्रांति को वास्तव में कोई भी केंद्रीय नेतृत्व नहीं मिल पाया। मुग़ल बादशाह बहादुरशाह जफ़र ने इच्छा के विरुद्ध इस क्रांति में भाग लिया था। साथ ही क्रांति में सैन्य नेतृत्व का भी अभाव था जिससे क्रांति को सही तरीके से समन्वयित नहीं किया जा सका।
- सीमित क्षेत्र– इस क्रांति का मुख्य केंद्र उत्तर-भारत ही रहा एवं देश के अन्य भागों से इसे व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया। यही कारण रहा की क्रांति सीमित क्षेत्र में ही प्रदर्शित हुयी।
- मध्यम वर्ग की उदासीनता– भारत के मध्य वर्ग के अंग्रेजी पढ़े लिखे नागरिको एवं अनेक रजवाड़ो और रियासतों ने इस क्रांति में अंग्रेजो का साथ दिया जिससे की इसे आसानी से दबा दिया गया।
- सीमित साधन– 1857 की क्रान्ति में क्रांतिकारियों के पास सीमित संसाधन थे जिसके कारण इस क्रांति को क्रियान्वित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। वही आधुनिक शस्त्रों से लैस अंग्रेजो के लिए इस क्रांति को दबाना आसान था।
इन सभी प्रमुख कारणों से अंग्रेज आसानी से इस क्रांति का दमन करने में सफल हुए।
1857 की क्रान्ति के परिणाम
1857 की क्रान्ति के परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार की राजसत्ता हिल गयी। क्रांति के पश्चात ब्रिटिश ताज द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने हाथ में ले लिया गया एवं गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत में वायसराय की नियुक्ति की गयी। साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में अधिक ब्रिटिश सैनिको की भर्ती की गयी एवं उत्तर-भारत में अवध, बिहार एवं क्रांति में भाग लेने वाले क्षेत्रों के सिपाहियों को गैर-लड़ाकू घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यपगत सिद्धांत की समाप्ति करके साम्राज्यवाद के विस्तार पर रोक एवं भारतीय रियासतों के आतंरिक मामलो में हस्तक्षेप की नीति को भी खत्म किया गया।
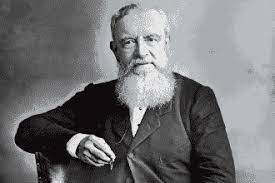
सरकार द्वारा भारत के नागरिको के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर हस्तक्षेप ना करके उन्हें विभिन पदों पर नियुक्ति के अधिकार प्रदान किये गये। हालांकि इस क्रांति का सबसे व्यापक प्रभाव यह रहा की देश में स्वतंत्रता की चेतना का विकास हुआ जिसके परिणामस्वरूप देश अंतत आजाद हुआ।
इन्हें भी देखें –
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी (1600 – 1858)
- ब्रिटिश राज (1857 – 1947)
- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (1885-1947)
- सैयद वंश (1414-1451 ई.)
- टीपू सुल्तान (1750-1799 ई.)
- तुगलक वंश (1320-1413ई.)
- भारतीय परमाणु परीक्षण (1974,1998)
- लोदी वंश (1451-1526 ई.)
- भारत के स्वतंत्रता सेनानी: वीरता और समर्पण
- Revolutionary Database Management System | DBMS
- HTML’s Positive Potential: Empower Your Web Journey|1980 – Present
- A Guide to Database Systems | The World of Data Management
- Kardashev scale