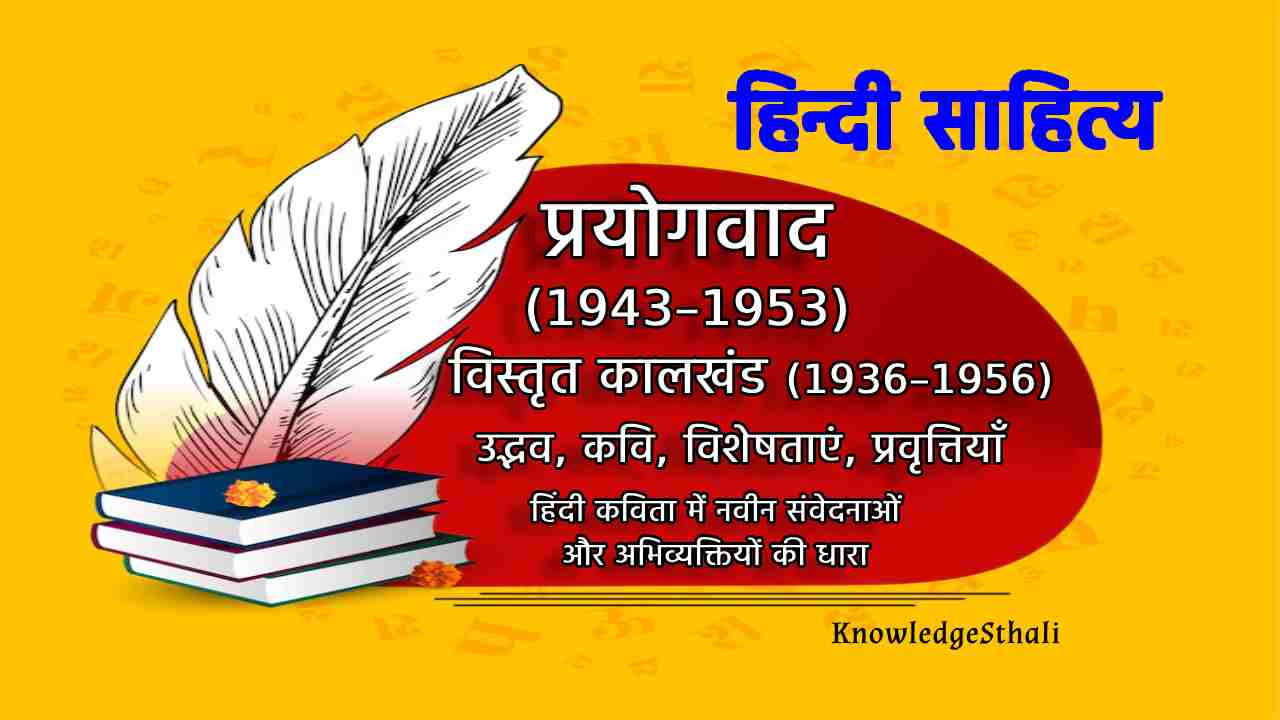हिंदी साहित्य में कविता की अनेक धाराएं समय-समय पर जन्म लेती रही हैं। प्रत्येक साहित्यिक आंदोलन अपने समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानसिक चेतना का प्रतिबिंब होता है। हिंदी कविता में एक ऐसा ही महत्त्वपूर्ण और युगांतकारी आंदोलन रहा है प्रयोगवाद, जिसकी शुरुआत 1943 ई. में मानी जाती है। इस आंदोलन ने कविता की परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा, शैली और विषयवस्तु दोनों में नवीन प्रयोग किए, और हिंदी कविता को एक नई दृष्टि, संवेदना तथा अभिव्यक्ति दी।
यद्यपि हिंदी कविता में प्रयोग तो छायावाद, प्रगतिवाद या उससे पूर्व भी होते आए हैं, परंतु ‘प्रयोगवाद’ एक विशिष्ट अवधारणा बनकर उभरा जो 1943 में प्रकाशित ‘तार सप्तक’ के माध्यम से सामने आया। प्रयोगवाद ने केवल एक नए काव्य शिल्प का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि उसने आधुनिक संवेदनाओं को, जीवन की नग्न यथार्थता को, वैयक्तिक अनुभवों को, नए प्रतीकों और बिंबों में बांध कर प्रस्तुत करने का अभिनव प्रयास किया।
प्रयोगवाद की परिभाषा एवं मूल स्वभाव
प्रयोग शब्द का सामान्य अर्थ है – ‘नई दिशा में अन्वेषण का प्रयास’। जीवन के हर क्षेत्र की तरह साहित्य में भी निरंतर प्रयोग होते रहे हैं। जब कोई कवि या लेखक पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर नई शैली, नई भाषा या नई संवेदना के साथ सृजन करता है, तो वह प्रयोग करता है। किंतु हिंदी कविता में ‘प्रयोगवाद’ शब्द विशेष रूप से उस कविता को रेखांकित करता है जिसमें 1940 के दशक से एक नई काव्य चेतना, नया भाव-बोध और नया अभिव्यक्ति शिल्प दिखाई देने लगा।
डॉ. गणपतिचंद्र गुप्त के अनुसार –
“नयी कविता, नए समाज के नए मानव की नई वृत्तियों की नई अभिव्यक्ति, नई शब्दावली में है, जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है।”
प्रयोगवादी कविता का लक्ष्य केवल नवाचार करना नहीं था, बल्कि वह वैयक्तिक अनुभूतियों, नग्न यथार्थ, विद्रोह, अस्वीकृति, विखंडन और नवीन संवेदनात्मक स्तरों को व्यक्त करने के लिए नए शिल्प और भाषा की तलाश कर रही थी। उसमें शब्द और अर्थ दोनों स्तरों पर नूतन प्रयोग हुए।
प्रयोगवाद का ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भ
प्रयोगवाद का जन्म ‘छायावाद’ और ‘प्रगतिवाद’ की रुढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। छायावाद की वैयक्तिकता, भावुकता और अतिंद्रिय सौंदर्यबोध समय के यथार्थ से कटता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर, प्रगतिवाद पूरी तरह से सामाजिक यथार्थ और राजनीति से प्रेरित होकर व्यक्तिगत अनुभवों और कला के स्वायत्त सौंदर्य को गौण कर रहा था।
डॉ. नगेन्द्र के शब्दों में –
“भाव क्षेत्र में छायावाद की अतिन्द्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत, मूर्त और ऐन्द्रिय चेतना का विकास हुआ और सौंदर्य की परिधि में केवल मसृण और मधुर के अतिरिक्त पुरुष, अनगढ़, भदेश आदि का समावेश हुआ।”
यानी छायावाद की सुंदरता-संवेदना से हटकर प्रयोगवाद ने असौंदर्य को भी सौंदर्य का विषय बनाया। इसी तरह, प्रगतिवाद की सामाजिकता और वैचारिकता से हटकर प्रयोगवाद ने वैयक्तिकता, आत्मबोध और जीवन की विडंबनाओं को प्रस्तुत किया।
प्रयोगवाद का उद्भव: एक प्रतिक्रियात्मक जन्म
प्रयोगवाद का जन्म हिंदी कविता की दो प्रमुख धाराओं — छायावाद और प्रगतिवाद — की रूढ़ियों और सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह एक स्वाभाविक और समयानुकूल साहित्यिक आंदोलन था, जिसने पूर्ववर्ती आंदोलनों की अतियों और जड़ता से विद्रोह कर नवीन काव्य प्रवृत्तियों की नींव रखी।
डॉ. नगेन्द्र प्रयोगवाद के उदय की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए लिखते हैं:
“भाव-क्षेत्र में छायावाद की अतिन्द्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत, मूर्त और ऐन्द्रिय चेतना का विकास हुआ और सौंदर्य की परिधि में केवल मसृण और मधुर के अतिरिक्त पुरुष, अनगढ़, भदेश आदि का समावेश हुआ।”
यह कथन दर्शाता है कि जहाँ छायावाद में सौंदर्यबोध को केवल कोमलता, कल्पना और रहस्यात्मकता तक सीमित कर दिया गया था, वहीं प्रयोगवाद ने इस सौंदर्य की परिधि को विस्तार देते हुए कठोर, असंस्कृत, नग्न और यथार्थ अनुभवों को भी कविता में स्थान दिया।
छायावाद में यद्यपि वैयक्तिकता थी, लेकिन वह उदात्त भावना, अध्यात्म, और रहस्यात्मक प्रेम से परिपूर्ण थी। इसके विपरीत प्रगतिवाद में यथार्थ की अभिव्यक्ति तो थी, पर वह पूरी तरह से सामाजिक समस्याओं और राजनीतिक विचारधारा तक सीमित थी, जहाँ व्यक्ति गौण हो गया था।
इन दोनों के अतियों की प्रतिक्रिया में प्रयोगवाद का उद्भव हुआ – एक ऐसी काव्यधारा जो:
- छायावाद की कल्पनाओं से हटकर ठोस यथार्थ को अपनाती है,
- प्रगतिवाद की विचारधारात्मक कठोरता से मुक्त होकर व्यक्तिपरक अनुभव को केंद्र में लाती है।
इसीलिए प्रयोगवाद को एक ‘घोर अहंमवादी’, ‘वैयक्तिकता’ प्रधान, और ‘नग्न यथार्थवाद’ से युक्त आंदोलन कहा गया, जहाँ कवि अपनी आंतरिक संवेदनाओं, विद्रोह, उलझनों और अस्तित्व की जटिलताओं को व्यक्त करने के लिए नए रूप और शिल्प का सहारा लेता है।
इस प्रकार प्रयोगवाद का जन्म अतिरिक्त भावुकता और अत्यधिक सामाजिकता – इन दोनों के बीच एक नई काव्य चेतना के रूप में हुआ, जो कविता को नई दृष्टि, नई शैली और नई सच्चाई देने वाला सिद्ध हुआ।
प्रयोगवादी कविता की संज्ञा और प्रारंभिक पहचान
प्रयोगवादी कविता को ‘प्रयोगवाद’ नाम सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। उन्होंने हिंदी कविता की उस प्रवृत्ति को रेखांकित किया जो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की सीमाओं से असंतुष्ट होकर नई संवेदनाओं, प्रतीकों और शिल्प प्रयोगों के सहारे एक नया मार्ग तलाश रही थी। इस तरह की कविताएँ अपने प्रारंभिक रूप में 1940 के दशक के आरंभ में सामने आने लगीं।
प्रयोगवाद का वैचारिक आधार
प्रयोगवाद मूलतः प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ आंदोलन था। जबकि प्रगतिवाद ने समाज को केंद्र में रखा और जनसरोकारों पर बल दिया, प्रयोगवाद ने व्यक्ति को समाज से पहले और अनुभव को विचारधारा से ऊपर स्थान दिया। यह एक ऐसी काव्यधारा थी जो विषयवस्तु की तुलना में कलात्मकता, अनुभव और शिल्प को प्राथमिकता देती थी।
इसलिए कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद भाव में ‘व्यक्ति-सत्य’ और शिल्प में ‘रूपवाद’ का पोषक रहा।
प्रयोगवाद का कालखंड (1943–1953)
प्रयोगवादी काव्यधारा का सक्रिय काल 1943 से 1953 ई. तक माना जाता है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित ‘तार सप्तक’ से हुई, जिसने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। इस दौर में प्रयोगवादी कवि भाषा, शिल्प, विषय और शैली के स्तर पर लगातार नवाचार करते रहे।
1953 के बाद, यही प्रवृत्तियाँ अधिक सघन रूप में ‘नई कविता’ के रूप में विकसित हो गईं, जिसके कारण प्रयोगवाद एक संक्रमणकालीन आंदोलन बनकर इतिहास में दर्ज हुआ।
प्रयोगवाद की शुरुआत और ‘तार सप्तक’
यद्यपि प्रयोगवादी प्रवृत्तियाँ 1939 के आसपास ‘उच्छृंखल’ जैसी पत्रिकाओं में दिखाई देने लगी थीं, किंतु इसे साहित्य में एक स्पष्ट आंदोलन का रूप मिला 1943 में प्रकाशित ‘तार सप्तक’ से। इसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ ने किया था। इस संकलन में सात कवियों – अज्ञेय, भारतभूषण अग्रवाल, गिरिजाकुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा और नागार्जुन – की कविताएं संकलित थीं।
‘तार सप्तक’ ने हिंदी कविता की जड़ता को झकझोरा। यह कोई एकरूपी आंदोलन नहीं था, बल्कि विभिन्न प्रवृत्तियों और दृष्टियों का समुच्चय था। इन कवियों में एकता थी – नई भाषा, नई शैली और नए विषयों की खोज की चेतना।
प्रथम तार सप्तक (1943) के बाद दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद तीसरा और चौथा तार सप्तक भी आए। इन संकलनों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और अंततः यह ‘नई कविता’ के रूप में विकसित हुआ।
प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की तुलना
प्रगतिवादी कवियों ने जहाँ निम्न वर्ग/शोषित वर्ग के जीवन को चित्रित किया, जो उनके लिए एक कल्पित सामाजिक यथार्थ था, वहीं प्रयोगवादी कवियों ने उस मध्यवर्गीय यथार्थ को व्यक्त किया जो उन्होंने स्वयं जीया था।
इसीलिए प्रयोगवादी कविता में विस्तार की बजाय गहराई है। यह कविता सतह पर सरल प्रतीत होती है लेकिन भीतर से गहन अनुभूतियों और बौद्धिकता से समृद्ध होती है।
प्रयोगवाद और ‘नई कविता’ का संबंध
प्रयोगवाद एक संक्रमणकालीन आंदोलन था, जिसने छायावाद और प्रगतिवाद के बीच पुल का कार्य किया और आगे चलकर ‘नई कविता’ का मार्ग प्रशस्त किया। नई कविता का आधारभूत ढांचा प्रयोगवाद से ही निर्मित हुआ।
‘नई कविता’ में जीवन की जटिलता, अस्तित्व का संकट, नगरबोध, तनाव, युद्धबोध, अकेलापन आदि प्रमुख विषय बने, और इनकी अभिव्यक्ति के लिए वही प्रयोगवादी शिल्प, भाषा और प्रतीकों को अपनाया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद का पर्यवसान ‘नई कविता’ में हुआ।
प्रयोगवाद के प्रमुख कवि और उनके योगदान
- अज्ञेय – प्रयोगवाद के जन्मदाता और प्रवर्तक माने जाते हैं। ‘अरी ओ करुणा प्रभामय’ से लेकर ‘हरी घास पर क्षण भर’ तक उनकी कविताओं में आत्मबोध, चिंतनशीलता, नवीन बिंब योजना और शिल्प चेतना का समावेश मिलता है।
- भारतभूषण अग्रवाल – उन्होंने सामाजिक यथार्थ को आधुनिक दृष्टि से देखा और उसमें व्यक्तिगत भावबोध जोड़ा।
- गिरिजाकुमार माथुर – उनकी कविताएं प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक शैली में होती थीं, जिनमें आधुनिक सभ्यता की पीड़ा को रेखांकित किया गया।
- नागार्जुन – यद्यपि वे प्रगतिशील चेतना के कवि माने जाते हैं, लेकिन उनके कई प्रयोगवादी गीत और प्रतीकात्मक कविताएं इस धारा को समृद्ध करती हैं।
- प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा – इन कवियों ने नए शिल्प और वैचारिक गहराई के माध्यम से प्रयोगवाद की सीमाओं का विस्तार किया।
इनके अलावा धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन आदि कवियों ने भी प्रयोगवादी आंदोलन का नेतृत्व किया।
इन्हीं के साथ नकेनवादियों – नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, और नरेश की कविताएं भी प्रयोगवादी काव्य की धारा में आती हैं। इन तीनों ने अपने काव्य को ‘प्रयोग पद्य’ यानी ‘प्रपद्य’ कहा, इस कारण उनकी धारा को ‘प्रपद्यवाद’ भी कहा जाता है।
प्रयोगवाद की आलोचना
प्रयोगवाद पर यह आरोप भी लगाए गए कि यह अत्यधिक वैयक्तिक है, जन-सामान्य की समझ से परे है, और उसकी जटिलता आम पाठक के लिए संवादहीन हो जाती है। इस पर अत्यधिक बौद्धिकता, निराशावाद, अराजकता और आत्मकेंद्रितता का आरोप भी लगाया गया।
श्री लक्ष्मी कांत वर्मा ने कहा –
“छायावाद ने अपने शब्दाडंबर में बहुत से शब्दों और बिंबों के गतिशील तत्त्वों को नष्ट कर दिया था, जबकि प्रगतिवाद ने सामाजिकता के नाम पर विभिन्न भाव-स्तरों को अभिधात्मक बना दिया था।”
इसलिए नए कवियों को सर्वथा नई भाषा, नया स्वर और नई शैली अपनानी पड़ी।
प्रयोगवाद की उपलब्धियाँ
- कविता को वैचारिक बंधनों से मुक्त किया।
- व्यक्तित्व और आत्मबोध को काव्य का केंद्र बनाया।
- भाषा, शिल्प, प्रतीकों और बिंबों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया।
- नई कविता और आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों की नींव रखी।
निष्कर्ष
प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में केवल एक शैली या प्रवृत्ति नहीं था, बल्कि यह संवेदनात्मक और बौद्धिक आंदोलन था जिसने कविता को नयी दिशा, नया शिल्प और नये विचार दिये। यह आंदोलन छायावाद की भावुकता और प्रगतिवाद की वैचारिकता – दोनों से आगे बढ़कर व्यक्तित्व की गहराइयों, जीवन की नग्न सच्चाइयों, और मानव अस्तित्व की गुत्थियों को अभिव्यक्त करता है।
प्रयोगवाद का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि उसने नए प्रयोग किए, बल्कि इस बात में भी है कि उसने हिंदी कविता को आधुनिक युग के अनुरूप परिवर्तित किया और उसे विश्व साहित्य की समकालीन धारा के समकक्ष खड़ा किया।
इस प्रकार, प्रयोगवाद हिंदी कविता के इतिहास में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी मोड़ है, जो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है।
महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर (FAQs)
प्रयोगवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं, जो परीक्षा, निबंध लेखन, प्रतियोगी परीक्षाओं या साहित्यिक अध्ययन के लिए उपयोगी हो सकते हैं:
✅ 1. प्रयोगवाद क्या है?
उत्तर:
प्रयोगवाद हिंदी कविता की वह काव्यधारा है जो छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में 1943 ई. में ‘तार सप्तक’ के माध्यम से सामने आई। इसमें नई संवेदना, वैयक्तिकता, नग्न यथार्थ और शिल्पगत प्रयोगों को प्राथमिकता दी गई।
✅ 2. प्रयोगवाद का जन्म कैसे और क्यों हुआ?
उत्तर:
प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिभावुकता और प्रगतिवाद की विचारधारात्मक सीमाओं की प्रतिक्रिया में हुआ। यह आंदोलन व्यक्ति की अनुभूति, आत्मबोध और कलात्मक स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर विकसित हुआ।
✅ 3. प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
उत्तर:
‘प्रयोगवादी कविता’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था।
✅ 4. प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन-कौन हैं?
उत्तर:
प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में शामिल हैं:
- अज्ञेय
- गिरिजा कुमार माथुर
- मुक्तिबोध
- भारत भूषण अग्रवाल
- रघुवीर सहाय
- धर्मवीर भारती
- नेमिचंद जैन
- नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, और नरेश (नकेनवादी)
✅ 5. प्रयोगवाद के उद्भव में छायावाद और प्रगतिवाद की क्या भूमिका थी?
उत्तर:
छायावाद की अतिन्द्रिय भावुकता और प्रगतिवाद की विचारधारात्मक कठोरता से असंतोष ने एक नए वैयक्तिक और यथार्थपरक काव्य दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसे प्रयोगवाद कहा गया।
✅ 6. ‘तार सप्तक’ का प्रयोगवाद में क्या योगदान है?
उत्तर:
1943 में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित ‘तार सप्तक’ को प्रयोगवादी कविता की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। इसमें सात कवियों की कविताएँ थीं, जिनमें नई चेतना, नई शैली और नवीन शिल्प का प्रयोग स्पष्ट था।
✅ 7. नकेनवाद और प्रपद्यवाद में क्या संबंध है?
उत्तर:
नकेनवादी कवियों – नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, और नरेश – ने अपनी कविताओं को ‘प्रयोग पद्य’ या ‘प्रपद्य’ कहा, इसलिए नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है।
✅ 8. प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:
- व्यक्तिवाद और अहंमवाद
- नग्न यथार्थ का चित्रण
- शिल्प और भाषा में नवीन प्रयोग
- विचारधारा का विरोध
- नई राहों की खोज
- बौद्धिकता और दार्शनिकता
- काम-भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति
- रूपवाद का आग्रह
✅ 9. प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है?
उत्तर:
प्रगतिवाद समाज और जनसरोकार पर केंद्रित होता है जबकि प्रयोगवाद व्यक्ति के आंतरिक अनुभव, आत्मबोध और शिल्पगत सौंदर्य पर। प्रगतिवाद में विचारधारा प्रमुख होती है, जबकि प्रयोगवाद में कलात्मकता और संवेदनशीलता।
✅ 10. प्रयोगवादी कविता को ‘रूपाकाराग्रही कविता’ क्यों कहा गया?
उत्तर:
क्योंकि इसमें कवियों ने रूप (Form), शिल्प और संरचना को विशेष महत्व दिया। शिल्प के प्रति विशेष आग्रह के कारण आलोचकों ने इन कविताओं को ‘रूपाकाराग्रही कविता’ और कवियों को ‘रूपवादी’ (Formist) कहा।
✅ 11. प्रयोगवादी कविता में कौन-से वर्ग का यथार्थ चित्रित हुआ है?
उत्तर:
प्रयोगवादी कविता ने मुख्यतः मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रित किया, जो कवियों का स्वयं का अनुभूत और जिया हुआ अनुभव था।
✅ 12. अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है?
उत्तर:
अज्ञेय ने 1943 में ‘तार सप्तक’ का संपादन कर प्रयोगवाद को एक संगठित काव्य आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने नई कविता की भाषा, शिल्प और चेतना को दिशा दी। इसीलिए उन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है।
✅ 13. प्रयोगवाद में ‘अहंमवाद’ का क्या अर्थ है?
उत्तर:
यहाँ ‘अहंमवाद’ का अर्थ कवि की आत्म-संवेदना, वैयक्तिक अनुभव और व्यक्तित्व के बोध से है। प्रयोगवादी कवि स्वयं को केंद्र में रखकर अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति करता है।
✅ 14. प्रयोगवाद में ‘नग्न यथार्थ’ की अवधारणा क्या है?
उत्तर:
प्रयोगवाद में ‘नग्न यथार्थ’ का अर्थ है – जीवन की असुविधाजनक, कुरूप, विद्रूप और असहज सच्चाइयों का बिना अलंकरण के चित्रण।
✅ 15. प्रयोगवाद किन साहित्यिक प्रवृत्तियों का विरोध करता है?
उत्तर:
प्रयोगवाद ने छायावाद की भावुकता और कल्पनात्मकता तथा प्रगतिवाद की विचारधारात्मकता और राजनीतिक रंग का विरोध किया।
✅ 16. ‘नई कविता’ और ‘प्रयोगवाद’ में क्या संबंध है?
उत्तर:
प्रयोगवाद ने ही नई कविता का मार्ग प्रशस्त किया। नई कविता की शिल्प, भाषा और वैयक्तिक संवेदना की जड़ें प्रयोगवाद में ही हैं।
✅ 17. प्रयोगवादी कविता में ‘काम-भावना’ की भूमिका क्या है?
उत्तर:
प्रयोगवादी कवियों ने काम-संवेदना को नैसर्गिक रूप में प्रस्तुत किया। देह, प्रेम, वासना आदि विषयों को संकोच के बिना, सौंदर्य और यथार्थ के साथ लिखा।
✅ 18. प्रयोगवादी कविता में भाषा का क्या स्वरूप होता है?
उत्तर:
भाषा अधिकतर मुक्त, प्रतीकात्मक, आधुनिक, और कभी-कभी दुरूह होती है। परंपरागत अलंकार और छंदबद्धता की जगह प्रयोगशीलता और स्वाभाविकता को प्राथमिकता दी गई।
✅ 19. ‘प्रपद्यवाद’ क्या है?
उत्तर:
‘प्रपद्यवाद’ शब्द नकेनवादियों द्वारा प्रयुक्त ‘प्रयोग पद्य’ (प्रपद्य) से निकला है। यह एक विशिष्ट प्रयोगवादी प्रवृत्ति थी, जिसमें गहन वैयक्तिकता और बिंबात्मकता प्रमुख थीं।
✅ 20. प्रयोगवाद किस वर्ग की संवेदना को अभिव्यक्त करता है?
उत्तर:
प्रयोगवाद मुख्यतः मध्यवर्गीय व्यक्ति की संवेदनाओं, दुविधाओं, असुरक्षाओं और अस्तित्वगत उलझनों को व्यक्त करता है।
✅ 21. प्रयोगवादी कविता का प्रभाव हिंदी साहित्य पर क्या पड़ा?
उत्तर:
प्रयोगवाद ने हिंदी कविता को परंपरा की रूढ़ियों से मुक्त कर, उसे आधुनिक, वैश्विक और वैयक्तिक काव्यधारा से जोड़ दिया। यह कविता की नई संवेदना और नई भाषा का आधार बनी।
इन्हें भी देखें –
- नयी कविता: हिंदी कविता की नवीन धारा का उद्भव, कवि और विकास
- नवगीत: नए गीत का नामकरण, विकास, प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाएं
- हिंदी उपन्यास: विकास, स्वरूप और साहित्यिक महत्त्व
- हिंदी उपन्यास और उपन्यासकार: लेखक और रचनाओं की सूची
- मुहावरा और लोकोक्तियाँ 250+
- वर्तनी किसे कहते है? उसके नियम और उदहारण
- रस- परिभाषा, भेद और उदाहरण
- छायावादोत्तर युग (शुक्लोत्तर युग: 1936–1947 ई.) | कवि और उनकी रचनाएँ