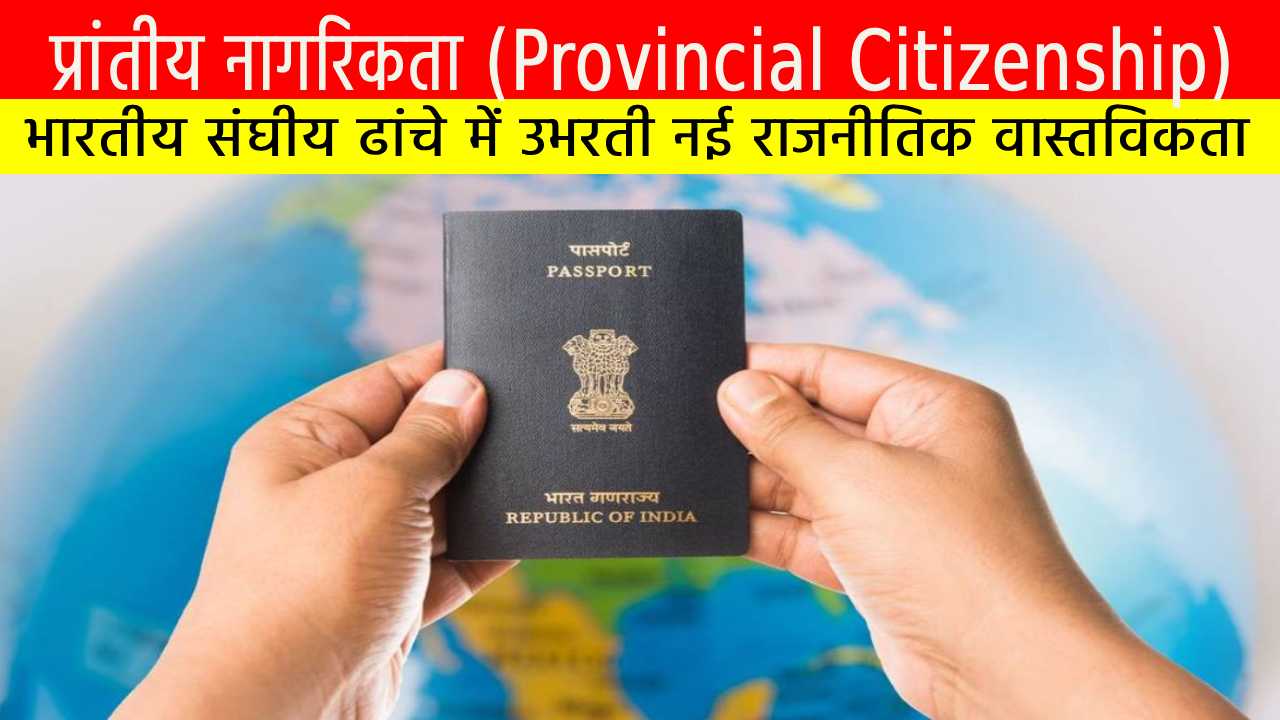भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है और एकल राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा को मान्यता देता है। संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि भारत जैसे बहुभाषी, बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज में नागरिकता केवल “भारतीय” पहचान पर आधारित हो, न कि प्रांतीय या क्षेत्रीय आधार पर। इसीलिए भारतीय संविधान में केवल एक ही राष्ट्रीय नागरिकता (Single Citizenship) का प्रावधान किया गया।
लेकिन व्यावहारिक राजनीति और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों ने इस आदर्श को कई बार चुनौती दी है। हाल के वर्षों में “प्रांतीय नागरिकता” (Provincial Citizenship) की अवधारणा तेजी से उभरकर सामने आई है। यह अवधारणा विशेषकर उन राज्यों में दिखाई देती है, जहाँ स्थानीय पहचान, संसाधनों पर अधिकार और प्रवासियों के प्रति संदेह या अस्वीकार की भावना राजनीतिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। झारखंड, जम्मू–कश्मीर और असम इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं।
यह लेख प्रांतीय नागरिकता की अवधारणा, उसके ऐतिहासिक और राजनीतिक आधार, भारतीय संघीय ढांचे पर उसके प्रभाव, और भविष्य में इससे उत्पन्न संभावित चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
प्रांतीय नागरिकता की परिभाषा और विचारधारा
प्रांतीय नागरिकता को समझने के लिए इसे निवास-आधारित पहचान की राजनीति कहा जा सकता है। इसका मूल आधार “स्थानीयतावादी भावना” (nativist sentiment) है, जिसमें यह माना जाता है कि किसी राज्य के संसाधनों, नौकरियों और राजनीतिक अवसरों पर सबसे पहला अधिकार वहाँ के “मूल निवासियों” का है।
- विचारधारात्मक दृष्टि से यह स्थानीय जनता के बीच असुरक्षा और उपेक्षा की भावना से उत्पन्न होती है।
- राजनीतिक दृष्टि से यह नेताओं के लिए समर्थन जुटाने का प्रभावी हथियार बन जाती है।
- सामाजिक दृष्टि से यह आंतरिक प्रवासियों को हाशिए पर डाल देती है और “हम बनाम वे” (us vs them) की खाई को गहरा करती है।
इस प्रकार, प्रांतीय नागरिकता एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जो संविधान में वर्णित “भारतीय नागरिकता” के आदर्श के समानांतर एक अनौपचारिक लेकिन प्रभावी पहचान निर्मित करती है।
भारत में प्रांतीय नागरिकता का प्रचलन
भारत के अलग-अलग राज्यों में प्रांतीय नागरिकता का प्रभाव अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है।
- डोमिसाइल (Domicile) स्थिति
- कई राज्यों में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र आवश्यक कर दिया गया है।
- यह प्रमाणपत्र यह साबित करता है कि व्यक्ति या उसके पूर्वज लंबे समय से उस राज्य में रह रहे हैं।
- राजनीतिक mobilization
- चुनावों के दौरान स्थानीय बनाम बाहरी (insider vs outsider) का मुद्दा उठाकर जनसमर्थन जुटाया जाता है।
- इससे स्थानीय जनता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी पहचान और अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे।
- संवैधानिक आदर्श को चुनौती
- भारतीय संविधान का मूल आदर्श “एक राष्ट्र, एक नागरिकता” है।
- लेकिन प्रांतीय नागरिकता का चलन इस आदर्श को चुनौती देता है और नागरिकता की बहुस्तरीय समझ उत्पन्न करता है।
राजनीतिक वास्तविकता और लोकतांत्रिक जटिलताएँ
प्रांतीय नागरिकता केवल पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संघीय राजनीति पर गहरा असर डालती है।
- आंतरिक प्रवास और विवाद
- भारत में लाखों लोग बेहतर अवसरों की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं।
- जब वे नए राज्य में बसते हैं, तो अक्सर स्थानीय जनता उन्हें बाहरी (outsider) मानकर विरोध करती है।
- लोकतांत्रिक निर्णयों पर असर
- क्षेत्रीय पार्टियाँ डोमिसाइल आधारित नीतियों को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करती हैं।
- इससे लोकतांत्रिक निर्णय-making जटिल हो जाता है क्योंकि यह राष्ट्रीय नागरिकता की एकरूपता को कमजोर करता है।
- संघीय ढांचे की चुनौती
- भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है।
- लेकिन जब यह स्वायत्तता नागरिकता की समानता पर प्रश्न उठाने लगे, तो यह संघीय एकता के लिए खतरा बन जाती है।
हालिया अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष
एक हालिया अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रांतीय नागरिकता का प्रभाव भारत के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है। इसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:
- राज्यों के उदाहरण
- झारखंड: यहाँ डोमिसाइल राजनीति का इस्तेमाल क्षेत्रीय पहचान और ऐतिहासिक शिकायतों को उजागर करने के लिए किया जाता है।
- जम्मू–कश्मीर: अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा और वहाँ की नागरिकता (स्थायी निवास प्रमाणपत्र) का विशेष महत्व रहा है।
- असम: यहाँ स्थानीयतावादी राजनीति NRC (National Register of Citizens) और CAA (Citizenship Amendment Act) जैसे विवादों के केंद्र में रही है।
- स्थानीयतावादी और बहुसंख्यक भावनाएँ
- डोमिसाइल नीतियाँ अक्सर बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को प्राथमिकता देती हैं।
- इससे अल्पसंख्यक या प्रवासी समुदाय उपेक्षित हो जाते हैं।
- संवैधानिक आदर्श का ह्रास
- “एक राष्ट्र, एक नागरिकता” की अवधारणा कमजोर पड़ती है।
- नागरिकता का स्वरूप बहुस्तरीय हो जाता है – एक तरफ राष्ट्रीय नागरिकता, दूसरी तरफ प्रांतीय पहचान।
झारखंड का विशेष मामला
झारखंड प्रांतीय नागरिकता की राजनीति का सबसे प्रमुख उदाहरण है।
- पृष्ठभूमि: झारखंड का गठन 2000 में हुआ था, और इसका मूल आधार था कि यहाँ की आदिवासी और स्थानीय जनता को उनके अधिकार मिलें।
- डोमिसाइल आंदोलन: बार-बार यह मांग उठती रही है कि सरकारी नौकरियाँ और संसाधन केवल उन्हीं लोगों को मिलें जो झारखंड के मूल निवासी हों।
- राजनीतिक उपयोग: विभिन्न पार्टियाँ चुनावों के समय इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती हैं और जनता को आश्वासन देती हैं कि बाहरी लोगों से उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
- संवैधानिक संकट: यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा को कमजोर करती है और प्रवासी मजदूरों या अन्य राज्यों से आए लोगों को हाशिए पर डाल देती है।
प्रांतीय नागरिकता के पक्ष और विपक्ष
पक्ष में तर्क
- स्थानीय संसाधनों की रक्षा
- प्रांतीय नागरिकता स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देती है, जिससे उन्हें अपने संसाधनों पर अधिकार मिलता है।
- सांस्कृतिक संरक्षण
- बाहरी प्रवासियों के दबाव से स्थानीय भाषा और संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जाता है।
- आर्थिक समानता
- स्थानीय जनता को नौकरियों और अवसरों में प्राथमिकता मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।
विपक्ष में तर्क
- संवैधानिक विरोधाभास
- यह भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा के खिलाफ है।
- राष्ट्रीय एकता पर खतरा
- “हम और वे” की भावना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है।
- प्रवासी मजदूरों का शोषण
- आंतरिक प्रवासी अक्सर अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और उन्हें समाज में हाशिए पर धकेल दिया जाता है।
भारतीय संघवाद पर प्रभाव
प्रांतीय नागरिकता भारतीय संघवाद (federalism) पर गहरे प्रभाव डालती है।
- यह राज्यों की स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन को चुनौती देती है।
- यदि यह प्रवृत्ति और बढ़ती है, तो भारत के संघीय ढांचे में असमानता और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
भविष्य की चुनौतियाँ
- संवैधानिक संतुलन
- राज्यों की स्वायत्तता और नागरिकता की समानता के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है।
- प्रवासी अधिकार
- आंतरिक प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है ताकि वे किसी भी राज्य में भेदभाव का शिकार न हों।
- राजनीतिक दुरुपयोग
- प्रांतीय नागरिकता को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति को सीमित करना होगा।
समाधान और संभावित मार्ग
- संवैधानिक सुधार नहीं, व्यावहारिक नीति
- संविधान में बदलाव की बजाय राज्यों को संतुलित नीतियाँ बनाने की जरूरत है, जिससे स्थानीय जनता की चिंता भी दूर हो और प्रवासियों को भी समान अवसर मिलें।
- समान अवसर आयोग
- केंद्र और राज्य मिलकर एक ऐसा आयोग बना सकते हैं जो आंतरिक प्रवासियों के अधिकारों की निगरानी करे।
- सांस्कृतिक संवाद
- स्थानीय और प्रवासी समुदायों के बीच सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए ताकि टकराव की स्थिति न बने।
निष्कर्ष
प्रांतीय नागरिकता भारतीय लोकतंत्र और संघवाद की एक नई और जटिल वास्तविकता है। यह स्थानीय जनता की चिंताओं और अधिकारों को तो सामने लाती है, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय नागरिकता की एकरूपता को भी चुनौती देती है। झारखंड, जम्मू–कश्मीर और असम जैसे राज्यों में इसके उदाहरण यह दर्शाते हैं कि यह मुद्दा केवल क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के लिए गहरी चुनौती बन चुका है।
भविष्य में भारत को इस चुनौती का समाधान लोकतांत्रिक संवाद, संतुलित नीतियों और नागरिकता के संवैधानिक आदर्शों की पुनः पुष्टि के माध्यम से खोजना होगा। तभी हम “एक राष्ट्र, एक नागरिकता” के उस आदर्श को बचा पाएँगे, जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।
इन्हें भी देखें –
- पैरासिटामोल और ऑटिज़्म: मिथक, वैज्ञानिक साक्ष्य और वैश्विक बहस
- चाबहार पोर्ट: भारत की कनेक्टिविटी और भू-राजनीति में बदलता परिदृश्य
- सर एम. विश्वेश्वरैया: भारतीय इंजीनियरिंग के जनक और राष्ट्र निर्माण के प्रेरणास्तंभ
- स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास: विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, बनीं सबसे तेज़ शतक जड़ने वाली भारतीय क्रिकेटर
- राज्यों का बढ़ता सार्वजनिक ऋण : एक गंभीर चुनौती
- एनवीडिया–ओपनएआई सौदा: 100 अरब डॉलर का निवेश और एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषा
- भाषा और लिपि : उद्भव, विकास, अंतर, समानता और उदाहरण
- भारतीय आर्यभाषाओं का ऐतिहासिक विकास: प्राचीन से आधुनिक काल तक
- भारत की भाषाएँ: संवैधानिक मान्यता, आधिकारिक स्वरूप और विश्व परिप्रेक्ष्य में भाषाई विविधता
- विश्व की भाषाएँ : विविधता, विकास और वैश्विक प्रभाव