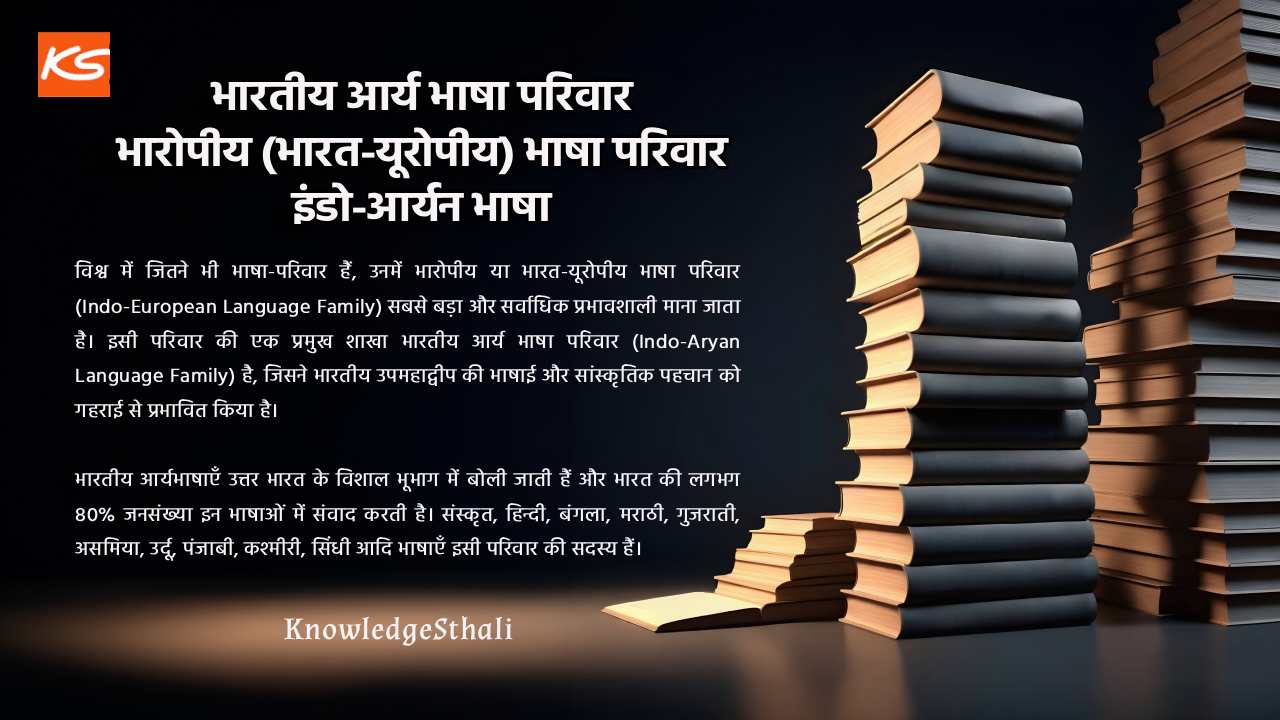मानव सभ्यता के विकास में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भाषा न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि यह संस्कृति, ज्ञान और विचारों की वाहक भी है। विश्व में जितने भी भाषा-परिवार हैं, उनमें भारोपीय या भारत-यूरोपीय भाषा परिवार (Indo-European Language Family) सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसी परिवार की एक प्रमुख शाखा भारतीय आर्य भाषा परिवार (Indo-Aryan Language Family) है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया है।
भारतीय आर्यभाषाएँ उत्तर भारत के विशाल भूभाग में बोली जाती हैं और भारत की लगभग 80% जनसंख्या इन भाषाओं में संवाद करती है। संस्कृत, हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, असमिया, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी आदि भाषाएँ इसी परिवार की सदस्य हैं।
भारोपीय (भारत–यूरोपीय) भाषा परिवार का परिचय
भारोपीय या भारत-यूरोपीय भाषा परिवार संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यह न केवल भारत और यूरोप तक सीमित है, बल्कि एशिया, रूस, ईरान और अमेरिका जैसे देशों में भी इसकी शाखाएँ पाई जाती हैं। अनुमानतः विश्व की लगभग 45% जनसंख्या इस भाषा परिवार की किसी न किसी भाषा को बोलती है।
इस परिवार में अनेक प्राचीन एवं आधुनिक भाषाएँ सम्मिलित हैं — जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, फ़ारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पेनी, इतालवी, रूसी, हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि।
भारोपीय भाषा परिवार की विशेषता यह है कि इसकी अधिकांश भाषाओं में व्याकरणिक ढांचा, शब्द मूल (root forms) तथा ध्वनि परिवर्तन के नियमों में समानता पाई जाती है। भाषाविज्ञानियों के अनुसार, इन सभी भाषाओं का मूल स्रोत एक सामान्य पूर्वज भाषा — “प्रोटो-इंडो-यूरोपीय” (Proto-Indo-European) — रही होगी, जो लगभग 4000–3000 ई.पू. के आसपास बोली जाती थी।
भारतीय आर्य भाषा परिवार की उत्पत्ति
भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा को भारतीय आर्यभाषा परिवार (Indo-Aryan Language Family) कहा जाता है। यह शाखा मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
इस परिवार की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, जिसे भारतीय आर्यभाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत से ही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और तत्पश्चात आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ।
भारतीय आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास
भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को सामान्यतः चार प्रमुख कालों में विभाजित किया जाता है —
1. वैदिक संस्कृत काल (1500 ई.पू. – 800 ई.पू.)
यह भारतीय आर्यभाषाओं का प्रारंभिक और सबसे प्राचीन रूप था। इसी काल में चारों वेद — ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। वैदिक संस्कृत की भाषा अत्यंत परिष्कृत, जटिल और दार्शनिक थी। इसमें स्वर और व्यंजन की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया।
2. लौकिक संस्कृत काल (800 ई.पू. – 500 ई.पू.)
यह वैदिक संस्कृत का विकसित रूप था, जिसे संस्कृत भाषा का शास्त्रीय युग कहा जाता है। इस काल में रामायण, महाभारत, उपनिषद, महाकाव्य, नाटक और नीति शास्त्रों की रचना हुई। पाणिनि, कालिदास, भास, बाणभट्ट जैसे महान रचनाकारों ने संस्कृत साहित्य को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्रदान की।
3. पाली और प्राकृत काल (500 ई.पू. – 500 ई.)
इस काल में संस्कृत के सरल और लोकव्यवहारिक रूप के रूप में पाली और प्राकृत भाषाओं का प्रचलन हुआ। पाली भाषा मुख्यतः बौद्ध साहित्य की भाषा बनी, जबकि जैन और लोककथाओं में प्राकृत का प्रयोग हुआ। प्राकृत के प्रमुख रूप — मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी आदि — थे।
4. अपभ्रंश काल (500 ई. – 1000 ई.)
प्राकृत भाषाओं से आगे चलकर अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। यह संस्कृत और प्राकृत से अधिक सरल और लोकप्रचलित रूप था। अपभ्रंश से ही आगे चलकर आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव पड़ी। इस काल में शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री अपभ्रंश प्रमुख थे, जिन्होंने क्रमशः हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया जैसी भाषाओं को जन्म दिया।
भारोपीय या भारत–यूरोपीय भाषा परिवार का वर्गीकरण
विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह भारोपीय (Indo-European) या भारत–यूरोपीय भाषा परिवार है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अनेक महत्वपूर्ण भाषाएँ सम्मिलित हैं। यह परिवार न केवल यूरोप, बल्कि एशिया के विस्तृत भूभाग में भी फैला हुआ है।
प्राचीन भारोपीय भाषाएँ
प्राचीन काल में इस परिवार की प्रमुख भाषाएँ थीं — संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवेस्ता, यूनानी (ग्रीक), लैटिन और प्राचीन फ्रांसीसी। इन भाषाओं ने आगे चलकर विविध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को जन्म दिया। विशेष रूप से संस्कृत ने भारतीय उपमहाद्वीप में साहित्य, दर्शन और धर्म का आधार तैयार किया।
आधुनिक भारोपीय भाषाएँ
समय के साथ इस भाषा परिवार की अनेक आधुनिक भाषाएँ विकसित हुईं, जैसे — अंग्रेज़ी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फ़ारसी, हिन्दी, बंगला, गुजराती और मराठी। ये भाषाएँ आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान और साहित्य की प्रमुख माध्यम बन चुकी हैं।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ
भारत की अधिकांश प्रमुख भाषाएँ आज आर्यभाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें से प्रमुख भाषाएँ हैं —
- हिन्दी – उत्तर भारत की संपर्क भाषा, तथा भारत की राजभाषा
- पंजाबी – पंजाब और हरियाणा क्षेत्र की प्रमुख भाषा
- उर्दू – फ़ारसी और अरबी प्रभाव से विकसित भाषा
- कश्मीरी – उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख भाषा
- सिंधी – सिंधु घाटी और पश्चिमी भारत में प्रचलित
- गुजराती – गुजरात की राजभाषा
- मराठी – महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा
- बांग्ला – पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा
- उड़िया (ओड़िया) – ओडिशा की प्रमुख भाषा
- असमिया – असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्यभाषा
इन सभी भाषाओं की व्याकरणिक संरचना और शब्द भंडार में संस्कृत का गहरा प्रभाव है। कई शब्द, धातुएँ और वाक्य संरचनाएँ लगभग समान पाई जाती हैं। इसीलिए भारतीय आर्य भाषाओं के वक्ताओं को एक-दूसरे की भाषा समझने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास
भारतीय आर्य भाषाएँ अपने मूल स्रोत संस्कृत से विकसित होकर कई चरणों से गुज़रीं — पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि रूपों में। विशेष रूप से अपभ्रंश काल (500 ई. से 1000 ई. तक) भारतीय आर्य भाषाओं के गठन का महत्वपूर्ण युग रहा। इसी अवधि में देशभर में शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री अपभ्रंश जैसी बोलियाँ प्रचलित थीं, जिन्होंने आगे चलकर आधुनिक भारतीय भाषाओं — हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया आदि — को जन्म दिया।
इस विकास प्रक्रिया को एक निरंतर भाषाई प्रवाह के रूप में देखा जा सकता है —
वैदिक संस्कृत → लौकिक संस्कृत → पाली/प्राकृत → अपभ्रंश → आधुनिक आर्य भाषाएँ
भारतीय आर्य भाषाओं की पारस्परिक समानता
संस्कृत से विकसित होने के कारण भारतीय आर्य परिवार की भाषाओं में कई व्याकरणिक और शब्दात्मक समानताएँ पाई जाती हैं। इनकी वाक्य संरचना, धातु प्रणाली तथा शब्दकोशीय मूल में गहरा सामंजस्य है। यही कारण है कि हिन्दी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, असमिया, सिंधी, उर्दू और कश्मीरी जैसी भाषाओं के वक्ता परस्पर संवाद में अपेक्षाकृत सहज महसूस करते हैं।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और आधुनिक भारोपीय भाषाएँ : संबंध और अंतर
भाषा-विज्ञान के दृष्टिकोण से भारतीय आर्य भाषाएँ (Indo-Aryan Languages) और भारोपीय या भारत–यूरोपीय भाषाएँ (Indo-European Languages) आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, किंतु दोनों एक ही नहीं हैं। वास्तव में, भारतीय आर्य भाषाएँ भारोपीय भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण उपशाखा हैं। इस संबंध को समझने के लिए हमें उनके ऐतिहासिक विकासक्रम और संरचनात्मक वर्गीकरण को देखना आवश्यक है।
भाषावैज्ञानिक वर्गीकरण (Linguistic Classification)
भारोपीय या भारत–यूरोपीय भाषा परिवार विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसका प्रसार भारत से लेकर यूरोप के सुदूर पश्चिम तक फैला हुआ है। इस परिवार से अनेक शाखाएँ निकलीं, जिनमें से एक प्रमुख शाखा है — हिन्द–ईरानी शाखा (Indo-Iranian branch)।
इसी हिन्द–ईरानी शाखा की एक उपशाखा है — भारतीय आर्य शाखा (Indo-Aryan sub-branch)।
इस वंशानुक्रम को सरल रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है —
भारोपीय (Indo-European) भाषा परिवार
└── हिन्द–ईरानी शाखा (Indo-Iranian branch)
├── ईरानी शाखा (Iranian branch) – फ़ारसी, कुर्दी, पश्तो आदि
└── भारतीय आर्य शाखा (Indo-Aryan branch) – हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, असमिया आदि
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि “भारतीय आर्य भाषाएँ” “भारोपीय भाषा परिवार” का एक भाग हैं, न कि उससे पृथक या समान स्तर की इकाई।
दोनों के बीच मुख्य अंतर
| तुलना का बिंदु | भारोपीय (Indo-European) भाषाएँ | भारतीय आर्य (Indo-Aryan) भाषाएँ |
|---|---|---|
| स्तर | सबसे बड़ा भाषा परिवार (macro family) | उसी परिवार की एक उपशाखा |
| भौगोलिक क्षेत्र | यूरोप और एशिया के व्यापक भागों में | मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में |
| उद्भव काल | लगभग 4000–3500 ई.पू. में एक सामान्य मातृभाषा “प्रोटो-भारोपीय” से | लगभग 1500 ई.पू. में वैदिक संस्कृत से |
| प्रमुख शाखाएँ | जर्मैनिक, लैटिन (Italic), स्लाविक, सेल्टिक, ईरानी, हिन्द–आर्य आदि | केवल हिन्द–आर्य शाखा |
| उदाहरण भाषाएँ | अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, ग्रीक, लैटिन, रूसी, फ़ारसी, हिन्दी आदि | हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, असमिया, उर्दू आदि |
सरल रूप में समझें
“भारोपीय भाषाएँ” समूचे भाषा–परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं —
जिनमें भारत, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया की अनेक भाषाएँ शामिल हैं।
वहीं “भारतीय आर्य भाषाएँ” केवल उसी परिवार की एक भारतीय उपशाखा हैं, जो मुख्यतः भारतवर्ष और उसके आस-पास के क्षेत्रों में विकसित हुईं।
अतः
हर भारतीय आर्य भाषा एक भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य है,
परंतु हर भारोपीय भाषा भारतीय आर्य नहीं होती।
उदाहरण के लिए, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी या रूसी — ये सभी भारोपीय हैं, पर भारतीय आर्य नहीं; जबकि हिन्दी और बंगला — दोनों भारोपीय परिवार की भारतीय आर्य शाखा से संबंधित हैं।
उदाहरणात्मक तुलना
| भाषा | भाषा–परिवार | उपशाखा |
|---|---|---|
| English | Indo-European | Germanic |
| French | Indo-European | Italic (Romance) |
| Russian | Indo-European | Slavic |
| Persian (Farsi) | Indo-European | Iranian |
| Hindi | Indo-European | Indo-Aryan |
संक्षेप में कहा जाए तो —
भारतीय आर्य भाषाएँ, भारोपीय भाषा परिवार की एक सशक्त और जीवंत शाखा हैं। इनके विकास की जड़ें वैदिक संस्कृत में निहित हैं, जबकि भारोपीय भाषा परिवार का दायरा उससे कहीं अधिक विस्तृत है।
भारतीय आर्य भाषाएँ आज भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन की वाहक हैं, वहीं भारोपीय परिवार की अन्य शाखाएँ (जैसे जर्मैनिक या रोमांस) यूरोप के भाषायी इतिहास को आकार देती रही हैं। इस दृष्टि से दोनों का संबंध “वंशगत एकता” और “भौगोलिक विविधता” — दोनों को प्रदर्शित करता है।
आर्य भाषाओं पर बाह्य प्रभाव
भारतीय भाषाओं का विकास केवल आंतरिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं था; इन पर समय-समय पर विदेशी भाषाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ा।
1. फारसी और अरबी प्रभाव
मुगल काल में जब भारत में फारसी शाही भाषा थी, तब फारसी और अरबी शब्द बड़ी मात्रा में हिन्दी और उर्दू में सम्मिलित हुए। विशेष रूप से उर्दू भाषा ने अरबी-फारसी से अपना बड़ा शब्द-भंडार ग्रहण किया। जैसे — इन्सान, किताब, ज़िन्दगी, अदालत, मोहब्बत आदि शब्द।
2. अंग्रेज़ी का प्रभाव
औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ी भाषा ने भारतीय आर्य भाषाओं को विशेष रूप से प्रभावित किया। अंग्रेज़ी शब्द शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश कर गए — जैसे कंप्यूटर, ट्रेन, स्टेशन, डॉक्टर, मोबाइल, रिपोर्ट आदि।
आज भी अंग्रेज़ी का प्रभाव जारी है, और यह ज्ञान-विज्ञान की वैश्विक भाषा के रूप में भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द-संवर्धन में योगदान दे रही है।
भाषा परिवार का भाषावैज्ञानिक वर्गीकरण
भारोपीय भाषा परिवार को प्रमुखतः निम्नलिखित शाखाओं में बाँटा गया है —
- भारतीय आर्य शाखा (Indo-Aryan Branch)
- ईरानी शाखा (Iranian Branch) – फ़ारसी, अवेस्ता
- यूनानी (Greek)
- लैटिन (Italic)
- जर्मनिक (Germanic) – अंग्रेज़ी, जर्मन, डच
- स्लाविक (Slavic) – रूसी, पोलिश
- सेल्टिक (Celtic)
- बाल्टिक (Baltic)
इनमें से भारतीय आर्य शाखा भारत की प्रमुख भाषाओं का समूह है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, साहित्य और संस्कृति को एक साझा सूत्र में बाँधा है।
संवैधानिक मान्यता और संरक्षण
भारत के संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनमें से अधिकांश इंडो–आर्यन भाषाएँ हैं — जैसे हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, उर्दू और गुजराती। भारत सरकार शिक्षा, मीडिया, प्रशासन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनके प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
इन भाषाओं के संरक्षण के लिए विभिन्न संस्थाएँ, अकादमियाँ और विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, जो इनके अध्ययन, शिक्षण और साहित्यिक प्रसार में योगदान दे रहे हैं।
दक्षिण एशियाई संस्कृति में इंडो–आर्यन भाषाओं की भूमिका
इंडो–आर्यन भाषाएँ दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। इनकी विविधता के बावजूद एक साझा भाषाई आत्मा विद्यमान है, जिसने भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका को सांस्कृतिक रूप से जोड़े रखा है।
भक्ति आंदोलन, लोककाव्य, सूफी साहित्य, आधुनिक राष्ट्रवाद और लोकगीत — सभी ने इन भाषाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। आज भी हिन्दी, बंगला, मराठी या उर्दू के साहित्य में उस एकता और साझा भाव की झलक मिलती है, जो भारतीय सभ्यता की आत्मा को दर्शाती है।
इंडो–आर्यन भाषा परिवार का वैश्विक परिप्रेक्ष्य
इंडो–आर्यन भाषा परिवार न केवल दक्षिण एशिया, बल्कि मध्य एशिया और विश्व के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का समूह है। भाषाविज्ञानियों का अनुमान है कि इस परिवार की 1000 से अधिक भाषाएँ और उपभाषाएँ अस्तित्व में हैं, और हर दशक में इनकी संख्या में कुछ वृद्धि होती रहती है। प्रवासी भारतीय समुदायों के कारण ये भाषाएँ ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम आदि देशों में भी बोली जाती हैं।
इनमें सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाएँ हैं — हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, उर्दू और गुजराती। हिन्दी और बांग्ला विश्व की दस सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल हैं। इन भाषाओं का न केवल जनसांख्यिकीय विस्तार विशाल है, बल्कि इनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा भी अत्यंत समृद्ध है। इन भाषाओं में आधुनिक साहित्य, नाटक, पत्रकारिता, सिनेमा और शिक्षा के विविध रूप फले-फूले हैं।
भारतीय आर्य भाषाओं का सांस्कृतिक योगदान
भारतीय आर्यभाषाएँ केवल संचार का माध्यम नहीं रहीं; इन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म, साहित्य और दर्शन को भी गहराई से प्रभावित किया है।
- संस्कृत ने वेद, उपनिषद, महाकाव्य और शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से विश्व को ज्ञान और दर्शन की धरोहर दी।
- पाली और प्राकृत ने बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार में भाषा का माध्यम बनकर समाज में नैतिकता और अहिंसा के संदेश फैलाए।
- हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू जैसी आधुनिक आर्यभाषाओं ने भक्ति, राष्ट्रवाद और जन-जागरण के युग में सांस्कृतिक एकता का कार्य किया।
इन भाषाओं के साहित्य ने भारत को एक गहन भावनात्मक और सांस्कृतिक बंधन में जोड़ा।
इंडो-आर्यन भाषाओं का वैश्विक महत्व
आज इंडो-आर्यन भाषाएँ केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। प्रवासी भारतीय समुदायों के कारण ये भाषाएँ ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम आदि देशों में भी बोली जाती हैं।
हिन्दी और बांग्ला विश्व की दस सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल हैं। अनुमानतः 1000 से अधिक इंडो-आर्यन भाषाएँ और उपभाषाएँ आज दक्षिण एशिया में प्रचलित हैं।
आधुनिक परिदृश्य और चुनौतियाँ
यद्यपि भारतीय आर्य भाषाएँ अत्यंत समृद्ध और व्यापक हैं, फिर भी इनके समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं —
- अंग्रेज़ी का अत्यधिक प्रभाव
- डिजिटल माध्यमों में स्थानीय भाषाओं की सीमित उपस्थिति
- शहरीकरण के कारण बोलियों का लुप्त होना
- भाषा शिक्षा में असंतुलन
इन चुनौतियों के समाधान के लिए शिक्षा, मीडिया और प्रशासन में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।
निष्कर्ष
भारतीय आर्य भाषा परिवार न केवल भारत की भाषाई विविधता का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के विकास का साक्षी भी है। संस्कृत से लेकर आधुनिक हिन्दी और बंगला तक की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज ने भाषा के माध्यम से निरंतर परिवर्तन, नवाचार और एकता को साधा है।
भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा ने मानवता को ज्ञान, साहित्य, दर्शन और संस्कृति की वह परंपरा दी है, जो आज भी विश्वभर में सम्मानित है। अतः आवश्यक है कि हम इन भाषाओं के संरक्षण, अध्ययन और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्न करें ताकि हमारी भाषाई धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवंत बनी रहे।
इन्हें भी देखें –
- मातृभाषा: परिभाषा, अर्थ, विशेषताएँ और दिवस – संस्कृति, पहचान और अभिव्यक्ति का आधार
- राष्ट्रभाषा : स्वरूप, अवधारणा, परिभाषा और महत्व
- राजभाषा : भारत की राजभाषा, राज्यों की राजभाषाएं, परिभाषा, महत्व और सूची
- गुजराती भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, दिवस, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, साहित्य और इतिहास
- कश्मीरी भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, वर्णमाला, शब्द, वाक्य और इतिहास
- पंजाबी भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, बोली क्षेत्र, वर्णमाला, शब्द, वाक्य और इतिहास
- सिंधी भाषा : उद्भव, विकास, लिपि, वर्णमाला, शब्द, वाक्य और भाषिक संरचना
- रीतिकाल के कवि और रचनाएँ