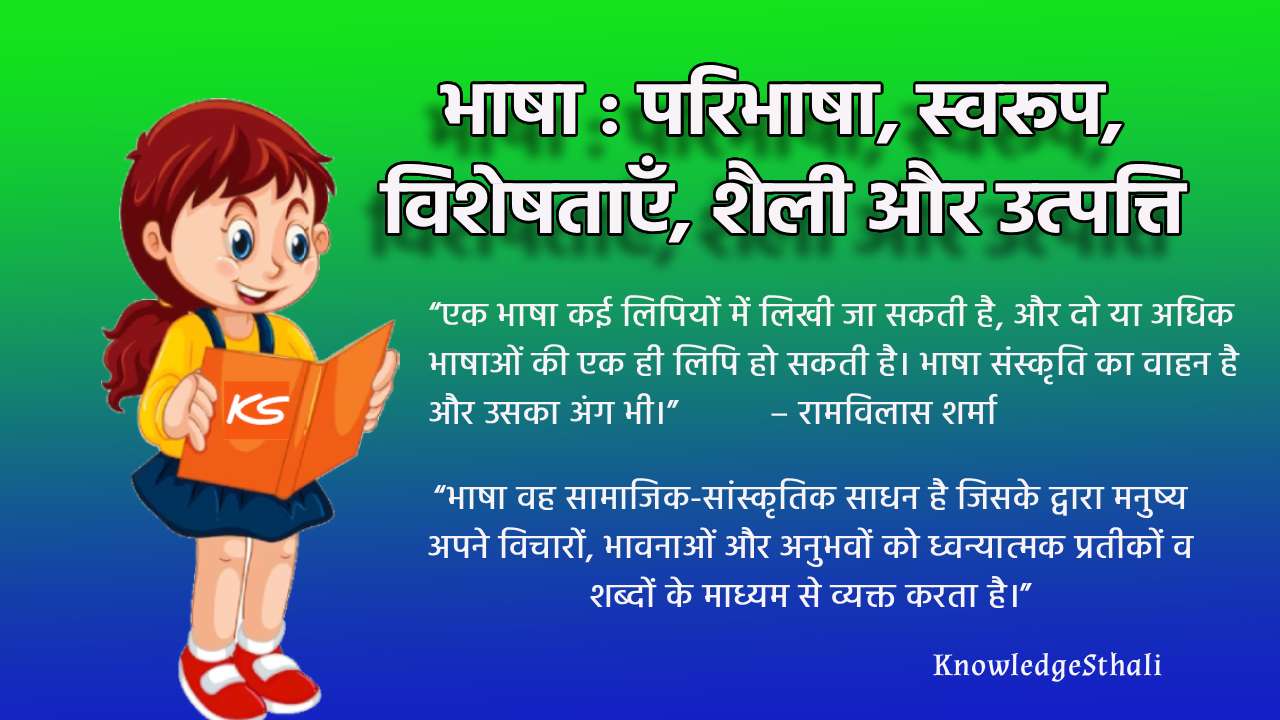मानव सभ्यता का मूल आधार भाषा है। यदि मनुष्य को विचारशील प्राणी कहा जाता है, तो यह केवल उसकी भाषागत क्षमता के कारण संभव हुआ है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मनोभावों, विचारों और अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। समाज, संस्कृति, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान का संवाहक होने के नाते भाषा का महत्व अद्वितीय है। वास्तव में, भाषा के बिना मानव-जीवन अधूरा है।
भाषा परंपरागत दृष्टि से केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि यह संस्कृति का संवाहक, विचारों का आधार और समाज की पहचान भी है। किसी भी राष्ट्र के लिए भाषा केवल बोलने का उपकरण नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व और विकास की आत्मा होती है।
भाषा की संकल्पना
भाषा का सबसे सामान्य अर्थ है – “मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह, जिनके द्वारा मन की बात दूसरों तक पहुँचाई जाती है।”
दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा, व्यक्त नाद की वह समष्टि है जिसकी सहायता से किसी समाज या समुदाय के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार व्यक्त करते हैं।
इस प्रकार भाषा को बोली, जबान और वाणी जैसे पर्यायों से भी समझा जा सकता है।
रामविलास शर्मा का कथन है –
“एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। भाषा संस्कृति का वाहन है और उसका अंग भी।”
भाषा की परिभाषा
“भाषा वह सामाजिक और सांस्कृतिक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को ध्वन्यात्मक प्रतीकों, शब्दों और वाक्यों के रूप में प्रकट करता है। यह न केवल संचार का साधन है, बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को दृढ़ करने, ज्ञान और संस्कृति को पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुँचाने तथा मानवीय चेतना को अभिव्यक्त करने का सबसे प्रभावी उपकरण भी है।”
संक्षिप्त परिभाषा
“भाषा वह सामाजिक-सांस्कृतिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को ध्वन्यात्मक प्रतीकों व शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है।”
विद्वानों द्वारा दी गयी भाषा की परिभाषाएँ
भाषा की परिभाषा प्राचीन काल से ही दी जाती रही है। अनेक दार्शनिकों और भाषाविदों ने अपनी दृष्टि से इसे समझाने का प्रयास किया।
- प्लेटो – “विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक बातचीत है, वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं।”
- स्वीट – “ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।”
- वेंद्रीय – “भाषा एक तरह का चिह्न है। चिह्न से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। इनमें श्रोत्रग्राह्य प्रतीक सर्वश्रेष्ठ हैं।”
- ब्लॉक तथा ट्रेगर – “भाषा यादृच्छिक भाषाई प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है।”
- स्त्रुत्वा – “भाषा यादृच्छिक भाषाई प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते हैं।”
इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भाषा न केवल ध्वनियों का संयोजन है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक क्रिया भी है।
भाषा का अर्थ और व्युत्पत्ति
‘भाषा’ शब्द संस्कृत की “भाष्” धातु से बना है, जिसका अर्थ है – बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए।
एक अन्य दृष्टिकोण से भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है –
“भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि-संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परंपरा विचारों का आदान-प्रदान करता है।”
इस कथन से भाषा की चार मुख्य विशेषताएँ सामने आती हैं –
- भाषा एक पद्धति है – यह सुसंगठित योजना या संघटन है, जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म आदि सुव्यवस्थित ढंग से आते हैं।
- भाषा संकेतात्मक है – ध्वनियाँ प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होती हैं और किसी वस्तु अथवा कार्य का बोध कराती हैं।
- भाषा वाचिक ध्वनि-संकेत है – मनुष्य अपनी वागिन्द्रियों से जो ध्वनि संकेत उच्चारित करता है, वही भाषा में आता है।
- भाषा यादृच्छिक संकेत है – किसी विशेष ध्वनि का विशेष अर्थ से दार्शनिक सम्बन्ध नहीं होता, बल्कि वह परंपरा और समाज की मान्यता पर आधारित होता है।
भाषा का स्वरूप
भाषा का स्वरूप बहुआयामी है। यह केवल ध्वनि का समूह नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति और समाज के बीच संचार स्थापित होता है।
भाषा के चार प्रमुख संयोजक तत्व माने गए हैं –
- प्रेषक (Sender) – जो संबोधित करता है।
- प्राप्तकर्ता (Receiver) – जिसे संबोधित किया जाता है।
- संकेतित वस्तु (Object) – जिस विषय पर संचार हो रहा है।
- प्रतीकात्मक संवाहक (Symbolic Medium) – ध्वन्यात्मक या लिखित रूप, जो संकेतित वस्तु की ओर संकेत करता है।
इस प्रकार भाषा का स्वरूप संवादात्मक और सामाजिक दोनों है।
भाषा की विशेषताएँ
- सामाजिकता – भाषा समाज में पनपती है। बिना समाज के भाषा अधूरी है।
- सांस्कृतिकता – भाषा संस्कृति की संवाहक है। प्रत्येक पीढ़ी अपने अनुभव भाषा के माध्यम से आगे बढ़ाती है।
- परंपरानुकूलता – भाषा के शब्द और ध्वनियाँ परंपरा से मान्य होती हैं।
- यादृच्छिकता – शब्दों का अर्थ परंपरा और सहमति से तय होता है, प्राकृतिक रूप से नहीं।
- गतिशीलता – भाषा समय के साथ बदलती रहती है।
- संगठनात्मकता – इसमें ध्वनि, शब्द और वाक्य सुसंगठित रूप से व्यवस्थित होते हैं।
भाषा और शैली
भाषा का विकास समाज के साथ-साथ होता है। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में भी उच्चारण, शब्द भंडार और वाक्य-विन्यास में भिन्नता देखने को मिलती है। यही भिन्नता भाषा की शैली कहलाती है।
भाषा की शैली व्यक्ति, क्षेत्र, वर्ग और परिस्थिति के आधार पर बदलती रहती है। यही कारण है कि एक ही भाषा की अनेक बोलियाँ और उपभाषाएँ विकसित होती हैं।
भाषा की उत्पत्ति : विवाद और सिद्धांत
भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न प्राचीनकाल से ही विद्वानों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है।
कुछ विद्वानों का मत है कि भाषा की उत्पत्ति पर चर्चा करना भाषा-विज्ञान का विषय ही नहीं है क्योंकि यह मात्र संभावनाओं पर आधारित है। वहीं दूसरी ओर अनेक भाषाविद मानते हैं कि भाषा का प्रारंभिक विकास भी भाषा-विज्ञान का अभिन्न अंग है।
भाषा-उत्पत्ति पर अब तक कोई सर्वमान्य सिद्धांत प्रस्तुत नहीं हो सका है, किन्तु कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं –
- ध्वन्यात्मक या अनुकृति सिद्धांत (Bow-Wow Theory) – भाषा की उत्पत्ति पशु-पक्षियों और प्रकृति की ध्वनियों की नकल से हुई।
- सहजोत्पत्ति सिद्धांत (Pooh-Pooh Theory) – भाषा की उत्पत्ति हर्ष, पीड़ा, आश्चर्य आदि भावनात्मक ध्वनियों से हुई।
- गान सिद्धांत (La-La Theory) – भाषा की उत्पत्ति गीत और संगीत की धुनों से हुई।
- सहकार सिद्धांत (Yo-He-Ho Theory) – भाषा की उत्पत्ति सामूहिक श्रम और कार्य करते समय निकली ध्वनियों से हुई।
- संकेत सिद्धांत (Gesture Theory) – भाषा का आरंभ संकेतों और मुद्राओं से हुआ, बाद में यह वाचिक रूप में विकसित हुई।
इन सभी मतों में वैज्ञानिक आधार की कमी है, अतः आज भी भाषा-उत्पत्ति विवादास्पद विषय बना हुआ है।
भाषा और समाज
भाषा केवल व्यक्तिगत साधन नहीं है। यह समाज की धरोहर है। भाषा के बिना समाज की कल्पना असंभव है।
- व्यक्ति के लिए भाषा विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन है।
- समाज के लिए भाषा आपसी सहयोग और संपर्क का माध्यम है।
- राष्ट्र के लिए भाषा एकता और संस्कृति की पहचान है।
भाषा का विकास
1. विश्व की भाषाएँ और उनकी विविधता
वर्तमान समय में संसार में हजारों भाषाएँ बोली जाती हैं। अधिकांश भाषाएँ केवल अपने-अपने भाषाभाषियों को ही समझ में आती हैं। व्यक्ति अपने समाज या देश की भाषा तो बचपन से ही सीख लेता है और उसमें दक्ष होता है, परंतु दूसरे देशों या समाजों की भाषाएँ उसके लिए कठिन होती हैं। यही कारण है कि भाषाओं की विविधता और भिन्नता मानव समाज की एक विशेष पहचान मानी जाती है।
2. भाषाओं का वर्गीकरण
भाषाविज्ञान के विद्वानों ने विश्व की भाषाओं को उनके स्वरूप और पारस्परिक साम्य के आधार पर कई वर्गों में बाँटा है। प्रमुख वर्गों में –
- आर्य (Indo-European)
- सेमेटिक (Semitic)
- हेमेटिक (Hamitic)
इन वर्गों की अलग-अलग शाखाएँ बनाई गईं और फिर उन शाखाओं के भी अनेक उपवर्ग निर्धारित किए गए। प्रत्येक वर्ग और उपवर्ग के अंतर्गत बड़ी-बड़ी भाषाओं के साथ उनकी उपभाषाएँ और बोलियाँ रखी गई हैं।
3. हिंदी और उसकी उपभाषाएँ
उदाहरण के लिए हिंदी भाषा, भाषाविज्ञान की दृष्टि से आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है। इसकी अनेक उपभाषाएँ और बोलियाँ हैं, जैसे –
- ब्रजभाषा
- अवधी
- बुंदेलखंडी
ये सभी हिंदी की उपशाखाएँ हैं। पास-पास बोली जाने वाली उपभाषाओं में पर्याप्त साम्य होता है, और उसी साम्य के आधार पर उनके वर्ग बनाए जाते हैं। यही बात बड़ी भाषाओं पर भी लागू होती है, जहाँ परस्पर साम्य कम होते हुए भी कुछ अंशों में विद्यमान रहता है।
4. भाषा का ऐतिहासिक विकास
संसार की अन्य सभी बातों की भाँति भाषा का भी निरंतर विकास होता रहा है। आदिम अवस्था के अव्यक्त नाद से लेकर आधुनिक भाषाओं तक यह क्रम लगातार जारी है।
भारतीय भाषाओं के विकास का क्रम इस प्रकार है –
- वैदिक भाषा → संस्कृत
- संस्कृत → प्राकृत
- प्राकृत → अपभ्रंश
- अपभ्रंश → आधुनिक भारतीय भाषाएँ
इस प्रकार भाषा समय के साथ रूपांतरित होती रही और नई-नई भाषाएँ अस्तित्व में आती गईं।
5. भाषा का महत्व और सामाजिक भूमिका
भाषा केवल बाहरी संचार का साधन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक अभिव्यक्ति का भी सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यह हमारी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संबंधों का आधार है। भाषा के बिना मनुष्य अपूर्ण है और अपने इतिहास व परंपरा से कट जाता है।
6. भाषा और लिपि का संबंध
सामान्यतः भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा और लिपि दोनों भाव-अभिव्यक्ति के अभिन्न पहलू हैं।
- एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है।
- कई भाषाएँ एक ही लिपि में भी लिखी जा सकती हैं।
उदाहरण –
- पंजाबी भाषा गुरूमुखी और शाहमुखी दोनों लिपियों में लिखी जाती है।
- हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली आदि सभी भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं।
भारतीय भाषाओं का विकास : कालक्रमिक सारणी
| काल/अवधि | भाषा का रूप | प्रमुख विशेषताएँ | उदाहरण/प्रयोग क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| वैदिक काल (1500 ई.पू. – 600 ई.पू.) | वैदिक भाषा | सर्वप्रथम साहित्यिक भाषा; वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदों की भाषा | ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद |
| उत्तर वैदिक से शास्त्रीय काल (600 ई.पू. – 200 ई.) | संस्कृत | व्याकरण-संहित भाषा; पाणिनि का व्याकरण; साहित्य और दर्शन की समृद्ध परंपरा | महाभारत, रामायण, कालिदास कृतियाँ |
| प्राकृत काल (200 ई. – 600 ई.) | प्राकृत भाषाएँ | बोलचाल की भाषाएँ; जनसाधारण की भाषा; जैन और बौद्ध साहित्य की भाषा | अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री |
| अपभ्रंश काल (600 ई. – 1200 ई.) | अपभ्रंश भाषाएँ | प्राकृत से विकसित रूप; आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच संक्रमणकालीन भाषा | “पउमचरिउ” (जैन काव्य) आदि |
| मध्यकाल से आधुनिक काल (1200 ई. से वर्तमान) | आधुनिक भारतीय भाषाएँ | क्षेत्रीय भाषाओं का विकास; साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रभाषाओं का निर्माण | हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया आदि |
👉 इस सारणी से स्पष्ट होता है कि वैदिक भाषा → संस्कृत → प्राकृत → अपभ्रंश → आधुनिक भारतीय भाषाएँ – यही भारतीय भाषाओं के विकास की मुख्य धारा रही है।
विश्व भाषाओं का वर्गीकरण
| क्रम | भाषा-परिवार (Language Family) | प्रमुख शाखाएँ | उदाहरण भाषाएँ |
|---|---|---|---|
| 1 | हिन्द-यूरोपीय / आर्य (Indo-European / Aryan) | 1. इंडो-ईरानी (Indo-Iranian) 2. यूरोपीय शाखा (Germanic, Romance, Slavic, Celtic, Greek) | हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी |
| 2 | सेमेटिक (Semitic) | 1. हिब्रू 2. अरबी 3. अम्हारिक | हिब्रू, अरबी, अम्हारिक (इथियोपिया) |
| 3 | हेमेटिक / अफ्रीकी (Hamitic / Afro-Asiatic) | 1. बर्बर 2. कूशिटिक 3. मिस्री (प्राचीन) | सोमाली, बर्बर भाषाएँ, कॉप्टिक (मिस्री) |
| 4 | चीनी-तिब्बती (Sino-Tibetan) | 1. चीनी 2. तिब्बती-बर्मी | मंदारिन, कैंटोनीज़, तिब्बती, बर्मी |
| 5 | द्रविड़ (Dravidian) | 1. दक्षिणी 2. मध्य | तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम |
| 6 | तुर्की-मंगोल (Turkic-Mongolic) | 1. तुर्की 2. मंगोल | तुर्की, उज़्बेक, मंगोलियाई |
| 7 | फिनो-उग्रिक (Finno-Ugric / Uralic) | 1. फिनिश 2. हंगेरियन | फिनिश, हंगेरियन, एस्टोनियन |
| 8 | ऑस्ट्रो-एशियाई (Austro-Asiatic) | 1. ख्मेर 2. मोन-खमेर | ख्मेर (कंबोडिया), वियतनामी |
| 9 | ऑस्ट्रो-नेशियन (Austronesian) | 1. मलय-पोलीनेशियन | मलय, इंडोनेशियाई, तागालोग |
| 10 | एस्किमो-एल्युट (Eskimo-Aleut) | 1. एस्किमो 2. एल्युट | इनुइट भाषाएँ |
| 11 | जापानी-कोरियाई (Japanese-Korean) | स्वतंत्र परिवार | जापानी, कोरियाई |
भाषा के प्रकार (भेद)
भाषा अपने प्रयोग और रूपों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। मुख्यतः भाषा के रूप निम्नलिखित हैं –
- मौखिक भाषा
- लिखित भाषा
- सांकेतिक भाषा
- मानक भाषा
- संपर्क भाषा
- नेत्रहीनों की भाषा (ब्रेल पद्धति)
1. मौखिक भाषा
भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार और भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं।
- उदाहरण: किसी से आमने-सामने बातचीत करना या फोन पर बात करना।
- यह सहज रूप से सीखी जाती है। जैसे- हम अपनी मातृभाषा को परिवार और समाज से अनुकरण द्वारा स्वयं सीख जाते हैं।
2. लिखित भाषा
जब मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं।
- उदाहरण: पत्र, लेख, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार इत्यादि।
- लिखित भाषा सीखने के लिए विशेष अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है।
3. सांकेतिक भाषा
सांकेतिक भाषा वह भाषा है, जिसमें विचारों को बोलने की बजाय संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसमें हाथ के आकार, विन्यास, संचालन, शरीर की गतियाँ और चेहरे के हाव-भाव का प्रयोग होता है।
- उदाहरण: छोटा बच्चा अपनी माँ को रोकर या इशारों से अपनी भूख या इच्छा प्रकट करता है।
- इसका प्रयोग मुख्यतः शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (जैसे- बधिर और मूक) के लिए किया जाता है।
4. मानक भाषा
भाषा का स्थिर और सुनिश्चित रूप मानक भाषा कहलाता है। यह शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार और व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण और उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है।
- मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं।
- पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन प्रायः इसी रूप में होता है।
- उदाहरण: हिन्दी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि।
5. सम्पर्क भाषा
विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी जब एक विशिष्ट भाषा को लोगों के बीच संवाद और संचार का माध्यम बनाया जाता है, तो वह सम्पर्क भाषा कहलाती है।
- आज भारत में हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकृत है।
6. नेत्रहीनों की भाषा (ब्रेल पद्धति)
दृष्टिबाधित (नेत्रहीन) व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई भाषा को ब्रेल भाषा कहते हैं।
- इसका आविष्कार 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया।
- ब्रेल एक विशेष लिपि है, जिसे छूकर पढ़ा और लिखा जाता है।
- यह प्रणाली आज पूरे विश्व में नेत्रहीनों की शिक्षा और संचार का प्रमुख साधन है।
भाषा के अंग और उसकी प्रक्रिया
भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, बल्कि मनुष्य को सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर पर जोड़ने वाली कड़ी भी है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने अनुभव, भावनाएँ, ज्ञान और चिंतन को दूसरों तक पहुँचा सकता है। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके अंगों और प्रयोग की प्रक्रिया को जानना अत्यंत आवश्यक है।
भाषा के मुख्य पाँच अंग माने जाते हैं— ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। इसी प्रकार, भाषा के प्रयोग की प्रक्रिया पाँच चरणों— सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना और लिखना— में संपन्न होती है। आइए, इनका विस्तृत अध्ययन करें।
भाषा के अंग
1. ध्वनि
हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि ही भाषा का आधार है। यह मौखिक भाषा में प्रयुक्त होती है और भाषा का मूल स्वरूप ध्वनि के माध्यम से ही बनता है।
- उदाहरण: जब हम “अ”, “क” या “म” का उच्चारण करते हैं तो ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं।
2. वर्ण
वह मूल ध्वनि जिसे और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाती है। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है।
- उदाहरण: अ, क्, भ्, म्, त् आदि।
वर्ण ही मिलकर शब्द बनाते हैं।
3. शब्द
वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। शब्द ही भाषा को जीवंत बनाते हैं और इनके माध्यम से ही हम अपने विचार व्यक्त करते हैं।
- उदाहरण:
- क् + अ + म् + अ + ल् + अ = कमल
- भ् + आ + ष् + आ = भाषा
4. वाक्य
सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य ही भाषा की सबसे संगठित इकाई है जिसके द्वारा विचार पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं।
- उदाहरण: कमल हिन्दी भाषा पढ़ रहा है।
यदि शब्दों का क्रम बिगाड़ दिया जाए, जैसे— “हिन्दी है रहा कमल पढ़ भाषा” तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता और वह वाक्य नहीं कहलाता।
5. लिपि
मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है।
- उदाहरण: हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है।
भाषा की प्रक्रिया
भाषा एक संप्रेषण (Communication) का माध्यम है। इसके प्रयोग की प्रक्रिया पाँच मुख्य चरणों में संपन्न होती है—
1. सुनना (Listening)
भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम किसी की बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो संदेश अधूरा रह जाएगा।
- उदाहरण: यदि शिक्षक कहे कि “कल आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाने हैं” और छात्र उसे सुने ही न, तो वह कार्य पूरा नहीं कर पाएगा।
2. देखना (Seeing)
संचार में देखना भी उतना ही आवश्यक है जितना सुनना। कई बार संदेश ध्वनि के साथ-साथ दृश्य के माध्यम से भी संप्रेषित होता है।
- उदाहरण: यदि गणित का प्रश्न हल करने की प्रक्रिया शिक्षक बोर्ड पर समझाए तो विद्यार्थियों को बोर्ड पर ध्यान देना आवश्यक है।
आज इंटरनेट और ऑडियो-विज़ुअल माध्यम (जैसे YouTube) इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं।
3. बोलना (Speaking)
भाषा के प्रभावी संप्रेषण के लिए शुद्ध बोलना आवश्यक है। बोलना मनुष्य द्वारा सीखा जाने वाला पहला कौशल है।
- व्याकरण का ज्ञान बोलने के लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु सही संप्रेषण के लिए यह उपयोगी है।
- सही बोलने की आदत ही सही लिखने और पढ़ने की नींव रखती है।
4. पढ़ना (Reading)
किसी भाषा को पढ़ने के लिए उसके वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है।
- व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाता है।
- पढ़ने से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और भाषा पर पकड़ मजबूत होती है।
5. लिखना (Writing)
लिखना भाषा की सबसे जटिल प्रक्रिया है। इसमें भाषा की सम्पूर्ण संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है।
- सही लेखन के लिए वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण की समझ होना अनिवार्य है।
- व्याकरण के बिना शुद्ध लेखन संभव नहीं है।
भाषा के अंग और उसकी प्रक्रिया को समझना किसी भी भाषा की गहराई को जानने के लिए आवश्यक है। ध्वनि से लेकर लिपि तक की संरचना भाषा का स्वरूप बनाती है और सुनने से लेकर लिखने तक की प्रक्रिया भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाती है।
मनुष्य के संचार, शिक्षा और ज्ञान के विस्तार में भाषा की यही भूमिका उसे अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाती है।
बोली, विभाषा और भाषा
भाषा के स्वरूप और उसके विविध रूपों में बोली, विभाषा और भाषा के बीच स्पष्ट अंतर करना कठिन है, क्योंकि इनका मुख्य भेद प्रायः इनके व्यवहार-क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करता है। एक ही भाषा के विभिन्न रूप समाज में दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से इन्हें तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है— बोली, विभाषा और भाषा (परिनिष्ठित या आदर्श भाषा)।
1. बोली
बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका सम्बन्ध किसी ग्राम या मंडल, अर्थात सीमित क्षेत्र से होता है।
- इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल की रहती है।
- देशज और घरेलू शब्दावली का बाहुल्य पाया जाता है।
- लहजा (उच्चारण-शैली) कुछ दूरी पर बदल जाता है।
- यह सामान्यतः लिपिबद्ध नहीं होती, इसलिए साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है।
- व्याकरणिक दृष्टि से इसमें विसंगतियाँ मिलती हैं।
उदाहरण: कन्नौजी, कुमाउनी, मेवाती आदि।
2. विभाषा
विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है।
- एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती हैं।
- विभाषा में साहित्यिक रचनाएँ भी मिलती हैं।
- विभाषा को उपभाषा भी कहा जाता है।
उदाहरण: ब्रज और अवध।
3. भाषा
भाषा, विभाषा का विकसित रूप होती है। इसे परिनिष्ठित या आदर्श भाषा भी कहा जाता है।
- भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और इसे राष्ट्र-भाषा या टकसाली-भाषा भी कहा जाता है।
- इसमें साहित्य की प्रचुरता और महत्ता होती है।
- यह सुव्यवस्थित व्याकरण और समृद्ध शब्दावली से सम्पन्न होती है।
- भाषा का प्रयोग साहित्य के साथ-साथ राजकार्य में भी होता है।
उदाहरण: हिन्दी, अंग्रेज़ी।
बोली और भाषा में अंतर
- बोली का क्षेत्र कुछ जिलों या ग्रामों तक सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है।
- बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और विकसित नहीं होती, जबकि भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप होती है।
- बोली में साहित्य लेखन क्षेत्रीय स्तर तक सीमित होता है, जबकि भाषा में साहित्य की प्रचुरता होती है।
- बोली का प्रयोग राजकार्यों में नहीं होता, जबकि भाषा का प्रयोग राजकार्य में भी होता है।
- बोली का व्याकरण सीमित या अस्पष्ट होता है, जबकि भाषा का व्याकरण सुव्यवस्थित एवं पूर्ण होता है।
भाषा और विभाषा में अंतर
- भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि विभाषा का क्षेत्र सीमित होता है।
- भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप होती है, जबकि विभाषा बोली का अर्ध-विकसित रूप होती है।
- भाषा में साहित्य की प्रचुरता और महत्ता होती है, जबकि विभाषा में साहित्य तो मिलता है पर उसे उतनी महत्ता नहीं मिलती।
- भाषा का प्रयोग राजकार्य में भी होता है, जबकि विभाषा केवल बोलचाल और साहित्य तक सीमित रहती है।
बोली, विभाषा और भाषा | तुलनात्मक सारणी
| विशेषताएँ | बोली | विभाषा | भाषा (परिनिष्ठित/आदर्श) |
|---|---|---|---|
| क्षेत्र | ग्राम या मंडल (सीमित) | प्रांत/उप-प्रांत (मध्यम) | व्यापक, राष्ट्रीय स्तर |
| विकास स्तर | सीमित, स्थानीय | अर्ध विकसित | पूर्ण विकसित |
| साहित्य | क्षेत्रीय स्तर तक | मिलता है पर महत्ता कम | प्रचुर और महत्वपूर्ण |
| राजकार्य में प्रयोग | नहीं | केवल साहित्य और बोलचाल तक | हाँ, राजकार्य में भी |
| व्याकरण | अस्पष्ट या सीमित | आंशिक व्यवस्थित | सुव्यवस्थित और पूर्ण |
| उदाहरण | कन्नौजी, कुमाउनी, मेवाती | ब्रज, अवध | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
| लिपिबद्धता | नहीं | कभी-कभी | हाँ, व्यवस्थित रूप में |
| उच्चारण/लहजा | क्षेत्र विशेष में बदलता रहता है | स्थानीय भेदों के आधार पर | स्थिर और मानकीकृत |
राज्यभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा
भाषा के विभिन्न रूपों और उनके सामाजिक-संवैधानिक महत्व को समझने के लिए राज्यभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बीच अंतर जानना आवश्यक है।
1. राज्यभाषा
किसी राज्य की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राज्यभाषा कहते हैं।
- यह भाषा सम्पूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन-समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है।
- प्रशासनिक दृष्टि से पूरे राज्य में इसका महत्त्व समान रूप से होता है।
2. राजभाषा
भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएँ राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई हैं।
- राज्य की विधानसभाएँ बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को राजभाषा घोषित कर सकती हैं।
- उदाहरण: भारत में हिन्दी और अंग्रेज़ी भारत सरकार की राजभाषा हैं। राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषाएँ भी होती हैं।
3. राष्ट्रभाषा
राष्ट्रभाषा सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है।
- यह वह भाषा होती है जिसे राष्ट्र के अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं।
- प्राय: राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा भी होती है।
- राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता, गौरव और अस्मिता का प्रतीक होती है।
- महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को “राष्ट्र की आत्मा” कहा है।
- एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है; उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी अमेरिका, इंग्लैण्ड और कनाडा की राष्ट्रभाषा है।
- संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया है, किन्तु इसकी व्यापकता के कारण इसे राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है।
4. मातृभाषा
मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे व्यक्ति जन्म लेने के बाद सबसे पहले सीखता है।
- यह किसी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान होती है।
- मातृभाषा में प्रायः क्षेत्रीय बोलियाँ शामिल होती हैं।
- उदाहरण: कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, मालावी आदि।
राज्यभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा | तुलनात्मक सारणी
| विशेषताएँ | राज्यभाषा | राजभाषा | राष्ट्रभाषा | मातृभाषा |
|---|---|---|---|---|
| परिभाषा | किसी राज्य की सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा | संविधान द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अपनाई गई भाषा | सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा | जन्म के समय व्यक्ति द्वारा सबसे पहले सीखी जाने वाली भाषा |
| क्षेत्र | राज्य स्तर | राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश स्तर | राष्ट्रीय स्तर | व्यक्ति विशेष का परिवार और स्थानीय क्षेत्र |
| प्रयोग | प्रशासनिक कार्यों में | प्रशासन और राज्य कार्यों में | राष्ट्रव्यापी संचार और गौरव का प्रतीक | व्यक्तिगत और पारिवारिक संचार में |
| साहित्य और विकास | क्षेत्रीय स्तर तक | साहित्य और प्रशासनिक उपयोग | व्यापक साहित्य और राष्ट्रीय महत्ता | क्षेत्रीय बोलियों और पारंपरिक रूपों में |
| उदाहरण | तमिल (तमिलनाडु), कन्नड़ (कर्नाटक) | हिन्दी (राज्य/केंद्र), अंग्रेज़ी | हिन्दी, अंग्रेज़ी (भारत) | कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, मालावी |
| व्यापकता | सम्पूर्ण राज्य में | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में | सम्पूर्ण राष्ट्र में | परिवार और स्थानीय समाज तक |
| राजकार्य में उपयोग | हाँ | हाँ | प्राय: हाँ | नहीं |
| गौरव और प्रतीक | क्षेत्रीय महत्व | प्रशासनिक महत्त्व | राष्ट्रीय गौरव और अस्मिता का प्रतीक | व्यक्तिगत/सामाजिक पहचान का प्रतीक |
प्रायः देखा गया है कि विभिन्न विभाषाओं में से कोई एक विभाषा अपने गुण-गौरव, साहित्यिक अभिवृद्धि और जन-सामान्य में प्रचलन के आधार पर राजभाषा या राज्यभाषा के रूप में चुन ली जाती है। यही भाषा आगे चलकर समाज और राष्ट्र की पहचान बनती है।
विश्व की भाषाएँ
विश्व में भाषाओं की विविधता अद्भुत है। लगभग 6800 से अधिक भाषाएँ हैं, जिनमें से लगभग 40% भाषाओं को एक हजार से भी कम लोग बोलते हैं। इसका अर्थ है कि कई भाषाएँ अत्यंत सीमित समूहों द्वारा बोली जाती हैं।
प्रमुख तथ्य
- संख्या और व्यापकता
- दुनिया में लगभग 23 भाषाएँ प्रमुख हैं, जो वैश्विक आबादी का आधा हिस्सा समेटती हैं।
- भारत में लगभग 600 भाषाएँ बोली जाती हैं।
- देश विशेष की भाषाएँ
- अमेरिका की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है।
- पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) में विश्व की सबसे अधिक भाषाएँ हैं— 840 से अधिक, जिनमें से 40 मुख्य भाषाएँ हैं।
- प्राचीन और ऐतिहासिक भाषाएँ
- सुमेरियन भाषा 3300 ई०पू० की लिखित भाषा है और इसे सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में गिना जाता है।
- बाइबिल को 683 भाषाओं में अनुवादित किया गया और इसके भागों को 3000 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया। मूल रूप से यह हिब्रू, अरामी और कोइन ग्रीक में लिखी गई थी।
भाषाओं के रोचक तथ्य
- फ्रेंच को दुनिया में ‘प्यार की भाषा’ कहा जाता है।
- रूसी को ‘युद्ध की भाषा’ कहा जाता है।
- पापुआन (Rotokas) भाषा में सबसे कम वर्ण— 11— पाए जाते हैं।
- कम्बोडियन भाषा में सबसे अधिक वर्ण— 73 से अधिक— हैं।
- चीन की मंदारिन भाषा में वर्णों की जगह प्रतीकों (symbols) का प्रयोग होता है। इसे दुनिया की सबसे कठिन भाषा माना जाता है। इसमें लगभग 9000 प्रतीक हैं, जिनमें से 3000 का ज्ञान अखबार पढ़ने के लिए आवश्यक है।
- छापाखाने या प्रिंटिंग में प्रयुक्त पहली भाषा जर्मन थी।
अंग्रेजी का वैश्विक प्रभाव
- अंग्रेजी विश्व की सबसे प्रभावी भाषा है, लेकिन यह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है।
- इंटरनेट की दुनिया में अंग्रेजी और फ्रेंच सबसे अग्रणी हैं।
- कई देशों ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया है।
- आने वाले दशकों में अंग्रेजी दुनिया की अधिकांश भाषाओं पर प्रभुत्व स्थापित कर सकती है।
- उदाहरण: अफ्रीका में अंग्रेजी प्रथम भाषा बन गई है; नाइजीरिया में लगभग 9 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि ब्रिटेन में 6 करोड़।
- अमेरिका में अंग्रेजी के 24 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं।
विश्व की प्रमुख भाषाएँ और उनकी लिपियाँ
विश्व में भाषाओं की विविधता अत्यंत व्यापक है। लगभग 6800 भाषाएँ हैं, जिनमें से कुछ भाषाएँ अत्यधिक प्रभावशाली हैं और बहुत बड़ी आबादी बोलती है। नीचे विश्व विश्व की प्रमुख भाषाएँ, भाषा परिवार, बोलने वालों की संख्या, लिपि तथा उदाहरण को एक सारणी में दिया गया है –
| क्रम | भाषा (Language) | भाषा परिवार (Family) | वक्ता (Speakers) | लिपि (Script) | उदाहरण (Example) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंग्रेजी | इंडो-यूरोपियन | 145.2 करोड़ | रोमन | The boys are playing. |
| 2 | मंदारिन (मानक चीनी) | सिनो-तिब्बतीयन | 111.8 करोड़ | प्रतीक | 孩子们在玩耍। |
| 3 | हिन्दी | इंडो-यूरोपियन | 60.2 करोड़ | देवनागरी | बच्चे खेल रहे हैं। |
| 4 | स्पैनिश | इंडो-यूरोपियन | 54.8 करोड़ | रोमन | Los chicos están jugando. |
| 5 | फ्रेंच | इंडो-यूरोपियन | 27.41 करोड़ | रोमन | Les garçons jouent. |
| 6 | अरबी (मानक) | अफ्रीकी-एशियाई | 27.4 करोड़ | फ़ारसी/अरबी | الأولاد يلعبون. |
| 7 | बंगाली | इंडो-यूरोपियन | 27.27 करोड़ | बंगाली | ছেলেরা খেলছে। |
| 8 | रूसी | इंडो-यूरोपियन | 25.82 करोड़ | रूसी | Мальчики играют. |
| 9 | पुर्तगाली | इंडो-यूरोपियन | 25.77 करोड़ | रोमन | Os meninos estão brincando. |
| 10 | उर्दू | इंडो-यूरोपियन | 23.13 करोड़ | फ़ारसी/उर्दू | لڑکے کھیل رہے ہیں۔ |
| 11 | इंडोनेशियन | ऑस्ट्रोनेशियाई | 19.9 करोड़ | रोमन | Anak-anak sedang bermain. |
| 12 | जर्मन | इंडो-यूरोपियन | 13.46 करोड़ | रोमन | Die Jungen spielen. |
| 13 | जापानीज़ | जपोनिक | 12.54 करोड़ | कैनजी/हिरागाना/काताकाना | 子供たちは遊んでいる。 |
| 14 | नाइजीरियाई पिजिन | अंग्रेज़ी क्रियोल | 12.07 करोड़ | रोमन | Di pikin dem dey play. |
| 15 | मराठी | इंडो-यूरोपियन | 9.91 करोड़ | देवनागरी | मुले खेळत आहेत। |
| 16 | तेलुगु | द्रविड़ | 9.57 करोड़ | तेलुगु | పిల్లలు ఆడుతున్నారు. |
| 17 | तुर्की | तुर्की | 8.81 करोड़ | रोमन | Çocuklar oynuyor. |
| 18 | तमिल | द्रविड़ | 8.64 करोड़ | तमिल | பிள்ளைகள் விளையாடுகிறார்கள். |
| 19 | यू चीनी | सिनो-तिब्बतीयन | 8.56 करोड़ | प्रतीक | 孩子们在玩。 |
| 20 | वियतनामी | ऑस्ट्रोएशियाटिक | 8.53 करोड़ | रोमन | Các em đang chơi. |
| 21 | तागालोग | ऑस्ट्रोनेशियन | 8.23 करोड़ | रोमन | Ang mga bata ay naglalaro. |
| 22 | वू चीनी | सिनो-तिब्बतीयन | 8.18 करोड़ | प्रतीक | 小囝仔在玩。 |
| 23 | कोरीयन | कोरीयन | 8.17 करोड़ | हांगुल | 아이들이 놀고 있어요. |
| 24 | ईरानी पर्शियन | इंडो-यूरोपियन | 7.74 करोड़ | फ़ारसी | بچهها در حال بازی هستند. |
| 25 | हौसा | अफ्रीकी-एशियाई | 7.71 करोड़ | रोमन | Yara suna wasa. |
| 26 | अरबी (मिश्र) | अफ्रीकी-एशियाई | 7.48 करोड़ | फ़ारसी/अरबी | الأولاد يلعبون. |
| 27 | स्वाहिली | नाइजर-कांगो | 7.14 करोड़ | रोमन | Watoto wanacheza. |
| 28 | जावानीज़ | ऑस्ट्रोनेशियन | 6.83 करोड़ | रोमन | Bocah-bocah lagi dolanan. |
| 29 | इटालियन | इंडो-यूरोपियन | 6.79 करोड़ | रोमन | I ragazzi stanno giocando. |
| 30 | पश्चिमी पंजाबी | इंडो-यूरोपियन | 6.64 करोड़ | गुरमुखी/फ़ारसी | بچے کھیل رہے ہیں۔ |
नोट: यह चार्ट विश्व की प्रमुख भाषाओं और उनके बोलने वालों की संख्या को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। प्रत्येक भाषा की लिपि उसकी मूल लिपि है, लेकिन भाषाओं को अन्य लिपियों में भी लिखा जा सकता है।
विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएँ
1. अंग्रेजी की प्रमुखता
अंग्रेजी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें देशी और गैर-देशी दोनों तरह के वक्ता शामिल हैं। इसे लगभग 1.4 बिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है।
मुख्य विशेषताएँ:
- अंग्रेजी वैश्विक व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और यात्रा में व्यापक रूप से इस्तेमाल होती है।
- यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुकी है।
- अंग्रेजी 165 से अधिक देशों में फैली हुई है और 57 देशों में आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है।
2. मंदारिन चीनी की प्रमुखता
यदि केवल उन लोगों की संख्या गिनी जाए जो किसी भाषा को अपनी पहली भाषा (मूल वक्ता) के रूप में बोलते हैं, तो मंदारिन चीनी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है।
मुख्य विशेषताएँ:
- यह चीन में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
- मंदारिन चीनी के मूल वक्ताओं की संख्या अंग्रेजी से अधिक है।
- यह भाषा सिनो-तिब्बतीयन भाषा परिवार से संबंधित है और इसकी लिपि Chinese Characters (प्रतीक) है।
3. हिंदी की प्रमुखता
हिंदी दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है और इसे लगभग 60.2 करोड़ लोग बोलते हैं। यह इंडो-यूरोपियन भाषा परिवार की सदस्य है और इसकी लिपि देवनागरी है।
मुख्य विशेषताएँ:
- हिंदी भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है।
- यह भारत की राज्यभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
- हिंदी में साहित्य, मीडिया और शैक्षणिक सामग्री का समृद्ध भंडार मौजूद है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है, विशेषकर भारत में प्रवास करने वाले लोगों और सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम से।
- उदाहरण वाक्य: “बच्चे खेल रहे हैं।”
तुलनात्मक दृष्टि: अंग्रेजी, मंदारिन चीनी और हिंदी
| भाषा | कुल वक्ता | मूल वक्ता | भाषा परिवार | लिपि | वैश्विक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी | 1.4 बिलियन | ~3.8 करोड़ | इंडो-यूरोपियन | रोमन | अंतरराष्ट्रीय भाषा, 57 देशों में आधिकारिक |
| मंदारिन चीनी | ~11.18 करोड़ | सबसे अधिक मूल वक्ता | सिनो-तिब्बतीयन | प्रतीक | चीन में प्रमुख, दुनिया की सबसे बड़ी मूल भाषा |
| हिंदी | 60.2 करोड़ | ~60.2 करोड़ | इंडो-यूरोपियन | देवनागरी | भारत में व्यापक, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रमुखता |
निष्कर्ष
भाषा मानव जीवन की अनिवार्यता है। यह विचारों की वाहक, संस्कृति की संवाहक और समाज की आत्मा है। यद्यपि भाषा-उत्पत्ति पर सर्वसम्मत सिद्धांत उपलब्ध नहीं है, किन्तु यह निश्चित है कि भाषा ने ही मानव को मानव बनाया।
भाषा के बिना न साहित्य संभव है, न संस्कृति, न ही सभ्यता। यही कारण है कि विश्व के सभी विद्वान भाषा को मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं।
इन्हें भी देखें –
- पदबन्ध (Phrase) | परिभाषा, भेद एवं उदाहरण
- शब्द किसे कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द
- सवा सेर गेंहूँ | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- नागपूजा | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- बूढ़ी काकी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह : अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलन्त | परिभाषा, प्रयोग एवं महत्व
- हिंदी वर्णमाला में व्यंजन : परिभाषा, प्रकार और भेद
- राज्यों का बढ़ता सार्वजनिक ऋण : एक गंभीर चुनौती
- पाक–सऊदी रक्षा समझौता: पश्चिम एशिया की बदलती भू–राजनीति
- भारतीय संसद | लोक सभा और राज्य सभा | राज्यों में सीटें
- भारत में महारत्न कंपनियों की सूची