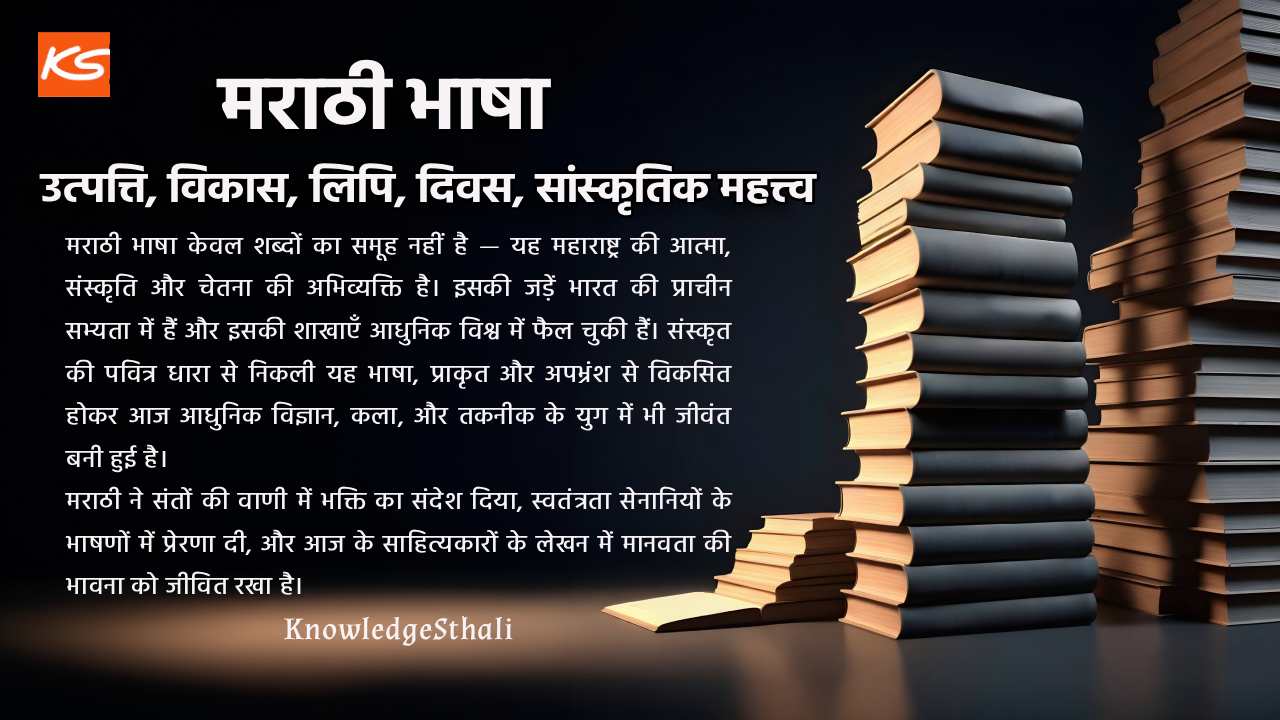भारत की भाषाई विविधता विश्व में अद्वितीय है। यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और हजारों बोलियाँ सह-अस्तित्व में हैं, जिनमें प्रत्येक भाषा अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक विकास और साहित्यिक विरासत को संजोए हुए है। इन्हीं में से एक है मराठी भाषा, जो न केवल महाराष्ट्र की आत्मा है बल्कि भारत की सांस्कृतिक धारा की एक जीवंत कड़ी भी है।
मराठी भाषा का इतिहास लगभग 2300 वर्षों पुराना माना जाता है। यह आर्य भाषा परिवार की एक प्रमुख शाखा — इंडो-आर्यन (Indo-Aryan) — से संबंधित है। वर्तमान में लगभग 8.3 करोड़ लोग मराठी भाषा बोलते हैं, जिससे यह भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनती है, हिंदी और बंगाली के बाद। यह महाराष्ट्र और गोवा की राजभाषा है, और भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल है।
मराठी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र की सामाजिक चेतना, लोकसंस्कृति, साहित्यिक परंपरा और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक भी है। आइए इस भाषा की उत्पत्ति, विकास, प्रसार, बोलियों, साहित्य और वैश्विक उपस्थिति पर विस्तार से दृष्टि डालें।
मराठी भाषा का परिचय
| भाषा | मराठी (Marathi) |
|---|---|
| लिपि | देवनागरी (प्रचलित), मोडी लिपी (ऐतिहासिक) |
| बोली क्षेत्र | महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ |
| वक्ता | लगभग 8.3 करोड़ |
| भाषा परिवार | आर्य भाषा परिवार (इंडो-आर्यन / भारोपीय) |
| राजभाषा | महाराष्ट्र और गोवा |
| राजभाषा दिवस | 1 मई |
| भाषा गौरव दिवस | 27 फरवरी |
मराठी भाषा आज के समय में न केवल भारत के भीतर बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। यह भाषा अपनी सांस्कृतिक गहराई, सरलता, और साहित्यिक परंपरा के लिए जानी जाती है।
मराठी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
मराठी भाषा की जड़ें संस्कृत में हैं। ऐसा माना जाता है कि यह भाषा प्राचीन महाराष्ट्र प्रदेश में बोली जाने वाली किसी संस्कृत-प्राकृत जनभाषा से विकसित हुई।
मराठी का विकास क्रम इस प्रकार से रहा —
संस्कृत → प्राकृत → अपभ्रंश → मराठी
मराठी भाषा के सबसे पुराने लिखित साक्ष्य 9वीं शताब्दी में मिलते हैं। सबसे प्राचीन मराठी शिलालेख 890 ईस्वी का बताया जाता है। 13वीं–14वीं शताब्दी के बीच मराठी ने स्वतंत्र रूप में एक परिपक्व भाषा का रूप ले लिया। इसी काल में मराठी में धार्मिक और भक्ति साहित्य की रचना शुरू हुई, जिसने इसकी लोकप्रियता को जनमानस तक पहुँचाया।
मराठी भाषा के विकास के प्रमुख चरण
मराठी भाषा के विकास को सामान्यतः तीन ऐतिहासिक चरणों में बाँटा जाता है—
(क) पुरानी मराठी (800–1600 ईस्वी)
यह मराठी भाषा का प्रारंभिक चरण था। इस अवधि में मराठी, संस्कृत और प्राकृत से विकसित होकर एक स्वतंत्र रूप लेने लगी थी। धार्मिक, दार्शनिक और राजकीय अभिलेखों में इसका प्रयोग होने लगा।
इस काल में मराठी का उपयोग मुख्यतः धार्मिक साहित्य, संत वाणी, और शिलालेखों में हुआ। संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई आदि ने इस भाषा को आध्यात्मिक गहराई दी। ज्ञानेश्वर की ‘ज्ञानेश्वरी’, जो भगवद्गीता का मराठी भावानुवाद है, इस काल की अमर कृति है।
(ख) मध्यकालीन मराठी (1600–1800 ईस्वी)
यह मराठी साहित्य के उत्कर्ष का काल था। भाषा अब अधिक व्यवस्थित और साहित्यिक रूप ले चुकी थी। इस युग में मराठी में भक्ति, नीति, वीररस और लोककथाओं पर आधारित ग्रंथों की भरमार हुई।
छत्रपति शिवाजी महाराज के समय मराठी राजकाज की भाषा बनी और प्रशासनिक स्तर पर प्रतिष्ठित हुई। इसी काल में मोडी लिपी का प्रचलन हुआ, जो राजकीय लेखन में व्यापक रूप से प्रयुक्त थी।
संत तुकाराम, एकनाथ, रामदास स्वामी जैसे संतों ने इस काल में मराठी साहित्य को ऊँचाइयाँ दीं। उनकी भाषा में जनभाषा का सौंदर्य और भक्ति की सहजता दोनों ही दृष्टिगोचर होती हैं।
(ग) आधुनिक मराठी (1800–वर्तमान)
औपनिवेशिक काल में शिक्षा और मुद्रण के प्रसार से मराठी भाषा का पुनर्जागरण हुआ। इस युग में देवनागरी लिपि का प्रयोग बढ़ा और मोडी लिपि धीरे-धीरे अप्रचलित होने लगी।
समाज-सुधार आंदोलनों, प्रेस, और नवजागरण के प्रभाव से मराठी गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। लोकहितवादी, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर जैसे महान व्यक्तियों ने मराठी में सामाजिक चेतना को नई दिशा दी।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मराठी ने जनजागरण का माध्यम बनकर राष्ट्रीय चेतना को प्रखर किया। आधुनिक काल में मराठी साहित्य ने उपन्यास, नाटक, कविता और आलोचना सभी विधाओं में समृद्धि प्राप्त की।
मराठी साहित्य का कालविभाजन तालिका
मराठी साहित्य का विकास कालक्रमानुसार तीन प्रमुख युगों में विभाजित किया जा सकता है — प्राचीन मराठी साहित्य (800–1600 ईस्वी), मध्य मराठी साहित्य (1600–1800 ईस्वी) और आधुनिक मराठी साहित्य (1800 ईस्वी से वर्तमान काल तक)।
यह कालविभाजन न केवल भाषा के विकास को समझने में सहायक है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की झलक भी प्रस्तुत करता है।
| क्रम | काल / युग | समयावधि | प्रमुख विशेषताएँ | प्रमुख कवि / लेखक | प्रमुख कृतियाँ / प्रवृत्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राचीन मराठी साहित्य | 800–1600 ईस्वी | भक्ति आंदोलन का उत्कर्ष; संत काव्य परंपरा; धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं पर आधारित साहित्य | संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखामेळा, मुकुंदराज | ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, अभंग साहित्य |
| 2 | मध्य मराठी साहित्य | 1600–1800 ईस्वी | पंडित परंपरा का विकास; राजकीय विषय, नीति-काव्य और व्यावहारिक गद्य का उदय; शिवकालीन लेखन में मोडी लिपि का प्रयोग | समर्थ रामदास, तुकाराम, मोरोपंत, श्रीधर | दासबोध, तुकाराम गाथा, आर्यावृत्त छंद |
| 3 | आधुनिक मराठी साहित्य | 1800–वर्तमान | राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार, यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक दृष्टि का उदय; नाटक, उपन्यास और आलोचना का उत्कर्ष | कुसुमाग्रज (वि. वि. शिरवाडकर), वि. स. खांडेकर, पु. ल. देशपांडे, विजय तेंदुलकर, भालचंद्र नेमाडे | नटसम्राट, ययाती, घासीराम कोतवाल, आधुनिक कथा और रंगमंच साहित्य |
मराठी साहित्य की यह ऐतिहासिक यात्रा साधना, समाज और संवेदना का अद्भुत संगम है। संत कवियों की भक्ति भावना से लेकर आधुनिक लेखकों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ तक — मराठी साहित्य ने सदैव अपने युग के विचार और चेतना को अभिव्यक्त किया है।
मराठी भाषा की लिपि : देवनागरी और मोडी का ऐतिहासिक विकास
मराठी भाषा का लेखन-संस्कार अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रहा है। इसकी लिपि व्यवस्था समय के साथ विकसित हुई है और आज यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किंतु अतीत में मराठी के लिए एक विशिष्ट लिपि — मोडी लिपी — का भी व्यापक प्रयोग होता था। इस प्रकार मराठी भाषा की लिपिकीय यात्रा को दो प्रमुख चरणों में देखा जा सकता है — देवनागरी (प्रचलित लिपि) और मोडी (ऐतिहासिक लिपि)।
(क) देवनागरी लिपि — आधुनिक और मानक रूप
वर्तमान समय में मराठी का लेखन देवनागरी लिपि में किया जाता है, जो भारत की कई प्रमुख भाषाओं — जैसे हिंदी, संस्कृत और नेपाली — की भी लिपि है। देवनागरी का स्वरूप अत्यंत सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक माना जाता है। यह एक ध्वन्यात्मक (Phonetic) लिपि है, अर्थात इसमें शब्दों का लेखन और उच्चारण लगभग समान रहता है — जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है।
देवनागरी लिपि को मराठी में लगभग 13वीं शताब्दी से प्रयोग में लाया गया और समय के साथ यह भाषा की मानक (Standard) लिपि बन गई। इस लिपि में 12 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं, जिनसे मराठी की समृद्ध ध्वनि-संरचना का निर्माण होता है।
इस लिपि का सौंदर्य इसकी स्पष्टता और लचीलापन है — यह न केवल साहित्यिक रचनाओं के लिए उपयुक्त है, बल्कि प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी लेखन में भी समान रूप से सक्षम है। इसी कारण देवनागरी आज मराठी भाषा का आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकृत लेखन माध्यम है।
(ख) मोडी लिपी — ऐतिहासिक महत्व और उपयोग
देवनागरी के व्यापक प्रयोग से पहले मराठी का लेखन मोडी लिपी में किया जाता था। इसका विकास भी लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था, और इसे मराठी की एक विशिष्ट प्रशासनिक लिपि कहा जा सकता है। मोडी लिपी का प्रयोग विशेषकर व्यापारिक दस्तावेज़ों, शाही आदेशों, और पत्राचार में होता था।
छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में मोडी लिपी ने अपनी सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की। उस समय यह मराठी राज्य की राजकीय लिपि (Official Script) मानी जाती थी, और सभी राजकीय पत्राचार, आदेश तथा प्रशासनिक अभिलेख इसी लिपि में लिखे जाते थे।
मोडी लिपी की संरचना तेज़ लेखन के अनुकूल थी — इसके अक्षर आपस में जुड़े हुए और प्रवाही (cursive) रूप में होते थे, जिससे दस्तावेज़ जल्दी लिखे जा सकते थे। यही कारण है कि यह व्यापारी समुदाय और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रही।
हालाँकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में देवनागरी के प्रसार और शिक्षण संस्थानों में इसके मानकीकरण के कारण मोडी लिपी का प्रयोग धीरे-धीरे घटता चला गया। आज यह प्रायः ऐतिहासिक अभिलेखों, हस्तलिखित ग्रंथों और प्राचीन दस्तावेज़ों में देखने को मिलती है।
महाराष्ट्र के कुछ विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में अब भी मोडी लिपी अध्ययन को इतिहास और अभिलेख विज्ञान (Paleography) के एक विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, ताकि इस लुप्तप्राय लिपि की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके।
लिपि परिवर्तन का सांस्कृतिक प्रभाव
देवनागरी और मोडी दोनों लिपियों ने मराठी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोडी ने मराठी को प्रशासनिक और व्यावहारिक धरातल पर सशक्त बनाया, जबकि देवनागरी ने उसे साहित्यिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय पहचान प्रदान की।
इन दोनों लिपियों का अध्ययन यह दर्शाता है कि मराठी भाषा ने सदियों तक न केवल अपने शब्दकोश और व्याकरणिक रूप को, बल्कि अपनी लेखन पद्धति को भी निरंतर विकसित किया है। यही कारण है कि आज मराठी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक बन चुकी है।
मराठी भाषा का भौगोलिक विस्तार
मराठी भाषा मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है, जो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव और प्रयोग पड़ोसी राज्यों में भी व्यापक है —
- गोवा — यहाँ मराठी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
- कर्नाटक — विशेष रूप से बेलगाम, धारवाड़, गुलबर्गा क्षेत्रों में।
- गुजरात — दक्षिणी भाग में मराठीभाषी जनसंख्या निवास करती है।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना — हैदराबाद और सीमावर्ती जिलों में मराठी प्रभाव देखा जा सकता है।
- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ — नागपुर और बालाघाट जैसे क्षेत्रों में मराठी बोली जाती है।
- तमिलनाडु — चेन्नई के कुछ हिस्सों में मराठी समुदाय निवास करता है।
इसके अलावा केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली में भी मराठी बोली जाती है।
भारत के बाहर मराठी की उपस्थिति
मराठी मूल के लोग व्यापार, प्रवास और रोजगार के कारण विश्व के अनेक देशों में बसे हुए हैं। मॉरिशस और इस्राइल में मराठी समुदाय उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त मराठी भाषी जनसंख्या निम्न देशों में भी पाई जाती है—
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
- दक्षिण अफ्रीका
- सिंगापुर
- जर्मनी
- ब्रिटेन
- ऑस्ट्रेलिया
- न्यूज़ीलैंड
- वेस्ट इंडीज
इन प्रवासी समुदायों ने मराठी भाषा और संस्कृति को विदेशों में भी जीवित रखा है। मॉरिशस में मराठी साहित्यिक संगठन कार्यरत हैं और अमेरिका तथा ब्रिटेन में मराठी सांस्कृतिक सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।
मराठी साहित्यिक परंपरा
मराठी साहित्य का इतिहास भारतीय साहित्य की सबसे समृद्ध परंपराओं में से एक है। इसे मोटे तौर पर तीन कालों में बाँटा जा सकता है —
- भक्ति काल (13वीं–17वीं शताब्दी)
- संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, मुक्ताबाई आदि ने भक्ति को लोकभाषा में पहुँचाया।
- ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘अभंग’, ‘भारुद’ जैसे रूप इसी काल में विकसित हुए।
- पेशवा काल (18वीं शताब्दी)
- मराठी निबंध, पत्र और ऐतिहासिक लेखन का विकास।
- वीररस और नीति साहित्य की प्रधानता।
- आधुनिक काल (19वीं शताब्दी से आगे)
- मराठी उपन्यास, नाटक, और आधुनिक कविता का जन्म।
- विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, ह. ना. आपटे, वि. स. खांडेकर, पु. ल. देशपांडे, भीमसेन जोशी जैसे रचनाकारों ने साहित्य, संगीत और कला को नई ऊँचाइयाँ दीं।
मराठी भाषा दिवस (राजभाषा दिवस) और मराठी भाषा गौरव दिवस
मराठी भाषा के संवर्धन और उसकी गौरवशाली परंपरा को स्मरण करने के लिए महाराष्ट्र में दो विशिष्ट दिवस मनाए जाते हैं — मराठी राजभाषा दिवस (1 मई) और मराठी भाषा गौरव दिवस (27 फरवरी)।
- राजभाषा दिवस (1 मई) – महाराष्ट्र राज्य के गठन दिवस के अवसर पर मनाया जाता है।
- भाषा गौरव दिवस (27 फरवरी) – सुप्रसिद्ध मराठी कवि वि. स. खांडेकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
ये दोनों दिवस मराठी भाषियों के लिए न केवल गर्व का विषय हैं, बल्कि अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी का भी प्रतीक हैं। इन अवसरों पर साहित्यिक कार्यक्रम, वाद-विवाद, कविता पाठ, भाषाई संगोष्ठियाँ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाती हैं।
(क) मराठी राजभाषा दिवस — 1 मई
मराठी राजभाषा दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को पूरे महाराष्ट्र में बड़े उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया जाता है। इस दिन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना (1 मई 1960) से जुड़ी है।
1 मई 1960 को भाषाई पुनर्गठन के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ, जिससे मराठी भाषियों को एक एकीकृत राज्य प्राप्त हुआ। इसी ऐतिहासिक अवसर को सम्मानित करने के लिए इस दिन को ‘मराठी राजभाषा दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
वर्ष 1964 में पारित “महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम” के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक ने मराठी को महाराष्ट्र की आधिकारिक राजभाषा (Official Language) घोषित किया। यह निर्णय न केवल भाषाई गौरव का प्रतीक बना, बल्कि प्रशासन, शिक्षा, और सांस्कृतिक जीवन में मराठी के सशक्त प्रयोग को भी सुनिश्चित किया।
राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और सांस्कृतिक संगठनों में इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें मराठी साहित्य, कविता, नाटक, और भाषण प्रतियोगिताएँ शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य मराठी भाषा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना और इसे सार्वजनिक जीवन में अधिकाधिक प्रोत्साहन देना है।
(ख) मराठी भाषा गौरव दिवस — 27 फरवरी
मराठी साहित्य की समृद्ध परंपरा और उसके महान रचनाकारों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिन सुप्रसिद्ध मराठी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और दार्शनिक विष्णु वामन शिरवाडकर की जयंती का प्रतीक है।
शिरवाडकर जी अपने साहित्यिक नाम “कुसुमाग्रज” से प्रसिद्ध हैं। उनके लेखन में मराठी समाज की भावनाएँ, संस्कृति और आधुनिक विचारधारा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी कृतियों ने मराठी साहित्य को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं और भाषा की साहित्यिक गरिमा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया।
उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी उपलब्धि और उनके मराठी प्रेम को स्मरण करने के लिए 27 फरवरी को ‘मराठी भाषा गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन महाराष्ट्र भर में साहित्यिक आयोजन, काव्य-पाठ, विचार-गोष्ठियाँ और पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को मराठी साहित्य और भाषा के गौरव से परिचित कराया जाता है, ताकि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान और अभिमान महसूस करे।
भाषा गौरव के प्रतीक रूप में दोनों दिवसों का महत्व
इन दोनों अवसरों का सार यह है कि —
- 1 मई मराठी भाषा की राजकीय पहचान और प्रशासनिक प्रतिष्ठा* का प्रतीक है,
- जबकि 27 फरवरी मराठी की सांस्कृतिक और साहित्यिक गरिमा का उत्सव है।
दोनों दिवस मिलकर इस बात की याद दिलाते हैं कि मराठी केवल एक संवाद की भाषा नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन-शैली, विचारधारा और सांस्कृतिक धरोहर है।
मराठी भाषा दिवस और गौरव दिवस न केवल भाषाई चेतना को सशक्त करते हैं, बल्कि यह भी प्रेरणा देते हैं कि अपनी मातृभाषा के संवर्धन और प्रयोग में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है।
मराठी की बोलियाँ और क्षेत्रीय विविधता
मराठी भाषा के भीतर अनेक क्षेत्रीय बोलियाँ हैं जो भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार बदलती हैं। इनमें प्रमुख हैं —
- अहिराणी (खानदेश क्षेत्र)
- वऱ्हाडी (विदर्भ क्षेत्र)
- कोकणी मराठी (पश्चिमी तटीय क्षेत्र)
- देसस्थी (पुणे, सतारा)
- मालवणी (कोंकण तट)
- गोंडी मराठी (गोंडवाना क्षेत्र)
इन बोलियों ने मराठी की अभिव्यक्ति को विविध रंगों से सजाया है।
आधुनिक युग में मराठी का स्थान
वर्तमान समय में मराठी केवल एक क्षेत्रीय भाषा नहीं, बल्कि एक आधुनिक प्रशासनिक, शैक्षणिक और तकनीकी भाषा है। महाराष्ट्र में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम मराठी है।
मराठी पत्रकारिता भी भारत की सबसे पुरानी और सशक्त पत्रकारिता परंपराओं में से एक है। 1835 में प्रकाशित ‘दर्पण’ मराठी का पहला समाचारपत्र था। आज ‘लोकसत्ता’, ‘सकाळ’, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ जैसे प्रमुख दैनिक पत्र मराठी में प्रकाशित होते हैं।
इसके अलावा मराठी सिनेमा (Marathi Cinema) ने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। रंजीत देसाई, पु. ल. देशपांडे, और नागराज मंजुळे जैसे रचनाकारों ने मराठी कला-संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है।
मराठी भाषा और संविधान
भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में मराठी को संवैधानिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। इससे इसे समान प्रशासनिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त हुई। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी के संवर्धन के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की है, जैसे—
- महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ
- मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ
- महाराष्ट्र साहित्य परिषद
इन संस्थानों के माध्यम से भाषा के प्रचार-प्रसार, शोध और आधुनिक प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
मराठी साहित्य
मराठी साहित्य भारतीय भाषाओं में अत्यंत समृद्ध और जीवंत परंपराओं में से एक है, जिसकी शुरुआत लगभग 13वीं शताब्दी से मानी जाती है। इस साहित्य में कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध और कथा जैसी अनेक विधाएँ शामिल हैं, जो मराठी भाषी समाज की सांस्कृतिक चेतना, जीवन मूल्यों और ऐतिहासिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण करती हैं।
प्रारंभिक विकास और भक्ति आंदोलन का प्रभाव
मराठी साहित्य का सबसे प्राचीन और प्रभावशाली रूप “भक्ति काव्य” माना जाता है, जिसने 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य समाज में धार्मिक समरसता और मानवीय मूल्यों का संदेश फैलाया। संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ जैसे संत-कवियों ने मराठी में ऐसी भक्ति रचनाएँ कीं जिन्होंने भाषा को जनता की आत्मा से जोड़ दिया। भक्ति परंपरा ने मराठी साहित्य को नैतिकता, भक्ति और समानता के भाव से समृद्ध किया।
आधुनिक मराठी साहित्य का पुनरुत्थान
19वीं और 20वीं शताब्दी आते-आते मराठी साहित्य में आधुनिक विचारधारा, राष्ट्रवाद और सामाजिक यथार्थवाद का समावेश होने लगा। इस काल में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों की चेतना साहित्य में प्रकट हुई। कवियों, नाटककारों और उपन्यासकारों ने अपने लेखन के माध्यम से समाज की जटिलताओं और बदलते जीवन मूल्यों को स्वर दिया।
प्रमुख साहित्यकार और उनका योगदान
वी. वी. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) – मराठी साहित्य के शिखर पुरुषों में गिने जाने वाले शिरवाडकर कवि, नाटककार और चिंतक थे। उन्होंने मराठी भाषा को आधुनिक संवेदना और दार्शनिक गहराई दी। उनकी साहित्यिक साधना के लिए उन्हें “ज्ञानपीठ पुरस्कार” से सम्मानित किया गया।
वी. एस. खांडेकर – उपन्यास और नाटक विधा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले खांडेकर का साहित्य मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसने मराठी साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया।
पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे (पु. ल. देशपांडे) – हास्य, व्यंग्य और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम उनके लेखन की पहचान है। उन्होंने नाटक, लघुकथाओं और आत्मकथात्मक गद्य के माध्यम से मराठी जीवन के विविध पहलुओं को सहज और रोचक शैली में प्रस्तुत किया।
पी. एल. देशपांडे – बहुमुखी प्रतिभा के धनी देशपांडे ने कथा, निबंध और नाटक सहित अनेक विधाओं में लेखन किया। उनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन का व्यंग्यपूर्ण किंतु करुण चित्र दिखाई देता है।
विजय तेंदुलकर – मराठी रंगमंच के क्रांतिकारी नाटककार के रूप में तेंदुलकर ने सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर तीखी दृष्टि डाली। उनके नाटक “घासीराम कोतवाल”, “सखाराम बाइंडर” और “सिल्विया प्लाथ” जैसे कार्य सामाजिक चेतना के प्रतीक बन गए।
भालचंद्र नेमाडे – आधुनिक मराठी उपन्यास के प्रणेता माने जाने वाले नेमाडे की रचनाएँ सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और आधुनिकता के टकराव पर आधारित हैं। वे मराठी साहित्य में स्वभाषा और स्वसंस्कृति के प्रवक्ता रहे हैं।
महेश एलकुंचवार – मराठी नाट्य-जगत के प्रमुख नाटककारों में एक, जिनके नाटकों में व्यक्ति की आंतरिक जटिलताओं और आधुनिक जीवन की विसंगतियों का गहन विश्लेषण मिलता है।
एस. एन. पेंडसे – साहित्य, संपादन और आलोचना के क्षेत्र में समान रूप से सक्रिय रहे। उन्होंने मराठी कथा-साहित्य को सामाजिक और दार्शनिक गहराई दी।
रत्नाकर मटकरी – समकालीन मराठी साहित्य में एक प्रमुख नाम, जिनके नाटक और कहानियाँ सामाजिक यथार्थ, मनोवैज्ञानिक दृष्टि और मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण करती हैं।
सुधा मूर्ति – यद्यपि वे मुख्यतः कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं, किन्तु उनकी रचनाओं का मराठी अनुवाद अत्यंत लोकप्रिय है। बाल साहित्य के माध्यम से उन्होंने मराठी पाठकों के बीच भी व्यापक प्रभाव डाला है।
मराठी साहित्य की यह समृद्ध परंपरा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की आत्मा का दर्पण है। यह भाषा और संस्कृति के उस संगम का प्रतीक है जिसने समाज में लोकचेतना और मानवीयता का संचार किया। आज भी मराठी भाषा साहित्य, पत्रकारिता, रंगमंच, शिक्षा और लोकसंस्कृति के क्षेत्र में समान रूप से जीवंत है।
मराठी साहित्य न केवल महाराष्ट्र की पहचान है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता का गौरवशाली अध्याय भी है।
प्रमुख मराठी साहित्यकार और उनका योगदान | सारणी
| क्रम | साहित्यकार | प्रमुख विधा / क्षेत्र | योगदान का सारांश | प्रमुख कृतियाँ / उपलब्धियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वी. वी. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) | कविता, नाटक, चिंतन | मराठी साहित्य के शिखर पुरुष; आधुनिक संवेदना और दार्शनिक दृष्टि से मराठी कविता को नई ऊँचाई दी; सामाजिक समानता और मानवीय मूल्य उनके लेखन का केंद्र रहे। | विश्वास, नटसम्राट; ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त |
| 2 | वी. एस. खांडेकर | उपन्यास, नाटक | मानवीय मनोविज्ञान और नैतिकता की सूक्ष्म व्याख्या करने वाले उपन्यासकार; मराठी गद्य को नवीन जीवनदृष्टि दी। | ययाती; ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त |
| 3 | पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे (पु. ल. देशपांडे) | हास्य, व्यंग्य, आत्मकथात्मक गद्य | हास्य और मानवीय संवेदनाओं का अनोखा संगम; मराठी समाज के जीवन-सूत्रों को सहज और रोचक शैली में अभिव्यक्त किया। | व्यक्ती आणि वल्ली, बटाट्याची चाळ |
| 4 | पी. एल. देशपांडे | कथा, निबंध, नाटक | बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक; सामाजिक जीवन का व्यंग्यपूर्ण किंतु संवेदनशील चित्रण; मानवीय रिश्तों की करुण व्याख्या। | असामी असामी, अपुलकी |
| 5 | विजय तेंदुलकर | नाटक, पटकथा लेखन | मराठी रंगमंच के यथार्थवादी और क्रांतिकारी नाटककार; सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर तीखी दृष्टि। | घासीराम कोतवाल, सखाराम बाइंडर |
| 6 | भालचंद्र नेमाडे | उपन्यास, आलोचना | आधुनिक मराठी उपन्यास के प्रणेता; स्वभाषा और स्वसंस्कृति के प्रवक्ता; पहचान, परंपरा और आधुनिकता के संघर्ष पर लेखन। | कोसला, हिंदू – जगण्याची समृद्ध अधोरेखा |
| 7 | महेश एलकुंचवार | नाटक, रंगमंच | आधुनिक मराठी रंगमंच के प्रमुख सर्जक; व्यक्ति की आंतरिक जटिलताओं और अस्तित्वगत संघर्षों का गहन विश्लेषण। | वाडा चिरेबंदी, महापुर |
| 8 | एस. एन. पेंडसे | कथा, आलोचना, संपादन | कथा-साहित्य में दार्शनिक गहराई और सामाजिक यथार्थ का संयोजन; मराठी साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में भी योगदान। | गर्भ, रथचक्र |
| 9 | रत्नाकर मटकरी | नाटक, लघुकथा | समकालीन समाज की समस्याओं पर गहरी दृष्टि; मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विषयों पर प्रभावशाली नाट्यलेखन। | चार दिवस प्रेमाचे, डब्बा गुल |
| 10 | सुधा मूर्ति | बाल साहित्य, प्रेरक लेखन | मराठी अनुवादों के माध्यम से बच्चों में नैतिकता और सहानुभूति के मूल्य स्थापित किए; सामाजिक कार्यों से भी प्रसिद्ध। | Wise and Otherwise (मराठी अनुवाद), The Magic Drum |
यह तालिका मराठी साहित्य के विविध युगों के प्रमुख रचनाकारों का एक समेकित परिचय प्रस्तुत करती है — जहाँ भक्ति युग की करुणा, राष्ट्रवाद युग की चेतना, और आधुनिक काल की यथार्थवादी दृष्टि सभी का संगम दिखाई देता है।
मराठी का वैश्विक प्रभाव और भविष्य
आज मराठी भाषा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी सशक्त रूप से उपस्थित है। सोशल मीडिया, ब्लॉग, ई-पत्रिकाएँ, ऑनलाइन शिक्षा, और मोबाइल एप्लिकेशनों में मराठी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।
मराठी विकिपीडिया, मराठी ब्लॉगिंग और ई-बुक्स ने इस भाषा को विश्व के कोने-कोने तक पहुँचाया है। विदेशों में बसे मराठी समुदायों ने अपनी मातृभाषा को नई पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए संस्थान, विद्यालय और सांस्कृतिक समूह स्थापित किए हैं।
भविष्य की दृष्टि से, मराठी भाषा में अपार संभावनाएँ हैं। इसकी मजबूत साहित्यिक परंपरा, जीवंत संस्कृति और विशाल वक्ता-समुदाय इसे भारत की प्रमुख भाषाओं में स्थायी स्थान प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष
मराठी भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है — यह महाराष्ट्र की आत्मा, संस्कृति और चेतना की अभिव्यक्ति है। इसकी जड़ें भारत की प्राचीन सभ्यता में हैं और इसकी शाखाएँ आधुनिक विश्व में फैल चुकी हैं।
संस्कृत की पवित्र धारा से निकली यह भाषा, प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित होकर आज आधुनिक विज्ञान, कला, और तकनीक के युग में भी जीवंत बनी हुई है।
मराठी ने संतों की वाणी में भक्ति का संदेश दिया, स्वतंत्रता सेनानियों के भाषणों में प्रेरणा दी, और आज के साहित्यकारों के लेखन में मानवता की भावना को जीवित रखा है।
वास्तव में, मराठी भाषा भारत की भाषाई विविधता का एक अनमोल रत्न है — जो अतीत की गौरवशाली परंपरा, वर्तमान की सांस्कृतिक सजीवता और भविष्य की संभावनाओं, तीनों को एक साथ अपने में समाहित करती है।
इन्हें भी देखें –
- हिंदी साहित्य में रेखाचित्र : साहित्य में शब्दों से बनी तस्वीरें
- हिन्दी की जीवनी और जीवनीकार : जीवनी लेखक और रचनाएँ
- संस्मरण – अर्थ, परिभाषा, विकास, विशेषताएँ एवं हिंदी साहित्य में योगदान
- मातृभाषा: परिभाषा, अर्थ, विशेषताएँ और दिवस – संस्कृति, पहचान और अभिव्यक्ति का आधार
- राष्ट्रभाषा : स्वरूप, अवधारणा, परिभाषा और महत्व
- राजभाषा : भारत की राजभाषा, राज्यों की राजभाषाएं, परिभाषा, महत्व और सूची
- गुजराती भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, दिवस, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, साहित्य और इतिहास
- कश्मीरी भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, वर्णमाला, शब्द, वाक्य और इतिहास
- पंजाबी भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, बोली क्षेत्र, वर्णमाला, शब्द, वाक्य और इतिहास
- सिंधी भाषा : उद्भव, विकास, लिपि, वर्णमाला, शब्द, वाक्य और भाषिक संरचना
- रीतिकाल के कवि और रचनाएँ