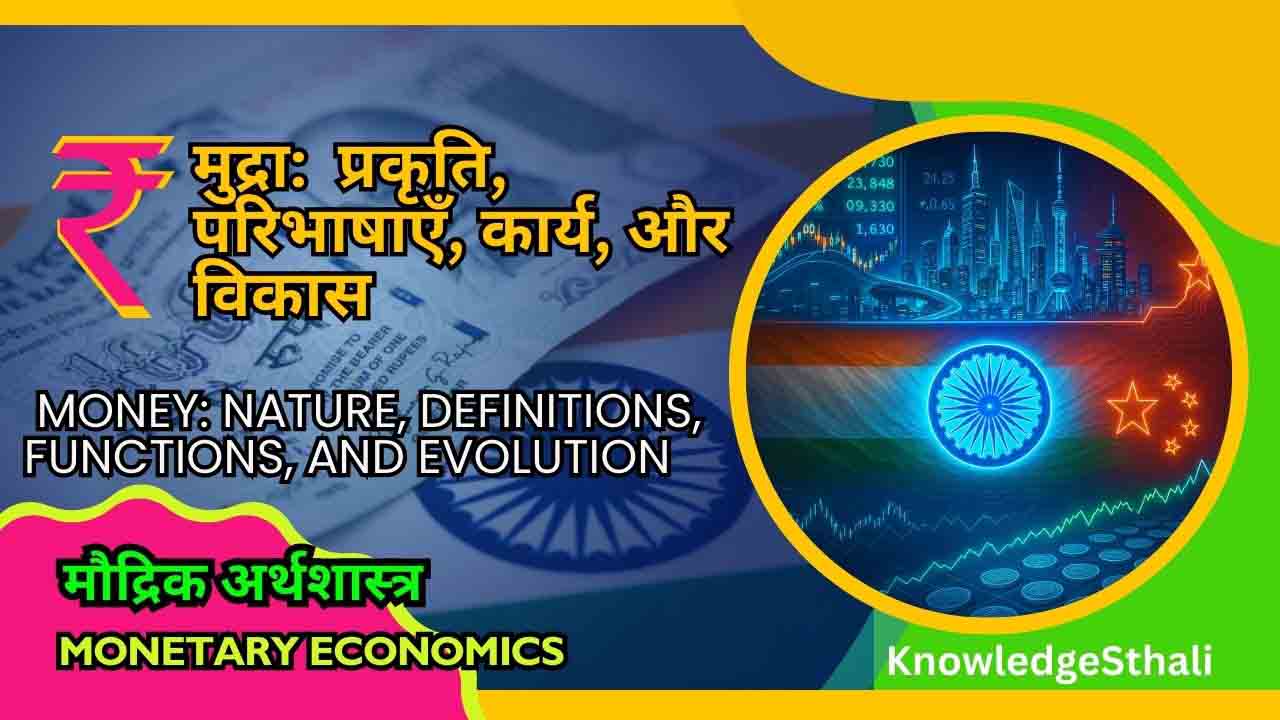मुद्रा मानव सभ्यता की एक प्राचीन आविष्कार है, जिसका विकास आर्थिक आवश्यकताओं और सामाजिक संगठन के साथ क्रमिक रूप से हुआ। प्रारंभ में वस्तु-विनिमय प्रणाली (barter system) प्रचलित थी, जहाँ वस्तुओं का सीधा आदान-प्रदान होता था। किंतु इस प्रणाली की कठिनाइयों (जैसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या) ने मुद्रा के उद्भव को अनिवार्य बना दिया।
प्राचीन काल में पशु, अनाज, खाल, नमक, और कौड़ियाँ जैसी वस्तुएँ मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती थीं। धातुओं (सोना, चाँदी, ताँबा) के आगमन के साथ सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। आधुनिक युग में कागजी मुद्रा, बैंक जमाराशियाँ, और डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ मुद्रा के नए रूप हैं।
मुद्रा का ऐतिहासिक संदर्भ
मुद्रा मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। इसके बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रारंभ में, मनुष्य ने वस्तु-विनिमय (barter system) के माध्यम से अपनी आवश्यकताएँ पूरी कीं, लेकिन इस प्रणाली में अनेक कमियाँ थीं। उदाहरण के लिए, यदि एक किसान के पास गेहूँ है और उसे कपड़े की आवश्यकता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती थी जो कपड़े के बदले गेहूँ लेने को तैयार हो। इसे “आवश्यकताओं के दोहरे संयोग (Double Coincidence of Wants)” की समस्या कहा जाता है। इसके अलावा, वस्तु-विनिमय में मूल्य के मापन, संचय, और विभाजन की समस्याएँ भी थीं।
इन समस्याओं के समाधान के रूप में वस्तु-मुद्रा (Commodity Money) का उदय हुआ। प्राचीन काल में लोगों ने ऐसी वस्तुओं को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जो टिकाऊ, विभाज्य, और सर्वमान्य थीं। उदाहरण के लिए, भारत में अनाज, पशु, और नमक; अफ्रीका में मोती; और चीन में कछुआ खोल। कालांतर में, धातुओं (सोना, चाँदी, ताँबा) ने मुद्रा का रूप लिया क्योंकि वे टिकाऊ, दुर्लभ, और सुवाह्य थे।
वस्तु-विनिमय प्रणाली एवं उसकी सीमाएँ
प्राचीन काल में, मनुष्य ने वस्तु-विनिमय (Barter System) के माध्यम से अपनी आवश्यकताएँ पूरी कीं। इस प्रणाली में वस्तुओं का सीधा आदान-प्रदान होता था। उदाहरण के लिए, एक किसान गेहूँ के बदले बुनकर से कपड़ा प्राप्त कर सकता था। हालाँकि, इस प्रणाली में कई गंभीर समस्याएँ थीं:
- आवश्यकताओं का दोहरा संयोग (Double Coincidence of Wants): विनिमय के लिए दोनों पक्षों की आवश्यकताओं का मेल होना आवश्यक था। यदि किसान को कपड़ा चाहिए, तो उसे ऐसे बुनकर की तलाश करनी पड़ती थी जो गेहूँ लेने को तैयार हो।
- मूल्य के मापन की कठिनाई: वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करना कठिन था। उदाहरण के लिए, एक बकरी के बदले कितने किलो गेहूँ दिए जाएँ?
- विभाज्यता का अभाव: कुछ वस्तुएँ (जैसे पशु) छोटे हिस्सों में नहीं बाँटी जा सकती थीं।
- संचय की असमर्थता: नाशवान वस्तुएँ (जैसे फल, अनाज) लंबे समय तक संचित नहीं की जा सकती थीं।
मुद्रा के उद्भव की आवश्यकता
वस्तु-विनिमय प्रणाली के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के रूप में वस्तु-मुद्रा (Commodity Money) का उदय हुआ। समाज ने ऐसी वस्तुओं को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जो सर्वमान्य, टिकाऊ, और विभाज्य थीं। उदाहरण के लिए:
- भारत: गाय, अनाज, नमक।
- चीन: कछुआ खोल, चाकू।
- अफ्रीका: मोती, हाथी दाँत।
- मिस्र: धातु के छल्ले और सिक्के।
धातुओं (सोना, चाँदी, ताँबा) ने धीरे-धीरे वस्तु-मुद्रा का स्थान ले लिया, क्योंकि वे टिकाऊ, दुर्लभ, और सुवाह्य थीं।
प्राचीन सभ्यताओं में मुद्रा
- सुमेरियन सभ्यता (मेसोपोटामिया, 3000 ईसा पूर्व): चाँदी के सिक्के “शेकेल” का प्रयोग।
- मिस्र (2000 ईसा पूर्व): सोने के छल्ले और कौड़ियाँ।
- भारत (6वीं शताब्दी ईसा पूर्व): “पंचमार्क” सिक्के, जिन पर पेड़, बैल, और हाथी के चिह्न अंकित थे।
- चीन (7वीं शताब्दी ईसा पूर्व): कांस्य के उपकरण और कछुआ खोल।
मुद्रा की परिभाषाएँ: विद्वानों के दृष्टिकोण | Definition of Money
मुद्रा को परिभाषित करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि यह समाज और अर्थव्यवस्था के साथ गतिशील रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से मुद्रा को परिभाषित किया है:
वर्णनात्मक परिभाषाएँ (Descriptive Definition)
- फ्रांसिस वॉकर (Francis Walker): “मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।”
- हार्टले विदर्स (Hartley Withers): “मुद्रा वह सामग्री है जिसके द्वारा हम वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं।”
- एस.ई. थॉमस: “मुद्रा समुदाय के सदस्यों पर एक प्रकार का अधिकार है, जिसे स्वामी अपनी इच्छानुसार भुगतान के लिए प्रयोग कर सकता है।”
आलोचना: ये परिभाषाएँ मुद्रा के कार्यों पर तो प्रकाश डालती हैं, लेकिन इनमें वैज्ञानिक सटीकता और सार्वभौमिकता का अभाव है।
वैधानिक परिभाषाएँ (Legal Definition)
- नैप (Georg Friedrich Knapp): “मुद्रा राज्य द्वारा घोषित वह वस्तु है जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो।”
- हॉट्रे (Ralph Hawtrey): “मुद्रा ऋणों के शोधन और मूल्य-मापक का साधन है।”
आलोचना : इन परिभाषाओं के अनुसार, मुद्रा की स्वीकृति कानूनी बाध्यता पर निर्भर करती है। हालाँकि, मुद्रास्फीति या आर्थिक संकट के दौरान कानूनी मुद्रा भी लोगों का विश्वास खो सकती है। ये परिभाषाएँ मुद्रा को केवल कानूनी दृष्टि से देखती हैं, जबकि व्यावहारिक रूप में मुद्रा की स्वीकृति जनता के विश्वास पर निर्भर करती है।
सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ (Definition Based on General Acceptability)
- क्राउथर (Crowther): “मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य-मापक, और संचय के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और साथ ही मूल्य-मापक तथा मूल्य-संचय का कार्य करती है।”
- रॉबर्टसन (Dennis Robertson): “मुद्रा वह है जिसे सामान्यतः ऋणों के निपटारे के लिए स्वीकार किया जाता है।”
यह दृष्टिकोण मुद्रा के सामाजिक-आर्थिक (व्यावहारिक) पहलू को उजागर करता है, जहाँ जनता का विश्वास मुख्य आधार है।
आधुनिक दृष्टिकोण
- मिल्टन फ्रिडमैन (Milton Friedman): “मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी निवास (Temporary Abode of Purchasing Power) है।”
- पॉल सैम्युल्सन (Paul Samuelson): “मुद्रा वह सामाजिक संस्था है जो विनिमय और संचय को सुविधाजनक बनाती है।”
मुद्रा के गुणों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि, “मुद्रा वह वस्तु है जिसे एक व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य-मापक, ऋण-भुगतान, तथा मूल्य-संचय के रूप में स्वतंत्र और सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।”
मुद्रा के कार्य | Functions of Money
मुद्रा के प्रमुख कार्यों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है: प्राथमिक कार्य और गौण कार्य।
प्राथमिक कार्य
- विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange):
- मुद्रा ने वस्तु-विनिमय की कठिनाइयों को समाप्त किया। उदाहरण: एक शिक्षक फीस के रूप में नकदी स्वीकार करता है, न कि सब्जियाँ।
- यह कार्य मुद्रा को “सामान्य स्वीकृति” प्रदान करता है।
- मूल्य का मापक (Measure of Value):
- मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक सामान्य इकाई (जैसे रुपया, डॉलर) में व्यक्त करती है।
- उदाहरण: एक सेब का मूल्य ₹10 और एक किताब का मूल्य ₹200।
गौण कार्य
- मूल्य का संचय (Store of Value):
- मुद्रा भविष्य के उपयोग के लिए मूल्य को सुरक्षित रखती है।
- उदाहरण: बैंक में जमा राशि, सोने के गहने।
- भविष्य में भुगतान का आधार (Standard of Deferred Payments):
- मुद्रा दीर्घकालिक ऋणों और अनुबंधों का आधार है।
- उदाहरण: घर का किश्तों में भुगतान, शिक्षा ऋण।
- मूल्य का हस्तांतरण (Transfer of Value):
- मुद्रा के माध्यम से धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- उदाहरण: विदेशों में रुपया भेजना, ऑनलाइन भुगतान।
मुद्रा के प्रकार (Kinds of Money) | विस्तृत वर्गीकरण
मुद्रा को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है:
प्रकृति के आधार पर
- वास्तविक मुद्रा (Real Money): भौतिक रूप में उपस्थित मुद्रा, जैसे सिक्के, नोट, और डिजिटल करेंसी।
- लेखा मुद्रा (Money of Account): लेखांकन और मूल्यांकन की इकाई, जैसे रुपया, डॉलर, येन।
वैधानिकता के आधार पर
- विधिग्राह्य मुद्रा (Legal Tender):
- सीमित: छोटे सिक्के (जैसे ₹1, ₹2, ₹5), जिन्हें एक निश्चित सीमा तक स्वीकार करना अनिवार्य है।
- असीमित: नोट और बड़े सिक्के (जैसे ₹10, ₹20), जिन्हें किसी भी राशि के भुगतान में स्वीकार किया जाना चाहिए।
- ऐच्छिक मुद्रा (Optional Money):
- चेक, डिजिटल वॉलेट (Paytm, Google Pay), और क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन), जिन्हें स्वीकार करना विक्रेता की इच्छा पर निर्भर करता है।
मुद्रा-सामग्री के आधार पर
- धातु मुद्रा (Metallic Money):
- प्रामाणिक सिक्के: ऐतिहासिक रूप से सोने और चाँदी के सिक्के, जिनका धातु मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता था।
- सांकेतिक सिक्के: आधुनिक सिक्के (जैसे ₹10 का सिक्का), जिनका धातु मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है।
- पत्र मुद्रा (Paper Money):
- परिवर्तनीय: ऐतिहासिक नोट जिन्हें सोने में बदला जा सकता था।
- अपरिवर्तनीय: आधुनिक नोट (जैसे ₹500, ₹2000), जिन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- साख मुद्रा (Credit Money):
- बैंक जमाराशियाँ, क्रेडिट कार्ड, और डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ।
तरलता के आधार पर
- पूर्ण तरल (Perfectly Liquid): नकद मुद्रा, जिसे तुरंत खर्च किया जा सकता है।
- अर्ध-तरल (Semi-Liquid): फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड, जिन्हें नकदी में बदलने में समय लगता है।
ऋण के आधार पर (गुरले एवं शॉ का सिद्धांत)
- आंतरिक मुद्रा (Inside Money):
- बैंकों द्वारा निर्मित साख, जैसे बैंक जमाराशियाँ। यह निजी क्षेत्र के ऋण पर आधारित होती है।
- बाह्य मुद्रा (Outside Money):
- सरकार द्वारा जारी नोट और सिक्के, जो सरकारी ऋण पर आधारित होते हैं।

मुद्रा का विकास: चरणबद्ध अध्ययन
मुद्रा के विकास को पाँच प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है:
प्रथम चरण: वस्तु-मुद्रा (Commodity Money)
- उदाहरण:
- मिस्र में अनाज और कपड़ा।
- भारत में नमक और गाय।
- चीन में कछुआ खोल और चाकू।
- समस्याएँ:
- टिकाऊपन की कमी (जैसे अनाज सड़ जाता था)।
- विभाज्यता का अभाव (जैसे पशु को छोटे हिस्सों में नहीं बाँटा जा सकता)।
द्वितीय चरण: धातु-मुद्रा (Metallic Money)
- सोने-चाँदी के सिक्के:
- लाएंड्रा सभ्यता (Lydia, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व): विश्व के पहले सिक्के।
- भारत में पंचमार्क सिक्के: महाजनपद काल में चाँदी के सिक्के।
- प्रामाणिक सिक्कों की विशेषताएँ:
- स्वतंत्र ढलाई (Free Coinage): कोई भी व्यक्ति धातु लाकर सिक्के ढलवा सकता था।
- असीमित विधिग्राह्यता (Unlimited Legal Tender)।
तृतीय चरण: पत्र-मुद्रा (Paper Money)
- चीन में प्रथम कागजी मुद्रा (7वीं शताब्दी): तांग राजवंश के दौरान “जिआोज़ी” नामक नोट।
- यूरोप में गोल्डस्मिथ नोट्स (17वीं शताब्दी): सोने के जमानत पर जारी नोट।
- भारत में पत्र-मुद्रा का प्रचलन:
- 1861 का पेपर करेंसी एक्ट: ब्रिटिश सरकार द्वारा नोट जारी करना।
- RBI की स्थापना (1935): नोट निर्गमन का केन्द्रीयकरण।
चतुर्थ चरण: साख-मुद्रा (Credit Money)
- बैंक जमाराशियाँ (Bank Deposits):
- चालू खाता (Current Account): बिना ब्याज के, असीमित निकासी।
- बचत खाता (Savings Account): सीमित निकासी, ब्याज सहित।
- क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान:
- प्लास्टिक मुद्रा: Visa, MasterCard।
- डिजिटल वॉलेट: Paytm, PhonePe।
पंचम चरण: डिजिटल मुद्रा (Digital Currency)
- क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency):
- बिटकॉइन (2009): सातोशी नाकामोतो द्वारा आविष्कार।
- एथेरियम, डॉजकॉइन: स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग।
- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):
- भारत का डिजिटल रुपया (2023): RBI द्वारा जारी, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित।
मुद्रा और अर्थव्यवस्था: सम्बन्ध
मुद्रा अर्थव्यवस्था का रक्त है। इसके बिना उत्पादन, विनिमय, और वितरण की प्रक्रिया असंभव है।
मौद्रिक नीति (Monetary Policy)
- उद्देश्य: मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन।
- उपकरण:
- रेपो दर (Repo Rate): बैंकों को RBI से उधार लेने की दर।
- नकद आरक्षी अनुपात (CRR): बैंकों को RBI के पास रखी जाने वाली नकदी।
मुद्रास्फीति और अवस्फीति
- मुद्रास्फीति (Inflation): मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट।
- कारण: मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, माँग-आपूर्ति असंतुलन।
- अवस्फीति (Deflation): कीमतों में सामान्य गिरावट।
- प्रभाव: निवेश में कमी, बेरोजगारी।
विनिमय दर (Exchange Rate)
- निर्धारण: मुद्रा की माँग और आपूर्ति पर आधारित।
- प्रणालियाँ:
- निश्चित विनिमय दर (Fixed Exchange Rate): सरकार द्वारा निर्धारित।
- लचीली विनिमय दर (Floating
मुद्रा एक गतिशील संकल्पना है, जिसका स्वरूप आर्थिक प्रगति और तकनीकी नवाचारों के साथ बदलता रहता है। आज यह न केवल विनिमय का माध्यम है, बल्कि आर्थिक नीति का प्रमुख उपकरण भी है। मुद्रा की परिभाषा, प्रकार और कार्यों को समझना आर्थिक विश्लेषण के लिए आवश्यक है। भविष्य में डिजिटल मुद्राएँ और ब्लॉकचेन तकनीक मौद्रिक प्रणाली को और अधिक परिष्कृत बनाएंगी।

भारत में मुद्रा का इतिहास
भारत की मौद्रिक प्रणाली का इतिहास अत्यंत समृद्ध है:
प्राचीन काल
- पंचमार्क सिक्के (छठी शताब्दी ईसा पूर्व): चाँदी के सिक्के, जिन पर पेड़, बैल, और हाथी के चिह्न अंकित थे।
- मौर्य काल (322–185 ईसा पूर्व): चाँदी के “कार्षापण” सिक्के।
मध्यकाल
- शेरशाह सूरी (1540–1545): “रुपया” का प्रचलन, जो 178 ग्राम चाँदी का बना होता था।
- मुगल काल: सोने के “मोहर” और चाँदी के “रुपया”।
आधुनिक काल
- ब्रिटिश शासन (1858–1947): “कागजी रुपया” का प्रचलन।
- स्वतंत्रता के बाद:
- 1957 में दशमलव प्रणाली का प्रारंभ (1 रुपया = 100 पैसे)।
- 2016 में विमुद्रीकरण (Demonetization): ₹500 और ₹1000 के नोट बंद।
- 2023 में डिजिटल रुपया (CBDC) का प्रारंभ।
मुद्रा मानव सभ्यता की गतिशीलता और नवाचार का प्रतीक है। वस्तु-विनिमय से लेकर डिजिटल मुद्रा तक, इसका विकास समाज की बदलती आवश्यकताओं का दर्पण है। आज मुद्रा न केवल विनिमय का माध्यम है, बल्कि आर्थिक नीति, वैश्विक व्यापार, और तकनीकी प्रगति का केन्द्रबिंदु भी है। भविष्य में ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी तकनीकें मौद्रिक प्रणाली को और अधिक परिष्कृत बनाएंगी।
Monetary Economics – KnowledgeSthali
इन्हें भी देखें –
- मुद्रा की परिभाषा एवं सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोण
- मुद्रा एवं मुद्रा मूल्य | Money and Value of Money
- मुद्रा एवं सन्निकट मुद्रा | Money and Near Money
- मुद्रा के प्रकार | Kinds of Money
- मुद्रा के कार्य | Functions of Money
- मुद्रा का महत्व | Significance of Money
- मुद्रा की तटस्थता | Neutrality of Money
- मुद्रा भ्रम (Money Illusion) | एक मनोवैज्ञानिक स्थिति का आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण
- क्लोनिंग, जीन एडिटिंग और विलुप्ति-उन्मूलन
- विलुप्त डायर वुल्फ का पुनर्जन्म | विज्ञान की अद्भुत उपलब्धि
- माउंट कनलाओन | Mount Kanlaon
- भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी | सहयोग का नया युग
- RBI रेमिटेंस सर्वेक्षण 2025 | भारत में विदेशी प्रेषण का बदलता परिदृश्य