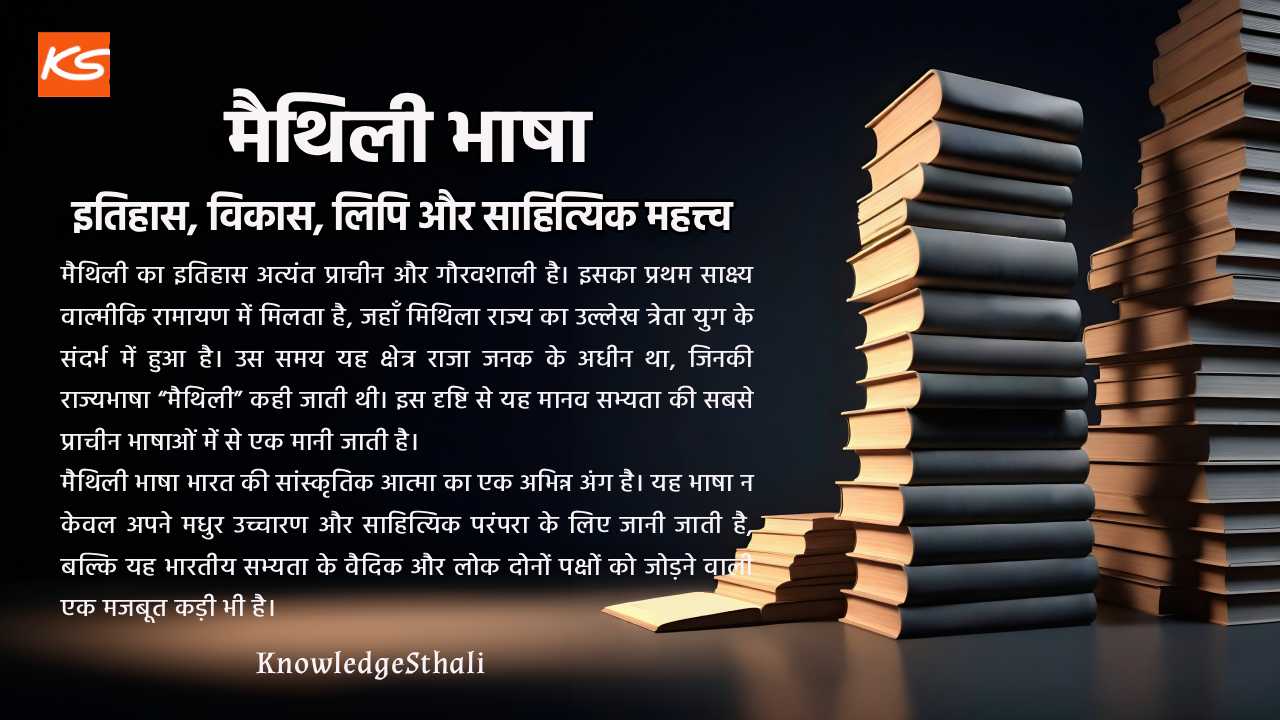भारत की भाषाई विविधता में मैथिली का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण और प्राचीन है। यह भाषा न केवल बिहार और झारखंड राज्यों में, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के तराई क्षेत्र में भी समान रूप से बोली और समझी जाती है। मैथिली का उद्भव हिन्द-आर्य भाषा परिवार की मागधी शाखा से हुआ है, और इसे भारतीय भाषाओं के विकास-क्रम में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इसकी मधुरता, शालीनता और सुसंस्कृत अभिव्यक्ति इसे अन्य बोलियों से अलग बनाती है।
मैथिली मात्र एक बोली नहीं, बल्कि एक समृद्ध साहित्यिक भाषा है, जिसने भारतीय सांस्कृतिक धारा को अभिव्यक्ति देने में सदियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी जड़ें मिथिला की ऐतिहासिक और दार्शनिक परंपरा से जुड़ी हुई हैं — वही मिथिला, जो राजा जनक, सीता, याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विद्वान हस्तियों की भूमि रही है।
मैथिली का भौगोलिक विस्तार
मैथिली भाषा मुख्य रूप से भारत के उत्तर बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं —
दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, वैशाली, सहरसा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर।
भारत के अतिरिक्त, नेपाल के तराई क्षेत्र के आठ जिलों — धनुषा, सिरहा, सुनसरी, सर्लाही, सप्तरी, महोत्तरी, मोरंग और रौतहट में भी मैथिली व्यापक रूप से बोली जाती है। इस प्रकार मैथिली का भौगोलिक विस्तार भारत-नेपाल की सीमा से परे एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में दिखाई देता है।
आज भारत और नेपाल दोनों में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मैथिली को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। यह संख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.6 प्रतिशत है, जो इसे भारत की प्रमुख भाषाओं में शामिल करती है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
मैथिली का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। इसका प्रथम साक्ष्य वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहाँ मिथिला राज्य का उल्लेख त्रेता युग के संदर्भ में हुआ है। उस समय यह क्षेत्र राजा जनक के अधीन था, जिनकी राज्यभाषा “मैथिली” कही जाती थी। इस दृष्टि से यह मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है।
भाषाविज्ञान के अनुसार मैथिली का विकास मागधी प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से हुआ। प्रारंभिक मैथिली का स्वरूप 700 ईस्वी के आसपास स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, जब इसमें साहित्यिक रचनाएँ प्रारंभ हुईं। इसके विकास में अवहट्ट का विशेष योगदान रहा, जो अपभ्रंश और आरंभिक आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी थी।
मैथिली भाषा के सर्वप्रथम उल्लेख 11वीं से 12वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलते हैं, जहाँ इसे “वैदेही” या “तिरहुता” के नाम से संबोधित किया गया है।
मैथिली का विकास और आधुनिक प्रसार
मैथिली भाषा का उद्भव अत्यंत प्राचीन काल में हुआ माना जाता है। इसके प्रारंभिक प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं, जहाँ इसका संबंध मिथिला नरेश राजा जनक के राज्य से बताया गया है। यह उस युग की राजभाषा रही होगी, जिससे इसकी प्राचीनता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इस दृष्टि से मैथिली भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है।
भाषावैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मैथिली का प्रारंभिक विकास मागधी प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ। लगभग सातवीं शताब्दी (700 ईस्वी) के आसपास मैथिली में रचनात्मक साहित्य की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे यह लोकजीवन की सजीव अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई।
मैथिली के विकास में अवहट्ट भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच का संक्रमणीय रूप थी। इस युग में मैथिली साहित्य का उत्कर्ष हुआ और विद्यापति के रूप में इस भाषा ने अपने स्वर्णकाल में प्रवेश किया। विद्यापति को मैथिली का आदिकवि माना जाता है। उन्होंने केवल मैथिली ही नहीं, बल्कि संस्कृत और अवहट्ट में भी विपुल साहित्य रचा। उनके काव्य में भक्ति, प्रेम, सौंदर्य और लोकानुभव की अद्भुत समन्विति देखने को मिलती है।
आज मैथिली भाषा भारत और नेपाल दोनों देशों में व्यापक रूप से बोली जाती है। अनुमानतः 7 से 8 करोड़ लोग इसे मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.6 प्रतिशत है। मिथिला क्षेत्र से बाहर भी मैथिली बोलने वाले समुदाय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, असम, झारखंड, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश, मॉरीशस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में फैले हुए हैं।
भाषा की समृद्धता केवल इसके प्राचीन साहित्य तक सीमित नहीं रही; आधुनिक युग में भी मैथिली निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। आज यह भाषा भारत की राजभाषाओं में से एक है तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान प्राप्त कर चुकी है।
जहाँ एक ओर सरकारी स्तर पर इसके प्रचार-प्रसार के प्रयास अपेक्षाकृत सीमित रहे हैं, वहीं गैर-सरकारी संस्थाएँ, विश्वविद्यालय, सामाजिक संगठन और मीडिया मंच इसके विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
वर्तमान समय में 15 से 20 रेडियो स्टेशन ऐसे हैं जो नियमित रूप से मैथिली में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इन प्रसारणों में समाचार, नाटक, साक्षात्कार, लोकगीत और सांस्कृतिक चर्चाएँ सम्मिलित होती हैं। कुछ रेडियो चैनलों में तो 50 प्रतिशत से अधिक सामग्री मैथिली भाषा में प्रस्तुत की जा रही है। यह प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में तीव्र गति से बढ़ी है और आज भी निरंतर जारी है।
टीवी माध्यमों में भी मैथिली ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नेपाल के कई लोकप्रिय चैनल जैसे — नेपाल वन, सागरमाथा चैनल, तराई टीवी और मकालू टीवी — मैथिली भाषा में समाचार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इससे इस भाषा को न केवल अपने पारंपरिक क्षेत्र में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान प्राप्त हो रही है।
इन नवीन संचार माध्यमों ने मैथिली को आधुनिकता के साथ जोड़ा है और इसे तकनीकी युग में भी सशक्त बनाए रखा है। यह तथ्य इस बात का प्रतीक है कि मैथिली केवल अतीत की भाषा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य दोनों में अपनी पहचान बनाए रखने वाली जीवंत और गतिशील भाषा है।
मैथिली का विकास-क्रम (कालानुक्रमिक सारणी)
| काल | प्रमुख रूप | विशेषताएँ |
|---|---|---|
| मागधी प्राकृत काल (600 ई.पू. – 200 ई.) | मागधी प्राकृत | प्रारंभिक जनभाषा, पाली और जैन ग्रंथों में प्रयोग |
| अपभ्रंश काल (200 ई. – 800 ई.) | अपभ्रंश भाषाएँ | प्राकृत से विकसित रूप, काव्यात्मक भाषा का प्रारंभ |
| मध्यकालीन मैथिली (800 ई. – 1500 ई.) | अवहट्ट और प्रारंभिक मैथिली | विद्यापति युग, मैथिली साहित्य का स्वर्णकाल |
| आधुनिक मैथिली (1500 ई. – वर्तमान) | मानकीकृत मैथिली | देवनागरी लिपि में लेखन, साहित्य, शिक्षा और संविधान में मान्यता |
मैथिली लिपि
मैथिली की लिपि का इतिहास भी उसकी भाषा जितना ही समृद्ध और रोचक है। प्रारंभ में इसे मिथिलाक्षर या कैथी लिपि में लिखा जाता था। मिथिलाक्षर को तिरहुता या वैदेही लिपि के नाम से भी जाना जाता है।
यह लिपि बांग्ला, असमिया और उड़िया लिपियों की जननी मानी जाती है। वास्तव में, विद्वानों के अनुसार, मैथिली लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ था, जो नागरी लिपि के उत्तर-पूर्व भारत में प्रचार से बहुत पहले ही प्रचलन में आ चुकी थी।
बौद्ध ग्रंथ ‘ललितविस्तर’ में इसका उल्लेख “वैदेही” नाम से मिलता है। इस लिपि में लिखित प्राचीन ग्रंथों का प्रमाण जापान और चीन जैसे देशों में भी मिलता है, जो मिथिला की सांस्कृतिक पहुंच को दर्शाता है।
कालांतर में देवनागरी लिपि के प्रसार और मुद्रण तकनीक के विकास के साथ मैथिली में देवनागरी लिपि का प्रयोग व्यापक हो गया। आज अधिकांश मैथिली साहित्य, पत्रकारिता और शिक्षण देवनागरी लिपि में ही होता है।
मैथिली साहित्यिक परंपरा और प्रमुख कवि
मैथिली साहित्य का इतिहास अत्यंत समृद्ध है। इसका स्वर्णयुग चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी में माना जाता है, जब महाकवि विद्यापति ने अपनी काव्य-प्रतिभा से इसे विश्वविख्यात बनाया।
विद्यापति : मैथिली के आदिकवि
विद्यापति न केवल मैथिली साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, बल्कि उन्हें आदिकवि के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने मैथिली के अतिरिक्त संस्कृत और अवहट्ट में भी रचनाएँ कीं। उनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम, नीति और सौंदर्य का अद्भुत संगम है।
विद्यापति की रचनाएँ, विशेषकर उनकी शिव-भक्ति की कविताएँ और राधा-कृष्ण प्रेम गीत, आज भी मिथिला की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं।
अन्य प्रमुख कवि और साहित्यकार
मैथिली के अन्य प्रमुख कवियों और लेखकों में गोविन्ददास, हरिमोहन झा, चंदा झा, यशोधर झा ‘यात्री’, राजकमल चौधरी, नागेन्द्र झा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
इन कवियों और लेखकों ने मैथिली में प्रेम, लोकजीवन, हास्य-व्यंग्य, दर्शन और सामाजिक चेतना के विविध विषयों पर लेखन किया। हरिमोहन झा की रचनाएँ अपनी हास्य-व्यंग्य शैली के कारण आज भी लोकप्रिय हैं।
मैथिली लोकसाहित्य
मैथिली का लोकसाहित्य अत्यंत समृद्ध है। इसमें लोकगीत, सोहर, विवाह गीत, झूमर, बिरहा और पर्वगीत शामिल हैं। इन गीतों में मिथिला की संस्कृति, भावनाएँ, ऋतुचक्र, लोकमान्यताएँ और धार्मिकता की गहरी झलक मिलती है।
मैथिली की भाषिक विशेषताएँ
मैथिली की अपनी विशिष्ट ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक संरचना है, जो इसे हिंदी, भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाओं से अलग करती है।
मुख्य भाषिक विशेषताएँ
- ध्वनि-परिवर्तन: ‘श’, ‘ष’ और ‘स’ के स्थान पर ‘ह’ का प्रयोग — उदाहरण: पुष्प → पुहुप।
- स्वर-प्रचुरता: मैथिली में स्वर अधिक प्रचुर हैं, जिससे इसकी ध्वनि को मधुरता प्राप्त होती है।
- व्याकरणिक संरचना: संज्ञा और क्रिया के रूपों में संख्या, लिंग और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है।
- तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग: मैथिली पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है; कई शब्द संस्कृत से तत्सम या तद्भव रूप में ग्रहण किए गए हैं।
- सांस्कृतिक शब्दावली: मैथिली में मिथिला की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवनशैली से संबंधित अनेक स्थानीय शब्द हैं — जैसे अंगना, सोहर, बखरी, नेम-धेम आदि।
संविधान में मैथिली की स्थिति
मैथिली भाषा को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक मान्यता वर्ष 2003 में प्रदान की गई, जब इसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
इस निर्णय की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुपौल जिले के निर्मली में की थी। इस प्रकार मैथिली भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में सम्मिलित हो गई।
नेपाल में भी मैथिली को विशेष दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2007 के नेपाल के अन्तरिम संविधान में मैथिली को प्रादेशिक राजभाषा और क्षेत्रीय नेपाली भाषा का दर्जा दिया गया। वहीं झारखंड राज्य में इसे द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
मैथिली का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व
मैथिली केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक संस्कृति और जीवन-शैली है। मिथिला क्षेत्र के त्यौहार, संगीत, नृत्य, लोककथाएँ और धार्मिक परंपराएँ इस भाषा में रची-बसी हैं। मिथिला पेंटिंग (मधुबनी कला) का सौंदर्य भी मैथिली संस्कृति का ही विस्तार है।
इस भाषा में निहित शालीनता, विनम्रता और भावनात्मकता इसके बोलने वालों के स्वभाव में झलकती है। मैथिली लोकगीतों में स्त्री के स्नेह, विरह, और भक्ति की गहन अनुभूति प्रकट होती है।
आधुनिक युग में मैथिली
21वीं शताब्दी में भी मैथिली भाषा अपने अस्तित्व और विकास की दिशा में निरंतर अग्रसर है। हालांकि सरकारी स्तर पर इसके संवर्द्धन के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं, परंतु गैर-सरकारी संस्थाएँ, साहित्यिक संगठन, विश्वविद्यालय और मीडिया मंच अब मैथिली के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
मैथिली साहित्य परिषद, विद्यापति सेवा संस्थान, ऑल इंडिया मैथिली मंच जैसी संस्थाएँ नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों और पुरस्कार कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।
डिजिटल युग में मैथिली के लिए कई वेबसाइटें, यूट्यूब चैनल, और ऑनलाइन पत्रिकाएँ सक्रिय हैं। मैथिली विकिपीडिया (mai.wikipedia.org) इस भाषा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।
चुनौतियाँ और भविष्य
यद्यपि मैथिली को संविधानिक मान्यता प्राप्त है, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं —
- शिक्षा और प्रशासनिक स्तर पर इसका सीमित प्रयोग।
- नई पीढ़ी में हिंदी या अंग्रेज़ी की ओर झुकाव।
- सरकारी पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथिली का अभाव।
इन चुनौतियों के बावजूद मैथिली का भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते इसके संरक्षण और प्रचार के लिए समाज और सरकार मिलकर प्रयास करें।
निष्कर्ष
मैथिली भाषा भारत की सांस्कृतिक आत्मा का एक अभिन्न अंग है। यह भाषा न केवल अपने मधुर उच्चारण और साहित्यिक परंपरा के लिए जानी जाती है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के वैदिक और लोक दोनों पक्षों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी भी है।
विद्यापति की काव्यधारा से लेकर आधुनिक लेखकों के समाज-सापेक्ष साहित्य तक, मैथिली ने हर युग में अपनी पहचान को सशक्त किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस भाषा को शिक्षा, प्रशासन और तकनीक के क्षेत्र में और अधिक स्थान मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा सकें।
इस प्रकार मैथिली भाषा न केवल बिहार या नेपाल की, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है — एक ऐसी भाषा, जिसमें प्रेम की मधुरता, भक्ति की गहराई और संस्कृति की सुगंध एक साथ प्रवाहित होती है।
इन्हें भी देखें –
- मैथिली साहित्य: आदिकाल से आधुनिक युग तक
- मगही या मागधी भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि और साहित्यिक परंपरा
- संस्कृत भाषा : इतिहास, उत्पत्ति, विकास, व्याकरण, लिपि और महत्व
- कन्नड़ भाषा : उत्पत्ति, इतिहास, लिपि, वर्णमाला, शब्द, वाक्य और साहित्य
- कोंकणी भाषा : इतिहास, विकास, लिपि, वर्णमाला, शब्द-संरचना, वाक्य-रचना और साहित्यिक विरासत
- ब्राह्मी लिपि से आधुनिक भारतीय लिपियों तक: उद्भव, विकास, शास्त्रीय प्रमाण, अशोक शिलालेख
- पाठ्य-मुक्तक और गेय-मुक्तक : परिभाषा, विशेषताएँ, उदाहरण, विश्लेषण, साहित्यिक महत्व
- गीत : स्वर, ताल, लय और भावों की भारतीय परंपरा
- महिला क्रिकेट विश्व कप 2025: भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास
- निपाह वायरस (Nipah Virus) : भारत में स्वदेशी उपचार विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम
- एन्सेफैलोमायोकार्डाइटिस वायरस (EMCV): एक उभरता हुआ घातक पशु संक्रमण