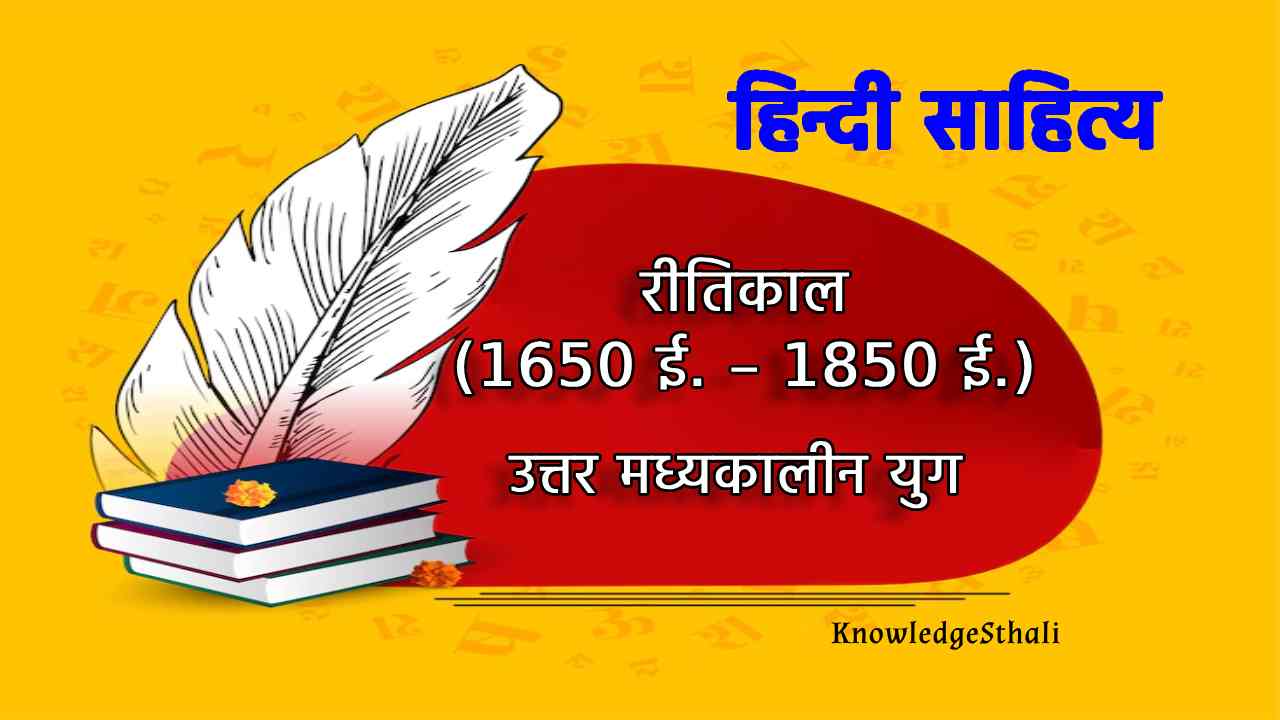हिंदी साहित्य का इतिहास अपने विविधता भरे काल-विभाजनों के लिए प्रसिद्ध है। आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के बीच का यह युग, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, हिंदी काव्यधारा का एक विशेष और विशिष्ट अध्याय है। यह काल न केवल साहित्यिक शैलियों के विकास के लिए, बल्कि दरबारी संस्कृति और शृंगारिक प्रवृत्तियों के उत्कर्ष के लिए भी स्मरणीय है। रीतिकाल का समय-सीमा आमतौर पर 1650 ई. से 1850 ई. तक मानी जाती है। इस काल को लेकर विद्वानों में नामकरण, स्वरूप और महत्व पर काफी मतभेद भी हैं, जो इसे और रोचक बनाते हैं।
हिंदी साहित्य का रीतिकाल (1650 ई. – 1850 ई.)
रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी विशेषताओं के कारण अलग पहचान रखता है। रीतिकाल में काव्य के शास्त्रीय नियमों और लक्षणों का अनुपालन विशेष रूप से हुआ। रस, अलंकार, रीति, नायिका भेद और संचारी भावों पर कवियों ने गहनता से कार्य किया। इस युग की कविता में शृंगार रस का आधिपत्य रहा। नायक-नायिका के प्रेम, उनकी मनोभावनाओं, विरह और मिलन के अत्यंत नाजुक चित्रण ने रीतिकाव्य को विशिष्ट बना दिया। रीतिकाल मुख्यतः मुक्तक रचनाओं का युग था। इसमें कवित्त, सवैये, और दोहे प्रमुख छंद रहे।
कवियों की अधिकांश रचनाएँ दरबारों में हुईं। वे राजाओं के आश्रित थे, जिससे कविता में चमत्कारपूर्ण व्यंजना तो आई, लेकिन यह सामान्य जनता से विमुख हो गई। इस काल के कवि कलात्मक और चमत्कारपूर्ण अलंकारों के प्रयोग में दक्ष थे। उनके लिए काव्य एक सजग कला और शिल्प का क्षेत्र था।
रीतिकाल : नामकरण और अवधारणात्मक मतभेद
रीतिकाल शब्द अपने आप में ही रीति और काल से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य उस युग से है जिसमें काव्य में “रीति” अर्थात् काव्यशास्त्रीय नियमों, अलंकारों, रसों और नायिका भेद आदि की प्रधानता थी। किंतु इस युग को केवल रीतियों तक सीमित करना इसके बहुआयामी स्वरूप को संकुचित कर देता है।
हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का नामकरण विवादास्पद रहा है। विभिन्न विद्वानों ने इस काल को अलग-अलग नामों से परिभाषित किया है—
- मिश्र बंधु ने इसे “अलंकृत काल” कहा, जो इस युग की अलंकार प्रधानता की ओर संकेत करता है।
- विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार यह “शृंगार काल” है। इन्होने इसे श्रृंगारकाल नाम देकर शृंगार रस की अत्यधिक उपस्थिति को रेखांकित किया।
- जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे “रीतिकाल” कहा और यही नाम सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का “रीतिकाल” कहना इसके रीतिमूलक साहित्यिक ढांचे की ओर इंगित करता है।
यहाँ “रीति” का अर्थ है काव्यरीति या काव्यशास्त्र, क्योंकि इस काल के कवियों ने रस, अलंकार, नायिका भेद, और काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति से निरूपण किया। इस प्रकार काव्य में रीति-निष्णात प्रवृत्तियों के कारण इसे रीतिकाव्य या रीतिकाल कहा गया।
इन नामों से यह स्पष्ट होता है कि इस युग की विविध प्रवृत्तियों को लेकर विद्वानों की भिन्न-भिन्न दृष्टियां रहीं हैं, और सभी दृष्टियों का यथार्थ एक ही युग को विभिन्न कोणों से देखने का प्रयास है।
रीतिकाल का उद्भव: आचार्यों के विचार
रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि रीतिकाल की कविता का जन्म जनता की रुचि से नहीं, बल्कि आश्रयदाता राजाओं और दरबारों की अभिरुचि से हुआ। उन्होंने कहा:
“इस काल की कविता आश्रयदाताओं की रुचि का परिणाम है। वीरता और कर्मण्यता का जीवन समाप्त हो चुका था। अतः कविता केवल चमत्कारपूर्ण शृंगारिकता में लिप्त हो गई।”
हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, यदि भक्तिकाल के कवियों ने प्राचीन संस्कृत साहित्य (विशेषकर रामायण और महाभारत) से प्रेरणा ली, तो रीतिकाल के कवियों ने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रभाव ग्रहण किया। इस प्रभाव में नायिका भेद, अलंकारशास्त्र, संचारी भाव और लक्ष्मण ग्रंथों की परंपरा सम्मिलित थी।
रीतिकाव्य की प्रवृत्तियां
रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है:
1. शृंगार रस की प्रधानता
रीतिकाव्य की आत्मा शृंगार रस है। इस युग में शृंगार रस के दो रूप—संयोग और वियोग—का विशद चित्रण मिलता है, किंतु संयोग शृंगार का पक्ष अधिक प्रभावशाली रहा। नायक-नायिका के सौंदर्य, प्रेम-प्रसंग, हाव-भाव, नख-शिख वर्णन आदि विषय प्रमुख रहे।
2. नायिका भेद
इस युग में नायिकाओं के विविध भेदों का विश्लेषण किया गया। स्थायी, संचारी और व्यभिचारी भावों को आधार बनाकर नायिकाओं का वर्गीकरण किया गया। अभिसारिका, खंडिता, वासकसज्जा, स्वाधीनभर्तृका आदि नायिका भेदों का सुंदर वर्णन मिलता है।
3. लक्षण-लक्ष्य शैली
इस युग में रचनाएं अधिकतर लक्षण-लक्ष्य शैली में लिखी गईं। काव्यशास्त्र के सिद्धांतों को दोहों में लक्षण रूप में प्रस्तुत किया गया तथा कवित्त या सवैया छंदों में उदाहरण स्वरूप लक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
4. मुक्तक काव्य की प्रमुखता
रीतिकालीन कवियों ने प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक काव्य की रचना को अधिक महत्व दिया। सवैया, कवित्त और दोहे प्रमुख छंद थे जिनमें सौंदर्य, प्रेम, नायिका भेद, ऋतु वर्णन आदि को अत्यंत कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया।
5. राजाश्रय और दरबारी संस्कृति
रीतिकाव्य दरबारी संस्कृति की उपज थी। कवि दरबारों में आश्रय प्राप्त कर अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में काव्य रचते थे। इससे साहित्य में यथार्थ से दूरी और कृत्रिमता बढ़ी, लेकिन कला की दृष्टि से यह युग उत्कृष्ट रहा।
रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके दरबार
रीतिकाल में अनेक कवि हुए, जिन्होंने काव्यशास्त्र के विविध अंगों पर अद्भुत रचनाएँ कीं। इनमें कई कवि स्वयं शासक थे, और कई शासकों के आश्रय में काव्य रचना करते थे। नीचे रीतिकाल के प्रमुख कवियों और उनके आश्रयदाताओं की सूची दी गई है:
| क्रम संख्या | रीतिकाल के कवि | दरबार / आश्रयदाता |
|---|---|---|
| 1. | केशवदास | ओरछा |
| 2. | प्रताप सिंह | चरखारी |
| 3. | बिहारी | जयपुर, आमेर |
| 4. | मतिराम | बूँदी |
| 5. | भूषण | पन्ना |
| 6. | चिंतामणि | नागपुर |
| 7. | देव | पिहानी |
| 8. | भिखारीदास | प्रतापगढ़-अवध |
| 9. | रघुनाथ | काशी |
| 10. | बेनी | किशनगढ़ |
| 11. | गंग | दिल्ली |
| 12. | टीकाराम | बड़ौदा |
| 13. | ग्वाल | पंजाब |
| 14. | चन्द्रशेखर बाजपेई | पटियाला |
| 15. | हरनाम | कपूरथला |
| 16. | कुलपति मिश्र | जयपुर |
| 17. | नेवाज | पन्ना |
| 18. | सुरति मिश्र | दिल्ली |
| 19. | कवीन्द्र उदयनाथ | अमेठी |
| 20. | ऋषिनाथ | काशी |
| 21. | रतन कवि | श्रीनगर-गढ़वाल |
| 22. | बेनी बन्दीजन | अवध |
| 23. | बेनी प्रवीन | लखनऊ |
| 24. | ब्रह्मदत्त | काशी |
| 25. | ठाकुर बुन्देलखण्डी | जैतपुर |
| 26. | बोधा | पन्ना |
| 27. | गुमान मिश्र | पिहानी |
कई कवि तो स्वयं राजा थे, जैसे:
- महाराज जसवंत सिंह (तिर्वा)
- भगवंत राय खींची
- भूपति
- रसनिधि (दतिया के जमींदार)
- महाराज विश्वनाथ
- द्विजदेव (महाराज मानसिंह)
रीतिकाव्य का आरंभ: केशवदास या चिंतामणि?
रीतिकाव्य की शुरुआत को लेकर विद्वानों में मतभेद है।
केशवदास का योगदान (1555–1617 ई.)
आचार्य केशवदास को कई विद्वान रीतिकाव्य का आरंभकर्ता मानते हैं। उन्होंने कविप्रिया, रसिकप्रिया और रामचंद्रिका जैसी महत्वपूर्ण रचनाएँ कीं।
- कविप्रिया में अलंकारों का शास्त्रीय विवेचन है।
- रसिकप्रिया में रसों का सोदाहरण निरूपण किया गया।
- रामचंद्रिका में भक्ति के स्थान पर कलात्मकता और शिल्प कौशल की झलक मिलती है।
चिंतामणि त्रिपाठी (17वीं सदी)
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार केशवदास ने भले ही रीतिग्रंथों की रचना की हो, किंतु रीतिकाव्य की अविरल और अखंड परंपरा की शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से होती है। उन्होंने कहा:
““केशवदास ने काव्य के अंगों का शास्त्रीय निरूपण किया, लेकिन हिंदी रीतिग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से ही प्रारंभ होती है। अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए।”
इस दृष्टिकोण के अनुसार, चिंतामणि और उनके समकालीन कवियों ने एक निश्चित काव्यरीति को परिपक्व रूप में प्रस्तुत किया जिससे रीतिकाव्य का विधिवत उद्भव हुआ।
रीतिकाल का साहित्यिक मूल्यांकन
रीतिकाल को अक्सर “दरबारी कविता का युग” कहा गया है। इसकी आलोचना यह कहकर की गई कि यह जनता से कटा हुआ और केवल सौंदर्यबोध में डूबा हुआ था। किंतु यह भी सत्य है कि इस काल में हिंदी काव्यशास्त्र को गहन आधार मिला। अलंकार, रस और नायिका भेद जैसे तत्वों का सुचिंतित निरूपण रीतिकाल की अमूल्य देन है।
रीतिकाल के कवि: तीन धाराएँ
हिंदी साहित्य का इतिहास अपने विविध कालखंडों में विभाजित है, जिनमें प्रत्येक काल की अपनी विशिष्टताएँ हैं। इसमें रीतिकाल (1650 ई.–1850 ई.) का स्थान विशेष महत्व रखता है। यह युग मुख्यतः श्रृंगारिक और आलंकारिक काव्य की प्रधानता के लिए जाना जाता है। इस काल के कवियों ने काव्यशास्त्र, रस, अलंकार और नायिकाभेद पर विशेष बल दिया, जिससे हिंदी काव्य में एक नया सौंदर्यबोध विकसित हुआ।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को “काव्य में रीति का युग” कहा है। वास्तव में, इस युग ने काव्य को कला, कल्पना और शास्त्रीय अनुशासन के माध्यम से समृद्ध किया।
रीतिकाल के कवियों को उनके काव्य-स्वभाव और रीति परंपरा के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर तीन प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है:
✅ रीतिबद्ध कवि
✅ रीतिसिद्ध कवि
✅ रीतिमुक्त कवि
ये तीनों धाराएँ रीतिकाल की विविधता और उसकी कलात्मक ऊँचाई का परिचायक हैं। आइए, इन तीनों वर्गों के कवियों और उनके काव्य योगदान का विस्तृत और सुस्पष्ट परिचय प्राप्त करें।
रीतिबद्ध कवि: रीति परंपरा के सजग वाहक
रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रत्यक्ष रूप से काव्यशास्त्र के नियमों और लक्षण ग्रंथों का अनुसरण किया। इनके काव्य में रीति परंपरा का कठोर अनुपालन दिखाई देता है। उन्होंने रस, अलंकार और नायिका भेद जैसे शास्त्रीय तत्वों को अपने काव्य का मूल आधार बनाया।
इन कवियों ने शृंगार रस को केंद्र में रखते हुए अलंकारों के चमत्कारपूर्ण प्रयोग और शब्दों की कलात्मकता से हिंदी काव्य को नया सौंदर्य प्रदान किया। उनके काव्य में सौंदर्य, विलास और श्रृंगार की दुनिया बसती है।
प्रमुख रीतिबद्ध कवि – केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, सेनापति और देव।
इनमें केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने “कठिन काव्य का प्रेत” कहा। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि केशवदास का काव्य गूढ़ और काव्यशास्त्रीय जटिलताओं से परिपूर्ण था, जो साधारण जन के लिए सहज नहीं था। जबकि देव अपने अनुप्रास और यमक प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हुए। मतिराम और सेनापति ने भी शृंगारिक काव्य को विलक्षण ऊँचाई दी।
रीतिबद्ध कवियों ने काव्यशास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इस वर्ग के प्रमुख कवियों – केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, सेनापति और देव का विवरण नीचे दिया गया है:
आचार्य केशवदास: कठिन काव्य का प्रेत
जन्म और जीवन परिचय
आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ई. में ओरछा (मध्यप्रदेश) में हुआ। वे जिझौतिया ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम काशीनाथ था। केशवदास का परिवार ओरछा दरबार में अत्यंत प्रतिष्ठित था। स्वयं केशवदास ओरछा नरेश महाराज रामसिंह के भाई इन्द्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इन्द्रजीत सिंह ने उन्हें इक्कीस गाँवों का अनुदान दिया था।
केशवदास एक आत्मसम्मानी और विलासमय जीवन जीने वाले कवि थे। उनका काव्य गहन शास्त्रीयता से युक्त था और उन्होंने हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना कर इस युग को साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध किया।
रचनाएँ
केशवदास की प्रमुख रचनाएँ हैं –
- रसिकप्रिया
- कविप्रिया
- रामचंद्रिका
- वीर सिंहदेव चरित
- जहांगीर जसचंद्रिका
विशेषताएँ
केशवदास की काव्य शैली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। उन्होंने रसिकप्रिया में नायिकाओं और नायक के भेद, अलंकारों और काव्यशास्त्र के नियमों का विवेचन किया। उनका काव्य उस समय के दरबारी वातावरण का सजीव प्रतिबिंब है।
चिंतामणि: कविकुलकल्पतरु के रचयिता
जीवन परिचय
चिंतामणि यमुना के समीपवर्ती गाँव टिकमापुर (या त्रिविक्रमपुर, जिला कानपुर) के निवासी थे। वे काश्यप गोत्रीय कान्यकुब्ज त्रिपाठी ब्राह्मण थे। उनका जन्म संवत् 1666 विक्रमी और रचनाकाल संवत् 1700 विक्रमी माना जाता है।
उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी (कहीं-कहीं रतिनाथ भी उल्लेखित) था। चिंतामणि प्रसिद्ध कविवर भूषण, मतिराम और नीलकंठ के ज्येष्ठ भ्राता थे।
रचनाएँ
अब तक चिंतामणि की निम्नलिखित रचनाएँ ज्ञात हैं –
- काव्यविवेक
- कविकुलकल्पतरु
- काव्यप्रकाश
- छंदविचार पिंगल
- रामायण
- रसविलास
- शृंगारमंजरी
- कृष्णचरित
इनमें कविकुलकल्पतरु का विशेष महत्व है। यह संस्कृत के काव्यप्रकाश ग्रंथ के आदर्श पर आधारित है और इसे चिंतामणि की कीर्ति का मुख्य आधार माना जाता है।
विशेषताएँ
चिंतामणि के काव्य में काव्यशास्त्रीय गहनता और परंपरा का निर्वाह स्पष्ट दिखाई देता है। वे न केवल काव्य के रचनाकार थे, बल्कि काव्यशास्त्र के गंभीर अध्येता भी थे।
मतिराम: रसराज के सृजक
जीवन परिचय
मतिराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रजभाषा कवि थे। उनका जन्म संवत् 1660 विक्रमी के आसपास माना जाता है। वे चिंतामणि और भूषण के छोटे भाई थे।
रचनाएँ
मतिराम की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं –
- फूलमंजरी
- रसराज
- ललित ललाम
- मुक्तावली
- नखसिख
- श्रृंगारशतक
- रसपंचाध्यायी
- रसचूड़ामणि
इनमें रसराज उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कृति है। यह श्रृंगार रस और नायिकाभेद पर केंद्रित है।
विशेषताएँ
मतिराम के काव्य में भावों की कोमलता, शब्दों की ललितता और श्रृंगारिक सौंदर्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। रसराज को रीतिकाल का बिहारी सतसई कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी संक्षिप्त और प्रभावशाली दोहों का उपयोग हुआ है।
सेनापति: कवित्त रत्नाकर के रचयिता
जीवन परिचय
सेनापति रीतिकाल के प्रारंभिक चरण के अत्यंत प्रतिभाशाली ब्रजभाषा कवि माने जाते हैं। उनके जीवन का विस्तृत विवरण दुर्लभ है और उनका परिचय मुख्यतः उनकी एकमात्र उपलब्ध कृति ‘कवित्त रत्नाकर’ पर आधारित है। सेनापति का वास्तविक नाम अज्ञात है, लेकिन उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है कि वे विदग्ध काव्य परंपरा के समर्थ कवि थे।
रचनाएँ
सेनापति के दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है –
- कवित्त रत्नाकर
- काव्यकल्पद्रुम
हालाँकि, वर्तमान में केवल कवित्त रत्नाकर ही उपलब्ध है। काव्यकल्पद्रुम अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।
कवित्त रत्नाकर का रचनाकाल संवत् 1706 विक्रमी माना जाता है। यह ग्रंथ पांच तरंगों में विभाजित है –
- प्रथम तरंग: 97 कवित्त
- द्वितीय तरंग: 74 कवित्त
- तृतीय तरंग: 62 कवित्त और 8 कुंडलिया
- चतुर्थ तरंग: 76 कवित्त
- पंचम तरंग: 88 कवित्त
इस प्रकार, इस ग्रंथ में कुल 405 छंद संग्रहीत हैं।
विशेषताएँ
सेनापति का काव्य प्रौढ़ता और शिल्प सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। उनके छंदों में लालित्य और श्लेषयुक्तता का सुंदर सामंजस्य है। श्रृंगार, षट्ऋतु वर्णन और रामकथा के छंद विशेष रूप से उत्कृष्ट हैं। सेनापति की भाषा में काव्य की कोमलता और भावुकता स्पष्ट झलकती है। उन्होंने ध्वनि योजना और काव्य लालित्य के माध्यम से हिंदी काव्य को समृद्ध किया।
देव: अनुप्रास और यमक के जादूगर
जीवन परिचय
देव रीतिकाल के प्रमुख रीतिग्रंथकार कवि हैं। उनका पूरा नाम देवदत्त था। वे अपने जीवनकाल में विभिन्न आश्रयदाताओं के संपर्क में रहे। औरंगजेब के पुत्र आलमशाह के दरबार में भी उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। बाद में उन्हें सर्वाधिक संतोष और सम्मान भोगीलाल नामक सहृदय आश्रयदाता के यहाँ मिला। भोगीलाल ने देव के काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति का दान दिया।
रचनाएँ
देव की काव्य प्रतिभा का प्रमाण उनकी विपुल साहित्यिक कृतियाँ हैं। उनकी कुल रचनाओं की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। प्रमुख रचनाएँ हैं –
- रसविलास
- भावविलास
- भवानीविलास
- कुशलविलास
- अष्टयाम
- सुमिल विनोद
- सुजानविनोद
- काव्यरसायन
- प्रेमदीपिका
- प्रेमचंद्रिका
इन रचनाओं में श्रृंगार रस, नायिका भेद और काव्यशास्त्रीय अलंकरणों का अद्भुत मिश्रण है।
विशेषताएँ
देव के काव्य में अनुप्रास और यमक का अत्यंत कलात्मक प्रयोग मिलता है। उनके छंदों में ध्वनि योजना इतनी उत्कृष्ट है कि पंक्ति दर पंक्ति में शब्दों का संगीत झंकृत होता है। देव ने श्रृंगार रस के उदात्त रूप का सौंदर्यपूर्ण चित्रण किया है। उनके कवित्त और सवैये प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र प्रस्तुत करते हैं।
उनके काव्य में जहाँ एक ओर रूप-सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण है, वहीं दूसरी ओर रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है।
रीतिबद्ध कवियों का साहित्यिक महत्व
रीतिबद्ध कवियों ने हिंदी साहित्य को काव्यशास्त्रीय दृष्टि से समृद्ध किया। उन्होंने रस, अलंकार और नायिकाभेद की बारीकियों को अपने काव्य में सजाया। यद्यपि इनका काव्य सामान्य जन के लिए कठिन प्रतीत होता है, फिर भी काव्यशास्त्र के विद्यार्थी और साहित्य प्रेमियों के लिए यह अत्यंत मूल्यवान है।
केशवदास, चिंतामणि और मतिराम जैसे कवियों ने रीतिकाल की काव्य परंपरा को एक नई ऊँचाई दी। उनकी रचनाएँ आज भी हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए अध्ययन का विषय हैं।
रीतिसिद्ध कवि: रीति परंपरा का संतुलित अनुकरण
रीतिसिद्ध कवि वे हैं जिन्होंने काव्यशास्त्र का गहन अध्ययन कर उसे अपने काव्य में सहज और स्वाभाविक ढंग से आत्मसात किया। ये कवि रीति परंपरा के अनुयायी तो हैं, परंतु उन्होंने उसमें जड़ता या कृत्रिमता को स्थान न देकर भावों की स्वाभाविकता को प्रमुखता दी।
इनका काव्य न तो रीतिबद्ध कवियों की तरह कठोर शास्त्रीय अनुकरण का उदाहरण है और न ही रीतिमुक्त कवियों की भाँति परंपरा से विद्रोह। यह संतुलन ही रीतिसिद्ध कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है। उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ व्यंजना, माधुर्य और सहजता का अनूठा समन्वय दिखाई देता है।
रीतिसिद्ध कवियों के काव्य में श्रृंगार रस का वर्चस्व है, लेकिन उसमें केवल रीति की रूढ़िबद्धता नहीं, बल्कि भावों की स्वाभाविकता और काव्यशास्त्र का गहन अध्ययन भी झलकता है। इस वर्ग के कवियों में बिहारी और रसनिधि प्रमुख स्थान रखते हैं, जिनकी रचनाओं ने रीतिकाल की काव्य परंपरा को एक नयी ऊँचाई दी।
प्रमुख रीतिसिद्ध कवि – बिहारी और रसनिधि।
बिहारी की “सतसई” शृंगारिक भावों का सार है और हिंदी साहित्य की कालजयी कृति मानी जाती है। रसनिधि का “रतनहजारा” बिहारी की दोहापद्धति पर आधारित है, लेकिन उसमें फारसी शायरी का भी असर दिखता है।
बिहारी: सतसई के अमर कवि
जीवन परिचय
बिहारीलाल रीतिकाल के श्रेष्ठतम कवियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म संवत् 1595 (1538 ई.) में ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे (चतुर्वेदी) थे। उनके पिता का नाम केशवराय था। जब बिहारी केवल आठ वर्ष के थे, तब उनके पिता उन्हें ओरछा ले आए। उनका बचपन बुंदेलखंड के सांस्कृतिक वातावरण में बीता।
बिहारी के गुरु नरहरिदास थे। युवावस्था का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने ससुराल मथुरा में व्यतीत किया, जिसने उनके काव्य में राधा-कृष्ण भक्ति और ब्रज संस्कृति के गहन प्रभाव को जन्म दिया।
रचनाएँ
बिहारी की ख्याति उनके एकमात्र ग्रंथ ‘सतसई’ पर आधारित है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का अद्भुत रत्न है जिसमें केवल सात सौ सैंतीस (737) दोहे हैं।
सतसई के दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, किन्तु इनमें नीति, भक्ति, प्रकृति और दर्शन के भी अनेक अनमोल विचार समाहित हैं। बिहारी का काव्य संक्षिप्तता में गहराई और व्यंजना की दृष्टि से अद्वितीय है।
विशेषताएँ
1. श्रृंगार रस का सूक्ष्म चित्रण
बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत सजीव और कोमल चित्रण किया है। संयोग में नायिकाओं के हावभाव, लज्जा, उल्लास और चंचलता का सुंदर वर्णन मिलता है –
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।
सोह करे, भौंहनु हंसे दैन कहे, नटि जाय॥
वहीं वियोग में बिहारी ने नायिकाओं की व्याकुलता और विरह-वेदना का मार्मिक वर्णन किया है। हालांकि, उनके वियोग वर्णन में कहीं-कहीं अतिशयोक्ति भी दिखाई देती है –
इति आवत चली जात उत, चली, छसातक हाथ।
चढी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनु साथ॥
2. सूफी प्रभाव
बिहारी पर सूफी कवियों की अहात्मक पद्धति का भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने विरह की तीव्रता को इस प्रकार व्यक्त किया –
औंधाई सीसी सुलखि, बिरह विथा विलसात।
बीचहिं सूखि गुलाब गो, छीटों छुयो न गात॥
3. भक्ति भावना
यद्यपि बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, उनके काव्य में राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति भी प्रकट होती है। सतसई के आरंभ में राधा के प्रति यह मंगला-चरण उनकी भक्ति-भावना का प्रमाण है –
मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोय।
जा तन की झाई परे, स्याम हरित दुति होय॥
4. नीति और ज्ञान
बिहारी ने कुछ नीति और ज्ञान से युक्त दोहे भी लिखे हैं। उदाहरण के लिए धन-संग्रह पर उनका यह दोहा –
मति न नीति गलीत यह, जो धन धरिये जोर।
खाये खर्चे जो बचे तो जोरिये करोर॥
5. प्रकृति चित्रण
प्रकृति-चित्रण में बिहारी का स्थान भी अत्यंत उच्च है। उन्होंने ऋतुओं के बदलते रंग और सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु का यह चित्र –
कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ।
जगत तपोतवन सो कियो, दारिग़ दाघ निदाघ॥
6. भाषा और शैली
बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। इसमें सूरदास की चलती ब्रजभाषा का परिष्कृत और विकसित रूप मिलता है। उनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू और फारसी के शब्दों का भी सुंदर समावेश है।
शब्दों का चयन अत्यंत सार्थक और भावों के अनुरूप है। उन्होंने कहीं-कहीं मुहावरों का भी चमत्कारपूर्ण उपयोग किया है –
मूड चढाऐऊ रहै फरयौ पीठि कच-भारु,
रहै गिरैं परि, राखिबौ तऊ हियैं पर हारु॥
7. शैली के प्रकार
बिहारी की शैली विषय के अनुसार तीन प्रकार की मानी जाती है –
- माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली – वियोग के दोहों में।
- प्रसादगुण से युक्त सरस शैली – भक्ति और नीति के दोहों में।
- चमत्कारपूर्ण शैली – दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषयक दोहों में।
बिहारी की सतसई का हर दोहा अल्पाक्षर में व्यापक अर्थ की दृष्टि से अद्वितीय है। उनका काव्य भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से रीतिकालीन काव्य परंपरा का शिखर है।
रसनिधि: प्रेम की विविध दशाओं के कवि
जीवन परिचय
रसनिधि रीतिकाल के उन कवियों में हैं जिन्होंने प्रेम की विविध दशाओं और चेष्टाओं का अपने काव्य में सुंदर चित्रण किया। उनका वास्तविक नाम पृथ्वीसिंह था। वे दतिया राज्य के बरौनी क्षेत्र के जमींदार थे और ‘रसनिधि’ उपनाम से काव्य रचना करते थे।
इनका रचनाकाल संवत् 1660 से 1717 विक्रमी तक माना जाता है। रसनिधि का जीवन दरबारी जगत से दूर, एक रसिक और प्रेमशील कवि के रूप में व्यतीत हुआ, जिन्होंने अपनी काव्य दृष्टि को फारसी शायरी के प्रभाव से विकसित किया।
रचनाएँ
रसनिधि की सर्वश्रेष्ठ कृति ‘रतनहजारा’ मानी जाती है। यह ग्रंथ बिहारी की सतसई को आदर्श मानकर रचा गया प्रतीत होता है और इसके दोहों में बिहारी की दोहापद्धति का गहरा प्रभाव झलकता है।
अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं –
- विष्णुपदकीर्तन
- बारहमासी
- रसनिधिसागर
- गीतिसंग्रह
- अरिल्ल और माँझ
- हिंडोला
इनके दोहों का एक संग्रह छतरपुर के श्री जगन्नाथप्रसाद ने प्रकाशित किया है, जिससे रसनिधि की काव्य यात्रा का आभास मिलता है।
विशेषताएँ
1. प्रेमदशाओं का सरस चित्रण
रसनिधि ने अपने काव्य में प्रेम की विविध दशाओं और नायिकाओं की चेष्टाओं का सुंदर और सरस चित्रण किया। उन्होंने रीतिबद्ध काव्य न लिखकर फारसी शायरी की शैली को अपनाया, जिससे उनके काव्य में प्रेम की व्यापकता और विविधता दिखाई देती है।
2. बिहारी का प्रभाव
रतनहजारा में बिहारी की सतसई के प्रभाव के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। दोहापद्धति का अनुकरण करते समय रसनिधि कहीं-कहीं बिहारी के भावों को ज्यों का त्यों अपने दोहों में ले आए हैं, जिससे उनके और बिहारी के काव्य में तुलनात्मक समानता दिखाई देती है।
3. भाषा और अभिव्यक्ति
भाषा और भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से रसनिधि का काव्य मिश्रित रूप का है। फारसी शायरी के प्रभाव से उनकी भाषा में शब्दों का असंतुलित प्रयोग और भावों की अभिव्यक्ति में कहीं-कहीं शालीनता का अभाव दृष्टिगोचर होता है।
4. स्वाभाविकता की सफलता
हालाँकि, जहाँ-जहाँ रसनिधि का प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ है, वहाँ उनके दोहे अत्यंत सुंदर और सरस बन पड़े हैं। ऐसे दोहों में भावों की कोमलता और शब्दों की मधुरता दोनों का सुंदर संगम मिलता है।
रसनिधि को रीतिसिद्ध कवि कहा जा सकता है क्योंकि उनकी रचनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का प्रभाव तो है, लेकिन उन्होंने काव्यशास्त्रीय जटिलताओं के स्थान पर प्रेम की सहज और प्राकृतिक अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया।
रीतिमुक्त कवि: रीति परंपरा से बाहर के स्वर
रीतिमुक्त कवि वे हैं जिन्होंने रीति परंपरा की जकड़न को तोड़कर अपने काव्य में भावों की स्वतंत्र और स्वाभाविक अभिव्यक्ति की। इन कवियों का काव्य रीति के बंधनों से मुक्त है और उसमें मानवीय संवेदनाओं, लौकिक प्रेम और व्यक्तिगत अनुभूतियों का गहन चित्रण मिलता है।
इन्होंने अपने समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी काव्य में स्थान दिया। इनका प्रेम-काव्य केवल शारीरिक सौंदर्य या अलंकारिक चमत्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें जीवन की विविधताएँ और यथार्थ के स्वर भी गूंजते हैं।
प्रमुख रीतिमुक्त कवि – घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा।
इनमें घनानंद का “सुजानहित” और आलम का “आलमकेलि” विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। बोधा की “विरहवारीश” उनके व्यक्तिगत प्रेम-विरह का मार्मिक चित्रण है, जबकि ठाकुर के काव्य में बुंदेलखंड की मिट्टी की खुशबू बसती है।
- घनानंद– रीतिमुक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्द कवि हैं। इनकी रचनाएँ हैं – कृपाकंद निबन्ध, सुजान हित प्रबन्ध, इश्कलता, प्रीती पावस, पदावली।
- आलम -आलम इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना “आलम केलि” है।
- ठाकुर– ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक।
- बोधा– विरह बारिश, इश्कनामा।
घनानंद: प्रेम और विरह के अद्वितीय स्वर
जीवन परिचय
घनानंद रीतिमुक्त काव्य परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली कवि माने जाते हैं। उनका जन्म संवत् 1730 (1673 ई.) के आसपास हुआ माना जाता है। हालांकि इनके जन्म स्थान और पितृ नाम के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इन्हें दिल्ली और उसके आसपास का निवासी मानते हैं।
घनानंद जाति से कायस्थ थे और साहित्य तथा संगीत दोनों में अद्वितीय गति रखते थे। वे प्रारंभ में दिल्ली में रहे और जीवन के उत्तरार्ध में वृंदावन चले गए। यहाँ वे भक्ति और प्रेम के स्वर में रमे रहे।
इनका एक अन्य नाम ‘आनंदघन’ भी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, घनानंद नादिरशाह के आक्रमण के समय मारे गए। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी इस मत का समर्थन किया है। ऐसा माना जाता है कि कवि का मूल नाम आनंदघन ही था, जो कालांतर में उनके छंदों की लयात्मकता और भावपूर्णता के कारण ‘घनानंद’ हो गया।
रचनाएँ
घनानंद की काव्य रचनाओं का विस्तार अत्यंत व्यापक है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 41 बताई जाती है। इनमें प्रमुख रचनाएँ हैं –
- सुजानहित प्रबन्ध
- कृपाकंद निबंध
- वियोगबेलि
- इश्कलता
- प्रीति पावस
- रस वसंत
- व्रजविलास
- पदावली
- अनुभव चंद्रिका
- दानघटा
- विचारसार
- प्रेम पत्रिका
- गोकुल गीत
- व्रजस्वरूप
- मनोरथ मंजरी
- मुरलिकामोद
- प्रेमपहेली
इनकी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना “सुजानहित” है, जिसमें 507 पद संगृहीत हैं। यह रचना प्रेम, रूप और विरह का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती है।
इनकी अन्य रचनाओं में व्रजवर्णन (यदि यह व्रजस्वरूप ही है) और दानघटा विशेष उल्लेखनीय हैं। घनानंद के नाम से लगभग चार हजार कवित्त और सवैये उपलब्ध बताए जाते हैं।
विशेषताएँ
1. व्यक्तिगत अनुभूति का मार्मिक चित्रण
घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम की स्वाभाविकता और व्यक्तिगत अनुभूति को अद्वितीय रूप में अभिव्यक्त किया। उन्होंने काव्य में कृत्रिमता और अलंकारों के बोझ से बचकर हृदय की गहराइयों से उपजे भावों को स्थान दिया।
2. विरह की तीव्रता
घनानंद के काव्य में विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। उन्होंने प्रेम की पीड़ा, आशा-निराशा और हृदय की व्याकुलता को जिस प्रकार व्यक्त किया है, वह हिंदी काव्य में विरल है।
3. भाषा और शैली
घनानंद की भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें सहजता, प्रवाह और माधुर्य का अद्भुत संयोग है। उन्होंने फारसी और उर्दू के शब्दों का भी प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है।
4. व्यापक रचनात्मकता
घनानंद की रचनाओं में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि भक्ति, दर्शन, और जीवन के विविध पक्षों का भी चित्रण मिलता है। उनकी रचनाओं का अंग्रेज़ी में भी अनुवाद हुआ है, जिससे उनकी लोकप्रियता का अंतरराष्ट्रीय आयाम भी स्पष्ट होता है।
घनानंद का काव्य रीतिकालीन कृत्रिमता से परे है। वे प्रेम और विरह की भावनाओं को जितनी सहजता और गहराई से व्यक्त करते हैं, वह हिंदी साहित्य में उन्हें अद्वितीय स्थान दिलाता है। उनके काव्य में अनुभूति की तीव्रता और अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता दोनों का सुंदर संगम है, जिसने उन्हें रीतिमुक्त काव्यधारा का सर्वोच्च कवि बना दिया।
आलम: प्रेम और भक्ति के मुक्त स्वर के कवि
जीवन परिचय
आलम रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनका वास्तविक नाम लालमणि त्रिपाठी था और उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में एक मुस्लिम महिला शेख नामक रंगरेजिन से विवाह के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर आलम रख लिया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आलम का कविता काल 1683 से 1703 ईस्वी के बीच रहा। वे मुगल सम्राट औरंगजेब के दूसरे पुत्र मुअज्जम (जो बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा) के आश्रय में रहे।
आलम का जीवन प्रेम, भक्ति और लोकसंग्रह के बीच गहरे रूप में रमा हुआ था। उन्होंने अपने काव्य में रूढ़िबद्ध रीति परंपरा की बजाय भावनात्मक और सहज अभिव्यक्ति को महत्व दिया।
रचनाएँ
आलम की प्रमुख रचनाएँ हैं:
- माधवानल कामकंदला – एक प्रेमाख्यानक काव्य।
- श्यामसनेही – रुक्मिणी के विवाह का वर्णन करने वाला प्रबंध काव्य।
- सुदामाचरित – श्रीकृष्ण की भक्ति पर आधारित काव्य।
- आलमकेलि – लौकिक प्रेम की भावनात्मक और परंपरा-मुक्त अभिव्यक्ति। यह श्रृंगार और भक्ति दोनों के अद्भुत संगम का उदाहरण है।
विशेषताएँ
आलम के काव्य में भावों की स्वाभाविकता और आत्मीयता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने श्रृंगार और भक्ति को मिलाकर एक ऐसा अनोखा काव्य संसार रचा, जो कृत्रिम अलंकारों और रीति-नियमों से मुक्त था। उनकी भाषा में सहज प्रवाह, सरसता और कोमलता है।
ठाकुर: बुंदेलखंड के ठसक वाले कवि
जीवन परिचय
ठाकुर रीतिकाल के एक विशिष्ट और प्रभावशाली कवि थे, जो प्रेम और ठसक के लिए प्रसिद्ध रहे। उनका वास्तविक नाम ठाकुरदास श्रीवास्तव था। ठाकुर का जन्म संवत 1823 में ओरछा (बुंदेलखंड) में हुआ और उनका निधन संवत 1880 के आसपास माना जाता है।
ठाकुर जैतपुर (बुंदेलखंड) के निवासी थे और वहीं के स्थानीय राजा केसरीसिंह के दरबारी कवि थे। इनके पिता गुलाबराय महाराजा ओरछा के मुसाहब थे और पितामह खंगराय काकोरी (लखनऊ) के मनसबदार थे। ठाकुर का संबंध बुंदेलखंड के लगभग सभी राजदरबारों से था। बिजावर नरेश ने उन्हें एक गाँव देकर सम्मानित किया था।
राजा केसरीसिंह के पुत्र पारीछत ने सिंहासनासीन होने पर ठाकुर को अपनी सभा का एक रत्न बनाया। वे बाँदा के हिम्मतबहादुर गोसाईं के यहाँ भी जाते रहते थे, जो पद्माकर के भी प्रमुख आश्रयदाता थे।
चूंकि ठाकुर और पद्माकर समकालीन थे, इसलिए दोनों की कई बार काव्य स्पर्धा होती रहती थी। यह उनकी रचनात्मक प्रतिस्पर्धा के किस्से बुंदेलखंड में आज भी लोककथाओं के रूप में प्रचलित हैं।
रचनाएँ
ठाकुर की प्रमुख रचनाएँ हैं:
- ठाकुर ठसक – जिसमें उनके व्यक्तिगत ठसक और काव्य का स्वाभिमान झलकता है।
- ठाकुर शतक – सौ छंदों का एक सुंदर संग्रह।
विशेषताएँ
ठाकुर का काव्य प्रेम, ठसक और व्यंग्य से परिपूर्ण है। उनके काव्य में बुंदेलखंडी जीवन की झलक मिलती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति को महत्व दिया और दरबारी काव्य की कृत्रिमता से बचते हुए सहज शैली का उपयोग किया। उनकी भाषा में बुंदेलखंड की मिट्टी की महक और ठेठपन है।
आलम और ठाकुर दोनों ही रीतिकालीन काव्य परंपरा में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जहां आलम ने प्रेम और भक्ति के भावपूर्ण चित्रण के माध्यम से रीतिमुक्त काव्यधारा को समृद्ध किया, वहीं ठाकुर ने अपने काव्य में ठसक, व्यंग्य और प्रेम का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। दोनों कवि रीतिकाल की रूढ़ियों से हटकर एक व्यक्तिगत और स्वाभाविक काव्यधारा के प्रवर्तक बने।
बोधा: प्रेम, विरह और हाजिरजवाबी का कवि
जीवन परिचय
बोधा रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों में गिने जाते हैं। वे एक रसिक प्रवृत्ति के कवि थे, जिनका जीवन प्रेम और काव्य दोनों में रमणीयता से परिपूर्ण था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, बोधा पन्ना के राजदरबार में अक्सर जाया करते थे।
राजदरबार में ही उनकी भेंट सुबहान (सुभान) नामक एक नर्तकी से हुई और वे उनसे अत्यंत प्रेम करने लगे। जब पन्ना के महाराज को इस बात का पता चला, तो उन्होंने बोधा को छह महीने के लिए देशनिकाले की सजा दे दी।
वेश्या सुबहान के वियोग में व्याकुल होकर बोधा ने अपनी प्रसिद्ध कृति “विरहवारीश” की रचना कर डाली। देशनिकाले की अवधि समाप्त होने पर जब वे पुनः दरबार में उपस्थित हुए, तो महाराज ने व्यंग्यपूर्वक पूछा –
“कहिए कविराज! अकल ठिकाने आयी? इन दिनों कुछ लिखा क्या?”
बोधा ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपनी पुस्तक विरहवारीश के कुछ कवित्त सुनाए, जिससे महाराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बोधा से कहा –
“शृंगार की बातें बहुत हो चुकीं, अब कुछ नीति की बात सुनाइए।”
इस पर बोधा ने एक नीति से भरा छंद सुनाया:
हिलि मिलि जानै तासों मिलि के जनावै हेत, हित को न जानै ताको हितू न विसाहिए।
होय मगरूर तापै दूनी मगरूरी करै, लघु ह्वै के चलै तासों लघुता निवाहिए॥
बोधा कवि नीति को निबेरो यही भाँति अहै, आपको सराहै ताहि आपहू सराहिए।
दाता कहा, सूर कहा, सुन्दरी सुजान कहा, आपको न चाहै ताके बाप को न चाहिए॥
महाराज उनकी काव्य प्रतिभा और हाजिरजवाबी से बहुत प्रसन्न हुए और कहा –
“कविराज, कोई वर माँगिए।”
बोधा के मुख से तत्काल निकला – “सुभान अल्लाह!”
महाराज उनके इस उत्तर से हँस पड़े और उन्होंने सुबहान को बोधा को उपहारस्वरूप दे दिया। इस प्रकार बोधा के प्रेम की कहानी साहित्य और लोककथाओं में अमर हो गई।
रचनाएँ
बोधा की प्रमुख कृतियाँ हैं:
- विरहवारीश – वियोग और शृंगार रस की अत्यंत मार्मिक कविताओं का संग्रह।
- इश्कनामा – लौकिक प्रेम की विविध अवस्थाओं का सुंदर चित्रण करने वाला काव्य।
विशेषताएँ
विरह का तीव्र और स्वाभाविक चित्रण
बोधा के काव्य में विरह की वेदना और प्रेम की कोमलता का अद्भुत मिश्रण है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को काव्य में इतनी स्वाभाविकता से पिरोया कि पाठक उनके भावों में डूब जाता है।
प्रेम में व्यंग्य और हाजिरजवाबी
बोधा न केवल एक कोमल हृदय के कवि थे, बल्कि उनके पास तीव्र बुद्धि और व्यंग्य की शक्ति भी थी। महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने में उनकी चतुराई ने उन्हें और अधिक लोकप्रिय बनाया।
रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रवक्ता
बोधा ने कृत्रिम अलंकारों और शास्त्रीय जटिलताओं से मुक्त रहकर मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण किया। उनके काव्य में सहजता, प्रवाह और रागात्मकता विशेष रूप से देखने को मिलती है।
बोधा का जीवन और काव्य दोनों ही प्रेम की तीव्रता और हृदय की सरलता का अद्भुत उदाहरण हैं। उन्होंने साहित्य को वह विरह-वेदना दी, जो रीतिकालीन शृंगारिक कृत्रिमता से परे एक आत्मानुभूति बन गई। उनकी रचनाएँ आज भी हिंदी प्रेमकाव्य की परंपरा में विशेष स्थान रखती हैं।
रीति काव्य (रीतिकाल) की विशेषताएँ
हिंदी साहित्य का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभाजित है, जिनमें रीतिकाल (1650 ई.–1850 ई.) को एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह युग मुख्यतः श्रृंगारिक भावों और अलंकारप्रधान काव्य के लिए प्रसिद्ध है। रीतिकाल में काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का गहन अनुशीलन हुआ और कवियों ने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को केंद्र में रखते हुए साहित्य की रचना की। इस युग को अक्सर आलोचना का विषय भी बनाया गया, परंतु इसके काव्य में नकारात्मकताओं के साथ अद्भुत सौंदर्य और कलात्मकता का भी अद्वितीय संगम है।
आइए विस्तार से रीतिकाल और उसके काव्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करें—
1. संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रभाव
रीति काव्य का आधार मुख्य रूप से संस्कृत के लक्षण-ग्रंथ हैं। इस काल के कवियों ने साहित्य की रचना करते समय संस्कृत आचार्यों जैसे आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि की परंपराओं का पालन किया। अलंकारशास्त्र, रसशास्त्र और नायिका भेद संबंधी अवधारणाएँ रीतिकालीन काव्य का मूल आधार बनीं।
हिंदी में संस्कृत की तरह कवि और आचार्य का भेद नहीं रह गया। संस्कृत में कवि का कार्य भावों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति करना था और आचार्य का कार्य काव्यशास्त्र का विवेचन करना। परंतु रीतिकाल में प्रत्येक कवि स्वयं को आचार्य सिद्ध करने का प्रयास करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे न तो पूर्णत: आचार्य बन पाए और न ही उनके काव्य में वह गहराई आ सकी, जो कविता की आत्मा होती है।
2. मौलिकता का अभाव और अनुकरण की प्रवृत्ति
रीतिकालीन कवियों में मौलिकता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का न केवल अनुकरण किया, बल्कि उसे ही अपनी साहित्यिक साधना का मूल मान लिया। यही कारण है कि इस काल के अधिकांश लक्षण-ग्रंथों में मौलिक चिंतन का अभाव रहा।
फिर भी, इस अनुकरण की प्रवृत्ति के बावजूद रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस के क्षेत्र में अनूठे और अत्यंत सुंदर प्रयोग किए, जिनमें भावों की कोमलता और कल्पना की विलक्षणता देखने को मिलती है।
3. काव्यांगों का असमान और अपूर्ण विवेचन
रीतिकाल के आचार्यों ने काव्यांगों का विस्तार से विवेचन किया, परंतु यह विवेचन समान रूप से सभी अंगों पर नहीं हुआ।
- शब्दशक्ति (अर्थगौरव) की ओर रीतिकालीन कवियों का ध्यान लगभग नहीं गया।
- रसों में भी केवल श्रृंगार रस को ही प्रधानता दी गई। करुण, वीर या हास्य रस की उपेक्षा हुई।
- लक्षण पद्य में देने की परंपरा के कारण कई बार उनके लक्षण अस्पष्ट और अपूर्ण रह गए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा है –
“हिंदी में लक्षण-ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे।”
4. श्रृंगार रस की प्रधानता
रीतिकाव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है – श्रृंगार रस का उत्कर्ष। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार को ही काव्य का जीवनतत्व मान लिया। इसमें नायक-नायिका के संयोग-वियोग, शृंगारिक चेष्टाएँ, हाव-भाव, साज-सज्जा और नायिकाओं के विविध प्रकारों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया।
उदाहरण:
बिहारी का प्रसिद्ध दोहा –
“बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।
सोह करे, भौंहनु हंसे, दैन कहे, नटि जाय॥”
यहाँ संयोग का सूक्ष्म और चमत्कारी वर्णन है।
5. अलंकारों का अद्भुत प्रयोग
रीतिकालीन कवियों ने काव्य को अलंकारों से सुसज्जित किया। अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, श्लेष आदि अलंकारों के प्रयोग ने उनकी रचनाओं को आभूषण की भाँति शोभायमान कर दिया।
हालाँकि, कई बार इस अलंकारप्रधानता ने काव्य में भाव-संवेदनाओं की जगह कृत्रिमता उत्पन्न कर दी। फिर भी, इन कवियों के अलंकार-विधान ने हिंदी काव्य को अद्वितीय सौंदर्य प्रदान किया।
6. भाषा और कल्पना की विशेषताएँ
रीतिकाल की भाषा मुख्यतः ब्रजभाषा है, जो अपनी मधुरता, लयात्मकता और कोमलता के कारण श्रृंगारिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है।
रीतिकालीन कवियों ने कल्पना की उड़ान भरते हुए काव्य को सौंदर्य के चरम तक पहुँचाया। नायिकाओं के रूप, प्रेम, श्रृंगार और प्रकृति के चित्रण में इनकी कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रदर्शन हुआ।
7. लक्षण ग्रंथों का काव्यात्मक महत्व
रीतिकाल के लक्षण-ग्रंथों में शास्त्रीय त्रुटियों के बावजूद, उनका काव्यात्मक महत्व अत्यंत उच्च है। अलंकारों, रसों और नायिकाभेद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत पद्य अत्यंत सरस और रोचक हैं।
श्रृंगार रस के जितने उदाहरण रीतिकाल में लिखे गए, उतने सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में भी नहीं मिलते।
8. भाव और कला का अद्वितीय संगम
रीतिकाल की कविता में भावों की कोमलता, कल्पना की ऊँची उड़ान और भाषा की मधुरता का सुंदर समन्वय मिलता है। यह युग भले ही शास्त्रीय दृष्टि से आलोचना का विषय रहा हो, किंतु काव्य-कला की दृष्टि से यह हिंदी साहित्य का एक सौंदर्यमय युग रहा।
रीतिकाल का काव्य शास्त्रीय अनुशासन और श्रृंगारिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। यद्यपि इस युग में मौलिकता और भाव-संवेदनाओं की कमी कही जाती है, फिर भी इसके काव्य ने हिंदी साहित्य को शास्त्रीय सौंदर्य, भाषा की मधुरता और अलंकारिक चमत्कार से समृद्ध किया। रीतिकाल का साहित्य आज भी हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए अध्ययन और रसास्वादन का केंद्र बना हुआ है।
रीतिकाल के काव्य-अंगों का विवेचन
रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह विशिष्ट कालखंड है, जिसमें काव्यशास्त्र के विभिन्न अंगों पर कवियों ने विशेष रूप से विचार किया। इस युग में काव्यशास्त्रीय परंपरा का पालन करते हुए काव्यांगों का विवेचन किया गया, परंतु यह विवेचन पूर्ण और समान नहीं था। इस काल के कवियों ने अधिकतर अलंकार, रस और नायिकाभेद जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, किंतु काव्य के अन्य आवश्यक तत्वों की उपेक्षा भी की।
आइए विस्तार से रीतिकाल के काव्य-अंगों का विवेचन करें—
1. शब्द-शक्ति की उपेक्षा
रीतिकाल के कवियों ने शब्द-सौंदर्य और अलंकार-विधान पर तो विशेष ध्यान दिया, लेकिन शब्द-शक्ति (शब्दार्थ की गहनता और प्रभाव) की ओर उनका ध्यान नहीं गया।
संस्कृत काव्यशास्त्र में शब्द और अर्थ दोनों के सामंजस्य पर जोर दिया गया था, किंतु रीतिकाल के कवियों ने शब्दों को मात्र श्रृंगारिक और अलंकारिक सजावट का साधन बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई बार काव्य में भाव-संवेदनाओं की गहराई कम और सजावटी चमत्कार अधिक दिखाई देने लगा।
2. रस विवेचन में एकपक्षीयता
रीतिकाल में रस-विवेचन मुख्यतः श्रृंगार रस तक सीमित रहा। आचार्यों और कवियों ने श्रृंगार को ही काव्य का प्राण माना और शृंगारिक संयोग-वियोग के सूक्ष्म चित्रण में अद्भुत कौशल दिखाया।
हालाँकि, अन्य रस जैसे वीर, करुण, हास्य, अद्भुत आदि की लगभग पूरी तरह उपेक्षा हुई। यह एक रस-संकुचन की स्थिति थी, जिसने रीतिकाव्य को एकांगी बना दिया।
उदाहरण:
बिहारी के दोहे, केशवदास और देव की रचनाओं में नायक-नायिकाओं के प्रेम और विरह का अत्यंत निपुण चित्रण इस प्रवृत्ति का प्रमाण हैं।
3. अलंकारों का अत्यधिक आग्रह
रीतिकाल के कवियों ने अलंकार-विधान को काव्य की आत्मा समझा। इस युग में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का अद्भुत प्रयोग हुआ।
यह अलंकारप्रियता कभी-कभी काव्य को चमत्कारपूर्ण तो बना देती थी, परंतु भाव-संवेदनाओं की गहराई को प्रभावित करती थी। फिर भी, इस युग के काव्य में अलंकारों ने सौंदर्य और माधुर्य का जो वातावरण रचा, वह अद्वितीय है।
4. लक्षण-ग्रंथों की विशेषताएँ और सीमाएँ
रीतिकाल के कवियों ने लक्षण-ग्रंथों की परंपरा का पालन किया। उन्होंने संस्कृत आचार्यों की तरह पद्यात्मक शैली में काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया।
✅ विशेषताएँ:
- लक्षण-ग्रंथों में रस, अलंकार और नायिकाभेद पर सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए गए।
- उदाहरणस्वरूप पद्य अत्यंत सरस और काव्यात्मक हैं।
❌ सीमाएँ:
- कई लक्षण अस्पष्ट और अपूर्ण रह गए।
- शास्त्रीय विवेचना का क्रमबद्ध और गहन स्वरूप इन ग्रंथों में नहीं मिल पाता।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे लेकर टिप्पणी की है:
“हिंदी में लक्षण-ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे।”
5. भाव, कल्पना और भाषा का अद्वितीय संगम
रीतिकाल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है—भावों की कोमलता, कल्पना की ऊँची उड़ान और भाषा की मधुरता।
कवियों ने श्रृंगारिक भावों का सूक्ष्म, कोमल और आकर्षक चित्रण किया। नायिकाओं के हाव-भाव, नख-शिख वर्णन, ऋतु-वर्णन आदि में उनकी कल्पना शक्ति ने अद्भुत रंग भर दिए।
उदाहरण:
घनानंद का विरह वर्णन –
“प्रेम पथिक हिय की हाय भरी, यह कुमति की गति आननदी।
प्रिय मिलन की सुधि भरमाय रही, यह विरह के व्यथित घनानंदी॥”
6. श्रृंगार रस का अद्वितीय भंडार
रीतिकाल में श्रृंगार रस के जितने उदाहरण प्रस्तुत हुए, उतने शायद ही किसी अन्य भाषा के साहित्य में उपलब्ध हों।
नायक-नायिका के संयोग-वियोग, प्रकृति के सुंदर रूप और प्रेम की विविध अवस्थाओं का जितना सूक्ष्म और सरस चित्रण रीतिकाल में मिलता है, वह हिंदी साहित्य का अमूल्य धरोहर है।
रीतिकाल के अन्य प्रमुख कवि
रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों के अतिरिक्त भी कई ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस युग की काव्य-धारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कुछ कवि अपने वीर रस, श्रृंगार रस या नीति काव्य के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ ने काव्यशास्त्रीय ग्रंथों और टीकाओं की रचना कर इस युग को समृद्ध किया। इन कवियों की कृतियों में उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परिवेश की झलक मिलती है।
1. भूषण
भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म कानपुर के यमुना किनारे स्थित तिकवांपुर गाँव में हुआ था। भूषण ने वीर रस की कविताओं के माध्यम से तत्कालीन समाज में राष्ट्रभक्ति और पराक्रम का संचार किया। इनके छह ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से तीन – भूषणहज़ारा, भूषणउल्लास और दूषणउल्लास – अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। शेष तीन रचनाएँ – “शिवराज भूषण”, “शिवा बावनी” और “छत्रसाल दशक” – उपलब्ध हैं और इनमें शिवाजी तथा बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के शौर्य का सुंदर चित्रण किया गया है।
2. सैय्यद मुबारक़ अली बिलग्रामी
सैय्यद मुबारक़ अली बिलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ। इनके काव्यकाल को संवत 1670 के आसपास माना जाता है। इनके सैकड़ों कवित्त और दोहे पुराने काव्यसंग्रहों में मिलते हैं, जो इनकी काव्यप्रतिभा का प्रमाण हैं। हालांकि वर्तमान में इनके केवल दो ग्रंथ उपलब्ध हैं – “अलकशतक” और “तिलशतक”। इसके अतिरिक्त, शिवसिंह सरोज में इनकी पाँच कविताएँ संकलित हैं, जिनमें चार कवित्त और एक सवैया शामिल है।
3. बेनी
बेनी रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। वे असनी के बंदीजन थे। यद्यपि इनके किसी भी ग्रंथ का अभी तक पता नहीं चला है, किंतु इनके कई फुटकर कवित्त प्रचलित हैं। इन कवित्तों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि इन्होंने नख-शिख वर्णन और षट्ऋतु विषयक काव्य रचनाएँ की होंगी।
4. मंडन
मंडन बुंदेलखंड के जेतपुर के निवासी थे। ये रीतिकालीन काव्य परंपरा के समर्थ कवि माने जाते हैं। इनके भी कई फुटकर कवित्त और सवैये उपलब्ध हैं, किंतु कोई ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। शोध से इनके पाँच ग्रंथों का उल्लेख मिलता है:
- रसरत्नावली
- रसविलास
- जनक पचीसी
- जानकी जू को ब्याह
- नैन पचासा
5. कुलपति मिश्र
कुलपति मिश्र आगरा के निवासी थे और ‘माथुर चौबे’ के रूप में प्रसिद्ध थे। वे महाकवि बिहारी के भानजे थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं:
- रस रहस्य
- मम्मट
अन्य रचनाएँ जो बाद में मिलीं, वे हैं: - द्रोणपर्व (संवत 1737)
- युक्तितरंगिणी (1743)
- नखशिख
- संग्रहसार
- गुण रसरहस्य (1724)
6. सुखदेव मिश्र
सुखदेव मिश्र का संबंध दौलतपुर (जिला रायबरेली) से था। वे मुगलकालीन रीतिकालीन कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ सात ग्रंथों में संकलित हैं:
- वृत्तविचार (संवत 1728)
- छंदविचार
- फाजिलअलीप्रकाश
- रसार्णव
- श्रृंगारलता
- अध्यात्मप्रकाश (संवत 1755)
- दशरथ राय
7. कालिदास त्रिवेदी
कालिदास त्रिवेदी अंतर्वेद के निवासी और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ये भी मुग़लकालीन रीतिकालीन कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं:
- वार वधू विनोद (संवत 1749)
- जँजीराबंद (32 कवित्तों की लघु कृति)
- राधा माधव बुधा मिलन विनोद
- कालिदास हज़ारा (प्रसिद्ध संग्रह ग्रंथ)
8. राम
राम रीतिकालीन कवि थे। शिवसिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 में बताया गया है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार सौरभ प्रमुख है, जिसमें नायिका भेद का सुंदर और मनोरम चित्रण मिलता है। इसके अलावा, इनका एक नाटक हनुमान नाटक भी प्राप्त हुआ है।
9. नेवाज
नेवाज अंतर्वेद क्षेत्र के निवासी ब्राह्मण थे। इनका काव्यकाल संवत 1737 के आसपास माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना शकुंतला नाटक है, जिसका निर्माण संवत 1737 में हुआ था। यह नाटक दोहा, चौपाई और सवैया छंदों में लिखा गया है।
10. श्रीधर (मुरलीधर)
श्रीधर या मुरलीधर प्रयाग के निवासी थे। इन्होंने कई ग्रंथ और फुटकर कविताएँ लिखीं। इनके प्रमुख रीतिग्रंथ हैं:
- नायिकाभेद
- चित्रकाव्य
- जंगनामा
11. सूरति मिश्र
सूरति मिश्र आगरा के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने टीकाकार और कवि दोनों रूपों में योगदान दिया। इनकी रचनाएँ और टीकाएँ:
- अलंकारमाला (संवत 1766)
- अमरचंद्रिका टीका (संवत 1794)
- बिहारी सतसई, कविप्रिया, और रसिकप्रिया पर टीकाएँ
अन्य रीतिग्रंथ: - रसरत्नमाला
- रससरस
- रसग्राहकचंद्रिका
- नखशिख
- काव्यसिद्धांत
- रसरत्नाकर
12. कवींद्र (उदयनाथ)
कवींद्र का जन्म 1680 ई. में हुआ। इनका वास्तविक नाम उदयनाथ था। वे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इनके द्वारा रचित तीन ग्रंथ हैं:
- रस-चन्द्रोदय
- विनोद चन्द्रिका
- जोगलीला
13. श्रीपति
श्रीपति रीतिकाल के एक प्रतिष्ठित कवि थे। ये कालपी के निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 में “काव्यसरोज” नामक महत्वपूर्ण रीति ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त श्रीपति के अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ हैं:
- कविकल्पद्रुम
- रससागर
- अनुप्रासविनोद
- विक्रमविलास
- सरोज कलिका
- अलंकारगंगा
14. बीर
बीर रीतिकाल के कवि थे और दिल्ली के निवासी ‘श्रीवास्तव कायस्थ’ थे। इन्होंने संवत 1779 में “कृष्णचंद्रिका” नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ रस और नायिका भेद विषयक है और श्रृंगार रस की प्रधानता लिए हुए है।
15. कृष्ण
कृष्ण रीतिकाल के कवि और महाकवि बिहारी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध थे। वे माथुर चौबे थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना “बिहारी सतसई” पर लिखी गई टीका है, जो विद्वानों द्वारा अत्यंत प्रशंसित मानी जाती है।
16. पराग
कवि पराग का उल्लेख संवत 1883 में काशी के महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में आश्रित कवि के रूप में मिलता है। इन्होंने “अमरकोश” की भाषा का सृजन किया था, जो तीन खंडों में विभाजित है।
17. गजराज उपाध्याय
गजराज उपाध्याय का उल्लेख शिवसिंह सरोज में संवत 1874 में किया गया है। इन्होंने पिंगल भाषा में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ “वृहत्तर तथा रामायण” की रचना की।
18. रसिक सुमति
रसिक सुमति रीतिकाल के कवि और प्रसिद्ध कवि ईश्वरदास के पुत्र थे। इन्होंने अलंकारशास्त्र पर आधारित “अलंकार चंद्रोदय” नामक ग्रंथ की रचना की। यह कृति कुवलयानंद के आधार पर दोहों में लिखी गई है।
19. गंजन
गंजन रीतिकाल के कवि और काशी के निवासी गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में श्रृंगार रस पर आधारित ग्रंथ “कमरुद्दीन खाँ हुलास” की रचना की।
20. अली मुहीब ख़ाँ (प्रीतम)
अली मुहीब ख़ाँ आगरा के निवासी थे और रीतिकाल के हास्य रस के कवि थे। इनका उपनाम ‘प्रीतम’ था। इन्होंने संवत 1787 में “खटमल बाईसी” नामक हास्यरस प्रधान कृति लिखी।
21. भिखारी दास
भिखारी दास प्रतापगढ़ (अवध) के टयोंगा गाँव के निवासी श्रीवास्तव कायस्थ थे। ये रीतिकाल के बहुप्रतिभाशाली कवि थे। इनके कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है:
- रससारांश संवत
- छंदार्णव पिंगल
- काव्यनिर्णय
- श्रृंगार निर्णय
- नामप्रकाश कोश
- विष्णुपुराण भाषा
- छंद प्रकाश
- शतरंजशतिका
- अमरप्रकाश
22. भूपति
भूपति अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह थे और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार रस के दोहों की एक “सतसई” की रचना की। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं:
- कंठाभरण
- सुरसरत्नाकर
- रसदीप
- रसरत्नावली
23. तोषनिधि
तोषनिधि रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि थे। इनका संबंध शृंगवेरपुर (सिंगरौर, ज़िला इलाहाबाद) से था। इन्होंने संवत 1791 में “सुधानिधि” नामक ग्रंथ लिखा। इनके अन्य दो ग्रंथ हैं:
- विनयशतक
- नखशिख
24. बंसीधर
बंसीधर ब्राह्मण थे और अहमदाबाद (गुजरात) के निवासी थे। इन्होंने दलपति राय के साथ मिलकर संवत 1792 में उदयपुर के महाराणा जगतसिंह के नाम पर “अलंकार रत्नाकर” की रचना की।
25. दलपति राय
दलपति राय महाजन और अहमदाबाद (गुजरात) के रहने वाले थे। इन्होंने बंसीधर के साथ संयुक्त रूप से संवत 1792 में “अलंकार रत्नाकर” की रचना की।
26. सोमनाथ माथुर
सोमनाथ माथुर भरतपुर के महाराज बदनसिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के आश्रय में रहते थे। इन्होंने संवत 1794 में “रसपीयूषनिधि” नामक ग्रंथ लिखा। इनके अन्य तीन ग्रंथ हैं:
- कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी
- सुजानविलास
- माधवविनोद नाटक
रीतिकालीन काव्यांगों का विवेचन यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि इस युग में काव्यशास्त्र का गंभीर और संतुलित विश्लेषण नहीं हुआ, फिर भी इस युग के काव्य ने हिंदी साहित्य को अलंकारिक सौंदर्य, मधुरता और श्रृंगारिक अभिव्यक्ति की चरम ऊँचाई प्रदान की। इसकी कविता में भाव, भाषा और कल्पना का ऐसा संगम मिलता है, जिसने रीतिकाल को हिंदी साहित्य में “काव्य का सौंदर्य युग” बना दिया।
निष्कर्ष
रीतिकाल हिंदी साहित्य का ऐसा युग है जो अपनी शास्त्रीय प्रवृत्तियों, अलंकारपूर्ण काव्यशैली और दरबारी संस्कृति के कारण अनूठा बन गया। यह युग भले ही सामान्य जनता से थोड़ा दूर रहा हो, पर हिंदी साहित्य की कलात्मक ऊँचाइयों को छूने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आचार्य केशवदास, बिहारी, मतिराम, देव और भूषण जैसे कवियों ने इस काल को स्वर्णिम बना दिया।
इन्हें भी देखें –
- अष्टछाप के कवि: परिचय, रचनाएँ और ऐतिहासिक महत्व
- भक्ति काल के कवि और उनके काव्य (रचनाएँ)
- हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि और काव्य (रचनाएँ)
- निर्गुण भक्ति काव्य धारा: अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और साहित्यिक विशेषताएँ
- सूफी काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- संत काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- कृष्ण भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- राम भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- सुहाग की साड़ी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- दिल की रानी | एक ऐतिहासित कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- लॉर्ड्स MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण: भारतीय क्रिकेट का ऐतिहासिक गौरव
- प्रिया नायर: हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला CEO
- धम्मचक्कप्पवत्तन दिवस: बौद्ध धम्म के प्रथम प्रवर्तन की वैश्विक स्मृति