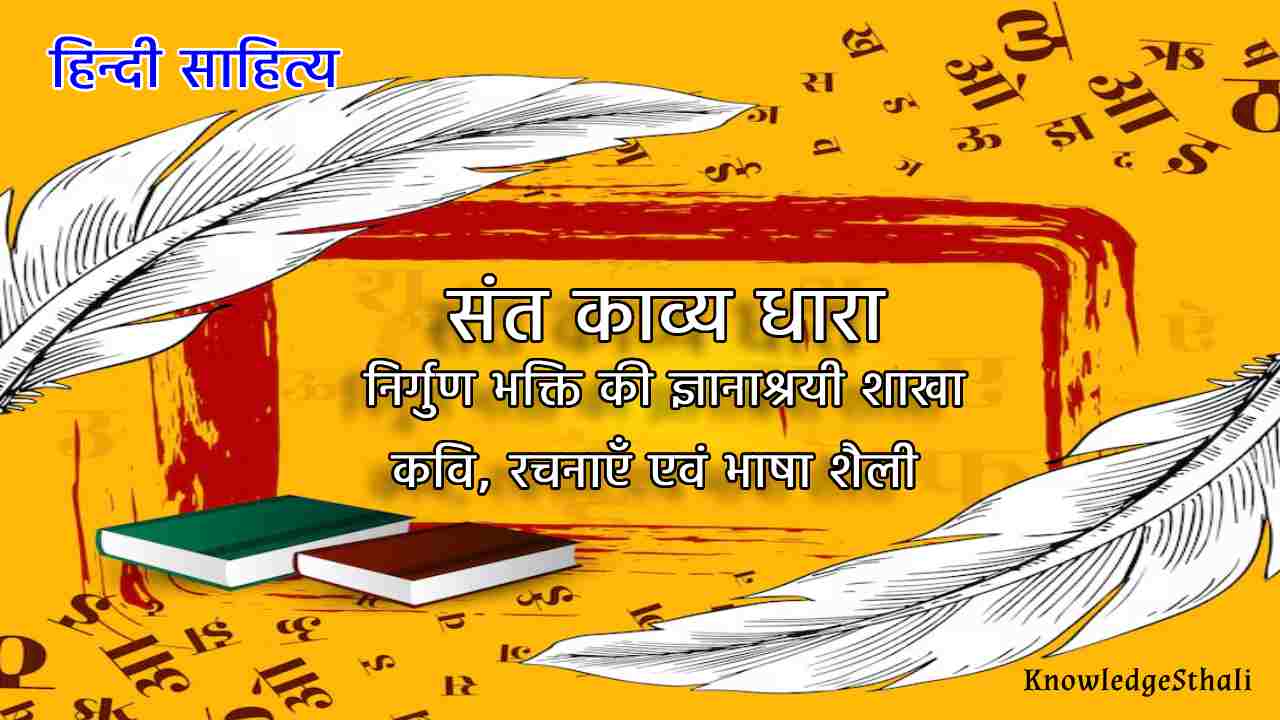यह लेख हिंदी साहित्य के भक्ति काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धारा – संत काव्य या ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्य – पर एक समग्र और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें संत काव्य की धार्मिक, सामाजिक एवं भाषिक विशेषताओं का गहन अध्ययन किया गया है। लेख में बताया गया है कि कैसे संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को केंद्र में रखते हुए गुरु की महत्ता, अनुभव की प्रामाणिकता, जाति और संप्रदाय विरोध, तथा सामाजिक समरसता जैसे विचारों को अपने काव्य में स्थान दिया। कबीर, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू, मलूकदास, सुंदरदास, सहजोबाई जैसे संत कवियों की जीवनी, रचनाएँ, सामाजिक पृष्ठभूमि और उनके विचारों की गहराई को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है।
साथ ही, इस लेख में संत काव्य की शिल्पगत विशेषताएँ जैसे सधुक्कड़ी भाषा, उलटबाँसी शैली, प्रतीकों का प्रयोग आदि का भी विश्लेषण किया गया है। यह लेख न केवल छात्रों, शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन पाठकों के लिए भी पठनीय है जो हिंदी साहित्य की संत परंपरा को गहराई से समझना चाहते हैं। संत काव्यधारा केवल साहित्यिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का शक्तिशाली माध्यम थी, यही इस लेख का केंद्रीय भाव है।
प्रस्तावना
हिंदी साहित्य के भक्ति काल को “स्वर्ण युग” कहा गया है। यह वह कालखंड था जब धर्म, अध्यात्म और सामाजिक चेतना ने काव्य का रूप लेकर जन-जन तक पहुँचने का माध्यम अपनाया। इस काल में भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख रूप देखने को मिले—सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इन दोनों ही प्रवृत्तियों ने तत्कालीन समाज को वैचारिक, धार्मिक और सामाजिक स्तर पर गहराई से प्रभावित किया। इनमें निर्गुण भक्ति की ज्ञानमार्गी शाखा, जिसे संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
इस लेख में हम संत काव्य धारा, इसके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएँ, सामाजिक-धार्मिक विशेषताएँ, भाषा-शैली एवं संत काव्य के व्यापक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करेंगे।
संत काव्य की परिभाषा
‘संत काव्य’ का सामान्य अर्थ है – संतों द्वारा रचित काव्य। किंतु हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जब ‘संत काव्य’ की बात की जाती है तो उसका आशय होता है – निर्गुणोपासक ज्ञानमार्गी संतों द्वारा रचित वह काव्य, जिसमें ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की उपासना, सामाजिक सुधार, गुरु महिमा, वैराग्य, अनुभव की महत्ता तथा धार्मिक रूढ़ियों का खंडन मुखर होता है।
संतमत का प्रारंभ
भारत में संतमत का प्रारंभ लगभग 13वीं सदी में हुआ। विद्वानों के अनुसार, संत नामदेव (1267 ई.) को इस परंपरा का आरंभकर्ता माना जाता है। हालांकि इस परंपरा को व्यापक और सशक्त रूप में दिशा देने का कार्य कबीरदास ने किया, जिन्हें इस धारा का प्रवर्तक माना जाता है।
संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएँ
1. धार्मिक विशेषताएँ:
- निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना:
संत काव्य के कवि निर्गुण ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं। वे मूर्तियों, अवतारों, तीर्थों और कर्मकांडों को निरर्थक मानते हैं। - गुरु की महत्ता:
संत काव्य परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान प्राप्त है। कबीर कहते हैं—
“गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए॥” - योग और भक्ति का समन्वय:
संत कवियों ने ज्ञान और भक्ति को योग के माध्यम से आत्मसात किया और उन्हें साधना का आवश्यक अंग माना। - अनुभूति की प्रामाणिकता:
संत कवि शास्त्रों के ज्ञान से अधिक व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देते हैं। उनके लिए आत्मबोध सर्वोपरि है। - आडंबर और पाखंड का विरोध:
इन कवियों ने तीर्थ, व्रत, मूर्तिपूजा, जातिवाद जैसे आडंबरों का प्रबल विरोध किया। - संप्रदायवाद का विरोध:
संत कवियों ने किसी एक धर्म, पंथ या संप्रदाय की सीमा में नहीं बंधकर मानवता को सर्वोच्च धर्म माना।
2. सामाजिक विशेषताएँ:
- जातिप्रथा का विरोध:
संत काव्य ने भारतीय समाज की कठोर जातिव्यवस्था पर प्रहार किया और समानता का संदेश दिया। रैदास ने कहा—
“मन चंगा तो कठौती में गंगा।” - समानता और समरसता का भाव:
इन कवियों ने ब्राह्मण से लेकर चमार तक सभी को समान माना और मानव मात्र को भगवान का अंश बताया। - स्त्रियों की प्रतिष्ठा:
संत साहित्य में कई महिला संत कवि जैसे सहजोबाई ने भी भाग लिया, जिससे स्त्रियों की भागीदारी और चेतना का विस्तार हुआ।
3. शिल्पगत विशेषताएँ:
- मुक्तक काव्य-रूप:
संत कवि लंबे आख्यानों की बजाय साखी, रमैनी और सबद जैसी संक्षिप्त रचनाओं में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। - मिश्रित भाषा (सधुक्कड़ी):
इनकी भाषा सामान्य जन की बोली से जुड़ी हुई है, जिसमें खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, पंजाबी आदि बोलियों का मेल होता है। - उलटबाँसी शैली:
उलटबाँसी अर्थात ऐसी शैली जिसमें प्रतीकों, विरोधाभासों और संकेतों के माध्यम से गूढ़ विचार प्रकट किए जाते हैं। - पौराणिक और योगिक प्रतीकों का प्रयोग:
हठयोग, तंत्र, पौराणिक कथाओं के प्रतीकों का प्रयोग व्यापक रूप से देखने को मिलता है।
4. भाषा और शैली
- रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को “सधुक्कड़ी” कहा है – एक ऐसी भाषा जो संप्रेषणीयता और प्रभावशीलता में सक्षम हो।
- श्यामसुंदर दास ने कबीर की भाषा को “पंचमेल खिचड़ी” कहा, क्योंकि उसमें विभिन्न बोलियों का मिश्रण है।
- हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को “वाणी का डिक्टेटर” कहकर उनकी भाषिक सशक्तता की सराहना की।
संत काव्य धारा के प्रमुख कवि और रचनाएँ
| क्रम | कवि का नाम | रचनाएँ / ग्रंथ |
|---|---|---|
| 1 | कबीरदास | बीजक – (रमैनी, सबद, साखी) |
| 2 | नामदेव | अभंग वाणी, कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में |
| 3 | रैदास (रविदास) | बानी, पद (गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित) |
| 4 | गुरु नानक देव | जपजी साहिब, अन्य गुरु ग्रंथ साहिब में |
| 5 | दादू दयाल | दादू वाणी |
| 6 | मलूकदास | रत्न खान, ज्ञानबोध |
| 7 | सुंदरदास | सुंदर विलाप |
| 8 | चरनदास | चरनदास वाणी |
| 9 | धर्मदास | कबीरवाणी का संकलन |
| 10 | रज्जब | साखियाँ, पद |
| 11 | सहजोबाई | सहजोबाई वाणी |
संत कवियों की सामाजिक पृष्ठभूमि
संत काव्य परंपरा की विशेषता यह भी है कि इसके अधिकांश कवि निम्न वर्ग या कामगार वर्ग से आते थे:
- कबीर – जुलाहा
- नामदेव – दर्जी
- रैदास – चमार
- दादू – बुनकर
- सेना – नाई
- सदना – कसाई
यह दर्शाता है कि इस परंपरा ने जाति-पाति और उच्च-नीच की भावना को नकारते हुए समता और बंधुत्व का संदेश दिया।
संत काव्य का काल और उसका स्थान
संत काव्य का समय भक्ति काल (1350–1650 ई.) में आता है। यह काल धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति का समय था, जब समाज में ब्राह्मणवाद, मूर्तिपूजा, जातिवाद जैसी कुरीतियाँ फैली थीं। इन संत कवियों ने अपनी वाणी से इस अंधकार को मिटाने का प्रयास किया।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को “ईसायत की देन” कहा, परंतु यह धारणा सीमित है। संत काव्य पूरी तरह भारतीय मनीषा की उपज है।
संत काव्य में प्रमुख रस और भाव
संत काव्य में शांत रस की प्रमुखता देखी जाती है। यह भक्ति, वैराग्य, आत्मचिंतन और शांति की भावना से ओतप्रोत होता है। साथ ही करुणा, सहजता और स्नेह के भाव भी प्रबल होते हैं।
संत काव्य का प्रभाव और महत्त्व
1. सामाजिक प्रभाव:
- जातिवाद का विरोध
- स्त्री-पुरुष समानता का संदेश
- श्रम और कर्म की महत्ता
2. धार्मिक प्रभाव:
- निर्गुण भक्ति की प्रतिष्ठा
- गुरु की सर्वोच्चता
- धर्म से अधिक कर्म और अनुभव की प्राथमिकता
3. साहित्यिक प्रभाव:
- बोली आधारित साहित्य का विकास
- सधुक्कड़ी जैसी मिश्रित भाषा की स्थापना
- जनमानस से जुड़ा काव्य-साहित्य
निष्कर्ष
संत काव्य धारा हिंदी साहित्य में एक ऐसा उज्ज्वल अध्याय है, जिसने न केवल भाषा और साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद और असमानता को चुनौती दी। कबीर, रैदास, नामदेव, नानक जैसे संतों ने काव्य को जन-जागरण और आत्मबोध का सशक्त माध्यम बनाया।
इस काव्यधारा की मूल आत्मा है – सत्य की खोज, गुरु की महत्ता, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, और मानव मात्र के प्रति समभाव। यही इसकी शाश्वतता और लोकप्रियता का कारण है। संत काव्य, केवल साहित्य नहीं बल्कि मानवता का अनमोल पथप्रदर्शक है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. संत कबीर किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं?
➤ संत कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कवि हैं।
2. संत काव्य का दूसरा नाम क्या है?
➤ संत काव्य को ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के नाम से भी जाना जाता है।
3. संत काव्य धारा में कबीर का स्थान?
➤ कबीर न केवल प्रमुख संत कवि हैं बल्कि युग-चिंतक और समाज-सुधारक भी हैं।
4. निर्गुण भक्ति धारा के अन्य कवि कौन हैं?
➤ कबीर, रैदास, नामदेव, दादू, नानक, मलूकदास आदि।
5. भक्ति काल के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं?
➤ भक्ति काव्य के क्रांतिकारी प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं।
6. संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है?
➤ शांत रस की प्रधानता है।
7. संत काव्य और सूफी काव्य में क्या अंतर है?
➤ संत काव्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना और ज्ञानमार्ग की प्रधानता होती है, जबकि सूफी काव्य में प्रेम को माध्यम मानते हुए ईश्वर की प्राप्ति की बात होती है। संत काव्य हिंदू भक्ति परंपरा से जुड़ा है, वहीं सूफी काव्य इस्लामी रहस्यवाद से प्रभावित होता है।
8. संत काव्य में ‘अनुभव की प्रामाणिकता’ का क्या अर्थ है?
➤ संत काव्य में अनुभव की प्रामाणिकता का अर्थ है कि ईश्वर की सच्ची पहचान और आत्मबोध केवल शास्त्रों के अध्ययन से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव, साधना और आत्मचिंतन से संभव है। संत कवि मानते हैं कि बिना स्वानुभव के सभी धार्मिक ज्ञान व्यर्थ है। कबीर कहते हैं—
“पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।”
9. संत काव्य में स्त्री कवियों का क्या योगदान है?
➤ संत काव्य परंपरा में स्त्री संत कवियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें सहजोबाई और मीरा बाई प्रमुख हैं। सहजोबाई ने निर्गुण भक्ति के गूढ़ विचारों को सहज भाषा में व्यक्त किया, जबकि मीरा बाई ने कृष्ण भक्ति को सगुण रूप में अपनाया। इनकी वाणी स्त्री-चेतना, समर्पण और आत्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है।
10. संत काव्य में प्रयुक्त प्रमुख काव्य विधाएँ कौन-कौन सी हैं?
➤ प्रमुख विधाएँ हैं – साखी (दोहे), सबद (पद), रमैनी (छोटी कथाएँ)। ये मुक्तक शैली में लिखे गए हैं और इनमें जीवन-दर्शन, नीति और अनुभव की झलक मिलती है।
11. संत कबीर की भाषा की विशेषता क्या थी?
➤ कबीर की भाषा को ‘सधुक्कड़ी’ कहा गया है। यह बोलचाल की भाषा थी जिसमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि का मिश्रण था। उनकी भाषा में लोकोक्तियाँ, प्रतीक, विरोधाभास और उलटबाँसी शैली का प्रयोग हुआ है।
12. सहजोबाई कौन थीं और उनका योगदान क्या है?
➤ सहजोबाई एक प्रमुख महिला संत कवयित्री थीं। वे दादू पंथ से जुड़ी थीं। उनके काव्य में स्त्री चेतना, भक्ति और अनुभव की प्रामाणिकता का गहन चित्रण मिलता है।
13. सुंदरदास को अन्य संतों से अलग क्यों माना जाता है?
➤ सुंदरदास एकमात्र ऐसे संत कवि हैं जो ब्राह्मण परिवार से थे। अन्य संत कवि सामान्यतः निम्नवर्गीय या शिल्पकार समाज से आए थे। उनकी रचनाएँ दार्शनिक एवं विवेचनात्मक हैं, जैसे— सुंदर विलाप।
14. संत काव्य के प्रमुख संदेश क्या हैं?
➤ ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्मकांड नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मानुभव ज़रूरी है। मानव सेवा, जातिवाद का विरोध, गुरु की भक्ति, और सत्य की खोज ही संत काव्य के मूल संदेश हैं।
15. गुरु ग्रंथ साहिब में किन-किन संत कवियों की रचनाएँ शामिल हैं?
➤ गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव, रैदास, कबीर, भिखन, सदना, पीपा, धन्ना आदि कई संतों की वाणियाँ संकलित हैं।
16. क्या संत काव्य आंदोलन एक सामाजिक सुधार आंदोलन भी था?
➤ हाँ, यह न केवल धार्मिक चेतना का काव्य था, बल्कि एक सामाजिक सुधार आंदोलन भी था, जिसने जातिवाद, पाखंड, ब्राह्मणवाद, और स्त्री-विरोध जैसी समस्याओं पर सीधा प्रहार किया।
17. कबीर की ‘उलटबाँसी’ का क्या अर्थ है?
➤ ‘उलटबाँसी’ एक विशेष काव्य शैली है जिसमें कवि प्रतीकों, विरोधाभासों और पहेलीनुमा भाषा में गूढ़ तात्विक बातें कहता है। उदाहरण— “पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।”
यदि आपके मन में संत काव्य धारा – निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हो, तो आप नीचे टिप्पणी कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं।
Hindi – KnowledgeSthali
इन्हें भी देखें –
- कृष्ण भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- राम भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- यह मेरी मातृभूमि है | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- आकाशदीप कहानी- जयशंकर प्रसाद
- क़लम का सिपाही | प्रेमचन्द जी की जीवनी : अमृत राय
- कबीर दास जी के दोहे एवं उनका अर्थ | साखी, सबद, रमैनी
- कबीर दास जी | जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएँ एवं भाषा
- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ
- हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास
- हिंदी के विराम चिन्ह और उनका प्रयोग | 50 + उदाहरण
- भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य | Folk dances and Classical dances of India