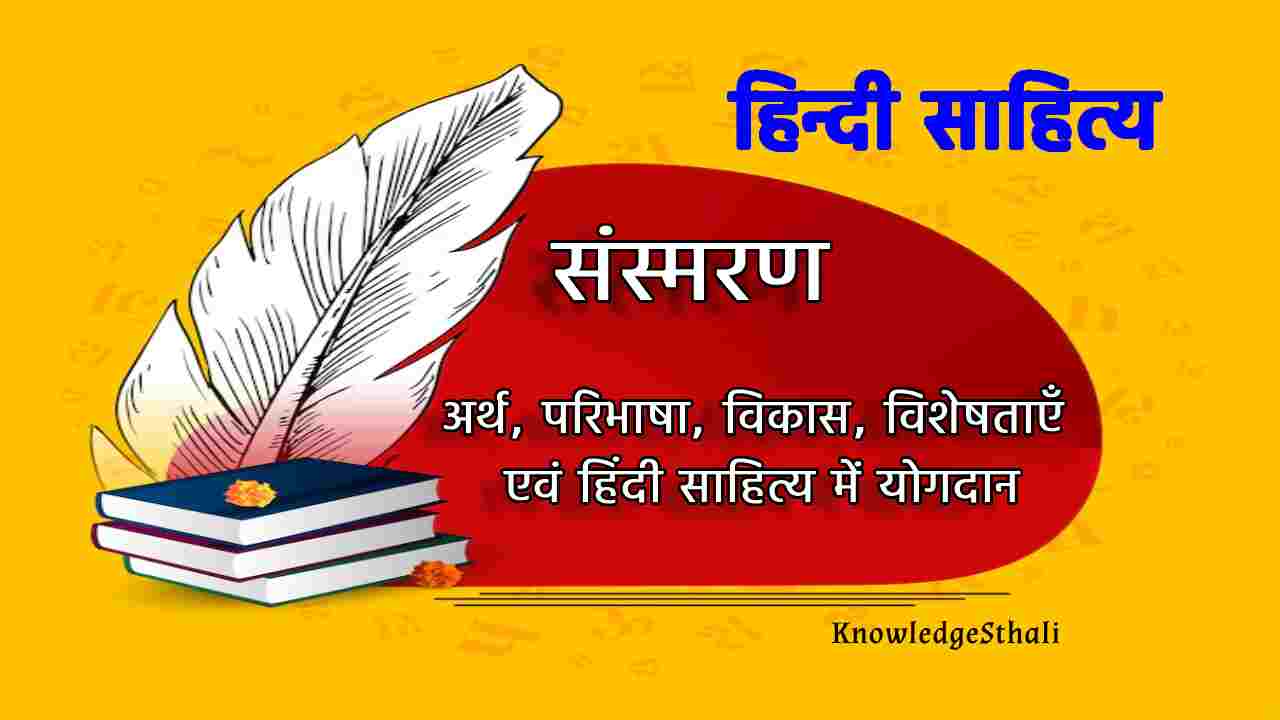हिंदी साहित्य में संस्मरण एक ऐसी विधा है, जिसमें लेखक अपने जीवन के किसी अनुभव, व्यक्ति, घटना या स्थान का आत्मीय स्मरण भावनात्मक और चित्रात्मक शैली में करता है। यह केवल तथ्यों की प्रस्तुति भर नहीं है, बल्कि इसमें लेखक की संवेदनशीलता, दृष्टिकोण और अनुभवजन्य सत्य निहित होते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में संस्मरण का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल अतीत को जीवंत करता है, बल्कि पाठक के सामने इतिहास और समाज के एक विशिष्ट कालखंड की झलक भी प्रस्तुत करता है।
संस्मरण का अर्थ और व्युत्पत्ति
“संस्मरण” शब्द स्मृ धातु में सम् उपसर्ग तथा ल्यूट प्रत्यय (अन्) जोड़कर बना है। इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ है — “सम्यक् स्मरण” अर्थात किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का पूर्ण रूप से और आत्मीयता के साथ स्मरण करना।
साहित्य में इसका आशय लेखक के निजी अनुभव और स्मृतियों का भावनात्मक एवं सत्यनिष्ठ रूप से चित्रण करना है।
संस्मरण की परिभाषा
संस्मरण वह गद्य-विधा है, जिसमें लेखक अपने जीवन से जुड़े किसी अनुभव, व्यक्ति या घटना का इस प्रकार वर्णन करता है कि उसका चित्र पाठक के सामने सजीव हो उठे। इसमें प्रस्तुत अनुभव काल्पनिक नहीं होते, बल्कि वास्तविक और सत्य पर आधारित होते हैं। संस्मरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के जीवन या घटना के महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करना होता है।
हिंदी का प्रथम संस्मरण
हिंदी साहित्य में प्रथम संस्मरण को लेकर साहित्येतिहासकारों और शोधकर्ताओं में मतभेद पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अलग-अलग विद्वान और उपलब्ध स्रोत इस विधा के आरंभिक रूप की पहचान अलग दृष्टिकोण से करते हैं। साहित्यिक प्रमाणों और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर, इस चर्चा में दो नाम विशेष रूप से सामने आते हैं—बालमुकुंद गुप्त और पद्मसिंह शर्मा।
बालमुकुंद गुप्त और ‘प्रतापनारायण मिश्र’ पर संस्मरण
सन् 1907 में हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर बालमुकुंद गुप्त ने प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रतापनारायण मिश्र पर एक संस्मरण लिखा। यह रचना मिश्र के जीवन, व्यक्तित्व, साहित्यिक योगदान और उनसे जुड़ी निजी यादों का अत्यंत आत्मीय, सजीव और प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करती है। विषय के प्रति लेखक का गहरा जुड़ाव और वर्णन की सहजता इस संस्मरण को विशेष बनाती है। अनेक साहित्येतिहासकार इस रचना को हिंदी का प्रथम संस्मरण मानते हैं।
‘हरिऔध जी का संस्मरण’
प्रतापनारायण मिश्र पर संस्मरण लिखने के बाद, बालमुकुंद गुप्त ने सुप्रसिद्ध कवि हरिऔध (श्री श्यामसुंदर दास ‘हरिऔध’) पर आधारित संस्मरणों की एक विस्तृत श्रृंखला रची। यह श्रृंखला पंद्रह संस्मरणों का संग्रह थी, जिसे बाद में ‘हरिऔध जी का संस्मरण’ शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। यह कृति भी 1907 ई. में ही लिखी गई थी। इसमें हरिऔध के साहित्यिक व्यक्तित्व, काव्य-रचनाओं, निजी स्वभाव और जीवन के कई रोचक प्रसंगों का चित्रात्मक और आत्मीय विवरण मिलता है। इसे हिंदी संस्मरण साहित्य की प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तकाकार रचना माना जाता है, जिसने इस विधा को साहित्य में ठोस पहचान दिलाई।
पद्मसिंह शर्मा और ‘पद्म-पराग’ (1929)
संस्मरण को गद्य की स्वतंत्र और प्रतिष्ठित विधा के रूप में स्थापित करने में पद्मसिंह शर्मा (1876–1932) का योगदान भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उनकी कृतियाँ ‘प्रबंध मंजरी’ और ‘पद्म-पराग’ (1929) संस्मरण साहित्य के विकास में मील के पत्थर मानी जाती हैं। कुछ विद्वान ‘पद्म-पराग’ को हिंदी का प्रथम संस्मरण भी मानते हैं, किंतु यह मत सर्वसम्मत नहीं है, क्योंकि इससे पहले बालमुकुंद गुप्त के संस्मरण साहित्य जगत में आ चुके थे।
‘पद्म-पराग’ की विशेषता यह है कि इसमें संस्मरण और रेखाचित्र — दोनों विधाओं के गुण विद्यमान हैं। इसमें चित्रात्मकता, संक्षिप्तता और भावनात्मक निकटता जैसे रेखाचित्र के गुण दिखाई देते हैं, वहीं संस्मरण की आत्मीयता, यथार्थपरकता और लेखक के व्यक्तिगत अनुभव का स्पर्श भी स्पष्ट है। यही कारण है कि ‘पद्म-पराग’ को साहित्येतिहास में अक्सर “संस्मरणात्मक रेखाचित्र” की संज्ञा दी जाती है।
निष्कर्ष रूप में —
उपलब्ध ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर, हिंदी का पहला (प्रथम) संस्मरण अधिकांश विद्वानों द्वारा बालमुकुंद गुप्त के 1907 में लिखित प्रतापनारायण मिश्र पर संस्मरण को माना जाता है। इसके साथ ही, उनकी पुस्तक ‘हरिऔध जी का संस्मरण’ को हिंदी संस्मरण साहित्य की पहली महत्वपूर्ण पुस्तकाकार कृति के रूप में स्वीकार किया गया है।
वहीं, पद्मसिंह शर्मा की ‘पद्म-पराग’ (1929) इस विधा के विकास और विस्तार में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसने संस्मरण और रेखाचित्र दोनों को साहित्य में एक नई ऊँचाई दी।
संस्मरण की विशेषताएँ
संस्मरण लेखन के पाँच प्रमुख नियामक उपकरण माने जाते हैं —
- भाव प्रवणता – लेखक का प्रस्तुतीकरण भावनाओं से ओत-प्रोत होता है।
- चित्रोपमता – वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने चित्र उपस्थित हो जाए।
- वैयक्तिकता – इसमें लेखक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अनुभव प्रमुख रहते हैं।
- जीवन के खंड विशेष का वर्णन – संपूर्ण जीवन नहीं, बल्कि उसका एक विशेष अंश या प्रसंग वर्णित होता है।
- सत्यात्मकता – तथ्य और अनुभव सत्य पर आधारित होते हैं, अतिरंजना या कल्पना का न्यूनतम प्रयोग होता है।
सत्यात्मकता का महत्व
संस्मरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सत्यनिष्ठा है। इसमें लेखक को दोषों और कमियों का भी ईमानदारी से उल्लेख करना पड़ता है। यही कारण है कि संस्मरण को जीवनी के लिए सामग्री एकत्र करने वाला स्रोत माना जाता है।
जहाँ जीवनी संस्मरण के आधार पर बन सकती है, वहीं जीवनी स्वयं संस्मरण के लिए सामग्री नहीं देती।
संस्मरण और अन्य साहित्यिक विधाओं में अंतर
(1) जीवनी और संस्मरण में अंतर
- व्यक्तिगत संपर्क – जीवनी लिखने के लिए लेखक का विषय से प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक नहीं, जबकि संस्मरण में व्यक्तिगत संपर्क अनिवार्य है।
- चित्रण का स्वरूप – जीवनी लेखक प्रायः नायक के गुणों का ही चित्रण करता है, जबकि संस्मरण में गुण-दोष दोनों का उल्लेख होता है।
- व्याप्ति – जीवनी संपूर्ण जीवन का वृत्तांत देती है, संस्मरण केवल किसी विशेष कालखंड या प्रसंग का।
(2) संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर
डॉ. नगेन्द्र के अनुसार, संस्मरण और रेखाचित्र में मौलिक अंतर नहीं है, और संस्मरण को रेखाचित्र का एक प्रकार भी माना गया है, परंतु दोनों स्वतंत्र विधाएँ हैं।
मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:
- अतिरंजना – रेखाचित्र में अतिरंजना संभव है, संस्मरण में नहीं।
- काल – संस्मरण केवल अतीत का होता है, रेखाचित्र वर्तमान या भविष्य का भी हो सकता है।
- दृष्टिकोण – रेखाचित्र बाहरी विशेषताओं पर केंद्रित होता है, संस्मरण आंतरिक गुणों पर।
- चरित्र चित्रण – रेखाचित्र चरित्र का रूपरेखा देता है, संस्मरण चरित्र का दर्पण बनता है।
- कल्पना और सत्य – रेखाचित्र कल्पना प्रधान, संस्मरण सत्य आधारित।
- भाव – रेखाचित्र में तटस्थता, संस्मरण में आत्मीयता प्रमुख।
(3) संस्मरण और रिपोर्ताज में अंतर
- स्रोत – रिपोर्ताज प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है, संस्मरण स्मृति पर।
- काल – घटना घटित होते ही रिपोर्ताज लिखा जाता है, अतीत की घटना संस्मरण बनती है।
- दृष्टिकोण – रिपोर्ताज में तटस्थता या उपदेशात्मक भाव संभव है, संस्मरण में आत्मीयता और भावनात्मक स्वर प्रमुख होते हैं।
(4) संस्मरण और निबंध में अंतर
- विचार बनाम अनुभव – निबंध मुख्यतः तर्क-वितर्क और विचार प्रधान होता है, जबकि संस्मरण अनुभव और भावनाओं पर आधारित।
- शैली – निबंध में तार्किकता, संस्मरण में संवेदनशीलता अधिक होती है।
हिंदी में संस्मरण साहित्य का विकास
द्विवेदी युग में संस्मरण
हिंदी में संस्मरण साहित्य का प्रारंभ द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन ने इस विधा को बढ़ावा दिया।
- महावीर प्रसाद द्विवेदी – अनुमोदन का अंत (1905), सभ्यता की सभ्यता (1907), विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर (1918)
- अन्य लेखक – रामकुमार खेमका (इधर-उधर की बातें, 1918), जगतबिहारी सेठ, जगन्नाथ खन्ना, भोलादत्त पाण्डेय (मेरी नई दुनिया सम्बन्धी राम कहानी, 1906)
छायावाद युग के संस्मरण
सरस्वती, विशाल भारत, सुधा और माधुरी पत्रिकाओं में कृपानाथ मिश्र, राम नारायण मिश्र, भगवानदीन दुबे, रामेश्वरी नेहरू, श्री मन्नारायण अग्रवाल आदि के संस्मरण प्रकाशित हुए।
- पं. पद्मसिंह शर्मा – इनके संस्मरण पद्म पराग में संकलित हैं।
- श्रीराम शर्मा – विषय को शब्दों में मूर्त करने और नुकीली भाषा-शैली के लिए प्रसिद्ध।
छायावादोत्तर काल के संस्मरण
इस काल की सबसे प्रमुख संस्मरणकार महादेवी वर्मा रहीं।
उनकी रचनाएँ – अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी, स्मारिका, मेरा परिवार
अन्य लेखक:
- प्रकाशचन्द्र गुप्त – पुरानी स्मृतियाँ
- राधिका रमण प्रसाद सिंह – मौलवी साहब, देवी बाबा
- कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’ – जिन्दगी मुस्कुराई
- देवेन्द्र सत्यार्थी – रेखाएँ बोल उठीं, क्या गोरी और साँवरी
- जैनेन्द्र कुमार – ये और वे
अन्य प्रमुख संस्मरणकार और कृतियाँ
- चतुरसेन शास्त्री – वातायन
- शान्ति प्रिय द्विवेदी – पथ चिह्न
- कैलाश नाथ काटजू – मैं भूल नहीं सकता
- इन्द्र विद्यावाचस्पति – मैं इनका ऋणी हूँ
- विनोद शंकर व्यास – प्रसाद और उसके समकालीन
- सम्पूर्णानन्द – कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार
- रायक्रष्ण दास – जवाहर भाई-उनकी आत्मीयता और सहदयता
- कुन्तल गोयाल, डॉ. सहरगुलाल, पद्मिनी मेनन, लक्ष्मी नारायण सुधांशु आदि के योगदान भी उल्लेखनीय हैं।
संस्मरण के उदाहरण
नीचे संस्मरण के उदाहरण के रूप में प्रमुख संस्मरण और उनके संस्मरणकार ने नामों को टेबल में व्यवस्थित रूप में दिया गया है –
| क्रम | संस्मरण | संस्मरणकार |
|---|---|---|
| 1 | अनुमोदन का अंत (1905) सभा की सभ्यता (1907) | महावीर प्रसाद द्विवेदी |
| 2 | हरिऔध जी का संस्मरण | बालमुकुंद गुप्त |
| 3 | शिकार (1936) बोलती प्रतिमा (1937) भाई जगन्नाथ प्राणों का सौदा (1939) जंगल के जीव (1949) | श्रीराम शर्मा |
| 4 | लाल तारा (1938), माटी की मूरतें (1946) गेहूँ और गुलाब (1950) जंजीर और दीवारें (1955) मील के पत्थर (1957) | रामवृक्ष बेनीपुरी |
| 5 | अतीत के चलचित्र (1941) स्मृति की रेखाएँ (1947) पथ के साथी (1956) क्षणदा (1957) स्मारिका (1971) | महादेवी वर्मा |
| 6 | तीस दिन : मालवीय जी के साथ (1942) | रामनरेश त्रिपाठी |
| 7 | हमारे आराध्य (1952) | बनारसीदास चतुर्वेदी |
| 8 | जिंदगी मुस्कराई (1953) दीप जले शंख बजे (1959) माटी हो गई सोना (1959) | कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’ |
| 9 | ये और वे (1954) | जैनेंद्र कुमार |
| 10 | बचपन की स्मृतियाँ (1955) असहयोग के मेरे साथी (1956) जिनका मैं कृतज्ञ (1957) | राहुल सांकृत्यायन |
निष्कर्ष
संस्मरण न केवल व्यक्तिगत स्मृतियों का दस्तावेज़ है, बल्कि यह समय, समाज और व्यक्ति के अंतर्संबंधों का भी आईना है। इसकी सत्यनिष्ठा, आत्मीयता और चित्रात्मक शैली इसे अन्य गद्य-विधाओं से अलग बनाती है। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग से लेकर आज तक संस्मरणकारों ने अपने अनुभवों को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वे न केवल साहित्यिक महत्व के बने, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में भी अमूल्य दस्तावेज़ सिद्ध हुए।
इन्हें भी देखें –
- संस्मरण और संस्मरणकार : प्रमुख लेखक और रचनाएँ
- जीवनी – परिभाषा, स्वरूप, भेद, साहित्यिक महत्व और उदाहरण
- हिंदी की आत्मकथा और आत्मकथाकार : लेखक और रचनाएँ
- आत्मकथा – अर्थ, विशेषताएँ, भेद, अंतर और उदाहरण
- हिंदी निबंध लेखन : स्वरूप, प्रकार एवं कला
- हिंदी निबंध का विकास : एक ऐतिहासिक परिदृश्य
- एक चिनगारी घर को जला देती है – मुंशी प्रेमचंद | हिंदी अनुवाद
- सौत कहानी – मुंशी प्रेमचंद | पात्र परिचय, चरित्र चित्रण, सारांश
- नमक का दरोगा- मुंशी प्रेमचंद | सारांश, पात्र परिचय, चरित्र चित्रण, समीक्षा
- क़लम का सिपाही | प्रेमचन्द जी की जीवनी : अमृत राय
- भोर से पहले | कहानी – अमृत राय
- आख़िरी तोहफ़ा | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- कबीर दास जी के दोहे एवं उनका अर्थ | साखी, सबद, रमैनी
- कबीर दास जी | जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएँ एवं भाषा
- मुंशी प्रेमचंद जी और उनकी रचनाएँ