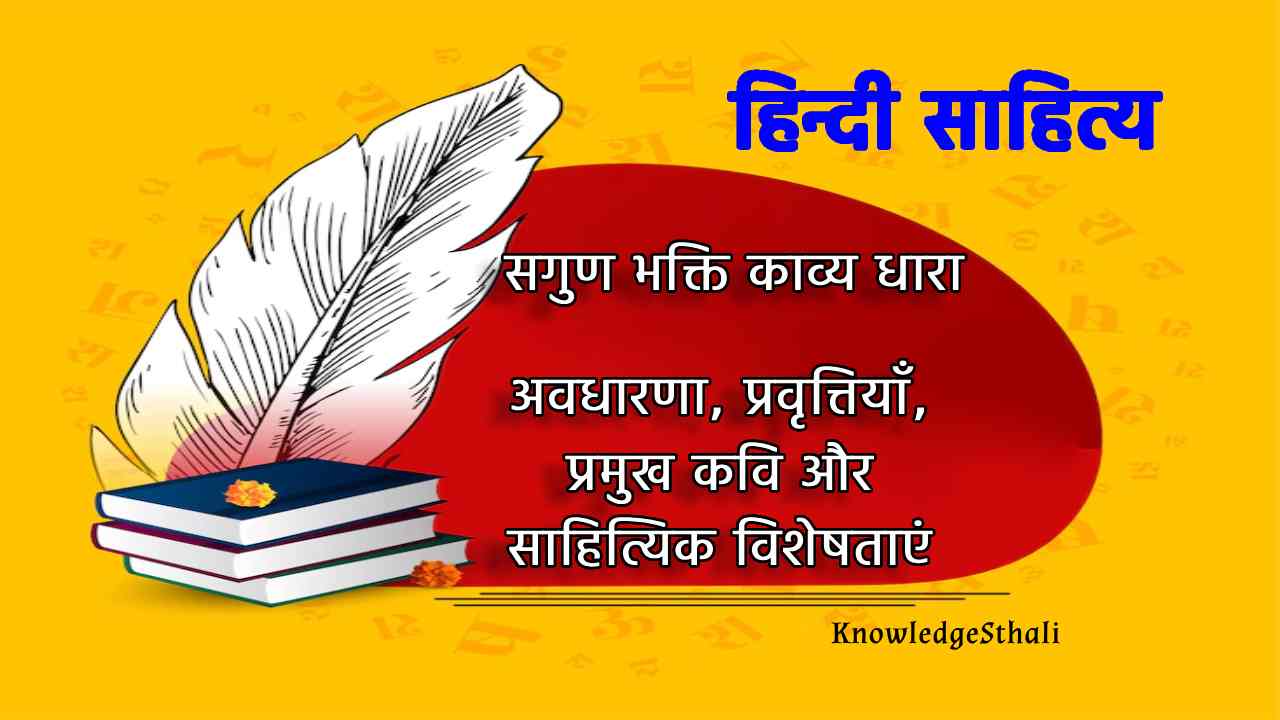हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक कालखंडों में विभाजित है। इन कालखण्डों में भक्तिकाल जिसकी समयावधि लगभग 1350 ई. से 1700 ई. के मध्य मानी जाती है, भक्तिमार्ग पर आधारित साहित्यिक सृजन का युग था। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है। धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से यह युग अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। इस युग के कवियों ने धर्म और अध्यात्म को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया। इस काल में भक्ति की दो प्रमुख धाराएं विकसित हुईं—निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। इस लेख में हम सगुण काव्य धारा का गहन अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं की विवेचना करेंगे।
सगुण भक्ति धारा की अवधारणा
‘सगुण’ शब्द का अर्थ है—गुणों से युक्त, अर्थात ऐसा ईश्वर जो साकार रूप में अवतरित होता है, जिसे देखा, अनुभव किया और भजा जा सकता है। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर की मूर्ति या अवतार को केंद्र में रखकर भक्ति की जाती है। भक्त अपने आराध्य को व्यक्तिगत रूप में प्रेम करता है—वह उसका प्रियतम, सखा, पति या स्वामी होता है।
सगुण भक्ति का आधार वेद, उपनिषद, पुराण और विशेषतः श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित अवतारवाद की परंपरा है। इस धारा में ईश्वर को दो प्रमुख रूपों—राम और कृष्ण—में पूजा गया।
सगुण भक्ति का उद्भव
सगुण भक्ति की जड़ें दक्षिण भारत की वैष्णव संत परंपरा में मिलती हैं, जो नायनार और आलवार संतों द्वारा प्रवाहित हुई। उत्तरी भारत में भक्ति की यह धारा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण और भी सशक्त रूप से उभरी।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जब भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ और हिंदू समाज पर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दबाव पड़ा, तब जनमानस ने अपनी शक्ति और आत्मगौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए भक्ति को माध्यम बनाया। मंदिरों का विध्वंस, मूर्तियों का अपमान और सामाजिक विघटन ने जनमानस को गहरे संकट में डाल दिया। उस परिस्थिति में भक्ति मार्ग ही शांति, सहारा और आत्मसम्मान का माध्यम बना।
सगुण भक्ति धारा के प्रकार
सगुण भक्ति को दो धाराओं में बाँटा गया है:
1. राम भक्ति काव्य धारा
राम भक्ति धारा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पूजा की जाती है। यह धारा तुलसीदास के नेतृत्व में पुष्पित-पल्लवित हुई। राम को परब्रह्म का रूप माना गया जो धर्म, मर्यादा और आदर्श के प्रतीक हैं।
प्रमुख रामभक्त कवि
राम भक्ति शाखा में भगवान राम को साक्षात् ईश्वर का रूप मानते हुए उनके चरित्र, आदर्शों और लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास, नाभादास, और स्वामी अग्रदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
तुलसीदास (1532? – 1623)
तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनका जन्म स्थान राजापुर (बांदा, उत्तर प्रदेश) माना जाता है, हालांकि उनके जन्म काल को लेकर मतभेद हैं। तुलसीदास ने श्रीराम को भगवान विष्णु का अवतार मानते हुए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी। उन्होंने रामकथा को अवधी भाषा में लिखकर जनसामान्य के लिए सरल बना दिया।
तुलसीदास की प्रमुख रचनाएँ:
तुलसीदास जी की कुल 13 रचनाएँ प्रसिद्ध हैं:
- रामचरितमानस – तुलसीदास की सबसे प्रमुख कृति। इसमें राम के जीवन की कथा है।
- दोहावली – नीति, भक्ति और जीवन-दर्शन के दोहों का संग्रह।
- कवितावली – रामकथा के प्रसंगों को कविता में वर्णित किया गया है।
- गीतावली – गीतों के माध्यम से राम की महिमा का गान।
- कृष्ण गीतावली – भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन।
- विनय पत्रिका – भगवान से की गई करुण विनती।
- राम लला नहछू – बाल राम की स्तुति।
- वैराग्य संदीपनी – वैराग्य पर आधारित रचना।
- बरवै रामायण – रामकथा को बरवै छंद में लिखा गया।
- पार्वती मंगल – शिव-पार्वती विवाह की कथा।
- जानकी मंगल – राम-सीता विवाह की कथा।
- हनुमान बाहुक – हनुमान जी की स्तुति।
- रामाज्ञा प्रश्न – प्रश्नोत्तर शैली में धर्मोपदेश।
नाभादास (संवत् 1657 के आसपास)
नाभादास अग्रदास जी के शिष्य और तुलसीदास जी के समकालीन थे। ये महान भक्त और संत थे, जिन्होंने संतों की जीवनी पर आधारित काव्य लिखा। इन्होंने संत परंपरा को सहेजने का कार्य किया और कई संतों की वंदना करते हुए उन्हें लोकचेतना का भाग बनाया।
प्रमुख रचनाएँ:
- भक्तमाल – यह इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें 200 से अधिक संतों का वर्णन है।
- रामाष्टयाम – भगवान राम की स्तुति।
- रामचरित संग्रह – रामकथा पर आधारित रचना।
स्वामी अग्रदास (1556 के लगभग)
स्वामी अग्रदास कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे और रामानंद की परंपरा के साधक थे। इन्होंने भी राम के उपासक के रूप में अनेक काव्य रचनाएँ कीं। इनकी भाषा सरल और भक्ति से ओतप्रोत है।
प्रमुख रचनाएँ:
- हितोपदेश उपखाणाँ बावनी – नीति और भक्ति के उपदेश।
- ध्यानमंजरी – ध्यान पर केंद्रित रचना।
- रामध्यानमंजरी – भगवान राम के ध्यान की विधि।
- राम अष्ट्याम – राम की स्तुति के आठ पद।
2. कृष्ण भक्ति काव्य धारा
कृष्ण भक्ति धारा में भगवान श्रीकृष्ण को परम आराध्य मानकर उनकी विविध लीलाओं का गायन किया गया। यह धारा भाव, रस, संगीत और काव्य की त्रिवेणी है।
कृष्ण का स्वरूप
कृष्ण को ‘सच्चिदानंद’ रूप माना गया है—सत, चित और आनंद का मूर्त रूप। वे बालक रूप में माखनचोर हैं, युवा रूप में रासलीला नायक, तो कहीं अर्जुन के सारथी और गीता उपदेशक। भक्त उन्हें अपने-अपने भावों के अनुसार आराध्य रूप में देखते हैं—कोई उन्हें बालक मानता है, कोई सखा, कोई प्रेमी और कोई पति।
कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय
भक्तिकाल में कृष्ण भक्ति से जुड़े कई संप्रदाय उभरे:
- वल्लभाचार्य – पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक
- निंबार्काचार्य – निंबार्क संप्रदाय
- हित हरिवंश – राधावल्लभ संप्रदाय
- स्वामी हरिदास – हरिदासी संप्रदाय
- चैतन्य महाप्रभु – गौड़ीय संप्रदाय
अष्टछाप के कवि
वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति की धारा को गीतिकाव्य के माध्यम से प्रवाहित किया। इन आठ कवियों को ‘अष्टछाप’ कहा गया। इनका साहित्य श्रीमद्भागवत के आधार पर श्रीकृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं से युक्त है।
वल्लभाचार्य के चार शिष्य:
- सूरदास
- कुंभनदास
- परमानंददास
- कृष्णदास
विट्ठलनाथ के चार शिष्य:
- नंददास
- गोविंदस्वामी
- छीतस्वामी
- चतुर्भुजदास
प्रमुख कृष्णभक्त कवि
कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान कृष्ण को साकार ईश्वर मानते हुए उनकी बाल लीलाओं, रासलीला, प्रेम, और दिव्य गुणों का चित्रण किया गया है। इस शाखा में ब्रजभाषा का विशेष प्रयोग हुआ। प्रमुख कवियों में सूरदास, कुंभनदास, नंददास, रसखान और मीराबाई का नाम प्रमुख है।
सूरदास (1478–1573)
सूरदास को कृष्णभक्ति काव्यधारा का सर्वोच्च कवि माना जाता है। ये जन्म से नेत्रहीन थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने अपने पदों में बालकृष्ण की लीलाओं का अत्यंत कोमल और हृदयस्पर्शी चित्रण किया। इनकी रचनाओं में वात्सल्य रस का अद्भुत संयोग है।
प्रमुख रचनाएँ:
- सूरसागर – कृष्ण की बाल और युवा लीलाओं का अद्वितीय वर्णन, जिसमें पहले 125,000 पद थे, किंतु अब लगभग 45,000 पद ही प्राप्त होते हैं।
- सूरसारावली – 1103 पदों का संकलन।
- साहित्य लहरी – काव्य शास्त्र और भक्ति का समन्वय।
कुंभनदास (1468–1582)
कुंभनदास अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये वल्लभ सम्प्रदाय के अनन्य भक्त थे। इन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में कई पदों की रचना की। इनके पदों में माधुर्य और आध्यात्मिकता का संगम मिलता है। इनकी रचनाएँ फुटकर पदों के रूप में मिलती हैं।
इनकी सबसे प्रसिद्ध उक्ति है:
“संतन को कहां सिख दरबार।”
नंददास (1513–1583)
नंददास भी अष्टछाप के कवि थे। इन्होंने ब्रजभाषा में कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सरस और सुंदर चित्रण किया है। इनकी रचनाओं में राधा-कृष्ण की रासलीला, गोवर्धन पूजा, और प्रेम की अनुभूतियाँ प्रमुख हैं।
प्रमुख रचनाएँ:
- रासपंचाध्यायी
- सिद्धांत पंचाध्यायी
- अनेकार्थ मंजरी
- मानमंजरी
- रूपमंजरी
- विरहमंजरी
- भँवरगीत
- गोवर्धनलीला
- श्यामसगाई
- रुक्मिणीमंगल
- सुदामाचरित
- भाषादशम स्कंध
- पदावली
रसखान (1533–1588)
रसखान का असली नाम सैय्यद इब्राहिम था। ये एक मुस्लिम कवि थे जिन्होंने कृष्णभक्ति को जीवन का आधार बना लिया था। वे जन्म से मुस्लिम होते हुए भी श्रीकृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थे। इनके पदों में माधुर्य रस और कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम देखने को मिलता है।
प्रमुख रचनाएँ:
- सुजान रसखान
- प्रेमवाटिका – 52 दोहों में भक्ति और प्रेम का सुन्दर समन्वय।
इनकी प्रसिद्ध पंक्ति:
“मानुष हौं तो वही रसखानि, बसौं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।”
मीराबाई (1498–1547)
मीरा कृष्णभक्ति शाखा की एक विलक्षण कवयित्री थीं, जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ कर भक्ति का मार्ग चुना। वे राजघराने में जन्मी थीं, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर कृष्ण को पति मानकर जीवन भर उनकी भक्ति की।
मीरा के पद अत्यंत गेय और भावप्रवण होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत यातनाएँ झेलीं, लेकिन भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं हुईं। मीरा के पदों में प्रेम, विरह, समर्पण और संघर्ष का समन्वय है।
प्रमुख रचना:
- मीराबाई पदावली – इसमें उनके गाये हुए पदों का संकलन है।
उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ:
“पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।”
सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएँ
1. साकार ईश्वर की आराधना:
सगुण काव्यधारा में ईश्वर को साकार रूप में देखा गया है—राम और कृष्ण दो प्रमुख रूप हैं।
2. भावप्रधान काव्य:
इस काव्य में तर्क और दर्शन की अपेक्षा भाव, प्रेम, समर्पण और अनुभूति पर बल दिया गया।
3. लोकभाषा में रचना:
इस युग के कवियों ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि जनभाषाओं में रचना की, जिससे यह काव्य जन-जन तक पहुँचा।
4. संगीतात्मकता:
सगुण काव्यधारा के अधिकांश पद गेय हैं। इनमें संगीत की अनूठी छटा है।
5. नारी दृष्टिकोण:
कई भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति नायिका के रूप में प्रेम व्यक्त किया, जैसे मीरा, रसखान, सूरदास आदि।
6. सांस्कृतिक समरसता:
इस धारा ने जाति-पांति, धर्म, वर्गभेद को पीछे छोड़कर भक्ति को जीवन का मुख्य उद्देश्य माना।
सगुण भक्ति काव्य का प्रभाव
सगुण भक्ति धारा ने हिंदी साहित्य को आत्मा, भाव, रस और संगीत से भर दिया। इसने समाज को धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक एकता और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया। लोकभाषा में रचित इन रचनाओं ने जनता को न केवल आध्यात्मिक आनंद प्रदान किया, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक दिशा भी दी।
निष्कर्ष
सगुण काव्य धारा हिंदी साहित्य का वह अमर स्तंभ है, जिसकी छाया में आज भी भक्तों और साहित्यप्रेमियों की आत्मा भीगती है। यह धारा केवल भक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि मनुष्य के भावात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास की यात्रा भी है। राम और कृष्ण जैसे साकार ईश्वर के प्रति जनमानस के समर्पण ने जो अद्भुत काव्य रचा, वह आज भी हिंदी साहित्य के आकाश में दीपस्तंभ के रूप में उज्ज्वल है।
भक्ति का यह स्वर्णिम युग अपने समरसतावादी दृष्टिकोण, जन-जन तक पहुँचने वाली भाषा, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक ऊँचाइयों के कारण साहित्य और संस्कृति का आधार स्तंभ बन गया है।
सगुण भक्ति काव्य धारा: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. सगुण भक्ति काव्य धारा क्या है?
उत्तर: सगुण भक्ति काव्य धारा वह साहित्यिक परंपरा है जिसमें ईश्वर को साकार रूप में (जैसे राम या कृष्ण) देखा और पूजा गया है। इसमें भक्त अपने आराध्य के रूप, गुण, लीलाओं आदि का वर्णन करता है।
2. सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है?
उत्तर: सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार (रूपवान) माना जाता है जबकि निर्गुण भक्ति में निराकार (रूपहीन) ईश्वर की उपासना की जाती है।
3. सगुण भक्ति की दो प्रमुख शाखाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर:
- राम भक्ति शाखा
- कृष्ण भक्ति शाखा
4. भक्ति काल का समय कब से कब तक माना जाता है?
उत्तर: भक्ति काल को 1350 ई. से 1650 ई. तक का काल माना जाता है।
5. भक्ति काल को हिंदी साहित्य का ‘स्वर्ण युग’ क्यों कहा जाता है?
उत्तर: इस काल में साहित्य ने धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और जन-प्रिय रूप धारण किया, इसलिए इसे ‘स्वर्ण युग’ कहा गया।
6. राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं?
उत्तर: तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास प्रमुख रामभक्त कवि हैं।
7. कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं?
उत्तर: सूरदास, मीरा, रसखान, नंददास, कुंभनदास आदि प्रमुख कृष्णभक्त कवि हैं।
8. तुलसीदास की प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, आदि।
9. सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है?
उत्तर: सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है।
10. मीरा किसकी भक्ति करती थीं?
उत्तर: मीरा श्रीकृष्ण की उपासिका थीं और उन्हें अपना पति मानती थीं।
11. रसखान कौन थे और क्या विशेषता थी उनकी?
उत्तर: रसखान एक मुस्लिम भक्त कवि थे जिन्होंने श्रीकृष्ण को प्रेमपूर्वक अपनाया और ब्रजभाषा में काव्य रचना की। उन्हें प्रेम रस की खान कहा जाता है।
12. ‘अष्टछाप’ क्या है?
उत्तर: अष्टछाप श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ के आठ प्रमुख शिष्यों का समूह था, जिन्होंने श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित पदों की रचना की।
13. अष्टछाप के कवि कौन-कौन थे?
उत्तर: सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविन्दस्वामी, नंददास, छीतस्वामी और चतुर्भुजदास।
14. सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:
- ईश्वर का साकार रूप में चित्रण
- भावनात्मकता और प्रेमपूर्ण भक्ति
- सरल, सरस और गेय भाषा
- लोकभाषा का प्रयोग (ब्रज, अवधी)
- नायक-नायिका भावों में ईश्वर का चित्रण
15. सगुण काव्य में कौन-सी भाषाएं प्रमुख थीं?
उत्तर: मुख्य रूप से ब्रजभाषा और अवधी का प्रयोग हुआ।
16. राम भक्ति धारा किस सम्प्रदाय से संबंधित है?
उत्तर: रामानंद सम्प्रदाय से।
17. कृष्ण भक्ति काव्य पर किस सम्प्रदाय का प्रभाव रहा?
उत्तर: वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग सम्प्रदाय का।
18. ‘भक्ति’ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
उत्तर: ‘भक्ति’ शब्द संस्कृत की ‘भज’ धातु से बना है जिसका अर्थ है– प्रेमपूर्वक सेवा या आराधना
19. रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है?
उत्तर: अवधी भाषा में।
20. सगुण भक्ति कवियों की रचनाओं में कौन-से रस प्रमुख हैं?
उत्तर: श्रृंगार रस और भक्ति रस प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं।
21. कृष्ण को ‘पूर्ण ब्रह्म’ क्यों कहा गया है?
उत्तर: श्रीमद्भागवत के अनुसार कृष्ण को सत, चित और आनंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म माना गया है, जो सम्पूर्ण शक्तियों से युक्त हैं।
22. सगुण भक्ति काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
उत्तर: भगवान के प्रति निष्काम प्रेम और आत्मसमर्पण की भावना को जागृत करना।
23. सगुण भक्ति काव्य में स्त्री कवियों की भूमिका कैसी रही?
उत्तर: मीरा जैसी कवयित्री ने समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए सगुण भक्ति काव्य को एक सशक्त स्वर दिया।
24. क्या सगुण भक्ति कवि किसी एक धर्म या जाति से थे?
उत्तर: नहीं, इन कवियों में सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग थे, जैसे रसखान (मुस्लिम), रविदास (दलित), मीरा (राजपूत स्त्री) आदि।
25. सगुण भक्ति काव्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर: इसने सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और जातिवाद के विरुद्ध एक नई चेतना का प्रसार किया।
इन्हें भी देखें –
- निर्गुण भक्ति काव्य धारा: अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और साहित्यिक विशेषताएँ
- सूफी काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- संत काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- कृष्ण भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- राम भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- सुहाग की साड़ी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- दिल की रानी | एक ऐतिहासित कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- जुलूस | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- शतरंज के खिलाड़ी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- ईदगाह | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- Preposition: Definition, Types, and 100+ Examples
- Wh- Word and Wh- Question
- Article: Definition, Types, and 100+ Examples
- Determiner: Definition, Types, and 100+ Examples
- Phrase: Definition, Types, and 100+ Examples
- Sentence Analysis with examples
- उत्तर वैदिक काल | 1000-500 | ई.पू. The Post Vedic Age
- धार्मिक आन्दोलन Religious Movements(600 ईसा पूर्व)