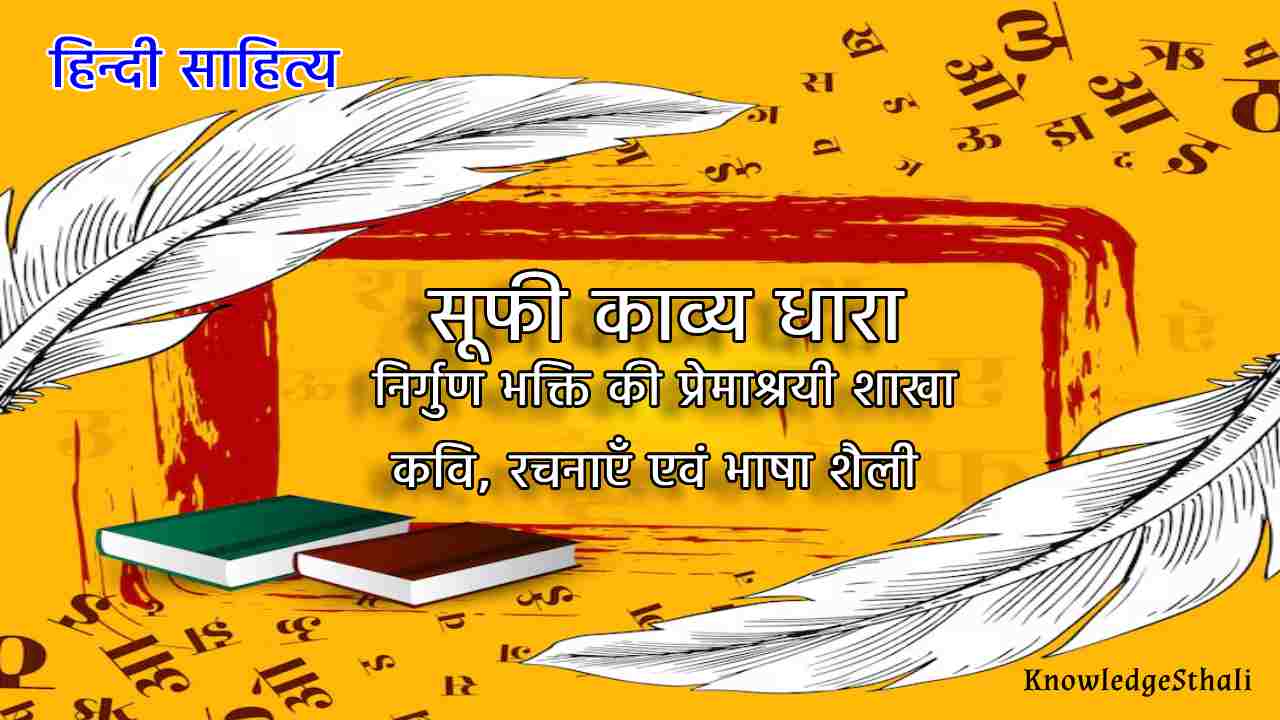सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेममार्गी या प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जाता है, हिन्दी साहित्य की एक समृद्ध, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। यह धारा भारतीय और फारसी परंपराओं का संगम है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम (इश्क-ए-हकीकी) की प्राप्ति को प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इस काव्यधारा में मसनवी शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और यह मुख्यतः अवधी भाषा में विकसित हुई।
सूफी कवियों ने हिन्दू लोककथाओं, प्रतीकों और चरित्रों को आधार बनाकर प्रेम की अनुभूति को गहराई से प्रस्तुत किया। प्रमुख सूफी कवियों में जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन, कुतुबन, नूर मोहम्मद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाएं जैसे पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मधुमालती इत्यादि केवल प्रेमकथाएँ नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीकात्मक व्याख्याएँ हैं। सूफी काव्य न केवल धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है, बल्कि हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह धारा श्रृंगार, भक्ति, दर्शन, और मानवतावाद के गहन तत्वों को समेटे हुए है, जो आज भी हिन्दी साहित्य में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है।
सूफी काव्य धारा
हिन्दी साहित्य की विविध काव्य धाराओं में सूफी काव्य धारा एक विशिष्ट और आत्मिक रंग लिए हुए है। यह धारा केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह काव्यधारा मानव-हृदय की उस भावना को स्वर देती है जो प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानती है। इसे प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेममार्गी काव्य, प्रेमाख्यान काव्य या रोमांटिक कथा काव्य के रूप में भी जाना जाता है।
सूफी शब्द का अर्थ और उद्भव
“सूफी” शब्द अरबी मूल का है, जो “सूफ” (ऊन) से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है – “पवित्र वस्त्रधारी”। सूफियों का जीवन अत्यंत सरल, सात्त्विक, और भौतिकता से रहित होता था। वे सफेद ऊन के चोगे पहनते थे, जो उनकी वैराग्यवृत्ति और पवित्रता का प्रतीक था। सूफी संप्रदाय का मूल आधार प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता पर टिका है।
सूफी मत का प्रसार भारत में 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसे लोकप्रिय और सामाजिक स्तर पर फैलाने का कार्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। उन्होंने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, मानवता और प्रेम के आदर्शों को प्रचारित किया।
सूफी काव्य की विशेषताएँ
सूफी काव्य धारा में एक विशिष्ट प्रकार का आध्यात्मिक प्रेम है जिसे इश्क हकीकी (अलौकिक प्रेम) कहा जाता है। इसकी अभिव्यक्ति इश्क मिजाजी (लौकिक प्रेम) के माध्यम से की जाती है। सूफी कवि लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा ईश्वर के साथ आत्मा के मिलन की कल्पना करते हैं। इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- मसनवी शैली का प्रभाव – फारसी साहित्य की मसनवी (कथा-काव्य) परंपरा का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें प्रायः ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति, गुरु प्रशंसा आदि का वर्णन होता है।
- अलौकिक प्रेम की व्यंजना – प्रेम का उद्देश्य केवल नायिका को पाना नहीं होता, बल्कि उस माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करना होता है।
- नायक-नायिका की प्रतीकात्मकता – नायक आत्मा है और नायिका परमात्मा। रचनाओं में प्रतीकात्मक चरित्र और स्थानों के माध्यम से दार्शनिक तत्वों की प्रस्तुति होती है।
- श्रृंगार रस की प्रधानता – प्रेम की कोमल और सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रृंगार रस का व्यापक उपयोग होता है।
- कथा-संगठन में रूढ़ियाँ – सूफी प्रेमाख्यानों में कथानक की विशेष रूप से एक नियत संरचना होती है – जैसे राजा, राजकुमारी, गुरु, विरोधी शक्तियाँ आदि।
- हिन्दू लोककथाओं का समावेश – भारतीय लोक संस्कृति से जुड़ी कहानियों को आधार बनाकर उन्हें सूफी दर्शन से जोड़ा गया है।
- सम्प्रदायिक कट्टरता का अभाव – इन काव्य रचनाओं में किसी धर्म या सम्प्रदाय की आलोचना नहीं है, बल्कि समन्वय और प्रेम पर बल दिया गया है।
- भाषाई शैली – प्रमुखतः अवधी भाषा में रचनाएं हुईं, लेकिन ब्रज, राजस्थानी व अन्य बोलियों का भी प्रभाव देखा जाता है।
सूफी प्रेमाख्यान काव्य: प्रतीक और दार्शनिक तत्व
सूफी काव्य में प्रेमकथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि गूढ़ तत्वज्ञान का भी माध्यम हैं। विशेषकर मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें पात्रों को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है:
- चितौड़ – शरीर
- रत्नसेन – मन
- पद्मावती – सात्विक बुद्धि
- सिंहलद्वीप – हृदय
- हीरामन तोता – गुरु
- राघवचेतन – शैतान
- नागमती – संसार
- अलाउद्दीन – माया रूपी आसुरी शक्ति
इस तरह पूरी प्रेमकथा एक आत्मिक यात्रा बन जाती है जो आत्मा के ईश्वर मिलन की ओर ले जाती है।
सूफी काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएँ
| क्रम | कवि (रचनाकार) | प्रमुख रचनाएँ |
|---|---|---|
| 1 | मुल्ला दाऊद | चंदायन (लोरकहा) – 1372 ई. (अवधी, कडवक शैली) |
| 2 | कुतुबन | मृगावती – आचार्य शुक्ल ने इसे पहला सूफी ग्रंथ माना |
| 3 | मंझन | मधुमालती – एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण |
| 4 | जायसी | पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा |
| 5 | असाइत | हंसावली – राजस्थानी भाषा में |
| 6 | दामोदर कवि | लखमसेन पद्मावती कथा – राजस्थानी |
| 7 | ईश्वर दास | सत्यवती कथा |
| 8 | नंददास | रूप मंजरी – ब्रजभाषा में प्रेम कथा |
| 9 | उस्मान | चित्रावली |
| 10 | शेख नबी | ज्ञानदीप |
| 11 | कासीम शाह | हंस जवाहिर |
| 12 | नूर मोहम्मद | इन्द्रावती, अनुराग बांसुरी (बरवै छंद में) |
| 13 | जान कवि | कथारूप मंजरी |
| 14 | पुहकर कवि | रसरतन |
| 15 | आलम | माधवानल कामकंदला |
प्रसिद्ध रचनाएँ और उनकी विशेषताएं
1. चंदायन (मुल्ला दाऊद)
- हिन्दी का पहला सूफी काव्य, 1372 ई.
- अवधी भाषा में रचित
- ‘लोरिक-चंदा’ की प्रेमकथा
- कडवक शैली का प्रयोग (पाँच अर्द्धालियाँ और एक दोहा)
2. मृगावती (कुतुबन)
- नायिका-प्रधान प्रेमकथा
- इस ग्रंथ को सूफी काव्य परंपरा का आरंभ माना गया
- कथा शैली में शुद्ध भारतीयता और सूफी तत्त्वों का समावेश
3. मधुमालती (मंझन)
- प्रेम का प्रतीकात्मक चित्रण
- प्रेम में एकनिष्ठता पर बल
- नायक की तपस्या और साधना के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति
4. पद्मावत (मलिक मोहम्मद जायसी)
- सूफी काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति
- अलंकार, प्रतीक और दर्शन का सुंदर संयोजन
- 1540 ई. में रचित
- पद्मावती के माध्यम से आत्मा की परमात्मा से मिलने की कथा
5. अनुराग बांसुरी (नूर मोहम्मद)
- बरवै छंद में रचित
- प्रेम को संगीत और अध्यात्म से जोड़ने वाला काव्य
सूफी काव्य में भाषा और शैली
सूफी काव्य मुख्यतः अवधी भाषा में रचा गया है। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा, राजस्थानी और अन्य क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। भाषा में सहजता, सरलता और भावप्रवणता होती है। शैली में मसनवी, कडवक, बरवै आदि छंदों का प्रयोग होता है।
महत्वपूर्ण आलोचकों की दृष्टि से
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल – सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रभाव तथा प्रतीकात्मक प्रेम का विवेचन।
- रामकुमार वर्मा – चंदायन से सूफी परंपरा का आरंभ मानते हैं।
- गणपति चन्द्रगुप्त – इसे रोमांटिक कथा काव्य की संज्ञा दी।
सूफी कवियित्री: राबिया
सूफी परंपरा में राबिया एक प्रमुख महिला संत थीं, जिन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्याख्या की। उनके प्रेम-भावना परक भजन इस परंपरा में नारी-सशक्तिकरण और आध्यात्मिकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
निष्कर्ष
सूफी काव्य धारा केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संवाद भी था। इस धारा ने हिन्दू-मुस्लिम समाज को जोड़ने का कार्य किया। इसमें प्रेम को आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम बनाया गया। सूफी कवियों ने प्रेम के माध्यम से धार्मिक रूढ़ियों को तोड़कर मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखा। इस काव्य परंपरा की सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक समरसता और दार्शनिक गहराई आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी।
इस प्रकार, सूफी काव्य धारा प्रेम, भक्ति, दर्शन, साहित्य और सांप्रदायिक समरसता का अद्भुत संगम है, जो हिन्दी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: सूफी काव्य धारा क्या है?
उत्तर:
सूफी काव्य धारा हिन्दी साहित्य की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें प्रेम को आध्यात्मिक अनुभूति और ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना गया है। यह प्रेमाश्रयी या प्रेममार्गी काव्य कहलाता है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम (ईश्वरीय मिलन) की प्राप्ति का चित्रण होता है।
प्रश्न 2: सूफी शब्द का क्या अर्थ है?
उत्तर:
सूफी शब्द ‘सूफ’ (ऊन) से बना है, जिसका अर्थ है ‘पवित्र वस्त्र’। यह सूफी संतों की साधना, वैराग्य और आध्यात्मिक जीवनशैली का प्रतीक है। सूफी लोग सफेद ऊन के वस्त्र पहनते थे और आत्मिक पवित्रता में विश्वास रखते थे।
प्रश्न 3: सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:
सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं:
- मसनवी शैली का प्रभाव
- प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति
- प्रतीकात्मक पात्रों और कथाओं का प्रयोग
- श्रृंगार रस की प्रधानता
- सम्प्रदायिक कट्टरता का अभाव
- अवधी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग
- हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय
प्रश्न 4: सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था?
उत्तर:
इस काव्य का उद्देश्य लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से पाठकों को आध्यात्मिक प्रेम और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर प्रेरित करना था। यह धार्मिक समरसता, प्रेम, करुणा और आत्मिक उन्नति का संदेश देता है।
प्रश्न 5: सूफी काव्य के प्रमुख कवि कौन-कौन हैं?
उत्तर:
सूफी काव्य के प्रमुख कवि हैं:
- मुल्ला दाऊद (चंदायन)
- कुतुबन (मृगावती)
- मंझन (मधुमालती)
- मलिक मोहम्मद जायसी (पद्मावत)
- नूर मोहम्मद (अनुराग बांसुरी, इन्द्रावती)
- नंददास (रूपमंजरी)
- दामोदर कवि, असाइत, शेख नबी, पुहकर आदि
प्रश्न 6: मलिक मोहम्मद जायसी की ‘पद्मावत’ काव्य की विशेषताएं क्या हैं?
उत्तर:
‘पद्मावत’ एक रूपक काव्य है जिसमें पात्र प्रतीकात्मक हैं। यह काव्य आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा को दर्शाता है। इसमें चितौड़, रत्नसेन, पद्मावती, हीरामन तोता आदि प्रतीकों के माध्यम से दार्शनिक भावों की प्रस्तुति की गई है।
प्रश्न 7: सूफी काव्य में ‘इश्क मिजाजी’ और ‘इश्क हकीकी’ का क्या अर्थ है?
उत्तर:
- इश्क मिजाजी का अर्थ है लौकिक प्रेम (नायक-नायिका का प्रेम)।
- इश्क हकीकी का अर्थ है अलौकिक प्रेम (आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम)।
सूफी काव्य में लौकिक प्रेम को माध्यम बनाकर अलौकिक प्रेम की ओर ले जाया जाता है।
प्रश्न 8: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सूफी काव्य को किस प्रकार परिभाषित किया है?
उत्तर:
आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य में फारसी मसनवी शैली का प्रभाव माना है। उन्होंने कुतुबन की ‘मृगावती’ को हिन्दी का पहला सूफी ग्रंथ माना है और जायसी की ‘पद्मावत’ को प्रतीकात्मक आध्यात्मिक प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है।
प्रश्न 9: क्या सूफी काव्य केवल मुस्लिम कवियों द्वारा रचा गया है?
उत्तर:
नहीं, सूफी काव्य केवल मुस्लिम कवियों द्वारा ही नहीं रचा गया है। यद्यपि सूफी परंपरा मूलतः इस्लाम से जुड़ी हुई है और इसके प्रमुख कवि मुस्लिम ही थे, लेकिन भारतीय संदर्भ में सूफी काव्य की पहुँच संप्रदाय, धर्म और जाति से परे रही है। इस कवियों ने हिन्दू समाज की लोककथाओं, प्रतीकों और संस्कृति को अपनाया और किसी धर्म की निंदा नहीं की। इस काव्य में सांस्कृतिक समन्वय का अनुपम उदाहरण मिलता है।
कबीर, रविदास, दादू जैसे हिंदू संतों की वाणी में भी सूफी दर्शन के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। रसखान जैसे मुस्लिम कवि तो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में विलीन हो गए और सगुण काव्यधारा का ही अंग बन गए।
विस्तार से समझिए:
✅ 1. सूफी काव्य का मूल स्वर:
- सूफी काव्य में प्रेम, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात होती है।
- यह सांसारिक सीमाओं को लांघते हुए मानवता, प्रेम और ईश्वर से मिलन की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति करता है।
✅ 2. मुस्लिम सूफी कवि:
- बुल्लेशाह, अमीर खुसरो, शाह हुसैन, वारिस शाह, शेख फरीद, मलिक मुहम्मद जायसी आदि प्रमुख मुस्लिम सूफी कवि रहे हैं।
✅ 3. हिंदू कवियों पर सूफी प्रभाव:
- कई हिंदू कवियों ने भी सूफी विचारधारा से प्रेरणा लेकर काव्य रचना की। उदाहरणस्वरूप:
- रसखान – यद्यपि मुस्लिम थे, उन्होंने सूफी प्रेम मार्ग के साथ-साथ कृष्ण भक्ति में विलीन होकर काव्य रचा।
- कबीर – निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे, जिनके विचारों में सूफी और वैष्णव भक्ति दोनों का गहरा प्रभाव दिखता है।
- धन्ना, सदना, पीपा, रविदास जैसे संतों की रचनाओं में सूफी भाव दृष्टिगोचर होते हैं।
✅ 4. सूफी काव्य की बहुधार्मिक प्रकृति:
- सूफी संतों ने अक्सर स्थानीय भाषाओं में लिखा और अपना संदेश सभी समुदायों तक पहुँचाया।
- इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में समान रूप से स्थान पाया।
सूफी काव्य की आत्मा धर्म से ऊपर है। यद्यपि इसकी जड़ें इस्लामी सूफी परंपरा में हैं, पर भारतीय सांस्कृतिक धरातल पर यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समन्वय की परंपरा बन गई जिसमें मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों कवियों ने योगदान दिया।
प्रश्न 10: सूफी काव्य किस भाषा में लिखा गया था?
उत्तर:
सूफी काव्य मुख्यतः अवधी भाषा में लिखा गया, लेकिन इसमें ब्रज, राजस्थानी और अन्य क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव देखा जाता है
प्रश्न 11: संत कबीर किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं?
➤ संत कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कवि हैं।
प्रश्न 12: सूफी काव्य धारा को किन अन्य नामों से जाना जाता है?
➤ सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी, प्रेममार्गी, प्रेमाख्यानक, और रोमांटिक कथा काव्य के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न 13: हिन्दी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है?
➤ हिन्दी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है।
प्रश्न 14: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने किसे पहला सूफी कवि माना है?
➤ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कुतुबन को पहला सूफी कवि माना है।
प्रश्न 15: सूफी काव्य में किस शैली का प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई देता है?
➤ सूफी काव्य में फारसी मसनवी शैली का प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जाता है
प्रश्न 16: जायसी की प्रमुख रचना कौन-सी है?
➤ जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत है।
प्रश्न 17: ‘चंदायन’ काव्य के रचयिता कौन हैं?
➤ मुल्ला दाऊद ‘चंदायन’ काव्य के रचयिता हैं।
प्रश्न 18: ‘मृगावती’ नामक प्रेमकथा काव्य किसने लिखा है?
➤ मृगावती की रचना कुतुबन ने की है।
प्रश्न 19: ‘मधुमालती’ किस सूफी कवि की रचना है?
➤ ‘मधुमालती’ मंझन की रचना है।
प्रश्न 20: जायसी के गुरु का नाम क्या था?
➤ जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी और सैय्यद अशरफ था।
प्रश्न 21: ‘अनुराग बांसुरी’ किस कवि की रचना है?
➤ ‘अनुराग बांसुरी’ की रचना नूर मोहम्मद ने की है।
प्रश्न 22: ‘रूप मंजरी’ किस कवि की रचना है और किस भाषा में है?
➤ ‘रूप मंजरी’ नंददास द्वारा रचित एक प्रेमकथा है, जो ब्रजभाषा में लिखी गई है
प्रश्न 23: सूफी काव्य की भाषा क्या थी?
➤ सूफी काव्य मुख्यतः अवधी भाषा में रचा गया था, साथ ही क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव था।
प्रश्न 24: सूफी काव्य में कौन-से रस की प्रधानता होती है?
➤ सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है।
प्रश्न 25: ‘पद्मावत’ एक रूपक काव्य है – इसमें चितौड़ किसका प्रतीक है?
➤ ‘पद्मावत’ में चितौड़ शरीर का प्रतीक है।
प्रश्न 26: सूफी काव्य में ‘इश्क मिजाजी’ और ‘इश्क हकीकी’ का क्या अर्थ है?
➤ इश्क मिजाजी का अर्थ लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी का अर्थ अलौकिक, ईश्वरीय प्रेम है।
प्रश्न 27: ‘ज्ञानदीपक’ रचना किस कवि ने लिखी?
➤ ‘ज्ञानदीपक’ की रचना शेख नबी ने की है।
प्रश्न 28: ‘हंसावली’ किस भाषा में लिखी गई रचना है और इसके रचयिता कौन हैं?
➤ ‘हंसावली’ राजस्थानी भाषा में रचित काव्य है, जिसे असाइत ने लिखा है।
प्रश्न 29: ‘लखमसेन पद्मावती कथा’ के रचयिता कौन हैं?
➤ ‘लखमसेन पद्मावती कथा’ के रचयिता दामोदर कवि हैं।
प्रश्न 20: ‘हंस जवाहिर’ नामक रचना किसने लिखी है?
➤ ‘हंस जवाहिर’ की रचना कासीम शाह ने की है।
यदि आपके मन में सूफी काव्य या प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हो, तो आप नीचे टिप्पणी कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं।
Hindi – KnowledgeSthali
इन्हें भी देखें –
- संत काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- कृष्ण भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- राम भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- सुहाग की साड़ी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- पूस की रात | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- मृत्यु के पीछे | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- बूढ़ी काकी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- नागपूजा | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- सवा सेर गेंहूँ | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- शब्द किसे कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द
- पदबन्ध (Phrase) | परिभाषा, भेद एवं उदाहरण