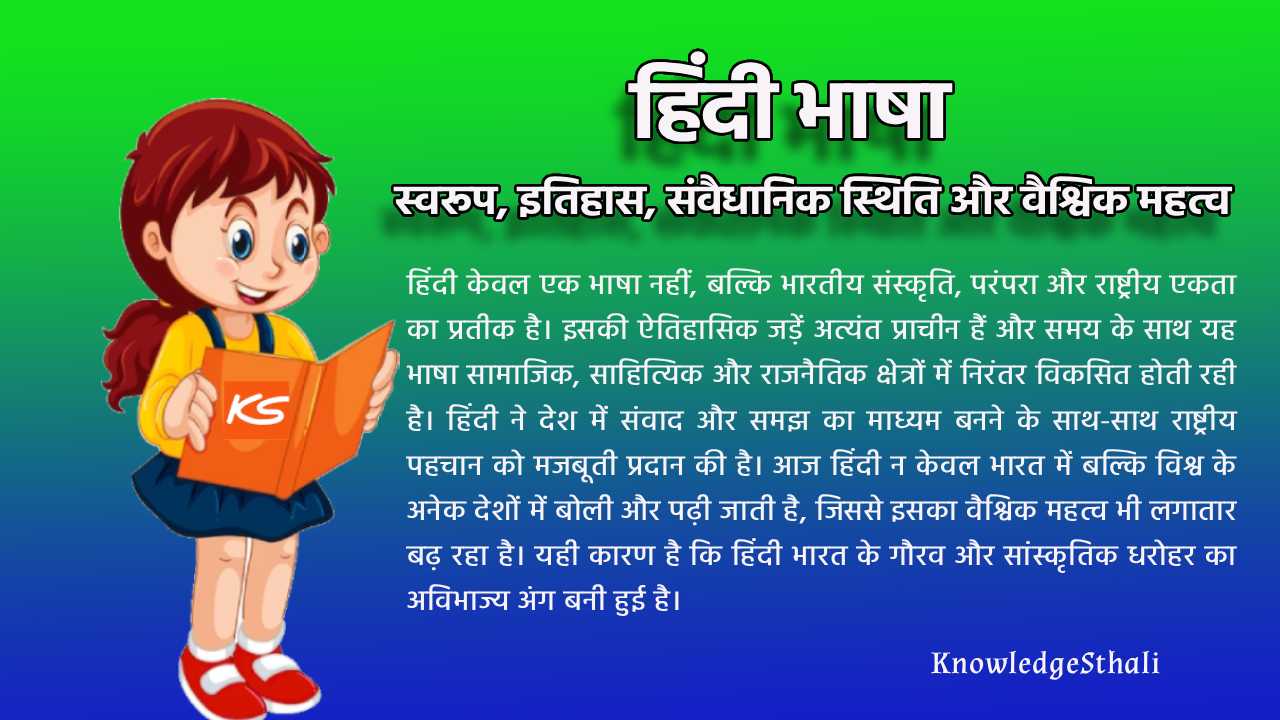हिंदी भाषा विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह भारत की राजभाषा है और भारतीय समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में हिंदी बोलने वालों की संख्या 72 करोड़ से अधिक है, जिसमें से लगभग 61 करोड़ लोग इसे मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। यह विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है।
अक्सर हिंदी को भारत की “राष्ट्रभाषा” मान लिया जाता है, किंतु यह एक भ्रांति है। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। संविधान ने हिंदी को राजभाषा का स्थान अवश्य दिया है और अंग्रेज़ी को सह-आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है।
हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और भाषा परिवार
“हिंदी” शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के “सिन्धु” शब्द से मानी जाती है। “सिन्धु” से “हिंद” और फिर “हिंदी” शब्द का निर्माण हुआ। यह भाषा भारोपीय भाषा परिवार (Indo-European Family) की सदस्य है और इसका विकास प्राचीन संस्कृत से हुआ है। हिंदी की जड़ें प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में पाई जाती हैं।
भारत की भौगोलिक सीमाएँ और उनके नाम समय-समय पर बदलते रहे हैं। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त, भारतखण्ड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और भारत कहा गया। समय के साथ “हिंद” और “हिंदुस्तान” शब्द भी भारत की संज्ञा के रूप में प्रचलित हुए, जिनकी उत्पत्ति ईरानी सम्पर्क से मानी जाती है। विद्वानों के अनुसार “हिंदी” शब्द “हिंदुस्तान” से भी अधिक प्राचीन है।
“हिंद” और “हिंदुस्तान” शब्द का का विकास
पारसी धार्मिक ग्रंथ ‘दसातीर’ में “हिंद” शब्द का उल्लेख मिलता है। पं. रामनरेश त्रिपाठी का मत है कि महर्षि वेदव्यास के समय में ही ईरान के लोग भारत को “हिंद” कहने लगे थे।
- ऋग्वेद में “सिन्धु” और “सप्त सिन्धवः” शब्द नदियों और विशेष प्रदेश के लिए प्रयुक्त हुए हैं।
- प्राचीन ईरानी साहित्य में भी “हिंद” शब्द सिन्धु नदी और उसके आस-पास के प्रदेश के लिए प्रयुक्त हुआ।
- महाभारत में भी “हिंद” शब्द एक विशेष प्रदेश की संज्ञा के रूप में मिलता है।
संभवतः यही शब्द याजकों और विद्वानों के साथ ईरान पहुँचे और वहाँ यह हैन्दु, हिन्दू, हफ्त हिन्दवः (अवेस्ता में) के रूप में प्रचलित हुआ। भाषाशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय आर्यभाषा की “स” ध्वनि ईरानी भाषाओं में “ह” में बदल जाती है। जैसे –
- सप्त → हफ्त
- असुर → अहुर
प्राचीन पह्लवी भाषा में “हिन्दू, हिन्दुक और हिन्दश” शब्द मिलते हैं। मध्यकालीन ईरानी में विशेष प्रत्यय “ईक” जोड़कर “हिन्दीक” और आगे चलकर “हिन्दीग” शब्द बना, जिससे आधुनिक “हिंदी” शब्द का जन्म हुआ।
‘हिन्दू’ और ‘हिन्दी’ शब्द की उत्पत्ति
भाषाविद् डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार ‘हिन्दू’ शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रचित ग्रंथ ‘निशीथचूर्णि’ में मिलता है। यह शब्द मूलतः फारसी है, जो संस्कृत के ‘सिन्धु’ शब्द का रूपान्तर है।
- ऋग्वेद में ‘सिन्धु’ का प्रयोग कभी सामान्यतः नदी, कभी किसी विशेष नदी और कभी उसके आसपास के क्षेत्र के लिए हुआ है।
- लगभग 500 ईसा पूर्व दारा प्रथम के समय में यह क्षेत्र ईरानियों के नियंत्रण में आ गया और संस्कृत का ‘सिन्धु’ वहाँ ‘हिन्दू’ बन गया।
- धीरे-धीरे इसका प्रयोग सिन्धु नदी के आसपास की भूमि और फिर भारतवर्ष तक विस्तृत हो गया।
ध्वन्यात्मक कारणों से इसमें ‘उ’ ध्वनि लुप्त हो गई और यह रूप ‘हिन्द’ बन गया। आगे चलकर इसमें विशेषणार्थक प्रत्यय ‘ईक’ जुड़ने से ‘हिन्दीक’ बना, और फिर ‘क’ के लोप से आधुनिक शब्द ‘हिन्दी’ का जन्म हुआ।
व्याकरणिक विकास क्रम:
सिन्धु (संस्कृत) → हिन्दु (अवेस्ता/फारसी) → हिन्द → हिन्दीक → हिन्दी
यूनानी और यूरोपीय दृष्टिकोण
यूनानी लेखकों ने सिन्धु नदी को ‘इन्दोस’, यहाँ के निवासियों को ‘इन्दोई’ और पूरे क्षेत्र को ‘इन्दिका’ कहा। यही शब्द आगे चलकर अंग्रेज़ी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में ‘इण्डिया’ बन गया।
यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी प्राचीन आर्यभाषा में ‘हिन्दी’ शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। केवल जैन महाराष्ट्री साहित्य में ‘हिन्दुग’ शब्द मिलता है, जैसे—
“सूरिणा भणियम् रामाणो जेण हिन्दुग देसम् बच्चामो।”
हिंदी भाषा का उद्भव और विकास क्रम
(क) शब्द-व्युत्पत्ति और नामकरण की प्रक्रिया
हिंदी शब्द का विकास संस्कृत के “सिन्धु” से होकर हुआ, जो आगे चलकर हिन्दु → हिन्द → हिन्दीक → हिन्दी बना। यह परिवर्तन मुख्यतः भाषाशास्त्रीय और ध्वन्यात्मक बदलावों का परिणाम था, जिसमें ईरानी और यूनानी प्रभाव भी जुड़ते गए।
(ख) भाषा-विकास की प्रक्रिया
हिंदी भाषा स्वयं संस्कृत से निकलकर कई चरणों से गुज़री:
संस्कृत → पालि → प्राकृत → अपभ्रंश → अवहट्ट → प्राचीन हिंदी → आधुनिक हिंदी
यह क्रम भाषाई एवं साहित्यिक विकास को दर्शाता है, जिसके माध्यम से हिंदी धीरे-धीरे एक समृद्ध भाषा बनी और आज विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है।
यही क्रम आगे चलकर आधुनिक हिंदी के रूप में विकसित हुआ, जिसने आज विश्व की प्रमुख भाषाओं में स्थान प्राप्त किया है।
(1) शब्दगत विकास तालिका
| चरण | शब्द-रूप | स्रोत/प्रभाव | विशेष टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | सिन्धु | संस्कृत | नदी और क्षेत्र विशेष का नाम |
| 2 | हिन्दु | अवेस्ता/फ़ारसी | ‘स’ ध्वनि का ‘ह’ में रूपांतरण |
| 3 | हिन्द | ईरानी प्रभाव | क्षेत्र का नाम |
| 4 | हिन्दीक | व्याकरणिक प्रत्यय ‘ईक’ | विशेषणात्मक रूप |
| 5 | हिन्दी | आधुनिक रूप | वर्तमान प्रयोग में भाषा का नाम |
(2) भाषाई विकास तालिका
| चरण | भाषा-रूप | समय/कालखंड | विशेषता |
|---|---|---|---|
| 1 | संस्कृत | वैदिक और शास्त्रीय युग | भारतीय आर्य भाषाओं की जननी |
| 2 | पाली | 6वीं–3री शताब्दी ई.पू. | बुद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा |
| 3 | प्राकृत | 3री शताब्दी ई.पू.–6वीं ई. | सरल बोलचाल की भाषा |
| 4 | अपभ्रंश | 6वीं–10वीं शताब्दी | क्षेत्रीय भाषाओं की आधारभूमि |
| 5 | अवहट्ट | 10वीं–12वीं शताब्दी | प्राचीन हिंदी की कड़ी |
| 6 | प्राचीन हिंदी | 12वीं–14वीं शताब्दी | आदिकालीन हिंदी साहित्य |
| 7 | आधुनिक हिंदी | 14वीं शताब्दी से वर्तमान | संपर्क भाषा और विश्वस्तरीय महत्व |
हिंदी का ऐतिहासिक विकास
हिंदी भाषा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसका विकास कई चरणों से होकर हुआ है:
- वैदिक संस्कृत (1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व) – भारत की प्राचीन धार्मिक भाषा, जिसमें ऋग्वेद और अन्य वेद रचे गए।
- लौकिक संस्कृत और प्राकृत (600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी) – आम बोलचाल की भाषा के रूप में प्राकृत और पालि का विकास हुआ।
- अपभ्रंश (6वीं से 12वीं शताब्दी) – प्राकृत से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जिनसे आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ निकलीं।
- प्रारंभिक हिंदी (12वीं से 18वीं शताब्दी) – इस काल में अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का उदय हुआ। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रहीम जैसे संत कवियों ने हिंदी को लोकप्रिय बनाया।
- आधुनिक हिंदी (19वीं शताब्दी से वर्तमान) – हिंदी को देवनागरी लिपि में मानक रूप दिया गया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने एकता की भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
‘हिन्दी’ शब्द का मूल अर्थ और प्रयोग
‘हिन्दी’ शब्द का मूल अर्थ
‘हिन्दी’ शब्द का मूल अर्थ है – ‘हिन्द का’ अथवा ‘भारतीय’। व्याकरण की दृष्टि से यह शब्द एक योगरूढ़ शब्द है। इस प्रकार के नामकरण अन्य देशों और भाषाओं में भी प्रचलित हैं, जैसे – जापानी, चीनी, नेपाली, भूटानी, रूसी, अमरीकी आदि।
धीरे-धीरे ‘हिन्द’ शब्द का प्रयोग केवल देश को सूचित करने के बजाय वहाँ के निवासियों और वस्तुओं के लिए भी होने लगा। उदाहरणस्वरूप, आरम्भिक काल में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पहचान हेतु भी “हिन्दी” शब्द का उपयोग होता था। अरबी और फारसी भाषाओं में “हिन्दी” शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की तलवार (भारतीय इस्पात से बनी हुई) के लिए किया जाता था।
‘हिन्दी’ शब्द का प्रयोग
हिंदी शब्द के प्रचलन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी प्राचीन भाषाओं में “हिंदी” शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। मुसलमानों के भारत आगमन से पूर्व भाषा के लिए “भाषा” या “भारवा” शब्द प्रचलित थे और इनका प्रयोग 1800 ई. के बाद तक होता रहा।
उदाहरणस्वरूप, संस्कृत ग्रंथों की टीकाओं को “भाषा-टीका” कहा जाता था। यहाँ तक कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए लल्लूलाल और सदल मिश्र को भी “भाषा मुंशी” अथवा “भारवा मुंशी” कहा गया।
मुसलमानों के भारत आगमन (13वीं–14वीं शताब्दी ई.) के बाद मध्यप्रदेश और उत्तर भारत की जनसामान्य की बोली के लिए हिंदी, हिन्दवी, हिन्दुई आदि नाम प्रचलित हुए।
‘हिन्दी’ शब्द का प्रारम्भिक भाषाई प्रयोग
‘हिन्दी’ शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में पहली बार पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ ‘पंचतंत्र’ से जुड़ा मिलता है। इस ग्रंथ का अनुवाद छठी शताब्दी में पह्लवी (प्राचीन ईरानी) भाषा में कराया गया था। उस समय के ईरानी सम्राट नौशेरवाँ (531–579 ई.) ने अपने दरबारी विद्वान वरजवैह (बर्जूयह/बजरोया) को भारत भेजा, जिन्होंने संस्कृत से पह्लवी में अनुवाद का कार्य किया।
नौशेरवाँ के मंत्री बर्जुरमहर ने इस अनुवाद की प्रस्तावना में उल्लेख किया कि यह कार्य “जबाने-हिन्दी” से किया गया है। यही वह अवसर था जब विदेशी ग्रंथों में संस्कृत या भारतीय भाषाओं के लिए ‘हिन्दी’ शब्द प्रयुक्त हुआ।
बाद के समय में यह पह्लवी अनुवाद लोकप्रिय हुआ और अनेक भाषाओं में रूपांतरित किया गया। उन सभी में ग्रंथ की मूल भाषा को ‘जबाने-हिन्दी’ ही कहा गया। सातवीं से दसवीं शताब्दी के बीच यह शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की पहचान के रूप में मिलता है। इसके बाद मध्यकालीन रचनाकारों ने ‘जबाने-हिन्दी’ के स्थान पर ‘हिन्दी’ और ‘हिन्दवी’ शब्दों का चलन आरम्भ कर दिया।
संवैधानिक स्थिति और आधिकारिक मान्यता
भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) में मिलता है।
- अनुच्छेद 343 के अनुसार, भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी होगी।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें हिंदी भी प्रमुख है।
- आठवीं अनुसूची की भाषाएँ हैं – कश्मीरी, सिन्धी, पंजाबी, हिन्दी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगू, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि केवल राजभाषा है।
हिंदी: राष्ट्रभाषा बनने की संभावनाएँ
हिंदी भारतीय भाषाओं में वह एकमात्र भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की सबसे अधिक संभावना रही है। इसका कारण यह है कि हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली और समझी जाती है। यह भाषा समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सम्पर्क माध्यम के रूप में सक्षम है तथा इसे सीखना अपेक्षाकृत सरल है।
हिंदी भाषा के विकास में समाज और संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, विशेषकर उत्तर भारतीय राज्यों की। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है और उसी से विभिन्न कालखंडों में हुए विभाजन और रूपांतरण से हिंदी का उद्भव हुआ।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी जनता की भाषा और एकता का प्रतीक बन गई। इस दौर में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हुई। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की जोरदार वकालत की। यद्यपि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।
‘हिन्दुस्तानी’ शब्द की व्युत्पत्ति और प्रयोग
‘हिन्दुस्तानी’ शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। प्रारम्भिक धारणा यह थी कि यह अंग्रेज़ी प्रभाव से प्रचलित हुआ, किन्तु शोध से स्पष्ट होता है कि इसका प्रयोग यूरोपीय उपस्थिति से पूर्व ही भारत में होने लगा था। शाहजहाँ (1627–1657 ई.) के समय की कृतियों — तारीख़-ए-फ़रिश्ता और बादशाहनामा — में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। इससे भी पहले, संत स्वामी प्राणनाथ (1581–1694 ई.) ने अपनी रचना कुलजम स्वरूप में ‘हिन्दुस्तान’ को भाषा की संज्ञा दी थी।
यद्यपि आरंभिक प्रयोग भारतीय विद्वानों द्वारा हुआ, परन्तु इस शब्द का व्यापक प्रसार यूरोपीय लेखकों और यात्रियों ने किया। डच मिशनरी जे. केटलार (1715 ई.) ने अपने देशवासियों की सुविधा के लिए Hindustani Grammar नामक व्याकरण ग्रंथ तैयार किया। आगे चलकर फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा विभाग के अध्यक्ष गिलक्राइस्ट ने भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख भाषा को ‘हिन्दुस्तानी’ कहा और इस पर अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए।
उर्दू और हिन्दी के साथ सम्बन्ध
अठारहवीं शताब्दी में जब ‘उर्दू’ एक स्वतंत्र भाषा-रूप के रूप में स्थापित हुई, तो हिन्दी और उर्दू के मिश्रित स्वरूप को ‘हिन्दुस्तानी’ कहा जाने लगा। किन्तु उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हिन्दी–उर्दू विवाद तेज़ हो गया। इसके परिणामस्वरूप हिन्दी समर्थकों ने ‘हिन्दी’ शब्द को ही मान्यता देने पर बल दिया। इसी पृष्ठभूमि में नागरी प्रचारिणी सभा (1893) और हिन्दी साहित्य सम्मेलन (1910) की स्थापना हुई।
इसके विपरीत महात्मा गांधी ‘हिन्दुस्तानी’ के समर्थक बने रहे। उनका मानना था कि हिन्दी–उर्दू विवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। वे इसके लिए देवनागरी और फ़ारसी दोनों लिपियों के समानांतर प्रयोग के पक्षधर थे।
अंग्रेज़ी विद्वानों का दृष्टिकोण
गिलक्राइस्ट के समय तक ‘हिन्दुस्तानी’ शब्द अकादमिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर प्रचलित रहा। किन्तु बाद में अंग्रेज़ विद्वानों ने धीरे-धीरे ‘हिन्दी’ अथवा ‘हिन्दवी’ का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उदाहरणस्वरूप, कैप्टन टेलर (1812 ई.) ने फोर्ट विलियम कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘रेख्ता’ (फ़ारसी लिपि में प्रयुक्त भाषा) को अलग रखते हुए हिन्दी का उल्लेख उस भाषा के रूप में किया, जिसकी अपनी लिपि है, जो अरबी–फ़ारसी शब्दावली से मुक्त है और मुसलमान आक्रमण से पहले उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में बोली जाती थी।
हिंदी भाषी राज्य
भारत के कई राज्यों में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी भाषी बहुलता वाले राज्य हैं –
- बिहार
- छत्तीसगढ़
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- झारखंड
- मध्य प्रदेश
- राजस्थान
- उत्तराखंड
- जम्मू और कश्मीर
- उत्तर प्रदेश
- दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
इन राज्यों में हिंदी न केवल सरकारी कार्यों की भाषा है बल्कि आम जनजीवन की भी प्रमुख भाषा है।
हिंदी की लिपि – देवनागरी
हिंदी भाषा की मानक लिपि देवनागरी है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि (phonetic script) है, जिसमें उच्चारण और लेखन में समानता पाई जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ।
देवनागरी लिपि की विशेषताएँ:
- 11 स्वर और 33 व्यंजन
- मात्राओं का प्रयोग
- संयुक्ताक्षर की परंपरा
- लेखन में स्पष्टता और उच्चारण में शुद्धता
हिंदी और इसकी बोलियाँ
हिंदी भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत कई बोलियाँ शामिल हैं। प्रमुख बोलियाँ हैं –
- अवधी
- ब्रजभाषा
- भोजपुरी
- बुंदेली
- बघेली
- हरियाणवी
- राजस्थानी
- खड़ी बोली (आधुनिक मानक हिंदी की आधार बोली)
इन बोलियों की साहित्यिक परंपरा भी समृद्ध रही है। तुलसीदास ने अवधी में “रामचरितमानस” लिखा, जबकि सूरदास ने ब्रजभाषा में “सूरसागर” की रचना की।
भाषा के रूप में ‘हिन्दी’ के विभिन्न अर्थ
इतिहास और भाषावैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ‘हिन्दी’ शब्द का अर्थ समय के साथ बदलता गया। आरम्भ में यह केवल किसी भौगोलिक क्षेत्र को सूचित करता था, बाद में वहाँ की वस्तुओं और निवासियों के लिए प्रयुक्त होने लगा और अंततः एक विशिष्ट भाषा के नाम के रूप में स्थापित हो गया। वर्तमान संदर्भ में भी ‘हिन्दी’ शब्द तीन स्तरों पर समझा जाता है—
1. व्यापक अर्थ
भाषाविद बाबू श्यामसुन्दर दास और डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार व्यापक अर्थ में हिन्दी उन सभी बोलियों की प्रतिनिधि है, जो हिन्दी-प्रदेश में बोली जाती हैं। इसमें कुल 18 बोलियाँ सम्मिलित हैं, जैसे—
- पश्चिमी हिन्दी : खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली, बाँगरू (हरियाणवी)
- पूर्वी हिन्दी : अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
- पहाड़ी भाषाएँ : नेपाली (पूर्वी पहाड़ी), जौनसारी (मध्यवर्ती पहाड़ी)
- राजस्थानी : ढुंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, कठियावाड़ी
- बिहारी : मैथिली, मगही, भोजपुरी
2. सामान्य अर्थ
जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषा वैज्ञानिक हिन्दी का दायरा सीमित मानते हैं। उनके अनुसार केवल पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ ही वास्तविक हिन्दी की श्रेणी में आती हैं। इस दृष्टि से हिन्दी को आठ प्रमुख बोलियों (पश्चिमी की पाँच और पूर्वी की तीन) की प्रतिनिधि भाषा माना जाता है, जिसका उद्गम शौरसेनी और अर्द्धमागधी अपभ्रंश से जुड़ा है।
3. विशिष्ट अर्थ
समसामयिक परिप्रेक्ष्य में ‘हिन्दी’ का तात्पर्य मुख्यतः खड़ी बोली पर आधारित मानक हिन्दी से है। यही रूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120, 210 और 343–351 के अंतर्गत ‘राजभाषा’ के रूप में स्वीकृत है तथा 8वीं अनुसूची में प्रमुख भाषाओं की सूची में भी शामिल है।
आज की परिनिष्ठित हिन्दी लगभग 42 प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है और लगभग 30 प्रतिशत अन्य भारतीयों द्वारा भी समझी और बोली जाती है। इसी कारण यह आधुनिक भारत की सर्वाधिक प्रभावी संपर्क भाषा मानी जाती है।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी
हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के कई देशों में बोली और समझी जाती है।
प्रमुख देश जहाँ हिंदी बोली जाती है:
- नेपाल – यहाँ बड़ी संख्या में हिंदीभाषी लोग हैं।
- फ़िजी – हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
- मॉरिशस – यहाँ प्रवासी भारतीय समुदाय हिंदी का प्रयोग करता है।
- गयाना और सूरीनाम – भारतीय मूल के लोगों के कारण हिंदी यहाँ जीवित है।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) – यहाँ हिंदी व्यापार और प्रवासी भारतीय समुदाय की प्रमुख भाषा है।
फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी गई, जो हिंदी की वैश्विक स्वीकार्यता का बड़ा उदाहरण है।
हिंदी साहित्य और संस्कृति
हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संत साहित्य, भक्ति आंदोलन, रीति काल और आधुनिक काल सभी ने हिंदी को समृद्ध बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का “आधुनिकीकरण” करने का श्रेय दिया जाता है। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय आदि ने हिंदी साहित्य को नई ऊँचाइयाँ दीं।
सिनेमा, संगीत, रंगमंच और पत्रकारिता ने भी हिंदी के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी फिल्मों ने इसे वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई।
हिंदी और प्रौद्योगिकी
आज के डिजिटल युग में हिंदी इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल एप्स की प्रमुख भाषा बन रही है। यूनिकोड और अन्य तकनीकी उपकरणों के कारण हिंदी टाइपिंग सरल हो गई है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और अन्य टेक कंपनियाँ हिंदी आधारित सेवाएँ उपलब्ध करवा रही हैं।
हिंदी के सामने चुनौतियाँ
हालाँकि हिंदी का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं:
- अंग्रेज़ी के अत्यधिक प्रभाव के कारण हिंदी का सीमित प्रयोग।
- क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के बीच संतुलन बनाए रखना।
- तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली में हिंदी का मानकीकरण।
- हिंदी लेखन और पठन की रुचि में कमी।
महत्वपूर्ण तथ्य सारणी (Quick Reference Table)
| भाषा नाम | हिंदी या मानक हिंदी |
|---|---|
| मातृभाषी वक्ता | 61 करोड़ |
| कुल वक्ता | 72 करोड़ |
| लिपि | देवनागरी |
| राजभाषा मान्यता | भारत |
| राष्ट्रभाषा मान्यता | कहीं नहीं |
| भारत में बोली क्षेत्र | बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली |
| विश्व में बोली क्षेत्र | फ़िजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, यूएई |
| नियंत्रक संस्था | केंद्रीय हिंदी निदेशालय |
| भाषा परिवार | भारोपीय भाषा परिवार |
| व्युत्पत्ति | संस्कृत शब्द “सिन्धु” से |
| ISO भाषा कोड | hi, hin |
निष्कर्ष
हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसकी ऐतिहासिक जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं और समय के साथ यह भाषा सामाजिक, साहित्यिक और राजनैतिक क्षेत्रों में निरंतर विकसित होती रही है। हिंदी ने देश में संवाद और समझ का माध्यम बनने के साथ-साथ राष्ट्रीय पहचान को मजबूती प्रदान की है। आज हिंदी न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में बोली और पढ़ी जाती है, जिससे इसका वैश्विक महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि हिंदी भारत के गौरव और सांस्कृतिक धरोहर का अविभाज्य अंग बनी हुई है।
आज आवश्यकता है कि हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे ज्ञान, तकनीक और वैश्विक संवाद की भाषा के रूप में भी विकसित किया जाए। हिंदी भाषा विश्व को जोड़ने और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में निरंतर योगदान देती रहेगी।
इन्हें भी देखें –
- भाषा और लिपि : उद्भव, विकास, अंतर, समानता और उदाहरण
- कबीर दास जी | जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएँ एवं भाषा
- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ
- हिंदी साहित्य का मध्यकाल : भक्ति और रीति धाराओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप
- हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास
- हिंदी के विराम चिन्ह और उनका प्रयोग | 50 + उदाहरण
- भारतीय आर्यभाषाओं का ऐतिहासिक विकास: प्राचीन से आधुनिक काल तक
- भारत की भाषाएँ: संवैधानिक मान्यता, आधिकारिक स्वरूप और विश्व परिप्रेक्ष्य में भाषाई विविधता
- भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य | Folk dances and Classical dances of India
- प्रांतीय नागरिकता (Provincial Citizenship): भारतीय संघीय ढांचे में उभरती नई राजनीतिक वास्तविकता
- पैरासिटामोल और ऑटिज़्म: मिथक, वैज्ञानिक साक्ष्य और वैश्विक बहस