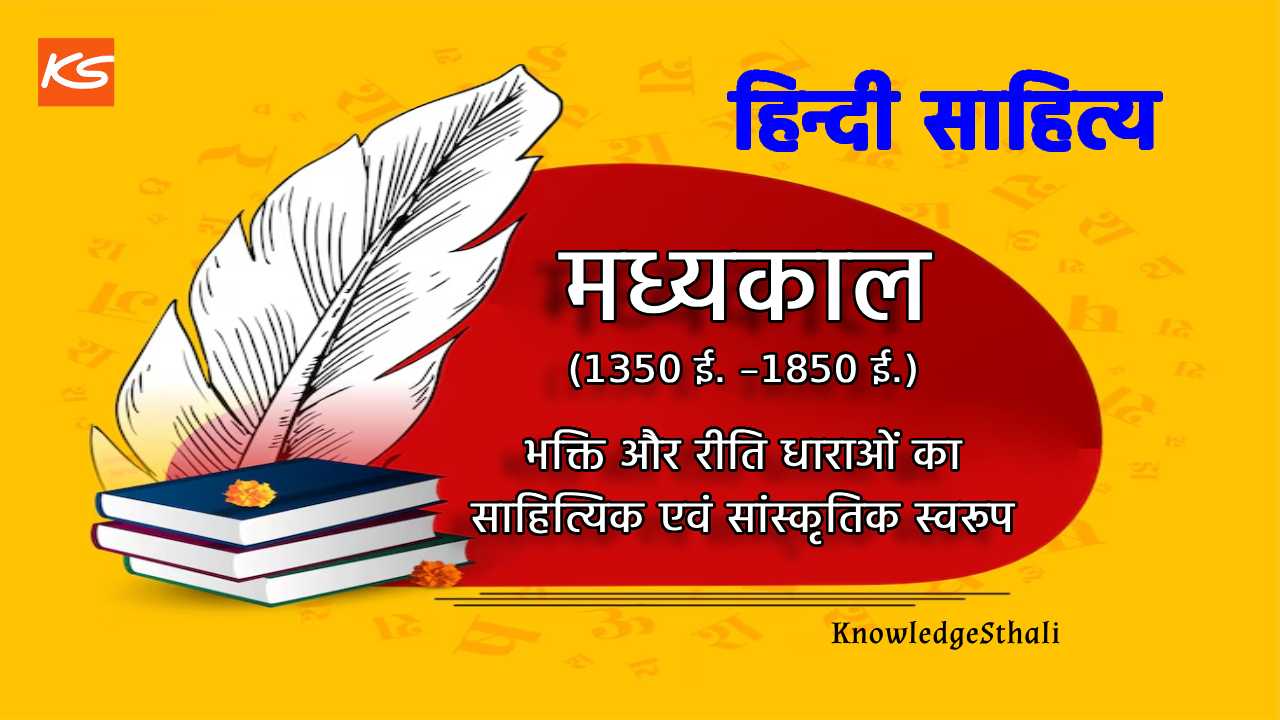हिंदी साहित्य का इतिहास व्यापक और समृद्ध परंपरा का द्योतक है। इसे सामान्यतः तीन प्रमुख कालखंडों में बाँटा गया है—आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिककाल। इन तीनों युगों में साहित्य की प्रवृत्तियाँ, भाषाई स्वरूप और सामाजिक दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न रूप में सामने आते हैं।
इनमें से मध्यकाल का विशेष महत्व है, क्योंकि यही वह दौर था जब हिंदी साहित्य ने अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण किया और जनमानस से गहरा संबंध स्थापित किया। आदिकाल में साहित्य अधिकतर वीरगाथाओं और राजदरबारी परंपराओं तक सीमित था, किंतु मध्यकाल में परिस्थितियाँ बदल गईं। इस युग का साहित्य केवल दरबारी या अभिजात वर्ग की रुचि तक सीमित न रहकर आम जनता की भावनाओं, आस्थाओं और दैनिक जीवन से सीधे-सीधे जुड़ गया।
मध्यकालीन हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें जनभाषाओं—विशेषकर अवधी और ब्रजभाषा—का प्रयोग किया गया, जिससे साहित्य जनसाधारण के लिए अधिक सुलभ, बोधगम्य और लोकप्रिय हो गया। यही कारण है कि इस युग को हिंदी साहित्य का लोकप्रियता का युग कहा जाता है।
हिंदी साहित्य का मध्यकाल लगभग 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक (1350–1850 ई.) माना जाता है। इस काल में भक्ति आंदोलन की धारा ने साहित्य को धर्म, अध्यात्म और भक्ति से जोड़ते हुए सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया और समरसता, समानता तथा प्रेम का संदेश दिया। साथ ही, रीतिकालीन काव्यधारा ने हिंदी को कलात्मकता, अलंकरण और श्रृंगार के नवीन आयाम प्रदान किए। इस प्रकार, मध्यकाल न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ।
हिंदी साहित्य का मध्यकाल
हिंदी साहित्य का मध्यकाल साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और समृद्ध युग माना जाता है। इसका विस्तार लगभग 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी (1350–1850 ई.) तक माना जाता है। इस लंबे कालखंड में हिंदी साहित्य ने अपने वास्तविक स्वरूप को पाया और लोकजीवन से गहरा संबंध स्थापित किया। यही कारण है कि इसे हिंदी साहित्य का लोकप्रियता का युग भी कहा जाता है।
समय-सीमा
मध्यकाल की अवधि लगभग 1350 ई. से 1850 ई. तक मानी जाती है। इस दौरान हिंदी साहित्य ने अनेक धाराएँ और प्रवृत्तियाँ विकसित कीं, जिन्होंने आगे चलकर आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए मजबूत आधार तैयार किया।
प्रमुख धाराएँ
हिंदी साहित्य का मध्यकाल दो मुख्य धाराओं में विभाजित है—
- भक्ति काल (1350–1650 ई.)
- इस धारा में भक्ति आंदोलन की गहरी छाप दिखाई देती है।
- संत कवियों (कबीर, रैदास, दादू) ने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया।
- सगुण भक्त कवियों (तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई) ने राम और कृष्ण की भक्ति को जन-जन तक पहुँचाया।
- अवधी और ब्रजभाषा जैसी बोलियों का साहित्यिक रूप में प्रयोग हुआ।
- रीतिकाल (1650–1850 ई.)
- भक्ति के स्थान पर यहाँ श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता रही।
- दरबारी संस्कृति और काव्यशास्त्र के नियमों से युक्त काव्य रचनाएँ हुईं।
- रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों प्रकार की काव्यधाराएँ विकसित हुईं।
- प्रमुख कवि—केशवदास, बिहारी, मतिराम और घनानंद।
इन दोनों धाराओं ने न केवल हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और धार्मिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला।
समय-सीमा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
हिंदी साहित्य का मध्यकाल लगभग 500 वर्षों तक फैला हुआ है। यह काल भारतीय इतिहास में भी एक संक्रमणकाल था। एक ओर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व था, तो दूसरी ओर भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा समाज में फैल रही थी।
- 14वीं शताब्दी (1350 ई.) से हिंदी में भक्ति साहित्य की लहर शुरू हुई।
- 16वीं शताब्दी तक आते-आते सूर, तुलसी, मीराबाई और कबीर जैसे महान कवियों ने हिंदी साहित्य को जन-जन तक पहुँचा दिया।
- 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब दरबारी संस्कृति का विस्तार हुआ, तब रीति काव्यधारा का विकास हुआ।
- 19वीं शताब्दी (1850 ई.) तक हिंदी साहित्य ने नई राह पकड़ते हुए आधुनिक काल की ओर कदम बढ़ाया।
इस प्रकार, ऐतिहासिक दृष्टि से मध्यकाल वह समय था जब साहित्य ने धर्म, दर्शन, प्रेम और सौंदर्य सभी का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया।
मध्यकाल की प्रमुख विशेषताएँ
1. भाषा का विकास
मध्यकाल में हिंदी की बोलियों—अवधी और ब्रजभाषा—का साहित्यिक स्वरूप में प्रयोग हुआ।
- अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ उपयोग तुलसीदास ने किया, जिनकी रामचरितमानस ने अवधी को अमर कर दिया।
- ब्रजभाषा को सूरदास और अन्य रीतिकालीन कवियों ने काव्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया।
इन दोनों भाषाओं ने हिंदी साहित्य को जनभाषा का रूप प्रदान किया।
2. भक्ति आंदोलन
मध्यकालीन साहित्य का सबसे बड़ा योगदान भक्ति आंदोलन है। यह आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत तक फैला। भक्ति काव्य ने जाति-पाँति और ऊँच-नीच की दीवारों को तोड़ा और ईश्वर-प्रेम को सर्वोच्च मूल्य माना।
- निर्गुण भक्ति धारा : कबीर, दादू, रैदास जैसे संत कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की।
- सगुण भक्ति धारा : तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई ने राम और कृष्ण के रूपों की भक्ति का काव्य रचा।
3. सूफी रहस्यवाद
मध्यकालीन साहित्य पर सूफी संतों का गहरा प्रभाव पड़ा। अमीर खुसरो और जायसी जैसे कवियों ने प्रेम और ईश्वर को एक ही सत्ता का रूप माना। इससे हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की भावना प्रबल हुई।
4. रीतिकाल का विकास
भक्ति साहित्य के बाद हिंदी काव्य में रीति काव्यधारा का उदय हुआ। इसमें रस, अलंकार और श्रृंगार की प्रधानता रही।
- रीतिबद्ध काव्य : कवियों ने काव्यशास्त्रीय नियमों के अनुसार काव्य रचना की।
- रीतिमुक्त काव्य : भावनाओं की स्वच्छंद अभिव्यक्ति पर बल दिया गया।
केशवदास, बिहारी, मतिराम और घनानंद इसके प्रमुख कवि थे।
5. स्त्री स्वर की अभिव्यक्ति
मध्यकाल में मीराबाई जैसी कवयित्रियों ने साहित्य में स्त्री की आवाज़ को प्रखरता से रखा। मीरा का काव्य स्त्री के आत्मिक प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है।
6. नैतिकता और नीतिकाव्य
अब्दुर्रहीम ख़ानख़ाना (रहीम) ने नीति, जीवन-मूल्यों और मानवीय संबंधों पर आधारित काव्य लिखा। उनकी दोहे आज भी लोकजीवन में उद्धृत किए जाते हैं।
मध्यकाल की समय-सीमा और प्रमुख धाराएँ
हिंदी साहित्य का मध्यकाल लगभग 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक (1350–1850 ई.) माना जाता है। इस लंबे कालखंड को दो मुख्य धाराओं में विभाजित किया गया है—
भक्ति काल (1350–1650 ई.) | पूर्व मध्यकाल
परिचय
भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल में धर्म, आस्था और अध्यात्म के विविध रूप सामने आए। भक्ति साहित्य दो धाराओं में विभाजित रहा—निर्गुण और सगुण।
निर्गुण भक्ति धारा
निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना गया। यहाँ मूर्तिपूजा का विरोध करते हुए सीधे ईश्वर से संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया।
- कबीर : समाज में व्याप्त पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया। उनके दोहे आज भी जनमानस को प्रेरित करते हैं।
- दादू : प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया।
- रैदास : जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और समरसता पर बल दिया।
सगुण भक्ति धारा
सगुण धारा में ईश्वर को मूर्त रूप में पूजा गया। इसे दो भागों में बाँटा जाता है—
- राम भक्ति धारा – इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। उनकी रामचरितमानस ने न केवल हिंदी साहित्य को गौरव प्रदान किया, बल्कि लोकजीवन पर अमिट छाप छोड़ी।
- कृष्ण भक्ति धारा – इसके प्रमुख कवि सूरदास हैं, जिनकी सूरसागर कृष्ण-लीलाओं का अनुपम चित्रण करती है। साथ ही मीराबाई की कृष्ण भक्ति कविताएँ स्त्री की आत्मिक पुकार का सशक्त उदाहरण हैं।
रीतिकाल (1650–1850 ई.) | उत्तर मध्यकाल
परिचय
रीतिकाल भक्ति काल के बाद का साहित्यिक युग है, जिसमें भक्ति की जगह श्रृंगार और सौंदर्य ने केंद्र स्थान प्राप्त किया। इस काल को कभी-कभी “अलंकृत काव्य का युग” भी कहा जाता है।
प्रवृत्तियाँ
- श्रृंगार रस की प्रधानता
- नायक-नायिका भेद और अलंकारों का विशद वर्णन
- दरबारी संस्कृति का प्रभाव
- शास्त्रीयता और अलंकरण
प्रमुख कवि और कृतियाँ
- केशवदास – रसिकप्रिया और कविप्रिया जैसी ग्रंथों के रचयिता।
- बिहारी – बिहारी सतसई के लिए प्रसिद्ध, जिसमें संक्षिप्त दोहों में श्रृंगार और नीति का अद्भुत समन्वय है।
- मतिराम – श्रृंगार काव्य के प्रमुख कवि।
- घनानंद – अपनी स्वच्छंद भावनाओं और आत्मीय काव्य के लिए चर्चित।
मध्यकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
- लोकप्रियता : कवियों ने जनभाषाओं (अवधी और ब्रज) का प्रयोग किया, जिससे साहित्य अभिजन की सीमा से निकलकर जनता तक पहुँचा।
- धार्मिकता और भक्ति : ईश्वर प्रेम, आध्यात्मिकता और आस्था साहित्य की मूल प्रवृत्तियाँ थीं।
- सामाजिक समरसता : सूफी और संत कवियों ने हिंदू-मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश दिया।
- नैतिकता और नीति : रहीम और अन्य कवियों ने नीतिपरक दोहों और काव्यों की रचना की।
- स्त्री स्वर की अभिव्यक्ति : मीराबाई ने भक्ति साहित्य में स्त्री दृष्टिकोण को विशेष स्थान दिया।
मध्यकालीन हिंदी साहित्य का महत्व
- सांस्कृतिक महत्व : इस काल ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया।
- भाषाई महत्व : अवधी और ब्रजभाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा मिली, जिसने आधुनिक हिंदी के विकास की नींव रखी।
- सामाजिक महत्व : संत कवियों ने सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों का विरोध करके समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया।
- कलात्मक महत्व : रीतिकालीन साहित्य ने काव्यशास्त्र और अलंकारों के माध्यम से हिंदी काव्य को कलात्मक ऊँचाई दी।
निष्कर्ष
हिंदी साहित्य का मध्यकाल (1350–1850 ई.) न केवल साहित्यिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस काल में भक्ति की अमृतधारा और रीति के श्रृंगारमय स्वर दोनों ने हिंदी को समृद्ध किया। भक्ति काल ने जहाँ ईश्वर प्रेम, भक्ति, लोकसुलभता और समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं रीतिकाल ने काव्य को सौंदर्य और कलात्मकता की ऊँचाई प्रदान की।
अतः मध्यकालीन हिंदी साहित्य भारतीय जीवन की संवेदनाओं, आध्यात्मिकता और सौंदर्यबोध का जीवंत दर्पण है, जिसने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव को मजबूत आधार प्रदान किया।
इन्हें भी देखें –
- कबीर दास जी के दोहे एवं उनका अर्थ | साखी, सबद, रमैनी
- कबीर दास जी | जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएँ एवं भाषा
- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ
- हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास
- भक्ति काल के कवि और उनके काव्य (रचनाएँ)
- प्रकीर्णक (लौकिक) साहित्य: श्रृंगारिकता और लोकसंवेदना का आदिकालीन स्वरूप
- भारतेंदु युग (नवजागरण काल) की समय-सीमा, स्वरूप और युग-निर्धारण की समीक्षा
- भारतीय आर्यभाषाओं का ऐतिहासिक विकास: प्राचीन से आधुनिक काल तक
- द्विवेदी युग (1900–1920 ई.): हिंदी साहित्य का जागरण एवं सुधारकाल
- भाषा और लिपि : उद्भव, विकास, अंतर, समानता और उदाहरण
- भारतीय आर्यभाषाओं का ऐतिहासिक विकास: प्राचीन से आधुनिक काल तक