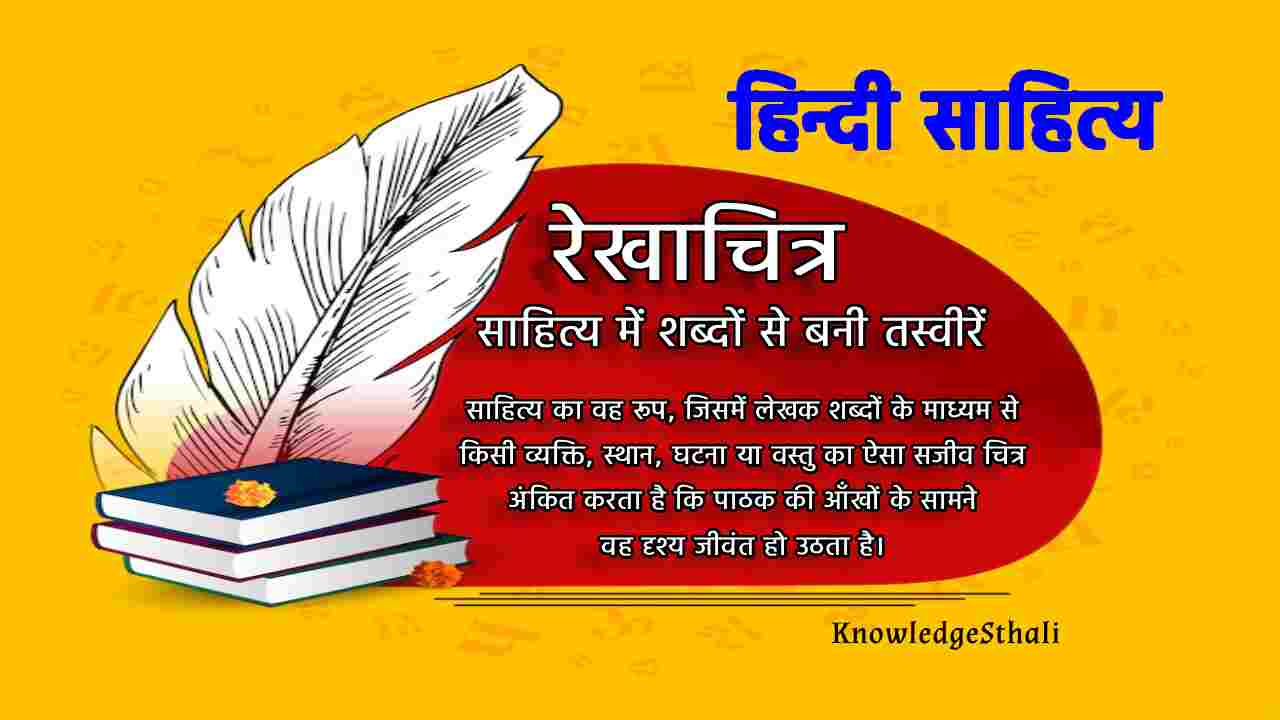साहित्यिक सृजन केवल कथाओं और कविताओं तक सीमित नहीं है। गद्य में भी अनेक ऐसी विधाएँ हैं, जो अपनी विशिष्टता और प्रभावशीलता के कारण पाठकों के हृदय को स्पर्श करती हैं। इन्हीं में से एक है रेखाचित्र — साहित्य का वह रूप, जिसमें लेखक शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या वस्तु का ऐसा सजीव चित्र अंकित करता है कि पाठक की आँखों के सामने वह दृश्य जीवंत हो उठता है।
रेखाचित्र को अंग्रेज़ी के ‘स्केच’ (Sketch) का हिंदी रूप माना जाता है, किंतु इसका साहित्यिक अर्थ और महत्व अंग्रेज़ी ‘स्केच’ से कहीं गहरा और व्यापक है।
रेखाचित्र की परिभाषा और स्वरूप
शब्द ‘रेखाचित्र’ का मूल अर्थ है — रेखाओं से बना हुआ चित्र। चित्रकला में जब कलाकार बिना रंग भरे केवल टेढ़ी-मेढ़ी, सीधी या तिरछी रेखाओं के माध्यम से चित्र बनाता है, तो उसे रेखाचित्र कहा जाता है। यही विचार साहित्य में आया, और जब साहित्यकार शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या दृश्य का हू-ब-हू चित्रण करता है, तो उस रचना को साहित्यिक रेखाचित्र कहते हैं।
इस प्रकार रेखाचित्र को ‘शब्दचित्र’ भी कहा जाता है — जहाँ चित्र में रेखाएँ वही भूमिका निभाती हैं, जो साहित्य में शब्द निभाते हैं।
हिंदी साहित्य कोश के अनुसार:
“रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है।”
अर्थात रेखाचित्र में अलंकारिक विस्तार से अधिक सूक्ष्मता, मार्मिकता और सजीवता का महत्व होता है। यह वर्णन-प्रधान होता है और प्रायः एक ही विषय पर केंद्रित रहता है।
रेखाचित्र की मुख्य विशेषताएँ
रेखाचित्र को अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग पहचान दिलाने वाली कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं—
- सूक्ष्म निरीक्षण — रेखाचित्र में लेखक का गहरा अवलोकन और सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक होती है। वह छोटे-से-छोटे भाव या संकेत को भी पकड़कर शब्दों में ढालता है।
- संक्षिप्तता और सघनता — इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होता। सीमित शब्दों में गहरी बात कही जाती है।
- शब्द-रेखाओं का प्रयोग — जैसे चित्रकार रेखाओं से आकृति बनाता है, वैसे ही लेखक शब्दों से रूपरेखा खींचता है, और रंग भरने का कार्य पाठक की कल्पना पर छोड़ देता है।
- सजीव यथार्थ — इसमें यथार्थ को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन लेखक की कल्पना यथार्थ को और अधिक आकर्षक बनाने में सहायक होती है।
- चित्रात्मकता — रेखाचित्र का उद्देश्य यह है कि पाठक के सामने एक स्पष्ट चित्र उभर आए, मानो वह किसी चित्रकार की कृति देख रहा हो।
- श्रृंखलाबद्धता — वर्णन में क्रमबद्धता बनी रहती है, जिससे चित्र का प्रभाव और गहरा होता है।
रेखाचित्र का इतिहास और विकास
हिंदी साहित्य में रेखाचित्र का इतिहास अपेक्षाकृत नया है।
हिंदी का प्रथम रेखाचित्र ‘पद्म पराग’ माना जाता है, जिसके लेखक पद्म सिंह शर्मा हैं। हालांकि यह संस्मरणात्मक-रेखाचित्र है, परंतु इसे स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है।
रेखाचित्र का व्यवस्थित विकास छायावादोत्तर काल में दिखाई देता है।
1939 में ‘हंस’ पत्रिका (सं. श्रीपति राय) और 1946 में ‘मधुकर’ पत्रिका (सं. बनारसीदास चतुर्वेदी) ने रेखाचित्र पर विशेषांक प्रकाशित करके इसके विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।
प्रमुख रेखाचित्रकार और उनकी कृतियाँ
हिंदी में कई साहित्यकारों ने इस विधा को समृद्ध किया, परंतु दो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं —
- महादेवी वर्मा — अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, मेरा परिवार, पथ के साथी।
- रामवृक्ष बेनीपुरी — माटी की मूरतें, मील का पत्थर।
इसके अतिरिक्त—
- बनारसीदास चतुर्वेदी — सेतुबंध
- श्रीराम शर्मा — प्राणों का सौदा
— भी रेखाचित्र के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों पर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ उन्हें संस्मरण मानते हैं, क्योंकि उनमें वर्णित पात्र और घटनाएँ लेखक के जीवन से जुड़ी प्रतीत होती हैं। परंतु निर्णायक प्रमाण न मिलने के कारण इन्हें प्रायः संस्मरणात्मक शैली में लिखे गए रेखाचित्र माना जाता है।
रेखाचित्र के प्रकार
मुख्यतः रेखाचित्र पाँच प्रकार के होते हैं—
- वर्णनात्मक रेखाचित्र — जिसमें व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सूक्ष्म वर्णन हो।
- संस्मरणात्मक रेखाचित्र — अतीत की स्मृतियों पर आधारित, किंतु चित्रात्मकता प्रधान।
- चरित्र-प्रधान रेखाचित्र — किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर केंद्रित।
- व्यंग्यात्मक रेखाचित्र — व्यंग्य के माध्यम से चित्रण।
- मनोविश्लेषणात्मक रेखाचित्र — पात्र के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का विश्लेषण।
रेखाचित्र के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत
रेखाचित्र की साहित्यिक पहचान को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपनी दृष्टि प्रस्तुत की है—
- जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल —
“गद्य का वह रूप, जिसमें भाषा के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रण या मानसिक प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, रेखाचित्र कहलाता है।” - शशिभूषण सिंघल —
“रेखाचित्र शब्दों के द्वारा निर्मित सांकेतिक चित्र हैं। उसमें प्रस्तुत व्यक्ति की झलक प्रस्तुत की जाती है। लेखक ने उसके विषय में जो धारणा बनाई है, उसका यथासाध्य वस्तुपरक चित्रण करते हुए लेखक स्वतः गौण हो जाता है।” - बनारसीदास चतुर्वेदी —
“साफ चित्रण के लिए रेखाचित्रकार में विश्लेषणात्मक बुद्धि तथा भावुकतापूर्ण हृदय दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। संवेदनशीलता, विवेक और संतुलन इसकी अनिवार्य शर्तें हैं।” - महादेवी वर्मा —
“चित्रकार वस्तु या व्यक्ति का रंगहीन चित्र जब कुछ रेखाओं में इस प्रकार आंक देता है कि उसकी विशेष मुद्रा पहचानी जा सके, तब उसे रेखाचित्र कहते हैं। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर यह है कि संस्मरण में लेखक का व्यक्तिगत संबंध अधिक स्पष्ट होता है, जबकि रेखाचित्र में नहीं।” - मैथिलीशरण गुप्त —
“लोग माटी की मूरतें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूरतें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं।”
रेखाचित्र और संस्मरण : एक तुलना
रेखाचित्र और संस्मरण में कई समानताएँ हैं — दोनों में यथार्थ घटनाओं का चित्रण होता है, दोनों में चित्रात्मकता और श्रृंखलाबद्धता आवश्यक होती है।
लेकिन इन दोनों में कुछ बुनियादी अंतर भी हैं—
| पहलू | रेखाचित्र | संस्मरण |
|---|---|---|
| प्रधानता | विषय-प्रधान | विषयी-प्रधान |
| विषय | विविध — व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना | प्रायः किसी विशेष व्यक्ति या घटना |
| लेखक का संबंध | आवश्यक नहीं | आवश्यक है |
| काल | अतीत, वर्तमान या भविष्य | केवल अतीत |
| तथ्य | कल्पना की छूट | पूर्णतः यथार्थ |
| लेखक का व्यक्तित्व | गौण | स्पष्ट झलक |
| वर्णन शैली | संक्षिप्त, सघन, प्रभावी | विस्तृत, प्रसंगयुक्त, कहानीनुमा |
रेखाचित्र और संस्मरण : समानताएँ एवं अंतर
| पहलू | समानताएँ | रेखाचित्र में अंतर | संस्मरण में अंतर |
|---|---|---|---|
| वर्णन की प्रकृति | दोनों में यथार्थ घटनाओं, व्यक्तियों या दृश्यों का चित्रात्मक वर्णन होता है। | विषय-प्रधान, संक्षिप्त और सघन वर्णन। | विषयी-प्रधान, विस्तृत और प्रसंगयुक्त वर्णन। |
| चित्रात्मकता | दोनों में चित्रात्मकता आवश्यक है — शब्दों से दृश्य पाठक की आँखों के सामने उभर आता है। | शब्द-रेखाओं से चित्र बनाना, रंग भरने की गुंजाइश पाठक की कल्पना को। | तथ्यात्मक चित्रण, कल्पना की छूट नहीं। |
| श्रृंखलाबद्धता | दोनों में घटनाओं या प्रसंगों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। | शब्द-चित्रों की श्रृंखला को व्यवस्थित रूप से रखना। | अतीत की घटनाओं का कालक्रम और प्रसंगानुसार क्रम। |
| लेखक का संबंध | दोनों में लेखक अपने अनुभव या अवलोकन से प्रेरित होकर लिख सकता है। | लेखक का वर्णित विषय से व्यक्तिगत संबंध आवश्यक नहीं। | लेखक का वर्णित विषय से व्यक्तिगत संबंध अनिवार्य। |
| काल | दोनों में बीते हुए समय का चित्रण संभव है। | अतीत, वर्तमान और भविष्य — सभी काल का चित्रण संभव। | केवल अतीत की घटनाओं का चित्रण। |
| तथ्य एवं कल्पना | दोनों में तथ्यात्मक आधार रहता है। | तथ्य के साथ कल्पना की स्वतंत्रता। | केवल वास्तविक तथ्यों का वर्णन, कल्पना की अनुमति नहीं। |
| लेखक का व्यक्तित्व | दोनों में लेखक की संवेदनशीलता और दृष्टि झलकती है। | लेखक का व्यक्तित्व गौण, विषय पर अधिक ध्यान। | लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख, निजी विचार और भाव झलकते हैं। |
| विषय का स्वरूप | दोनों में व्यक्ति, घटना, दृश्य आदि का चित्रण हो सकता है। | विषय विविध — व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना आदि। | सामान्यतः किसी विशेष व्यक्ति या घटना पर केंद्रित। |
संक्षेप में, संस्मरण आत्मपरक होता है, जबकि रेखाचित्र वस्तुपरकता की ओर झुकाव रखता है।
रेखाचित्र की साहित्यिक महत्ता
रेखाचित्र हिंदी साहित्य में एक ऐसी विधा है, जो चित्रकला और साहित्य का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है। यह पाठक के मन में गहरी छाप छोड़ने की क्षमता रखती है।
जहाँ कहानी या उपन्यास के लिए घटनाओं का विस्तार और कथानक आवश्यक होता है, वहीं रेखाचित्र में केवल शब्दों के सहारे क्षणचित्र (Snapshot) जैसा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है।
महादेवी वर्मा और बेनीपुरी जैसे रचनाकारों ने रेखाचित्र के माध्यम से न केवल अपने समय और समाज के चरित्र प्रस्तुत किए, बल्कि मानव स्वभाव, संवेदनशीलता और सामाजिक परिवेश की गहरी झलक भी दी।
महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र : उदाहरण और विश्लेषण
1. महादेवी वर्मा के रेखाचित्र
महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में ‘आधुनिक मीरा’ और ‘रेखाचित्रों की रानी’ कहा जाता है। उनके रेखाचित्रों में करुणा, संवेदनशीलता, और सूक्ष्म अवलोकन की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है।
उनकी प्रमुख रेखाचित्र-आधारित कृतियाँ हैं —
- अतीत के चलचित्र
- स्मृति की रेखाएँ
- मेरा परिवार
- पथ के साथी
(क) “गिल्लू” (मेरा परिवार से)
इस रेखाचित्र में महादेवी ने एक गिलहरी के साथ अपने संबंध का चित्रण किया है।
- चित्रात्मकता — गिल्लू की छोटी-सी आकृति, उसकी चमकती आँखें और शरारती हरकतें इतनी स्पष्ट रूप से वर्णित हैं कि पाठक के सामने वह सजीव हो उठती है।
- भावनात्मक पक्ष — महादेवी ने गिल्लू को केवल एक पशु के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह प्रस्तुत किया है। इसमें उनकी ‘परदुःखकातरता’ स्पष्ट झलकती है।
- विशेषता — यथार्थ और कल्पना का अद्भुत मेल। गिल्लू के व्यवहार को मानवीय संवेदनाओं से जोड़ना पाठक को भावुक कर देता है।
(ख) “नीलकंठ”
- प्रकृति चित्रण — नीलकंठ पक्षी के रंग, उड़ान और स्वभाव का बारीक वर्णन।
- प्रतीकात्मकता — नीलकंठ को स्वतंत्रता, सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक माना गया है।
- रेखाचित्र की खूबी — इसमें दृश्य इतना जीवंत है कि पाठक मानो अपने सामने पक्षी को उड़ते देख रहा हो।
(ग) “सन्नाटा”
- इसमें महादेवी ने एकांत और मौन के अनुभव को स्थान और वातावरण के चित्रण के माध्यम से व्यक्त किया है।
- विशेष गुण — रेखाचित्र यहाँ केवल व्यक्ति या पशु पर नहीं, बल्कि अवस्था पर केंद्रित है, जो इसकी विविधता दर्शाता है।
निष्कर्ष (महादेवी वर्मा पर) — उनके रेखाचित्रों में स्मृतिचित्र और संस्मरण का मिश्रण है, लेकिन तटस्थता और संक्षिप्तता उन्हें रेखाचित्र के और करीब लाती है। प्रकृति, पशु-पक्षी और मानव के बीच भावनात्मक सेतु स्थापित करने में उनकी कला अद्वितीय है।
2. रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र
रामवृक्ष बेनीपुरी को बनारसीदास चतुर्वेदी ने हिंदी का श्रेष्ठ रेखाचित्रकार माना है। उनके रेखाचित्र जीवन के ठोस यथार्थ, ग्रामीण परिवेश और लोक-संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं।
उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं —
- माटी की मूरतें
- मील का पत्थर
(क) “माटी की मूरतें”
- विषय — ग्रामीण जीवन के साधारण लोगों के चरित्र-चित्रण।
- चित्रात्मकता — गाँव के बुजुर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएँ — सभी के हावभाव, पहनावा और बोलचाल का सजीव चित्र।
- विशेष गुण — पात्रों की सादगी और संघर्ष को लेखक ने संवेदनशील दृष्टि से पकड़ा है। उनकी मूरतें माटी की हैं, लेकिन उनमें जीवन की गर्माहट है।
(ख) “मील का पत्थर”
- विषय — लेखक के जीवन में घटित विशेष घटनाएँ और उनसे जुड़े व्यक्तित्व।
- शैली — वर्णन में आत्मीयता, लेकिन रेखाचित्र की संक्षिप्तता बनी रहती है।
- विशेषता — घटनाओं का चयन इस तरह किया गया है कि वे किसी युग या समाज के व्यापक चित्र का हिस्सा बन जाते हैं।
(ग) अन्य रेखाचित्र
बेनीपुरी के रेखाचित्रों में राजनीतिक चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृतियाँ, और ग्रामीण भारत का जीवंत चित्रण मिलता है। वे यथार्थ को बिना अलंकरण के, परंतु हृदयस्पर्शी तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
निष्कर्ष (बेनीपुरी पर) — उनके रेखाचित्रों में विषय की विविधता, भाषा की सादगी और मार्मिक यथार्थ चित्रण प्रमुख है। वे पात्रों को महिमामंडित नहीं करते, बल्कि उन्हें उनके वास्तविक रूप में सामने लाते हैं।
समानताएँ और भिन्नताएँ (महादेवी वर्मा बनाम बेनीपुरी)
| पहलू | महादेवी वर्मा | रामवृक्ष बेनीपुरी |
|---|---|---|
| मुख्य विषय | प्रकृति, पशु-पक्षी, भावनात्मक संबंध | ग्रामीण जीवन, लोक-संस्कृति, संघर्ष |
| शैली | काव्यात्मक, मार्मिक, कोमल संवेदना | यथार्थवादी, सादगी, प्रत्यक्ष चित्रण |
| चित्रात्मकता | सूक्ष्म, रंगीन और भावप्रधान | ठोस, स्पष्ट और वास्तविक |
| दृष्टिकोण | भावुकता और प्रतीकात्मकता | यथार्थ और सामाजिक दृष्टि |
महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भावनाओं के रंगों से सजे चित्र हैं, जो पाठक के मन में कोमलता और करुणा का संचार करते हैं। वहीं रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र जीवन के कठोर यथार्थ के दस्तावेज़ हैं, जो समाज, राजनीति और संस्कृति की तस्वीर उकेरते हैं।
दोनों की विधा-निपुणता यह सिद्ध करती है कि रेखाचित्र केवल दृश्य वर्णन नहीं, बल्कि लेखक के अनुभव, दृष्टि और संवेदनशीलता का अद्वितीय संगम है।
निष्कर्ष
रेखाचित्र हिंदी साहित्य में एक सशक्त गद्य-विधा है, जो अपने संक्षिप्त, सजीव और मार्मिक चित्रण के कारण पाठकों को बांधे रखती है। इसमें चित्रकार की तरह सूक्ष्म दृष्टि और संवेदनशील हृदय की आवश्यकता होती है।
यथार्थ और कल्पना के संतुलित प्रयोग से रेखाचित्रकार पाठक के सामने ऐसा दृश्य उपस्थित कर देता है, जिसे वह लंबे समय तक भूल नहीं पाता।
आज भी रेखाचित्र पत्रकारिता, यात्रा-वृत्तांत, संस्मरण और ललित निबंध जैसी विधाओं के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से भी साहित्य में अपनी पहचान बनाए हुए है।
इन्हें भी देखें –
- पद्म सिंह शर्मा कृत ‘पद्म-पराग’ : रेखाचित्र अथवा संस्मरण?
- रेखाचित्र – अर्थ, तत्व, विकास, प्रमुख रेखाचित्रकार और उदाहरण
- संस्मरण और संस्मरणकार : प्रमुख लेखक और रचनाएँ
- संस्मरण – अर्थ, परिभाषा, विकास, विशेषताएँ एवं हिंदी साहित्य में योगदान
- हिन्दी की जीवनी और जीवनीकार : जीवनी लेखक और रचनाएँ
- सगुण भक्ति काव्य धारा: अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और साहित्यिक विशेषताएँ
- अष्टछाप के कवि: परिचय, रचनाएँ और ऐतिहासिक महत्व
- नाथ संप्रदाय (साहित्य): योग, तंत्र और साधना की भारतीय परंपरा का अनूठा अध्याय
- चारणी साहित्य (रासो साहित्य): वीरगाथात्मक परंपरा का अद्भुत विरासत
- हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि और काव्य (रचनाएँ)
- प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता: छायावादोत्तर युग के अंग या स्वतंत्र साहित्यिक प्रवृत्तियाँ?
- द्विवेदी युग (1900–1920 ई.): हिंदी साहित्य का जागरण एवं सुधारकाल