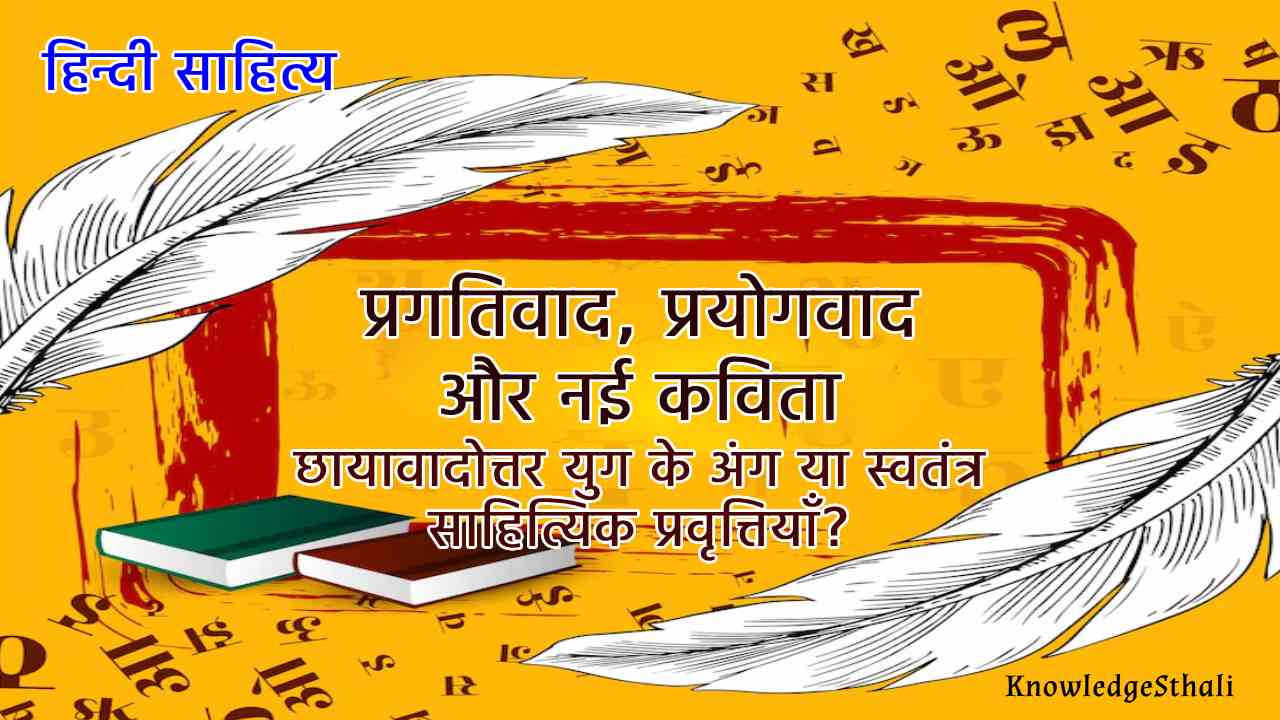हिंदी साहित्य का इतिहास केवल घटनाओं या धाराओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर चल रही वैचारिक उथल-पुथल, सांस्कृतिक जागरण और मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्व का लेखा-जोखा भी है। छायावाद यद्यपि हिंदी कविता का स्वर्णकाल रहा, परंतु उसकी भावुकता, रहस्यवाद और व्यक्तिगत संवेदनशीलता धीरे-धीरे बदलते यथार्थ से टकराने लगी। 1936 के बाद का युग, जिसे छायावादोत्तर युग कहा जाता है, इसी टकराव का परिणाम था।
यह समय एक संक्रमणकाल था जिसमें हिंदी कविता छायावादी कोमलता से निकलकर सामाजिक यथार्थ, वर्गसंघर्ष, वैयक्तिक द्वंद्व और अस्तित्व की विडंबनाओं की ओर बढ़ी। इसी वैचारिक भूमि पर हिंदी कविता के तीन प्रमुख आंदोलन– प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता – विकसित हुए।
यहाँ प्रश्न यह उठता है कि –
क्या ये तीनों प्रवृत्तियाँ छायावादोत्तर युग के अंग हैं, या अपने विषय, शिल्प और दृष्टिकोण के आधार पर स्वतंत्र साहित्यिक युग मानी जाएँ?
इस लेख में हम इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए एक गहन आलोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करेंगे।
छायावादोत्तर युग – संक्रण की साहित्यिक भूमि (1936–1947)
छायावादोत्तर युग को केवल “छायावाद के बाद” का युग नहीं माना जा सकता। यह युग राष्ट्रीय आंदोलन, समाजवादी चेतना, औपनिवेशिक असंतोष, सामंतवाद विरोध और सांस्कृतिक अस्थिरता से ओत-प्रोत था। इस समय लेखकों और कवियों ने रहस्यवाद और प्रेम की भावुक अभिव्यक्ति से ऊपर उठकर समाज की पीड़ाओं, असमानताओं, राजनीतिक उथल-पुथल और आत्मसंघर्ष की ओर रुख किया।
प्रमुख विशेषताएँ:
- सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण
- राष्ट्रीय चेतना और जनजागरण
- काव्य-शैली में परिवर्तन की शुरुआत
- नए विषयों और दृष्टिकोण की खोज
प्रमुख कवि:
माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंशराय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत (उत्तर छायावादी काल में)
छायावादोत्तर युग में कविता न तो पूरी तरह सामाजिक हो पाई थी, न पूरी तरह वैयक्तिक। यह वह भूमि थी जहाँ कविता नए मार्गों की तलाश कर रही थी, और यही तलाश तीन अलग-अलग दिशाओं में विकसित होकर तीन आंदोलन बन गई – प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और नई कविता।
प्रगतिवाद (1936–1943): वर्ग चेतना और सामाजिक परिवर्तन की अभिव्यक्ति
उत्पत्ति:
प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ होती है। इस आंदोलन ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ने, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने और सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाने का संकल्प लिया।
प्रमुख विशेषताएँ:
- मार्क्सवाद से प्रेरणा
- वर्गसंघर्ष, पूँजीवाद-विरोध, किसान-मजदूर जीवन का चित्रण
- नारी, दलित और पिछड़े वर्गों की समस्याओं की अभिव्यक्ति
- यथार्थ को सीधे-सपाट शैली में प्रस्तुत करना
- साहित्य को “क्रांति का औज़ार” मानना
प्रमुख कवि और रचनाएँ:
- नागार्जुन – बलचनमा, रतिनाथ की चाची
- त्रिलोचन – ग्राम जीवन का यथार्थ
- केदारनाथ अग्रवाल – हे मेरी तुम!
- रामविलास शर्मा – साहित्य का समाजशास्त्रात्मक विवेचन
- मुक्तिबोध (प्रारंभिक चरण) – विचारशील क्रांतिकारी चेतना
छायावादोत्तर युग से संबंध:
प्रगतिवाद छायावाद की भावुकता के विपरीत यथार्थ की ठोस ज़मीन पर खड़ा था। माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर जैसे कवियों ने दोनों युगों की सेतु-संरचना में भूमिका निभाई। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद छायावादोत्तर युग की कोख से ही जन्मा, परंतु उसकी वैचारिक परिपक्वता, स्पष्ट उद्देश्य और स्पष्ट सौंदर्यबोध के कारण इसे एक स्वतंत्र साहित्यिक प्रवृत्ति माना जाना चाहिए।
प्रयोगवाद (1943–1953): आत्मसंघर्ष और शिल्प का नवाचार
उत्पत्ति:
प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित ‘तार सप्तक’ से मानी जाती है। इस आंदोलन ने कविता के शिल्प, भाषा और भावबोध में नवीन प्रयोगों की श्रृंखला प्रारंभ की। इसका केंद्र बिंदु समाज नहीं, व्यक्ति और उसका आत्मिक द्वंद्व था।
प्रमुख विशेषताएँ:
- वैयक्तिकता और आत्मसंघर्ष की प्रधानता
- छंदों की परंपरा से मुक्ति – छंदमुक्त कविता
- प्रतीकों, मिथकों और जटिलता का प्रयोग
- भाषा और शिल्प में नवीनता
- अस्तित्वगत प्रश्नों की आहट
प्रमुख रचनाकार:
- अज्ञेय – अरी ओ करुणा प्रभामय, इत्यलम्
- शमशेर बहादुर सिंह – कुछ कविताएँ, चुका भी नहीं हूँ मैं
- भवानी प्रसाद मिश्र – जीवन और भाषा का सरल प्रयोग
- रघुवीर सहाय (प्रारंभिक चरण) – आत्मबोध
छायावादोत्तर युग से संबंध:
छायावादोत्तर युग ने कवियों को आंतरिक और सामाजिक असंतोष से जोड़ने का कार्य किया, जिससे व्यक्ति और समाज के बीच नया संवाद प्रारंभ हुआ। प्रयोगवाद इसी संवाद का आंतरिक रूप था, परंतु इसकी दृष्टि छायावादी कल्पनाओं और प्रगतिवादी यथार्थ से अलग, पूरी तरह स्वानुभूति और आत्मसंघर्ष की ओर उन्मुख थी।
अतः प्रयोगवाद को छायावादोत्तर की जमीन पर अंकुरित हुआ आंदोलन अवश्य कहा जा सकता है, लेकिन यह अपनी सौंदर्य दृष्टि और रचनात्मक उपकरणों के कारण पूर्णतः स्वतंत्र प्रवृत्ति है।
नई कविता (1951 से आगे): आधुनिकता, विडंबना और अस्तित्व की जटिलता
उत्पत्ति:
नई कविता आंदोलन का सूत्रपात 1950 के दशक के प्रारंभ में होता है, जो प्रयोगवाद से ही विकसित होता है लेकिन उससे कहीं अधिक गहराई और व्यापकता लिए होता है। यह कविता शहरीकरण, आधुनिक जीवन के तनाव, आत्मिक अकेलापन और अस्तित्व की निरर्थकता जैसे मुद्दों से जूझती है।
प्रमुख विशेषताएँ:
- शहरी जीवन की विडंबनाएँ और अकेलापन
- दार्शनिक और अस्तित्ववादी दृष्टिकोण
- जीवन की क्षणभंगुरता और निरर्थकता का चित्रण
- प्रतीकों और सूक्ष्म संवेदनाओं का उपयोग
- वैयक्तिक अनुभूति का गहन विश्लेषण
प्रमुख कवि:
- अज्ञेय (उत्तरकालीन) – आँगन के पार द्वार
- धर्मवीर भारती – कनुप्रिया, सपनों के से दिन
- केदारनाथ सिंह – जमीन पक रही है
- सर्वेश्वरदयाल सक्सेना – ख़ूब लड़ी मर्दानी, अगला युद्ध
- रघुवीर सहाय – हँसो हँसो जल्दी हँसो (बाद के वर्षों में विडंबनात्मक यथार्थ)
छायावादोत्तर युग से संबंध:
नई कविता का बीज उसी समय बोया गया जब कविता में समाज और व्यक्ति दोनों की अस्मिता के प्रश्न उठने लगे थे – यानी छायावादोत्तर युग। परंतु नई कविता के अंतर्विषय, शैली और भाषा छायावादोत्तर से अलग थे – इसमें दर्शन, मनोविश्लेषण, शहरी कुंठा और अर्थहीनता जैसे बिंदु केंद्र में थे।
अतः नई कविता को भी छायावादोत्तर से प्रेरित होने के बावजूद एक स्वतंत्र साहित्यिक युग कहना अधिक उपयुक्त है।
तुलनात्मक तालिका:
| प्रवृत्ति | समय | विषयवस्तु | सौंदर्यशास्त्र | छायावादोत्तर से संबंध | स्वतंत्रता का आधार |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रगतिवाद | 1936–1943 | वर्गसंघर्ष, सामाजिक यथार्थ | यथार्थवाद, सरल शैली | छायावादोत्तर की सामाजिक चेतना से विकसित | उद्देश्य, विषय और वैचारिक स्वतंत्रता |
| प्रयोगवाद | 1943–1953 | आत्मसंघर्ष, शिल्प प्रयोग | प्रतीकात्मकता, छंदमुक्त कविता | वैयक्तिक यथार्थ की जड़ों में छायावादोत्तर की भूमिका | शैली और दृष्टिकोण की नवीनता |
| नई कविता | 1951–1970 | अस्तित्व, अकेलापन, आधुनिक विडंबना | दार्शनिकता, गहन आत्मचिंतन | छायावादोत्तर युग की मनोभूमि पर उत्पत्ति | दर्शन, भाषा और अंतर्विषय की गहराई |
- छायावादोत्तर युग ने हिंदी कविता को नई वैचारिक ज़मीन दी।
- प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ और परिवर्तन की कविता है।
- प्रयोगवाद आत्मसंघर्ष और शिल्प प्रयोग की दिशा में अग्रसर रहा।
- नई कविता आधुनिक मनुष्य के अस्तित्व और अकेलेपन की अभिव्यक्ति है।
- तीनों प्रवृत्तियाँ छायावादोत्तर युग से प्रेरित होकर भी अपनी दृष्टि से स्वतंत्र साहित्यिक आंदोलन हैं।
निष्कर्ष
छायावादोत्तर युग को “सांस्कृतिक संक्रमण और वैचारिक परिवर्तन” का युग कहा जा सकता है, जिसने हिंदी साहित्य को भावुक कल्पना से निकालकर सामाजिक यथार्थ और आत्मबोध की नई दिशाओं की ओर अग्रसर किया। इस युग में जो विचारधारात्मक भूमि तैयार हुई, उसी पर आगे चलकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बीज अंकुरित हुए।
हालाँकि इन तीनों प्रवृत्तियों की वैचारिक जड़ें छायावादोत्तर युग में मौजूद हैं, फिर भी ये तीनों कालखंड, अपने विषय, उद्देश्य, शिल्प और सौंदर्यशास्त्र में इतनी भिन्न हैं कि उन्हें स्वतंत्र साहित्यिक युग कहा जाना ही उचित होगा।
इसलिए हम निस्संकोच कह सकते हैं:
“प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता – छायावादोत्तर युग से उत्पन्न तो अवश्य हैं, परंतु परंतु हिंदी कविता की तीन अलग-अलग शाखाएँ हैं और हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान और सौंदर्यशास्त्र के कारण स्वतंत्र साहित्यिक युग हैं।”
इन्हें भी देखें –
- रीतिकाल (1650 ई. – 1850 ई.): हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकालीन युग
- हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और उसका ऐतिहासिक विकास | 1850 ई. से वर्तमान तक
- बूढ़ी काकी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- भाड़े का टट्टू | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- मृत्यु के पीछे | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- मनोवृत्ति | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- पूस की रात | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- तालिस्मन सेबर (Talisman Sabre) 2025: बहुराष्ट्रीय रक्षा सहयोग का प्रतीक
- जरवा जनजाति: अंडमान की विलक्षण आदिवासी पहचान और संरक्षण की चुनौती
- बराक घाटी: पूर्वोत्तर भारत की उपेक्षित जीवनरेखा
- गुप्त साम्राज्य
- सम्राट हर्षवर्धन (590-647 ई.)