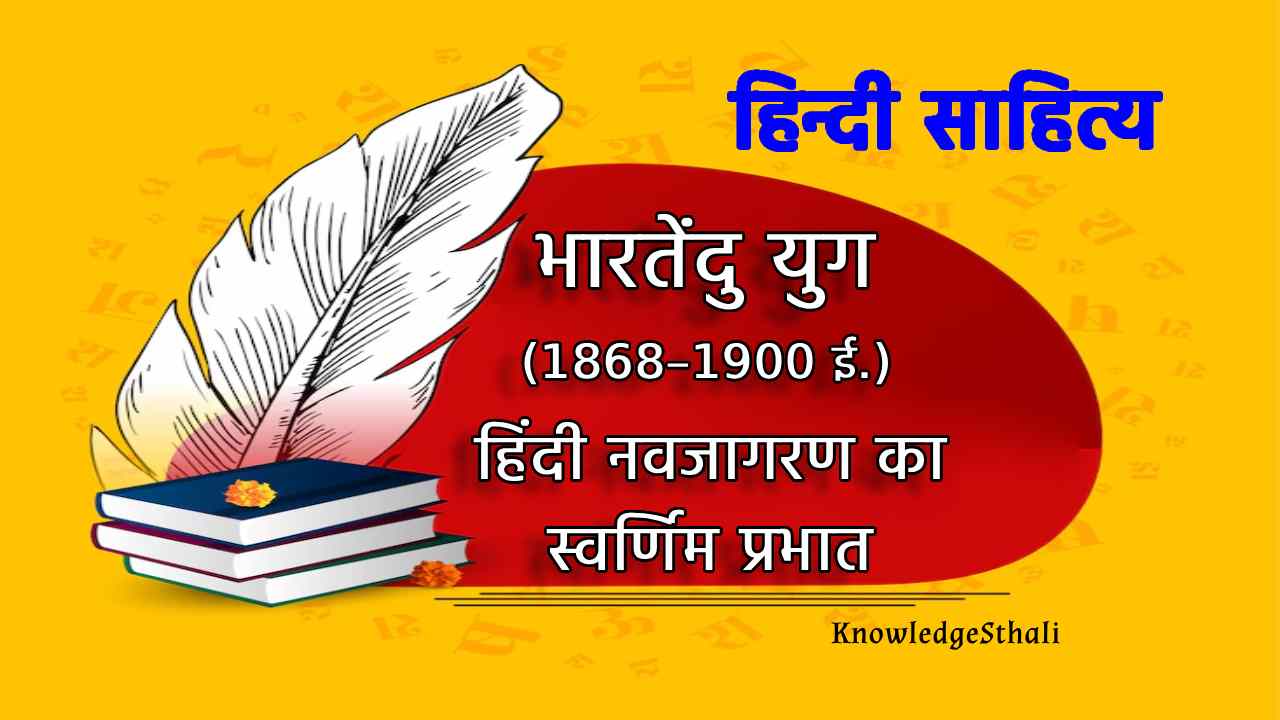हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अपने भीतर कई युगों को समाहित करता है, जिनमें “भारतेंदु युग” एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह युग हिंदी नवजागरण का प्रारंभिक चरण माना जाता है और इसका नामकरण इस युग के अग्रदूत, हिंदी के महान कवि, नाटककार, पत्रकार और समाजसेवी भारतेन्दु हरिश्चंद्र (1850–1885 ई.) के नाम पर किया गया है।
इस युग की प्रमुख विशेषताओं में सामाजिक चेतना, राष्ट्रवाद, भाषा प्रेम, भक्ति और शृंगार की भावना, रीतिकाल की आलोचना और नवीन विचारों का प्रचार प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युग केवल एक साहित्यिक युग नहीं, बल्कि वह एक वैचारिक आंदोलन था, जिसने हिंदी साहित्य को नए धरातल पर स्थापित किया।
भारतेन्दु युग (1868–1900 ई.)
हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चन्द्र (1850–1885 ई.) से माना जाता है। उनका काल (1868–1900 ई.) “भारतेन्दु युग” के नाम से विख्यात है। इस युग का नामकरण “भारतेंदु युग” इस युग के प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ, जिन्होंने न केवल साहित्य की रचना की बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक चेतना को भी साहित्य का हिस्सा बनाया। यह युग केवल साहित्यिक जागरण का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और भाषाई चेतना का उदयकाल भी था। इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि हिंदी साहित्य में विषय-वस्तु और अभिव्यक्ति की दृष्टि से नये प्रयोग प्रारंभ हुए। इसी कालखंड में भारतीय समाज की आत्मचेतना जागृत हुई और साहित्यकारों ने समाज को दिशा देने का कार्य करना आरंभ किया।
भारतेंदु युग (1868–1900 ई.) वह कालखंड है, जब हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को अपनाने की शुरुआत हुई और साहित्य की विषयवस्तु में भी व्यापक परिवर्तन आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को केवल साहित्यिक भाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा बनाने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने पत्रकारिता, नाटक, कविता, निबंध, आलोचना आदि विधाओं में साहित्य रच कर आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी।
भारतेन्दु युग का नामकरण और समयावधि
“भारतेन्दु युग” का नामकरण हिंदी साहित्य के महान अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। भारतेंदु का जीवनकाल 1850 से 1885 तक रहा, और इसी अवधि में उन्होंने हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की। उनके जीवन के पश्चात भी उनके विचारों और साहित्यिक चेतना से प्रेरित रचनाकारों ने साहित्य की गरिमा बढ़ाई। 1868 ई. में भारतेंदु जी की प्रमुख साहित्यिक सक्रियता के कारण 1868 से 1900 तक के काल को “भारतेंदु युग” के रूप में स्वीकार किया गया है।
भारतेंदु युग (नवजागरण काल) – समय-सीमा और स्वरूप
👉 समय-सीमा: 1868 ई. से 1900 ई.
युग-निर्धारण का आधार:
- भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवनकाल 1850 ई. से 1885 ई. तक रहा। इसी अवधि में उन्होंने हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की।
- भारतेंदु हरिश्चंद्र ने न केवल साहित्य की लगभग सभी विधाओं में रचना की, बल्कि हिंदी भाषा को आधुनिक चेतना से जोड़ने का कार्य भी किया।
- उनके निधन (1885) के पश्चात भी उनके विचारों और साहित्यिक चेतना से प्रेरित रचनाकारों – जैसे प्रतापनारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, प्रेमघन, जगमोहन सिंह आदि ने साहित्य की गरिमा को निरंतर ऊँचाइयों तक पहुँचाया।
- 1900 ई. तक आते-आते भारतेंदु के प्रमुख समकालीन साहित्यकारों – अंबिकादत्त व्यास, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी ‘प्रेमघन’, आदि की मृत्यु हो गई थी, जिससे इस युग का अवसान माना जाता है।
- इस प्रकार उनके जन्म वर्ष 1850 से 1900 तक का काल एक साहित्यिक नवजागरण का युग माना गया, जिसे इतिहास में “भारतेंदु युग” के रूप में स्वीकृति मिली।
- कुछ विद्वान 1902 ई. तक की सीमा मानते हैं, क्योंकि इस समय तक भारतेंदु परंपरा का प्रभाव स्पष्ट रूप से सक्रिय था।
- अधिकांश विद्वान (राम विलास शर्मा आदि) 1868 ई. से 1900 या 1902 ई. तक की समयसीमा मानते हैं, क्योंकि 1868 ई. में भारतेंदु जी की प्रमुख साहित्यिक सक्रियता शुरू हुई थी, अतः व्यापक दृष्टि से 1868 से 1900 ई. तक की अवधि को ही भारतेंदु युग की संपूर्ण कालावधि माना जाता है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक प्रतिभा का प्रारंभ और युग की समय-सीमा से संबंधित तथ्य
भारतेंदु हरिश्चंद्र बाल्यकाल से ही अद्भुत काव्य-प्रतिभा के धनी थे। मात्र पांच वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने यह प्रसिद्ध दोहा रचकर अपने पिता को सुनाया:
लै ब्योढ़ा ठाढ़े भए श्री अनिरुद्ध सुजान।
बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान॥
यह दोहा न केवल उनकी प्रारंभिक प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि यह बताता है कि भारतेंदु में बाल्यकाल से ही पौराणिक विषयों की समझ और रचनात्मक क्षमता थी।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आगे चलकर हिंदी साहित्य को जिस व्यापकता और नवीनता के साथ समृद्ध किया, उसी के फलस्वरूप कुछ विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में 1857 से 1900 तक की कालावधि को “भारतेंदु युग” कहा गया।
इस युग की शुरुआत को लेकर इन विद्वानों का मत है कि:
चूँकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक प्रभाव 1850 के दशक से ही दिखने लगता है परन्तु 1857 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना के जागरण का भी वर्ष था, अतः कई स्थलों पर 1857 ई. को भारतेंदु युग की औपचारिक शुरुआत का वर्ष भी माना जाता है।
इस प्रकार, बाल्यकाल से ही साहित्यिक रचनाशीलता में प्रवृत्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने वृहत साहित्यिक योगदान और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लेखन के कारण भारतेंदु युग को परिभाषित किया।
निष्कर्ष:
👉 भारतेंदु युग की सामान्य और प्रतीकात्मक समय-सीमा: 1850 ई. से 1900 ई.
👉 भारतेंदु युग की सर्वाधिक यथार्थवादी और स्वीकृत समय-सीमा: 1868 ई. से 1900 ई.
👉 इसे हिंदी साहित्य में नवजागरण काल या आधुनिक युग का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र: युगपुरुष और दिशा निर्देशक
भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पहले जागरूक, समर्पित और सामाजिक सरोकारों से जुड़े साहित्यकार थे। उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में साहित्य रचा, नाटक लिखे, पत्रिकाएं निकालीं और अपने विचारों से जनचेतना को जगाया। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं –
- प्रेम मालिका
- प्रेम सरोवर
- गीत गोविन्दानन्द
- वर्षा विनोद
- विनय प्रेम पचासा
- प्रेम फुलवारी
- वेणु गीति
- दशरथ विलाप
- फूलों का गुच्छा (खड़ी बोली में)
साथ ही उन्होंने ‘हरिश्चन्द्र मैगज़ीन’, ‘हरिश्चंद्र पत्रिका’ और ‘कविवचन सुधा’ जैसी पत्रिकाओं का संपादन कर हिंदी पत्रकारिता को भी समृद्ध किया।
भारतेन्दु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ न केवल साहित्य के अंत:सत्व को बदलने वाली थीं, बल्कि उन्होंने एक नया मार्ग प्रशस्त किया। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं:
- नवजागरण की चेतना – भारतेंदु युग नवजागरण का काल था। समाज, राजनीति, धर्म, भाषा और संस्कृति सभी क्षेत्रों में जागृति का संचार हुआ।
- सामाजिक चेतना का विकास – भारतेंदु युग के कवियों ने समाज की कुरीतियों, शोषण, अंधविश्वासों और अंग्रेजी शासन की विडंबनाओं को उजागर किया।
- भक्ति भावना का पुनर्प्रकाशन – यद्यपि भक्ति आंदोलन का चरम बीत चुका था, परंतु इसकी भावना अब भी रचनाओं में प्रतिबिंबित होती थी।
- श्रृंगारिकता और सौंदर्यबोध – भारतेंदु युगीन काव्य में श्रृंगार रस का समावेश मिला लेकिन वह रीतिकालीन अतिरेक से मुक्त होकर अधिक सामाजिक और सौम्य हो गया।
- रीति निरूपण की परंपरा – यद्यपि इस युग में रीतिबद्धता में कमी आई, परंतु काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अलंकार, रस, छंद आदि का उचित उपयोग हुआ।
- समस्या पूर्ति और शास्त्रीय अभ्यास – काव्य रचनाओं में निपुणता के लिए अनेक कवियों ने समस्या पूर्ति, शतक और सतसई जैसी विधाओं का अभ्यास किया।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (1850–1885) का जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्हें हिंदी का आधुनिक युग का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने जिस बहुआयामी कार्यक्षेत्र में लेखनी चलाई, उससे न केवल हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ, बल्कि राष्ट्रवादी चेतना को भी बल मिला।
उन्होंने निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से हिंदी को समृद्ध किया:
- पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान: ‘कविवचन सुधा’, ‘हरिश्चंद्र मैगज़ीन’, ‘हरिश्चंद्र पत्रिका’ जैसी पत्रिकाएं निकालकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की दिशा और दशा बदल दी।
- नाटक लेखन: उनके नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक आलोचना के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
- भाषा सुधार: उन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा बनाया और संस्कृतनिष्ठ हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया।
- राष्ट्रीयता का प्रचार: अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनमानस को जगाने के लिए उन्होंने लेखनी को हथियार बनाया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भावना उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से मिलती है।
नवजागरण काल के रूप में भारतेंदु युग
भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहा जाता है। नवजागरण का अर्थ है – आत्मचेतना का उदय। हिंदी साहित्य में यह युग उस काल का प्रतिनिधित्व करता है जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी विचारधारा और स्वतंत्रता की भावना का प्रवेश हुआ। प्रारंभिक काल (1843–1869) में यह चेतना अस्पष्ट थी, लेकिन 1870 के बाद सामाजिक चेतना तीव्र होने लगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य को इस चेतना का माध्यम बनाया और जनमानस को आत्मसजग किया।
ब्रजभाषा से खड़ी बोली की ओर संक्रमण
भारतेंदु युग से पहले हिंदी साहित्य मुख्यतः ब्रजभाषा में रचा जाता था और उसमें भक्ति व श्रृंगार विषयक रचनाएँ प्रमुख होती थीं। भारतेंदु ने खड़ी बोली को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जिससे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक नई धारा का जन्म हुआ। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठा मिलने लगी, जिससे भविष्य में खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप बन सकी।
भारतेंदु मंडल: एक सृजनशील सांस्कृतिक समूह
भारतेंदु हरिश्चंद्र अकेले नहीं थे। उनके चारों ओर कई रचनाकारों का एक ऐसा उज्ज्वल समूह था, जिन्हें हम “भारतेंदु मंडल” के नाम से जानते हैं। यह मंडल भारतेंदु की विचारधारा से प्रेरित था और इनके माध्यम से हिंदी साहित्य में एक नया युग प्रारंभ हुआ।
यह मंडल साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नयन का प्रतीक बन गया। इसमें सम्मिलित रचनाकारों ने न केवल भारतेंदु से प्रेरणा ली, बल्कि स्वयं भी युगचेतना के वाहक बने। इस मंडल ने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किए।
भारतेंदु मंडल के प्रमुख सदस्य (साहित्यकार):
- भारतेंदु हरिश्चंद्र
- प्रताप नारायण मिश्र
- बदरी नारायण चौधरी ‘प्रेमघन’
- बालकृष्ण भट्ट
- अम्बिका दत्त व्यास
- राधा चरण गोस्वामी
- ठाकुर जगमोहन सिंह
- लाला श्रीनिवास दास
- सुधाकर द्विवेदी
- राधा कृष्ण दास आदि।
इन साहित्यकारों ने कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास आदि विधाओं में रचना कर हिंदी के आधुनिक स्वरूप को दिशा दी।
भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ
भारतेंदु युग में कविता के साथ-साथ नाटक, निबंध, उपन्यास और कहानियों की रचना भी प्रारंभ हुई। इस काल की रचनाओं में जहां विषयों की विविधता है, वहीं भाषा में भी सहजता और प्रवाह देखने को मिलता है।
1. भारतेंदु हरिश्चंद्र
प्रमुख रचनाएँ:
- प्रेम मालिका
- प्रेम सरोवर
- गीत गोविन्दानन्द
- वर्षा विनोद
- विनय प्रेम पचासा
- प्रेम फुलवारी
- वेणु गीति
- दशरथ विलाप
- फूलों का गुच्छा
2. प्रताप नारायण मिश्र
प्रमुख रचनाएँ:
- प्रेम पुष्पावली
- मन की लहर
- लोकोक्ति शतक
- तृप्यन्ताम्
- श्रृंगार विलास
- दंगल खंड
- ब्रेडला स्वागत
3. बदरी नारायण चौधरी ‘प्रेमघन’
प्रमुख रचनाएँ:
- जीर्ण जनपद
- आनन्द अरुणोदय
- हार्दिक हर्षादर्श
- मयंक महिमा
- अलौकिक लीला
- वर्षा बिन्दु
- लालित्य लहरी
- बृजचन्द पंचक
4. अंबिका दत्त व्यास
प्रमुख रचनाएँ:
- पावस पचासा
- सुकवि सतसई
- हो हो होरी
5. जगमोहन सिंह
प्रमुख रचनाएँ:
- प्रेम संपत्ति लता
- श्यामालता
- श्यामा सरोजिनी
- देवयानी
- ऋतु संहार
- मेघदूत
6. राधाकृष्ण दास
प्रमुख रचनाएँ:
- कंस वध (अपूर्ण)
- भारत बारहमासा
- देश दशा
भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की सारणी
इस युग के रचनाकारों ने विविध साहित्यिक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई – कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता आदि। इन रचनाकारों की रचनाएँ न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि उनमें युगीन विचारधारा और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी दृष्टिगत होता है। नीचे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की सारणी के रूप में दिया गया है –
| क्रम | कवि | प्रमुख रचनाएँ |
|---|---|---|
| 1. | भारतेंदु हरिश्चंद्र | प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविन्दानन्द, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा |
| 2. | बदरी नारायण चौधरी ‘प्रेमघन’ | जीर्ण जनपद, आनन्द अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिन्दु, लालित्य लहरी, बृजचन्द पंचक |
| 3. | प्रताप नारायण मिश्र | प्रेमपुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यन्ताम्, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत |
| 4. | ठाकुर जगमोहन सिंह | प्रेमसंपत्ति लता, श्यामालता, श्यामा सरोजिनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत |
| 5. | अम्बिका दत्त व्यास | पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो हो होरी |
| 6. | राधा कृष्ण दास | कंस वध (अपूर्ण), भारत बारहमासा, देश दशा |
इन रचनाकारों की रचनाएँ विभिन्न विधाओं में विभाजित थीं, जिनमें भक्ति, श्रृंगार, हास्य, आलोचना, व्यंग्य, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार आदि विविध विषय शामिल थे।
भारतेंदु युग में साहित्यिक विधाओं का विकास
भारतेंदु युग में केवल कविता ही नहीं, अपितु हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में भी अद्भुत विकास हुआ। नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना और पत्रकारिता को नए आयाम मिले। युगीन साहित्य में विचारों की व्यापकता और भावों की गहराई देखने को मिलती है।
- नाटक – भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में देशप्रेम, सामाजिक कुरीतियों का विरोध और लोकशिक्षा की भावना प्रबल है।
- निबंध – बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जैसे साहित्यकारों ने विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक निबंधों की रचना की।
- पत्रकारिता – ‘हरिश्चंद्र मैगज़ीन’, ‘कविवचन सुधा’ जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्र और समाज को जागरूक किया गया।
गद्य साहित्य की उपलब्धियाँ
भारतेंदु युग में कविता एवं हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के साथ गद्य साहित्य का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। नाटक, निबंध, संवाद, कहानी, यात्रा वृत्तांत आदि विधाएं पनपने लगीं। विशेष रूप से नाटक विधा को भारतेंदु ने मंच और समाज से जोड़कर जनचेतना का माध्यम बनाया।
भारतेंदु युग की भाषाई विशेषताएँ
इस युग की भाषा विशेष रूप से सरस, सहज, प्रवाहमयी और लोकबोध से युक्त थी। ब्रजभाषा का प्रभाव क्रमशः कम होता गया और खड़ी बोली हिंदी ने काव्यात्मक तथा गद्यात्मक दोनों रूपों में स्थान बनाना आरंभ किया। युग की भाषा में संस्कृतनिष्ठता और तद्भव शब्दों का उचित संतुलन दिखाई देता है।
भाषा और शैली
भारतेंदु युग की भाषा मुख्यतः खड़ी बोली हिंदी है जो संस्कृतनिष्ठ, सरल, प्रवाहपूर्ण और भावनाओं की अभिव्यक्ति में समर्थ है। रचनाओं में लोकभाषा, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेज़ी के शब्दों का भी सहज प्रयोग हुआ है। इस युग की शैली संवादात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक और आलोचनात्मक है।
निष्कर्ष
भारतेन्दु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की प्रथम सीढ़ी है। यह युग साहित्य के माध्यम से समाज को चेतना देने वाला युग था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एक साहित्यिक क्रांति का जन्म हुआ, जिसने भाषा, भाव और विषय सभी स्तरों पर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनके साथियों और अनुयायियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और साहित्य को समाज का दर्पण बनाया।
भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में जागरण, विकास और सामाजिक क्रांति का युग है। यह युग साहित्य को कल्पनालोक से यथार्थ की ओर लाता है और भाषा को जन-जन की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के रचनाकारों ने हिंदी को साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना की भाषा बनाया। इस युग ने आने वाले द्विवेदी युग और छायावादी युग की नींव रखी और हिंदी साहित्य को आधुनिकता की दिशा में अग्रसर किया।
यह युग केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग के साहित्यकारों की देन आज भी हिंदी साहित्य की नींव के पत्थर के रूप में देखी जाती है। उनका कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और पथप्रदर्शक बना रहेगा।
इस प्रकार “भारतेंदु युग” केवल साहित्यिक युग नहीं, अपितु हिंदी नवजागरण का दीपस्तंभ है, जिसने भारतवर्ष के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन को नई दिशा दी।
भारतेंदु युग : प्रमुख प्रश्नोत्तरी एवं परीक्षा उपयोगी तथ्य (FAQs)
यहाँ “भारतेंदु युग” से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे UGC-NET, UPSC, TGT/PGT, CTET, आदि) तथा शैक्षणिक संदर्भों में अत्यंत उपयोगी हैं:
1. भारतेंदु युग का समयकाल क्या है?
उत्तर: भारतेंदु युग का समयकाल 1850 ई. से 1900 ई. तक माना जाता है।
2. भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है?
उत्तर: भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाम पर हुआ है।
3. भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
उत्तर: भारतेंदु युग को “हिंदी नवजागरण काल” भी कहा जाता है।
4. भारतेंदु युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कौन-कौन सी हैं?
उत्तर:
- नवजागरण चेतना
- सामाजिक चेतना
- भक्ति भावना
- शृंगारिकता
- रीति निरूपण
- समस्या पूर्ति
- राष्ट्रप्रेम और भाषा प्रेम
5. भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर:
- प्रेम मालिका
- प्रेम सरोवर
- गीत गोविन्दानन्द
- वर्षा विनोद
- दशरथ विलाप
- विनय प्रेम पचासा
- फूलों का गुच्छा (खड़ी बोली में)
6. भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन-कौन सी पत्रिकाएँ निकाली थीं?
उत्तर:
- कविवचन सुधा
- हरिश्चंद्र मैगजीन
- हरिश्चंद्र पत्रिका
7. भारतेंदु मंडल से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: भारतेंदु मंडल उन साहित्यकारों का समूह था जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर साहित्य सृजन किया। इनका उद्देश्य हिंदी साहित्य को जागरूक, राष्ट्रवादी और आधुनिक बनाना था।
8. भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार कौन थे?
उत्तर:
- प्रताप नारायण मिश्र
- बदरी नारायण चौधरी ‘प्रेमघन’
- बालकृष्ण भट्ट
- अंबिकादत्त व्यास
- राधा चरण गोस्वामी
- ठाकुर जगमोहन सिंह
- लाला श्रीनिवास दास
- राधाकृष्ण दास
- सुधाकर द्विवेदी
9. प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर:
- प्रेमपुष्पावली
- मन की लहर
- लोकोक्ति शतक
- श्रृंगार विलास
- ब्रेडला स्वागत
- दंगल खंड
10. बदरी नारायण चौधरी ‘प्रेमघन’ की कोई तीन प्रमुख रचनाएँ बताइए।
उत्तर:
- जीर्ण जनपद
- मयंक महिमा
- अलौकिक लीला
11. भारतेंदु युग की भाषा की विशेषता क्या थी?
उत्तर: भारतेंदु युग की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी थी, जिसमें सरलता, प्रवाह और जनसामान्य के लिए उपयुक्त अभिव्यक्ति की क्षमता थी।
12. भारतेंदु युग में गद्य साहित्य की कौन-कौन सी विधाएँ विकसित हुईं?
उत्तर:
- नाटक
- निबंध
- उपन्यास
- संवाद
- आलोचना
- कहानी
13. ‘कंस वध’ रचना किसकी है?
उत्तर: ‘कंस वध’ राधा कृष्ण दास की रचना है (हालांकि यह अपूर्ण है)।
14. ‘हो हो होरी’ किसकी रचना है?
उत्तर: यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है।
15. भारतेंदु युग के साहित्य में राष्ट्रवाद किस रूप में व्यक्त हुआ है?
उत्तर: भारतेंदु युग में राष्ट्रवाद साहित्य के माध्यम से जनमानस में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, विदेशी शासन की आलोचना, भाषा प्रेम, और भारत गौरव को स्थापित करने के रूप में दिखाई देता है।
इन्हें भी देखें –
- द्विवेदी युग (1900–1920 ई.): हिंदी साहित्य का जागरण एवं सुधारकाल
- सूफी काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- संत काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- कृष्ण भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- राम भक्ति काव्य धारा: सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- सुहाग की साड़ी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- पूस की रात | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- मृत्यु के पीछे | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY): भारत के कृषि क्षेत्र में समग्र सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम
- भारत में टेस्ला की ऐतिहासिक एंट्री: मुंबई के बीकेसी में पहला शोरूम और भारत के ईवी क्षेत्र का नया युग
- नई लाइकेन प्रजातियाँ और पश्चिमी घाट में सहजीवन का रहस्य: Allographa effusosoredica की खोज
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA): भारत में दत्तक ग्रहण की निगरानी और नियमन की आधारशिला
- दिल्ली में जियोसेल (Geocell) तकनीक से बनेगी पहली प्लास्टिक सड़क