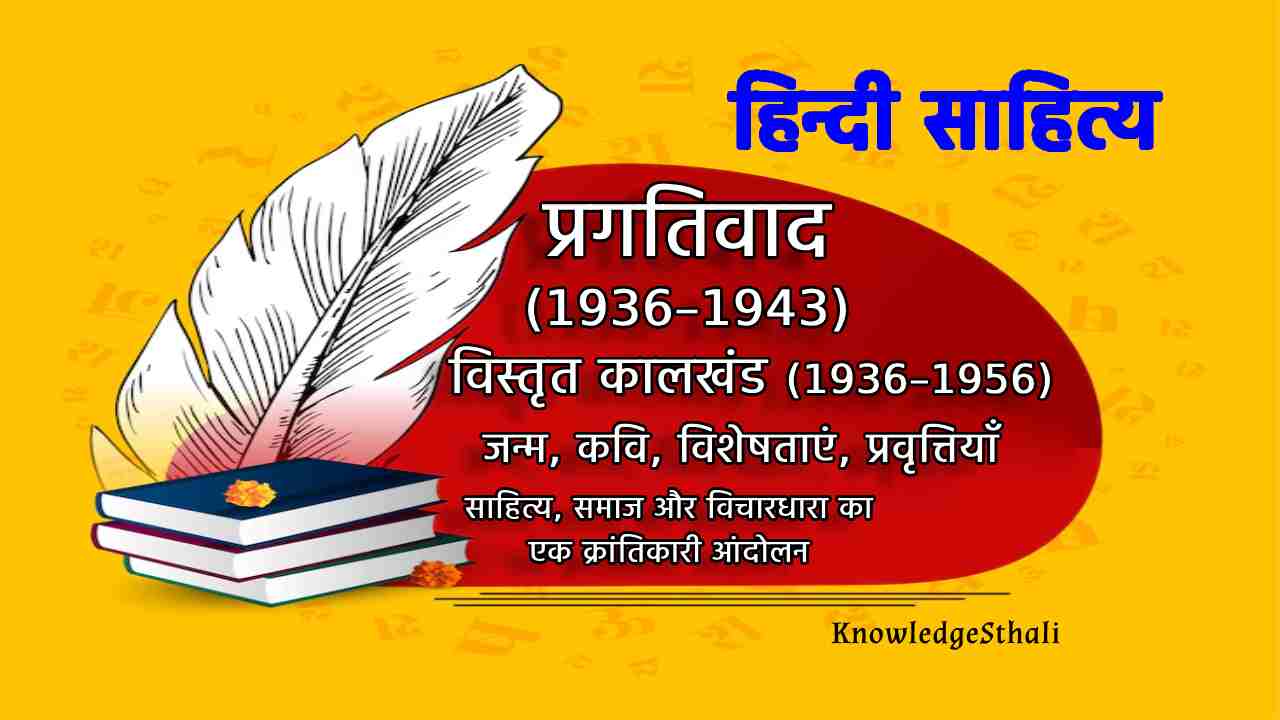‘प्रगतिवाद’ शब्द सुनते ही मन में एक गतिशील, उन्नतिशील और परिवर्तनकामी विचारों की धारा प्रवाहित होने लगती है। यह शब्द न केवल साहित्यिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका प्रयोग सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के सन्दर्भ में भी किया जाता है।
हिंदी साहित्य के इतिहास में ‘प्रगतिवाद’ एक ऐसे युग और आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है जिसने कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक को आम जनजीवन से जोड़ा, उसे जनसंघर्षों का स्वर प्रदान किया और सामाजिक न्याय के लिए साहित्य को एक हथियार बना दिया।
प्रगतिवाद का शाब्दिक और वैचारिक अर्थ
शब्द ‘प्रगति’ का अर्थ है – आगे बढ़ना, निरंतर उन्नति करते जाना। इस दृष्टि से ‘प्रगतिवाद’ का सामान्य अर्थ होता है – “समाज, राजनीति, साहित्य आदि के क्षेत्रों में निरंतर सुधार एवं उन्नति की आकांक्षा रखने वाला सिद्धांत।”
प्रगतिवाद केवल एक साहित्यिक विचारधारा नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतना का आंदोलन था, जो असमानता, शोषण, उत्पीड़न, सामंतवाद, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए उठ खड़ा हुआ।
प्रगतिवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
विश्व इतिहास में प्रगतिवाद की जड़ें औद्योगीकरण, उपनिवेशवाद और आधुनिकता के उन विचारों में छिपी हैं जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज के ढांचे को बुनियादी रूप से बदल दिया।
विशेषकर अमेरिका में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में प्रगतिवाद एक सशक्त सामाजिक-राजनैतिक आंदोलन के रूप में सामने आया। गृहयुद्ध के पश्चात अमेरिका में तीव्र औद्योगीकरण शुरू हुआ, जिसने श्रमिकों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर एक नई चेतना को जन्म दिया।
यही चेतना धीरे-धीरे दुनिया भर में फैलने लगी और ब्रिटेन, रूस, भारत जैसे देशों में भी सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की माँग ने जोर पकड़ा।
भारत में प्रगतिवाद का आगमन
भारत में प्रगतिवाद का आगमन 1930 के दशक में हुआ। यह वह समय था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी शासन, जातिवाद, सामंतवाद, गरीबी और अशिक्षा ने देश के एक बड़े वर्ग को शोषित और दमित बना दिया था।
इन्हीं परिस्थितियों में साहित्यकारों ने महसूस किया कि साहित्य केवल भावुकता, सौंदर्य या रहस्यवाद तक सीमित नहीं रह सकता। उसे समाज की सच्चाइयों को उद्घाटित करना चाहिए, शोषितों की आवाज बनना चाहिए और एक नया सामाजिक परिवर्तन लाने का माध्यम बनना चाहिए।
प्रगतिवाद का औपचारिक शुभारंभ (1936 ई.)
हिंदी में प्रगतिवाद के संगठित रूप की शुरुआत 1936 ई. में हुई, जब लखनऊ में ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ का स्थापना सम्मेलन आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता महान उपन्यासकार प्रेमचंद ने की।
प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में साहित्यकारों से आह्वान करते हुए कहा –
“साहित्य का उद्देश्य दबे-कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होना चाहिए।”
उनके इस वक्तव्य ने हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। इस अधिवेशन में यह स्पष्ट किया गया कि अब साहित्य सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति करेगा, जनता की भाषा में जनता के लिए लिखा जाएगा और उसमें सामाजिक संघर्ष, समानता और क्रांति की भावना होगी।
प्रगतिवाद का कालखंड
प्रगतिवाद युग का कालखंड सामान्यतः 1936 से 1943 ई. तक माना जाता है, परन्तु एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का इतिहास मुख्यतः 1936 ई. से 1956 ई. तक फैला हुआ है। यह वह काल था जब हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थ, श्रमिक चेतना, वर्ग संघर्ष और जनपक्षधरता जैसे विषय प्रमुखता से उभर कर सामने आए।
प्रगतिवाद एक प्रतिक्रियात्मक आंदोलन था जो छायावाद की व्यक्तिवादी, सौंदर्यवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध खड़ा हुआ और साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाने की वकालत करने लगा।
प्रगतिवाद युग (1936–1943) – सक्रिय आंदोलन की कालावधि
प्रगतिवाद युग की वास्तविक शुरुआत 1936 ई. में मानी जाती है, जब लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष प्रगतिशील लेखक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक वक्तव्य में साहित्य को समाज का दर्पण बताते हुए इसे सामाजिक परिवर्तन का औज़ार बनाने की बात कही थी।
इस काल में साहित्यकारों ने पूंजीवादी शोषण, सामाजिक विषमता, धार्मिक पाखंड, जमींदारी उत्पीड़न और स्त्री-असमानता जैसे विषयों को अपनी रचनाओं में केंद्र में रखा। छायावाद की भावुकता और सौंदर्यवादिता की जगह अब श्रम, संघर्ष और यथार्थ ने ली।
1936 से लेकर लगभग 1943 तक का समय प्रगतिवाद के सबसे अधिक सक्रिय और संगठित साहित्यिक आंदोलन का समय था। इस काल में राहुल सांकृत्यायन, सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, प्रेमचंद, यशपाल, नागार्जुन, रांगेय राघव और फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ जैसे लेखकों ने सामाजिक चेतना से ओतप्रोत रचनाएं लिखीं, जो जन-जीवन की समस्याओं से सीधे जुड़ी थीं।
प्रगतिवाद का विस्तृत कालखंड (1936–1956) – विचारधारा एवं प्रभाव का विस्तार
यद्यपि प्रगतिवाद का संगठित आंदोलन 1943 के बाद कुछ हद तक शिथिल पड़ने लगा, लेकिन उसकी विचारधारा और प्रभाव 1956 तक हिंदी साहित्य पर व्यापक रूप से बने रहे। इस काल को प्रगतिवाद का विस्तार काल या प्रभाव काल कहा जा सकता है। इसमें प्रगतिवाद एक संगठन या घोषणापत्र से अधिक एक संवेदना और दृष्टिकोण के रूप में कार्य कर रहा था।
इस समय अनेक साहित्यकारों ने भले ही खुद को “प्रगतिशील” घोषित न किया हो, लेकिन उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, वर्ग-संघर्ष, किसान-मजदूर जीवन और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथ ही, इस चरण में यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, व्यंग्य और आत्मचिंतन की प्रवृत्तियाँ भी उभरने लगीं, जो बाद में ‘नई कहानी’ और ‘अकहानी’ जैसे आंदोलनों की पृष्ठभूमि बनीं।
इस प्रकार 1936 से 1956 तक प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के केंद्र में बना रहा – पहले एक सक्रिय आंदोलन के रूप में, और फिर एक प्रभावशाली विचारधारा के रूप में, जिसने भारतीय समाज और साहित्य दोनों को गहरे रूप से प्रभावित किया।
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और विकास
प्रगतिशील लेखक संघ की संकल्पना सर्वप्रथम 1935 ई. में इंग्लैंड में हुई थी। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार ई. एम. फॉस्टर (E. M. Forster) ने पेरिस में ‘प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन’ की स्थापना की थी।
इससे प्रेरणा लेकर भारत में सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, अहमद अली, रशीदजहाँ आदि लेखकों ने 1936 में ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ (Progressive Writers’ Association – PWA) की नींव रखी।
इस आंदोलन का उद्देश्य था –
- साहित्य को जनसामान्य के जीवन से जोड़ना
- श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं को साहित्य में स्थान देना
- औपनिवेशिक शासन, सांप्रदायिकता और सामंतवाद का विरोध करना
- वर्गहीन, जातिविहीन, न्यायपूर्ण समाज की कल्पना को साहित्यिक रूप देना
प्रमुख प्रगतिवादी कवि (1936–1956)
प्रगतिवादी युग में जिन कवियों ने साहित्य को सामाजिक उद्देश्य की दिशा दी, उनके नाम इस प्रकार हैं:
- केदारनाथ अग्रवाल
- नागार्जुन
- रामविलास शर्मा
- रांगेय राघव
- शिवमंगल सिंह ‘सुमन’
- त्रिलोचन
इन कवियों की रचनाओं में समाज की पीड़ा, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और मेहनतकश जनता की आवाज मुखर होती है।
प्रगतिवादी साहित्य के प्रमुख लेखक
हिंदी में प्रगतिवाद के अंतर्गत कई लेखक और कवि सामने आए जिन्होंने इस आंदोलन को दिशा दी। प्रमुख नाम हैं:
कविता में:
- नागार्जुन
- त्रिलोचन
- केदारनाथ अग्रवाल
- शमशेर बहादुर सिंह
- रमेशचंद्र शाह
- भवानीप्रसाद मिश्र
कहानी में:
- प्रेमचंद
- यशपाल
- भीष्म साहनी
- अज्ञेय (प्रारंभिक कहानियाँ)
- सुभद्राकुमारी चौहान
उपन्यास में:
- फणीश्वरनाथ रेणु
- यशपाल
- राहुल सांकृत्यायन
- अमृतलाल नागर
- नरेंद्र कोहली
प्रगतिवादी काव्य की भाषा और शैली
प्रगतिवादी काव्य की भाषा शैली में निम्न विशेषताएँ पाई जाती हैं:
- सीधी, सहज, प्रखर और तीखी भाषा
- अत्यंत प्रभावशाली व्यंग्यात्मक तेवर
- क्रांतिकारी आग्रह
- नारेबाजी से दूर रहकर भी वैचारिक स्पष्टता और आक्रोश
इस प्रकार की शैली का उद्देश्य था – आम जनता तक स्पष्ट रूप से विचारों को पहुँचाना और उनके भीतर जागृति पैदा करना।
प्रगतिवाद: एक निरंतर विकसित होने वाली साहित्यधारा
यद्यपि प्रगतिवाद की ऐतिहासिक सीमा 1936 से 1956 के बीच मानी जाती है, परंतु व्यापक अर्थ में यह कोई स्थिर मतवाद या काव्यरूप नहीं है।
यह एक निरंतर विकसित होने वाली साहित्यधारा है, जो समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप को विस्तार देती रही है।
परवर्ती कवि, जिन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा को नई पीढ़ी में आगे बढ़ाया, उनमें प्रमुख हैं:
- केदारनाथ सिंह
- धूमिल
- कुमार विमल
- अरुण कमल
- राजेश जोशी
इन कवियों ने प्रगतिशीलता को नए सामाजिक संदर्भों और शिल्प में ढालते हुए उसे 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भी प्रासंगिक बनाए रखा।
साहित्य के उद्देश्य की प्रगतिवादी परिभाषा
प्रगतिवाद साहित्य को केवल सौंदर्यबोध की वस्तु नहीं मानता, बल्कि वह साहित्य को सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित सृजन मानता है।
इस आंदोलन का स्पष्ट मत है:
“कला, कला के लिए नहीं, बल्कि कला, जीवन के लिए होनी चाहिए।”
इसका अर्थ है कि साहित्य केवल आनंद या मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने और बदलाव लाने का उपकरण होना चाहिए।
प्रगतिवाद आनंदवाद की जगह भौतिक उपयोगितावादी मूल्यों को प्राथमिकता देता है, जहाँ साहित्य का लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष और न्याय की स्थापना में योगदान देना होता है।
वैचारिक आधार: मार्क्सवाद से प्रेरित पर सीमित नहीं
प्रगतिवादी काव्य का वैचारिक आधार मार्क्सवादी दर्शन रहा है, किंतु यह केवल मार्क्सवाद का साहित्यिक अनुवाद मात्र नहीं है।
प्रगतिवादी आंदोलन की वास्तविक पहचान जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण में निहित है, जो निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट होता है:
- पुराने रूढ़िबद्ध जीवन-मूल्यों का त्याग
- आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक अवधारणाओं के स्थान पर लोक-आधारित विचारों को महत्व
- हर प्रकार के शोषण और दमन का विरोध
- धर्म, जाति, लिंग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर गैर-बराबरी का विरोध
- स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र में अटूट विश्वास
- सतत परिवर्तन और प्रगति में भरोसा
- मेहनतकश वर्गों के प्रति सहानुभूति और समर्थन
- नारी उत्पीड़न का विरोध
- साहित्य को सामाजिक उत्तरदायित्व का वाहक मानना
प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
प्रगतिवाद केवल विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि यह एक सजग साहित्यिक प्रवृत्ति है, जिसमें निम्नलिखित गुण प्रमुखता से देखे जा सकते हैं:
- इतिहास चेतना:
प्रगतिवादी साहित्य इतिहास को सामाजिक संदर्भों में समझने का प्रयास करता है। - सामाजिक यथार्थ दृष्टि:
जीवन की कठोर सच्चाइयों को बेझिझक साहित्य में प्रस्तुत किया गया। - वर्ग चेतना:
श्रमिक वर्ग, किसान, दलित, स्त्रियाँ – सब शोषित वर्गों की पीड़ा साहित्य का केंद्र बनी। - प्रतिबद्धता या पक्षधरता:
लेखक केवल निरीक्षक नहीं, बल्कि सामाजिक संघर्षों का सहभागी और पक्षधर होता है। - गहरी जीवनासक्ति:
जीवन की जटिलताओं और सुंदरताओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण। - भविष्योन्मुखी दृष्टि:
साहित्य वर्तमान की आलोचना के साथ एक बेहतर भविष्य की कल्पना करता है।
प्रगतिवाद के प्रमुख सिद्धांत
प्रगतिवादी साहित्यकारों के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत थे, जो उनके लेखन में परिलक्षित होते हैं:
- सामाजिक यथार्थ का चित्रण:
साहित्य कल्पना और रहस्य से ऊपर उठकर अब समाज की वास्तविक परिस्थितियों का दर्पण बना। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, स्त्री-शोषण, जातिवाद आदि विषयों पर खुलकर लिखा गया। - जनता की पक्षधरता:
साहित्य का उद्देश्य जनता की पीड़ा को स्वर देना था। मजदूर, किसान, स्त्रियाँ और दलित अब साहित्य के नायक बने। - क्रांतिकारी चेतना:
पूंजीवादी व्यवस्था और उपनिवेशवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रगतिवादी साहित्य की आत्मा बनी। - समानता और बंधुत्व:
समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध और एक समतावादी समाज की स्थापना की आकांक्षा। - युद्ध और शांति:
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय प्रगतिवादी लेखकों ने युद्ध की विभीषिका के विरुद्ध साहित्य रचा और शांति की आकांक्षा व्यक्त की।
प्रगतिवाद और छायावाद का संबंध
प्रगतिवाद, हिंदी कविता में छायावादोत्तर युग की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। जहाँ छायावाद में व्यक्तिवाद, सौंदर्य और रहस्य का समावेश था, वहीं प्रगतिवाद ने सामाजिक यथार्थ, वस्तुनिष्ठता और क्रांतिकारी दृष्टिकोण को अपनाया।
यह कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद ने छायावादी कवियों की भावुकता और कल्पनाशीलता से आगे बढ़कर वस्तुगत यथार्थ की भूमि पर साहित्य को प्रतिष्ठित किया।
छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर
छायावाद और प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के दो प्रमुख युग हैं, जिनकी दृष्टि, भावना और उद्देश्य एक-दूसरे से भिन्न हैं। नीचे उनके प्रमुख अंतरों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है:
| विषय | छायावाद | प्रगतिवाद |
|---|---|---|
| कविता का उद्देश्य | ‘स्वान्तः सुखाय’ (अपने सुख के लिए) | ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ (समाज के लिए) |
| भावना की प्रकृति | वैयक्तिक भावना | सामाजिक भावना |
| विषयवस्तु | प्रेम, सौंदर्य, रहस्य, आत्मानुभूति | श्रमिक जीवन, सामाजिक अन्याय, संघर्ष |
| काव्य का स्वरूप | कल्पनाशीलता, रहस्यात्मकता | ठोस यथार्थ, यथार्थपरक चित्रण |
| भाषा शैली | क्लिष्ट, काव्यात्मक | सरल, व्यंग्यात्मक, जनभाषा |
| छंद | परंपरागत छंदों का प्रयोग | मुक्त छंद और लोकगीतों का आधार |
प्रगतिवादी काव्य सामाजिक यथार्थ का सार्थक चित्रण है। यह जनसरोकारों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहन प्रतिबद्धता रखता है। इसकी भाषा आमजन की है, शैली व्यंग्यात्मक और उद्देश्य व्यापक परिवर्तन का है।
प्रगतिवाद और समाजवाद का संबंध
जिस प्रकार राजनीति में ‘समाजवाद’ का स्थान महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार साहित्य में ‘प्रगतिवाद’ का स्थान है।
यह आंदोलन साहित्य को समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़कर क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर अग्रसर करता है।
प्रगतिवाद एक ऐसा मंच रहा, जहाँ लेखक, कवि, विचारक और समाज एक साथ आकर शोषण, अन्याय, असमानता और अंधविश्वास के विरुद्ध संघर्ष करते हैं।
प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएँ
प्रगतिवादी काव्य परंपरागत सौंदर्यपरकता से हटकर सामाजिक सरोकारों, यथार्थवाद और जनजीवन की पीड़ा को स्वर देने वाला साहित्य है। इसकी निम्नलिखित विशिष्टताएँ उल्लेखनीय हैं:
1. समाजवादी यथार्थवाद / सामाजिक यथार्थ का चित्रण
प्रगतिवादी काव्य का मूल आधार सामाजिक यथार्थवाद है। इसमें समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग की समस्याओं, संघर्षों और आकांक्षाओं का यथासंभव यथार्थपरक चित्रण किया गया है।
2. प्रकृति के प्रति लगाव
हालाँकि प्रगतिवाद मुख्यतः सामाजिक चेतना पर केंद्रित है, फिर भी इसमें प्रकृति के प्रति आत्मीय संबंध और सहभावना की झलक भी मिलती है। यह प्रकृति सौंदर्य के चित्रण तक सीमित न होकर जीवन संघर्षों से जुड़ी हुई दिखाई देती है।
3. नारी प्रेम और नारी चेतना
प्रगतिवादी कवियों ने नारी को केवल सौंदर्य का प्रतीक न मानकर उसके अधिकारों, संघर्षों और समाज में स्थिति को रेखांकित किया।
नारी प्रेम यहाँ केवल रोमांटिक नहीं, बल्कि सामाजिक सहानुभूति और समानता के भाव से युक्त है।
4. राष्ट्रीयता
इस आंदोलन के समय भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौर से गुजर रहा था, अतः राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति और स्वराज्य की भावना भी प्रगतिवादी काव्य में व्यापक रूप से अभिव्यक्त हुई।
5. सांप्रदायिकता का विरोध
प्रगतिवादी साहित्यकारों ने समाज में फैली धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिकता और जातीय भेदभाव का खुलकर विरोध किया और एक समानतावादी, धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की।
6. बोधगम्य भाषा और व्यंग्यात्मकता
प्रगतिवादी कवियों ने भाषा को जनसाधारण के अनुकूल बनाया।
- सीधी-सादी, सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया।
- व्यंग्यात्मकता का प्रयोग करके सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया।
यह काव्य “जनता की भाषा में जनता की बात” करने वाला साहित्य है।
7. मुक्त छंद का प्रयोग
प्रगतिवादी कवियों ने बंधे-बंधाए छंदों की परंपरा से हटकर मुक्त छंद को अपनाया।
इसका आधार लोकगीतों की शैलियाँ रहीं जैसे –
- कजरी,
- लावनी,
- ठुमरी इत्यादि।
इससे कविता में अधिक गति, लय और जीवन का संप्रेषण संभव हो पाया।
8. मुक्तक काव्य रूप का प्रयोग
इस आंदोलन में मुक्तक काव्य रूप को विशेष रूप से अपनाया गया, जिससे कवि को व्यक्तिगत विचारों और सामाजिक विषयों को संक्षेप में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की सुविधा मिली।
प्रगतिवाद पर आलोचनाएं
प्रत्येक आंदोलन की तरह प्रगतिवाद को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ प्रमुख आलोचनाएं थीं:
- साहित्य का अधिक राजनीतिकरण किया गया
- कलात्मकता की उपेक्षा की गई
- विचारों की एकरूपता के कारण साहित्य विविधता खो बैठा
- प्रचारात्मक भाषा और नारों की भरमार ने साहित्यिक गरिमा को प्रभावित किया
इसके बावजूद, प्रगतिवाद का ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व असंदिग्ध है।
प्रगतिवाद की विरासत और प्रभाव
प्रगतिवाद ने हिंदी साहित्य को जनता के संघर्षों से जोड़ा, साहित्य को सामाजिक सरोकारों का वाहक बनाया और लेखक की भूमिका को केवल सर्जक से बढ़ाकर सामाजिक कार्यकर्ता तक पहुँचा दिया।
इस आंदोलन की विरासत आज भी विभिन्न साहित्यिक आंदोलनों में देखी जा सकती है, जैसे:
- जनवादी आंदोलन
- नारीवादी साहित्य
- दलित साहित्य
- आदिवासी साहित्य
इन सभी आंदोलनों की जड़ें किसी न किसी रूप में प्रगतिवाद से जुड़ी हुई हैं।
निष्कर्ष
प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक जन-संवेदना से जुड़ा सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि इसने साहित्य को जनता के सरोकारों से जोड़ा, उसे सामाजिक उत्तरदायित्व का स्वरूप प्रदान किया।
प्रगतिवाद केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी – विचारों की, दृष्टिकोण की, और संवेदनाओं की। इसने साहित्य को जनता की जमीन से जोड़ा, भाषा को आम आदमी की बोली बनाया, और लेखक को समाज का सजग प्रहरी बनाया।
आज जब साहित्य फिर से बाजारवाद, व्यक्तिवाद और तकनीकी दुनिया के शोर में खोता जा रहा है, समाज फिर से असमानताओं और विद्वेष की ओर लौटता दिख रहा है, तब प्रगतिवाद की चेतना एक बार फिर न केवल प्रासंगिक बन जाती है, बल्कि आवश्यक भी।
महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर (FAQs)
प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर, जो स्कूल परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे UGC-NET, TGT/PGT हिंदी, UPSC) और अकादमिक अध्ययन के लिए उपयोगी हैं:
🔹 1. प्रगतिवाद क्या है?
उत्तर:
प्रगतिवाद एक साहित्यिक आंदोलन है जो साहित्य को सामाजिक यथार्थ, श्रमिक जीवन, शोषण, असमानता, अन्याय और जनसरोकारों से जोड़ता है। इसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और सुधार है।
🔹 2. हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की शुरुआत कब हुई?
उत्तर:
हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की औपचारिक शुरुआत 1936 ई. में लखनऊ में हुए प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना अधिवेशन से हुई।
🔹 3. प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की?
उत्तर:
भारत में सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, अहमद अली और रशीद जहाँ ने मिलकर 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की।
🔹 4. प्रगतिवाद के प्रारंभिक काल के प्रमुख कवि कौन-कौन थे?
उत्तर:
केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, रांगेय राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह ‘सुमन’ आदि।
🔹 5. प्रगतिवाद के परवर्ती प्रमुख कवियों के नाम लिखिए।
उत्तर:
केदारनाथ सिंह, धूमिल, कुमार विमल, अरुण कमल, राजेश जोशी आदि।
🔹 6. प्रगतिवाद किन सिद्धांतों पर आधारित है?
उत्तर:
- मार्क्सवादी दृष्टिकोण
- सामाजिक यथार्थवाद
- वर्ग चेतना
- जनपक्षधरता
- समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र में विश्वास
🔹 7. प्रेमचंद ने प्रगतिवादी अधिवेशन में क्या कहा था?
उत्तर:
“साहित्य का उद्देश्य दबे-कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए।”
🔹 8. प्रगतिवादी साहित्य की भाषा कैसी होती है?
उत्तर:
साधारण, सरल, स्पष्ट, जनभाषा में और अक्सर व्यंग्यात्मक।
🔹 9. प्रगतिवाद में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ?
उत्तर:
मुक्त छंद का प्रयोग, जो लोकगीतों जैसे कजरी, ठुमरी, लावनी आदि पर आधारित होता था।
🔹 10. प्रगतिवाद का काव्य रूप क्या है?
उत्तर:
अधिकतर मुक्तक काव्य रूप में लिखा गया, ताकि छोटे रूप में गहन भाव प्रस्तुत किया जा सके।
🔹 11. छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है?
उत्तर:
छायावाद में भावुकता, आत्मचिंतन और कल्पना प्रमुख है जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ, संघर्ष और परिवर्तन की भावना।
🔹 12. ‘कला के लिए कला’ और ‘कला जीवन के लिए’ में क्या अंतर है?
उत्तर:
‘कला के लिए कला’ सौंदर्य और आत्मसंतोष को प्राथमिकता देता है, जबकि ‘कला जीवन के लिए’ समाज सेवा और जनहित को।
🔹 13. प्रगतिवाद किस राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है?
उत्तर:
समाजवाद और मार्क्सवाद से।
🔹 14. क्या प्रगतिवाद स्थिर साहित्यिक मत है?
उत्तर:
नहीं, यह एक निरंतर विकासशील साहित्यधारा है जो समय के साथ बदलती रही है।
🔹 15. प्रगतिवादी कविता का उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
जनता की समस्याओं को उजागर करना, सामाजिक बदलाव लाना, शोषण और अन्याय का विरोध करना।
🔹 16. क्या प्रगतिवाद केवल कविता तक सीमित है?
उत्तर:
नहीं, यह कहानी, उपन्यास, नाटक सहित सभी साहित्यिक विधाओं में प्रकट होता है।
🔹 17. प्रगतिवादी काव्य में नारी चित्रण कैसा है?
उत्तर:
नारी को केवल सौंदर्य या प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्षशील और चेतनशील व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया।
🔹 18. प्रगतिवादी कविता में व्यंग्य का क्या स्थान है?
उत्तर:
व्यंग्य एक प्रभावशाली हथियार है जिससे सामाजिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया गया।
🔹 19. हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के पहले उपन्यासकार कौन माने जाते हैं?
उत्तर:
प्रेमचंद, जिनकी रचनाएँ जैसे ‘गोदान’, ‘कफन’ आदि प्रगतिशील चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं।
🔹 20. प्रगतिवाद के उद्देश्य को एक वाक्य में व्यक्त कीजिए।
उत्तर:
“साहित्य को जनता के संघर्षों और सरोकारों से जोड़कर सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाना।”
🔹 21. ‘धूमिल’ किस प्रकार के कवि माने जाते हैं?
उत्तर:
धूमिल एक क्रांतिकारी प्रगतिवादी कवि हैं जिन्हें जनतंत्र की भाषा में विद्रोह और आक्रोश का स्वर कहा जाता है।
प्रश्न: प्रगतिवाद का वास्तविक कालखंड क्या है? क्या यह केवल 1936–1943 तक सीमित है या इसका विस्तार 1956 तक होता है?
उत्तर:
प्रगतिवाद का कालखंड सामान्यतः दो चरणों में विभाजित किया जाता है:
1. प्रगतिवाद युग (1936–1943):
यह प्रगतिवाद का प्रारंभिक दौर था, जब हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना (1936) के साथ सामाजिक यथार्थ, श्रमिक वर्ग की चेतना, वर्ग संघर्ष, साम्राज्यवाद विरोध और जनसरोकारों की अभिव्यक्ति जोर पकड़ने लगी। इस काल में साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण माना गया और छायावाद की व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का विरोध किया गया।
यह संकीर्ण और विशेष अर्थों में प्रगतिवाद का मुख्य या प्रारंभिक चरण है। इस अवधि में:
- 1936 में प्रेमचंद द्वारा लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई।
- इस दौर में प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, यशपाल, आदि प्रमुख लेखक थे।
- यह काल छायावाद के विरुद्ध सक्रिय साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का शुद्ध रूप दिखाता है।
2. प्रगतिवाद का विस्तारित कालखंड (1936–1956):
हालांकि 1943 के बाद प्रगतिवाद की तीव्रता में कुछ ह्रास हुआ, किंतु विचारधारा के रूप में इसका प्रभाव 1956 तक बना रहा। इस अवधि में कई लेखक प्रगतिशील विचारों के साथ लिखते रहे, यद्यपि साहित्यिक प्रवृत्तियों में विविधता और प्रयोगशीलता का प्रवेश भी हुआ। यह काल मार्क्सवादी दृष्टिकोण से यथार्थवाद, दलित चेतना, स्त्री विमर्श और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े साहित्य के विकास का साक्षी रहा।
यह समय सीमा उस काल को दर्शाती है जब प्रगतिशील विचारधारा ने साहित्य में अपना प्रभाव बनाए रखा:
- इस काल में यद्यपि नयी कहानी, प्रयोगवाद और अंततः अज्ञेय का ‘तार सप्तक’ आदि आने लगे थे, लेकिन प्रगतिवादी विचार सक्रिय बने रहे।
- इसे प्रगतिवाद की प्रभावशीलता या विस्तार का काल भी कहा जा सकता है।
निष्कर्षतः
प्रगतिवाद का मूल युग 1936–1943 माना जाता है, परंतु इसका वैचारिक प्रभाव और साहित्यिक विस्तार 1956 तक देखा जा सकता है।
- यदि आप “प्रगतिवाद युग” शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो सही समय सीमा है: 1936–1943।
- यदि आप प्रगतिशील साहित्यिक प्रवृत्तियों के व्यापक प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो समय सीमा है: 1936–1956।
इन्हें भी देखें –
- मुहावरा और लोकोक्तियाँ 250+
- वर्तनी किसे कहते है? उसके नियम और उदहारण
- रस- परिभाषा, भेद और उदाहरण
- छायावादोत्तर युग (शुक्लोत्तर युग: 1936–1947 ई.) | कवि और उनकी रचनाएँ
- 8वां केंद्रीय वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण
- हाटी जनजाति: परंपरा, पहचान और कानूनी विमर्श का समावेशी विश्लेषण
- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC): वैश्विक न्याय प्रणाली में यूक्रेन की नई भागीदारी और भारत की दूरी
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: पद, प्रक्रिया और संभावित प्रभाव
- पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र | परिमंडल | Earth’s Domain | Circle
- विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय
- महान व्यक्तियों के उपनाम, स्थान, प्रमुख वचन एवं नारे
- Tense: Definition, Types, and 100+ Examples