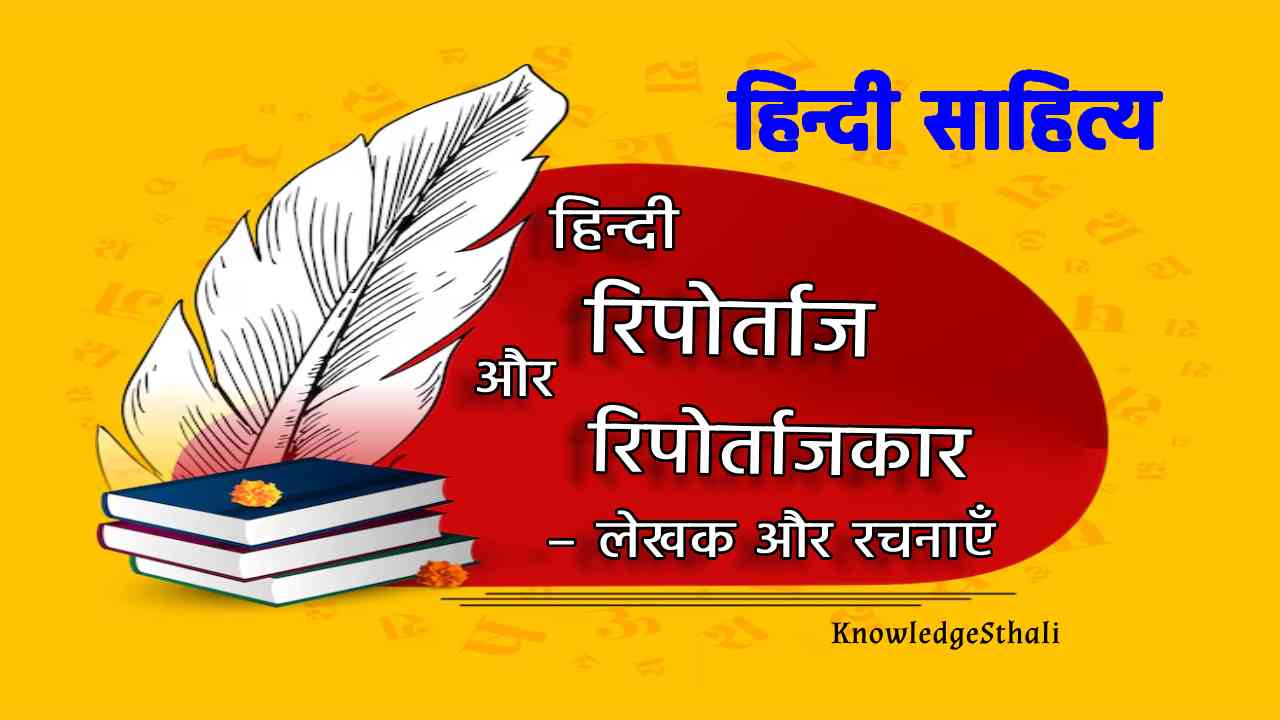हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में ‘रिपोर्ताज’ अपेक्षाकृत नई लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। यह न केवल किसी घटना का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है, बल्कि उसमें लेखक की संवेदनशील दृष्टि, साहित्यिकता और भावनात्मक ताप भी समाहित होता है। रिपोर्ट और रिपोर्ताज में सूक्ष्म लेकिन निर्णायक अंतर है—रिपोर्ट मात्र तथ्यों का संकलन है, जबकि रिपोर्ताज इन तथ्यों को साहित्यिक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है।
यह विधा विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुई और हिंदी साहित्य में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान बना। आइए, विस्तार से इसके अर्थ, स्वरूप, विकास, विशेषताओं और प्रमुख उदाहरणों पर विचार करें।
रिपोर्ताज का अर्थ
‘रिपोर्ताज’ शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से मानी जाती है, जो अंग्रेजी शब्द ‘Report’ से मेल खाता है। अंग्रेजी में ‘Report’ का अर्थ है किसी घटना का तथ्यों के आधार पर विवरण, जिसे समाचार पत्रों के संवाददाता तैयार करते हैं। इसका उद्देश्य पाठकों को घटित घटनाओं की जानकारी देना होता है।
लेकिन ‘रिपोर्ताज’ इस साधारण रिपोर्ट से अलग है। इसमें—
- तथ्यात्मकता के साथ साहित्यिकता होती है।
- कल्पना और संवेदना का पुट शामिल होता है।
- लेखक की निजी अनुभूति और दृष्टिकोण भी झलकता है।
हिंदी साहित्य कोष में स्पष्ट किया गया है—
“रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं।”
बाबू गुलाबराय के अनुसार—
“रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है किन्तु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है, जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसको प्रभावमय बना देता है।”
अर्थात, रिपोर्ट केवल तथ्यों का संकलन है, जबकि रिपोर्ताज में वही तथ्य एक जीवंत साहित्यिक अनुभव में रूपांतरित हो जाते हैं।
रिपोर्ताज की उत्पत्ति और विकास
रिपोर्ताज का विकास यूरोप में 1936 ई. के आसपास, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय हुआ। युद्ध के दौरान, लेखकों और पत्रकारों ने मोर्चे से प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित साहित्यिक रिपोर्ट लिखनी शुरू कीं। इन लेखन में युद्ध के भयावह दृश्य, सैनिकों का साहस, और जनता की पीड़ा का कलात्मक चित्रण था। यही साहित्यिक रिपोर्टें आगे चलकर ‘रिपोर्ताज’ कहलाने लगीं।
रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग को माना जाता है। उनके युद्धकालीन लेखन ने इस विधा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी।
भारत में, विशेषकर हिंदी साहित्य में, 20वीं सदी के मध्य से रिपोर्ताज लेखन की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक आंदोलनों, और ग्रामीण-शहरी जीवन की घटनाओं पर आधारित अनेक रिपोर्ताज सामने आए।
रिपोर्ताज का स्वरूप
रिपोर्ताज का स्वरूप बहुआयामी है। इसे समझने के लिए हम विभिन्न साहित्यकारों की परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं—
- डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के अनुसार— “किसी घटना की रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्ताज कहा जाता है।” वे आगे कहते हैं कि बिना कल्पना को अनुभव में बदले, सफल रिपोर्ताज नहीं लिखा जा सकता, और बिना अनुभव को कल्पना में पकाए भी यह सफल नहीं हो सकता।
- डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार— “कल्पना के सहारे रिपोर्ताज नहीं लिखी जा सकती… रिपोर्ताज लिखने के लिए जनता से सच्चा प्रेम होना चाहिए।”
- एक अन्य दृष्टिकोण में कहा गया है कि इसका संबंध केवल वर्तमान से होता है, लेकिन उसमें भूतकालीन मूल्य और भावनाएं, तथा भविष्य के प्रति उत्कट लालसा भी समाहित होती है।
निष्कर्षतः—
रिपोर्ताज में घटनाओं का यथार्थ चित्रण, लेखक की संवेदनशील दृष्टि, तथा कलात्मक अभिव्यक्ति का संगम होता है। यह केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि पाठक को घटना का प्रत्यक्ष अनुभव कराने का साधन है।
रिपोर्ताज की विशेषताएं
रिपोर्ताज की विशिष्टताएं इसे सामान्य रिपोर्ट या कथा से अलग करती हैं—
- आँखों देखी घटनाओं पर आधारित
- इसमें प्रत्यक्ष अनुभव का महत्व सर्वोपरि है।
- लेखक वही लिखता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो।
- तथ्य प्रधानता, सीमित कल्पना
- इसमें तथ्यों का सही और सटीक प्रस्तुतीकरण होता है।
- कल्पना का उपयोग केवल प्रभाव और साहित्यिकता बढ़ाने के लिए होता है।
- घटना-प्रधानता और कथा तत्व
- घटना का क्रमबद्ध और जीवंत वर्णन किया जाता है।
- संवाद, दृश्य और पात्रों का चित्रण भी किया जा सकता है।
- लेखक की संवेदनशीलता और पर्यवेक्षण शक्ति
- सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण पकड़ने की क्षमता आवश्यक है।
- केवल घटनाक्रम ही नहीं, उससे जुड़े माहौल और भावनाओं को भी व्यक्त किया जाता है।
- सरल, प्रवाहपूर्ण और भावनात्मक भाषा
- पाठक को घटना का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए भाषा सरल और प्रभावशाली होती है।
- सीमित परिधि में अधिक तथ्यों का प्रस्तुतीकरण
- आकार का बंधन नहीं है, लेकिन अनावश्यक विस्तार से बचा जाता है।
- साहित्यिकता और कलात्मकता का समावेश
- वर्णन में साहित्यिक सौंदर्य, उपमा, रूपक आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
हिंदी में प्रमुख रिपोर्ताज और लेखक
हिंदी साहित्य में अनेक महत्वपूर्ण लेखकों ने रिपोर्ताज विधा में उत्कृष्ट योगदान दिया है। नीचे कुछ प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत हैं—
| क्रम | लेखक | प्रमुख रिपोर्ताज |
|---|---|---|
| 1 | शिवदान सिंह चौहान | लक्ष्मीपुरा (1938), मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई |
| 2 | रांगेय राघव | तूफानों के बीच (1946) |
| 3 | प्रकाश चन्द्र गुप्त | स्वराज भवन, अल्मोड़ा का बाज़ार, बंगाल का अकाल, रेखाचित्र |
| 4 | भदंत आनंद कौसल्यायन | देश की मिट्टी बुलाती है |
| 5 | उपेन्द्र नाथ अश्क | पहाड़ों में प्रेममय संगीत, रेखाएँ और चित्र |
| 6 | शमशेर बहादुर सिंह | प्लाट का मोर्चा (1952) |
| 7 | कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’ | क्षण बोले कण मुस्काए (1953) |
| 8 | श्रीकांत वर्मा | अपोलो का रथ |
| 9 | लक्ष्मीचंद्र जैन | कागज की कश्तियां, नये रंग नए ढंग |
| 10 | शिवसागर मिश्र | वे लड़ेंगे हजारों साल (1966) |
| 11 | धर्मवीर भारती | युद्ध यात्रा (1972) |
| 12 | अज्ञेय | देश की मिट्टी बुलाती है |
| 13 | फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ | ऋण जल धन जल (1977), नेपाली क्रांति कथा (1978), श्रुत-अश्रुत पूर्व (1984), एकलव्य के नोट्स |
| 14 | विवेकी राय | जुलूस रुका है (1977), बाढ़! बाढ़!! बाढ़!!! |
| 15 | भागवत शरण उपाध्याय | खून के छीटें |
| 16 | राम कुमार वर्मा | पेरिस के नोट्स |
| 17 | निर्मल वर्मा | प्राग: एक स्वप्न |
| 18 | कमलेश्वर | क्रांति करते हुए आदमी को देखना |
| 19 | श्री कान्त वर्मा | मुक्ति फौज |
| 20 | यशपाल जैन | रूस में छियालीस दिन |
| 21 | मणि मधुकर | पिछला पहाड़, सूखे सरोवर का भूगोल |
| 22 | रामनारायण उपाध्याय | गरीब और अमीर पुस्तकें |
| 23 | विद्यानिधि सिद्वांतालंकार | शिवालिक की घाटियों में |
| 24 | मुनि कांतिसागर | खंडहरों का वैभव |
इन लेखकों के कार्यों में विविध सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों में लिखे गए रिपोर्ताज शामिल हैं, जो हिंदी साहित्य की इस विधा की समृद्धि को दर्शाते हैं।
हिंदी रिपोर्ताज और उसका विकास
हिंदी साहित्य में रिपोर्ताज का विकास एक क्रमिक और रोचक यात्रा रही है। यह विधा केवल समाचार या घटनाओं के सूखे विवरण तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की धड़कनों को शब्दों में बाँधने का माध्यम बनी। यूरोपीय परंपरा से प्रभावित होकर हिंदी में रिपोर्ताज की शुरुआत 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई, लेकिन समय के साथ इसमें देशज संवेदनाओं, स्थानीय रंगों और जनजीवन की वास्तविकताओं ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। इस विकास यात्रा में अनेक साहित्यकारों ने योगदान दिया, जिनमें प्रारंभिक दौर में शिवदान सिंह चौहान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
1. प्रारंभिक दौर और शिवदान सिंह चौहान
हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। उनका प्रसिद्ध रिपोर्ताज ‘लक्ष्मीपुरा’ हिंदी का पहला रिपोर्ताज माना जाता है, जो सुमित्रानंदन पंत के संपादन में निकलने वाली रूपाभ पत्रिका के दिसंबर, 1938 ई. के अंक में प्रकाशित हुआ था।
‘लक्ष्मीपुरा’ में एक गाँव के हलचल भरे जीवन का सजीव चित्रण है, जिसमें ग्रामीण समाज की जीवंतता, परिवेश और मानवीय संबंधों की झलक मिलती है। इसके तुरंत बाद ही हंस पत्रिका में उनका दूसरा रिपोर्ताज ‘मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई’ प्रकाशित हुआ।
संपादक के रूप में चौहान ने अपना देश नामक स्थायी स्तंभ प्रारंभ किया, जिसमें प्रतिमाह एक रिपोर्ताज प्रकाशित होता था। इस तरह उन्होंने हिंदी में रिपोर्ताज को एक नई दिशा और पहचान दी।
2. रांगेय राघव और युद्धकालीन विषय
1944 ई. में विशाल भारत पत्रिका में रांगेय राघव ने 1941 ई. के बंगाल अकाल पर आधारित ‘अदम्य जीवन’ शीर्षक से रिपोर्ताज लिखा, जिसे बाद में तूफानों के बीच में संकलित किया गया।
अमृतराय ने तूफानों के बीच के संदर्भ में लिखा—
“जहाँ तक मैं जानता हूँ रांगेय राघव के उन्हीं रिपोर्ताजों से हिंदी में लिखने का चलन शुरू हुआ। मैंने और दूसरों ने रिपोर्ताज लिखे, लेकिन जो बात रांगेय राघव के लिखने में थी, वह किसी को नसीब नहीं हुई।”
रांगेय राघव के रिपोर्ताजों में घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव, मानवीय संवेदना और समय की सच्चाई का गहन चित्रण मिलता है।
3. फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ का योगदान
फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ ने विपुल मात्रा में रिपोर्ताज लिखे, हालांकि उनमें से कई अब अनुपलब्ध हैं। उनका पहला रिपोर्ताज ‘विपादप नाच’ 1945 ई. में विश्वामित्र साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ था। उनका अंतिम रिपोर्ताज ‘पटना-जलप्रलय’ 1975 ई. में प्रकाशित हुआ।
उनका प्रसिद्ध संग्रह ‘ऋण जल धन जल’ (1977 ई.) 1966 ई. के बिहार के भयंकर सूखे और 1976 ई. की विनाशकारी बाढ़ का सजीव वर्णन प्रस्तुत करता है।
युद्ध पर उनका सबसे बड़ा रिपोर्ताज ‘नेपाली क्रांति-कथा’ है, जो दिनमान पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसमें 1950 ई. में राणाशाही के खिलाफ नेपाल में हुए सशस्त्र संघर्ष और प्रजातंत्र की स्थापना की कथा दर्ज है।
4. धर्मवीर भारती और युद्ध यात्राएं
धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका के माध्यम से कई चर्चित रिपोर्ताज लिखे। इनमें ‘ब्रम्हापुत्र की मोर्चाबंदी’ और ‘दानव की वृत्ति’ उल्लेखनीय हैं।
1971 ई. के बांग्लादेश युद्ध और भारत-पाक युद्ध पर आधारित रिपोर्ताज संग्रह ‘युद्ध यात्रा’ 1972 ई. में प्रकाशित हुआ।
शिवसागर मिश्र का रिपोर्ताज ‘लड़ेंगे हजार साल’ (1966 ई.) भी 1965 ई. के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें युद्ध की वास्तविकता और सैनिकों का साहस दिखाया गया है।
5. ग्राम्य जीवन और प्राकृतिक आपदाओं पर केंद्रित रिपोर्ताज
विवेकी राय के ‘जुलूस रुका है’ और ‘बाढ़! बाढ़!! बाढ़!!!’ स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन के दुःख-दर्द और संघर्षों की मार्मिक अभिव्यक्ति करते हैं।
मणि मधुकर के रिपोर्ताज संग्रह ‘पिछला पहाड़’ और ‘सूखे सरोवर का भूगोल’ मरुभूमि के जीवन संघर्षों और वहां के मानवीय अनुभवों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं।
6. अन्य महत्वपूर्ण योगदान
- अज्ञेय का संग्रह ‘देश की मिट्टी बुलाती है’ विशेष रूप से उनके रिपोर्ताज ‘जापानी युद्ध बंदियों के साथ’ के लिए प्रसिद्ध है।
- भगवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर माचवे, रामकुमार वर्मा, निर्मल वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, कमलेश्वर, विवेकी राय, अमृतराय आदि ने भी इस विधा को समृद्ध किया।
- अमृतराय के हंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ताज ‘लाल धरती’ में संकलित हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जीवंत करते हैं।
रिपोर्ताज का महत्व
रिपोर्ताज का महत्व इस बात में है कि यह—
- इतिहास का जीवंत दस्तावेज होता है।
- जनजीवन की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है।
- साहित्य और पत्रकारिता के बीच एक सेतु का कार्य करता है।
- पाठक को प्रत्यक्ष अनुभव की अनुभूति कराता है।
यह न केवल तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन करता है, बल्कि समाज की धड़कनों और समय की नब्ज़ को भी पकड़ता है।
निष्कर्ष
रिपोर्ताज हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है, जिसमें पत्रकारिता की तथ्यात्मकता और साहित्य की भावुकता का अनूठा संगम होता है। यह केवल घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि उन घटनाओं में निहित मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक संदर्भों को भी उजागर करता है।
द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर आज तक, रिपोर्ताज ने अनेक ऐतिहासिक क्षणों को अमर कर दिया है। इलिया एहरेनवर्ग से लेकर फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ और निर्मल वर्मा जैसे लेखकों तक, इस विधा ने साहित्य और समाज दोनों को गहराई से प्रभावित किया है।
आज के समय में, जब मीडिया के रूप बदल रहे हैं, रिपोर्ताज का महत्व और भी बढ़ गया है। यह हमें याद दिलाता है कि घटनाओं का यथार्थ केवल तथ्यों में नहीं, बल्कि मानवीय अनुभवों में भी निहित होता है।
इन्हें भी देखें –
- रिपोर्ताज – अर्थ, स्वरूप, शैली, इतिहास और उदाहरण
- हिन्दी के यात्रा-वृत्त और यात्रा-वृत्तान्तकार – लेखक और रचनाएँ
- यात्रा-वृत्त : परिभाषा, इतिहास, विशेषताएँ और विकास
- हिंदी डायरी साहित्य और लेखक
- डायरी – परिभाषा, महत्व, लेखन विधि, अंतर और साहित्यिक उदाहरण
- छायावादोत्तर युग (शुक्लोत्तर युग: 1936–1947 ई.) | कवि और उनकी रचनाएँ
- मुक्तक काव्य: अर्थ, परिभाषा, भेद, प्रकार, उदाहरण एवं विशेषताएं
- नवगीत: नए गीत का नामकरण, विकास, प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाएं
- प्रगतिवाद (1936–1956): उद्भव, कवि, विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ | प्रगतिवादी काव्यधारा
- प्रयोगवाद (1943–1953): उद्भव, कवि, विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ | प्रयोगवादी काव्य धारा
- हिंदी निबंध का विकास : एक ऐतिहासिक परिदृश्य
- हिन्दी निबंध साहित्य: परिभाषा, स्वरूप, विकास, विशेषताएं, भेद और उदाहरण