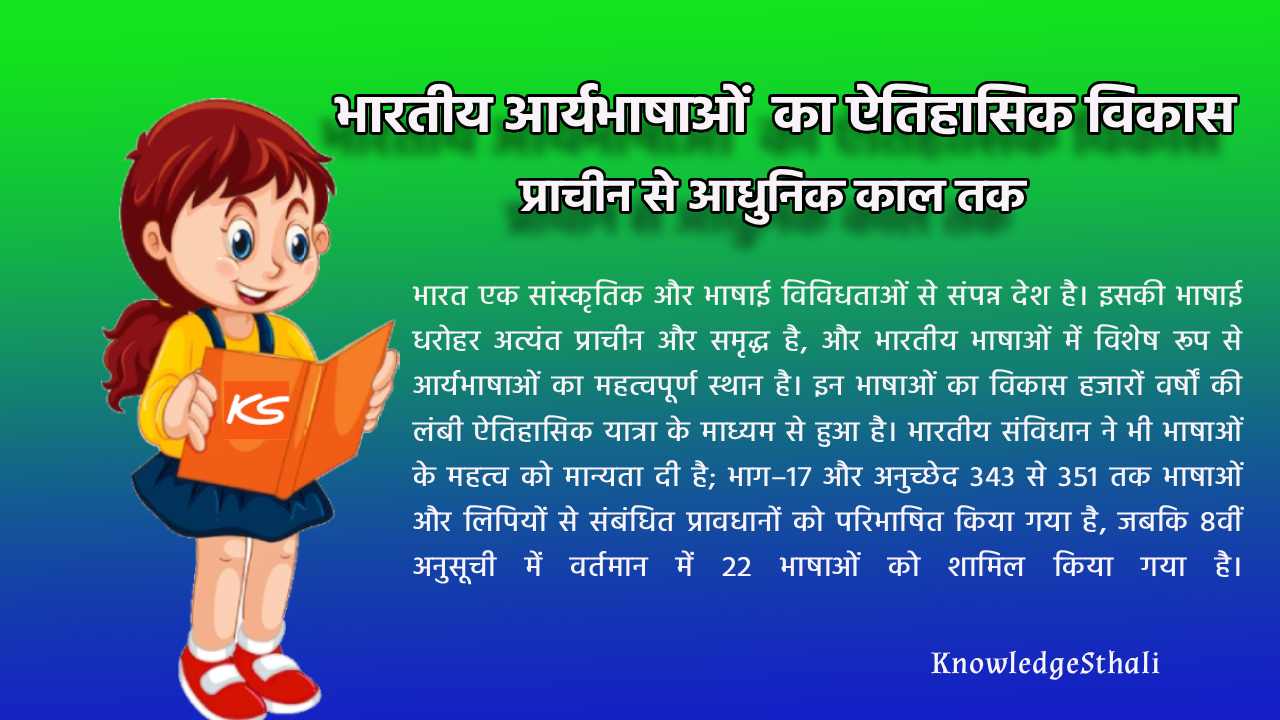भारत एक सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं से संपन्न देश है। इसकी भाषाई धरोहर अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है, और भारतीय भाषाओं में विशेष रूप से आर्यभाषाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इन भाषाओं का विकास हजारों वर्षों की लंबी ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से हुआ है। भारतीय संविधान ने भी भाषाओं के महत्व को मान्यता दी है; भाग–17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं और लिपियों से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित किया गया है, जबकि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है।
इस लेख में प्राचीन भारतीय आर्यभाषा से लेकर आधुनिक भारतीय आर्यभाषा तक की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाओं की विशेषताएँ, ध्वनियाँ और साहित्यिक योगदान समझाया गया है। मध्यकालीन आर्यभाषाओं—पालि, प्राकृत और अपभ्रंश—की उत्पत्ति, विकास और साहित्यिक-सांस्कृतिक महत्व को भी रेखांकित किया गया है। आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण और प्रमुख भाषाएँ जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमी, उड़िया और सिन्धी, उनकी बोलियाँ और लिपियाँ विस्तार से वर्णित हैं। यह लेख छात्रों, शोधार्थियों और भाषाविज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए भारतीय आर्यभाषाओं की संपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा को समझने का एक सम्पूर्ण अवसर प्रदान करता है।
भारत की संवैधानिक भाषाएं
भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ये हैं:
कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिन्दी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली।
हिन्दी को संविधान ने भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। साथ ही, अंग्रेज़ी को भी केन्द्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत की कोई “राष्ट्रभाषा” नहीं है, क्योंकि संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है।
इस भाषाई संरचना से स्पष्ट होता है कि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है जहाँ विभिन्न भाषाएं समानांतर रूप से अस्तित्व में रहकर एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं।
भारतीय भाषाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतीय भाषाओं का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। विशेष रूप से भारतीय आर्य भाषाएं भारत के भाषाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
आर्यों का आगमन और भाषाई प्रभाव
सामान्यतः यह माना जाता है कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच आर्यों का आगमन भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ। वे प्रारंभ में पंजाब और सप्त-सिंधु क्षेत्र में बस गए। धीरे-धीरे उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ते हुए मध्यदेश, काशी, कोशल, मगध, विदेह, अंग, बंगाल और कामरूप तक अपना प्रभाव स्थापित किया।
आर्यों की विजय केवल राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि वे अपने साथ एक विकसित भाषा और यज्ञ-परायण संस्कृति भी लेकर आए थे। आर्यों की भाषा ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया।
अनार्य जातियों का प्रभाव
भारत पहले से ही एक समृद्ध सभ्यता का केंद्र था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि आर्यों के आगमन से पहले सिन्धु घाटी सभ्यता अत्यधिक विकसित थी। इसलिए जब आर्य यहाँ आए तो उनकी भाषा और संस्कृति पर स्थानीय अनार्य जातियों का भी प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत तक में अनार्य तत्वों की उपस्थिति देखी जा सकती है।
भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण
भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम के आधार पर चार मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है।
- प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (2000 ई.पू. से 500 ई.पू. तक)
- वैदिक संस्कृत (2000 ई.पू. से 800 ई.पू. तक)
- संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत (800 ई.पू. से 500 ई.पू. तक)
- मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा (500 ई.पू. से 1000 ई. तक)
- पालि (500 ई.पू. से 1 ई. तक)
- प्राकृत (1 ई. से 500 ई. तक)
- अपभ्रंश (500 ई. से 1000 ई. तक)
- आधुनिक भारतीय आर्यभाषा(1000 ई. से अब तक)
1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (2000 ई.पू. – 500 ई.पू.)
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को अध्ययन की दृष्टि से दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है—
- वैदिक संस्कृत (2000 ई.पू. – 800 ई.पू. तक)
- संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत (800 ई.पू. – 500 ई.पू. तक)
(क) वैदिक संस्कृत (2000 ई.पू. – 800 ई.पू.)
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का सबसे प्राचीन स्वरूप वैदिक संस्कृत है। वैदिक साहित्य का सृजन इसी भाषा में हुआ। इसे वैदिकी, वैदिक, छन्दस् अथवा छान्दस् भी कहा जाता है।
वैदिक साहित्य को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है—
- संहिता
- ब्राह्मण
- उपनिषद्
भाषाविज्ञान के दृष्टिकोण से, विद्वानों में वैदिक ध्वनियों की संख्या को लेकर मतभेद है।
- डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. उदय नारायण तिवारी और डॉ. कपिल देव द्विवेदी जैसे विद्वानों के अनुसार वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ थीं— जिनमें 13 स्वर और 39 व्यंजन सम्मिलित हैं।
- वहीं डॉ. हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है।
(ख) लौकिक संस्कृत (संस्कृत) (800 ई.पू. – 500 ई.पू.)
लौकिक संस्कृत ‘प्राचीन भारतीय आर्य भाषा’ का वह रूप है जिसका विस्तार और विवेचन पाणिनि की प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ ‘अष्टाध्यायी’ में मिलता है। इसे शास्त्रीय संस्कृत भी कहा जाता है।
वैदिक संस्कृत से भिन्न, लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कम हो गई।
- वैदिक संस्कृत की 52 ध्वनियों में से 4 ध्वनियाँ— ळ, ळह, जिह्वमूलीय और उपध्मानीय —लुप्त हो गईं।
- परिणामस्वरूप, लौकिक संस्कृत में कुल 48 ध्वनियाँ शेष रह गईं।
इस प्रकार, लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा मानी जाती है, जिसने आगे चलकर भारतीय साहित्य, दर्शन और काव्य परंपरा को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं।
2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा (500 ई.पू. – 1000 ई.)
मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का कालखंड 500 ई.पू. से 1000 ई. तक माना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इसे तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है—
- पाली (500 ई.पू. से 1 ई. तक)
- प्राकृत (1 ई. से 500 ई. तक)
- अपभ्रंश (500 ई. से 1000 ई. तक)
(क) पाली (500 ई.पू. – 1 ई.)
‘पाली’ शब्द का अर्थ है ‘बुद्ध वचन’। इस कारण यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली भाषा में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई।
त्रिपिटक तीन प्रकार के हैं—
- सुत्त पिटक
- विनय पिटक
- अभिधम्म पिटक
सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र त्रिपिटक ग्रंथों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु श्रीलंका गए। वहाँ के राजा वट्टगामनी (ई.पू. 291) के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक (बुद्ध के उपदेशों का संकलन) लिपिबद्ध किया गया। इस प्रकार पाली भाषा भारत की प्रथम देशभाषा कही जाती है।
(ख) प्राकृत (1 ई. – 500 ई.)
प्राकृत मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का महत्वपूर्ण चरण है। इसकी व्युत्पत्ति और स्वरूप को लेकर दो प्रमुख मत प्रचलित हैं—
- प्राचीन जनभाषा मत
नमि साधु के अनुसार—
“प्राक् पूर्व कृतं प्राकृत”
अर्थात् जो भाषा मूल से चली आ रही है, वही प्राकृत है। - प्राकृतिक भाषा मत
नमि साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है—
“प्राकृतेति सकल-जगज्जन्तूनां व्याकरणादि मिरनाहत संस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृति: प्रकृति तत्र भवः सेव वा प्राकृतम्।”
अर्थात् प्राकृत वह सहज वाणी है जो व्याकरणीय संस्कारों से रहित होकर जनसामान्य की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है।
वाक्पतिराज ने प्राकृत की सार्वभौमिकता को रेखांकित करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वही से निकलता है, उसी प्रकार सभी भाषाएं प्राकृत में प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं।
इस प्रकार प्राकृत संस्कृत से निकट होते हुए भी अधिक लोकाभिमुख और सरल भाषा थी, जिसने जैन आगम साहित्य और अनेक नाटकों में प्रमुख स्थान पाया।
(ग) अपभ्रंश (500 ई. – 1000 ई.)
अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के बीच की संधिकालीन भाषा है।
- व्याडि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को ‘अपभ्रंश’ कहा।
- भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम् में लिखा है—
“शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षते।
तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम्॥”
पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ‘अपभ्रंश’ का प्रयोग ‘अपशब्द’ के समानार्थी रूप में किया है। वहीं भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में भी ‘अपभ्रंश’ का उल्लेख ‘विभ्रष्ट’ नाम से मिलता है।
भाषा के अर्थ में ‘अपभ्रंश’ शब्द का प्रथम प्रामाणिक प्रयोग चण्ड (6वीं शताब्दी) ने अपने प्राकृत-लक्षण ग्रंथ में किया।
रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार, अपभ्रंश शब्द का उपयोग सबसे पहले बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जहाँ उनके पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि कहा गया है।
भामह ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा माना—
“संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा।”
दण्डी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र—इन चार वर्गों में विभाजित किया और अपभ्रंश को ‘आभीर’ भी कहा।
विद्वानों ने अपभ्रंश को समय-समय पर विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पटमंजरी, अवहत्थ, औहट आदि नामों से भी संबोधित किया है।
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे ‘ण–ण भाषा’ की संज्ञा दी।
इस प्रकार, मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का विकास क्रम पाली से प्राकृत और फिर अपभ्रंश तक पहुँचा। पाली ने धार्मिक ग्रंथों को भाषा दी, प्राकृत ने लोकजीवन और साहित्य को अभिव्यक्ति दी, जबकि अपभ्रंश ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं (जैसे हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि) के निर्माण की नींव रखी।
3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा (1000 ई. – अब तक)
आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का कालखंड 1000 ई. से अब तक माना जाता है। इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्यभाषा से अभिप्राय स्वतंत्रता-पूर्व अविभाजित भारत से है, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। कुछ विद्वानों ने इसमें श्रीलंका और वर्मा (म्यांमार) को भी सम्मिलित माना है, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पूर्व ये सभी क्षेत्र भारत का ही अंग थे।
(क) आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण
- डॉ. ए. एफ. आर. हार्नले (1880 ई.)
- पूर्वी गौडियन – पूर्वी हिन्दी, बंगला, असमी, उड़िया।
- पश्चिमी गौडियन – पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, सिन्धी, पंजाबी।
- उत्तरी गौडियन – गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी।
- दक्षिणी गौडियन – मराठी।
- डॉ. जॉर्ज ग्रियर्सन (1920) – लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया
- बाहरी उपशाखा –
(i) उत्तरी-पश्चिमी समुदाय – लहँदा, सिन्धी।
(ii) दक्षिणी समुदाय – मराठी।
(iii) पूर्वी समुदाय – उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। - मध्य उपशाखा – पूर्वी हिन्दी।
- भीतरी उपशाखा –
(i) केन्द्रीय समुदाय – पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी, राजस्थानी।
(ii) पहाड़ी समुदाय – नेपाली, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी।
- बाहरी उपशाखा –
- डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी – ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक आधार पर
- उदीच्य – सिन्धी, लहँदा, पंजाबी।
- प्रतीच्य – राजस्थानी, गुजराती।
- मध्यदेशीय – पश्चिमी हिन्दी।
- प्राच्य – पूर्वी हिन्दी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला।
- दक्षिणात्य – मराठी।
- डॉ. धीरेन्द्र वर्मा – संशोधित वर्गीकरण
- उदीच्य – सिन्धी, लहँदा, पंजाबी।
- प्रतीच्य – गुजराती।
- मध्यदेशीय – राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी।
- प्राच्य – उड़िया, असमिया, बंगला।
- दक्षिणात्य – मराठी।
- सीताराम चतुर्वेदी – संबंधसूचक परसर्गों के आधार पर
- का – हिन्दी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी।
- दा – पंजाबी, लहँदा।
- ज – सिन्धी, कच्छी।
- नो – गुजराती।
- एर – बंगाली, उड़िया, असमिया।
- भोलानाथ तिवारी – क्षेत्रीय तथा अपभ्रंश-आधारित वर्गीकरण
- शौरसेनी (मध्यवर्ती) – पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती।
- मागधी (पूर्वीय) – बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया।
- अर्धमागधी (मध्यपूर्वीय) – पूर्वी हिन्दी।
- महाराष्ट्री (दक्षिणी) – मराठी।
- व्राचड-पैशाची (पश्चिमोत्तरी) – सिन्धी, लहँदा, पंजाबी।
(ख) प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ एवं उनकी विशेषताएँ
- सिन्धी भाषा – संस्कृत सिन्धु से व्युत्पन्न। मुख्य बोलियाँ: विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी। लिपि: लंडा; साथ ही गुरुमुखी व फारसी लिपि।
- लहँदा भाषा – अर्थ: ‘पश्चिमी’। अन्य नाम: पश्चिमी पंजाबी, हिन्दकी, जटकी, मुल्तानी आदि। लिपि: लंडा (शारदा लिपि की उपशाखा)।
- पंजाबी भाषा – पंजाब (पाँच नदियों का देश) से व्युत्पन्न। लिपि: लंडा → सुधारकर गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी। मुख्य बोलियाँ: माझी, डोगरी, दोआबी, राठी।
- गुजराती भाषा – गुर्जर जाति से सम्बन्धित। लिपि: गुजराती (कैथी से मिलती-जुलती; इसमें शिरोरेखा नहीं लगती)।
- मराठी भाषा – महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा। प्रमुख बोलियाँ: कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, माहारी। लिपि: देवनागरी, साथ ही मोडी।
- बंगला भाषा – संस्कृत बंग + आल से निर्मित। यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव। लिपि: बंगला (प्राचीन देवनागरी से विकसित)।
- असमी भाषा – असम प्रदेश की भाषा। मुख्य बोली: विश्नुपुरिया। लिपि: बंगला।
- उड़िया भाषा – उत्कल/ओडिशा की भाषा। मुख्य बोलियाँ: गंजामी, सम्भलपुरी, भत्री। लिपि: ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित।
हिन्दी का उद्भव और विकास
हिन्दी का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है। यद्यपि हिन्दी सीधे संस्कृत से नहीं निकली, लेकिन संस्कृत इसकी मूल आधारभूत भाषा रही है। प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट से होते हुए हिन्दी का आधुनिक स्वरूप सामने आया।
- प्रारंभिक हिन्दी (1000 – 1400 ई.)
अपभ्रंश से अवहट्ट और फिर प्रारंभिक हिन्दी का विकास हुआ। इस काल की भाषा को “अभिनव हिन्दी” भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की रचनाओं में प्रारंभिक हिन्दी की झलक मिलती है। - भक्ति काल (1400 – 1700 ई.)
तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा आदि संत कवियों ने हिन्दी को जनभाषा और लोकभाषा के रूप में स्थापित किया। - रीति काल (1700 – 1900 ई.)
इस काल में हिन्दी में शृंगार, वीरगाथा और रीति-काव्य का विकास हुआ। - आधुनिक हिन्दी (1900 ई. से अब तक)
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलनों में हिन्दी एक सशक्त माध्यम बनी। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकारों ने इसे आधुनिक रूप दिया।
भारतीय भाषाओं में परस्पर प्रभाव
भारत की भाषाएं एक-दूसरे से निरंतर प्रभावित होती रही हैं। संस्कृत ने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं को आधार प्रदान किया। वहीं, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के आगमन से भारतीय भाषाओं में नए शब्द और भाव जुड़े। हिन्दी, उर्दू और अन्य आधुनिक भाषाएं इस सांस्कृतिक मिलन की प्रत्यक्ष गवाह हैं।
भारतीय भाषाओं का वर्तमान स्वरूप
आज भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती हैं। यद्यपि संविधान ने 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी है, फिर भी भारत का भाषाई परिदृश्य इससे कहीं व्यापक है। जनगणना के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या 1200 से अधिक है।
सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, साहित्य और वैश्वीकरण ने भारतीय भाषाओं को नए अवसर और चुनौतियां दी हैं। हिन्दी और अंग्रेज़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद का मुख्य साधन बनी हुई हैं, वहीं अन्य भाषाएं क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त कर रही हैं।
निष्कर्ष
भारत की भाषाएं केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, साहित्य और इतिहास का जीवंत दर्पण हैं। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं तक की यात्रा हमें यह सिखाती है कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील और विकसित होती रहती है।
भारतीय आर्य भाषाओं का क्रमिक विकास यह स्पष्ट करता है कि भारतीय भाषाई परंपरा हजारों वर्षों से निरंतर चल रही है और आज भी जीवंत है। हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाएं आने वाले समय में भी न केवल भारत बल्कि विश्व की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करती रहेंगी।
इन्हें भी देखें –
- भारत की भाषाएँ: संवैधानिक मान्यता, आधिकारिक स्वरूप और विश्व परिप्रेक्ष्य में भाषाई विविधता
- विश्व की भाषाएँ : विविधता, विकास और वैश्विक प्रभाव
- हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह : अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलन्त | परिभाषा, प्रयोग एवं महत्व
- लिपि : परिभाषा, अर्थ, इतिहास, प्रकार, रूपांतरण और उदाहरण
- भाषा और लिपि : उद्भव, विकास, अंतर, समानता और उदाहरण
- हिंदी ध्वनियों (वर्णों) के उच्चारण स्थान, वर्गीकरण एवं विशेषतायें
- ब्राह्मी लिपि से आधुनिक भारतीय लिपियों तक: उद्भव, विकास, शास्त्रीय प्रमाण, अशोक शिलालेख
- क्या अमेरिका के H-1B वीज़ा की तरह है चीन का K-वीज़ा? जानिए किसे मिलेगा
- जियो पेमेंट्स बैंक का “सेविंग्स प्रो”: निष्क्रिय पैसों से ज्यादा कमाई का स्मार्ट तरीका
- एनवीडिया–ओपनएआई सौदा: 100 अरब डॉलर का निवेश और एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषा