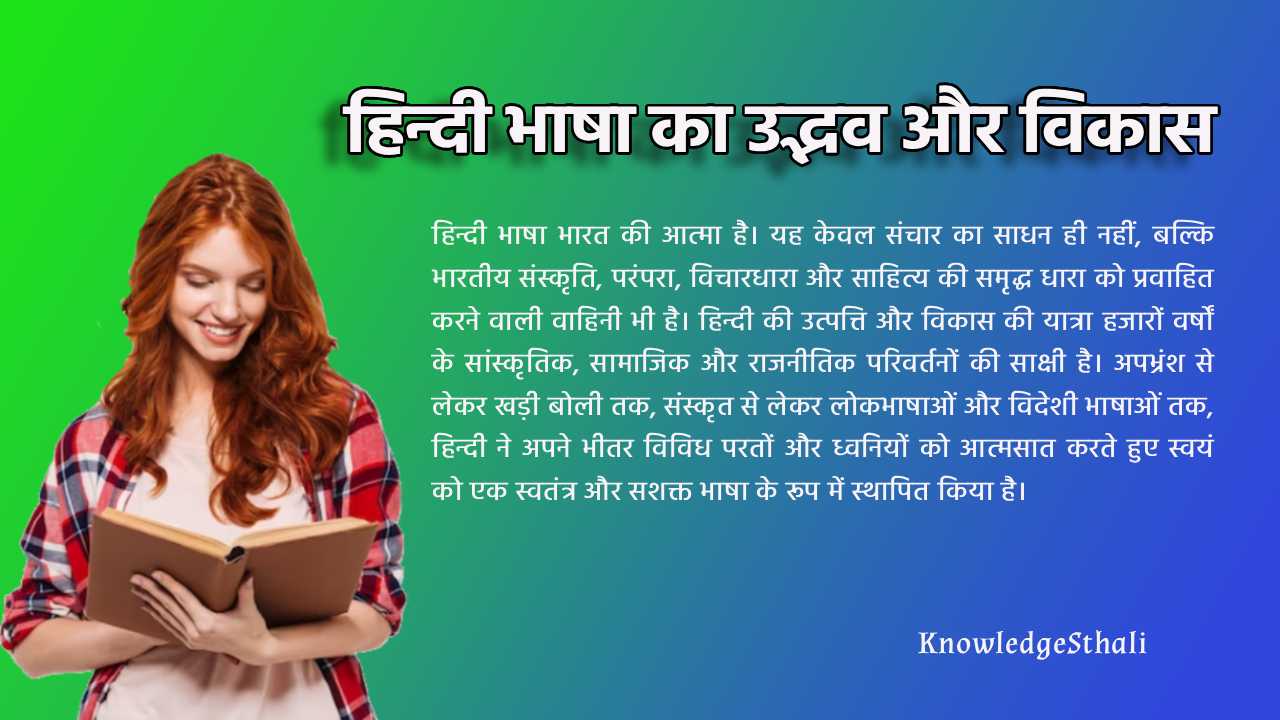हिन्दी भाषा भारत की आत्मा है। यह केवल संचार का साधन ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, विचारधारा और साहित्य की समृद्ध धारा को प्रवाहित करने वाली वाहिनी भी है। हिन्दी की उत्पत्ति और विकास की यात्रा हजारों वर्षों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की साक्षी है। अपभ्रंश से लेकर खड़ी बोली तक, संस्कृत से लेकर लोकभाषाओं और विदेशी भाषाओं तक, हिन्दी ने अपने भीतर विविध परतों और ध्वनियों को आत्मसात करते हुए स्वयं को एक स्वतंत्र और सशक्त भाषा के रूप में स्थापित किया है।
हिन्दी भाषा का उद्भव
हिन्दी की जड़ें संस्कृत भाषा में निहित हैं। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिन्दी की यात्रा हुई। यह यात्रा केवल भाषाई परिवर्तन भर नहीं थी, बल्कि इसमें उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभावों की गहरी छाप भी परिलक्षित होती है।
- संस्कृत से प्राकृत : वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत प्राचीन भारत की विद्या और संस्कृति की भाषा थी। लेकिन समय के साथ बोलचाल की सहजता के लिए प्राकृत भाषाएँ विकसित हुईं।
- प्राकृत से अपभ्रंश : प्राकृत भाषाएँ आगे चलकर अपभ्रंश में परिवर्तित हुईं। यही अपभ्रंश हिन्दी का सीधा पूर्वज माना जाता है।
- अपभ्रंश से हिन्दी : 10वीं शताब्दी तक आते-आते अपभ्रंश का स्वरूप लगभग 40% तक हिन्दी जैसा हो चुका था। 1000 ई. के आसपास हिन्दी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में पहचानी जाने लगी।
भाषा के रूप में ‘हिन्दी’ का प्रयोग
भाषा के संदर्भ में ‘हिन्दी’ शब्द का इतिहास फारस और अरब क्षेत्र से प्रारंभ होता है। ईरान के सम्राट नौशेरवाँ (531–579 ई.) ने अपने दरबारी चिकित्सक बाजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतन्त्र का अनुवाद कराने के लिए नियुक्त किया। बाजरोया ने इसे ‘कलीला व दिमना’ के रूप में अनूदित किया और इसकी भूमिका में यह उल्लेख किया गया कि यह अनुवाद ‘जबाने-हिन्दी’ से किया गया है। यहाँ ‘जबाने-हिन्दी’ शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की प्रमुख भाषाओं—संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश—के लिए हुआ।
फारसी कवि औफी ने 1228 ई. में ‘हिन्दवी’ शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यह केवल मध्यदेशीय स्थानीय भाषाओं के लिए था। इसके बाद 1424 ई. में तैमूरलंग के पोते शरफुद्दीन यज्दी ने अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिन्दी भाषा के अर्थ में ‘हिन्दी’ शब्द का उल्लेख किया।
अमीर खुसरो को भी 13–14वीं शताब्दी में हिन्दी, हिन्दकी या हिन्दुई शब्दों के प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। हालांकि, डॉ. भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार, खुसरो ने ‘हिन्दी’ शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया था, जबकि ‘हिन्दवी’ शब्द स्थानीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त हुआ।
हिन्दी कवि नूर मुहम्मद ने अपनी रचनाओं में लिखा:
“हिन्दू मग पर पाँव न राखौ।
का जो बहुतै हिन्दी भाख्यौ।”
18वीं शताब्दी तक ‘हिन्दी’ मुसलमानों की भाषा से हिन्दुओं की भाषा की ओर बढ़ गई। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह ‘उर्दू’ या ‘रेख्ता’ के पर्याय के रूप में प्रयोग होती रही।
उर्दू शब्द तुर्की मूल का है, जिसका अर्थ है ‘शाही शिविर’। ‘रेख्ता’ शब्द फारसी में ‘गिरा हुआ या व्यवस्थित किया हुआ ढेर’ अर्थ में प्रयोग होता था और 18वीं–19वीं शताब्दी तक उर्दू के लिए प्रयुक्त हुआ।
हिन्दी का आधुनिक अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टिन टेलर ने 1812 ई. में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया।
आज ‘हिन्दी’ मुख्यतः निम्न अर्थों में उपयोग हो रही है:
- भाषाई क्षेत्र : हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार—इस पूरे क्षेत्र को हिन्दी प्रदेश कहा जाता है।
- संविधानिक अर्थ : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा, तथा राष्ट्रभाषा के प्रतीक के रूप में।
इस प्रकार हिन्दी ने समय के साथ क्षेत्रीय और धार्मिक दृष्टि से व्यापक स्वरूप अपनाया और आज भारत की प्रमुख संपर्क भाषा बनकर उभरी है।
हिन्दी भाषा का विकास
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास को तीन प्रमुख कालखंडों में बाँटा जाता है—
इन तीनों कालों में हिन्दी ने ध्वन्यात्मक, व्याकरणिक, रूपगत और साहित्यिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे और अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुँची।
1. आदिकाल (1000 ई. से 1350 ई. तक)
राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि
आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का समय था। देश में सर्वत्र मत्स्यन्याय (बड़े का छोटे पर शासन) की स्थिति बनी हुई थी। संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता के बावजूद इस काल में साहित्यिक चेतना का प्रसार हुआ। भोग और योग का अद्भुत समन्वय यहाँ की रचनाओं में झलकता है।
साहित्यिक परंपरा
इस काल में राजाश्रय और धर्माश्रय के अंतर्गत साहित्य रचा गया। विभिन्न भाषिक स्वरूप जैसे डिंगल, पिंगल, दक्खिनी, अवधी और ब्रज, माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त हुए। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में हिन्दी साहित्य की रचनाएँ सामने आईं।
प्रमुख योगदान
- प्रारम्भिक व्याकरण : इस समय आचार्य हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन या सिद्ध-हेम व्याकरण की रचना की, जो हिन्दी विकास में एक आधारशिला साबित हुआ।
- ध्वन्यात्मक परिवर्तन :
- अपभ्रंश के 8 स्वर (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ) के साथ हिन्दी में ओ और औ का विकास हुआ।
- डु और ढ़ जैसे नए व्यंजन हिन्दी में प्रचलित हुए।
- न्ह, ल्ह, यह जैसे संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र रूप में स्वीकार किए गए।
- व्याकरणिक परिवर्तन :
- सहायक क्रियाओं और उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग प्रारंभ हुआ।
- नपुंसकलिंग शब्दों का लोप होने लगा।
- वाक्य-रचना अपेक्षाकृत स्थिर और निश्चित हो गई।
- शब्दसंपदा :
- संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बढ़ा।
- अरबी, फारसी, तुर्की और पश्तो से कई शब्द हिन्दी में आए।
निष्कर्षतः, आदिकाल हिन्दी की नींव रखने वाला काल था, जिसमें भाषा ने अपभ्रंश से अलग होकर अपना स्वतंत्र स्वरूप ग्रहण करना प्रारंभ किया।
2. मध्यकाल (1350 ई. से 1850 ई. तक)
सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
मध्यकाल हिन्दी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक स्थिरता, शांति और कलात्मक उत्कर्ष ने भाषा के विकास को गति दी। संस्कृत का पाण्डित्य प्रभाव अब भी विद्यमान था, परन्तु संतों और भक्त कवियों ने लोकभाषाओं को साहित्यिक गरिमा प्रदान की।
साहित्यिक परंपरा
- कृष्णभक्ति और रामभक्ति काव्य ने ब्रज और अवधी को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। सूरदास (कृष्णभक्ति) और तुलसीदास (रामभक्ति) ने हिन्दी साहित्य को अभूतपूर्व ऊँचाई दी।
- सूफी संतों, रीतिकालीन कवियों और मुक्तक परंपरा के कवियों ने तद्भव और देशज शब्दों को अपनाकर भाषा को और अधिक समृद्ध बनाया।
भाषिक विकास
- ध्वन्यात्मक परिवर्तन :
- फारसी सम्पर्क के कारण पाँच नई ध्वनियाँ प्रचलित हुईं— क़, ख़, ग़, ज़, फ़।
- शब्दांत में ‘अ’ का उच्चारण समाप्त होने लगा।
- व्याकरणिक विकास :
- हिन्दी का व्याकरणिक स्वरूप स्थिर हो गया।
- वियोगात्मकता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई।
- शब्दसंपदा का विस्तार :
- अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो से लगभग 6000 शब्द हिन्दी में शामिल हुए।
- तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रचलन बढ़ा।
- यूरोपीय भाषाओं (पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रेंच और अंग्रेजी) से अनेक शब्द हिन्दी में शामिल हुए।
निष्कर्षतः, मध्यकाल में हिन्दी भाषा ने अपना साहित्यिक स्वर्णकाल देखा। भक्तिकाव्य और सूफी परंपरा ने इसे जनमानस से जोड़ा और विविध शब्दसंपदा से समृद्ध किया।
3. आधुनिक काल (1850 ई. से आज तक)
सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
आधुनिक काल हिन्दी भाषा का वास्तविक उत्कर्ष काल है। अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के बाद प्रशासनिक दृष्टि से खड़ी बोली को संरक्षण मिला। 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन ने हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई।
साहित्यिक परंपरा
- खड़ी बोली हिन्दी गद्य और पद्य दोनों की भाषा बनी।
- फोर्ट विलियम कॉलेज (कलकत्ता) के अध्यक्ष गिलक्राइस्ट ने हिन्दी गद्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- स्वदेशी आंदोलन (1905) और राष्ट्रवादी आंदोलनों ने हिन्दी को एकजुटता और स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया।
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिन्दी का परिष्कार करके उसे साहित्यिक गरिमा प्रदान की।
- छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और आधुनिक साहित्य ने हिन्दी को विविध आयाम प्रदान किए।
भाषिक विकास
- उर्दू और फारसी के प्रभाव से क़, ख़, ग़, ज़, फ़ वर्ण प्रचलित रहे, परंतु धीरे-धीरे क, ख, ग रूप में प्रयोग होने लगे।
- अंग्रेजी के प्रभाव से नई ध्वनियाँ प्रचलित हुईं :
- ‘ऑ’ (कॉलेज, डॉक्टर)
- संयुक्त व्यंजन ‘ड्र’ (ड्रग, ड्रिप)
- शब्दांत में ‘अ’ का उच्चारण लगभग समाप्त हो गया (राम, श्याम)।
- विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा और प्रशासनिक क्षेत्रों के कारण पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण और समन्वय हुआ।
वर्तमान स्वरूप
आज हिन्दी भाषा के कम-से-कम तीन रूप प्रचलित हैं :
- साहित्यिक हिन्दी – साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त।
- सामान्य हिन्दी –
- शिष्ट समाज की बातचीत की हिन्दी।
- पारिवारिक स्तर की हिन्दी।
- मित्रों के बीच प्रयोग की उन्मुक्त हिन्दी।
- वैज्ञानिक और प्रशासनिक हिन्दी – शासन, विज्ञान, वाणिज्य और तकनीक की भाषा।
हिन्दी भाषा के विविध रूप
मानव जीवन में भाषा अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। कभी हम अपने विचारों को बोलकर सामने वाले तक पहुँचाते हैं और कभी उन्हें लिखकर दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। इस दृष्टि से भाषा के दो प्रमुख रूप माने जाते हैं—
- उच्चारित या मौखिक भाषा
- लिखित भाषा
1. उच्चारित या मौखिक भाषा
मौखिक भाषा वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करता है। इसका उद्भव मानव जीवन के प्रारंभिक काल से ही माना जाता है, क्योंकि जैसे ही मनुष्य ने ध्वनियों का उच्चारण करना सीखा, उसने संवाद की कला भी विकसित कर ली।
इस भाषा का आधार ध्वनि है। ध्वनियों के संयोजन से शब्द बनते हैं और शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि मौखिक भाषा तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार क्षणिक और अस्थायी रूप में सामने आती है। इसका प्रयोग मुख्यतः तब किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने उपस्थित हो।
2. लिखित भाषा
लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा की अपेक्षा बहुत बाद में हुआ। जब मनुष्य को यह आवश्यकता महसूस हुई कि उसके विचार केवल तत्कालीन संवाद तक सीमित न रहें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहें या दूरस्थ व्यक्तियों तक भी पहुँच सकें, तब उसने लिखने की विधि का आविष्कार किया।
इस भाषा का आधार वर्ण हैं, जिन्हें ध्वनियों के प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया। इन वर्णों के लिए विशेष चिह्नों और आकृतियों का प्रयोग किया गया, जिन्हें हम ‘लिपि’ कहते हैं। लिखित भाषा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि यह स्थायी रूप में विचारों को सुरक्षित रखने का साधन है।
मौखिक और लिखित भाषा का संबंध
यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भाषा का मूल स्वरूप मौखिक ही है। लिखित भाषा उसका परिष्कृत और स्थायी विस्तार है। जिन लोगों को पढ़ना-लिखना नहीं आता, वे भी मातृभाषा को सहज रूप से बोलना और समझना सीख जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ निरक्षर लोग भी अनेक भाषाओं को बोल और समझ सकते हैं। इस प्रकार, मौखिक भाषा को भाषा का आदि रूप तथा लिखित भाषा को उसका विकसित स्वरूप माना जा सकता है।
निष्कर्ष
हिन्दी भाषा का इतिहास केवल भाषाई विकास की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा का दस्तावेज है। अपभ्रंश की जड़ों से निकलकर हिन्दी ने आदिकाल में अपनी नींव रखी, मध्यकाल में स्वर्णकाल देखा और आधुनिक काल में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनकर उभरी।
आज हिन्दी न केवल भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। शिक्षा, तकनीक, व्यापार, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में इसका निरंतर विस्तार हो रहा है।
इस प्रकार, हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास भारतीयता की निरंतरता और जीवंतता का प्रतीक है।
इन्हें भी देखें –
- हिंदी भाषा : स्वरूप, इतिहास, संवैधानिक स्थिति और वैश्विक महत्व
- हिन्दी साहित्य – काल विभाजन, वर्गीकरण, नामकरण और इतिहास
- हिंदी साहित्य का मध्यकाल : भक्ति और रीति धाराओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप
- काव्य और कविता : परिभाषा, उदाहरण, अंतर, समानता एवं साहित्यिक महत्व
- हिन्दी साहित्य के 350+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर
- पद्यकाव्य: परिभाषा, विशेषताएँ, प्रकार, उदाहरण और ऐतिहासिक विकास
- लेखक: परिभाषा, प्रकार और प्रमुख साहित्यकार
- वैदिक सभ्यता | वैदिक काल | Vedic Age | 1500ई.पू.-500 ई.पू.
- सूफी और भक्ति आंदोलन | मध्यकालीन भारतीय समाज में सामाजिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण
- भक्ति काल के कवि और उनके काव्य (रचनाएँ)