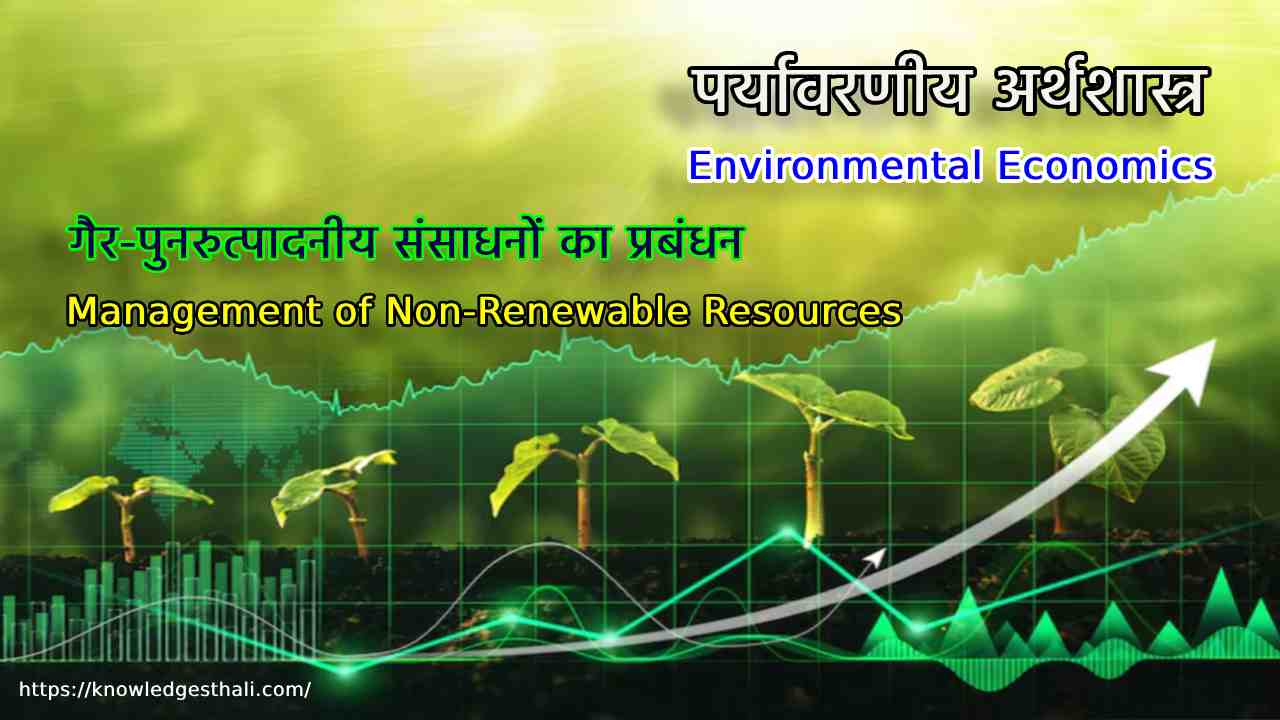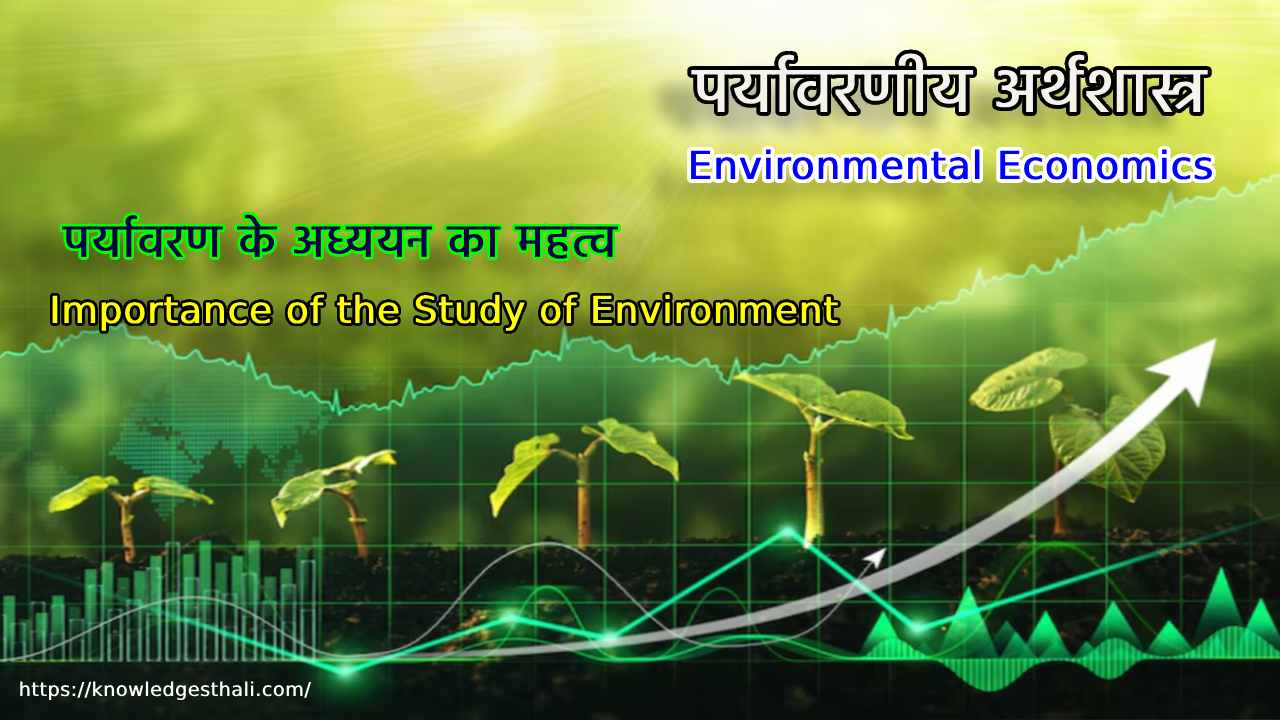पर्यावरणीय अर्थशास्त्र (Environmental Economics) अर्थशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करती है। इसका उद्देश्य सतत विकास (Sustainable Development) को बढ़ावा देना है—जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए आर्थिक वृद्धि संभव हो।
यह विषय प्रकृति और अर्थव्यवस्था के मध्य संतुलन की खोज करता है—जहाँ पारिस्थितिकीय संसाधनों का दोहन इस प्रकार किया जाए कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें।
प्रमुख अध्ययन क्षेत्र:
- पर्यावरणीय संसाधनों का मूल्य निर्धारण
हवा, जल, मिट्टी, जैव विविधता आदि संसाधनों का आर्थिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए—यह पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का मूल प्रश्न है। क्योंकि ये संसाधन प्रायः “सार्वजनिक वस्तुएँ” (Public Goods) होती हैं, जिनका बाज़ार मूल्य नहीं होता। - बाह्यताएँ (Externalities)
जब कोई आर्थिक गतिविधि तीसरे पक्ष पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है (जैसे प्रदूषण), तो उसे बाह्यता कहा जाता है। इसका समाधान पर्यावरणीय कर, सब्सिडी, या बाज़ार आधारित उपायों से किया जाता है। - प्रदूषण नियंत्रण एवं नीति निर्माण
पर्यावरणीय कर (Carbon Tax), उत्सर्जन व्यापार (Emission Trading), पर्यावरणीय नियमों एवं प्रोत्साहनों का आर्थिक विश्लेषण। - प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग
जैसे—भूमि, जल, खनिज, ऊर्जा स्रोतों आदि का संरक्षण इस प्रकार किया जाए कि आर्थिक विकास भी हो और पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहे। - जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सहयोग
पर्यावरणीय अर्थशास्त्र वैश्विक तापवृद्धि, कार्बन उत्सर्जन, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों (जैसे Paris Agreement) की आर्थिक विवेचना करता है।
पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का महत्व
- सतत विकास का आधार
यह सुनिश्चित करता है कि विकास केवल GDP वृद्धि तक सीमित न रह जाए, बल्कि प्राकृतिक पूँजी (Natural Capital) के संरक्षण को भी समाहित करे। - नीति निर्माण में योगदान
पर्यावरणीय अर्थशास्त्र पर आधारित नीतियाँ—जैसे पोल्यूशन टैक्स, ग्रीन सब्सिडी, या कार्बन ट्रेडिंग—सरकारों को प्रभावी और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती हैं। - जलवायु संकट से निपटने का उपाय
जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की क्षति और प्रदूषण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर यह अर्थशास्त्र ठोस ढांचागत रणनीति तैयार करने में सहायक है। - भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विशेष प्रासंगिकता
जहाँ गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ-साथ आवश्यक हैं, वहाँ यह विषय “हरित विकास” (Green Growth) का रास्ता दिखाता है।
पर्यावरणीय अर्थशास्त्र आज के युग की सबसे आवश्यक आर्थिक शाखाओं में से एक है, जो पारिस्थितिकीय और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाकर “हरित और समावेशी विकास” की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। यह न केवल अकादमिक अध्ययन का क्षेत्र है, बल्कि नीतिगत हस्तक्षेप का भी आधार है।