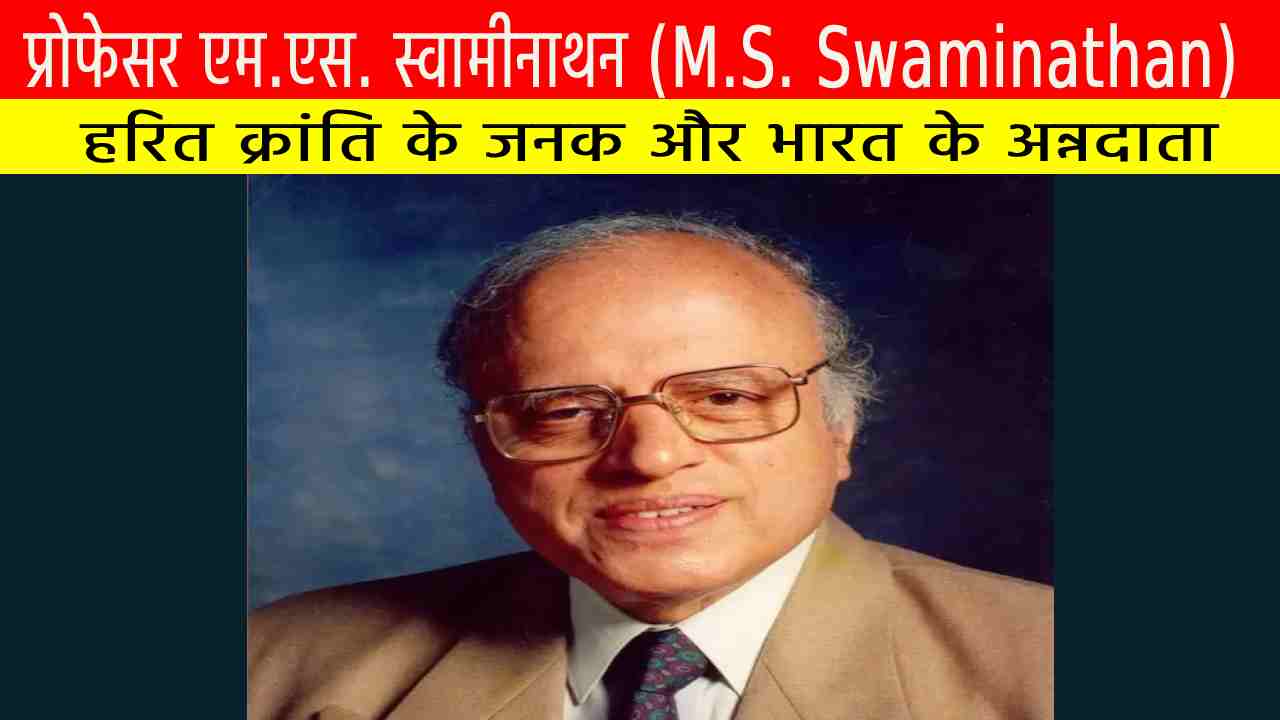भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनकी दूरदृष्टि और कार्यों ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन (M.S. Swaminathan) उन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं। उन्हें अक्सर “भारत की हरित क्रांति के जनक” और “भारत को भोजन देने वाले व्यक्ति” के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 2025 उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है, और यह अवसर हमें उनके असाधारण योगदान, उनकी विरासत और भारत के कृषि भविष्य के लिए उनकी स्थायी शिक्षाओं पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है।
हरित क्रांति से पहले भारत का खाद्य संकट
1943 का बंगाल अकाल: एक काला अध्याय
भारत की कृषि स्थिति 20वीं शताब्दी के मध्य तक अत्यंत दयनीय थी। 1943 का बंगाल अकाल, जिसमें लाखों लोग भुखमरी से मर गए, यह स्पष्ट कर गया था कि खाद्य सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा संभव नहीं है। यह अकाल केवल उत्पादन की कमी का परिणाम नहीं था, बल्कि वितरण की अव्यवस्था और औपनिवेशिक नीतियों का दुष्परिणाम भी था।
1960 का दशक: जहाज से मुँह तक
आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व, भारत की स्थिति यह थी कि वह अमेरिकी गेहूँ आयात पर अत्यधिक निर्भर था। अमेरिकी सहायता कार्यक्रम पब्लिक लॉ 480 (पीएल-480) के तहत गेहूँ आयात कर भारत अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इस स्थिति को ‘जहाज से मुँह तक’ कहा गया।
यह केवल एक आर्थिक संकट नहीं था, बल्कि राजनीतिक दबाव का साधन भी बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने वियतनाम युद्ध के समय भारत पर खाद्यान्न आपूर्ति रोककर दबाव बनाने का प्रयास किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत को विदेशी अनाज पर निर्भर रहने की कीमत अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता से चुकानी पड़ सकती है।
एम.एस. स्वामीनाथन का वैज्ञानिक सफर और शुरुआती असफलताएँ
कृषि में विज्ञान का प्रयोग
एम.एस. स्वामीनाथन का मानना था कि भूख मिटाने का सबसे सशक्त हथियार विज्ञान है। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलों की किस्में तैयार करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए।
उत्परिवर्तन की विफलता
प्रारंभिक वर्षों में स्वामीनाथन ने विकिरण आधारित उत्परिवर्तन (mutation breeding) की तकनीक का प्रयोग कर गेहूँ की पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन ये प्रयोग अपेक्षित सफलता नहीं दे पाए। यह अनुभव उनके लिए एक सबक बना कि वैज्ञानिक नवाचार में असफलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सफलता।
नोरिन 10 और नॉर्मन बोरलॉग से साझेदारी
जापानी बौना गेहूँ: नोरिन 10
1958 में स्वामीनाथन ने जापान की एक बौनी गेहूँ की किस्म नोरिन 10 के बारे में जाना। इसकी विशेषता थी कि इसमें छोटे लेकिन मजबूत डंठल थे, जो भारी दानों का भार उठा सकते थे।
नॉर्मन बोरलॉग से संपर्क
इसी समय मैक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग उच्च उपज वाली गेहूँ की किस्में विकसित कर रहे थे। स्वामीनाथन ने बोरलॉग से संपर्क साधा और उन्हें भारत आने के लिए प्रेरित किया।
बोरलॉग शुरू में अनिच्छुक थे क्योंकि उन्हें संदेह था कि भारत जैसी उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये बीज सफल नहीं होंगे। लेकिन स्वामीनाथन ने उन्हें विश्वास दिलाया। अंततः 1963 में बोरलॉग भारत आए और स्वामीनाथन के नेतृत्व में क्षेत्रीय परीक्षण शुरू हुए।
हरित क्रांति का प्रारंभ और राजनीतिक समर्थन
बीज आयात का ऐतिहासिक निर्णय
1966 में भारत ने मैक्सिको से 18,000 टन गेहूँ के बीज आयात किए। यह विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा बीज आयात था। उस समय इस निर्णय पर कई सवाल उठे। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और वामपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक गुटों ने इसे जोखिम भरा कदम कहा। लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम ने स्वामीनाथन का साथ दिया।
राजनीतिक इच्छाशक्ति और वैज्ञानिक नेतृत्व
लाल बहादुर शास्त्री स्वयं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के खेतों में पहुँचे और बीज परीक्षणों का अवलोकन किया। उनके समर्थन ने नौकरशाही अड़चनों को दूर किया और कार्यक्रम को गति दी।
हरित क्रांति की सफलता
अभूतपूर्व उत्पादन वृद्धि
1968 तक भारत ने गेहूँ की रिकॉर्ड पैदावार हासिल की। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन ने नए कीर्तिमान बनाए। कुछ ही वर्षों में भारत खाद्यान्न संकट से बाहर आ गया और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा।
भुखमरी से मुक्ति
जहाँ कभी भारत में भुखमरी और अकाल का डर था, वहीं 1970 के दशक तक खाद्यान्न उत्पादन इतना बढ़ गया कि भंडारण और वितरण एक नई चुनौती बन गया। करोड़ों लोग भुखमरी से बाहर आए।
अंतरराष्ट्रीय मान्यता
एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों ने भारत को दुनिया में कृषि क्रांति का उदाहरण बना दिया। यही कारण है कि बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार मिला और स्वामीनाथन को विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया।
स्वामीनाथन की दूरदृष्टि: स्थायी हरित क्रांति
स्वामीनाथन केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने समय रहते चेतावनी दी थी कि:
- अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी को नुकसान पहुँचा सकता है।
- भूजल का अंधाधुंध दोहन जल संकट को जन्म देगा।
- एक ही फसल पर अत्यधिक निर्भरता पारिस्थितिकी को असंतुलित करेगी।
उनका मानना था कि “हरित क्रांति को स्थायी बनाना होगा”। उन्होंने जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और किसान-केंद्रित कृषि अनुसंधान पर जोर दिया।
स्वामीनाथन की विरासत और शिक्षा
1. विज्ञान और राजनीति का सहयोग
हरित क्रांति ने दिखाया कि वैज्ञानिक अनुसंधान तभी सफल हो सकता है जब उसे राजनीतिक नेतृत्व का समर्थन मिले।
उदाहरण: शास्त्री जी ने नौकरशाही की आपत्तियों को दरकिनार कर बीज आयात का समर्थन किया।
2. जोखिम लेने का साहस
1960 के दशक में विदेशी बीज आयात करना एक बड़ा जोखिम था। 5 करोड़ रुपये मूल्य के बीज आयात का निर्णय अगर असफल होता तो यह सरकार की भारी आलोचना का कारण बनता। लेकिन यह कदम ऐतिहासिक सफलता बना।
3. वैज्ञानिक स्वायत्तता और संस्थागत मजबूती
स्वामीनाथन हमेशा वैज्ञानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के पक्षधर रहे। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया के शीर्ष 10 कृषि अनुसंधान संस्थानों में 8 चीन में हैं और भारत का कोई भी शीर्ष 200 में नहीं है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें उनकी शिक्षाओं से सीखने की आवश्यकता है।
भारत अपने कृषि जीडीपी का केवल 0.43% अनुसंधान एवं विकास में निवेश करता है, जबकि चीन इसका लगभग दोगुना करता है। यह अंतर हमें बताता है कि भविष्य में सफल होने के लिए मजबूत संस्थान और वैज्ञानिक स्वतंत्रता अनिवार्य हैं।
भविष्य के लिए सीख
- स्थायी कृषि मॉडल अपनाना होगा – रासायनिक खेती की जगह जैविक और मिश्रित खेती को बढ़ावा देना होगा।
- जल संरक्षण को प्राथमिकता – स्वामीनाथन का मानना था कि पानी ही कृषि का जीवन है। भविष्य की कृषि नीतियों में जल प्रबंधन सबसे अहम होना चाहिए।
- किसान-केंद्रित अनुसंधान – अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि किसानों की समस्याओं और जरूरतों पर केंद्रित होना चाहिए।
- संस्थागत सुधार – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा।
- युवाओं को कृषि में आकर्षित करना – स्वामीनाथन ने कहा था, “अगर हम कृषि को लाभकारी और नवाचारपूर्ण नहीं बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी इसमें नहीं आएगी।”
निष्कर्ष
एम.एस. स्वामीनाथन केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी राष्ट्रनिर्माता थे। उन्होंने भारत को खाद्यान्न संकट से उबारकर आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल उत्पादन वृद्धि पर ही नहीं, बल्कि स्थायित्व और पर्यावरणीय संतुलन पर भी ध्यान दिया।
उनकी जन्म शताब्दी पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएँगे—ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करेंगे जो उत्पादक, स्थायी, किसान-केंद्रित और पर्यावरण के अनुकूल हो।
एम.एस. स्वामीनाथन सचमुच वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को भोजन दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।
इन्हें भी देखें –
- विश्व मानवतावादी दिवस 2025: इतिहास, महत्व और वैश्विक एकजुटता का संदेश
- श्रीलंका में भारतीय सिनेमा महोत्सव: सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव
- चीन में शुरू हुआ ‘रोबोटों का ओलंपिक’: भविष्य की झलक दिखाते 16 देशों की 280 टीमें
- मनिका विश्वकर्मा बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025
- पुतिन–ट्रंप अलास्का शिखर सम्मेलन : शांति की उम्मीदों के बीच अधूरा समझौता