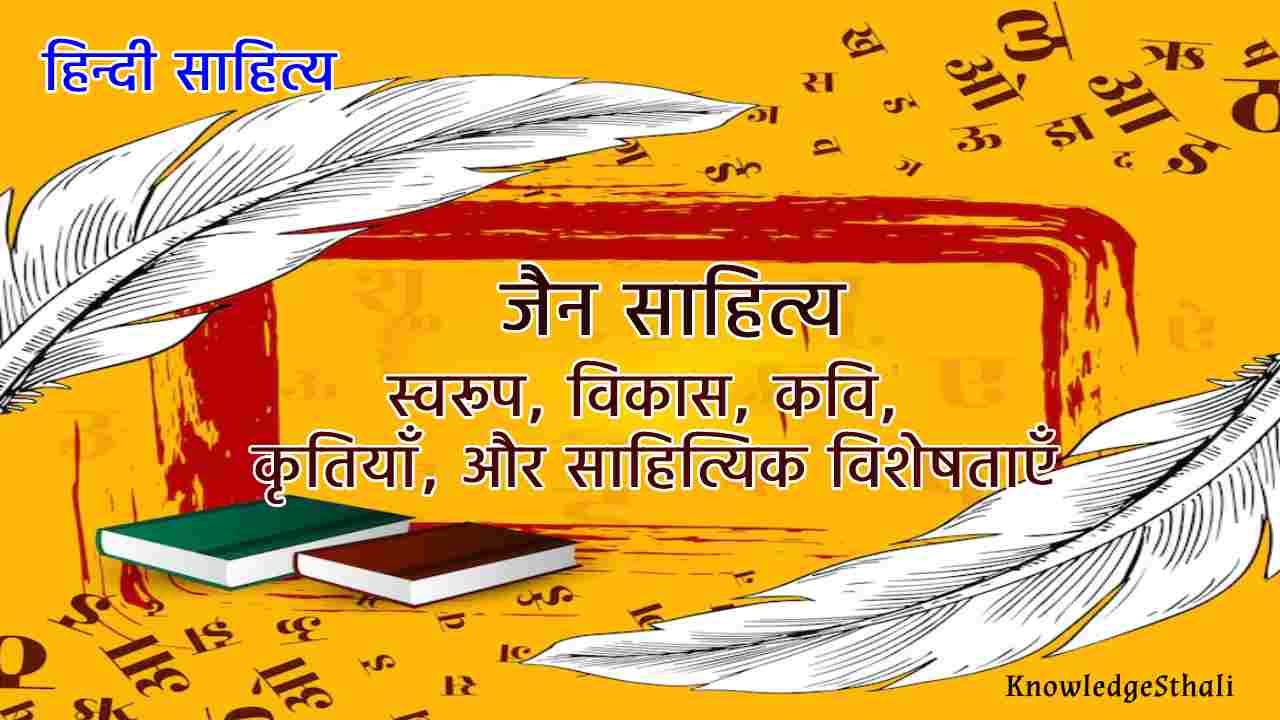भारतवर्ष की धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा में जैन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैन धर्म न केवल एक आध्यात्मिक मार्ग है, अपितु एक विशिष्ट साहित्यिक परंपरा का वाहक भी रहा है। जैन साहित्य, जो विविध भाषाओं और शैलियों में रचा गया, धर्म, दर्शन, नैतिकता और इतिहास की अनमोल धरोहर बन चुका है। इस लेख में हम जैन साहित्य के विविध पहलुओं—आगम, प्रकीर्ण, छेदसूत्र, पुराण, आचार-मीमांसा, टीकाएँ और आधुनिक योगदान—का विस्तृत अध्ययन करेंगे।
जैन साहित्य का परिचय
आमतौर पर अपभ्रंश साहित्य को जैन साहित्य कहा जाता है, क्योंकि इस साहित्य की रचना में जैन आचार्यों की प्रमुख भूमिका रही है। यह साहित्य धर्म और साहित्य का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत करता है — जहाँ धर्म उपदेश और जीवन दर्शन को काव्यात्मक शैली में पिरोया गया है। जैन कवि जब साहित्य निर्माण करते हैं तो उनकी रचनाएं सरस और कलात्मक हो जाती हैं, और जब वे उपदेशक रूप में आते हैं, तो रचनाएं धर्मोपदेशात्मक स्वरूप ले लेती हैं। इन उपदेशों में भी भारतीय जनजीवन की सामाजिक और सांस्कृतिक छवियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं।
जैन साहित्य की मूल प्रकृति और भाषा
जैन साहित्य को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इसे धर्म और साहित्य का मणिकांचन संयोग कहा जाता है। जैन कवि जब साहित्य रचते हैं तो उसमें काव्य सौंदर्य एवं गूढ़ उपदेशों का अद्भुत समन्वय होता है। जब वे उपदेश प्रधान भावभूमि पर उतरते हैं तो उनका काव्य रूपांतरण पद्यबद्ध धर्मोपदेश का रूप ले लेता है, जिसमें जनजीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का भी प्रतिफलन होता है।
जैन साहित्य मूलतः प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओं में रचा गया है। विशेष रूप से अपभ्रंश साहित्य को जैन साहित्य कहा जाता है क्योंकि इसके प्रमुख रचयिता जैन आचार्य ही थे। आचार्यों ने धर्मोपदेशों के माध्यम से ही साहित्यिक कृतियों का सृजन किया।
जैन आगम साहित्य
जैन धर्म के मूल सिद्धांत भगवान महावीर के उपदेशों में निहित हैं, जिन्हें आगम कहा जाता है। आगमों की रचना अर्धमागधी प्राकृत भाषा में हुई, और इन्हें 12 अंगों में संकलित किया गया है जिन्हें द्वादशांग आगम कहा जाता है।
द्वादशांग आगमों की सूची:
- आचरांग सूत्र
- सूर्यकडंक
- थानांग
- समवायांग
- भगवती सूत्र
- न्यायदम्मकहाओ
- उवासगदसाओं
- अंतगडदसाओ
- अणुत्तरोववाइयदसाओं
- पण्हावागरणिआई
- विवागसुयं
- द्विट्ठिवाय
इन ग्रंथों में विशेष रूप से आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार-विचारों का विवरण मिलता है और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन एवं शिक्षाओं की व्यापक झलक है।
इन प्रमुख आगमों के साथ-साथ जैन धर्म में निम्नलिखित ग्रंथ भी महत्त्वपूर्ण हैं:
- 10 प्रकीर्ण
- 6 छेदसूत्र
- 1 नंदि सूत्र
- 1 अनुयोगद्वार
- 4 मूलसूत्र
10 प्रकीर्ण ग्रंथ:
- चतुःशरण
- आतुर प्रत्याख्यान
- भक्तिपरीज्ञा
- संस्तार
- तांदुलवैतालिक
- चंद्रवेध्यक
- गणितविद्या
- देवेन्द्रस्तव
- वीरस्तव
- महाप्रत्याख्यान
6 छेदसूत्र:
- निशीथ
- महानिशीथ
- व्यवहार
- आचारदशा
- कल्प
- पंचकल्प
नंदि सूत्र एवं अनुयोगद्वार जैन अनुयायियों के लिए स्वतंत्र ग्रंथ और विश्वकोष की भूमिका निभाते हैं।
जैन पुराण साहित्य
जैन साहित्य में पुराण ग्रंथों को विशेष स्थान प्राप्त है। इन्हें चरित भी कहा जाता है और ये तीन भाषाओं—प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश—में लिखे गए हैं। ये न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा देते हैं, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी प्रदान करते हैं।
प्रमुख जैन पुराण ग्रंथ:
- पद्मपुराण
- हरिवंशपुराण
- आदिपुराण
- कालिकापुराण
- भद्रबाहुचरित
- परिशिष्ट पर्व
- आवश्यक सूत्र
- आचारांग सूत्र
- भगवती सूत्र
इन ग्रंथों की रचना 6वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। इनका उद्देश्य महापुरुषों के जीवन की घटनाओं के साथ-साथ उनके नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आदर्शों को प्रस्तुत करना होता है।
पुराण और इतिहास में अंतर
भारतीय धर्मग्रंथों में पुराण और इतिहास दो अलग-अलग विधाएँ हैं। इतिहास जहां मात्र घटनाओं के क्रम को प्रस्तुत करता है, वहीं पुराण उन घटनाओं के नैतिक परिणामों और धार्मिक संदेशों पर भी प्रकाश डालता है।
पुराण के पंचलक्षण:
- सर्ग
- प्रतिसर्ग
- वंश
- मन्वंतर
- वंशानुचरित
उपरोक्त लक्षणों के आधार पर पुराण ग्रंथ न केवल घटनाओं का वर्णन करते हैं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र-निर्माण के लिए नैतिक शिक्षाएँ भी प्रदान करते हैं।
जैन आचार-मीमांसा
जैन धर्म में श्रावक (गृहस्थ) और श्रमण (मुनि) के दो मार्ग हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए पहले श्रावकाचार अपनाना आवश्यक होता है। इसमें भोग और त्याग के बीच संतुलन साधते हुए व्यक्ति धीरे-धीरे श्रमण मार्ग की ओर अग्रसर होता है।
श्रावकाचार की भूमिका:
- संयमित जीवन
- धर्म पालन
- आत्मशुद्धि
- त्याग की भावना
जैन टीकाएं और व्याख्यान ग्रंथ
जैन धर्मग्रंथों पर कई महत्वपूर्ण टीकाएं भी लिखी गई हैं, जिनका उद्देश्य उन ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट करना और व्यापक समाज तक उन्हें पहुँचाना था।
प्रमुख टीकाएँ:
- गोम्मट पंजिका – आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोम्मटसार पर संस्कृत टीका। इसमें कुल 98 पत्र और लगभग 5000 श्लोक हैं।
- जीवतत्त्व प्रदीपिका (केशववर्णी की) – कन्नड़ मिश्रित संस्कृत में लिखी गई टीका, जिसमें जीवकाण्ड के रहस्य स्पष्ट किए गए हैं।
- जयधवल टीका – आचार्य वीरसेन और उनके शिष्य जिनसेनाचार्य द्वारा कसायपाहुड़ की व्याख्या। इस ग्रंथ की रचना में 21 वर्ष लगे।
- महापुराण – जिनसेन स्वामी द्वारा रचित, जिनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने इसका शेष भाग पूरा किया। इसमें आदिपुरुषों के चरित्र चित्रण और नैतिक शिक्षाओं का विस्तृत विवरण है।
- जीवतत्त्व प्रदीपिका (नेमिचन्द्रकृत) – यह केशववर्णी की टीका का ही संस्कृत रूपांतरण है जिसे नेमिचन्द्र ज्ञानभूषण के शिष्य, अन्य नेमिचन्द्र ने लिखा था।
आधुनिक युग में जैन साहित्य का योगदान
बीसवीं शताब्दी में जैन साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी ने जैन साहित्य में असाधारण योगदान दिया। उन्होंने न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, सिद्धांत, अध्यात्म, काव्य, पूजन आदि विविध विषयों पर 250 से अधिक पुस्तकें लिखीं जो जम्बूद्वीप-हस्तिनापुर से प्रकाशित हुई हैं।
उनका विशेष योगदान:
- षट्खंडागम पर 16 पुस्तकों की संस्कृत टीका – सिद्धांत चिन्तामणि
- हिन्दी टीका – उनकी शिष्या प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माताजी द्वारा रचित, जिनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
इस तरह से माताजी का कार्य संस्कृत टीका परंपरा को पुनर्जीवित करता है और आज भी समाज को आध्यात्मिक और नैतिक चेतना प्रदान करता है।
जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ
भारतीय साहित्यिक परंपरा में जैन साहित्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल धार्मिक उपदेशों का संग्रह नहीं, बल्कि काव्यात्मक सौंदर्य, दार्शनिक गहराई और समाज-सापेक्ष चिंतन का अनमोल कोष है। जैन धर्म के अनुयायियों ने प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत और बाद में हिंदी में जो रचनाएं प्रस्तुत की हैं, वे भारतीय साहित्य के विकास की दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान हैं।
इस लेख में आगे हम जैन साहित्य की सामान्य विशेषताओं, प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के साथ-साथ जैन साहित्यिक परंपरा के विविध पहलुओं पर समग्र रूप से विचार करेंगे।
जैन साहित्य के निर्माण में अनेक आचार्य, मुनि और कवियों ने अपनी सृजनशील प्रतिभा का योगदान दिया। इनकी रचनाएं उपदेशात्मकता, सामाजिक चेतना, भक्ति और आत्मज्ञान के विविध भावों से परिपूर्ण हैं।
| कवि का नाम | प्रमुख रचनाएँ |
|---|---|
| शालिभद्र सूरि | भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव चरित रास |
| स्थूलिभद्र सूरि | स्थूलिभद्र रास |
| विजयसेन सूरि | रेवन्तगिरि रास |
| सुमति गणि | नेमिनाथ रास |
| आसगु | जीव दया रास, चंदनबाला रास |
| सारमूर्ति | जिनिपद्म सूरि रास |
| उदयवन्त | गौतम स्वामी रास |
| देवसेन | श्रावकाचार |
इन रचनाओं में धार्मिक उपदेशों के साथ-साथ चरित्र-निर्माण की गहराई, करुणा, प्रेम, सत्य, तप और त्याग के आदर्शों का बारीक चित्रण मिलता है।
जैन साहित्य की सामान्य विशेषताएँ
जैन साहित्य को केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित करना अनुचित होगा, क्योंकि इसमें विषय-वस्तु, शैली और भावबोध की अपार विविधता है। इस साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. उपदेश मूलकता
जैन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है – उपदेशात्मकता। इसमें धर्म के प्रचार के लिए चरित नायकों, शलाका पुरुषों, श्रावकों और तपस्वियों की जीवनगाथाओं को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इन कथाओं के माध्यम से जीवन-मूल्य, आत्मसंयम और परोपकार जैसे गुणों का प्रचार किया गया।
2. विषय की विविधता
यद्यपि यह साहित्य धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है, फिर भी इसमें सामाजिक, ऐतिहासिक, लोककथात्मक और पौराणिक विषयों की प्रचुरता है। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों के पात्रों और कथाओं को जैन दृष्टिकोण से पुनः रचा गया है। इससे जैन साहित्य की कल्पनाशीलता और समन्वयी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है।
3. तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का चित्रण
जैन कवि राजाश्रय से मुक्त रहे, इसलिए उनकी रचनाओं में दरबारी चाटुकारिता नहीं मिलती। इन रचनाओं में उस युग की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण मिलता है। उदाहरण स्वरूप, भरतेश्वर बाहुबली रास में वीरता और संयम का अद्भुत संयोजन दिखता है।
4. कर्मकांड और रूढ़ियों का विरोध
जैन कवियों ने मंदिर-पूजा, मूर्तिपूजा, मंत्र-तंत्र, वर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव जैसी रूढ़ियों का विरोध किया है। वे आत्मशुद्धि और चारित्रिक विकास को ही मोक्ष का साधन मानते हैं। उनका विश्वास है कि परमात्मा की प्राप्ति शरीर के भीतर स्थित आत्मा से ही संभव है।
5. आत्मानुभूति की प्रधानता
जैन साहित्य में आत्मा के स्वरूप, अनुभव और परमानंद की विस्तृत चर्चा मिलती है। आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हुए जैन कवियों ने प्रेमभावना के प्रतीक प्रिय-प्रियतम की कल्पना का सहारा लिया है। यह आत्मा की खोज और उसमें लीन होने की साहित्यिक अभिव्यक्ति है।
6. रहस्यवादी विचारधारा का समावेश
कुछ जैन कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद स्पष्ट रूप से झलकता है। योगी रामसिंह, सूतभाचार्य और महानन्दि महचय जैसे कवियों ने अपने रहस्यवादी काव्यों में आत्मा को ही परमेश्वर माना है। उनका विश्वास था कि देहरूपी देवालय में स्थित आत्मा को जागृत कर ही परम समाधि की अवस्था पाई जा सकती है।
7. काव्यरूपों की विविधता
जैन साहित्य काव्यरूपों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख काव्यरूप मिलते हैं:
- रास
- फागु
- छप्पय
- चतुष्पदिका
- गाथा
- प्रबन्ध
- उत्साह
- स्तुति
- गीत
- गुर्वावली
इन विविध काव्यरूपों में जैन कवियों ने न केवल काव्य सौंदर्य को बनाए रखा, बल्कि उन्हें धर्मोपदेशों के प्रचार हेतु भी उपयोग किया।
8. शांत या निर्वेद रस की प्रधानता
यद्यपि जैन साहित्य में करुण, वीर, श्रृंगार जैसे रसों का भी प्रयोग हुआ है, तथापि शांत और निर्वेद रस इस साहित्य का प्रमुख रस बनकर उभरता है। उदाहरणतः –
- नेमिचंद चउपई – करुण रस
- भरतेश्वर बाहुबली रास – वीर रस
- स्थूलिभद्र फागु – श्रृंगार रस
किन्तु अंततः इन रचनाओं में निर्वेद और वैराग्य भाव हावी हो जाते हैं, जो जैन धर्म की मूल भावना को दर्शाते हैं।
9. प्रेम के विविध रूपों का चित्रण
जैन साहित्य में प्रेम के पाँच रूपों का उल्लेख मिलता है:
- विवाह पूर्व प्रेम – करकंडुचरिउ
- विवाहोत्तर प्रेम – पउमासिरिचरिउ
- असामाजिक प्रेम – जहसरचरिउ
- विषम प्रेम – पउमचरिउ (रावण और सीता)
- रोमांटिक प्रेम – अधिकांश काव्य में
इन प्रेम प्रसंगों का प्रयोग मुख्यतः धर्म की महिमा स्थापित करने और मानव चरित्र की परीक्षा के रूप में किया गया है।
10. गीतात्मकता की प्रधानता
जैन कवियों की रचनाओं में गीतात्मकता और गेयता प्रमुख हैं। छंदों का चयन करते समय उन्होंने उसकी लयात्मकता और संगीतबद्धता का विशेष ध्यान रखा। विशेष रूप से पुष्पदंत और स्वयंभू जैसे कवियों ने अपने छंदों में संगीत का अद्भुत पुट दिया है।
11. अलंकार योजना
जैन साहित्य में अर्थालंकारों को प्रमुखता प्राप्त है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, सन्देह आदि का सुंदर प्रयोग हुआ है। शब्दालंकार जैसे श्लेष, यमक और अनुप्रास भी मिलते हैं, परन्तु ये गौण रूप में हैं।
12. छंद विधान की समृद्धता
जैन साहित्य छंदों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। स्वयंभू और हेमचंद्राचार्य द्वारा रचित छंद ग्रंथों – स्वयंभूछंद और छन्दोनुशासन – में विस्तृत छंद विवेचना मिलती है। जैन कवियों ने अनेक छंदों का प्रयोग किया जैसे:
- कड़वक
- पट्पदी
- चतुष्पदी
- दुबई
- अहिल्या
- बिलसिनी
- सोरठा
- रासा
- चउपद्य
इनका प्रयोग रचनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
13. लोकभाषा की प्रतिष्ठा
जैन साधु-संत गाँव-गाँव घूमकर धर्म का प्रचार करते थे। इसीलिए उन्होंने लोकभाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इससे लोकभाषा को न केवल प्रतिष्ठा मिली, बल्कि धर्म का प्रचार-प्रसार भी अधिक प्रभावशाली हुआ।
निष्कर्ष
जैन साहित्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। इसमें धर्म, दर्शन, इतिहास, नैतिकता, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, काव्य और साहित्य के विविध रूपों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता का प्रेरक भी है।
जैन साहित्य ने हजारों वर्षों से मानव समाज को सत्य, अहिंसा, संयम, त्याग और आत्मकल्याण की दिशा में प्रेरित किया है और आज भी इसकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण बनी हुई है। वर्तमान में इस साहित्य का अध्ययन न केवल शोध के लिए आवश्यक है, बल्कि नैतिक मूल्यों के पुनर्जागरण हेतु भी अत्यंत उपयोगी है।
जैन साहित्य एक ऐसा समृद्ध साहित्यिक संसार है, जिसमें धर्म, दर्शन, इतिहास, काव्य और आत्मानुभूति का समावेश मिलता है। इसके रचनाकारों ने न केवल आत्मकल्याण के साधन प्रस्तुत किए बल्कि जनसामान्य को भी सच्चे धर्म, त्याग, संयम और आत्मबोध की दिशा में अग्रसर किया।
यह साहित्य न केवल प्राचीन भारत की सांस्कृतिक समझ को उजागर करता है, बल्कि आज के भौतिकतावादी युग में भी इसका नैतिक और आत्मिक मूल्य बना हुआ है। जैन साहित्य का पुनः अध्ययन और प्रचार आधुनिक समाज में नैतिक पुनर्जागरण का माध्यम बन सकता है।
इन्हें भी देखें –
- रस- परिभाषा, भेद और उदाहरण
- वर्तनी किसे कहते है? उसके नियम और उदहारण
- भक्ति काल के कवि और उनके काव्य (रचनाएँ)
- अष्टछाप के कवि: परिचय, रचनाएँ और ऐतिहासिक महत्व
- सगुण भक्ति काव्य धारा: अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और साहित्यिक विशेषताएँ
- सिद्ध साहित्य: हिन्दी साहित्य का आदिरूप और सामाजिक चेतना का संवाहक
- नाथ संप्रदाय (साहित्य): योग, तंत्र और साधना की भारतीय परंपरा का अनूठा अध्याय
- सगुण भक्ति काव्य धारा: अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और साहित्यिक विशेषताएँ
- प्राकृतिक संसाधनों का तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक होने के आधार पर वर्गीकरण
- इतिहास रचेंगी प्रिया नायर, बनेंगी हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ
- चम्पू साहित्य | गद्य और पद्य का अद्वितीय संगम
- लॉर्ड्स MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण: भारतीय क्रिकेट का ऐतिहासिक गौरव