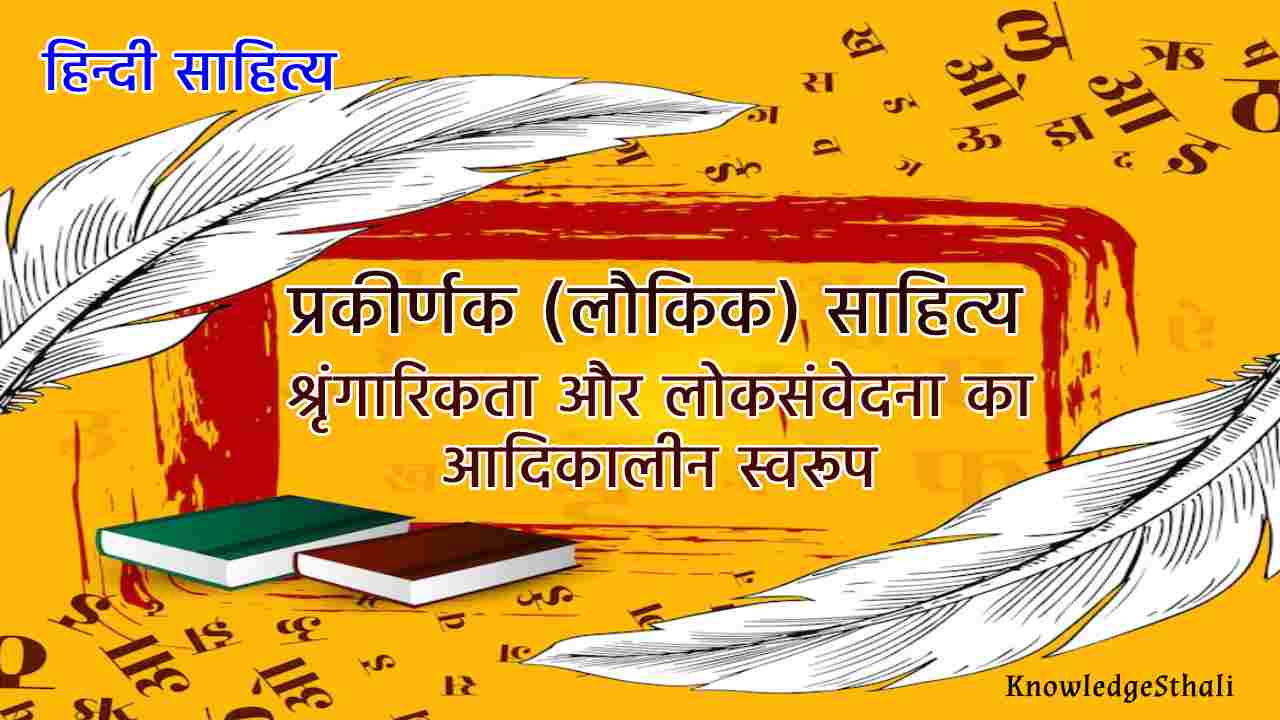हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम उसके आदिकालीन स्वरूप में देखते हैं, तो वहाँ वीर रसप्रधान रासो साहित्य और धर्माश्रित धार्मिक साहित्य के समानांतर एक तीसरी साहित्यिक धारा भी दृष्टिगत होती है – जिसे प्रकीर्णक साहित्य अथवा लौकिक साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य न तो राजाश्रय का प्रतिफल था और न ही धर्म प्रचार की भावना से अनुप्राणित। यह लोक की संवेदना, हास-विलास, श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य की उपज थी। यही कारण है कि इसमें मनुष्य की सहज भावनाओं – प्रेम, वियोग, हास्य और सौंदर्य – का चित्रण अत्यधिक सरसता और आत्मीयता से हुआ है।
यह साहित्य परंपरागत वीर-धारा और धार्मिक प्रवृत्ति के विरोध में न होकर, उससे भिन्न लोक-केन्द्रित अभिव्यक्ति का मार्ग था। आदिकालीन लौकिक साहित्य की यह विशेषता इसे साहित्येतिहास में एक विशिष्ट और आवश्यक स्थान प्रदान करती है।
रासो और धार्मिक साहित्य से भिन्न यह साहित्य लोकजीवन से जुड़ा हुआ, भावप्रधान और श्रृंगारिक था। इस लेख में ढोला मारू रा दूहा, बसन्त विलास, राउलवेल, वर्णरत्नाकर, अमीर खुसरो की रचनाएँ और विद्यापति की पदावली जैसी विशिष्ट काव्य कृतियों की समीक्षा की गई है। साथ ही, इसमें नख-शिख वर्णन, वियोग श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, गेयता और बोली भाषा के प्रयोग जैसी साहित्यिक विशेषताओं पर विस्तार से विचार किया गया है।
यह लेख न केवल हिंदी के प्रारंभिक साहित्यिक विकास को समझने का माध्यम है, बल्कि लोकसंवेदना और भाषा प्रयोग की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। शोधार्थियों, विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए यह लेख हिंदी की सांस्कृतिक और काव्यात्मक परंपराओं की एक सशक्त झलक प्रस्तुत करता है। इस लेख में हम प्रकीर्णक साहित्य की विभिन्न रचनाओं, रचनाकारों और उसकी शैलीगत तथा विषयगत विशेषताओं पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।
प्रकीर्णक साहित्य की अवधारणा और स्वरूप
‘प्रकीर्णक’ का अर्थ होता है – इधर-उधर बिखरा हुआ, विविधता से युक्त। इस दृष्टि से देखें तो यह साहित्य किसी एक रस या उद्देश्य में सीमित नहीं रहा, अपितु उसमें श्रृंगार, हास्य, नख-शिख वर्णन, प्रकृति चित्रण, बोली भाषा का प्रयोग और गीतात्मकता की विविध छवियाँ सम्मिलित हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह साहित्य लोक से जुड़ा, लोक के लिए रचा गया और लोक की ही वाणी में व्यक्त हुआ।
प्रकीर्णक साहित्य न तो दरबारी संस्कृति का उपज था और न ही धार्मिक नियमबद्धता का अनुयायी। इसने स्वांतः सुखाय सृजन को प्राथमिकता दी, जिससे यह अधिक मानवीय, भावपूर्ण और गेय बन गया।
प्रकीर्णक साहित्य की प्रमुख लौकिक रचनाएँ और उनका साहित्यिक मूल्य
ढोला मारू रा दूहा – लोकप्रेम की अमर गाथा
राजस्थान की लोक परंपरा में रची-बसी “ढोला मारू रा दूहा” एक अत्यंत लोकप्रिय काव्य कृति है जो ढोला और मारू की प्रेमकथा पर आधारित है। ढोला कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था, जबकि मारू पूगल के राजा पिंगल की रूपवती कन्या थी।
हालाँकि इस कथा का आधार ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है, परन्तु इसकी प्रस्तुति शैली, भावप्रधानता तथा लोकाभिव्यक्ति ने इसे पूर्णतः लोककाव्य बना दिया है। लोक भाषा में रची गई यह कथा पश्चिमी राजस्थान में न केवल मनोरंजन का साधन बनी, बल्कि जनमानस के हृदय में गहराई से रच-बस गई।
यह काव्य नारी सौंदर्य, प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन के मार्मिक प्रसंगों के माध्यम से श्रृंगार रस की उत्कृष्ट प्रस्तुति करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह रचना लोक की संवेदना से जुड़ी है और इसमें धार्मिकता या राजाश्रय की छाया नहीं दिखाई देती।
2. बसन्त विलास – श्रृंगार रस की सरस कृति
‘बसन्त विलास’ हिन्दी साहित्य की एक अत्यंत सरस और मनोहारी काव्य रचना है, जिसकी रचना-काल 13वीं से 14वीं सदी के मध्य मानी जाती है। डॉ. माताप्रसाद गुप्त के अनुसार, यद्यपि इस कृति के रचयिता का नाम ज्ञात नहीं है, परन्तु इसका काव्य सौंदर्य और श्रृंगारिक भावों की कोमल अभिव्यक्ति इसे अद्वितीय बनाती है।
‘बसन्त विलास’ में बसन्त ऋतु के आगमन, प्रकृति की सुषमा, प्रेमी-प्रेमिका के भाव, उनके मिलन और मनोवृत्तियों को अत्यंत कोमल और कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इस काव्य की भाषा, शैली और भाव-प्रवणता आधुनिक भारतीय आर्य-भाषा साहित्य के आदिकाल में एक विशिष्ट स्थान रखती है।
3. राउलवेल – चम्पू काव्य की प्राचीनतम कड़ी
‘राउलवेल’ हिन्दी गद्य-पद्य मिश्रित साहित्य की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। इसे चम्पू-काव्य का रूप कहा गया है। इस काव्य के रचयिता का नाम “रोढ़ा” माना जाता है और इसका रचना काल 10वीं शताब्दी के आसपास का अनुमानित है।
‘राउलवेल’ में ‘राउल’ नामक नायिका का नख-शिख वर्णन किया गया है। यह श्रृंगार रस का अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण है, जिसमें नारी सौंदर्य का विस्तारपूर्वक चित्रण मिलता है।
यह रचना यह सिद्ध करती है कि हिन्दी साहित्य का विकास केवल पद्य या वीररस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसमें गद्य का भी प्रारंभिक विकास हो चुका था और नारी श्रृंगार के प्रति एक कोमल दृष्टिकोण विकसित हो रहा था।
4. उक्ति-व्यक्ति प्रकरण – भाषावैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण
‘उक्ति-व्यक्ति प्रकरण’ एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरणिक ग्रन्थ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में दामोदर शर्मा द्वारा की गई थी।
यह ग्रंथ केवल व्याकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बनारस और आस-पास के क्षेत्रों की तत्कालीन संस्कृति, समाज और भाषा की झलक भी मिलती है। इसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उस काल में हिन्दी भाषा में तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।
इस ग्रंथ की भाषा में गद्य और पद्य दोनों शैलियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, जिससे यह ग्रंथ हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक विकास में एक अत्यंत उपयोगी स्रोत बन जाता है।
5. वर्णरत्नाकर – शब्दकोश के साथ साहित्यिक प्रतिभा
‘वर्णरत्नाकर’ मैथिली-हिन्दी में रचित एक महत्वपूर्ण गद्य ग्रंथ है जिसके रचयिता ज्योतिशेखर ठाकुर थे। डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसकी रचना को 14वीं शताब्दी का माना है।
यद्यपि यह ग्रंथ एक प्रकार का शब्दकोश है, परन्तु इसकी भाषा में काव्यात्मकता, अलंकारिकता और सौंदर्यग्राहिणी प्रतिभा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
‘वर्णरत्नाकर’ में प्रयुक्त भाषा न केवल तत्सम शब्दों की प्रधानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि हिन्दी गद्य लेखन में शब्दों की चयनशीलता, लय और अभिव्यक्ति की सजगता विकसित हो रही थी।
‘राउलवेल’ के बाद ‘वर्णरत्नाकर’ हिन्दी गद्य विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।
6. अमीर खुसरो की रचनाएँ – हास्य, व्यंग्य और खड़ी बोली की शुरुआत
अमीर खुसरो (1253–1325 ई.) का वास्तविक नाम अबुल हसन था। वे दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध सूफी कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिन्दी साहित्य में खड़ी बोली के प्रारंभिक प्रयोगों के लिए खुसरो को पहला कवि माना जाता है।
उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता को साहित्यिक माध्यम से प्रस्तुत किया और हास्य-व्यंग्य से भरपूर कविताओं की रचना की। उनकी पहेलियाँ, मुखरियाँ, दो सुखने और ढकोसले आज भी जनमानस में लोकप्रिय हैं।
खुसरो की प्रमुख रचनाएँ –
- पहेलियाँ:
- “एक थाल मोतियों से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा।
चारों ओर वह थाल फिरे, एक भी मोती नीचे न गिरे।” (उत्तर – आकाश) - “एक कहानी मैं बहूँ, सुन ले तू मेरे पुत।
बिना परों के वह उड़ गया, बाँध गले में सूत।।” (उत्तर – पतंग)
- “एक थाल मोतियों से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा।
- मुखरियाँ:
- “वह आवे तब शादी होय, उस बिन दूजा और न कोय।
मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखि साजन न सखि ढोल।” - जब मेरे मन्दिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे।
पढ़त फिरत वह विरह के अच्छर सखि साजन ना सखि मच्छर ।।
- “वह आवे तब शादी होय, उस बिन दूजा और न कोय।
- दो सुखने:
- “पान सड़ा क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों?” – (उत्तर – फेरा न था)
- ब्राह्मण प्यासा क्यों? गधा उदासा क्यों ? (उत्तर – लोटा न था)
- ढकोसला:
- “खीर पकाई जतन से, चर्खा दिया चलाय।
आया कुत्ता खा गया, तु बैठी ढोल बजाय।”
- “खीर पकाई जतन से, चर्खा दिया चलाय।
खुसरो की भाषा अत्यंत सहज, जनसामान्य की भाषा है जिसमें हास्य, तात्कालिकता और व्यंग्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
7. विद्यापति की पदावली – श्रृंगारिक गीतों के जनक
बिहार के दरभंगा जिले के विसपी गाँव में जन्मे विद्यापति को हिन्दी का प्रथम गीतिकाव्यकार कहा जाता है। वे संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली के प्रकांड विद्वान थे। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की कोमलता, प्रेम की अनुभूति और भावों की प्रचुरता देखने को मिलती है।
उनके पदों में राधा-कृष्ण के मिलन-विरह, मनोभावों की सजीवता और लोकधर्मी संवेदनाएँ अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुई हैं।
विद्यापति को ‘अभिनव जयदेव’ की संज्ञा दी गई है, जो उनकी पदावली की मधुरता और रसप्रवणता को उजागर करती है।
लौकिक साहित्य की विशेषताएँ
हिंदी साहित्य का इतिहास विविध रंगों और रसों से भरा हुआ है। इसमें धार्मिक, वीरगाथात्मक, भक्ति तथा लौकिक साहित्य की विभिन्न धाराएँ विकसित हुई हैं। लौकिक साहित्य, जिसे ‘प्रकीर्णक साहित्य’ भी कहा जाता है, हिंदी के आदिकालीन साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह साहित्य न तो किसी धार्मिक प्रचार-प्रसार का उद्देश्य रखता है, न ही केवल राजाओं और वीरों की प्रशंसा के लिए रचा गया है, बल्कि यह जन-मन के सहज भावों, लोक-रुचियों और सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है।
इस लेख में हम विस्तारपूर्वक उन विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे जो आदिकालीन लौकिक साहित्य को अन्य साहित्यिक धाराओं से अलग और विशिष्ट बनाती हैं।
1. स्वान्तः सुखाय सृजन की परंपरा
लौकिक साहित्य का सर्वप्रथम और सबसे प्रमुख गुण है—स्वान्तः सुखाय सृजन। इसका तात्पर्य है कि यह साहित्य आत्मानंद के लिए रचा गया, न कि किसी राजकीय संरक्षण या धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जहाँ रासो साहित्य में कवियों ने राजाओं, सेनाओं, युद्धों और विजयों का बखान किया, वहीं लौकिक साहित्य के रचनाकारों ने स्वयं की अनुभूतियों, भावनाओं और कल्पनाओं को प्राथमिकता दी। इसी कारण इसकी रचनाएँ सहज, आत्मस्फूर्त और मानवीय संवेदनाओं से ओत-प्रोत होती हैं।
उदाहरण: ‘ढोला मारू रा दूहा’ और ‘राडलवेल’ जैसे ग्रंथों में प्रेम, विरह, प्रकृति और लोकजीवन की अभिव्यक्ति इतनी प्रामाणिक और प्रभावशाली है कि वे पाठक को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं।
2. लोकमानस से आप्लावित साहित्य
लौकिक साहित्य का दूसरा महत्त्वपूर्ण गुण है—लोकमानस का प्रतिफलन। इसमें आम जनमानस की भावनाएँ, विचार, अभिलाषाएँ और जीवनशैली उभरकर सामने आती हैं। यह साहित्य शास्त्रीयता से बँधा हुआ नहीं है, बल्कि लोकगीतों, लोककथाओं, पर्व-त्योहारों और ग्रामीण संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है।
लोकतत्व की उपस्थिति के कारण यह साहित्य अत्यंत सरस, प्रभावकारी और जनप्रिय बन गया। रासो साहित्य जहाँ राजाश्रित था, वहीं लौकिक साहित्य जनाश्रित था। इसमें राजाओं के नहीं, बल्कि आम स्त्री-पुरुषों के जीवन, प्रेम, वियोग, सुख-दुख, हास-परिहास और संघर्षों को चित्रित किया गया है।
3. संयोग और वियोग श्रृंगार का सरस चित्रण
श्रृंगार रस आदिकालीन लौकिक साहित्य का प्रमुख तत्व है। इस साहित्य में संयोग (प्रेम मिलन) और वियोग (विरह) दोनों का सरस और हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है।
जहाँ संयोग में प्रेमी-प्रेमिका के मधुर मिलन, शृंगारिक क्षणों और सौंदर्य का वर्णन होता है, वहीं वियोग में प्रेमियों के बिछोह, तड़प और भावनात्मक वेदना का चित्रण अत्यंत मार्मिक ढंग से हुआ है।
विशेष तथ्य यह है कि लौकिक साहित्य का वियोग श्रृंगार अधिक समृद्ध और भावविह्वल है। इसमें विरह की आग में झुलसते मन की व्यथा, आँखों के आँसू और हृदय की वेदना को इतनी सूक्ष्मता से व्यक्त किया गया है कि वह पाठक के अंतर्मन को झकझोर देता है।
4. नख-शिख वर्णन परंपरा का प्रणयन
लौकिक साहित्य में नख-शिख वर्णन की परंपरा का आरंभ आदिकाल में ही हो चुका था। इसमें नायिका के शरीर सौंदर्य का वर्णन सिर से लेकर नख तक किया जाता है।
‘राउलवेल’ जैसी रचनाएँ इसका प्रमुख उदाहरण हैं। यह चम्पू शैली में रचित एक विशिष्ट काव्य है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन किया गया है।
नख-शिख वर्णन केवल शारीरिक सौंदर्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ, नारी के आभूषण, श्रृंगार-सज्जा और नारी की नज़रों का भाव भी समाहित होता है। यह परंपरा आगे चलकर भक्ति साहित्य और रीति साहित्य में भी दिखाई देती है।
5. प्रकृति चित्रण: आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में
लौकिक साहित्य में प्रकृति चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि वह काव्य के रस और भाव की वाहिका बन जाती है।
प्रकृति को आलंबन (मुख्य आधार) और उद्दीपन (भावों को उद्दीप्त करनेवाला कारक) दोनों रूपों में प्रयुक्त किया गया है। वसंत ऋतु, वर्षा, चंद्रमा, पक्षी, फूल, नदियाँ, झीलें और आकाश — इन सभी का अत्यंत प्रभावी और कलात्मक चित्रण लौकिक साहित्य में मिलता है।
श्रृंगार रस और प्रकृति का रिश्ता अटूट है। ऋतुओं के बदलते रंग, फूलों की सुगंध, कोयल की कूक और मेघों की गूँज—all these elements enhance the emotional resonance of the poem and connect the reader directly with the sensory world.
6. गेयता एवं संगीतात्मकता
आदिकालीन लौकिक साहित्य में भावों की प्रवणता (flow of emotions) इतनी तीव्र और स्वाभाविक है कि वह स्वतः गेयता और संगीतात्मकता उत्पन्न कर देती है।
इस धारा की अधिकांश रचनाएँ गीतात्मक हैं जिन्हें गाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकगीतों से प्रभावित ये रचनाएँ सहज लय, ताल और तुकांत योजना के कारण बहुत आकर्षक बन जाती हैं।
‘ढोला-मारू’, ‘विद्यापति की पदावली’, ‘राडलवेल’ आदि रचनाओं में गीतात्मकता इतनी प्रबल है कि वे आज भी लोकजीवन में जीवित हैं। ये रचनाएँ मंच पर, मेलों में, विवाहों में, और लोक-समारोहों में गाई जाती रही हैं।
7. बोली भाषा का परिष्कार
लौकिक साहित्य की एक अन्य विशेषता है—बोलियों का प्रयोग और उनका परिष्कार। जहाँ शास्त्रीय साहित्य संस्कृत या ब्रजभाषा जैसी परिनिष्ठित भाषाओं में लिखा गया, वहीं लौकिक साहित्य में अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मैथिली, खड़ी बोली जैसी जनभाषाओं का प्रयोग हुआ।
‘राडलवेल’ जैसी रचनाएँ इस बात की साक्षी हैं कि लौकिक साहित्य केवल साहित्यिक परंपरा की नहीं, बल्कि भाषिक परंपरा की भी नींव रखता है।
विद्यापति की मैथिली में रची गई पदावलियाँ हों या ढोला-मारू की राजस्थानी कथाएँ, इन सबमें क्षेत्रीय भाषाओं का वह भावमय, संगीतमय और सजीव प्रयोग मिलता है जो लोकजीवन से सीधे जुड़ता है।
8. स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की जीवंत अभिव्यक्ति
लौकिक साहित्य की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की मानवीय और स्वाभाविक अभिव्यक्ति की गई है।
यहाँ नारी केवल उपास्या नहीं है, न ही केवल सौंदर्य की वस्तु, बल्कि एक चेतन, भावनापूर्ण और स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उभरती है।
उसके प्रेम, उसकी पीड़ा, उसका विरह, उसका सौंदर्य, उसकी आकांक्षाएँ—सभी को अत्यंत सजीव रूप में चित्रित किया गया है। इससे तत्कालीन समाज में स्त्री की भूमिका और स्थान का भी अनुमान होता है।
9. चम्पू काव्य परंपरा का प्रयोग
लौकिक साहित्य में चम्पू काव्य परंपरा (गद्य और पद्य का मिश्रण) का सुंदर प्रयोग मिलता है। यह शैली कवियों को भाव और वर्णन की अधिक स्वायत्तता प्रदान करती थी।
‘राउलवेल’ एक विशिष्ट उदाहरण है, जिसमें गद्य की वाक्यात्मकता और पद्य की भावप्रवणता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। चम्पू शैली के प्रयोग से भावों को और अधिक विस्तार, गति और सजीवता मिलती है।
10. जनजीवन और सांस्कृतिक परंपराओं का दर्पण
लौकिक साहित्य केवल कल्पनालोक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समकालीन जनजीवन, लोकप्रथाओं, सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं का सजीव चित्रण करता है।
इसमें ग्रामीण जीवन, प्रेम विवाह, जातिगत व्यवहार, लोकविश्वास, देवी-देवताओं की मान्यताएँ, त्योहार, लोकगीत, विवाह गीत, और पारंपरिक रीति-रिवाजों का जीवंत चित्र देखने को मिलता है।
इससे यह साहित्य इतिहास और संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी बन जाता है।
निष्कर्ष
आदिकालीन लौकिक साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अनूठा और समृद्ध अध्याय है। यह साहित्य न केवल भावात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण है, बल्कि भाषिक, सांस्कृतिक और लोकमानसिक चेतना का भी प्रतिनिधित्व करता है।
इसकी विशेषताओं—स्वान्तः सुखाय सृजन, लोकमानस से जुड़ाव, संयोग-वियोग का मार्मिक चित्रण, प्रकृति और श्रृंगार का समन्वय, गेयता, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग, और स्त्री-पुरुष संबंधों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति—इन्हें देखकर यह स्पष्ट होता है कि यह साहित्य युगबोध और मानवबोध दोनों का वाहक है।
आज जब हम हिंदी साहित्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लौकिक साहित्य की उपेक्षा करना हमारी सांस्कृतिक जड़ों को भूलने जैसा होगा। यह साहित्य न केवल हमारे अतीत का दस्तावेज़ है, बल्कि हमारी भावनात्मक और सांस्कृतिक धरोहर भी है।
प्रकीर्णक या लौकिक साहित्य हिंदी के आदिकाल में एक सांस्कृतिक सेतु की भूमिका निभाता है, जो लोक और साहित्य, भाव और भाषा, सौंदर्य और अनुभव के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित करता है। यह हिन्दी साहित्य के आदिकाल का वह पक्ष है जिसमें लोक जीवन, श्रृंगारिकता, हास्य-विनोद, गद्य-पद्य का समन्वय तथा भाषिक प्रयोगों का आरंभिक स्वरूप सन्निहित है। इस साहित्य में न कोई धार्मिक आग्रह है, न ही कोई राजाश्रयी प्रतिबद्धता – इसका आधार है लोक की चेतना, जन की संवेदना और हृदय की अभिव्यक्ति।
चाहे वह ‘ढोला मारू रा दूहा’ की प्रेमगाथा हो, ‘बसन्त विलास’ की ऋतु सौंदर्यता, ‘राउलवेल’ का श्रृंगारिक वर्णन हो या ‘अमीर खुसरो’ की व्यंग्यपूर्ण सहजता – प्रत्येक कृति हिन्दी साहित्य को बहुआयामी बनाती है।
यह साहित्य हिन्दी के विकास की नींव तैयार करता है और यह सिद्ध करता है कि हिन्दी साहित्य का आदिकाल केवल वीर रस और धर्म से युक्त नहीं था, अपितु उसमें श्रृंगार, हास्य, व्याकरणिक विवेक और लोक जीवन की समृद्ध परंपराएँ भी समाहित थीं। यह साहित्य आज भी भाषा वैज्ञानिकों, साहित्यिकों और सांस्कृतिक शोधार्थियों के लिए बहुमूल्य संदर्भ सामग्री प्रदान करता है और लोकसंवेदना की उस निरंतर धारा का परिचायक है, जो आज भी जन-जन की वाणी में गूंज रही है।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
- प्रकीर्णक साहित्य किसे कहते हैं?
– वह साहित्य जो न राजाश्रय में रचा गया हो, न धार्मिक उद्देश्य से, बल्कि लोक और श्रृंगार की प्रेरणा से रचा गया हो। - ढोला मारू रा दूहा की प्रमुख विशेषता क्या है?
– यह एक प्रेमगाथा है जिसमें लोकभाषा, लोकप्रेम और गीतात्मकता का अद्भुत संयोग है। - राउलवेल का साहित्यिक महत्व क्या है?
– यह गद्य-पद्य मिश्रित चम्पू काव्य है जिसमें नख-शिख वर्णन परंपरा की शुरुआत होती है। - अमीर खुसरो की प्रमुख रचनात्मक विधाएँ कौन-सी हैं?
– पहेलियाँ, मुखरियाँ, दो सुखने और ढकोसले। - वर्णरत्नाकर किस भाषा में रचित है?
– यह मैथिली-हिंदी मिश्रित भाषा में रचित एक गद्य रचना है। - लौकिक साहित्य में कौन सा रस प्रमुख है?
– श्रृंगार रस, विशेषकर वियोग श्रृंगार, प्रमुख रूप से विद्यमान है। - बसन्त विलास का विषय क्या है?
– यह ऋतु बसंत और प्रकृति सौंदर्य के माध्यम से श्रृंगार रस का चित्रण करता है। - विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है?
– उन्हें ‘अभिनव जयदेव’ कहा जाता है। - उक्ति-व्यक्ति प्रकरण की विशेषता क्या है?
– यह व्याकरण ग्रंथ होते हुए भी तत्कालीन भाषा, संस्कृति और काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। - लौकिक साहित्य का महत्व क्यों है?
– यह साहित्य जनमानस की संवेदना, बोलचाल की भाषा और लोककला का प्रतिनिधि है।
इन्हें भी देखें –
- कबीर दास जी के दोहे एवं उनका अर्थ | साखी, सबद, रमैनी
- कबीर दास जी | जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएँ एवं भाषा
- आख़िरी तोहफ़ा | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- हिंदी के विराम चिन्ह और उनका प्रयोग | 50 + उदाहरण
- जैन साहित्य: स्वरूप, विकास, प्रमुख कवि, कृतियाँ और साहित्यिक विशेषताएँ
- सिद्ध साहित्य: हिन्दी साहित्य का आदिरूप और सामाजिक चेतना का संवाहक
- नाथ संप्रदाय (साहित्य): योग, तंत्र और साधना की भारतीय परंपरा का अनूठा अध्याय
- चम्पू साहित्य | गद्य और पद्य का अद्वितीय संगम
- इतिहास रचेंगी प्रिया नायर, बनेंगी हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ
- तैमूर लंग (1336 ई. – 1405 ई.)
- खिज्र खां (1414-1421ई.)
- आंग्ल-मराठा युद्ध | 1775-1818 ई.