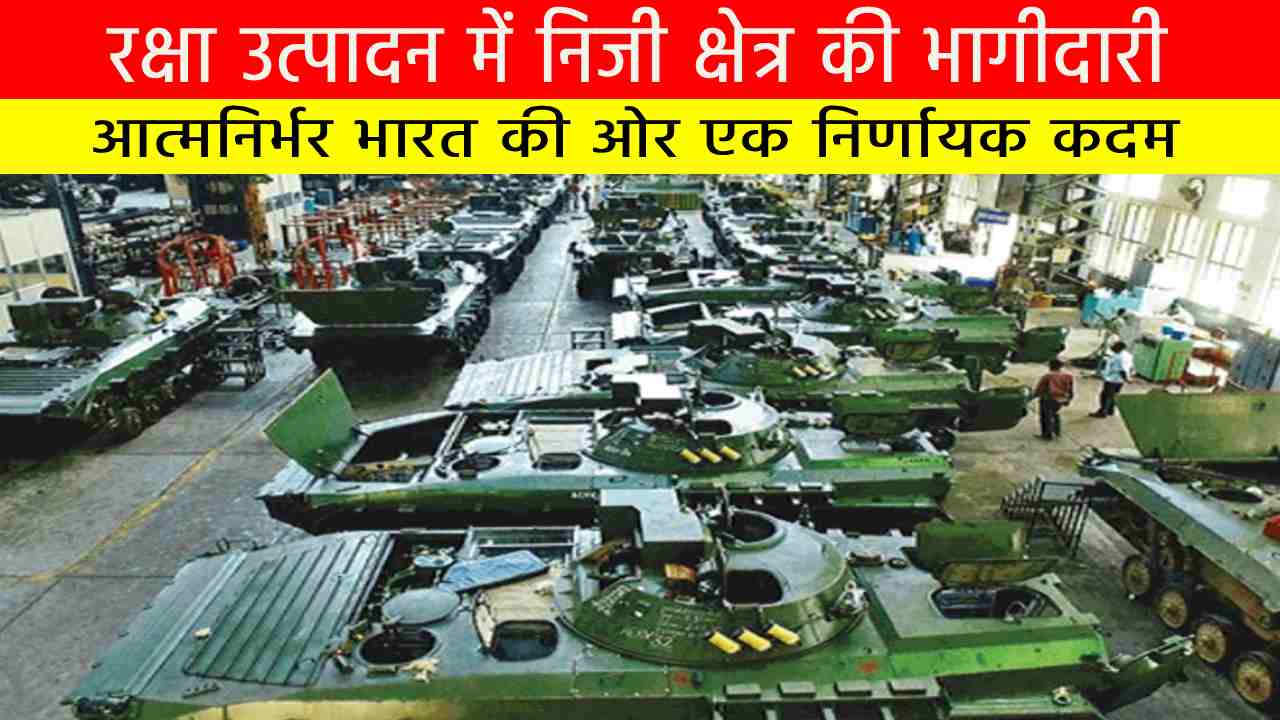भारत आज रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जहाँ कभी देश की सुरक्षा ज़रूरतें आयातित हथियारों और उपकरणों पर निर्भर हुआ करती थीं, वहीं आज ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल ने रक्षा उद्योग का स्वरूप ही बदल दिया है। विशेष रूप से निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी ने भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने का अवसर प्रदान किया है।
वित्त वर्ष 2024-25 के आँकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। इस अवधि में कुल रक्षा उत्पादन ₹1,50,590 करोड़ रहा, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान ₹33,979 करोड़ यानी 22.56% रहा। यह हिस्सा अब तक का सबसे ऊँचा है और 2016-17 के बाद पहली बार 20% के पार पहुँचा है। यह उपलब्धि भारत की रक्षा उत्पादन नीतियों, प्रोत्साहन उपायों और निजी उद्योगों के सक्रिय निवेश का परिणाम है।
भारत में रक्षा उत्पादन का परिदृश्य
रक्षा उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान संतुलित होते हुए भी विविध है।
- रक्षा सार्वजनिक उपक्रम (DPSUs): इनका योगदान सबसे अधिक यानी 57.50% है।
- भारतीय आयुध कारखाने (OFB): कुल उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 14.49% रही।
- गैर-रक्षा सार्वजनिक उपक्रम: इनका योगदान 5.4% दर्ज किया गया।
- निजी क्षेत्र: 23% के आसपास पहुँचकर एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र की वृद्धि दर 28% वार्षिक रही, जबकि DPSUs की वृद्धि दर 16% रही। यह अंतर इस ओर संकेत करता है कि निजी क्षेत्र आने वाले वर्षों में और भी तेज़ गति से रक्षा उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है।
रक्षा बजट और उत्पादन में वृद्धि
भारत का रक्षा बजट पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है।
- वर्ष 2013-14 में रक्षा बजट ₹2.53 लाख करोड़ था।
- वर्ष 2025-26 तक यह बढ़कर ₹6.81 लाख करोड़ पहुँच गया है।
इसी प्रकार, रक्षा उत्पादन में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।
- 2014-15 में कुल रक्षा उत्पादन ₹46,429 करोड़ था।
- 2024-25 में यह बढ़कर ₹1.50 लाख करोड़ हो गया।
इस प्रकार, एक दशक में उत्पादन तीन गुना से अधिक बढ़ा है। इसका सीधा संबंध सरकार द्वारा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र को नीति-निर्माण में साझेदार बनाने से है।
स्वदेशीकरण और आयात निर्भरता में कमी
कभी भारत की रक्षा ज़रूरतों का 65-70% आयात पर आधारित होता था। परंतु अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं।
- आज 65% रक्षा उपकरण देश में ही निर्मित हो रहे हैं।
- आयात पर निर्भरता घटकर लगभग 35% रह गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू हुई ‘आत्मनिर्भर भारत पहल’ का मूल उद्देश्य ही आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को रक्षा निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है।
रक्षा निर्यात में भारत की उपलब्धियाँ
भारत केवल घरेलू उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि निर्यात के क्षेत्र में भी नई ऊँचाइयाँ छू रहा है।
- वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात मात्र ₹686 करोड़ था।
- वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर ₹23,622 करोड़ हो गया।
यह लगभग 34 गुना वृद्धि है।
भारत का रक्षा निर्यात पोर्टफोलियो भी विविध हो गया है, जिसमें शामिल हैं:
- बुलेटप्रूफ जैकेट
- चेतक हेलीकॉप्टर
- तेज गति वाले इंटरसेप्टर बोट्स
- हल्के टॉरपीडो
आज भारत 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया 2023-24 में इसके प्रमुख खरीदार रहे।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का तुलनात्मक योगदान
भारत का रक्षा उत्पादन अभी भी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित है।
- सार्वजनिक क्षेत्र (DPSUs और अन्य यूनिट्स): लगभग 77% योगदान
- निजी क्षेत्र: लगभग 23% योगदान
हालाँकि निजी क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है।
- FY 2023-24 में निजी भागीदारी 21% थी।
- FY 2024-25 में यह बढ़कर 23% हो गई।
निजी क्षेत्र की 28% YoY वृद्धि यह दर्शाती है कि आने वाले वर्षों में इसका हिस्सा और अधिक बढ़ेगा।
नीतिगत सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान
निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की वृद्धि का मुख्य आधार नीतिगत सुधार हैं।
- स्वदेशीकरण (Indigenisation): सरकार ने हथियारों और रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण पर विशेष बल दिया।
- Ease of Doing Business: लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल किया गया और निजी कंपनियों को समान अवसर दिए गए।
- प्रतिबंधित आयात सूची: कई हथियारों और उपकरणों को आयात सूची से हटाकर घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दी गई।
- FDI सुधार: रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया।
आगे की राह
भारत का लक्ष्य है कि 2029 तक रक्षा उत्पादन को ₹3 लाख करोड़ तक पहुँचाया जाए। इसके लिए कई पहल की जा रही हैं।
1. कौशल विकास
- उभरती रक्षा तकनीकों (AI, क्वांटम, साइबर, स्पेस) के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों की साझेदारी।
2. संयुक्त उपक्रम
- विदेशी कंपनियों के साथ Co-development और Technology Transfer को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- अमेरिका, रूस, फ्रांस और इज़राइल जैसे देशों के साथ कई साझेदारियाँ बन चुकी हैं।
3. स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा
- iDEX (Innovations for Defence Excellence)
- ADITI (Aatmanirbhar Defence Initiatives for Technological Innovation)
इन योजनाओं के तहत रक्षा स्टार्ट-अप्स को फंडिंग और मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
4. समान अवसर
- पारदर्शी Procurement Policy लागू की जा रही है।
- निजी कंपनियों और DPSUs के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा रही है।
5. निर्यात तंत्र को मज़बूत करना
- नए वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच बनाने के प्रयास।
- निजी कंपनियों को निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में शामिल करना।
- “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” को रक्षा क्षेत्र में भी साकार करना।
चुनौतियाँ
हालाँकि प्रगति उल्लेखनीय है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं:
- उच्च तकनीकी रक्षा प्रणालियों (जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स, पनडुब्बी टेक्नोलॉजी) में अभी भी विदेशी निर्भरता।
- रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में निजी क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम निवेश।
- रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और स्पेयर पार्ट्स में आत्मनिर्भरता की कमी।
- परियोजनाओं में विलंब और लागत में वृद्धि की समस्या।
निष्कर्ष
भारत ने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर एक नया अध्याय रचा है। यह केवल उत्पादन के आँकड़ों में वृद्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में बड़ा कदम है।
आज भारत न केवल अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो रहा है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाज़ार में भी अपनी जगह बना रहा है। यदि यही रफ्तार बनी रही, तो 2029 तक भारत का ₹3 लाख करोड़ रक्षा उत्पादन लक्ष्य पूरा करना संभव होगा और भारत दुनिया के प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा।