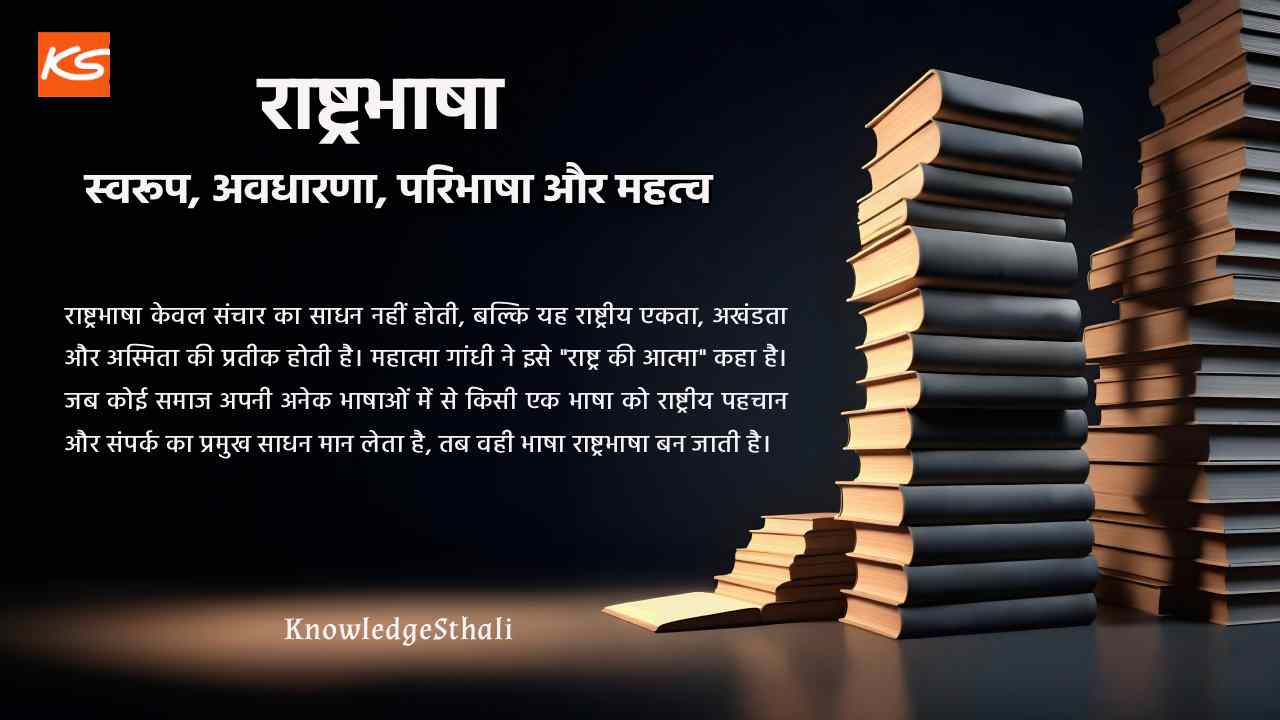किसी भी देश की भाषा उसकी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का मूल आधार होती है। भाषा न केवल संचार का माध्यम है बल्कि यह समाज की अस्मिता, गौरव और राष्ट्र की आत्मा को भी अभिव्यक्त करती है। इस दृष्टि से “राष्ट्रभाषा” शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसका शाब्दिक अर्थ है— “समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा”, अर्थात वह भाषा जिसे जन-जन सहजता से समझे और जिसके द्वारा विचार-विनिमय किया जा सके।
भारत जैसे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुधर्मी देश में भाषा का प्रश्न सदैव एक चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। संविधान में भले ही “राष्ट्रभाषा” शब्द का उल्लेख नहीं है, किन्तु ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
राष्ट्रभाषा की अवधारणा
राष्ट्रभाषा केवल संचार का साधन नहीं होती, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अस्मिता की प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने इसे “राष्ट्र की आत्मा” कहा है। जब कोई समाज अपनी अनेक भाषाओं में से किसी एक भाषा को राष्ट्रीय पहचान और संपर्क का प्रमुख साधन मान लेता है, तब वही भाषा राष्ट्रभाषा बन जाती है।
भारत के संदर्भ में हिन्दी ने यह भूमिका निभाई है। हिन्दी का व्यापक जनाधार, सहजता और लचीलापन इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करता है।
राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं?
‘राष्ट्रभाषा’ का अर्थ है वह भाषा जो पूरे राष्ट्र में संचार, विचार-विनिमय और जन-जन की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बने।
शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है – “समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा”।
किसी भी देश की राष्ट्रभाषा केवल बोली जाने वाली भाषा नहीं होती, बल्कि वह उस देश की एकता, अखण्डता, गौरव और अस्मिता की प्रतीक होती है। राष्ट्रभाषा का चयन केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के लिए किया जाता है।
महात्मा गांधी ने इसे “राष्ट्र की आत्मा” कहा था। उनके अनुसार, वही भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है—
- जिसे बहुसंख्यक लोग बोलते और समझते हों।
- जो सरल, सहज और सर्वसुलभ हो।
- जिसके माध्यम से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कार्य सहज रूप से हो सकें।
- जिसके साथ जनता का भावनात्मक जुड़ाव हो।
इस प्रकार राष्ट्रभाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक पहचान का आधार है।
भारत की राष्ट्रभाषा
भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से “राष्ट्रभाषा” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान की धारा 343 के अनुसार हिन्दी (देवनागरी लिपि में) और अंग्रेजी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है।
भारत में कुल 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, किन्तु पूरे देश की राष्ट्रभाषा किसी एक को घोषित नहीं किया गया।
फिर भी व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टि से हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना जाता है, क्योंकि—
- यह देश की लगभग आधी जनसंख्या की मातृभाषा है।
- यह सम्पर्क भाषा (Link Language) के रूप में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक प्रयुक्त होती है।
- स्वतंत्रता संग्राम के समय हिन्दी ने जन-आंदोलन की भाषा और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक भाषा के रूप में कार्य किया।
- साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा, सिनेमा और जनसंचार माध्यमों के जरिए हिन्दी पूरे देश में प्रचलित है।
महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं ने भी हिन्दी को ही भारत की संभावित राष्ट्रभाषा माना था। यही कारण है कि आज भी सामान्य बातचीत में हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है, जबकि संवैधानिक दृष्टि से इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
भारतीय संविधान और भाषाएँ
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं। इनमें कश्मीरी, सिन्धी, पंजाबी, हिन्दी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगू, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल हैं।
संविधान सभा ने गहन बहस के बाद यह निर्णय लिया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होगी, बल्कि ‘राजभाषा’ के रूप में हिन्दी (देवनागरी लिपि में) और अंग्रेजी को स्वीकार किया जाएगा।
संविधान सभा में भाषा पर बहस (11–14 सितम्बर, 1949)
संविधान सभा में केवल हिन्दी को लेकर चर्चा नहीं हुई, बल्कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दुस्तानी – चार भाषाओं पर दावे किए गए।
हालाँकि संघर्ष की स्थिति केवल हिन्दी और अंग्रेजी के समर्थकों के बीच ही दिखाई दी।
हिन्दी समर्थक वर्ग स्वयं दो गुटों में बँटा हुआ था–
- पहला गुट – देवनागरी लिपि वाली हिन्दी का समर्थक।
- दूसरा गुट – महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता, जो दो लिपियों वाली हिन्दुस्तानी के पक्षधर थे।
अंग्रेजी की दुविधा और हिन्दी का दावा
हालाँकि आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी), जिसे केवल 1–2% लोग पढ़-लिख और समझ सकते थे, राजभाषा नहीं बन सकती थी। परंतु अंग्रेजी को तुरंत छोड़ना भी कठिन था क्योंकि लगभग 150 वर्षों से अंग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा की प्रमुख भाषा रही थी।
दूसरी ओर, हिन्दी उस समय लगभग 46% भारतीयों की भाषा थी, इसलिए राजभाषा बनने का उसका दावा न्यायसंगत था। फिर भी प्रादेशिक भाषाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। यही कारण था कि संविधान निर्माताओं ने सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया।
मुंशी–आयंगार फॉर्मूला : समझौते का परिणाम
संविधान सभा के भीतर और बाहर हिन्दी को मिले व्यापक समर्थन को देखते हुए अन्ततः हिन्दी के पक्ष में निर्णय हुआ। यह निर्णय हिन्दी समर्थक और हिन्दी विरोधी नेताओं के बीच हुए समझौते, जिसे “मुंशी–आयंगार फॉर्मूला” कहा जाता है, के आधार पर सामने आया। इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं–
- हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा होगी।
- संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहभाषा के रूप में बनी रहेगी।
- अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि हिन्दी को राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रावधान के एक अस्पष्ट निर्देश के आधार पर हिन्दी और हिन्दुस्तानी के बीच चल रहे विवाद को समाप्त कर लिया गया।
संविधान में भाषा संबंधी उपबंध
संविधान ने राजभाषा के विषय को विशेष महत्व देते हुए भाषा संबंधी प्रावधान स्पष्ट किए।
- अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 – संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही में भाषा।
- भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) – राजभाषा संबंधी विस्तृत प्रावधान।
- आठवीं अनुसूची – भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का विवरण।
ये सभी उपबंध हिन्दी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए।
राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अंतर
- राष्ट्रभाषा : वह भाषा जो पूरे देश में भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रतीक हो।
- राजभाषा : वह भाषा जिसे प्रशासनिक और सरकारी कार्यों के लिए अधिकृत किया गया हो।
भारत में हिन्दी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला, जबकि राष्ट्रभाषा का दर्जा केवल व्यावहारिक और सामाजिक दृष्टि से हिन्दी को प्राप्त है।
स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रभाषा का प्रश्न
भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी आंदोलन था। अंग्रेजों के शासनकाल में प्रशासन और शिक्षा की भाषा अंग्रेजी थी, जिससे जनता और शासकों के बीच गहरा फासला था।
ऐसे समय में हिन्दी ने सम्पर्क भाषा का कार्य किया। विभिन्न प्रांतों के नेताओं, कवियों और समाज सुधारकों ने हिन्दी के माध्यम से जनता तक संदेश पहुँचाया।
- असम के शंकर देव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर और नामदेव, गुजरात के नरसी मेहता, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों और कवियों ने हिन्दी का प्रयोग किया।
- फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज अधिकारियों को हिन्दी सिखाई गई ताकि वे जनता से संवाद कर सकें।
1900 से 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिन्दी स्वतः ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई।
महात्मा गांधी और राष्ट्रभाषा
महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा के प्रबल समर्थक थे। वे कहते थे— “राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।” उनके अनुसार स्वराज प्राप्त करने के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना आवश्यक था।
1917 में गुजरात शिक्षा परिषद में गांधीजी ने राष्ट्रभाषा की पाँच विशेषताएँ बताईं—
- भाषा राजकीय अधिकारियों के लिए सरल हो।
- बहुत बड़ी संख्या में लोग उसे बोलते हों।
- उसके माध्यम से धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य हो सकें।
- भाषा पूरे राष्ट्र के लिए आसान हो।
- भाषा का चुनाव क्षणिक परिस्थिति से प्रभावित न हो।
गांधीजी ने हिन्दी प्रचार के लिए कई कदम उठाए—
- 1918 के इन्दौर अधिवेशन में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव।
- दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के लिए अपने पुत्र देवदास गांधी को भेजना।
- 1927 और 1936 में हिन्दी प्रचार सभाओं की स्थापना।
- कांग्रेस अधिवेशनों और समितियों का काम हिन्दी में करने का प्रस्ताव।
उनका मानना था कि यदि स्वराज्य केवल अंग्रेजी पढ़े लोगों का होगा तो संपर्क भाषा अंग्रेजी ही रहेगी, लेकिन यदि स्वराज्य करोड़ों निरक्षरों और आम जनता का होगा तो संपर्क भाषा केवल हिन्दी हो सकती है।
राष्ट्रभाषा आन्दोलन
20वीं सदी में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन निरंतर चलता रहा।
- 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन ने हिन्दी को कांग्रेस की कार्यभाषा बनाया।
- 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने राज्यों में हिन्दी शिक्षण को प्रोत्साहित किया।
- स्वतंत्रता से पूर्व हिन्दी को व्यापक जनसमर्थन मिल चुका था।
1942–1945 के बीच स्वतंत्रता संग्राम की लहर में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी से ओत-प्रोत रचनाएँ बड़ी संख्या में लिखी गईं। इस काल में हिन्दी वास्तव में जन-जन की आवाज बन गई।
संविधान सभा में भाषा पर बहस
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संविधान सभा में भाषा का प्रश्न उठा तो गहन बहस हुई। मुख्य रूप से दो मत सामने आए—
- देवनागरी लिपि वाली हिन्दी को अपनाने का मत।
- हिन्दुस्तानी (हिन्दी-उर्दू का सम्मिश्रण) को अपनाने का मत।
कुछ नेताओं ने संस्कृत और अंग्रेजी का समर्थन भी किया। अंततः समझौते के रूप में हिन्दी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा मान लिया गया।
राष्ट्रभाषा से संबंधित धार्मिक-सामाजिक संस्थाएँ
भारतीय समाज में राष्ट्रभाषा के विकास और प्रसार का संबंध केवल भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से भी जुड़ा रहा। 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक कई प्रमुख समाज-सुधारक संस्थाएँ स्थापित हुईं, जिन्होंने भारतीय जनमानस को जागरूक करने के साथ-साथ भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य किया।
ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज जैसे संगठनों ने भारतीय संस्कृति और भाषा को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार, थियोसोफिकल सोसायटी और रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थानों ने भी भारतीय समाज को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से संगठित करते हुए मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की प्रासंगिकता को बल दिया।
| नाम | मुख्यालय | स्थापना | संस्थापक |
|---|---|---|---|
| ब्रह्म समाज | कलकत्ता | 1828 ई. | राजा राम मोहन राय |
| प्रार्थना समाज | बंबई | 1867 ई. | आत्मारंग पाण्डुरंग |
| आर्य समाज | बंबई | 1875 ई. | स्वामी दयानंद सरस्वती |
| थियोसोफिकल सोसायटी | अडयार (मद्रास) | 1882 ई. | कर्नल एच. एस. आल्काट एवं मैडम ब्लावात्स्की |
| सनातन धर्म सभा (1902 से भारत धर्म महामंडल) | वाराणसी | 1895 ई. | पं० दीन दयाल शर्मा |
| रामकृष्ण मिशन | बेलूर | 1897 ई. | स्वामी विवेकानंद |
राष्ट्रभाषा से संबंधित साहित्यिक संस्थाएँ
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार को विशेष महत्व दिया गया। इसके लिए कई साहित्यिक और शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित हुईं, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा (1893) ने हिंदी को साहित्यिक रूप से सशक्त बनाया, जबकि प्रयाग का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (1910) हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की प्रमुख आवाज़ बना।
इसी क्रम में गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और हिन्दुस्तानी एकेडमी जैसी संस्थाओं ने हिंदी को शैक्षणिक और व्यावहारिक स्तर पर आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत में भी हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास, 1927) जैसी संस्थाएँ स्थापित हुईं, जिसने हिंदी को अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित करने का कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, नागरी लिपि परिषद और अन्य संस्थाओं ने हिंदी के विकास को और अधिक गति प्रदान की।
| नाम | मुख्यालय | स्थापना | विशेष तथ्य |
|---|---|---|---|
| नागरी प्रचारिणी सभा | काशी/वाराणसी | 1893 ई. | संस्थापक त्रयी – श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह |
| हिन्दी साहित्य सम्मेलन | प्रयाग | 1910 ई. | प्रथम सभापति – मदन मोहन मालवीय |
| गुजरात विद्यापीठ | अहमदाबाद | 1920 ई. | महात्मा गांधी के प्रयासों से |
| बिहार विद्यापीठ | पटना | 1921 ई. | – |
| हिन्दुस्तानी एकेडमी | इलाहाबाद | 1927 ई. | – |
| दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (पूर्व नाम: हिन्दी साहित्य सम्मेलन) | मद्रास | 1927 ई. | – |
| हिन्दी विद्यापीठ | देवघर | 1929 ई. | – |
| राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | वर्धा | 1936 ई. | – |
| महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा | पुणे | 1937 ई. | – |
| बंबई हिन्दी विद्यापीठ | बंबई | 1938 ई. | – |
| असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति | गुवाहटी | 1938 ई. | – |
| बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् | पटना | 1951 ई. | – |
| अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ | नई दिल्ली | 1964 ई. | – |
| नागरी लिपि परिषद् | नई दिल्ली | 1975 ई. | – |
हिन्दी का वर्तमान स्वरूप
आज भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हिन्दी केवल उत्तरी भारत तक सीमित नहीं, बल्कि दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत में भी सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है।
- राजभाषा के रूप में : केन्द्र सरकार के कार्यों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है।
- संपर्क भाषा के रूप में : विभिन्न राज्यों के लोग परस्पर संवाद के लिए हिन्दी का प्रयोग करते हैं।
- सांस्कृतिक भाषा के रूप में : साहित्य, सिनेमा, संगीत और मीडिया के माध्यम से हिन्दी का प्रसार वैश्विक स्तर पर हो चुका है।
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की विशेषताएँ
- व्यापक जनाधार – यह देश की लगभग आधी आबादी की मातृभाषा है।
- संपर्क भाषा – विभिन्न भाषाई समुदायों को जोड़ने का माध्यम है।
- भावनात्मक लगाव – जनता का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव हिन्दी से है।
- लचीलापन – हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता है।
- सांस्कृतिक प्रतीक – स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता की ध्वजा-वाहक भाषा है।
स्वतंत्रता के बाद हिन्दी की स्थिति : राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच
भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रभाषा का प्रश्न और भी अधिक प्रासंगिक हो गया। संविधान सभा में व्यापक बहस के बाद यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी को राजभाषा घोषित किया जाए, किन्तु अंग्रेज़ी को भी 15 वर्षों तक सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा जाए। यह व्यवस्था मूल रूप से अस्थायी थी, किन्तु गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के विरोध और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अंग्रेज़ी का प्रयोग आगे भी जारी रहा।
स्वतंत्रता के बाद हिन्दी ने शिक्षा, साहित्य, प्रसार माध्यम, राजनीति और आम जनजीवन में अपनी पहुँच को निरंतर विस्तृत किया। रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा के माध्यम से हिन्दी ने सम्पूर्ण भारत में संपर्क और अभिव्यक्ति की प्रभावशाली भाषा का रूप ग्रहण किया। यही नहीं, संसद की कार्यवाही, सरकारी अधिसूचनाएँ और नीतिगत दस्तावेजों में हिन्दी का प्रयोग लगातार बढ़ता गया। इस प्रकार हिन्दी ने राष्ट्रभाषा की भावनात्मक भूमिका और राजभाषा की प्रशासनिक भूमिका, दोनों को ही निभाने का प्रयास किया।
हालाँकि, चुनौतियाँ भी कम नहीं रहीं। दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में हिन्दी के प्रति विरोध दिखाई दिया। उच्च शिक्षा, न्यायपालिका और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अंग्रेज़ी का वर्चस्व बना रहा। परिणामस्वरूप, हिन्दी सम्पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी का स्थान नहीं ले सकी।
फिर भी, यह निर्विवाद सत्य है कि हिन्दी आज भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। उसने न केवल राजभाषा के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि राष्ट्रभाषा के भावनात्मक स्वरूप को भी सुदृढ़ किया। हिन्दी आज भी भारतीय एकता, सांस्कृतिक अस्मिता और जनसंपर्क की सबसे बड़ी धरोहर बनी हुई है।
निष्कर्ष
भारत की कोई संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं है, किन्तु व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टि से हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। यह भाषा न केवल प्रशासनिक और शैक्षिक प्रयोजनों की राजभाषा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक भी है।
महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और अन्य नेताओं ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। संविधान सभा ने इसे राजभाषा का दर्जा देकर अंग्रेजी के साथ सहअस्तित्व का मार्ग प्रशस्त किया।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हिन्दी को केवल राजभाषा न मानकर, राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहार में लाएँ। क्योंकि वास्तव में यही वह भाषा है जो जन-जन के हृदय से जुड़ी है और जो भारत की आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति है।
इन्हें भी देखें –
- राजभाषा : भारत की राजभाषा, राज्यों की राजभाषाएं, परिभाषा, महत्व और सूची
- मातृभाषा: परिभाषा, अर्थ, विशेषताएँ और दिवस – संस्कृति, पहचान और अभिव्यक्ति का आधार
- भारत की भाषाएँ: संवैधानिक मान्यता, आधिकारिक स्वरूप और विश्व परिप्रेक्ष्य में भाषाई विविधता
- हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह : अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलन्त | परिभाषा, प्रयोग एवं महत्व
- हिंदी भाषा के स्वर : परिभाषा, प्रकार और भेद
- भारतीय आर्यभाषाओं का ऐतिहासिक विकास: प्राचीन से आधुनिक काल तक
- भाषा और लिपि : उद्भव, विकास, अंतर, समानता और उदाहरण
- दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर के मालिक: एलन मस्क की अभूतपूर्व उपलब्धि
- रीतिकाल के कवि और रचनाएँ
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष: शताब्दी उत्सव, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी
- दशहरा 2025: राम, रावण और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी