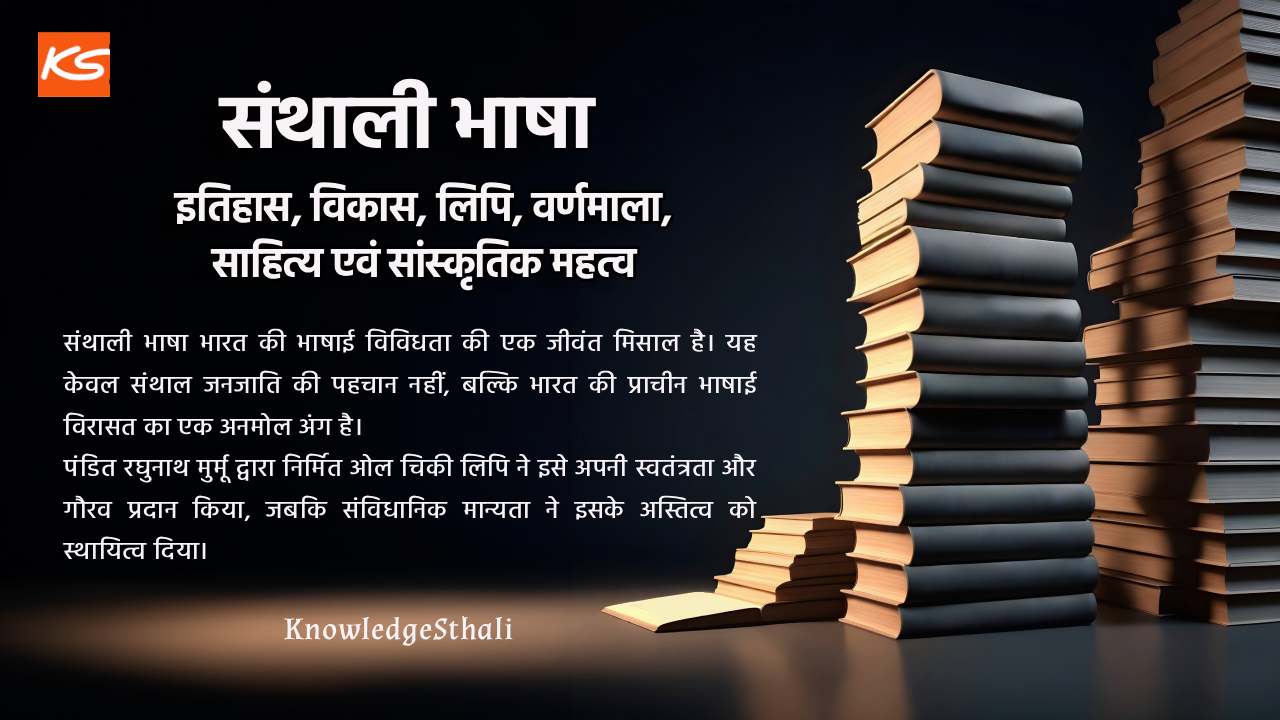भारत विविध भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों का देश है, जहाँ प्रत्येक भाषा अपने भीतर एक विशिष्ट पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा समेटे हुए है। इन्हीं भाषाओं में से एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध भाषा है — संथाली भाषा, जो भारत के आदिवासी समुदाय संथाल जनजाति की मातृभाषा है। यह भाषा न केवल झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बोली जाती है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक जड़ें असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा तक फैली हुई हैं।
संथाली भाषा ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है, जिसमें हो, मुण्डारी और भूमिज जैसी भाषाएँ भी सम्मिलित हैं। भारत में लगभग 76 लाख लोग इस भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा बन जाती है।
संथाली भाषा का परिचय (Introduction to Santali Language)
संथाली भाषा भारत की एक प्राचीन और जीवंत जनजातीय भाषा है, जो ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है। यह भाषा मुख्यतः संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है, जो भारत के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा राज्यों में व्यापक रूप से निवास करती है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसके बोलने वाले लोग पाए जाते हैं।
संथाली भारत में बोली जाने वाली प्रमुख जनजातीय भाषाओं में से एक है, जिसके करीब 76 लाख से अधिक मातृभाषी वक्ता हैं। यह भाषा अपनी विशिष्ट ध्वनि-प्रणाली, शब्द संरचना और लिपि के कारण अन्य भारतीय भाषाओं से भिन्न पहचान रखती है।
संथाली की लिपि “ओल चिकी (Ol Chiki)” है, जिसे 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। इस लिपि के निर्माण ने न केवल संथाली भाषा को एक लिखित स्वरूप प्रदान किया, बल्कि संथाल समुदाय की सांस्कृतिक एकता और आत्मगौरव को भी सुदृढ़ किया।
आज संथाली भाषा न केवल भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं (Constitutional Languages) में शामिल है, बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसे अतिरिक्त आधिकारिक भाषा (Additional Official Language) का दर्जा भी प्राप्त है।
संथाली भाषा अपने साहित्य, लोकगीतों, परंपराओं और बोलचाल की मधुरता के कारण भारतीय भाषाई परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है। यह केवल एक भाषा नहीं, बल्कि संथाल जनजाति की सांस्कृतिक आत्मा और पहचान का प्रतीक है, जो हजारों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप की बहुसांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग बनी हुई है।
संथाली भाषा का भाषाई परिवार और क्षेत्रीय प्रसार
| लिपि | ओल चिकी (ऑस्ट्रो-एशियाटिक) |
| बोली क्षेत्र | असम, झारखंड, ओड़िशा, छत्तीसगढ, बिहार, त्रिपुरा तथा बंगाल में संताल जनजाति |
| वक्ता | 76 लाख |
| परिवार | मुंडा भाषा परिवार (ऑस्ट्रो-एशियाटिक) |
| आधिकारिक भाषा | झारखंड, पश्चिम बंगाल |
संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की मुंडा शाखा से है। यह वही परिवार है जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया की कई भाषाएँ, जैसे — खमेर (कंबोडिया), वियतनामी (वियतनाम) और मोन (म्यांमार), भी संबंधित हैं। इस दृष्टि से संथाली भाषा भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण भाषाई कड़ी के रूप में देखी जाती है।
भारत में यह भाषा मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा राज्यों में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती देशों — बांग्लादेश, नेपाल, और भूटान में भी संथाली भाषी समुदाय विद्यमान हैं।
झारखंड के दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, और साहेबगंज जिलों में संथाली प्रमुख रूप से बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में यह बीरभूम, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में व्यापक रूप से प्रचलित है, जबकि ओडिशा में मयूरभंज और क्योंझर क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई देता है।
संथाली भाषा के वक्ता और संवैधानिक स्थिति
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार संथाली भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 76 लाख है। यह आंकड़ा इसे न केवल भारत की प्रमुख जनजातीय भाषाओं में शामिल करता है, बल्कि इसे भारत की 22 संवैधानिक भाषाओं (आठवीं अनुसूची में सम्मिलित) में से एक का दर्जा भी दिलाता है।
संथाली को झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार, इसे न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी समान अधिकार प्राप्त हैं। इस मान्यता ने संथाली भाषा के विकास, शिक्षा में इसके प्रयोग और सरकारी कार्यक्रमों में इसके उपयोग को बढ़ावा दिया है।
संथाली भाषा की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
संथाली भाषा की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है। भाषावैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी जड़ें हजारों वर्ष पूर्व की हैं और यह भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले प्रारंभिक ऑस्ट्रो-एशियाटिक समुदायों की भाषाओं में से एक है।
(1) प्राचीन काल और मौखिक परंपरा
संथाली भाषा का प्राचीन स्वरूप लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह लंबे समय तक मौखिक परंपरा पर आधारित रही। संताल समाज में गीत, लोककथाएँ, पहेलियाँ, धार्मिक मंत्र और कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संचारित होती रहीं। इस काल में संताली भाषा का प्रमुख माध्यम संगीत और नृत्य था — विशेष रूप से बाहा, सोहराय, करम जैसे त्योहारों में संताली गीतों का प्रयोग होता रहा।
इस मौखिक परंपरा ने संताली संस्कृति को जीवंत बनाए रखा और इसे सामाजिक एकता का माध्यम बनाया। भाषा का ध्वन्यात्मक स्वरूप (phonetic structure) अत्यंत समृद्ध है — इसमें स्वर और व्यंजनों की बड़ी संख्या के साथ-साथ विशिष्ट तानवाला प्रणाली (tonal system) विकसित हुई है।
(2) औपनिवेशिक काल और रोमन लिपि का प्रयोग
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, मिशनरियों ने संथाली भाषा में धार्मिक ग्रंथों और शिक्षण सामग्री के अनुवाद के प्रयास किए। इसी दौरान संताली भाषा को रोमन लिपि में लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई।
1840 के दशक में डेनमार्क के मिशनरी रेवरेंड जे. पी. स्कॉट और जे. कैंडल ने संताली के शब्दकोश और व्याकरण तैयार किए, जिससे यह भाषा यूरोपीय विद्वानों के अध्ययन का विषय बनी। हालांकि, उस समय यह प्रयास औपनिवेशिक उद्देश्यों से प्रेरित था, फिर भी इसने भाषा के संरक्षण में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई।
(3) ओल चिकी लिपि का आविष्कार – एक क्रांतिकारी परिवर्तन
संथाली भाषा का वास्तविक पुनर्जागरण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, जब पंडित रघुनाथ मुर्मू (1905–1982) ने “ओल चिकी” (Ol Chiki) लिपि का निर्माण किया।
उन्होंने यह महसूस किया कि संथाली भाषा की विशिष्ट ध्वनियाँ और संरचनाएँ देवनागरी या रोमन लिपि में सही रूप से व्यक्त नहीं हो सकतीं। इसलिए उन्होंने एक स्वतंत्र लिपि प्रणाली विकसित की, जिसमें भाषा के उच्चारण और ध्वनि-संरचना के अनुरूप प्रतीकों का निर्माण किया गया।
ओल चिकी लिपि में 30 अक्षर होते हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों का स्पष्ट भेद होता है। यह लिपि बाएँ से दाएँ लिखी जाती है, और इसका स्वरूप ध्वन्यात्मक रूप से अत्यंत सटीक है।
रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित “बिदू छाड़ा” और “दारोम तेताङ” जैसे नाटक इस लिपि के माध्यम से संथाली साहित्य की नींव बने।
संथाली भाषा का विकास क्रम
संथाली भाषा का विकास विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित रहा है। इसे चार प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है —
1. प्रारंभिक काल (मौखिक परंपरा का युग)
इस चरण में संथाली पूरी तरह से मौखिक माध्यम रही। गीत, नृत्य, कहानियाँ और मिथक भाषा के संरक्षण का साधन थे। इस काल में भाषा का प्राकृतिक रूप सुरक्षित रहा, क्योंकि बाहरी प्रभाव न्यूनतम थे।
2. औपनिवेशिक काल (1840–1900)
मिशनरी गतिविधियों के कारण संथाली का संपर्क अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं से हुआ। मिशनरियों ने भाषा का अध्ययन किया, जिससे शब्दकोश और व्याकरण बने। हालाँकि यह प्रयास सीमित समुदायों तक ही रहा।
3. ओल चिकी युग (1905–1982)
रघुनाथ मुर्मू के आविष्कार के बाद संथाली भाषा ने अपनी स्वतंत्र पहचान प्राप्त की। ओल चिकी लिपि ने न केवल भाषा को एक औपचारिक स्वरूप दिया, बल्कि संताली समुदाय में सांस्कृतिक आत्मगौरव भी स्थापित किया।
4. आधुनिक काल (1980 के बाद से वर्तमान तक)
इस काल में संथाली भाषा को शिक्षा, साहित्य, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से व्यापक प्रसार मिला। 2003 में इसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, जिससे इसका राष्ट्रीय स्तर पर पुनरुत्थान हुआ।
संथाली भाषा की लिपि : ओल चिकी का विकास और विशेषताएँ
प्रारंभिक काल में संथाली भाषा केवल मौखिक परंपरा तक सीमित थी और इसके लिए कोई निश्चित लिपि प्रचलन में नहीं थी। संताल समाज अपनी परंपराओं, गीतों और लोककथाओं को मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता रहा। किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, संताली भाषा को एक लिखित रूप प्रदान करने का महान कार्य पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया। उन्होंने सन् 1925 में संताली भाषा की ध्वन्यात्मक संरचना के अनुरूप एक स्वतंत्र लिपि — ओल चिकी (Ol Chiki) — का आविष्कार किया।
ओल चिकी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अल्फाबेटिक (alphabetic) है, न कि पारंपरिक भारतीय लिपियों की तरह सिलेबिक (syllabic)। इस कारण प्रत्येक अक्षर स्वतंत्र ध्वनि या वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे भाषा के उच्चारण को सटीकता से व्यक्त किया जा सकता है। लिपि बाएँ से दाएँ लिखी जाती है, और इसके प्रत्येक चिन्ह को इस प्रकार बनाया गया है कि वह संताली के स्वर और व्यंजन दोनों को स्पष्ट रूप से दर्शाए।
इस लिपि में विशेष ध्वन्यात्मक चिह्न (diacritical marks) का प्रयोग भी किया जाता है, जो स्वर या उच्चारण के स्वरूप को इंगित करते हैं। ओल चिकी की यह विशिष्टता इसे अन्य भारतीय लिपियों से भिन्न बनाती है। इसकी सरलता और ध्वन्यात्मक सटीकता के कारण आज यह संताली भाषा की आधिकारिक और मानक लिपि के रूप में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जा रही है।
ओल चिकी का निर्माण न केवल एक भाषाई उपलब्धि थी, बल्कि इसने संथाली समाज को अपनी पहचान, गौरव और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी प्रदान किया। आज शिक्षा, साहित्य, प्रशासन और डिजिटल माध्यमों में इस लिपि का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे संताली भाषा का भविष्य और भी उज्ज्वल होता जा रहा है।
संथाली भाषा की वर्णमाला और ध्वन्यात्मक विशेषताएँ
संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी (Ol Chiki) में लिखी जाती है, जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में विकसित किया था। यह एक अक्षरात्मक (alphabetic) लिपि है, जिसमें प्रत्येक वर्ण एक स्वतंत्र ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ओल चिकी लिपि बाएँ से दाएँ लिखी जाती है और इसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के लिए विशिष्ट प्रतीक निर्धारित हैं।
संथाली वर्णमाला की ध्वनियाँ अत्यंत सुसंगत हैं और इनका उच्चारण अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि (IPA) के अनुरूप किया जा सकता है। नीचे तालिका में कुछ प्रमुख वर्ण, उनके उच्चारण, आईपीए संकेत और अन्य भारतीय लिपियों (देवनागरी, बंगाली, ओड़िया) में उनके समतुल्य रूप दिए गए हैं —
| ओल चिकी वर्ण | उच्चारण | आईपीए (IPA) | देवनागरी | बंगाली | ओड़िया |
|---|---|---|---|---|---|
| ᱚ | la | /ɔ/ | अ / ऑ | অ | ଅ |
| ᱟ | laa | /a/ | आ | আ | ଆ |
| ᱤ | li | /i/ | ई | ই | ଇ |
| ᱩ | lu | /u/ | उ | উ | ଉ |
| ᱶ | ov | /w̃/ | उं | ঁ | ଁ |
| ᱮ | le | /e/ | ए | এ | ଏ |
| ᱳ | lo | /o/ | ओ | ও | ଓ |
| ᱠ | aak | /k/ | क | ক | କ |
| ᱜ | ag | /k’/, /g/ | ग | গ | ଗ |
| ᱝ | ang | /ŋ/ | ं | ং | ଂ |
| ᱪ | uch | /c/ | च | চ | ଚ |
| ᱡ | aaj | /c’/, /j/ | ज | জ | ଜ |
| ᱧ | iny | /ɲ/ | ञ | ঞ | ଞ |
| ᱴ | ott | /ʈ/ | ट | ট | ଟ |
| ᱰ | edd | /ɖ/ | ड | ড | ଡ |
| ᱲ | err | /ɽ/ | ड़ | ড় | ଳ |
| ᱬ | unn | /ɳ/ | ण | ণ | ଣ |
| ᱛ | at | /t/ | त | ত | ତ |
| ᱫ | ud | /t’/, /d/ | द | দ | ଦ |
| ᱱ | en | /n/ | न | ন | ନ |
| ᱯ | ep | /p/ | प | প | ପ |
| ᱵ | ob | /p’/, /b/ | ब | ব | ବ |
| ᱢ | aam | /m/ | म | ম | ମ |
| ᱭ | uy | /j/ | य | য় | ୟ |
| ᱨ | ir | /r/ | र | র | ର |
| ᱞ | al | /l/ | ल | ল | ଲ |
| ᱣ | aaw | /w/, /v/ | व | ওয় | ୱ |
| ᱥ | is | /s/ | स | স | ସ |
| ᱦ | ih | /ʔ/, /h/ | ह | হ | ହ |
| ᱷ | oh | /ʰ/ | ह (आस्पि.) | হ | ହ |
इस प्रकार, संथाली वर्णमाला ध्वन्यात्मक रूप से अत्यंत व्यवस्थित है, जो इसे अन्य भारतीय लिपियों से विशिष्ट बनाती है। ओल चिकी लिपि के प्रत्येक अक्षर में ध्वनि की स्पष्ट पहचान होती है, जिससे भाषा का उच्चारण और लेखन दोनों ही अत्यंत सटीक बनते हैं।
संथाली भाषा में संख्याएँ (ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱡ ᱠᱚᱱᱚ)
संथाली भाषा में संख्याएँ भी ओल चिकी लिपि में लिखी जाती हैं, जो इसके पूर्णत: स्वदेशी स्वरूप को दर्शाती हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा निर्मित इस लिपि में शून्य से नौ (0–9) तक के प्रत्येक अंक का अपना विशिष्ट प्रतीक है। ये अंक न केवल लिखने में सरल हैं, बल्कि ध्वन्यात्मक रूप से भी स्वतंत्र और स्पष्ट हैं।
संथाली अंकों की तुलना अन्य प्रमुख भारतीय लिपियों — देवनागरी, बंगाली और ओड़िया — के अंकों से नीचे दी गई तालिका में की गई है:
| अंक (संख्या) | ओल चिकी | बांग्ला | देवनागरी | ओड़िया |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ᱐ | ০ | ० | ୦ |
| 1 | ᱑ | ১ | १ | ୧ |
| 2 | ᱒ | ২ | २ | ୨ |
| 3 | ᱓ | ৩ | ३ | ୩ |
| 4 | ᱔ | ৪ | ४ | ୪ |
| 5 | ᱕ | ৫ | ५ | ୫ |
| 6 | ᱖ | ৬ | ६ | ୬ |
| 7 | ᱗ | ৭ | ७ | ୭ |
| 8 | ᱘ | ৮ | ८ | ୮ |
| 9 | ᱙ | ৯ | ९ | ୯ |
इन अंकों का उपयोग संथाली साहित्य, प्रशासनिक अभिलेखों और शिक्षा में किया जाता है।
ओल चिकी लिपि की अंक प्रणाली यह दर्शाती है कि संथाली भाषा केवल ध्वन्यात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि गणनात्मक रूप से भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखती है — जिससे यह भारत की समृद्ध भाषाई परंपरा में एक पूर्ण विकसित और स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है।
संथाली भाषा की शब्द संरचना (Word Structure in Santali)
संथाली भाषा की शब्द संरचना सरल, स्पष्ट और अत्यंत लचीली है। इस भाषा के अधिकांश शब्द एक या दो शब्दांशों (syllables) से बने होते हैं, जबकि कुछ जटिल शब्द तीन या उससे अधिक अक्षरों के संयोजन से निर्मित होते हैं। संथाली में स्वरों और व्यंजनों की समृद्ध ध्वनि प्रणाली मौजूद है, जो समान ध्वनि वाले शब्दों के बीच अर्थ का सूक्ष्म अंतर स्पष्ट करती है।
संथाली भाषा की यह विशेषता इसे एक सहज, प्राकृतिक और मधुर बोली बनाती है। इसके शब्द दैनिक जीवन, प्रकृति, परिवार और भावनाओं से गहराई से जुड़े होते हैं।
संथाली के शब्द सामान्यतः प्रकृति, परिवार, प्रेम, आस्था और दैनिक जीवन से जुड़े विषयों को अभिव्यक्त करते हैं। नीचे संथाली भाषा के कुछ सामान्य शब्दों के उदाहरण हिंदी और अंग्रेज़ी अर्थ सहित दिए गए हैं —
| संथाली (ओल चिकी) | लिप्यंतरण (Transliteration) | अर्थ (हिंदी में) | Meaning (in English) |
|---|---|---|---|
| ᱟᱢᱢᱟ | Amma | माँ | Mother |
| ᱵᱟᱵᱟ | Baba | पिता | Father |
| ᱫᱤᱫᱤ | Didi | बड़ी बहन | Elder Sister |
| ᱵᱷᱟᱭ | Bhai | भाई | Brother |
| ᱫᱩᱞᱟᱨ | Dular | प्यार | Love |
| ᱠᱷᱟᱱᱟ | Khana | खाना / भोजन | Food |
| ᱱᱚᱠᱥᱟ | Noksa | नहीं | No |
| ᱦᱟᱱ | Han | हाँ | Yes |
| ᱟᱥᱟ | Aasa | आशा | Hope |
| ᱡᱤᱵᱚᱱ | Jibon | जीवन | Life |
| ᱵᱚᱝᱜᱟ | Bonga | देवता / आत्मा | Spirit / Deity |
| ᱦᱟᱯᱨᱟᱢ | Hapram | पूर्वज / पुरखे | Ancestor |
| ᱫᱟᱠᱟ | Daka | बुलाना | To call |
| ᱪᱟᱴᱟ | Chata | छाता | Umbrella |
| ᱜᱩᱫᱤ | Gudi | घर | House |
| ᱯᱳᱨᱟ | Pora | पढ़ना | To read |
| ᱥᱟᱜᱩᱱ | Sagun | शुभ संकेत | Auspicious sign |
| ᱨᱩᱯᱤ | Rupi | स्त्री | Woman |
| ᱦᱚᱨ | Hor | मनुष्य / व्यक्ति | Human / Person |
इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि संथाली शब्दावली प्रकृति, पारिवारिक संबंधों, सामाजिक जीवन और भावनात्मक अनुभवों को सरल शब्दों में व्यक्त करती है।
भाषा की ध्वन्यात्मकता और शब्दों की संरचनात्मक लयात्मकता इसे गीत, कथा और संवाद के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है।
संथाली शब्दों में ध्वनि और अर्थ का यह सामंजस्य इसकी मौलिकता और सांस्कृतिक आत्मा का परिचायक है, जो इसे भारत की अन्य भाषाओं से अलग और विशिष्ट बनाता है।
संथाली साहित्य : मौखिक परंपरा से आधुनिक लेखन तक
संथाली साहित्य भारतीय जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का एक अद्वितीय और समृद्ध अध्याय है। यह साहित्य अपनी मौखिक परंपराओं, लोकगीतों, भजनों, कहावतों और समसामयिक रचनाओं के माध्यम से संथाल समाज की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। प्रारंभ में यह पूरी तरह से मौखिक रूप में विकसित हुआ था, किंतु ओल चिकी लिपि के आविष्कार के पश्चात् इसे लिखित स्वरूप मिला और इसका साहित्यिक संसार तेजी से विस्तारित हुआ।
मौखिक परंपरा और लोककथाएँ
संथाली साहित्य की जड़ें इसके लोकजीवन में गहराई तक फैली हुई हैं। संथाल समुदाय की लोककथाएँ और किंवदंतियाँ न केवल मनोरंजन का माध्यम रही हैं, बल्कि उन्होंने समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी संरक्षित किया है। इन कथाओं में अक्सर प्रकृति, पशु-पक्षी, आत्माएँ और अलौकिक शक्तियाँ प्रमुख पात्रों के रूप में दिखाई देती हैं।
इन कहानियों के माध्यम से जीवन के नैतिक सिद्धांत, सामाजिक एकता और मानव-प्रकृति संबंध का संदेश दिया जाता है। विशेष रूप से “बहा” जैसी पारंपरिक कथन-शैली में एक कथावाचक वीर नायकों के पराक्रम, संघर्ष और लोक-निष्ठा का वर्णन करता है। यह कथा-वाचन परंपरा आज भी ग्रामीण समाज में जीवित है।
धार्मिक गीत और भजन परंपरा
संथाली समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग हैं संथाल भजन — ये भक्ति और आस्था के प्रतीक हैं। संताली भाषा में रचे गए ये भजन मारंग बुरू (परमेश्वर), जाहेर आयो (वनदेवी) और अन्य स्थानीय देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं।
इन गीतों में संताल जीवन की गहराई, उनकी आस्था, उनके पर्व और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का सुंदर चित्रण मिलता है। इन भजनों ने न केवल धार्मिक जीवन को समृद्ध किया, बल्कि संताली भाषा को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी दी।
कहावतें और जनजीवन का व्यावहारिक ज्ञान
संथाली साहित्य में खेरवाल बीर नामक कहावतों का संग्रह अत्यंत प्रसिद्ध है। इन कहावतों में संथाल समाज की जीवन-दृष्टि, अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान समाहित है।
ये कहावतें न केवल नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि जनजीवन के गहन अवलोकन से उत्पन्न बुद्धिमत्ता को भी दर्शाती हैं। जैसे अन्य भारतीय भाषाओं में लोकोक्तियाँ समाज की चेतना का दर्पण होती हैं, उसी प्रकार संथाली कहावतें संताल संस्कृति की व्यावहारिक संवेदना को प्रकट करती हैं।
लिखित साहित्य का उद्भव और ओल चिकी का योगदान
संथाली साहित्य की वास्तविक प्रगति तब आरंभ हुई जब पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में ओल चिकी लिपि का निर्माण किया। इस आविष्कार ने संताली साहित्य को एक स्थायी लेखन-परंपरा प्रदान की।
रघुनाथ मुर्मू न केवल एक भाषाविद् थे, बल्कि वे संथाली साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। उनके नाटक, गीत और कविताएँ — जैसे “दारोम तेताङ” और “बिदू छाड़ा” — आज भी संथाल समाज की सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखते हैं।
उन्होंने साहित्य के माध्यम से भाषा, समाज और संस्कृति के पुनरुत्थान का कार्य किया, जिससे संथाली भाषा एक नई ऊर्जा और पहचान के साथ उभरी।
आधुनिक संताली साहित्य और समकालीन रचनाकार
ओल चिकी लिपि के बाद संथाली साहित्य ने आधुनिकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए। अनेक रचनाकारों ने कविता, उपन्यास, नाटक और आलोचना जैसे साहित्यिक विधाओं में योगदान दिया।
रामचंद्र मुर्मू, लखन सोरेन, कार्तिक चन्द्र तुडू, जोनास तुडू, सुधांशु बेसरा जैसे लेखकों ने संताली साहित्य को नई दृष्टि और सामाजिक चेतना से संपन्न किया।
उनकी रचनाओं में संथाल जनजीवन, आदिवासी संघर्ष, प्रकृति-प्रेम और सांस्कृतिक अस्मिता की गहन झलक मिलती है।
आज All India Santali Writers’ Association जैसी संस्थाएँ संताली साहित्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठित करने में सक्रिय हैं। साथ ही, विश्वविद्यालयों में संताली साहित्य पर शोध और अध्ययन को भी बढ़ावा मिल रहा है।
साहित्य में विषय-विविधता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति
संथाली साहित्य की विषय-वस्तु अत्यंत व्यापक है। इसमें धार्मिक आस्था, प्रकृति के प्रति श्रद्धा, सामाजिक संघर्ष, प्रेम, श्रम, उत्सव और पर्यावरणीय चेतना — सबका समावेश है।
लोकगीतों और कविताओं में संथाल समाज की सामूहिकता, नृत्य और संगीत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक संताली साहित्य ने न केवल पारंपरिक विषयों को अपनाया, बल्कि शिक्षा, समानता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय संतुलन जैसे समकालीन मुद्दों पर भी अपनी रचनात्मक दृष्टि प्रकट की है।
संताली साहित्य का सांस्कृतिक महत्व
संथाली साहित्य केवल लेखन या रचना का माध्यम नहीं, बल्कि यह संथाल समुदाय की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। इसने समाज में सामूहिक पहचान, भाषा-गौरव और परंपरागत ज्ञान को सशक्त बनाया है।
भाषा के माध्यम से लोकसंस्कृति का संरक्षण हुआ और संथाल समुदाय ने अपने इतिहास, मिथकों और सामाजिक मूल्यों को संरक्षित रखा। यही कारण है कि संताली साहित्य आज भी जीवंत, प्रासंगिक और सतत विकसित हो रहा है।
संथाली साहित्य का सफर मौखिक परंपरा से लेकर आधुनिक लेखन तक का एक जीवंत साक्ष्य है। यह साहित्य संथाल समाज की चेतना, संघर्ष, प्रेम और प्रकृति-संबंधी दर्शन का दर्पण है।
भले ही इसकी शुरुआत लोकगीतों और कथाओं से हुई, पर आज यह उपन्यास, नाटक, कविता, आलोचना और पत्रकारिता जैसे विविध माध्यमों में फैल चुका है।
इस साहित्य ने न केवल संथाली भाषा को समृद्ध किया है, बल्कि भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक परिदृश्य को भी एक अनमोल धरोहर प्रदान की है।
संथाली भाषा में शिक्षा और मीडिया
वर्तमान में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संताली भाषा में शिक्षा दी जाती है।
झारखंड के सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (दुमका) में संताली भाषा विभाग की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, Ranchi University और Visva-Bharati University (शांतिनिकेतन) में भी संताली भाषा का अध्ययन और शोध हो रहा है।
मीडिया क्षेत्र में भी संताली भाषा ने मजबूत उपस्थिति दर्ज की है —
- आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों से संताली कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते हैं।
- झारखंड और ओडिशा में कई संताली समाचार पत्र जैसे Sarik Soren, Aj Sari, और Chando Dolo प्रकाशित होते हैं।
- डिजिटल युग में संताली ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन कोर्स भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
संथाली भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व
संताली भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि संताल जनजाति की सांस्कृतिक आत्मा है।
इस भाषा के माध्यम से उनकी धार्मिक मान्यताएँ, लोककथाएँ, उत्सव, नृत्य और गीत जीवंत हैं। सारहुल, सोहराय, करम, मागे पर्व जैसे उत्सवों में संताली गीतों की अनिवार्य भूमिका रहती है।
भाषा की विशिष्टता यह है कि यह प्रकृति, पर्यावरण और सामूहिकता के मूल्यों पर आधारित है — जो आज के आधुनिक समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं।
संथाली भाषा के समक्ष चुनौतियाँ
भले ही संताली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है, फिर भी इसके समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं —
- शहरीकरण और भाषाई परिवर्तन : युवा पीढ़ी में हिंदी और अंग्रेजी की ओर झुकाव बढ़ रहा है।
- शिक्षण सामग्री की कमी : ओल चिकी लिपि में उच्च शिक्षा स्तर की पर्याप्त पुस्तकें और संसाधन अभी सीमित हैं।
- तकनीकी समावेशन की समस्या : डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संताली भाषा के लिए सॉफ्टवेयर, फॉन्ट और कीबोर्ड सपोर्ट अभी भी सीमित हैं।
- अनुसंधान और संरक्षण की आवश्यकता : संताली की बोलियों, व्याकरण और लोक साहित्य पर गहन शोध की आवश्यकता है।
संरक्षण और पुनरुद्धार के प्रयास
भारत सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाएँ संथाली भाषा के संरक्षण के लिए सक्रिय हैं।
- 2003 में इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
- झारखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में संथाली को माध्यम के रूप में शामिल किया है।
- संथाली अकादमी, संथाली भाषा बोर्ड, और सिदो-कान्हू-मुर्मू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएँ इसके प्रचार-प्रसार में कार्यरत हैं।
- यूनिकोड में ओल चिकी लिपि को शामिल किया गया है, जिससे डिजिटल क्षेत्र में इसका प्रयोग संभव हुआ है।
निष्कर्ष
संथाली भाषा भारत की भाषाई विविधता की एक जीवंत मिसाल है। यह केवल संथाल जनजाति की पहचान नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन भाषाई विरासत का एक अनमोल अंग है।
पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा निर्मित ओल चिकी लिपि ने इसे अपनी स्वतंत्रता और गौरव प्रदान किया, जबकि संविधानिक मान्यता ने इसके अस्तित्व को स्थायित्व दिया।
आज आवश्यकता इस बात की है कि इस भाषा को आधुनिक तकनीक, शिक्षा और साहित्यिक मंचों से और अधिक जोड़ा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसकी समृद्ध परंपरा को जीवित रख सकें।
इस प्रकार, संथाली भाषा न केवल एक भाषाई माध्यम है, बल्कि यह भारत की जनजातीय संस्कृति, सामुदायिक एकता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता का प्रतीक भी है — एक ऐसी धरोहर जिसे सुरक्षित रखना सम्पूर्ण मानवता का उत्तरदायित्व है।
इन्हें भी देखें –
- भारत की शास्त्रीय भाषाएँ : भाषाई विरासत, मानदंड, विकास और महत्व
- नेपाली भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, वर्णमाला, दिवस और साहित्य
- संस्कृत भाषा : इतिहास, उत्पत्ति, विकास, व्याकरण, लिपि और महत्व
- तमिल भाषा : तमिलनाडु की भाषा, उत्पत्ति, विकास, लिपि, वर्णमाला, इतिहास और वैश्विक महत्व
- तेलुगु भाषा : इतिहास, लिपि, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, विकास और साहित्यिक परंपरा
- मलयालम भाषा : इतिहास, उत्पत्ति, लिपि, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, विकास और साहित्य
- कोंकणी भाषा : इतिहास, विकास, लिपि, वर्णमाला, शब्द-संरचना, वाक्य-रचना और साहित्यिक विरासत
- कन्नड़ भाषा : उत्पत्ति, इतिहास, लिपि, वर्णमाला, शब्द, वाक्य और साहित्य
- कित्तूर की वीरांगना रानी चेन्नम्मा : भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): आदिवासी शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की ऐतिहासिक पहल