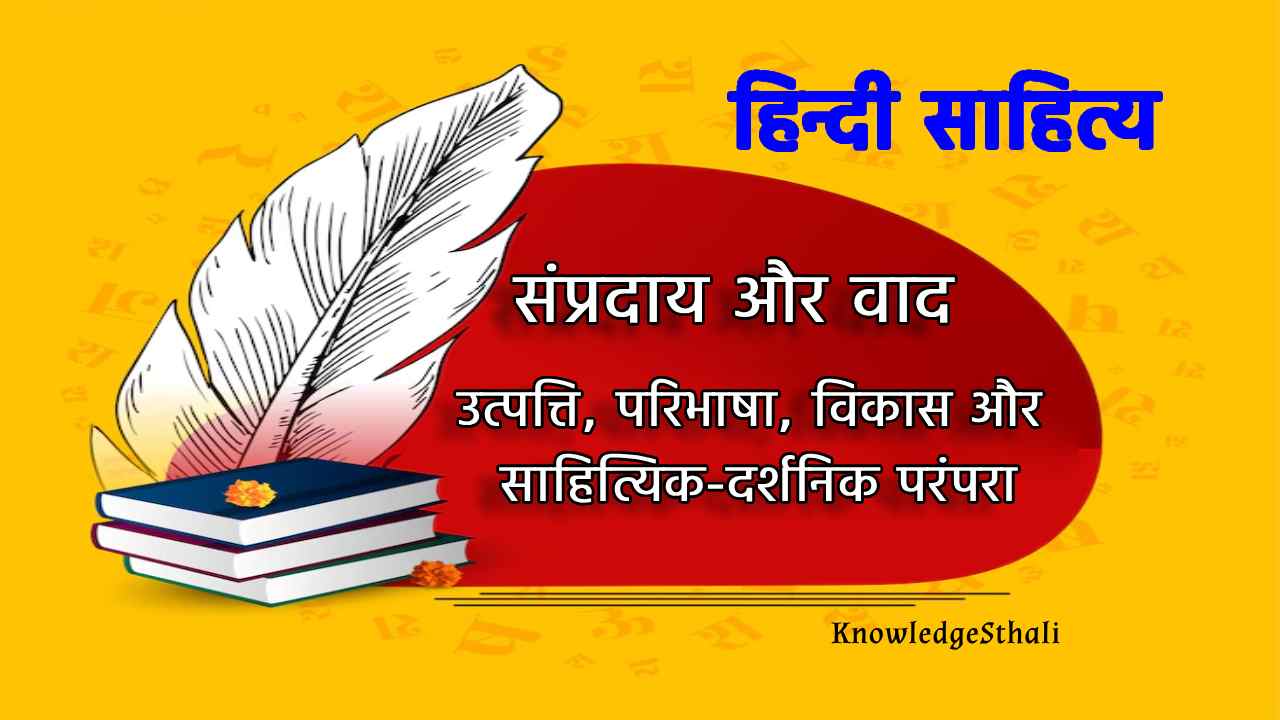मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ विचारधाराओं का उदय और विस्तार हुआ है। जब लोग किसी एक विचार, मान्यता या धार्मिक परंपरा को संगठित रूप से स्वीकार करते हैं और उसका अनुकरण करते हुए जीवन जीते हैं, तो उससे संप्रदाय का जन्म होता है। इसी प्रकार साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में जब किसी विशेष सिद्धांत या दृष्टिकोण को आधार बनाकर विचारों की धारा चलती है, तो उसे वाद कहा जाता है।
संप्रदाय और वाद, दोनों ही शब्द मानव की बौद्धिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक चेतना के विस्तार को दर्शाते हैं। धर्म में संप्रदाय का महत्व है तो साहित्य और काव्यशास्त्र में वादों का। यही कारण है कि भारतीय और पाश्चात्य चिंतन परंपरा में समय-समय पर विभिन्न संप्रदायों और वादों का उदय हुआ।
इस लेख में हम संप्रदाय और वाद की परिभाषा, उनके प्रकार, प्रमुख प्रवर्तकों तथा उनके योगदान का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।
संप्रदाय की परिभाषा और स्वरूप
संप्रदाय का शाब्दिक अर्थ है – संपत्ति, परंपरा या विचारधारा का समूह।
एक ही धर्म, दर्शन या सांस्कृतिक परंपरा के भीतर अलग-अलग विचारधाराओं को मानने वाले समूह को संप्रदाय कहा जाता है।
- संप्रदाय केवल धार्मिक नहीं होते, वे साहित्य, दर्शन, कला और राजनीति तक में देखे जा सकते हैं।
- हर संप्रदाय की अपनी आस्थाएँ, अनुष्ठान, पूजा-पद्धति और शिक्षाएँ होती हैं।
- संप्रदाय सामान्यतः किसी गुरु या प्रवर्तक की शिक्षाओं पर आधारित होते हैं।
वाद की परिभाषा और स्वरूप
वाद का अर्थ है – किसी विशेष विचारधारा या सिद्धांत पर आधारित साहित्यिक या दार्शनिक आंदोलन।
काव्यशास्त्र में वाद उस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को कहा जाता है जिसके आधार पर साहित्य की रचना और उसकी व्याख्या होती है।
- वाद प्रायः साहित्य और दर्शन से जुड़ा होता है।
- प्रत्येक वाद के पीछे एक प्रवर्तक (सिद्धांतकार या चिंतक) होता है।
- वाद समय-समय पर साहित्य के रूप, शैली, भाषा और अभिव्यक्ति को प्रभावित करते रहे हैं।
काव्यशास्त्र में संप्रदाय और वाद
भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास अत्यंत समृद्ध है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक विभिन्न संप्रदायों और वादों ने साहित्यिक प्रवृत्तियों को दिशा दी। वहीं पाश्चात्य साहित्य में भी अनेक वादों का उदय हुआ, जिन्होंने विश्व साहित्य को प्रभावित किया।
1. संस्कृत काव्यशास्त्र के संप्रदाय एवं प्रवर्तक
संस्कृत काव्यशास्त्र में अनेक महत्वपूर्ण संप्रदाय उत्पन्न हुए। ये संप्रदाय भारतीय साहित्यिक परंपरा की नींव माने जाते हैं।
| क्रम | संप्रदाय | प्रवर्तक | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| 1 | रस संप्रदाय | भरत मुनि | नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित; साहित्य का सार ‘रस’ है। |
| 2 | अलंकार संप्रदाय | भामह, मम्मट | साहित्य में सौंदर्य का आधार ‘अलंकार’। |
| 3 | रीति संप्रदाय | दण्डी, वामन | काव्य की आत्मा ‘रीति’ (शैली) मानी। |
| 4 | ध्वनि संप्रदाय | आनंदवर्धन | साहित्य का प्राण ‘ध्वनि’ अर्थात् अभिव्यक्ति का सूक्ष्म भाव। |
| 5 | वक्रोक्ति संप्रदाय | कुन्तक | साहित्य में ‘वक्रता’ (अप्रत्याशित, टेढ़ा-मेढ़ा कथन) का महत्व। |
| 6 | औचित्य संप्रदाय | क्षेमेन्द्र | काव्य में औचित्य (उचित संगति) ही सौंदर्य का आधार। |
इन संप्रदायों ने न केवल संस्कृत साहित्य बल्कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के काव्य को भी गहरे रूप से प्रभावित किया।
2. हिंदी काव्यशास्त्र के संप्रदाय एवं प्रवर्तक
हिंदी साहित्य का इतिहास विभिन्न वादों से परिपूर्ण है। यहाँ भाव, शैली और विचारधारा के आधार पर कई संप्रदाय उत्पन्न हुए।
| क्रम | वाद | प्रवर्तक | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| 7 | रीतिवाद | केशवदास (शुक्ल के अनुसार चिंतामणि) | काव्य का आधार रीति और रस। |
| 8 | स्वच्छंदतावाद | श्रीधर पाठक | व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वच्छंद अभिव्यक्ति। |
| 9 | छायावाद | जय शंकर प्रसाद | आत्मानुभूति, प्रकृति और रहस्यात्मकता। |
| 10 | हालावाद | हरिवंश राय बच्चन | जीवन की मधुरता और मदिरा-सौंदर्य का प्रतीकात्मक रूप। |
| 11 | प्रयोगवाद | अज्ञेय | नये प्रयोग और आधुनिक दृष्टिकोण। |
| 12 | प्रपद्यवाद/नकेनवाद | नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश | जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति। |
| 13 | मांसलवाद | रामेश्वर शुक्ल ‘अंचल’ | शरीर और कामना का यथार्थ चित्रण। |
| 14 | कैप्सूलवाद | ओकार नाथ त्रिपाठी | संक्षिप्त लेकिन प्रभावी अभिव्यक्ति। |
इन वादों ने हिंदी काव्य को नयी दिशाएँ दीं और उसे समयानुसार आधुनिक बनाया।
3. पाश्चात्य काव्यशास्त्र के संप्रदाय एवं प्रवर्तक
भारतीय काव्यशास्त्र की भांति पाश्चात्य साहित्य में भी अनेक वाद विकसित हुए।
| क्रम | वाद | प्रवर्तक | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| 15 | औदात्यवाद | लोंजाइनस (3री सदी ई.) | साहित्य का उद्देश्य उदात्तता और महत्ता। |
| 16 | अस्तित्ववाद | सॉरन कीर्कगार्द (1813–55) | मनुष्य के अस्तित्व और स्वतंत्रता पर बल। |
| 17 | मार्क्सवाद | कार्ल मार्क्स (1818–83) | वर्ग-संघर्ष और आर्थिक आधार पर साहित्य। |
| 18 | मनोविश्लेषणवाद | सिग्मंड फ्रॉयड (1856–1939) | अवचेतन मन और मानसिक प्रवृत्तियों की व्याख्या। |
| 19 | प्रतीकवाद | जीन मोरियस (1856–1910) | प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्ति। |
| 20 | अभिव्यंजनावाद | बेनेदेतो क्रोचे (1866–1952) | साहित्य में अंतर्ज्ञान और भाव की प्रधानता। |
| 21 | बिम्बवाद | टी. ई. हयूम (1883–1917) | बिम्बों और चित्रात्मक अभिव्यक्ति का महत्व। |
इन वादों ने आधुनिक विश्व साहित्य, विशेषकर कविता और उपन्यास, की शैली और विषयवस्तु को गहराई से प्रभावित किया।
धर्मों के संप्रदाय
धार्मिक संप्रदाय सबसे प्राचीन और प्रभावशाली संप्रदाय माने जाते हैं।
1. हिंदू धर्म के संप्रदाय
- शैव संप्रदाय – शिव को सर्वोच्च मानने वाले।
- वैष्णव संप्रदाय – विष्णु और उनके अवतार (राम, कृष्ण) की भक्ति।
- शाक्त संप्रदाय – शक्ति (देवी) की उपासना।
- सौर संप्रदाय – सूर्य की आराधना।
- गाणपत संप्रदाय – गणेश उपासक।
- नाथ संप्रदाय – मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ की परंपरा।
- दशनामी संप्रदाय – शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित संन्यासी परंपरा।
- श्रीकृष्ण प्रणामी संप्रदाय (निजानंद संप्रदाय) – कृष्ण भक्ति पर आधारित।
2. बौद्ध धर्म के संप्रदाय
- थेरवाद – मूल बौद्ध परंपरा।
- महायान – बोधिसत्व आदर्श पर आधारित।
- वज्रयान – मंत्र, तंत्र और साधना पर केंद्रित।
- झेन (Zen) – ध्यान और प्रत्यक्ष अनुभव।
- नवयान – डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रवर्तित।
3. इस्लाम के संप्रदाय
- सुन्नी – पैग़म्बर की सुन्नत और परंपरा का अनुसरण।
- शिया – अली और इमामों की परंपरा पर आधारित।
4. जैन धर्म के संप्रदाय
- श्वेतांबर – श्वेत वस्त्रधारी साधु।
- दिगंबर – नग्न तपस्या करने वाले साधु।
5. ईसाई धर्म के संप्रदाय
- रोमन कैथोलिक – पोप को सर्वोच्च मान्यता।
(बाद में प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय भी विकसित हुए।)
संप्रदाय और वाद का तुलनात्मक अध्ययन
- संप्रदाय मुख्यतः धर्म और अध्यात्म से संबंधित हैं, जबकि वाद साहित्य और दर्शन के क्षेत्र से।
- संप्रदाय का आधार भक्ति, आस्था और गुरु-परंपरा होती है, वहीं वाद का आधार सिद्धांत, तर्क और साहित्यिक प्रयोग।
- दोनों ही समाज और संस्कृति को नई दिशा देने का कार्य करते हैं।
समकालीन परिप्रेक्ष्य में महत्व
आज के समय में भी संप्रदाय और वाद का महत्व बना हुआ है।
- धार्मिक संप्रदाय सामाजिक एकता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- साहित्यिक वाद रचनाकारों को नये प्रयोगों और विचारों की प्रेरणा देते हैं।
- डिजिटल युग में भी नववाद और नवसंप्रदाय का उदय हो रहा है, जैसे – आधुनिक उत्तर-आधुनिकतावाद, नारीवाद, दलित साहित्य, पर्यावरण साहित्य आदि।
संप्रदाय एवं वाद : कालानुक्रमिक टाइमलाइन
| काल/शताब्दी | संप्रदाय/वाद | प्रवर्तक/प्रतिनिधि | प्रमुख विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| लगभग 2री सदी ई.पू. | रस संप्रदाय (संस्कृत) | भरतमुनि | नाट्यशास्त्र, साहित्य का सार रस। |
| 6ठी–7वीं सदी ई. | अलंकार संप्रदाय | भामह, मम्मट | काव्य की आत्मा अलंकार। |
| 7वीं–8वीं सदी ई. | रीति संप्रदाय | दण्डी, वामन | काव्य में रीति (शैली) की प्रधानता। |
| 9वीं सदी ई. | ध्वनि संप्रदाय | आनंदवर्धन | काव्य का प्राण ध्वनि। |
| 10वीं सदी ई. | वक्रोक्ति संप्रदाय | कुन्तक | साहित्य में वक्रता का महत्व। |
| 11वीं सदी ई. | औचित्य संप्रदाय | क्षेमेन्द्र | काव्य में औचित्य ही सौंदर्य। |
| 16वीं सदी ई. | रीतिवाद (हिंदी) | केशवदास (चिंतामणि) | रस और रीति की प्रधानता। |
| 19वीं सदी उत्तरार्ध | स्वच्छंदतावाद | श्रीधर पाठक | व्यक्ति की स्वतंत्रता, भावनात्मक अभिव्यक्ति। |
| 20वीं सदी प्रारंभ | छायावाद | जय शंकर प्रसाद | आत्मानुभूति, रहस्य, प्रकृति-चित्रण। |
| 20वीं सदी मध्य | हालावाद | हरिवंश राय बच्चन | जीवन की मधुरता, प्रतीकात्मकता। |
| 20वीं सदी मध्य | प्रयोगवाद | अज्ञेय | नये प्रयोग, आधुनिक दृष्टिकोण। |
| 20वीं सदी मध्य | प्रपद्यवाद/नकेनवाद | नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश | जीवन के यथार्थ का चित्रण। |
| 20वीं सदी मध्य | मांसलवाद | रामेश्वर शुक्ल ‘अंचल’ | यथार्थवादी शारीरिक और भावनात्मक चित्रण। |
| 20वीं सदी उत्तरार्ध | कैप्सूलवाद | ओकार नाथ त्रिपाठी | संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली काव्य-शैली। |
| 3री सदी ई. | औदात्यवाद (पाश्चात्य) | लोंजाइनस | साहित्य की उदात्तता। |
| 19वीं सदी | अस्तित्ववाद | सॉरन कीर्कगार्द | मनुष्य का अस्तित्व और स्वतंत्रता। |
| 19वीं सदी | मार्क्सवाद | कार्ल मार्क्स | वर्ग-संघर्ष, सामाजिक यथार्थ। |
| 19वीं–20वीं सदी | मनोविश्लेषणवाद | सिग्मंड फ्रॉयड | अवचेतन मन की भूमिका। |
| 19वीं–20वीं सदी | प्रतीकवाद | जीन मोरियस | प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्ति। |
| 20वीं सदी प्रारंभ | अभिव्यंजनावाद | बेनेदेतो क्रोचे | अंतर्ज्ञान और भाव की प्रधानता। |
| 20वीं सदी प्रारंभ | बिम्बवाद | टी.ई. हयूम | बिम्ब और चित्रात्मकता का महत्व। |
निष्कर्ष
संप्रदाय और वाद मानव सभ्यता के बौद्धिक विकास के दर्पण हैं। धर्म में संप्रदाय ने आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया, तो साहित्य और काव्यशास्त्र में वादों ने नये विचार और रचनात्मकता को जन्म दिया। संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य परंपरा के ये संप्रदाय और वाद आज भी साहित्य, समाज और संस्कृति को नई दृष्टि प्रदान करते हैं।
इन्हें भी देखें –
- हिंदी नाटक और नाटककार – लेखक और रचनाएँ
- हिंदी के प्रमुख एकांकीकार एवं एकांकी | लेखक और रचनाएँ
- हिंदी के निबंधकार और उनके निबंध : एक संपूर्ण सूची
- हिंदी निबंध का विकास : एक ऐतिहासिक परिदृश्य
- पूर्व भारतेंदु युग: हिंदी गद्य की नींव और खड़ी बोली का आरंभिक विकास
- जीवनी – परिभाषा, स्वरूप, भेद, साहित्यिक महत्व और उदाहरण
- पाठ्य-मुक्तक और गेय-मुक्तक : परिभाषा, विशेषताएँ, उदाहरण, विश्लेषण, साहित्यिक महत्व
- दृश्य काव्य : परिभाषा, स्वरूप, भेद, उदाहरण और साहित्यिक महत्त्व