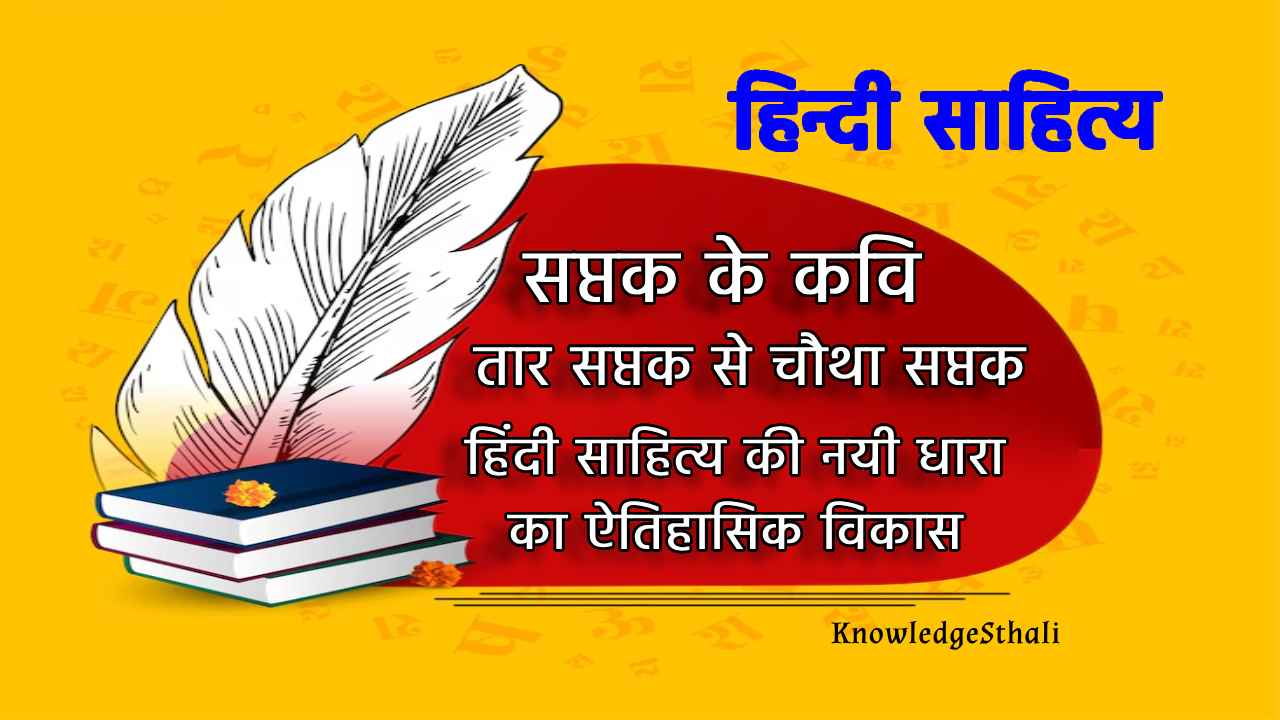हिंदी साहित्य में समय-समय पर अनेक धाराएँ और काव्य प्रवृत्तियाँ विकसित हुईं। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नयी कविता जैसी धाराओं ने न केवल कविता की संवेदनाओं को गहराई दी, बल्कि भाषा, शिल्प और अभिव्यक्ति के नए आयाम भी स्थापित किए। इन्हीं धाराओं में प्रयोगवाद और नयी कविता का जो विकास हुआ, उसका संगठित रूप हमें सप्तक के रूप में दिखाई देता है।
‘सप्तक’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है – सात कवियों का समूह। अज्ञेय ने समय-समय पर ऐसे सात कवियों को चुनकर उनकी कविताओं का संकलन प्रकाशित किया और हिंदी कविता की नयी संभावनाओं को सामने लाया। यह कार्य चार चरणों में हुआ – तार सप्तक (1943), दूसरा सप्तक (1951), तीसरा सप्तक (1959) और चौथा सप्तक (1979)।
इन सप्तकों के माध्यम से हिंदी कविता में अनेक नए कवि सामने आए, जिन्होंने अपने समय की समस्याओं, भावनाओं, जिज्ञासाओं और अंतर्द्वंद्वों को अभिव्यक्त किया। इन सप्तकों ने हिंदी कविता को परंपरा से आधुनिकता की ओर अग्रसर किया।
प्रयोगवाद और सप्तक की पृष्ठभूमि
सप्तक के कवियों की चर्चा करने से पहले प्रयोगवाद और नयी कविता की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है।
प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ई. से माना जाता है। यह धारा छायावाद और प्रगतिवाद से भिन्न थी। छायावाद जहाँ आत्मकेंद्रित भावुकता पर आधारित था और प्रगतिवाद सामाजिक-राजनीतिक चेतना को मुखर करता था, वहीं प्रयोगवाद ने भाषा और शिल्प के स्तर पर नए प्रयोग किए। इस धारा के कवि जीवन और कला के संबंध को नए दृष्टिकोण से देखने लगे।
अज्ञेय इस आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने न केवल स्वयं प्रयोगात्मक कविताएँ लिखीं, बल्कि नयी पीढ़ी के कवियों को सामने लाने का भी प्रयास किया। यही कारण है कि उन्होंने 1943 में ‘तार सप्तक’ का संपादन किया।
सप्तक का विभाजन
सप्तक के कवियों को उनके समय और काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है–
- प्रथम सप्तक (तार सप्तक – 1943 ई०) – प्रयोगवाद की नींव
- दूसरा सप्तक (1951 ई०) – नयी कविता की शुरुआत
- तीसरा सप्तक (1959 ई०) – नयी कविता का सशक्त रूप
- चौथा सप्तक (1979 ई०) – नयी कविता का विस्तार और नवीन संवेदनाएँ
सप्तकों का कालखंड : एक झलक
| सप्तक का नाम | प्रकाशन वर्ष | प्रमुख साहित्यिक धारा |
|---|---|---|
| तार सप्तक | 1943 ई० | प्रयोगवाद की नींव |
| दूसरा सप्तक | 1951 ई० | नयी कविता का आरंभ |
| तीसरा सप्तक | 1959 ई० | नयी कविता का सशक्त रूप |
| चौथा सप्तक | 1979 ई० | नयी कविता का विस्तार |
आइए अब क्रमवार इन सभी सप्तकों और उनके कवियों पर विस्तार से चर्चा करें।
प्रथम सप्तक (तार सप्तक – 1943 ई०)
संपादक – अज्ञेय
कवि – अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजाकुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा।
तार सप्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। 1943 में प्रकाशित इस संकलन ने नयी कविता और प्रयोगवाद की आधारशिला रखी। यह संग्रह केवल कविताओं का संकलन नहीं था, बल्कि एक नए युग की घोषणा थी।
इन कवियों ने भाषा, शिल्प, बिंब और प्रतीकों के स्तर पर नए प्रयोग किए। व्यक्तिगत अनुभवों, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, दार्शनिक चिंतन और आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को उन्होंने कविता में स्थान दिया।
- अज्ञेय – प्रयोगवाद के प्रवर्तक। उनकी कविताएँ आत्मान्वेषण, अस्तित्व-बोध और दार्शनिक गहराई से भरी हुई हैं।
- मुक्तिबोध – गहन वैचारिकता और सामाजिक चेतना से युक्त कवि। बाद में वे प्रगतिवाद और नयी कविता के प्रमुख स्तंभ बने।
- गिरिजाकुमार माथुर – संवेदनशील और प्रयोगशील कवि, जिन्होंने भाषा और लय में नवीनता लाई।
- प्रभाकर माचवे – प्रतीकात्मक और दार्शनिक काव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध।
- भारत भूषण अग्रवाल – मानवीय संवेदना और लोकधर्मी दृष्टिकोण से प्रभावित कवि।
- नेमिचंद्र जैन – आलोचक और कवि दोनों रूपों में महत्वपूर्ण।
- रामविलास शर्मा – प्रगतिशील दृष्टि से संपन्न कवि, आलोचक और चिंतक।
महत्व – तार सप्तक से हिंदी कविता में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। यह संग्रह हिंदी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी कदम माना जाता है।
दूसरा सप्तक (1951 ई०)
संपादक – अज्ञेय
कवि – रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास।
तार सप्तक की सफलता के बाद अज्ञेय ने दूसरी पीढ़ी के कवियों को सामने लाने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप 1951 में ‘दूसरा सप्तक’ प्रकाशित हुआ। यह संकलन नयी कविता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
- रघुवीर सहाय – व्यंग्यात्मक और सामाजिक चेतना से युक्त कवि।
- धर्मवीर भारती – संवेदनशील और रूमानी कवि, जिनकी कविताओं में गहरी भावुकता और दार्शनिकता मिलती है।
- नरेश मेहता – प्रतीक और बिंबों के माध्यम से गहन भावों की अभिव्यक्ति।
- शमशेर बहादुर सिंह – ‘हिंदी का केट्स’ कहे जाते हैं। उनकी कविताएँ चित्रात्मकता और सौंदर्य-बोध से परिपूर्ण हैं।
- भवानी प्रसाद मिश्र – लोकजीवन, सहजता और सामाजिक चेतना से जुड़े कवि।
- शकुंतला माथुर – स्त्री दृष्टि और संवेदना की आवाज।
- हरिनारायण व्यास – नए प्रयोगों के साथ सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने वाले कवि।
महत्व – दूसरा सप्तक नयी कविता की ठोस नींव रखने वाला संकलन था। इसने हिंदी साहित्य में नई पीढ़ी की चेतना को सामने रखा।
तीसरा सप्तक (1959 ई०)
संपादक – अज्ञेय
कवि – कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुँवर नारायण, विजयदेव नारायण साही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन।
तीसरे सप्तक के कवि हिंदी नयी कविता के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। इस संकलन ने हिंदी साहित्य को कई ऐसे कवि दिए, जिन्होंने आने वाले दशकों तक साहित्य की दिशा तय की।
- कुँवर नारायण – दार्शनिक गहराई और मानवीय संवेदना से परिपूर्ण कवि।
- केदारनाथ सिंह – ग्रामीण जीवन, प्रकृति और आधुनिक संवेदना के अद्भुत संगम के कवि।
- सर्वेश्वर दयाल सक्सेना – तीखे व्यंग्य और सामाजिक यथार्थ की पहचान।
- विजयदेव नारायण साही – वैचारिक गहराई और जटिल बिंबों के कवि।
- कीर्ति चौधरी – आधुनिक भाव-बोध और स्त्री दृष्टि से सशक्त कवयित्री।
- प्रयाग नारायण त्रिपाठी – बिंब और प्रतीकों के प्रयोग में दक्ष।
- मदन वात्स्यायन – गहन संवेदनशीलता और बौद्धिकता से संपन्न कवि।
महत्व – तीसरा सप्तक नयी कविता की परिपक्वता का प्रतीक है। इसके कवियों ने आधुनिक हिंदी कविता की धारा को समृद्ध किया।
चौथा सप्तक (1979 ई०)
संपादक – अज्ञेय
कवि – अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर।
चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन कवियों की कविताएँ संकलित की गईं, जो 70 के दशक की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित थे।
- अवधेश कुमार – सामाजिक सरोकार और जनजीवन की अभिव्यक्ति।
- राजकुमार कुंभज – यथार्थवादी दृष्टिकोण और आधुनिक संवेदना।
- स्वदेश भारती – लोक जीवन और सामाजिक चेतना से जुड़े कवि।
- नंद किशोर आचार्य – दार्शनिक गहराई और मानवीय मूल्यों के कवि।
- सुमन राजे – स्त्री संवेदना और मानवीय रिश्तों की कवयित्री।
- श्रीराम वर्मा – जीवन की जटिलताओं को सरल भाषा में व्यक्त करने वाले कवि।
- राजेंद्र किशोर – आधुनिक बोध और चिंतनशीलता के कवि।
महत्व – चौथा सप्तक हिंदी कविता में नयी पीढ़ी की उपस्थिति और उनके विचारों का दस्तावेज है।
सप्तकों के कवि : एकीकृत सूची
| सप्तक का नाम | वर्ष | कवि | विशेषता / पहचान |
|---|---|---|---|
| तार सप्तक (प्रथम सप्तक) | 1943 | अज्ञेय | प्रयोगवाद के प्रवर्तक, दार्शनिक गहराई |
| मुक्तिबोध | सामाजिक चेतना, गहन वैचारिकता | ||
| गिरिजाकुमार माथुर | भाषा और लय में नवीन प्रयोग | ||
| प्रभाकर माचवे | प्रतीकात्मक और दार्शनिक दृष्टि | ||
| भारत भूषण अग्रवाल | लोकधर्मी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना | ||
| नेमिचंद्र जैन | आलोचक और कवि दोनों रूपों में प्रभावी | ||
| रामविलास शर्मा | प्रगतिशील दृष्टि, आलोचना और चिंतन | ||
| दूसरा सप्तक | 1951 | रघुवीर सहाय | व्यंग्यात्मक शैली, सामाजिक चेतना |
| धर्मवीर भारती | संवेदनशीलता, दार्शनिकता और रूमानी रंग | ||
| नरेश मेहता | प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग | ||
| शमशेर बहादुर सिंह | चित्रात्मकता और सौंदर्य-बोध | ||
| भवानी प्रसाद मिश्र | लोकजीवन और सहज अभिव्यक्ति | ||
| शकुंतला माथुर | स्त्री दृष्टि और संवेदना | ||
| हरिनारायण व्यास | सामाजिक यथार्थ और प्रयोगशीलता | ||
| तीसरा सप्तक | 1959 | कुँवर नारायण | दार्शनिक गहराई, मानवीय संवेदना |
| केदारनाथ सिंह | ग्रामीण जीवन, प्रकृति और आधुनिक भाव | ||
| सर्वेश्वर दयाल सक्सेना | व्यंग्य और सामाजिक यथार्थ | ||
| विजयदेव नारायण साही | जटिल बिंब और वैचारिकता | ||
| कीर्ति चौधरी | आधुनिक भाव-बोध, स्त्री दृष्टि | ||
| प्रयाग नारायण त्रिपाठी | प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग | ||
| मदन वात्स्यायन | गहन संवेदनशीलता और बौद्धिकता | ||
| चौथा सप्तक | 1979 | अवधेश कुमार | सामाजिक सरोकार और जनजीवन |
| राजकुमार कुंभज | यथार्थवादी दृष्टिकोण | ||
| स्वदेश भारती | लोकजीवन और सामाजिक चेतना | ||
| नंद किशोर आचार्य | दार्शनिक गहराई, मानवीय मूल्य | ||
| सुमन राजे | स्त्री संवेदना, रिश्तों की अभिव्यक्ति | ||
| श्रीराम वर्मा | जीवन की जटिलताओं की सहज अभिव्यक्ति | ||
| राजेंद्र किशोर | आधुनिक बोध और चिंतनशीलता |
सप्तक का साहित्यिक महत्व
- नयी कविता की नींव – सप्तकों के माध्यम से हिंदी में नयी कविता का विकास हुआ।
- नए कवियों का परिचय – कई ऐसे कवि सामने आए जो आगे चलकर साहित्य के शिखर पुरुष बने।
- प्रयोगधर्मिता – भाषा, शिल्प और बिंबों के स्तर पर नए प्रयोग हुए।
- आधुनिक संवेदना – व्यक्तिगत, सामाजिक और दार्शनिक चिंतन को स्थान मिला।
- इतिहास का दस्तावेज – प्रत्येक सप्तक अपने समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है।
निष्कर्ष
सप्तक केवल कविताओं के संकलन नहीं थे, बल्कि हिंदी साहित्य में एक नई धारा की घोषणा थे। अज्ञेय ने इन्हें संपादित कर न केवल नए कवियों को मंच दिया, बल्कि कविता की संभावनाओं का भी विस्तार किया।
तार सप्तक से शुरू हुआ यह सफर चौथे सप्तक तक आया और हिंदी कविता में प्रयोगवाद से लेकर नयी कविता तक की यात्रा को समेट लिया। इन सप्तकों के कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थायी स्थान रखते हैं।
इन्हें भी देखें –
- मिश्र काव्य : परिभाषा, स्वरूप, प्रमुख छंद व उदाहरण
- पद्यकाव्य: परिभाषा, विशेषताएँ, प्रकार, उदाहरण और ऐतिहासिक विकास
- गद्यकाव्य : परिभाषा, विकास, प्रमुख रचनाएँ और साहित्य में महत्व
- हिंदी की प्रमुख गद्य विधाएँ, उनके रचनाकार और कृतियाँ
- भेंटवार्ता साहित्य : परिभाषा, स्वरूप, विकास और प्रमुख रचनाएँ
- मेलियोइडोसिस (Melioidosis): एक उभरती हुई संक्रामक चुनौती
- पल्लास की बिल्ली: पूर्वी हिमालय में खोजी गई एक दुर्लभ जंगली प्रजाति
- फ्रांस का राजनीतिक ढांचा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया और मौजूदा आर्थिक संकट
- डॉ. मनमोहन सिंह: आर्थिक सुधारों के शिल्पकार को मिला मरणोपरांत पी. वी. नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार
- इथेनॉल: संरचना, उपयोग, लाभ और चुनौतियाँ