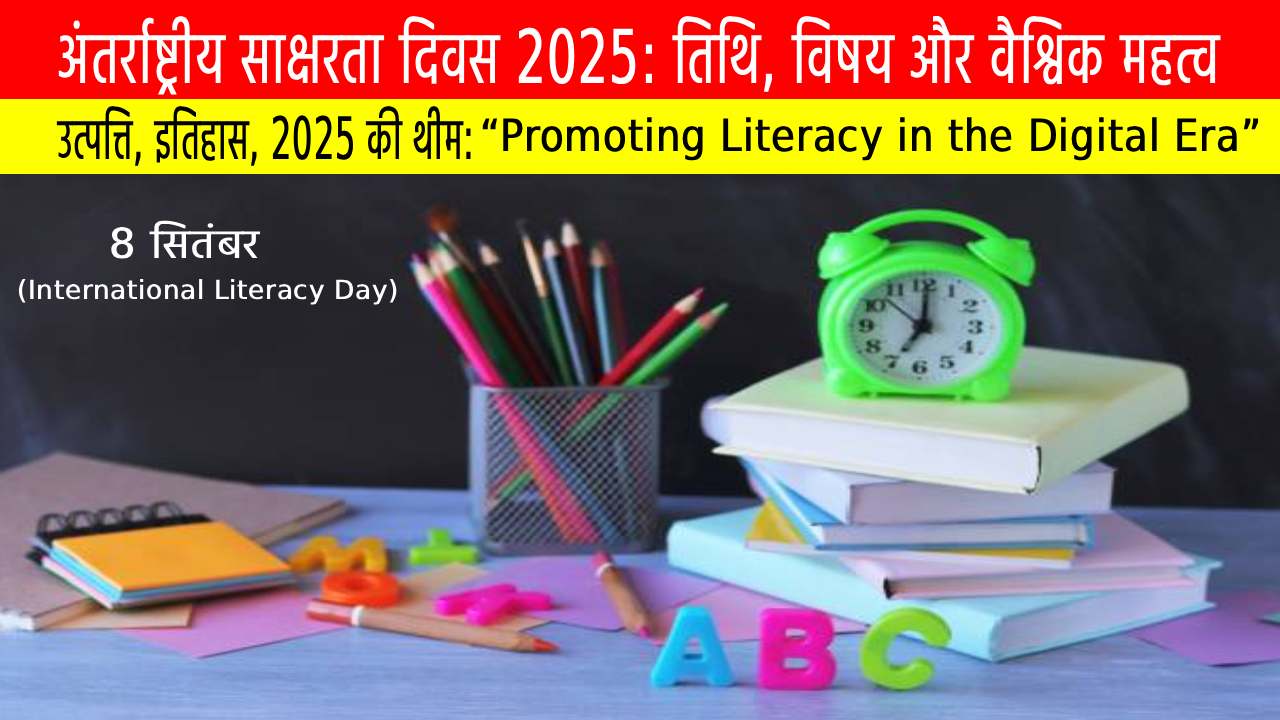हर वर्ष 8 सितंबर को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (International Literacy Day) मनाती है। यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की उस साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें शिक्षा और साक्षरता को प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह व्यक्ति को समाज, अर्थव्यवस्था और डिजिटल दुनिया में समान भागीदारी के लिए सशक्त बनाती है।
वर्ष 2025 में यह दिवस “Promoting Literacy in the Digital Era” (डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना) विषय के तहत मनाया जा रहा है। इसके साथ-साथ एक सह-थीम भी घोषित की गई है — “Promoting Multilingual Education: Literacy for Mutual Understanding and Peace” (बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना: परस्पर समझ और शांति हेतु साक्षरता)।
ये दोनों विषय हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि 21वीं सदी में साक्षरता का स्वरूप कितना बदल चुका है। आज के समय में जहाँ डिजिटल तकनीक जीवन का केंद्र बन चुकी है, वहीं भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की उत्पत्ति और इतिहास
1. तेहरान सम्मेलन से शुरुआत
इस दिवस की नींव 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित विश्व शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन (World Conference of Ministers of Education on the Eradication of Illiteracy) से पड़ी। इस सम्मेलन में निरक्षरता उन्मूलन को वैश्विक एजेंडा बनाने पर जोर दिया गया।
2. यूनेस्को की घोषणा
इसके बाद अक्टूबर 1966 में यूनेस्को (UNESCO) की 14वीं सामान्य सभा में आधिकारिक रूप से 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया।
3. पहली बार आयोजन
पहली बार यह दिवस 1967 में मनाया गया और तभी से यह हर वर्ष शिक्षा और साक्षरता पर वैश्विक चिंतन का अवसर बन गया है।
4. 8 सितंबर ही क्यों?
8 सितंबर को चुने जाने के पीछे एक प्रतीकात्मक कारण भी है। कई देशों में यह समय शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत का होता है, इसलिए यह तिथि शिक्षा और विकास पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने का सर्वोत्तम अवसर मानी गई।
2025 की थीम और उसका महत्व
1. डिजिटल युग में साक्षरता (Promoting Literacy in the Digital Era)
21वीं सदी में साक्षरता का अर्थ केवल किताब पढ़ने या कागज़ पर लिखने से आगे बढ़ चुका है। अब इसमें डिजिटल कौशल (Digital Skills) और सूचना साक्षरता (Information Literacy) भी शामिल है।
चुनौतियाँ
- डिजिटल खाई (Digital Divide): ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक इंटरनेट व तकनीक की पहुँच सीमित है।
- डिजिटल निरक्षरता: बहुत से लोग मोबाइल या कंप्यूटर तो चलाते हैं लेकिन सुरक्षित और सार्थक डिजिटल उपयोग नहीं कर पाते।
- साइबर असुरक्षा: डिजिटल साक्षरता की कमी ऑनलाइन धोखाधड़ी, फेक न्यूज़ और साइबर अपराधों की संवेदनशीलता बढ़ाती है।
अवसर
- डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शिक्षा को अधिक सुलभ बना रहे हैं।
- ऑनलाइन कोर्स, ई-लाइब्रेरी और वर्चुअल क्लासरूम ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं।
- रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर डिजिटल दुनिया से ही जुड़े हैं।
इसलिए डिजिटल युग में साक्षरता केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि समान अवसर और सामाजिक न्याय का आधार है।
2. बहुभाषी शिक्षा और साक्षरता (Promoting Multilingual Education)
आज की दुनिया में भाषाई विविधता को संरक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डिजिटल खाई को पाटना।
लाभ
- परस्पर समझ और शांति: बहुभाषी शिक्षा सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करती है और समाज में सौहार्द को बढ़ाती है।
- संज्ञानात्मक विकास: शोध बताते हैं कि बहुभाषी बच्चे एकल-भाषी बच्चों की तुलना में अधिक रचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं।
- समावेशन और न्याय: आदिवासी व अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देकर सशक्त किया जा सकता है।
- स्कूल छोड़ने की दर में कमी: यदि शिक्षा मातृभाषा में हो तो बच्चे ज्यादा देर तक पढ़ाई जारी रखते हैं।
यह थीम सीधे तौर पर SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) से जुड़ी है।
आज भी साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है?
दुनिया ने पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी विशाल हैं।
- 750 मिलियन वयस्क अभी भी मूलभूत साक्षरता से वंचित हैं।
- इनमें से दो-तिहाई महिलाएँ हैं।
- कई क्षेत्रों में निरक्षरता का सीधा संबंध गरीबी, संघर्ष, पलायन और डिजिटल बहिष्कार से है।
साक्षरता के बहुआयामी लाभ
- आर्थिक सशक्तिकरण: पढ़े-लिखे लोग बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त करते हैं।
- सामाजिक समानता: साक्षरता से महिलाएँ और वंचित समूह अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं।
- स्वास्थ्य जागरूकता: पढ़ाई-लिखाई से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से समझी और अपनाई जाती है।
- लोकतांत्रिक भागीदारी: साक्षर नागरिक वोटिंग, नीतियों और सामाजिक मुद्दों में सक्रिय भागीदारी करते हैं।
भारत और साक्षरता दिवस
भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाए जाते हैं। दोनों अवसर शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं।
भारत ने साक्षरता दर बढ़ाने में बड़ी प्रगति की है — 1951 में जहाँ साक्षरता दर केवल 18.3% थी, वहीं 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 74% तक पहुँच चुकी थी। हालाँकि, अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, पुरुष और महिला साक्षरता दर में असमानता मौजूद है।
भारत की पहलें
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988): वयस्क निरक्षरता को मिटाने के लिए शुरू किया गया।
- सर्व शिक्षा अभियान (2001): 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।
- समग्र शिक्षा अभियान (2018): पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक समग्र शिक्षा पर ध्यान।
- नयी शिक्षा नीति 2020: बहुभाषी शिक्षा, डिजिटल शिक्षण और सार्वभौमिक साक्षरता को प्राथमिकता।
- एनआईओएस और डिजिटल प्लेटफॉर्म: ओपन स्कूलिंग और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अवसरों का विस्तार।
भारत में शिक्षा और साक्षरता की प्रगति केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण और सामाजिक न्याय की आधारशिला है।
परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Quick Facts)
- तारीख़: 8 सितंबर
- घोषणा: यूनेस्को, 1966
- पहली बार मनाया गया: 1967
- ऐतिहासिक आरंभ: 1965 तेहरान सम्मेलन
- SDG लिंक: SDG 4 – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- 2025 की थीम: “Promoting Literacy in the Digital Era”
- सह-थीम: “Promoting Multilingual Education”
निष्कर्ष
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक प्रगति, शांति और सतत विकास का आधार है।
2025 की थीम डिजिटल युग की चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालती है, वहीं सह-थीम बहुभाषी शिक्षा के महत्व को सामने लाती है। दोनों ही यह स्पष्ट करते हैं कि भविष्य की दुनिया में साक्षरता का स्वरूप बहुआयामी होगा — जिसमें डिजिटल सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विविधता दोनों की भूमिका बराबर होगी।
भारत जैसे देशों के लिए यह अवसर है कि वे शिक्षा नीतियों को और अधिक समावेशी और तकनीक-सक्षम बनाकर साक्षरता को राष्ट्र-निर्माण का सशक्त साधन बनाएँ।
इन्हें भी देखें –
- एशिया कप 2025: कार्यक्रम, प्रमुख मैच, टीमें, इतिहास और पूरी जानकारी
- 7 सितंबर 2025 का चंद्रग्रहण: साल का आखिरी और सबसे लंबा ब्लड मून
- सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश: समावेशिता और लैंगिक समानता की चुनौती
- सेशेल्स और भारत: समुद्री साझेदारी का गहराता रिश्ता
- भारत में चार बड़े साँप (Big Four Snakes in India) और जलवायु परिवर्तन का खतरा