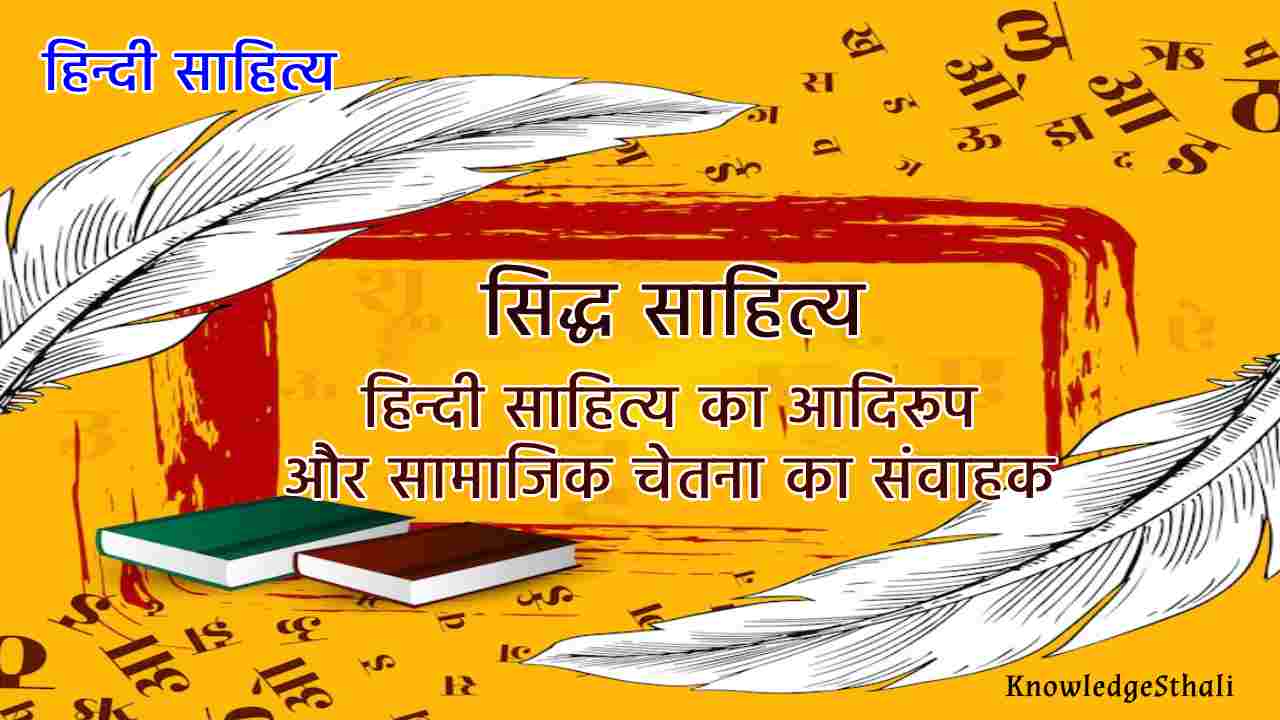सिद्ध साहित्य हिन्दी साहित्य की आदिम कड़ी है, जो न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान है। यह साहित्य भारत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबद्ध सिद्ध साधकों द्वारा रचित है, जो विशेषतः भारत के पूर्वी भाग—बिहार, बंगाल और असम—में सक्रिय थे। यह साहित्य 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ और इसकी रचना मुख्यतः लोकभाषा या देशज भाषा में हुई। इसकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है, जिसमें स्पष्टता और रहस्यात्मकता दोनों का मिश्रण मिलता है।
सिद्ध साहित्य को हिन्दी का आदिसाहित्य माना जाता है। डॉ. राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध कवि सरहपा को हिन्दी का प्रथम कवि घोषित किया। उनकी रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, जातिगत भेदभावों, धार्मिक पाखंडों पर तीखा प्रहार किया गया है और सहज साधना मार्ग को अपनाने का संदेश दिया गया है। यह साहित्य धार्मिक होते हुए भी मानवतावादी दृष्टिकोण से भरा हुआ है।
सिद्धों का उद्भव और सामाजिक पृष्ठभूमि
सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत हुआ, जो तंत्र, योग और साधना पर विशेष बल देती थी। इन सिद्धों की संख्या परंपरागत रूप से 84 मानी जाती है। ये लोग समाज के हर वर्ग से आते थे और इन्हें जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर बाँधना कठिन है। इनके नामों के अंत में प्रायः “पा” शब्द जुड़ा होता है, जैसे—सरहपा, लुइप्पा, डोम्भिपा, कुक्कुरिप्पा आदि।
इनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः पूर्वी भारत—बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम—था। सिद्धों की साधना का प्रमुख केंद्र नालंदा महाविहार था, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से भारी क्षति पहुँची। इस विनाश के पश्चात सिद्ध परंपरा तिब्बत (भोट देश) की ओर चली गई।
सिद्ध साहित्य की परिभाषा और प्रकृति
सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो साहित्य देशी भाषा में लिखा गया, वही “सिद्ध साहित्य” कहलाता है। यह साहित्य मुख्यतः लोकभाषा में लिखा गया ताकि जनसामान्य उसे समझ सके। इसमें दार्शनिकता, तांत्रिकता, साधना, रहस्यवाद, और सामाजिक चेतना का संगम मिलता है। यह साहित्य न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि उस युग की सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध क्रांति का भी स्वर है।
सिद्ध साहित्य को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- नीति या आचार संबंधित साहित्य
- उपदेशात्मक साहित्य
- साधनात्मक या रहस्यवादी साहित्य
प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएँ
- सरहपा: इन्हें सिद्ध परंपरा का अग्रदूत और हिन्दी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्होंने जातिवाद, पाखंड, और रूढ़ियों पर प्रहार किया और सहज साधना का मार्ग प्रशस्त किया। इनकी प्रमुख रचना दोहाकोश है।
- शबरपा: इनकी रचना चर्यापद के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें रहस्यमय अनुभूतियों का चित्रण है।
- डोम्भिपा: डोम्बिगीतिका, योगचर्या, और अक्षरद्विकोपदेश जैसी रचनाओं में साधनात्मक तत्वों का समावेश मिलता है।
सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ
1. सहजता और स्वाभाविकता में विश्वास
सिद्ध कवियों ने जीवन की कृत्रिमता को नकारते हुए सहज और स्वाभाविक जीवन को महत्व दिया। वे मानते थे कि सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार स्त्री-पुरुष का मिलन मात्र भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है—स्त्री प्रज्ञा और पुरुष करुणा का प्रतीक है, और इन दोनों के मिलन से ही ‘महासुख’ की प्राप्ति होती है।
2. गुरू-महिमा का प्रतिपादन
सिद्ध साहित्य में गुरू को अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। सरहपा ने कहा है कि गुरू के बिना साधना और मुक्ति संभव नहीं है। गुरू के उपदेश को अमृत समान माना गया है, जिससे आत्मा का कल्याण संभव है।
“गुरू उवएसि अमिरस धावण पीएड जे ही।
बहु सत्यत्य मरू स्थलहि तिसिय मरियड ते ही।।”
3. बाह्याडम्बर और पाखण्ड पर कटाक्ष
सिद्ध कवियों ने ब्राह्मणवाद, कर्मकाण्ड, जातिप्रथा, वेद-पुराणों की आड़ में फैले पाखंडों पर तीखा व्यंग्य किया। सरहपा ने ब्राह्मणत्व की आलोचना करते हुए पूछा कि यदि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे तो अब भी वे क्यों सामान्य मानव की तरह जन्म लेते हैं?
इसी तरह, दिगम्बर साधुओं, वेद पाठकों, और कर्मकांडियों पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं:
“यदि नंगे रहने से मुक्ति हो जाए तो सियार-कुत्ते भी मुक्त हो जाते,
और यदि केश बढ़ाने से मुक्ति मिले तो मयूर सबसे आगे होते।”
4. आशावाद का संचार
सिद्ध साहित्य का एक प्रमुख उद्देश्य था—हतोत्साहित और पराजित जनता में नया आत्मविश्वास भरना। जब जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता और सामाजिक अन्याय से पीड़ित थी, तब सिद्धों की वाणी ने उन्हें आध्यात्मिक सहारा प्रदान किया। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस साहित्य को “संजीवनी” कहा है।
5. रहस्यात्मक अनुभूति
सिद्ध साहित्य में रहस्यवाद प्रमुख है। महासुख की प्राप्ति को विविध रूपकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जैसे—नाव, वीणा, चूहा, हिरण आदि। साथ ही तांत्रिक प्रतीकों जैसे रवि, शशि, कुलिश, अवधूत आदि का प्रयोग भी मिलता है।
डॉ. धर्मवीर भारती ने अपने ग्रंथ ‘सिद्ध साहित्य’ में सिद्धों की शब्दावली का दार्शनिक और आध्यात्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है।
6. रस योजना
इस साहित्य में विशेष रूप से शृंगार और शांत रस की प्रधानता है। आनंद की अनुभूति को शृंगार रस के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जबकि साधना की उपलब्धि और शांति को शांत रस के माध्यम से चित्रित किया गया है।
7. जनभाषा का प्रयोग
सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है इसका जनभाषा में लिखा जाना। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के मिश्रण से बनी संध्या भाषा का प्रयोग हुआ है। यह भाषा कुछ स्पष्ट तो कुछ अस्पष्ट अर्थ देती है, जैसे साँझ के समय की रोशनी।
डॉ. रामकुमार वर्मा ने सिद्धों की भाषा को जनता की भाषा माना है। जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इसे ‘संध्या भाषा’ कहा है।
8. छन्द प्रयोग
सिद्ध साहित्य में छंद योजना का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें चर्या गीत की प्रधानता है, परन्तु दोहा, चौपाई, सोरठा और छप्पय जैसे छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। विशेष रूप से दोहा सिद्ध कवियों का प्रिय छंद रहा है।
9. साहित्य का आदिरूप
डॉ. रामकुमार वर्मा के अनुसार सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे हमारे साहित्य का आदिरूप प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है। यह साहित्य न केवल साहित्यिक विकास की धुरी है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत दस्तावेज भी है।
सिद्ध साहित्य की आलोचना और समर्थन
सिद्धों की साधना में वामाचार की प्रधानता के कारण बाद में इन्हें समाज में विरोध का सामना करना पड़ा। स्त्री को साधना में अनिवार्य मानने की प्रवृत्ति ने इन्हें सामाजिक आलोचना का केंद्र बना दिया। उस समय बिहार और बंगाल में नई वधुओं को सिद्धों के आकर्षण से बचने की चेतावनी दी जाती थी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत का खंडन करते हुए इसे सामाजिक रूप से जागरूक और सांस्कृतिक चेतना से युक्त साहित्य माना।
निष्कर्ष
सिद्ध साहित्य हिन्दी साहित्य का आदिरूप है, जिसमें केवल धार्मिक या तांत्रिक भावनाएँ ही नहीं, बल्कि तत्कालीन समाज की व्यथा, संघर्ष, और उसकी मुक्ति की कामना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह साहित्य लोकभाषा में रचा गया, इसलिए इसका प्रभाव जनमानस पर गहरा पड़ा। इसकी भाषा, शैली, छंद, विषय-वस्तु, और संदेश आज भी हिन्दी साहित्य के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अध्येताओं के लिए प्रेरणास्रोत है।
सिद्ध कवियों की रचनाएँ केवल तांत्रिक साधना की व्याख्या नहीं हैं, बल्कि सामाजिक विकृतियों के विरुद्ध क्रांति की उद्घोषणा भी हैं। यही कारण है कि यह साहित्य आज भी अपनी मौलिकता, प्रासंगिकता और सांस्कृतिक मूल्य के लिए स्मरणीय बना हुआ है।
संदर्भ:
- राहुल सांकृत्यायन – दोहाकोश की भूमिका
- डॉ. रामकुमार वर्मा – सिद्ध साहित्य और उसका साहित्यिक मूल्यांकन
- डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी – मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की रूपरेखा
- हरप्रसाद शास्त्री – बौद्धगान-ओ-दोहा
- डॉ. धर्मवीर भारती – सिद्ध साहित्य पर शोध
इन्हें भी देखे –
- मुहावरा और लोकोक्तियाँ 250+
- वर्तनी किसे कहते है? उसके नियम और उदहारण
- रस- परिभाषा, भेद और उदाहरण
- नाथ संप्रदाय (साहित्य): योग, तंत्र और साधना की भारतीय परंपरा का अनूठा अध्याय
- इतिहास रचेंगी प्रिया नायर, बनेंगी हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ
- चम्पू साहित्य | गद्य और पद्य का अद्वितीय संगम
- पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र | परिमंडल | Earth’s Domain | Circle
- विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय
- महान व्यक्तियों के उपनाम, स्थान, प्रमुख वचन एवं नारे
- Tense: Definition, Types, and 100+ Examples