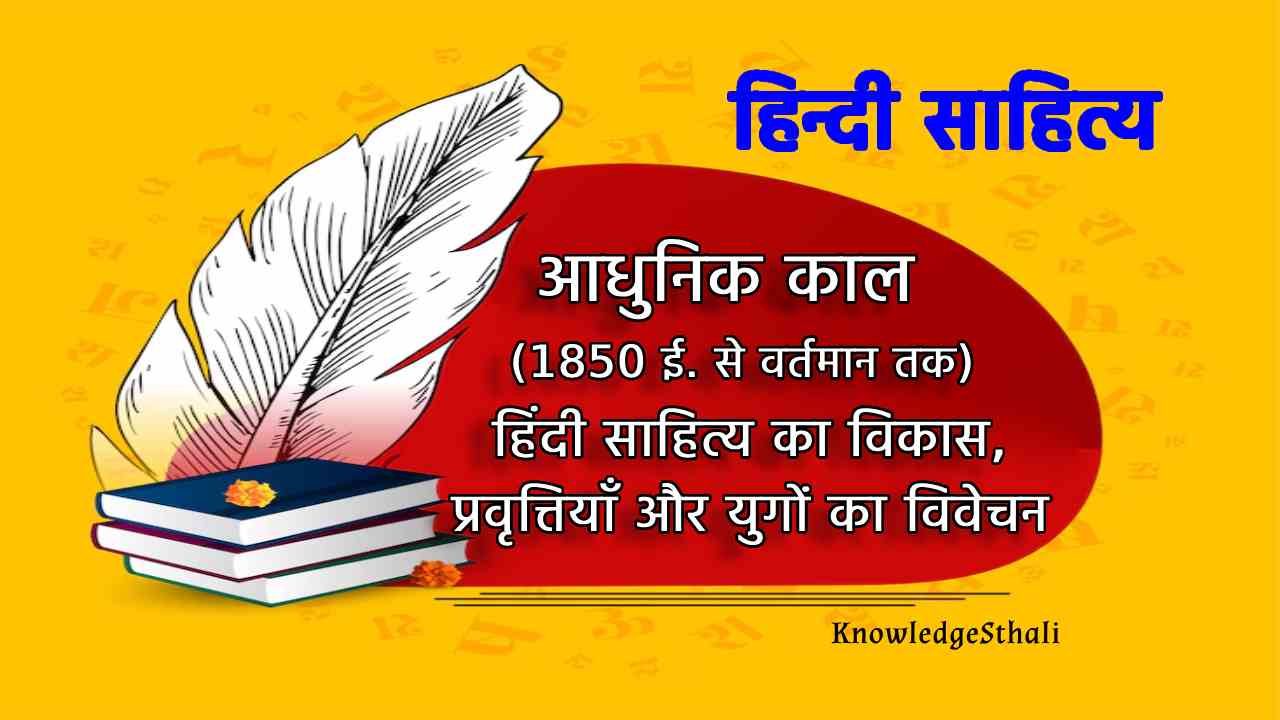यह लेख आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे समृद्ध और बहुआयामी युग—आधुनिक काल (1850 ई. से वर्तमान तक)—का एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें आधुनिक युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन, गद्य-पद्य का विकास, एवं साहित्यिक आंदोलनों की क्रमबद्ध चर्चा की गई है। भारत में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना के बाद हिंदी गद्य को मिली गति, मुद्रण प्रेस की भूमिका, और जनभाषा में साहित्य सृजन की बढ़ती प्रवृत्तियाँ इस काल की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
लेख में आधुनिक काल को सुव्यवस्थित रूप से उपयुगों में विभाजित किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन युग। प्रत्येक युग के समय, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार और साहित्यिक योगदान को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।
इसके साथ ही यह लेख एक गंभीर प्रश्न पर विचार करता है: क्या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता को छायावादोत्तर युग के अंतर्गत माना जाना चाहिए या उन्हें स्वतंत्र युग माना जाए? इसका ऐतिहासिक व साहित्यिक आधार पर विश्लेषण भी इसमें किया गया है।
साथ ही, लेख में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) को भी उत्तरों सहित शामिल किया गया है, जो छात्रों, शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
यह लेख हिंदी साहित्य के आधुनिक विकास को समझने के लिए एक संपूर्ण और शोधपरक संसाधन है।
परिचय: आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रस्तावना
हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जिसमें समय-समय पर विभिन्न युगों और प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इनमें से आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सबसे जागरूक, विविधतापूर्ण और उन्नत युग माना जाता है। यह युग केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल की शुरुआत लगभग 1850 ईस्वी से मानी जाती है, जो रीतिकाल के बाद आता है। इस काल में हिंदी साहित्य ने नए आयामों को छुआ—गद्य लेखन, पत्रकारिता, नाटक, कहानी, उपन्यास, समालोचना तथा कविता सभी विधाओं में अद्वितीय विकास हुआ।
आधुनिक काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1800 विक्रम संवत (लगभग 1743 ई.) के बाद भारत में अनेक यूरोपीय जातियों का आगमन व्यापारिक उद्देश्यों से हुआ। इन यूरोपीय शक्तियों, विशेषतः अंग्रेजों, ने भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक ताने-बाने में गहरा हस्तक्षेप किया। देशी राजाओं की पारस्परिक कलह और नीतिगत अस्थिरता के कारण अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। यह शासन केवल राजनैतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और भाषायी रूपांतरण का भी माध्यम बना।
अंग्रेजों ने शासन संचालन एवं धर्म-प्रचार के लिए स्थानीय जनता की भाषा को अपनाना आरंभ किया। चूँकि शासनिक एवं धार्मिक संप्रेषण के लिए गद्य शैली अधिक उपयुक्त होती है, अतः गद्य लेखन का तेजी से विकास हुआ। यह काल गद्य प्रधान साहित्य के विकास का प्रतीक बन गया।
आधुनिक काल का समय (1850 ई. से अब तक)
आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी से मानी जाती है और यह आज तक चलता आ रहा है। यह काल रीतिकाल के पश्चात आता है और इसे हिंदी साहित्य का सबसे विकसित और व्यापक युग माना जाता है।
- प्रारंभ: 1850 ई.
- अंत: अब तक (समकालीन युग तक)
मुद्रण कला और भाषायी विकास
आधुनिक काल में मुद्रण कला के आगमन ने साहित्यिक विकास में क्रांति ला दी। पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के छपने से ज्ञान का प्रसार आम जनता तक संभव हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की विचारधाराओं को हिंदी में प्रस्तुत किया, जिससे हिंदी गद्य का संवर्धन हुआ। साथ ही अंग्रेज मिशनरियों ने भी अपने धार्मिक साहित्य का प्रकाशन हिंदी गद्य में करवाया।
इन प्रयासों से हिंदी में गद्य लेखन की सुदृढ़ नींव पड़ी। अब तक जो भाषा काव्य तक सीमित थी, वह सामाजिक संवाद, आलोचना, रिपोर्टिंग और उपन्यास लेखन जैसी नई विधाओं में विकसित होने लगी।
खड़ी बोली का उत्थान
पूर्ववर्ती रीतिकालीन काव्य में ब्रजभाषा का वर्चस्व था, जो शृंगारिकता से परिपूर्ण थी। परंतु आधुनिक राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और यथार्थ के चित्रण के लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त मानी गई। साहित्यकारों ने इसे अपनाया और इसे साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र और अयोध्या प्रसाद खत्री जैसे साहित्यकारों ने खड़ी बोली के गद्य और पद्य—दोनों रूपों में विशेष कार्य किया। भारतेंदु बाबू को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने साहित्य के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रप्रेम को जनमानस तक पहुँचाया।
प्रमुख साहित्यकार और उनका योगदान
आधुनिक काल के प्रारंभिक कवियों में राजा लक्ष्मण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल आदि का नाम लिया जाता है, जिन्होंने ब्रजभाषा में रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने न केवल कविता बल्कि नाटक, गद्य और पत्रकारिता में भी योगदान दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य को प्रांजल, संयमित और परिष्कृत स्वरूप प्रदान किया।
इनके बाद आने वाले साहित्यकारों—मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, दिनकर, सुभद्राकुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी आदि—ने हिंदी साहित्य को राष्ट्रीयता, सामाजिक परिवर्तन और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने का कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हिंदी काव्य में अतुकांत छंदों (फ्री वर्स) का प्रचलन बढ़ा, जिससे कवियों को अधिक स्वतंत्रता मिली।
आधुनिक काल का विभाजन (सूची रूप में)
- भारतेंदु युग (1868 – 1900)
- द्विवेदी युग (1900 – 1920)
- छायावादी युग (1918 – 1936)
- छायावादोत्तर युग (1936 – 1947)
- प्रगतिवादी युग (1936 से आगे)
- प्रयोगवादी युग (1943 से आगे)
- नई कविता युग (1951 से अब तक)
आधुनिक काल का विभाजन (तालिका रूप में)
| क्रम | युग का नाम | समय सीमा | प्रमुख लेखक / कवि |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतेंदु युग | 1868 – 1900 ई. | भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन |
| 2 | द्विवेदी युग | 1900 – 1920 ई. | मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी |
| 3 | छायावादी युग | 1918 – 1936 ई. | जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा |
| 4 | छायावादोत्तर युग | 1936 – 1947 ई. | दिनकर, बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन |
| 5 | प्रगतिवादी युग | 1936 से 1943 ई | नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन |
| 6 | प्रयोगवादी युग | 1943 से 1953 ई. | अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भारतभूषण अग्रवाल |
| 7 | नई कविता युग | 1951 से अब तक | रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र |
आधुनिक काल का युग विभाजन
हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को अनेक उपयुगों में विभाजित किया गया है। इसका उद्देश्य अध्ययन को सरल बनाना है। हर युग की अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियाँ और प्रमुख लेखक रहे हैं।
1. भारतेंदु युग (1868–1900)
भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। यह युग हिंदी नवजागरण का प्रारंभिक चरण है जिसमें राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और धार्मिक आलोचना प्रमुख विषय बने। प्रमुख लेखक:
- भारतेंदु हरिश्चंद्र
- प्रताप नारायण मिश्र
- बद्रीनारायण चौधरी ‘प्रेमघन’
- अंबिकादत्त व्यास
- राधाचरण गोस्वामी
विशेषताएँ:
- खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक विकास
- नाटक, हास्य-व्यंग्य एवं पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान
- सामाजिक और धार्मिक सुधारवाद
2. द्विवेदी युग (1900–1920)
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। उन्होंने ‘सरस्वती’ पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी।
प्रमुख साहित्यकार:
- मैथिलीशरण गुप्त
- अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’
- रामनरेश त्रिपाठी
- श्रीधर पाठक
विशेषताएँ:
- खड़ी बोली का परिष्कृत रूप
- राष्ट्रप्रेम, इतिहासबोध और नैतिकता
- गद्य साहित्य का सशक्त विस्तार
3. छायावादी युग (1918–1936)
इस युग में कविता में आत्मचेतना, रहस्यवाद, प्रकृति-चित्रण और सौंदर्यबोध का प्राधान्य रहा। इसे हिंदी का ‘रोमांटिक युग’ कहा जा सकता है।
प्रमुख कवि:
- जयशंकर प्रसाद
- सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’
- सुमित्रानंदन पंत
- महादेवी वर्मा
मुख्य प्रवृत्तियाँ:
- काव्य में व्यक्तिवाद एवं कल्पनाशीलता
- भाषा की लयात्मकता एवं प्रतीकात्मकता
- नारी चेतना एवं करुणा का स्वर
4. छायावादोत्तर युग (1936–1947)
इस युग में कविता सामाजिक यथार्थ और राष्ट्र चेतना की ओर उन्मुख हुई। काव्य में स्वाधीनता संग्राम की झलक और जनसंघर्ष का चित्रण प्रमुख हुआ।
प्रमुख कवि:
- रामधारी सिंह ‘दिनकर’
- हरिवंश राय बच्चन
- सुभद्राकुमारी चौहान
- माखनलाल चतुर्वेदी
- बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’
विशेषताएँ:
- राष्ट्रीयता और समाजवाद का उदय
- वीर रस और जन आंदोलन का चित्रण
- कविता में नवचेतना का संचार
“छायावादोत्तर युग हिंदी साहित्य के इतिहास में न केवल छायावाद का अवसान है, बल्कि वह एक ऐसा परिवर्तनशील दौर भी है, जिससे अनेक नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता जैसी धाराएँ इसी युग की परिणतियाँ हैं या अपने आप में स्वतंत्र साहित्यिक युग हैं?”
छायावादोत्तर युग और उसकी परिधि: क्या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इसके अंतर्गत आते हैं?
हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादोत्तर युग एक ऐसा परिवर्तनकारी काल है, जहाँ छायावादी भावुकता और कल्पना-प्रधानता से हटकर साहित्य ने यथार्थ, समाज और विचार की ओर रुख किया। इस युग के समानांतर ही प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और बाद में नई कविता जैसी साहित्यिक धाराएँ भी उभरती हैं।
ऐसे में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या इन सभी धाराओं को छायावादोत्तर युग के अंतर्गत माना जाए? आइए इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझें।
कालक्रम (Chronological) दृष्टिकोण से विश्लेषण
| साहित्यिक प्रवृत्ति | प्रारंभ वर्ष | प्रमुख प्रतिनिधि लेखक |
|---|---|---|
| छायावादोत्तर युग | 1936 से 1947 ई. | रामधारी सिंह ‘दिनकर’, माखनलाल चतुर्वेदी, बच्चन |
| प्रगतिवाद | 1936 से 1943 ई. | नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन |
| प्रयोगवाद | 1943 से 1953 ई. | अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, भारतभूषण अग्रवाल |
| नई कविता | 1951 से आगे* | धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता |
टिप्पणी / नोट:
नई कविता युग का सामान्यतः समय 1951 ई. से आगे माना जाता है, किंतु कुछ साहित्य विशेषज्ञों के अनुसार, इस युग की स्पष्ट और संगठित शुरुआत 1954 ई. में “नई कविता” नामक पत्रिका के प्रकाशन से मानी जाती है। इस दृष्टि से 1954 को “नव लेखन काल” या “नई कविता आंदोलन” का वास्तविक प्रारंभ बिंदु भी माना जाता है।
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तीनों प्रवृत्तियाँ कालक्रम में छायावादोत्तर युग से या तो जुड़ी हुई हैं या उसके तुरंत बाद आई हैं।
अतः कालिक समीपता के आधार पर इनका छायावादोत्तर युग से संबंध स्वाभाविक है।
साहित्यिक प्रवृत्ति और उद्देश्य की दृष्टि से
- छायावादोत्तर युग में साहित्यकारों ने कविता को समाज और राष्ट्र के यथार्थ से जोड़ा।
- प्रगतिवाद ने मार्क्सवादी और समाजवादी चेतना के साथ साहित्य को जन-संघर्ष से जोड़ा।
- प्रयोगवाद ने भाषा, शैली और विचार में नवाचार किए और आत्मसंघर्ष तथा अस्तित्ववाद को स्थान दिया।
- नई कविता ने नव-मनुष्य की अनुभूतियों, शहरी अस्तित्व, एकाकीपन, विकृत जीवन अनुभवों को प्रमुख विषय बनाया।
👉 इन तीनों प्रवृत्तियों ने छायावादोत्तर युग की ही तरह छायावादी कल्पनाशीलता से मुक्ति और नवीन यथार्थ की ओर अग्रसरता दिखाई।
📌 इसलिए, साहित्यिक दृष्टिकोण से इन्हें छायावादोत्तर युग की “विस्तारित परिधि” में रखा जा सकता है, यद्यपि उनकी स्वतंत्र पहचान और आंदोलनात्मक स्वरूप भी रहे हैं।
विद्वानों का मत और आलोचनात्मक दृष्टिकोण
- कई साहित्य समीक्षक जैसे डॉ. नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी आदि का मानना है कि: “छायावाद के बाद आने वाली समस्त वैचारिक, सामाजिक और कलात्मक धाराएँ — चाहे वे प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो या नई कविता — सभी छायावाद की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुईं और छायावादोत्तर युग की समष्टिगत अभिव्यक्ति हैं।”
- वहीं कुछ अन्य विद्वान इन्हें पूर्ण स्वतंत्र युग मानते हैं, जिनका छायावादोत्तर युग से केवल ऐतिहासिक संबंध है, विचारधारा और उद्देश्य में नहीं।
📌 अतः यह स्पष्ट है कि आलोचनात्मक मतों में भिन्नता है, परंतु सामान्य सहमति यह है कि इन प्रवृत्तियों को छायावादोत्तर “कालखंड” का हिस्सा, लेकिन “युगात्मक रूप से स्वतंत्र” माना जाता है।
निष्कर्ष: समन्वित दृष्टिकोण
- छायावादोत्तर युग एक ऐसा परिवर्तनकाल है जिसने हिंदी साहित्य को समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के यथार्थ की ओर मोड़ा।
- प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता — तीनों इसी बौद्धिक और रचनात्मक प्रवाह के अंग हैं।
- यद्यपि इनकी स्वतंत्र पहचान और साहित्यिक आंदोलन के रूप में स्थिति स्पष्ट है, फिर भी इन्हें छायावादोत्तर प्रवृत्तियों के विकासात्मक क्रम में अवश्य शामिल किया जा सकता है।
🖋️ इसलिए, लेख में इन्हें छायावादोत्तर युग के “विस्तारित प्रभाव क्षेत्र” या “उत्तर-छायावादी चेतना” के प्रतिनिधि रूप में प्रस्तुत करना उचित एवं तार्किक दोनों है।
यह कहना उचित होगा कि — “प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता — छायावादोत्तर युग से प्रभावित अवश्य हैं, परंतु वे स्वयं में स्वतंत्र साहित्यिक युग हैं।“
5. प्रगतिवादी युग (1936 से 1943)
‘प्रगतिशील लेखक संघ’ की स्थापना के साथ यह युग आरंभ हुआ। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ समाजवादी, मार्क्सवादी और यथार्थवादी रहीं।
प्रमुख लेखक-कवि:
- नागार्जुन
- त्रिलोचन शास्त्री
- केदारनाथ अग्रवाल
- मुक्तिबोध
- शमशेर बहादुर सिंह
मुख्य प्रवृत्तियाँ:
- मजदूर, किसान, दलित, शोषितों की आवाज
- वर्ग-संघर्ष एवं सामाजिक असमानता का चित्रण
- सपाटबयानी और यथार्थपरक शैली
6. प्रयोगवादी युग (1943 से 1953)
प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय द्वारा संपादित ‘तारसप्तक’ (1943) से हुआ। यह युग व्यक्तिवाद और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रेरित था।
प्रमुख लेखक:
- अज्ञेय
- गिरिजाकुमार माथुर
- प्रभाकर माचवे
- भारतभूषण अग्रवाल
- मुक्तिबोध
- शमशेर बहादुर सिंह
विशेषताएँ:
- आत्माभिव्यक्ति और आधुनिकता की खोज
- भाषा और शैली में नवीनता
- मनोवैज्ञानिक गहराई
7. नई कविता आंदोलन (1951 से अब तक)
यह आंदोलन तारसप्तक के बाद दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ और उभरता गया। यह समकालीन भारतीय जीवन की जटिलताओं का प्रतिबिंब है।
प्रमुख कवि:
- रघुवीर सहाय
- धर्मवीर भारती
- नरेश मेहता
- भवानी प्रसाद मिश्र
मुख्य प्रवृत्तियाँ:
- शहरी जीवन का चित्रण
- अस्तित्ववाद, विखंडन और विसंगतियाँ
- गहरी दार्शनिकता और संवेदनशीलता
निष्कर्ष
आधुनिक काल हिंदी साहित्य के विकास की एक ऐसी यात्रा है, जिसमें भाषा, शैली, विषयवस्तु और दृष्टिकोण में निरंतर परिवर्तन होता रहा। यह यात्रा केवल साहित्यिक नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से भी जुड़ी रही है। गद्य की स्थापना से लेकर नई कविता तक का यह कालखंड हिंदी साहित्य को समग्र दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है।
सचमुच, आधुनिक काल ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा, नई दृष्टि और नया आत्मविश्वास प्रदान किया है। इस युग की विविधता और सृजनशीलता आज भी साहित्यकारों और पाठकों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनी हुई है।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. आधुनिक काल की समय-सीमा क्या मानी जाती है?
उत्तर: आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ई. से मानी जाती है और यह वर्तमान समय तक फैला हुआ है। यह काल रीतिकाल के बाद आता है और इसमें हिंदी साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ।
2. आधुनिक हिंदी साहित्य को कितने प्रमुख युगों में बाँटा गया है?
उत्तर: आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रमुखतः निम्न युगों में विभाजित किया गया है:
- भारतेंदु युग (1868–1900)
- द्विवेदी युग (1900–1920)
- छायावाद युग (1918–1936)
- छायावादोत्तर युग (1936–1947)
- प्रगतिवाद युग (1936–1943)
- प्रयोगवाद युग (1943–1953)
- नई कविता युग (1951 से आगे)
- समकालीन युग (1970 से अब तक)
3. प्रगतिवाद युग का समय क्या है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:
- समय: 1936–1943 ई.
- विशेषताएँ: इस युग में साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा, शोषण के विरुद्ध स्वर, समाज की वास्तविक समस्याएँ, और क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया।
- प्रमुख लेखक: नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद (अंतिम दौर)
4. प्रयोगवाद युग कब से कब तक रहा और इसकी विशेषता क्या थी?
उत्तर:
- समय: 1943–1953 ई.
- विशेषताएँ: इस युग में कवियों ने नवीन प्रयोग, व्यक्तिगत अनुभूति, गहन मनोविश्लेषण, और काव्य-भाषा में नवाचार पर बल दिया।
- प्रमुख कवि: अज्ञेय (संपादक – तार सप्तक), गिरिजाकुमार माथुर, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे
5. नई कविता युग की शुरुआत कब हुई और इसकी विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर:
- समय: 1951 ई. से आगे (कुछ विद्वानों के अनुसार 1954 में ‘नई कविता’ पत्रिका से औपचारिक आरंभ)
- विशेषताएँ:
- व्यक्तिगत अनुभव,
- शहरी जीवन की विडंबनाएँ,
- अस्तित्ववादी सोच,
- सामाजिक अलगाव और मानसिक द्वंद्व
- प्रमुख कवि: रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र
6. छायावादोत्तर युग में क्या प्रमुख बदलाव आए?
उत्तर: छायावादोत्तर युग में काव्य विषय कल्पनाशीलता से हटकर यथार्थ, राष्ट्रभक्ति, और जनसामान्य की पीड़ा की ओर उन्मुख हुआ। यह युग साहित्य के सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को दर्शाता है।
7. क्या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता को छायावादोत्तर युग में ही शामिल किया जाता है?
उत्तर: नहीं। यद्यपि इन प्रवृत्तियों का उद्भव छायावादोत्तर युग की पृष्ठभूमि में हुआ, फिर भी इनकी विशिष्ट विशेषताओं, कालवधि, और दृष्टिकोण के आधार पर इन्हें स्वतंत्र युग माना जाता है।
8. ‘तार सप्तक’ का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है?
उत्तर: ‘तार सप्तक’ (1943) हिंदी कविता के प्रयोगवादी युग की शुरुआत का प्रतीक है। इसे अज्ञेय ने संपादित किया और इसके माध्यम से सात नए कवियों को मंच मिला, जिन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा दी।
9. ‘नई कविता’ शब्द की पहली बार चर्चा कब हुई?
उत्तर: ‘नई कविता’ शब्द की अवधारणा 1951 से प्रचलन में आई, किंतु 1954 में ‘नई कविता’ नामक पत्रिका के प्रकाशन के बाद इसे एक संगठित आंदोलन के रूप में पहचान मिली।
10. आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन-कौन सी हैं?
उत्तर:
- यथार्थवाद
- राष्ट्रवाद
- सामाजिक चेतना
- नारी विमर्श
- दलित एवं आदिवासी विमर्श
- प्रयोगशीलता
- आधुनिकता और उत्तर-आधुनिकता
11. क्या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता छायावादोत्तर युग के अंतर्गत आते हैं?
उत्तर:
नहीं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता छायावादोत्तर युग से प्रभावित अवश्य हैं, किंतु वे स्वतंत्र साहित्यिक युग या प्रवृत्तियाँ माने जाते हैं। छायावादोत्तर युग (1936–1947) को एक संक्रमणकाल माना जाता है, जिसमें साहित्य छायावादी कल्पना और रहस्यवाद से हटकर यथार्थ, जनसरोकार और विचारधारा की ओर अग्रसर हुआ। यह काल आगामी साहित्यिक आंदोलनों की भूमिका तैयार करता है।
- प्रगतिवाद (1936–1943) – सामाजिक यथार्थ और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रेरित।
- प्रयोगवाद (1943–1953) – ‘तार सप्तक’ से प्रारंभ होकर भाषा और शिल्प के प्रयोगों पर केंद्रित।
- नई कविता (1951 से आगे) – आधुनिकता, अस्तित्ववाद और शहरी संवेदना की अभिव्यक्ति।
इस प्रकार, ये तीनों प्रवृत्तियाँ छायावादोत्तर युग की वैचारिक पृष्ठभूमि में विकसित हुईं, लेकिन अपनी विशिष्ट समय-सीमा, काव्य-शैली और सौंदर्यशास्त्र के कारण ये छायावादोत्तर युग के अंतर्गत नहीं आतीं, बल्कि स्वतंत्र साहित्यिक युग के रूप में स्थापित होती हैं।
निष्कर्षतः, यह कहना उपयुक्त होगा कि:
“प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता – छायावादोत्तर युग की उपज तो हैं, परंतु अपने वैचारिक व कलात्मक वैशिष्ट्य के कारण स्वतंत्र साहित्यिक युग माने जाते हैं।”
इन्हें भी देखें –
- सुहाग की साड़ी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- पूस की रात | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- मृत्यु के पीछे | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- बूढ़ी काकी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- नागपूजा | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- सवा सेर गेंहूँ | कहानी – मुंशी प्रेमचंद
- शब्द किसे कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द
- पदबन्ध (Phrase) | परिभाषा, भेद एवं उदाहरण