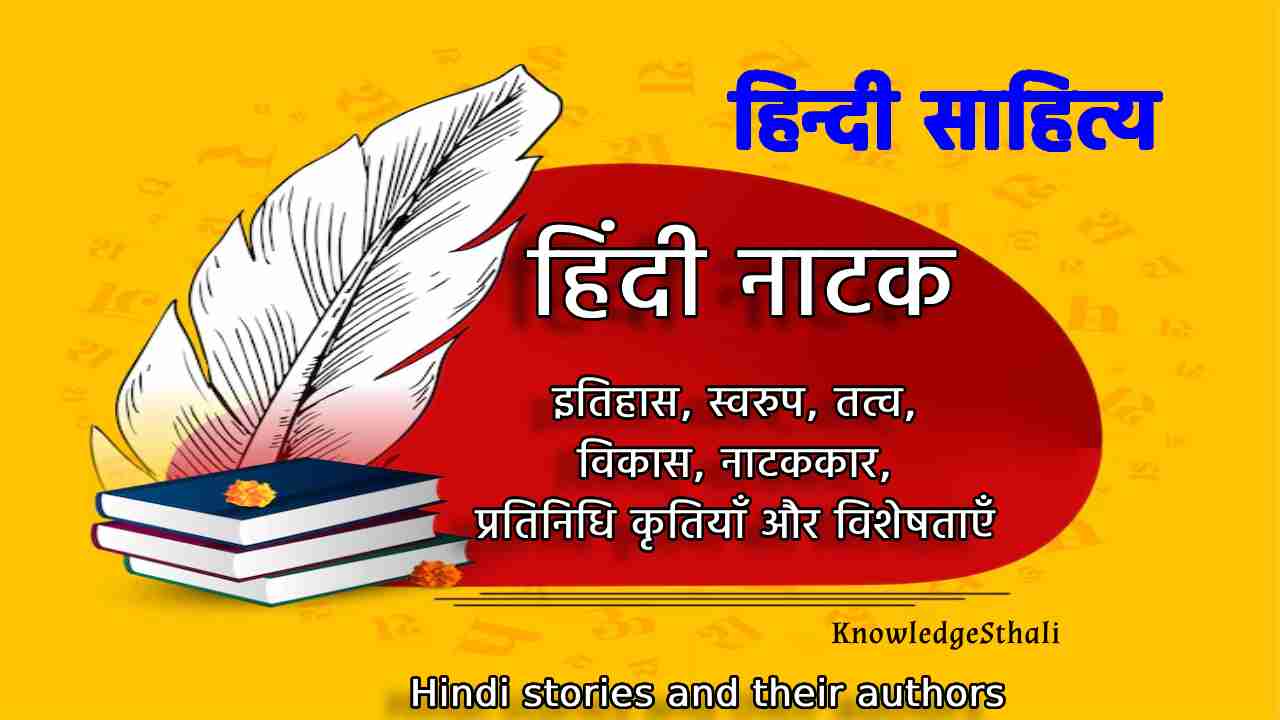मानव सभ्यता के आरंभिक काल से ही मनोरंजन, शिक्षा और विचार-प्रसार के विविध साधन प्रचलित रहे हैं। गीत, वाद्य और नृत्य जैसे कलात्मक माध्यमों के साथ-साथ नाटक भी एक प्रभावशाली और लोकप्रिय विधा के रूप में विकसित हुआ। नाटक केवल श्रवण के माध्यम से ही नहीं, बल्कि दृश्य अनुभव के माध्यम से भी रसास्वादन कराता है। यह साहित्य का वह रूप है जिसमें कथ्य और भाव का संप्रेषण अभिनय, संवाद, आंगिक-व्यंग, संगीत तथा मंच-सज्जा के सहारे किया जाता है।
नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज के विविध पक्षों को उजागर करना, नैतिक शिक्षा देना और मानवीय भावनाओं की गहराई तक पहुँचना भी है।
नाटक की परिभाषा
भरतमुनि के अनुसार —
“नाराभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्।
लोकवृत्तानुकरं नाट्यमेतन्मया कृतम्।।”
अर्थात, नाटक वह है जिसमें विविध प्रकार की अवस्थाओं से संपन्न पात्रों के माध्यम से लोकजीवन का अनुकरण किया जाता है।
सरल शब्दों में कहें तो — नाटक काव्य का ऐसा रूप है जो केवल श्रवण द्वारा ही नहीं, बल्कि दृष्टि के माध्यम से भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराता है। इसमें कथा को अभिनय, वाणी, हाव-भाव, संगीत, नृत्य और मंच-सज्जा के सहारे प्रस्तुत किया जाता है।
काव्य में नाटक का स्थान
इंद्रिय-ग्राह्यता के आधार पर काव्य के दो प्रमुख भेद माने गए हैं —
- श्रव्य काव्य — जिसे केवल सुना जा सकता है, जैसे — गीत, कविता, महाकाव्य।
- दृश्य काव्य — जिसे देखा और सुना, दोनों जा सकता है।
दृश्य काव्य को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है —
- रूपक
- उपरूपक
रूपक की परिभाषा है — “तदूपारोपात तु रूपम्”, अर्थात् किसी वस्तु का, किसी अन्य वस्तु में, कलात्मक रूप से आरोप ही रूपक है। नाटक रूपक का ही प्रमुख अंग है।
रूपक के भेद:
भारतीय आचार्यों ने वस्तु, नायक और रस के आधार पर रूपक के दस भेद बताए हैं —
- नाटक
- प्रकरण
- भाषा
- प्रहसन
- डिम
- व्यायोग
- समवकार
- वीथी
- अंक
- ईहामृग
इनमें नाटक सबसे प्रमुख और प्रचलित रूप है, इसलिए कई बार ‘रूपक’ शब्द का प्रयोग नाटक के लिए भी कर लिया जाता है।
आचार्यों के मतानुसार नाटक
- भरतमुनि — नाटक को तीनों लोकों के भावों का अनुकरण मानते हैं। उनका मत है कि इसमें नायक दिव्य, धीरोदात्त और उच्च कुल का होना चाहिए। कथा में सुख-दुख का संतुलन हो, रसों का समावेश हो, और प्रमुख रस श्रृंगार या वीर होना चाहिए। नाटक में पाँच से दस अंक होने चाहिए।
- धनंजय — नाटक को “अवस्था के अनुकरण” के रूप में परिभाषित करते हैं और इसके चार प्रकार के अभिनय मानते हैं — आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक।
- विश्वनाथ — नाटक की कथा इतिहास-प्रसिद्ध होनी चाहिए। कथानक पाँच संधियों (मुख, प्रतिमुख, गरभ, विमर्श, निरवहण) के अनुरूप हो और उसमें विलास, ऋद्धि आदि गुण हों। इसकी निबद्धता ऐसी हो जैसे गाय की पूँछ का अग्रभाग — अर्थात बीज रूप में कथा आरंभ होकर क्रमशः विकसित हो और चरमोत्कर्ष पर पहुँचे।
हिंदी का पहला नाटक
हिंदी साहित्य में नाटक विधा का प्रारंभिक चरण 19वीं शताब्दी के मध्य में देखा जाता है। हिंदी का पहला नाटक ‘नहुष’ है, जिसका रचनाकाल 1857 ई. माना जाता है। इसके रचनाकार गोपालचंद्र गिरधरदास थे। यह नाटक पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें राजा नहुष की कथा के माध्यम से सत्ता, अहंकार और नैतिक पतन के परिणाम को दर्शाया गया है।
‘नहुष’ न केवल हिंदी नाटक का प्रारंभिक उदाहरण है, बल्कि यह उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का भी प्रतिबिंब है। इसमें पौराणिक कथा के रूप में नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों का संदेश निहित है। यह नाटक संवादप्रधान है और इसका मंचन संभव होने के साथ-साथ पठनीय रूप में भी प्रभावशाली है।
1857 का काल भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम का समय था, इसलिए ‘नहुष’ में निहित सत्ता-लोलुपता और उसके दुष्परिणामों का संकेत उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों से भी जोड़ा जा सकता है। इस दृष्टि से यह नाटक केवल साहित्यिक रचना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी महत्व रखता है।
नाटक की संरचना
भारतीय नाट्यशास्त्र में नाटक की संरचना अत्यंत संगठित मानी गई है। इसके प्रमुख घटक हैं —
- कथानक (Plot) — मूल कथा, जो बीज रूप में प्रारंभ होकर क्रमशः विस्तार पाती है।
- पात्र (Characters) — नायक, नायिका, खलनायक, विदूषक, सहायक पात्र आदि।
- अंक (Acts) — प्राचीन नाटकों में प्रायः 5 से 10 अंक होते थे।
- संधियाँ (Junctures) — कथानक के पाँच चरण — मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निरवहण।
- रस और भाव (Rasa & Bhava) — नाटक का प्राण रस है। प्राचीन नाटक में श्रृंगार और वीर रस को प्रधानता दी जाती थी, किंतु हास्य, करुण, रौद्र, अद्भुत आदि रसों का भी प्रयोग होता है।
- अभिनय (Acting) — आंगिक (शारीरिक हाव-भाव), वाचिक (संवाद), आहार्य (वेशभूषा), सात्विक (मनःस्थितिजन्य भाव)।
- संवाद (Dialogue) — पात्रानुकूल, संक्षिप्त, भावपूर्ण, रसोत्पादक।
- मंच-सज्जा (Stagecraft) — दृश्य, प्रकाश, ध्वनि, वेशभूषा आदि।
नाटक के अंग (तत्व)
भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के आवश्यक अंगों में वस्तु (कथावस्तु), अभिनेता (पात्र) और रस को प्रमुख माना गया है, जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और शैली को भी समान महत्त्व प्रदान किया है।
इस प्रकार नाटक के सात मुख्य अंग होते हैं —
- वस्तु (कथावस्तु)
- अभिनेता (पात्र)
- रस
- कथोपकथन (संवाद)
- देशकाल (वातावरण)
- उद्देश्य
- शैली
1. वस्तु (कथावस्तु)
वस्तु से आशय नाटक की कथावस्तु से है। आचार्यों के अनुसार कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होनी चाहिए और मुखादि पाँच संधियों (मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहण), विलास, ऋद्धि आदि गुणों तथा विविध ऐश्वर्यों से युक्त होनी चाहिए।
इसकी निबद्धता गाय की पूँछ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए — अर्थात बीज रूप में कथा आरंभ होकर क्रमशः विकसित हो और अंत में फल प्राप्त करे।
कथावस्तु के भेद
- अधिकार दृष्टि से —
- आधिकारी कथा
- प्रासंगिक कथा (इसके भी दो भेद — पताका और प्रकरी)
- अभिनय दृष्टि से —
- दृश्य कथा
- श्रव्य कथा
- संवाद दृष्टि से —
- सर्व
- श्राव्य
- अश्राव्य (स्वागत तथा आकाशभाषित)
- नियत श्राव्य (इसके भी दो भेद — अपवारित और जनान्तिक)
- लोकवृत्त दृष्टि से —
- प्रख्यात
- उत्पाद्य
- मिश्र
कथावस्तु विन्यास के आधार
- कार्यावस्था — प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम
- अर्थ प्रकृति — बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी, कार्य
- संधि — मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहण
अर्थोपक्षेपक (कथा की सूचना देने वाले साधन) —
विषकम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार।
2. अभिनेता (पात्र)
पात्र नाटक का दूसरा प्रमुख अंग है। फल का अधिकारी पात्र नेता या नायक कहलाता है।
दशरूपककार के अनुसार नायक के गुण — विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रियवादी, लोकप्रिय, वाणी में निपुण, उच्चवंशीय, स्थिर स्वभाव वाला, युवा, बुद्धिमान, उत्साही, प्रज्ञावान, कलाविज्ञ, शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ और धार्मिक।
भरतमुनि के अनुसार नायक के चार प्रकार —
- धीरोदात्त
- धीरललित
- धीरप्रशांत
- धीरोद्धत
नायिका के तीन प्रकार —
- स्वकीया
- परकीया
- सामान्य
अन्य पात्र — पीठमर्द, प्रतिनायक, विदूषक, कंचुकी, प्रतिहार आदि।
3. रस
भरतमुनि के अनुसार नाटक में शांत रस को छोड़कर शेष सभी रसों का प्रयोग होना चाहिए।
मुख्य रस — श्रृंगार अथवा वीर, शेष रस — अंग रूप में प्रयुक्त।
नवरसों में से आठ का परिपाक —
- श्रृंगार
- हास्य
- रौद्र
- करुण
- वीर
- अद्भुत
- वीभत्स
- भयानक
अंगीरस निर्धारण के तीन मानक —
- नाटक में सर्वाधिक व्याप्त रस
- नाटक की परिणति में प्रकट होने वाला रस
- नायक में निहित रस की प्रवृत्ति
4. कथोपकथन (संवाद)
संवाद नाटक की आत्मा हैं। इनके माध्यम से ही कथानक का विकास और पात्रों का चरित्र-चित्रण होता है।
संवादों में —
- संक्षिप्तता
- रसानुभूति क्षमता
- सरलता
- औचित्य
- सजीवता
- पात्रानुकूलता
होना आवश्यक है।
गंभीर दार्शनिक विषयों का अधिक प्रयोग न हो, ताकि रसास्वादन में बाधा न आए।
कभी-कभी स्वागत कथन और गीत का भी प्रयोग किया जाता है।
5. देशकाल (वातावरण)
नाटक में देशकाल का चित्रण यथार्थ और युगानुकूल होना चाहिए।
पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में देशकाल अंतर्गत संकलनत्रय (समय, स्थान, कार्य) का उल्लेख है, जो यूनानी रंगमंच के अनुकूल था।
भारतीय दृष्टिकोण में यद्यपि यह अनिवार्य नहीं, परंतु स्वाभाविकता, औचित्य और सजीवता हेतु पात्रों की वेशभूषा, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों और युग-विशेष का ध्यान रखना आवश्यक है।
6. उद्देश्य
भारतीय दृष्टिकोण में नाटक का उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ समाज में उत्साह, आशा और नैतिक भावनाओं का संचार करना है।
संस्कृत नाटकों में अधिकांशतः सुखांत होते हैं।
पाश्चात्य प्रभाव से हिन्दी में कुछ दुखांत नाटक भी लिखे गए, परंतु अधिक दुखांत अंत दर्शकों में उदासी और निराशा उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनका प्रचार सीमित होना चाहिए।
7. शैली
नाटक सर्वसाधारण की कला है, अतः इसकी भाषा-शैली —
- सरल
- स्पष्ट
- सुबोध
होनी चाहिए, ताकि दर्शक को बौद्धिक श्रम न करना पड़े और रसास्वादन में बाधा न आए।
क्लिष्ट, दुरूह भाषा से बचना चाहिए और शैली परिस्थिति व पात्रानुकूल होनी चाहिए।
नाटक की विशेषताएँ
- दृश्य और श्रव्य दोनों का समन्वय — नाटक पढ़ा भी जा सकता है और मंच पर देखा भी जा सकता है।
- रसास्वादन की क्षमता — नाटक का उद्देश्य दर्शकों में रसानुभूति उत्पन्न करना है।
- संक्षिप्तता और सजीवता — संवाद और कथोपकथन अनावश्यक विस्तार से मुक्त, पात्र और स्थिति के अनुकूल।
- औचित्य — कथानक, संवाद, पात्र, वेशभूषा — सब में परिस्थितियों का उचित सामंजस्य।
- सजीव चरित्र-चित्रण — पात्रों के व्यक्तित्व में जीवंतता और यथार्थता।
- नैतिक और सामाजिक उद्देश्य — मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा और प्रेरणा।
अभिनय के चार अंग
धनंजय और अन्य आचार्यों ने अभिनय को चार अंगों में विभाजित किया है —
- आंगिक अभिनय — शरीर के हाव-भाव, मुद्राएँ, नेत्रों की गति।
- वाचिक अभिनय — संवाद की शैली, स्वर, लय, उच्चारण।
- आहार्य अभिनय — वस्त्र, आभूषण, मेकअप, मंच सज्जा।
- सात्विक अभिनय — मानसिक भावों का स्वाभाविक प्रदर्शन, जैसे भय, लज्जा, क्रोध, आनंद।
हिन्दी नाटक का इतिहास
हिन्दी साहित्य में नाटक का विकास अपेक्षाकृत देर से हुआ।
- हिन्दी का प्रथम नाटक — ‘नहुष’ (1857 ई.) लेखक — गोपाल चन्द्र गिरधरदास।
- प्रारंभिक दौर में नाटक का स्वरूप अनुवाद और रूपांतर पर आधारित था। बाद में मौलिक रचनाएँ सामने आईं।
- भारतेंदु हरिश्चंद्र (1850–1885) को हिन्दी नाटक का जनक माना जाता है। उनके नाटक ‘सत्य हरिश्चंद्र’, ‘अंधेर नगरी’ आदि आज भी लोकप्रिय हैं।
- द्विवेदी युग और छायावाद काल में नाटकों ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों को अपनाया।
- आधुनिक युग में मोहन राकेश, विजय तेंडुलकर, हबीब तनवीर, भीष्म साहनी आदि ने नाटक को नए प्रयोग, यथार्थवाद और प्रयोगधर्मिता की दिशा दी।
हिन्दी साहित्य में नाटकों का प्रारम्भ
हिन्दी साहित्य में नाट्यकला का व्यवस्थित विकास भारतेन्दु युग से माना जाता है। यद्यपि इसके पहले भी कुछ नाटकीय रचनाएँ हुईं, किन्तु वे या तो संस्कृत, फारसी अथवा अन्य भाषाओं के रूपांतरण थे और हिन्दी नाटक की स्वतंत्र परंपरा का हिस्सा नहीं बन पाए।
भारतेन्दु युग (1850–1900 ई.)
हिन्दी नाटकों के प्रारम्भ का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। उन्होंने अपने पिता गोपालचंद्र गिरिधरदास द्वारा रचित नहुष (1857) को हिन्दी का प्रथम नाटक स्वीकार किया।
भारतेन्दु स्वयं अत्यंत प्रतिभाशाली नाटककार थे। उन्होंने सत्रह मौलिक एवं अनूदित नाटकों की रचना की, जिनमें सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक सभी विषय शामिल थे।
उनके नाटक जैसे अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा ने हिन्दी नाटक को जन-जागरण का माध्यम बनाया।
द्विवेदी युग (1900–1920 ई.)
इस युग में हिन्दी नाटक साहित्यिक दृष्टि से बहुत आगे नहीं बढ़ सका। अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित थे।
इस काल की रचनाओं का महत्व मुख्यतः ऐतिहासिक है, क्योंकि इस समय नाट्य मंचन की परंपरा और पाठकीय आधार अभी विकसित हो रहे थे।
छायावाद युग (1918–1936 ई.)
छायावाद काल में जयशंकर प्रसाद ने हिन्दी नाटक को एक नई ऊँचाई प्रदान की।
उन्होंने स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त जैसे नाटकों के माध्यम से काव्यात्मक भाषा, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण और प्रतीकात्मकता का सुंदर मेल प्रस्तुत किया।
इसी समय पारसी रंगमंच के प्रभाव से भी अनेक नाट्य रचनाएँ मंच पर आईं, जो लोकप्रिय मनोरंजन के साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम बनीं।
छायावादोत्तर युग और आधुनिक नाटक
छायावाद के बाद के समय में नाट्य साहित्य की रचना अधिक मात्रा में होने लगी।
इस काल में मंच तकनीक, संवाद शैली और यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट दिखा।
प्रमुख नाटककार और उनकी कृतियाँ —
- लक्ष्मीनारायण मिश्र — चक्रव्यूह, सम्राट अशोक
- उपेन्द्रनाथ अश्क — अंजो दीदी
- विष्णु प्रभाकर — डॉक्टर
- जगदीशचंद्र माथुर — कोनार्क
- लक्ष्मीनारायण लाल — सुन्दर रस, मादा कैक्टस
- मोहन राकेश — आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस
- हरिकृष्ण प्रेमी, उदयशंकर भट्ट, विनोद रस्तोगी (नया हाथ)
- नरेश मेहता, सुरेन्द्र वर्मा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री (शुतुरमुर्ग)
- मुद्रा राक्षस — आगरा बाजार आदि
प्रमुख हिन्दी नाटककार और उनके प्रतिनिधि नाटक
1. प्रारंभिक दौर
- गोपाल चन्द्र गिरधरदास — नहुष
- भारतेंदु हरिश्चंद्र — अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र
2. द्विवेदी युग
- जयशंकर प्रसाद — स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त
- माधव शुक्ल — वीर अभिमन्यु
3. छायावाद और प्रगतिवाद
- सुमित्रानंदन पंत — राज्यपाल (काव्य-नाटक)
- धर्मवीर भारती — अंधा युग
- रमेशचंद्र शाह — पार्टी इज़ ओवर
4. आधुनिक और प्रयोगधर्मी रंगमंच
- मोहन राकेश — आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस
- विजय तेंडुलकर — घासीराम कोतवाल (यद्यपि मराठी में, हिन्दी मंच पर अत्यंत लोकप्रिय)
- हबीब तनवीर — चरणदास चोर, मिट्टी की गाड़ी
5. समकालीन और उत्तर-आधुनिक
- भीष्म साहनी — तमस (नाट्य रूपांतरण), कबिरा खड़ा बाज़ार में
- महेश दत्तानी (हिन्दी अनुवाद में चर्चित) — तारा
- गिरीश कर्नाड (हिन्दी अनुवाद में) — तुगलक, हयवदन
- उषा गांगुली — कोर्ट मार्शल, रुदाली
हिन्दी नाटक का विकास : कालानुक्रमिक चार्ट
| कालखंड / युग | समयावधि | प्रमुख विशेषताएँ | प्रतिनिधि नाटक |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक युग | 1850–1870 ई. | हिन्दी में नाटक लेखन का प्रारंभ, मुख्यतः अनुवाद और रूपांतर; पौराणिक व ऐतिहासिक कथानक | नहुष (गोपाल चन्द्र गिरधरदास, 1857) |
| भारतेंदु युग | 1870–1885 ई. | मौलिक हिन्दी नाटकों की शुरुआत; सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक विषय; भाषा सरल; जनजागरण का उद्देश्य | अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा (भारतेंदु हरिश्चंद्र) |
| द्विवेदी युग | 1900–1920 ई. | नाटकों में नैतिक शिक्षा और सुधारवादी दृष्टिकोण; ऐतिहासिक व सामाजिक समस्याओं पर जोर | वीर अभिमन्यु (जयशंकर प्रसाद), चंद्रगुप्त |
| छायावाद युग | 1920–1940 ई. | काव्यात्मक भाषा, प्रतीकात्मकता, ऐतिहासिक और पौराणिक पुनर्निर्माण | स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी (जयशंकर प्रसाद) |
| प्रगतिवादी युग | 1936–1950 ई. | यथार्थवादी दृष्टि, श्रमिक जीवन, सामाजिक संघर्ष, राष्ट्रीय चेतना | अंधा युग (धर्मवीर भारती), लहू के दो रंग |
| आधुनिक प्रयोगधर्मी युग | 1950–1980 ई. | मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सामाजिक विडंबनाएँ, मंच तकनीक में नवाचार | आषाढ़ का एक दिन, अंधेरों का दीपक (मोहन राकेश), घासीराम कोतवाल (विजय तेंडुलकर) |
| उत्तर-आधुनिक और समकालीन रंगमंच | 1980 से वर्तमान | समकालीन समस्याएँ, स्त्री विमर्श, दलित चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, बहुभाषिक प्रयोग | तमस (भीष्म साहनी), चरणदास चोर (हबीब तनवीर), मधुकर |
नाटक में अभिनय
अभिनय किसी भी नाटक का मूल भाव और प्रमुख विशेषता है। यह नाटक की वह शक्ति है जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें कथा, पात्र और भावनाओं से जोड़ती है। अभिनय के बिना नाटक केवल लिखित शब्दों तक सीमित रह जाता है; मंच पर उसे जीवन प्रदान करने का कार्य अभिनय ही करता है।
नाटककार के लिए यह आवश्यक है कि वह नाटक के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट, परिधान, मंच व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि सभी पहलुओं पर ध्यान दे, ताकि नाटक के सभी तत्व प्रभावी और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हों। रंगमंच के विधि-विधान और तकनीकी पक्ष भी अभिनय की सफलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अभिनय की गुणवत्ता मुख्य रूप से पात्रों के वाक्चातुर्य, शारीरिक हावभाव और अंतरंग भाव-प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यही एक सफल नाटक की पहचान होती है — जब दर्शक स्वयं को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं।
धनंजय के अनुसार अभिनय के चार प्रकार
- आंगिक अभिनय
- शरीर के हावभाव, नेत्रों की गति, हाथ-पाँव की मुद्राएँ, चेहरे के भाव आदि के माध्यम से किया जाने वाला अभिनय।
- उदाहरण: आश्चर्य व्यक्त करने के लिए नेत्र फैलाना, क्रोध के समय माथे पर बल डालना।
- वाचिक अभिनय
- संवाद बोलने की कला, स्वर की ऊँच-नीच, ठहराव, गति, लय और उच्चारण की सटीकता।
- उदाहरण: वीर रस के दृश्य में ऊँचे स्वर और दृढ़ लहजे का प्रयोग।
- आहार्य अभिनय
- वेशभूषा, आभूषण, मेकअप, मंच-सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और अन्य दृश्य-तत्व।
- उदाहरण: पौराणिक नाटक में पात्र के अनुरूप पोशाक और आभूषण का प्रयोग।
- सात्विक अभिनय
- मनोभावों का आंतरिक और स्वाभाविक प्रदर्शन, जो सीधे दर्शकों की संवेदनाओं को स्पर्श करे।
- उदाहरण: करुण दृश्य में आँखों से स्वतः आँसू आना, भय के समय शरीर का कांपना।
नाटक का संकलन
नाटक के निर्माण में संकलन का अर्थ है — कथानक, समय, स्थान और घटनाओं का ऐसा संयोजन, जिससे कथा में एकता, संगति और प्रभावशीलता बनी रहे। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में इसे विशेष महत्त्व दिया गया है और इसे संकलनत्रय कहा गया है।
संकलनत्रय (Three Unities)
- काल संकलन (Unity of Time)
- कथा का सम्पूर्ण घटनाक्रम सीमित समयावधि में घटित होना चाहिए, जिससे नाटक में यथार्थता और एकता बनी रहे।
- यूनानी नाटकों में प्रायः यह समयावधि 24 घंटे से अधिक नहीं होती थी।
- स्थल संकलन (Unity of Place)
- नाटक की समस्त घटनाएँ एक ही स्थान पर घटित हों या स्थान परिवर्तन बहुत सीमित और संगतिपूर्ण हो।
- इससे दर्शक का ध्यान कथा पर केंद्रित रहता है।
- कार्य संकलन (Unity of Action)
- कथा में एक ही मुख्य कथावस्तु हो और घटनाएँ उसी के इर्द-गिर्द बुनी जाएँ।
- उपकथाएँ भी मुख्य कथा से जुड़ी और उसे आगे बढ़ाने वाली हों।
भारतीय दृष्टिकोण में संकलन
भारतीय आचार्यों ने यद्यपि संकलनत्रय की अनिवार्यता पर बल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने नाटक में औचित्य, स्वाभाविकता और रस-प्रधानता को आवश्यक माना।
साथ ही, उन्होंने कुछ प्रसंगों को नाटक में शामिल करने की शास्त्रीय अनुमति नहीं दी —
- रंगमंच के लिए असुविधाजनक प्रसंग
- जीवन के असामान्य, अरोचक और अत्यधिक इतिवृत्तात्मक प्रसंग
- आतंकप्रद (बहुत भयावह) घटनाएँ
- अत्यधिक करुणाजनक या त्रासद घटनाएँ
- जगुप्साद्योतक (घृणाजनक) प्रसंग
- अश्लील या भारतीय संस्कृति के विपरीत दृश्य
भारतीय दृष्टि में नाटक का उद्देश्य केवल घटनाओं का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रसोत्पत्ति और सांस्कृतिक-नैतिक upliftment है। इसलिए संकलन का प्रयोग भी उसी के अनुरूप होना चाहिए।
नाटक के प्रकार
भारतीय परंपरा और आधुनिक संदर्भ में नाटकों के कई प्रकार हैं —
- प्राचीन रूपक नाटक — नाटक, प्रकरण, व्यायोग, प्रहसन आदि।
- आधुनिक विभाजन —
- सामाजिक नाटक
- ऐतिहासिक नाटक
- पौराणिक नाटक
- समस्या-प्रधान नाटक
- प्रयोगधर्मी नाटक
- एकांकी नाटक
- लोकनाट्य (जैसे नौटंकी, भवाई, यक्षगान, तमाशा)।
हिन्दी नाटकों के उदाहरण और उनके नाटककार
| क्रम | नाटक / कृतियाँ | नाटककार |
|---|---|---|
| 1 | रामायण महानाटक | प्राणचंद चौहान |
| 2 | आनंद रघुनंदन | महाराज विश्वनाथ सिंह |
| 3 | नहुष | गोपालचंद्र गिरिधरदास |
| 4 | अनूदित नाटक — विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखण्ड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत-जननी, मुद्राराक्षस, दुर्लभ बंधु मौलिक नाटक — वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्यहरिश्चंद्र, श्रीचंद्रावली, विषस्य विषमौषधम, भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, अँधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम योगिनी | भारतेंदु हरिश्चंद्र |
| 5 | कृष्ण-सुदामा नाटक | शिवनंदन सहाय |
| 6 | संयोगिता स्वयंवर, प्रह्लाद-चरित्र, रणधीर प्रेममोहिनी, तप्त संवरण | लाला श्रीनिवासदास |
| 7 | अमरसिंह राठौर, बूढ़े मुँह मुँहासे (प्रहसन) | राधाचरण गोस्वामी |
| 8 | मयंक मंजरी, प्रणयिनी-परिणय | किशोरीलाल गोस्वामी |
| 9 | भारत-दुर्दशा, कलिकौतुक रूपक, संगीत शाकुंतल, हठी हम्मीर | प्रताप नारायण मिश्र |
| 10 | कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर, जैसा काम वैसा परिणाम (प्रहसन), नई रोशनी का विष, वेणुसंहार | बालकृष्ण भट्ट |
हिन्दी नाटक का कालानुक्रमिक विकास — प्रमुख नाटककार और उनकी प्रतिनिधि कृतियाँ
| काल/युग | प्रमुख नाटककार | प्रतिनिधि कृतियाँ |
|---|---|---|
| भारतेन्दु युग (1870–1885) | गोपालचंद्र गिरिधरदास | नहुष |
| भारतेंदु हरिश्चंद्र | अंधेर नगरी, भारत-दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नीलदेवी, श्रीचंद्रावली, सती प्रताप | |
| प्राणचंद चौहान | रामायण महानाटक | |
| महाराज विश्वनाथ सिंह | आनंद रघुनंदन | |
| लाला श्रीनिवासदास | संयोगिता स्वयंवर, प्रह्लाद-चरित्र | |
| प्रताप नारायण मिश्र | कलिकौतुक रूपक, संगीत शाकुंतल, हठी हम्मीर | |
| बालकृष्ण भट्ट | दमयंती स्वयंवर, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल | |
| राधाचरण गोस्वामी | अमरसिंह राठौर, बूढ़े मुँह मुँहासे (प्रहसन) | |
| शिवनंदन सहाय | कृष्ण-सुदामा नाटक | |
| किशोरीलाल गोस्वामी | मयंक मंजरी, प्रणयिनी-परिणय | |
| द्विवेदी युग (1900–1920) | रघुनंदन प्रसाद | सूर्य विजय |
| श्रीधर पाठक | रत्नाकर, संध्या | |
| छायावाद युग (1920–1940) | जयशंकर प्रसाद | ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजयतशत्रु, राज्यश्री |
| सियाराम शरण गुप्त | तुलसीदास | |
| रामकुमार वर्मा | अग्निमित्र, वीर सिंह देव, सृजन की बेला | |
| छायावादोत्तर युग (1940–1960) | लक्ष्मीनारायण मिश्र | चक्रव्यूह, सम्राट अशोक, संन्यासिनी |
| उपेन्द्रनाथ अश्क | अंजो दीदी, एक आदमी | |
| विष्णु प्रभाकर | डॉक्टर, आवारा | |
| जगदीशचंद्र माथुर | कोनार्क, ओह किरण | |
| हरिकृष्ण प्रेमी | सागर मेघ | |
| उदयशंकर भट्ट | नवरत्न | |
| विनोद रस्तोगी | नया हाथ | |
| आधुनिक युग (1960–वर्तमान) | मोहन राकेश | आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे-अधूरे |
| नरेश मेहता | संस्कार की धार | |
| सुरेन्द्र वर्मा | मृगनयनी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक | |
| ज्ञानदेव अग्निहोत्री | शुतुरमुर्ग | |
| मुद्रा राक्षस | आगरा बाजार, अंधायुग पर प्रतिक्रिया | |
| धर्मवीर भारती | अंधायुग, कनुप्रिया | |
| असगर वजाहत | जिन लाहौर नहीं वेख्या, गोधूलि |
नाटक का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व
नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह —
- समाज का दर्पण है — उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है।
- नैतिक मूल्यों का प्रचार करता है।
- सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण और प्रसार करता है।
- भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि कलाओं का समन्वय करता है।
- जन-जागरण का माध्यम बनता है — राजनीतिक, सामाजिक आंदोलनों में नाटकों ने बड़ी भूमिका निभाई है।
निष्कर्ष
नाटक साहित्य की अत्यंत सशक्त विधा है, जिसमें शब्द, भाव, अभिनय और दृश्य सभी का अद्भुत संगम होता है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से लेकर आधुनिक प्रयोगधर्मी रंगमंच तक, नाटक ने समय के साथ नए रूप और नए विषय अपनाए हैं। यह न केवल रसास्वादन का साधन है, बल्कि समाज-जीवन की गहनतम सच्चाइयों को उजागर करने का माध्यम भी है।
इन्हें भी देखें –
- हिंदी नाटक और नाटककार – लेखक और रचनाएँ
- सूफी काव्य धारा: निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा | कवि, रचनाएँ एवं भाषा शैली
- निर्गुण भक्ति काव्य धारा: अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और साहित्यिक विशेषताएँ
- सगुण भक्ति काव्य धारा: अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और साहित्यिक विशेषताएँ
- भक्ति काल के कवि और उनके काव्य (रचनाएँ)
- अष्टछाप के कवि: परिचय, रचनाएँ और ऐतिहासिक महत्व
- चम्पू साहित्य | गद्य और पद्य का अद्वितीय संगम
- नाथ संप्रदाय (साहित्य): योग, तंत्र और साधना की भारतीय परंपरा का अनूठा अध्याय
- सिद्ध साहित्य: हिन्दी साहित्य का आदिरूप और सामाजिक चेतना का संवाहक
- जैन साहित्य: स्वरूप, विकास, प्रमुख कवि, कृतियाँ और साहित्यिक विशेषताएँ