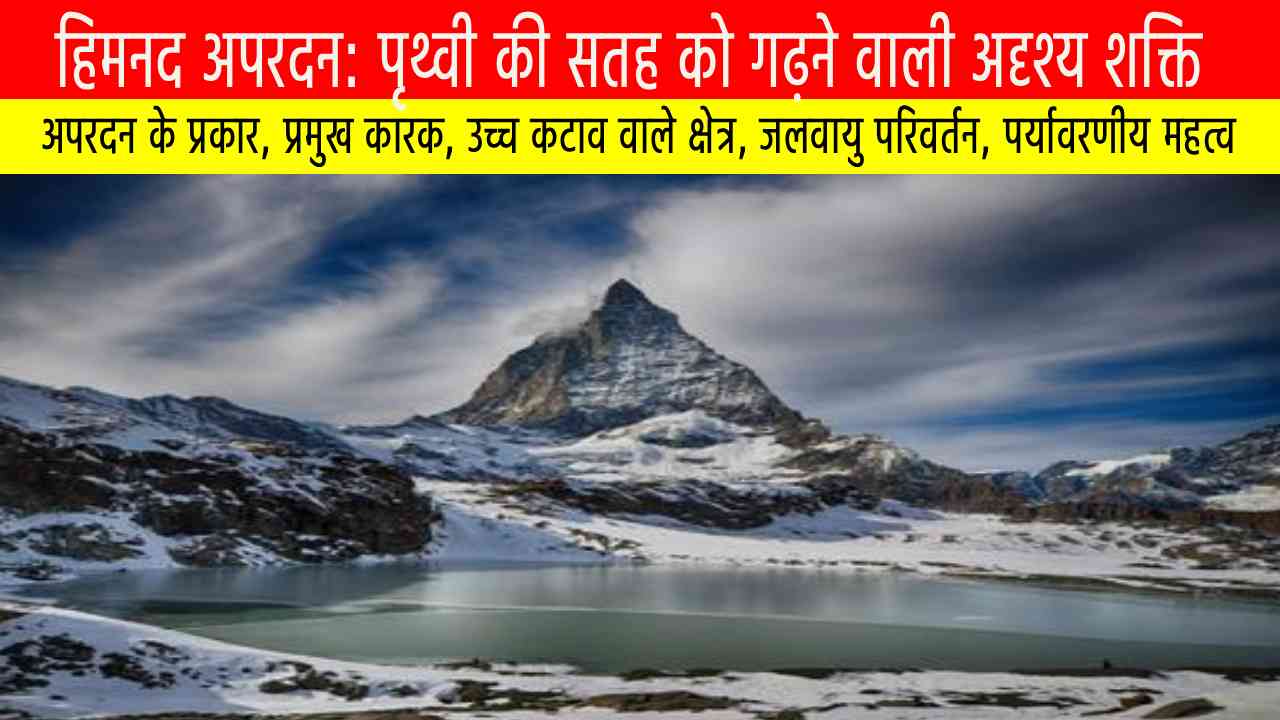पृथ्वी की सतह लगातार परिवर्तित होती रहती है। यह परिवर्तन कभी धीमे, तो कभी तेज़ रूप में घटित होता है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ या तूफान जैसे तात्कालिक प्राकृतिक आपदाएँ कुछ घंटों या दिनों में भूमि के स्वरूप को बदल सकती हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाएँ बेहद धीमी गति से कार्य करती हैं और लाखों वर्षों में परिदृश्य को नया आकार देती हैं। हिमनद अपरदन (Glacial Erosion) ऐसी ही एक प्रक्रिया है, जो भले ही हमारी नंगी आँखों से तुरंत दिखाई न दे, लेकिन इसका असर गहरा और स्थायी होता है।
हाल ही में नेचर जिओसाइंस में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन ने हिमनद अपरदन की दर और उसके प्रभावों के बारे में चौंकाने वाले आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस अध्ययन में भारत के प्रमुख ग्लेशियरों — गंगोत्री, डॉकरीआनी और सियाचिन — को भी शामिल किया गया है। इस शोध ने स्पष्ट किया है कि ग्लेशियर न केवल जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेतक हैं, बल्कि वे पृथ्वी की सतह को तराशने वाले सबसे प्रभावी प्राकृतिक औज़ारों में से एक हैं।
हिमनद अपरदन क्या है?
हिमनद अपरदन का अर्थ है, बर्फ की मोटी परतों — जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं — द्वारा चट्टानों और मिट्टी को घिसकर, काटकर और हटाकर नए भौगोलिक आकार बनाना। जब ग्लेशियर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और स्वयं के वजन के कारण नीचे की ओर खिसकते हैं, तो वे अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को खुरचते, तोड़ते और घसीटते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप घाटियाँ, झीलें, U-आकार की घाटियाँ, मोरेन और अन्य भू-आकृतिक संरचनाएँ बनती हैं।
अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष
1. कटाव दर (Erosion Rates)
इस वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि दुनिया के 99% ग्लेशियरों में अनुमानित कटाव दर 0.02 मिलीमीटर/वर्ष से 2.68 मिलीमीटर/वर्ष के बीच है। सुनने में यह आंकड़ा बेहद छोटा लगता है, लेकिन भूगर्भीय समयमान पर यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में लाखों वर्षों तक ग्लेशियर सक्रिय रहें, तो ये कुछ मीटर मोटी चट्टानी परत को पूरी तरह हटा सकते हैं।
2. अवसाद हटाना (Sediment Removal)
शोध के अनुसार, सभी ग्लेशियर मिलकर हर साल लगभग 23 गीगाटन चट्टानी सतह का क्षरण करते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि यह मात्रा लगभग 9,200 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूलों को ठोस चट्टानी सामग्री से भर सकती है। यह अवसाद नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुँचता है, जिससे समुद्र तल की संरचना, पारिस्थितिकी और पोषक चक्र प्रभावित होते हैं।
3. उच्च कटाव वाले क्षेत्र
वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ क्षेत्रों में ग्लेशियर अपरदन की दर अपेक्षाकृत अधिक है। इनमें प्रमुख हैं:
- अलास्का – यहाँ के मरीन-टर्मिनेटिंग ग्लेशियर समुद्र में मिलते हैं और अपनी उच्च गति के कारण चट्टानों को तेजी से घिसते हैं।
- मध्य व दक्षिण एशिया – हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश क्षेत्रों के ग्लेशियर बर्फ के विशाल भंडार हैं और तीव्र कटाव करते हैं।
- कॉकसस एवं मध्य पूर्व – यहाँ के पर्वतीय ग्लेशियर छोटे होने के बावजूद सक्रिय अपरदन करते हैं।
- न्यूज़ीलैंड – साउथ आइलैंड के फ्रांज जोसेफ और फॉक्स ग्लेशियर जैसे तेजी से बहने वाले ग्लेशियर अपरदन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
4. प्रमुख कारक (Main Drivers)
अध्ययन ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्लेशियर की गति (velocity) ही कटाव का एकमात्र निर्धारक कारक नहीं है। वास्तव में, वर्षा, ऊँचाई, लंबाई, अक्षांश (latitude) और भूविज्ञान जैसे कारक अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ग्लेशियर अधिक नमी पाकर तेज़ी से बढ़ते और गतिशील रहते हैं, जिससे अपरदन बढ़ता है।
- ऊँचाई और भूविज्ञान (चट्टानों का प्रकार और संरचना) यह तय करते हैं कि ग्लेशियर कितनी आसानी से चट्टान को काट सकते हैं।
5. पर्यावरण–विशिष्ट मॉडल
शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के ग्लेशियरों के लिए अलग-अलग समीकरण विकसित किए हैं:
- सर्ज-टाइप ग्लेशियर – जो अचानक तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्षों में अत्यधिक अपरदन कर सकते हैं।
- मरीन-टर्मिनेटिंग ग्लेशियर – जो समुद्र में समाप्त होते हैं और पिघलने के साथ-साथ समुद्र तल पर भी अवसाद जमा करते हैं।
- लैंड-टर्मिनेटिंग ग्लेशियर – जो भूमि पर समाप्त होते हैं और अक्सर नदी प्रणालियों में बड़े पैमाने पर अवसाद पहुंचाते हैं।
6. भारत की भागीदारी
भारत के संदर्भ में, गंगोत्री ग्लेशियर (उत्तराखंड), डॉकरीआनी ग्लेशियर (उत्तरकाशी) और सियाचिन ग्लेशियर (लद्दाख) को इस अध्ययन में शामिल किया गया।
- गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है और उत्तराखंड की जल-आपूर्ति, कृषि और धार्मिक महत्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- डॉकरीआनी ग्लेशियर यमुना नदी की सहायक धारा भागीरथी को जल देता है और इसके अपरदन से आने वाला अवसाद टिहरी क्षेत्र के नदी तल पर असर डालता है।
- सियाचिन ग्लेशियर, जिसे दुनिया का सबसे ऊँचा और सबसे लंबा सैन्यीकृत ग्लेशियर माना जाता है, सामरिक दृष्टि से भी अहम है और इसके अपरदन का अध्ययन जलवायु और भू-राजनीति दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
हिमनद अपरदन के प्रकार
वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमनद अपरदन मुख्यतः तीन तरीकों से होता है:
- प्लकिंग (Plucking) – जब बर्फ पिघलकर चट्टानों की दरारों में जाती है, फिर जमकर उन्हें तोड़ देती है और ग्लेशियर उन्हें अपने साथ खींच लेता है।
- अब्रेशन (Abrasion) – बर्फ के साथ घिसटती चट्टानें नीचे की सतह को सैंडपेपर की तरह रगड़ती हैं, जिससे चट्टान पर खरोंच और पॉलिश जैसी सतह बनती है।
- फ्रीज़–थॉ वेदरिंग (Freeze–Thaw Weathering) – बार-बार जमने और पिघलने से चट्टान टूटकर छोटे टुकड़ों में बदल जाती है।
हिमनद अपरदन का पर्यावरणीय महत्व
- नदी तल निर्माण – ग्लेशियरों द्वारा हटाए गए अवसाद नदियों में पहुँचकर उनके तल की गहराई, चौड़ाई और प्रवाह को प्रभावित करते हैं।
- झीलों का निर्माण – कई झीलें, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में, ग्लेशियर द्वारा बनाई गई घाटियों में पिघले पानी से भर जाती हैं।
- मृदा निर्माण – महीन अवसाद मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, जो कृषि के लिए लाभकारी है।
- बाढ़ जोखिम – अत्यधिक अवसाद नदियों के तल को ऊँचा कर सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।
जलवायु परिवर्तन और हिमनद अपरदन
ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण:
- ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अपरदन की गति में बदलाव आ रहा है।
- कुछ क्षेत्रों में ग्लेशियर पीछे हटने के कारण अपरदन कम हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक चरण में पिघलने से गति बढ़ने पर अपरदन दर अस्थायी रूप से तेज़ हो सकती है।
- अवसाद की अधिक मात्रा नदियों में जाकर जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकती है।
वैज्ञानिक और नीतिगत महत्त्व
इस अध्ययन के निष्कर्ष न केवल भूविज्ञान बल्कि जलवायु विज्ञान, जल संसाधन प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अहम हैं।
- जलवायु मॉडलिंग में ग्लेशियर अपरदन को शामिल करने से नदियों के भविष्य के प्रवाह का बेहतर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
- बाढ़ प्रबंधन योजनाओं में अवसाद प्रवाह के आंकड़ों का उपयोग करके बाँधों और जलाशयों की डिजाइनिंग अधिक सुरक्षित बनाई जा सकती है।
- पर्यावरण संरक्षण के तहत उच्च कटाव वाले क्षेत्रों में पर्यटन और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है।
निष्कर्ष
हिमनद अपरदन पृथ्वी की सतह के निर्माण और परिवर्तन में एक मौन लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। नेचर जिओसाइंस का यह अध्ययन दर्शाता है कि हर साल दुनिया भर के ग्लेशियर मिलकर अरबों टन चट्टानी सतह का क्षरण करते हैं और यह प्रक्रिया हमारे नदियों, समुद्रों और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालती है।
भारत के गंगोत्री, डॉकरीआनी और सियाचिन जैसे ग्लेशियर न केवल जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं, बल्कि वे हमारी नदियों और भू-आकृतियों के वास्तुकार भी हैं। भविष्य की जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए हिमनद अपरदन की सटीक निगरानी और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण अनिवार्य है।
इन्हें भी देखें –
- संचार मित्र योजना: एक डिजिटल जागरूकता पहल की विस्तृत समीक्षा
- चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता: कोल पामर का चमकदार प्रदर्शन
- विश्व मुक्केबाज़ी कप 2025 में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन: 11 पदक जीतकर रचा नया इतिहास
- एलन मस्क का नया राजनीतिक कदम: “अमेरिका पार्टी” की घोषणा
- निद्रा रोग (Sleeping Sickness): परिचय, स्थिति, और वैश्विक दृष्टिकोण
- संजोग गुप्ता बने ICC के नए CEO | विश्व क्रिकेट को मिलेगी नई दिशा और दृष्टि
- चारणी साहित्य (रासो साहित्य): वीरगाथात्मक परंपरा का अद्भुत विरासत
- प्रकीर्णक (लौकिक) साहित्य: श्रृंगारिकता और लोकसंवेदना का आदिकालीन स्वरूप