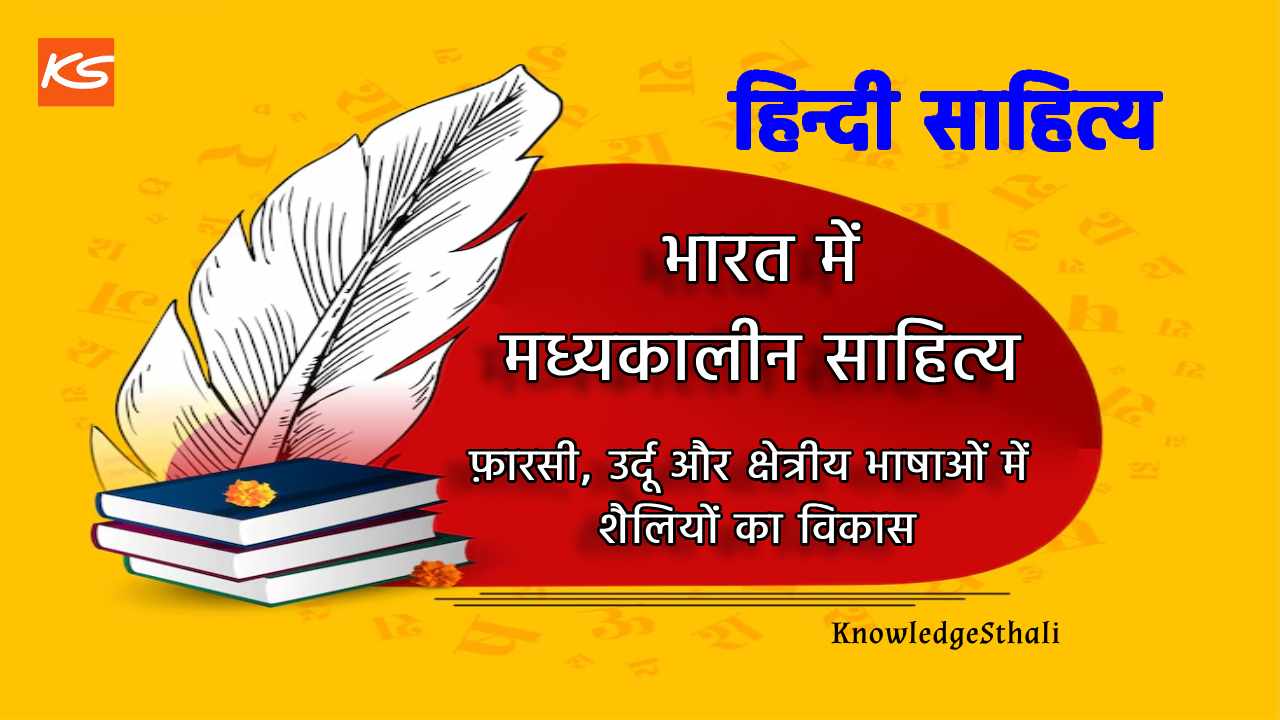भारत का साहित्यिक इतिहास बहुत ही समृद्ध और बहुआयामी रहा है। यदि हम मध्यकालीन साहित्य की चर्चा करें, तो यह समय भारतीय भाषाओं, संस्कृत परंपरा, फ़ारसी प्रभाव और उर्दू की उत्पत्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक फैले इस युग में भारतीय साहित्य ने विविध रूपों और शैलियों का विकास किया। भक्ति आंदोलन, सूफी परंपरा, दरबारी साहित्य और लोक साहित्य—all मिलकर इस काल को साहित्यिक दृष्टि से अत्यधिक जीवंत और समृद्ध बनाते हैं।
भारत में मध्यकालीन साहित्य
भारत का साहित्यिक इतिहास अपनी गहराई और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से मध्यकालीन काल (7वीं से 18वीं शताब्दी) भारतीय साहित्य के विकास का अत्यंत महत्त्वपूर्ण युग रहा है। इस समय साहित्य केवल शास्त्रीय संस्कृत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, फ़ारसी और उर्दू जैसी भाषाओं में भी अभूतपूर्व साहित्यिक कृतियाँ सामने आईं। इस काल में साहित्य ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं को स्वर दिया, बल्कि समाज, राजनीति और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया।
मध्यकालीन साहित्य को प्रायः दो हिस्सों में बाँटा जाता है—
- प्रारंभिक मध्यकालीन साहित्य (7वीं से 14वीं शताब्दी)
- उत्तर मध्यकालीन साहित्य (14वीं से 18वीं शताब्दी)
प्रारंभिक काल में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जहाँ अलवर और नयनार संतों ने तमिल में भक्ति काव्य की रचना की। उत्तर मध्यकाल में यह आंदोलन उत्तर भारत तक पहुँचा और कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक, सूरदास और मीराबाई जैसे कवियों ने भक्ति साहित्य को व्यापक रूप दिया।
मध्यकालीन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें लोकभाषाओं का व्यापक प्रयोग हुआ। संस्कृत का स्थान धीरे-धीरे क्षेत्रीय भाषाओं ने लेना शुरू किया। इस दौरान—
- फ़ारसी साहित्य दिल्ली सल्तनत और मुगल दरबारों में फला-फूला। अमीर खुसरो, बदायुनी और मोहसिन फानी जैसे विद्वानों ने इसे समृद्ध किया।
- उर्दू साहित्य का जन्म हुआ और रेख़्ता शैली से लेकर मीर तकी मीर और ग़ालिब की ग़ज़लों तक इसका उत्कर्ष हुआ।
- हिंदी साहित्य ने भक्ति और लोक परंपरा को आवाज दी। तुलसीदास की रामचरितमानस, कबीर के दोहे और सूरदास के पद आज भी जीवंत हैं।
- क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, मराठी आदि) में अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ सामने आईं, जिन्होंने साहित्य को सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों से जोड़ा।
संक्षेप में, भारत का मध्यकालीन साहित्य विभिन्न भाषाओं और शैलियों का संगम है। यह केवल धार्मिक भावनाओं का प्रवाह नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार, लोकजीवन की संवेदनाएँ और सांस्कृतिक एकता का संदेश देने वाला साहित्य भी था। इसी कारण यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अमूल्य धरोहर माना जाता है।
आइए अब हम विभिन्न भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं के अंतर्गत इस काल के विकास को विस्तार से समझें।
फ़ारसी साहित्य का विकास
मध्यकालीन भारत में फ़ारसी भाषा का साहित्य अत्यधिक प्रभावशाली रहा। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के शासकों ने फ़ारसी को दरबारी भाषा का दर्जा दिया। इसके चलते फ़ारसी साहित्य ने भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक धारा पर गहरा असर डाला।
- दिल्ली सल्तनत का संरक्षण: सल्तनती शासक फ़ारसी साहित्य और विद्वानों को संरक्षण देते थे। इस काल में अनेक कवि और लेखक फ़ारसी में रचनाएँ करने लगे।
- अमासाई का ‘गरशस्पनामा’: यह महाकाव्य एक ईरानी मिथक पर आधारित था और दिल्ली सल्तनत में अत्यंत लोकप्रिय हुआ।
- अमीर खुसरो: अलाउद्दीन खिलजी के समय के महान कवि अमीर खुसरो ने फ़ारसी और हिंदी दोनों में साहित्य रचा। उन्होंने कव्वाली, मर्सिया और ग़ज़ल जैसी विधाओं को नया आयाम दिया। उनकी ‘खमसा’ और ‘क़िरान-उस-सादेन’ आज भी महत्वपूर्ण साहित्यिक धरोहर हैं।
- सादी की ‘बुस्तान’: 13वीं सदी में लिखी गई इस कृति का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह अत्यंत लोकप्रिय बनी।
- मीर ख्वांद की ‘रौज़ात उस-सफ़ा’ (1502): इसमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और उनके शासन का विवरण मिलता है।
- अब्द अल-कादिर बदायुनी की ‘मुंतखब-उत-तवारीख’: अकबर के समय की यह कृति इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है।
- मोहसिन फानी की ‘दबिस्तान-ए मजाहिब’ (17वीं शताब्दी): इसमें मुगल काल की धार्मिक परिस्थितियों का विवरण मिलता है।
फ़ारसी साहित्य की रचनाओं ने न केवल इतिहास और संस्कृति का अभिलेखन किया बल्कि उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को भी गहराई से प्रतिबिंबित किया।
उर्दू साहित्य का विकास
उर्दू भाषा का उद्भव मध्यकालीन भारत में हुआ। यह फ़ारसी, अरबी और भारतीय भाषाओं (विशेषकर हिंदी) के मिश्रण से बनी। इसे शुरू में रेख़्ता कहा जाता था और यह दिल्ली सल्तनत व मुगल दरबारों में तेजी से लोकप्रिय हुई।
- अमीर खुसरो: इन्हें रेख़्ता शायरी का जनक माना जाता है। उन्होंने हिंदी और फ़ारसी का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया।
- मोहम्मद शाह (1719–1748) का काल: इस समय उर्दू साहित्य अपने उत्कर्ष पर पहुँचा।
- प्रमुख कवि: सौदा, मीर तकी मीर, दबीर जैसे कवियों ने ग़ज़ल, मसनवी, मर्सिया और शहरी आशोब जैसी शैलियों में साहित्य रचा।
- मीर तकी मीर: उनकी ग़ज़लों में गहन संवेदनशीलता है। उन्हें “ग़ज़लों का देवता” कहा गया।
- मिर्ज़ा दबीर और सौदा: इनकी मसनवियाँ और मर्सिए उर्दू साहित्य की पहचान बने।
- मिर्ज़ा ग़ालिब: दिल्ली स्कूल के महान शायर ग़ालिब ने अपनी ग़ज़लों में गहरी दार्शनिकता और भावनात्मकता दिखाई।
- रसखान: उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा। उनकी कृति “पंड नहीं सुनिया” सामाजिक बुराइयों की आलोचना करती है।
उर्दू साहित्य ने भावनाओं, दर्शन और सामाजिक यथार्थ का अनूठा संगम प्रस्तुत किया और इसे भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा बना दिया।
हिंदी साहित्य का विकास
मध्यकालीन भारत में हिंदी साहित्य का स्वरूप मुख्यतः भक्ति साहित्य और रीतिकालीन काव्य के रूप में उभरता है। यह काल लोकभाषाओं में रचनाओं की प्रचुरता का गवाह रहा।
- विद्यापति (14वीं सदी): मैथिली कवि विद्यापति की प्रेम और भक्ति विषयक कविताएँ हिंदी साहित्य की प्राचीन कृतियों में मानी जाती हैं।
- ख़ुसरो और हसन देहलवी: इन्होंने अवधी और खड़ी बोली में भी रचनाएँ कीं।
- तुलसीदास (16वीं सदी): उनकी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई और यह हिंदी भक्ति साहित्य की आधारशिला मानी जाती है।
- रहीम और ग़ालिब: यद्यपि रहीम दरबारी कवि थे, परंतु उन्होंने ब्रजभाषा और हिंदी में भी काव्य रचा।
- रसखान: कृष्ण भक्त कवि, जिन्होंने ब्रजभाषा में अत्यंत लोकप्रिय काव्य रचा।
हिंदी साहित्य ने धर्म, प्रेम, भक्ति और सामाजिक आलोचना के साथ-साथ लोकजीवन को भी अभिव्यक्ति दी।
क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य
भारत में मध्यकालीन काल के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इन भाषाओं ने अपने-अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में साहित्य रचा।
तमिल साहित्य
- अलवर संत: 5वीं से 10वीं शताब्दी में रचित दिव्य प्रबंधम (4000 कविताएँ) भक्ति आंदोलन का केंद्र बनी।
कन्नड़ साहित्य
- वचन साहित्य: वीरशैव आंदोलन के बसवन्ना और अन्य वचनकारों ने सरल कन्नड़ में समतावादी ग्रंथ लिखे।
- ‘वड्डाराधने’ (1012 ई.): रन्ना की यह चंपू शैली की कृति कन्नड़ की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है।
तेलुगु साहित्य
- अल्लासानी पेद्दाना: 14वीं सदी में उनकी मनुचरितमु तेलुगु की पहली धर्मनिरपेक्ष रचना मानी जाती है।
बंगाली साहित्य
- चंडीदास (14वीं सदी): उनकी कविताएँ राधा–कृष्ण प्रेम और वैष्णव भक्ति आंदोलन से प्रेरित थीं।
मराठी साहित्य
- वारकरी संप्रदाय: ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम जैसे संत कवियों ने अभंग रचकर लोकभाषा में आध्यात्मिक विचार प्रस्तुत किए।
इन क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य ने भक्ति और लोक संस्कृति को आधार बनाकर भारतीय समाज को एकजुट किया और लोगों की भाषा में धार्मिक और सामाजिक संदेश पहुँचाया।
निष्कर्ष
भारत का मध्यकालीन साहित्य फ़ारसी, उर्दू, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। फ़ारसी ने दरबारी और ऐतिहासिक साहित्य को समृद्ध किया, उर्दू ने भावनात्मक और दार्शनिक ग़ज़लों को जन्म दिया, हिंदी ने भक्ति और लोकजीवन को स्वर दिया, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं ने स्थानीय संस्कृति और धार्मिक आंदोलनों को बल प्रदान किया।
यह काल भारतीय साहित्य का स्वर्णिम अध्याय है, जिसने न केवल भाषाओं के विकास को गति दी बल्कि भारतीय समाज को एक साझा सांस्कृतिक पहचान भी प्रदान की। आज भी मध्यकालीन साहित्य हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों और विविधता का बोध कराता है।
इन्हें भी देखें –
- हिंदी भाषा का अतीत और वर्तमान
- हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास
- हिंदी साहित्य का मध्यकाल : भक्ति और रीति धाराओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप
- हिंदी भाषा : स्वरूप, इतिहास, संवैधानिक स्थिति और वैश्विक महत्व
- भाषा एवं उसके विभिन्न रूप
- हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास
- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ
- समास – परिभाषा, भेद और उदहारण
- संधि – परिभाषा एवं उसके भेद (Joining)
- हिंदी वर्णमाला- स्वर और व्यंजन (Hindi Alphabet)
- विश्व एवं भारत के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान | Awards and Honors
- भारत की चट्टानें: संरचना, वर्गीकरण, विशेषताएं| Rocks of India