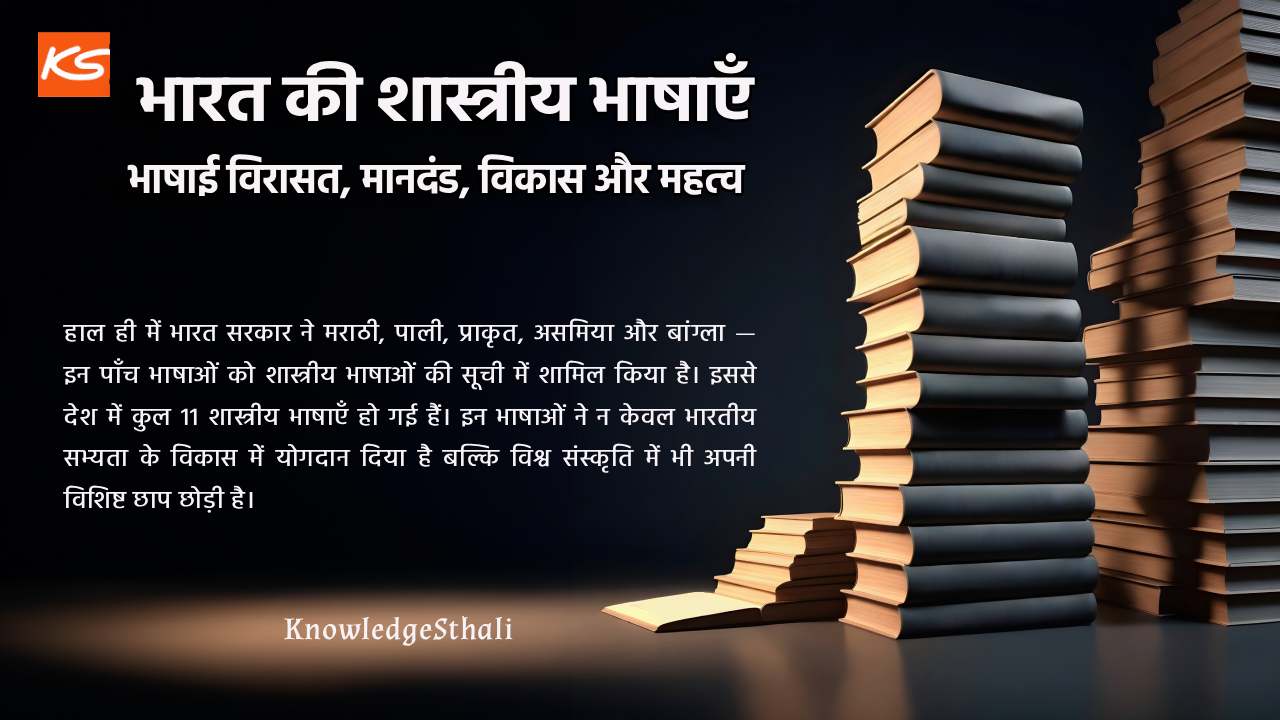भारत विविधताओं का देश है — यहाँ की संस्कृति, परंपराएँ, कला, साहित्य और भाषाएँ इस भूमि की आत्मा को परिभाषित करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप सदियों से भाषाई रूप से समृद्ध रहा है। प्रत्येक प्रदेश, जनजाति और समुदाय की अपनी विशिष्ट भाषा रही है जिसने भारत की सांस्कृतिक एकता में विविधता का रंग भरा है। इस भाषाई समृद्धि में कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिनकी प्राचीनता, साहित्यिक गहराई और सांस्कृतिक महत्ता इतनी व्यापक रही है कि उन्हें “शास्त्रीय भाषा” (Classical Language) का दर्जा दिया गया है।
हाल ही में भारत सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला — इन पाँच भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया है। इससे देश में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएँ हो गई हैं। इन भाषाओं ने न केवल भारतीय सभ्यता के विकास में योगदान दिया है बल्कि विश्व संस्कृति में भी अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है।
शास्त्रीय भाषा की परिभाषा
“शास्त्रीय भाषा” शब्द का तात्पर्य केवल किसी प्राचीन भाषा से नहीं है, बल्कि ऐसी भाषा से है जिसमें समय की कसौटी पर खरे उतरे हुए साहित्यिक, सांस्कृतिक और वैचारिक योगदान मौजूद हों। यह भाषा अपने भीतर किसी सभ्यता का इतिहास, दर्शन, धर्म और जीवन दर्शन समेटे होती है।
भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, किसी भाषा को शास्त्रीय का दर्जा तभी दिया जा सकता है जब उसमें प्राचीनता, मौलिक साहित्यिक परंपरा, और आधुनिक रूप से स्पष्ट भिन्नता जैसी विशेषताएँ मौजूद हों।
शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के मानदंड
भारत के संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) ने शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए कुछ ठोस मानदंड निर्धारित किए हैं। इन मानदंडों को 2024 में अद्यतन (revised) किया गया ताकि भाषाओं की प्राचीनता और साहित्यिक परंपरा का सटीक मूल्यांकन किया जा सके।
1. प्राचीनता (Antiquity):
भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों या लिखित प्रमाणों का इतिहास कम-से-कम 1,500 से 2,000 वर्ष पुराना होना चाहिए। अर्थात्, उस भाषा में उपलब्ध साहित्य या अभिलेख यह दर्शाएँ कि वह भाषा अत्यंत प्राचीन है और उस युग में भी उसका प्रयोग विद्वानों, समाज और शासन में प्रचलित था।
2. प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर:
भाषा में ऐसे प्राचीन साहित्य, ग्रंथ, महाकाव्य या शिलालेख मौजूद हों जिन्हें उसके वक्ताओं द्वारा महान सांस्कृतिक धरोहर (valuable heritage) माना गया हो। यह साहित्य केवल धार्मिक या दार्शनिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या कलात्मक भी हो सकता है।
3. मौलिक साहित्यिक परंपरा:
भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक (original) होनी चाहिए। अर्थात्, उस पर किसी अन्य भाषा की निर्भरता या अत्यधिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसकी साहित्यिक धारा स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हो।
4. आधुनिक रूपों से भिन्नता:
शास्त्रीय भाषा और उसके आधुनिक रूपों या उपभाषाओं में स्पष्ट भिन्नता होनी चाहिए। जैसे — संस्कृत और हिंदी में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। यह अंतर दर्शाता है कि भाषा समय के साथ विकसित तो हुई, परंतु उसके शास्त्रीय रूप का विशिष्ट अस्तित्व बना रहा।
5. ज्ञानग्रंथों की उपस्थिति:
भाषा में ज्ञान–विज्ञान, दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, कला और साहित्य से जुड़े ग्रंथों की उपलब्धता आवश्यक है। इसके साथ ही गद्य और पद्य दोनों रूपों में रचनाएँ होनी चाहिए तथा शिलालेखों या अभिलेखीय प्रमाणों का होना भी आवश्यक है।
इन सभी मानदंडों को पूरा करने पर किसी भाषा को “शास्त्रीय भाषा” घोषित किया जा सकता है।
भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची
भारत में अब तक कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इन भाषाओं में से छह भाषाएँ 2004 से 2024 के बीच घोषित की गई थीं, जबकि पाँच नई भाषाएँ 2024 में जोड़ी गईं।
पहले से मान्यता प्राप्त 6 शास्त्रीय भाषाएँ:
- तमिल – 2004
- संस्कृत – 2005
- कन्नड़ – 2008
- तेलुगु – 2008
- मलयालम – 2013
- ओड़िया – 2014
2024 में जोड़ी गई 5 नई शास्त्रीय भाषाएँ:
- मराठी
- पाली
- प्राकृत
- असमिया
- बांग्ला
इन सभी भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है, जिससे उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है।
प्रमुख शास्त्रीय भाषाओं का संक्षिप्त परिचय
(1) संस्कृत
संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और इसे “देववाणी” कहा जाता है। यह वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और विज्ञान की मूल भाषा रही है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता और अनेकों ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं।
(2) तमिल
तमिल भाषा की प्राचीनता लगभग 2,000 वर्ष पुरानी है। संगम साहित्य इसका स्वर्ण युग माना जाता है। यह द्रविड़ भाषाओं में सबसे पुरानी है और आज भी करोड़ों लोगों की मातृभाषा है।
(3) कन्नड़
कन्नड़ भाषा का शास्त्रीय साहित्य लगभग 1,500 वर्षों पुराना है। कवि पम्प, रण्ण, नागवर्मा जैसे विद्वानों ने इसे समृद्ध किया। इसमें धर्म, दर्शन, वीरगाथा और प्रेमकाव्य की समृद्ध परंपरा है।
(4) तेलुगु
तेलुगु को “इटैलियन ऑफ द ईस्ट” कहा गया है, इसकी ध्वनि और लय अत्यंत मधुर है। नन्नय, टिक्कना, एर्राप्रगडा जैसे कवियों ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद कर इसे गौरवशाली बनाया।
(5) मलयालम
मलयालम भाषा का उद्भव तमिल से हुआ लेकिन इसने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। यह केरल की प्रमुख भाषा है और इसके साहित्य में तोलकप्पियम, आर्यावैयम् जैसे ग्रंथ प्रमुख हैं।
(6) ओड़िया
ओड़िया भाषा का विकास प्राचीन उड़ीसा (कलिंग) में हुआ। इसमें सरला दास, जगतसिंह, उपेंद्र भंज जैसे कवियों ने शास्त्रीय काव्य परंपरा को समृद्ध किया।
(7) मराठी
मराठी की उत्पत्ति महराष्ट्र प्रदेश में प्राचीन अपभ्रंश रूपों से हुई। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव आदि ने इसे भक्तिकालीन साहित्य का केंद्र बनाया। मराठी में ज्ञानेश्वरी और तुकाराम गाथा जैसे ग्रंथ सांस्कृतिक धरोहर हैं।
(8) पाली
पाली भाषा मूलतः गौतम बुद्ध की उपदेश भाषा मानी जाती है। यह संस्कृत की प्राकृत रूपांतरित शाखा है जिसमें त्रिपिटक जैसे बौद्ध ग्रंथ रचे गए। पाली साहित्य दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया की बौद्ध परंपराओं का आधार है।
(9) प्राकृत
प्राकृत भाषाएँ मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का समूह हैं। इनका प्रयोग विशेष रूप से जैन धर्म के ग्रंथों में हुआ। आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
(10) असमिया
असमिया भाषा की जड़ें प्राचीन कामरूप क्षेत्र में हैं। इसमें चर्यापद, लोर गीत और शंकरदेव के ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। इसकी साहित्यिक परंपरा 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई।
(11) बांग्ला
बांग्ला भाषा भारत और बांग्लादेश दोनों में प्रमुख है। यह संस्कृत से विकसित हुई और 12वीं शताब्दी से इसका साहित्यिक इतिहास प्रारंभ होता है। काजी नजरुल इस्लाम, रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महान कवियों ने इसे विश्वस्तरीय पहचान दी।
शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का महत्व
शास्त्रीय भाषा का दर्जा केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि भाषाई संरक्षण, शैक्षणिक अनुसंधान, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा है।
1. शैक्षणिक सहायता (Academic Support):
सरकार इन भाषाओं के लिए विश्वविद्यालयों में विशेष अनुसंधान केंद्र (Research Centres) और अकादमिक चेयर्स (Academic Chairs) स्थापित करती है ताकि इन भाषाओं पर गहन अध्ययन और शोध हो सके।
2. पुरस्कार और सम्मान (Awards & Recognition):
संस्कृति मंत्रालय हर वर्ष दो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है — उन विद्वानों को जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट शोध या साहित्यिक योगदान किया हो।
3. वित्तीय सहायता (Funding):
शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण, प्रलेखन (documentation), और उनके प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण के लिए विशेष निधि (fund) उपलब्ध कराई जाती है।
4. सांस्कृतिक गौरव (Cultural Prestige):
जब किसी भाषा को शास्त्रीय का दर्जा मिलता है, तो उसके वक्ताओं में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न होती है। यह दर्जा भाषाई पहचान को सुदृढ़ करता है और युवाओं को अपनी मातृभाषा से जोड़ता है।
5. अंतरराष्ट्रीय पहचान (Global Recognition):
इन भाषाओं का अध्ययन और अनुवाद अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में बढ़ता है जिससे भारतीय भाषाएँ विश्व संस्कृति में अपना स्थान मजबूत करती हैं।
संविधान की आठवीं अनुसूची और भाषाई मान्यता
भारत का संविधान भाषाई विविधता को मान्यता देता है। आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में उन भाषाओं की सूची दी गई है जिन्हें भारत गणराज्य की राजकीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- संविधान का भाग XVII (Part XVII), अनुच्छेद 343 से 351 तक राजकीय भाषाओं से संबंधित है।
- वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं।
22 भाषाओं की सूची:
असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
ऐतिहासिक क्रम में सम्मिलन:
- प्रारंभ में — 14 भाषाएँ (1950 में)।
- सिंधी — 1967 में जोड़ी गई।
- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली — 1992 में जोड़ी गईं।
- बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली — 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गईं।
शास्त्रीय भाषाओं का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व
भारत की शास्त्रीय भाषाएँ केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और दर्शन का आधार हैं। इनके साहित्य में जीवन के हर पहलू — धर्म, समाज, राजनीति, कला, विज्ञान और नैतिकता — का गहन विश्लेषण मिलता है।
- संस्कृत ने वेदों, उपनिषदों और गीता के माध्यम से सार्वभौमिक ज्ञान दिया।
- तमिल और तेलुगु ने भक्ति और प्रेम के काव्य को जन-जन तक पहुँचाया।
- पाली और प्राकृत ने बौद्ध और जैन धर्म के उपदेशों को आम जनता तक पहुंचाया।
- मराठी और बांग्ला ने समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना को स्वर दिया।
इन भाषाओं ने भारतीय समाज को वैचारिक रूप से समृद्ध बनाया और एकता में विविधता के सिद्धांत को सशक्त किया।
निष्कर्ष
भारत की शास्त्रीय भाषाएँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा हैं। ये केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि सभ्यता का इतिहास, समाज की आत्मा और मानवता का दर्पण हैं। इन भाषाओं के अध्ययन और संरक्षण से न केवल हमारी जड़ों की पहचान बनी रहती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियाँ भी अपने अतीत से जुड़ी रहती हैं।
भारत सरकार द्वारा 2024 में पाँच नई भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा देना यह संदेश देता है कि भारत अपनी भाषाई परंपराओं के प्रति सजग और गर्वित है। यह निर्णय भाषाई समानता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय गौरव की दिशा में एक सशक्त कदम है।
इस प्रकार, भारत की शास्त्रीय भाषाएँ — संस्कृत से लेकर बांग्ला तक — भारतीयता की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं।
इनका संरक्षण और प्रसार ही भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का वास्तविक आधार है।
इन्हें भी देखें –
- नेपाली भाषा : उत्पत्ति, विकास, लिपि, वर्णमाला, दिवस और साहित्य
- संस्कृत भाषा : इतिहास, उत्पत्ति, विकास, व्याकरण, लिपि और महत्व
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): आदिवासी शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की ऐतिहासिक पहल
- एटॉमिक स्टेंसिलिंग : परमाणु स्तर पर नैनो प्रौद्योगिकी की नई क्रांति
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) और जन्म–मृत्यु पंजीकरण प्रणाली
- एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) और भारत की नेतृत्वकारी भूमिका
- भारत 2025 में वैश्विक एआई युद्धक्षेत्र के रूप में उभरेगा
- एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक और भारत की पनडुब्बी शक्ति: प्रोजेक्ट 75 इंडिया
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (National Youth Award)
- UPS से NPS तक : पेंशन प्रणाली में बदलाव की नई दिशा
- कित्तूर की वीरांगना रानी चेन्नम्मा : भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी